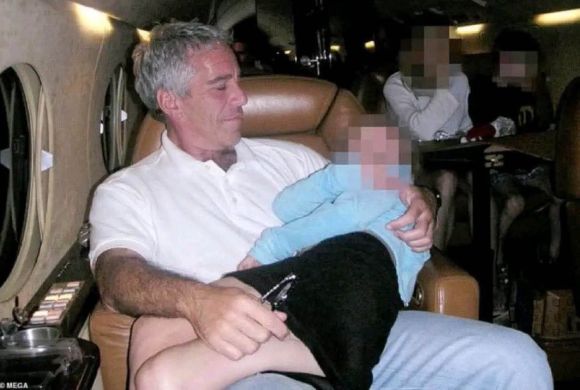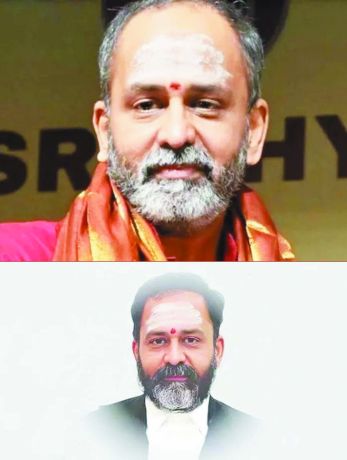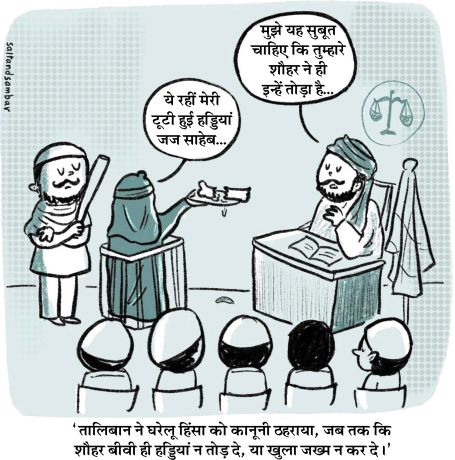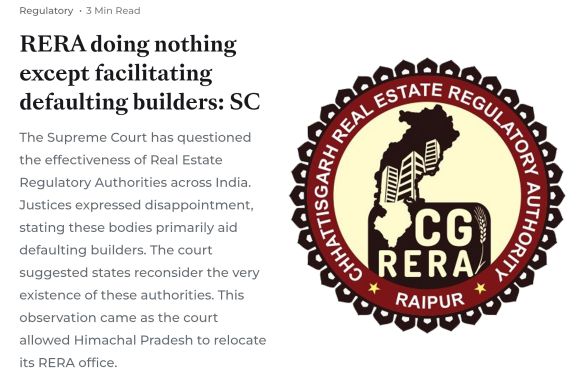संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट को लेकर केन्द्र सरकार का रूख एक पहेली की तरह बना हुआ है। पिछले कई महीनों से केन्द्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू तरह-तरह के कार्यक्रमों में या मीडिया से बात करते हुए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं, वह एक सिलसिले के रूप में देखने पर कोई मासूम हरकत नहीं लगती है। इसके पीछे कोई सोची-समझी बात है, और अदालत से केन्द्र सरकार का सतह के नीचे चलता कोई टकराव दिख रहा है। उन्होंने जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई कॉलेजियम प्रणाली की कड़ी आलोचना की, फिर कुछ और मामलों में अदालत के बारे में तरह-तरह की असहमति जताई। अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह नसीहत दी कि उसे जमानत के मामलों को, और जनहित याचिकाओं को नहीं सुनना चाहिए क्योंकि उनमें बहुत वक्त लगता है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों की लंबी छुट्टियों के बारे में कहा इससे वहां चल रहे मुकदमों के लोगों को बड़ी असुविधा होती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ तुर्की-ब-तुर्की जवाब भी दे रहे हैं।
इससे कम से कम एक यह बात तो समझ में आती है कि केन्द्र सरकार चन्द्रचूड़ के साथ उतनी सहूलियत महसूस नहीं कर रही है जितनी वह पिछले मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित के साथ महसूस करती थी। जजों की अपनी निजी राय रहती है, और सरकारें यह अंदाज लगा लेती हैं कि उसकी दिलचस्पी के मामलों में किस जज का क्या रूख रहेगा। इसी को देखते हुए केन्द्र सरकार कॉलेजियम के भेजे हुए नामों को मंजूरी देने के पहले उन्हें महीनों या बरसों तक टांगकर रखती है ताकि जिन जजों या वकीलों के नाम भेजे गए हैं, उनकी सोच अगर सरकार को माकूल नहीं लगती है, तो उन्हें मंजूरी न दी जाए। नतीजा यह होता है कि ऐसी लिस्ट में से कई वकील थककर अपने नाम वापिस ले लेते हैं क्योंकि उन्हें यह समझ आ जाता है कि वे एक तारीख के बाद जज बनने पर कभी चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे। अभी हाल में ही ऐसे कई लोगों ने अपने नाम वापिस ले लिए हैं। जजों की खाली पड़ी हुई कुर्सियों और सरकार के पास कॉलेजियम की भेजी गई फेहरिस्त का जब साथ-साथ साल-दो-साल इंतजार चलता है तो जाहिर है कि अदालत में मामलों का ढेर बढ़ते चलेगा। लेकिन मौजूदा सरकार को नामों की ऐसी लिस्ट को एक-दो बरस तक भी रोकने से कोई परहेज नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सार्वजनिक कार्यक्रम में भी इस बात को उठा चुके हैं, और अब तो ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट भी जनता के बीच अपनी स्थिति को रख देना चाहता है कि सरकार की किन बातों से उसके काम पर असर पड़ रहा है। फिर यह भी लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के तीन स्तंभों में से दो, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अधिकारों को लेकर भी एक खींचतान चल रही है। यह नौबत तब और गंभीर हो जाती है जब लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ, विधायिका, अपने भीतर सत्तारूढ़ पार्टी के असीमित बाहुबल के चलते भारतीय लोकतंत्र को अब दो स्तंभों का ही बना चुका है। अब देश में सरकार और अदालत इन्हीं दो का मतलब रह गया है क्योंकि संसद में न तो कोई विपक्ष कोई ताकत रखता, और न ही सरकार को उसकी कोई परवाह ही है। ऐसी हालत में सरकार अपने संसदीय बाहुबल के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट से दो-दो हाथ करने को उतावली दिख रही है। लेकिन आज के मुख्य न्यायाधीश सरकार के इस रूख के सामने झुकते हुए भी नहीं दिख रहे हैं।
दरअसल भारतीय संविधान जब बना, उस वक्त शायद देश में ऐसी संसदीय स्थिति की कल्पना नहीं रही होगी कि संसद में लगातार एक ही पार्टी का इतना बड़ा बहुमत जारी रहेगा, जो कि देश की तकरीबन तमाम विधानसभाओं तक भी फैला हुआ रहेगा। ऐसा बाहुबल सत्तारूढ़ पार्टी की सोच को संविधान संशोधन में बदलने की ताकत रखता है, और इसीलिए आज हिन्दुस्तान कई किस्म के नए कानूनों को देख रहा है, केन्द्र-राज्य संबंधों में नई तनातनी झेल रहा है, और अब केन्द्र में सत्तारूढ़ ताकतों को शायद यह लग रहा है कि ऐसे अभूतपूर्व जन-बहुमत के रहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट अगर एक प्रतिबद्ध-न्यायपालिका के रूप में काम नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? लोगों को याद होगा कि प्रतिबद्ध-न्यायपालिका शब्द का पिछला या पहला इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान हुआ था जब तानाशाह हो चुकी इंदिरा सरकार और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका से यह उम्मीद कर रही थी कि उसे सरकार के नजरिए से प्रतिबद्ध होकर चलना चाहिए। आज केन्द्रीय कानून मंत्री के लगातार बयानों से अगर सीधे-सीधे यह मतलब नहीं भी निकल रहा है, तो भी इससे सीधे-सीधे उसी दौर की याद आ रही है।
हम केन्द्र और सुप्रीम कोर्ट में किसी टकराव की चाहत के बिना यह उम्मीद जरूर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ देश के संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखे, और अगर उसके शब्दों के बीच व्याख्या की गुंजाइश है, तो जजों को अपने सरोकार सरकार के साथ नहीं, जनता के साथ जोडऩे चाहिए। लोकतंत्र में जैसे-जैसे सरकार मजबूत होती है, संसद एकतरफा होती है, वैसे-वैसे सुप्रीम कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी को अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत भी होती है। आज का यह दौर देश की सरकार के साथ-साथ देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर एक विचारधारा की ताकतों के एकाधिकार की कोशिश का दौर दिख रहा है। केन्द्र सरकार इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुई है, और मोदी सरकार के इन आठ बरसों में तकरीबन तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर लगभग-प्रतिबद्धता की नौबत आ चुकी है। यह वक्त एक बहुत जिम्मेदार और मजबूत रीढ़ वाले सुप्रीम कोर्ट की जरूरत का है, और चूंकि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल पर्याप्त बाकी है, इसलिए इतिहास इस दौर को गौर से दर्ज करेगा।