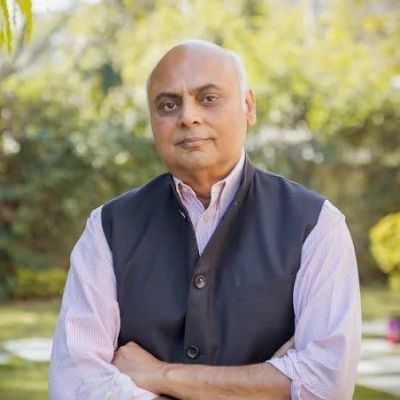विचार / लेख

बहुत दिनों गर्मी पडऩे के बाद जब बरसात की पहली फुहार आती है। उससे किसान के खेत या बागीचे तो नहीं लहलहाते। लेकिन लहलहाने वाली फसल की उम्मीद जगने लगती है। वर्षों से निढाल, अनुकूल और सहमते हुए सत्तासमर्थक लगते सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग संबंधी एक फैसला देकर उम्मीदों की बौछार तो की है। मौसम के बदलने का इशारा भी उसमें छिपा हो सकता है। भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग में रूढ़ अवधारणा पैठ गई है कि संविधान तो सिर माथे लगाने लायक है। उसे लेकर कोई विपरीत बहस, निंदा, आलोचना या पुर्नमूल्यांकन की बात भी नहीं करनी चाहिए। इसके बरक्स कुछ लोग संविधान को कुचल, बदल और खारिज कर ‘एक निशान, एक विधान, एक प्रधान’ जैसा गैरलोकतंत्रीय नारा लगाते हिन्दू राष्ट्र बनाने का ऐलान संविधान में दर्ज कर देना चाहते हैं। संविधान बनने के 70 वर्ष से ज्यादा हो जाने पर भी उसके विकल्प, विश्वसनीयता और भविष्यमूलकता को लेकर वक्त ने संदेह करने का मौका नहीं दिया। फिर भी लगातार परिवर्तन और पुनरीक्षण संविधान के लिए वे बौद्धिक चुनौतियां हैं, जिनका तार्किक उत्तर देना लोकतांत्रिक समझ के लिए बेहद जरूरी है। इस नजरिए से देखने पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला संविधान के गर्भगृह में पैदा हुई लेकिन अनदेखी कर दी गई उन घटनाओं और परिस्थितियों को उकेरना चाहेगा कि कहीं कोई चूक पहले ही हो गई है। उसके कारण भारतीय लोकतंत्र को केन्द्र सरकार की दादागिरी या बपौती का लगातार सामना करना पड़ता रहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसी तरह सभी बुनियादी संवैधानिक मसलों को ऐसे ही लेकर अपनी संभावित भूमिका को कारगर ढंग से समझता रहे। तो भारतीय संविधान की पोथी को केवल बांचने के अलावा उसके प्रति श्रद्धा कायम रहनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने 378 पृष्ठ के अपने लंबे फैसले में मामले से जुड़े सभी पक्षों, इतिहास, संभावनाओं और सरकारी कारनामों वगैरह पर विचार किया है। इसके बावजूद जाहिर कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने उन कई बातों का स्पर्ष नहीं किया जिन्हें लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे के सिलसिले में आजाद खयाल नागरिकों द्वारा विचार करना जरूरी है। यह आमफहम है कि संविधान निर्माता महान देषभक्त थे और जो कुछ उन्होंने कहा रचा, उस पर बहस मुबाहिसा करने के बाद उसे विवेक के माथे पर लीप लेना चाहिए। यह समझाइष ही वह रहस्यलोक है जहां सच की हिफाजत करना पुरखों की इज्जत करने से ज्यादा महत्वपूर्ण और आवष्यक संवैधानिक आचरण है। स्वतंत्र चुनाव आयोग की परिकल्पना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। यह दुनिया के सभी लोकतंत्रों में है। भारत की संविधान सभा में 15 और 16 जून 1949 को इस विषय पर जीवंत बहस हुई। दिलचस्प है कि संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर बहस के वक्त सबसे बड़ेे नेता जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, मौलाना आजाद आदि की गैरहाजिरी या चुप्पी के कारण भी कई अपूर्णताएं बल्कि गलतफहमियां रह गईं। उनके कारण भविष्य में सुप्रीम कोर्ट तक में पेचीदी स्थितियां पैदा होती रहीं। संविधान बनाने के लिए गठित मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक अधिकारों आदि की कुछ उपसमितियों में नागरिकों को वोट डालने की आजादी मूल अधिकार के रूप में देने की पेशकश हुई। बाद में उसके सामने आने पर संविधान सभा ने इसे बहुत महत्वपूर्ण समझते हुए तय किया कि मूल अधिकारों की फेहरिश्त में चुनाव में भाग लेने के अधिकार का उल्लेख भर कर देने से बात बनेगी नहीं। इसलिए पूरे चुनाव प्रबंधन को एक नए परिच्छेद में अलग से लिखकर उसका खुलासा किया जाए।
यही वजह है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. अंबेडकर ने पहले के प्रस्तावित प्रावधानों को अंतिम बहस के ठीक पहले बदल दिया। इस बदलाव के कारण लोकतंत्र की जवाबदेही की प्रतिनिधि भावना को राज्यों की सूची से हटाकर केन्द्र सरकार के जिम्मे कर दिया गया। संविधान सभा में षिब्बनलाल सक्सेना, हरिविष्णु पाटस्कर, हृदयनाथ कुंजरू और कुलाधर चालिहा आदि ने प्रस्तावित प्रावधान का कड़ा विरोध किया था। इन पुरखों के साथ ऐसा भी था कि वे कई बार बौद्धिक बहस करने के बदले अपने परस्पर कटाक्षों के लिए समय और नीयत निकाल लेते थे। कई बार डा. अंबेडकर अनावश्यक रूप से तल्ख होकर सदस्यों पर टिप्पणियां कर देते थे। ऐसे सदस्य भी पलटकर जवाबी हमला करने में कोताही नहीं करते थे। शिब्बनलाल सक्सेना ने बुनियादी बात यही कही कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यसभा और लोकसभा दोनों के दो तिहाई के बहुमत से ही होनी चाहिए। इससे सत्ताधारी पार्टी अपनी दादागिरी नहीं कर सकेगी। कुछ अन्य पार्टियों को भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। इससे पारदर्षिता आएगी। सक्सेना ने यह जोर देकर कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केवल केन्द्र सरकार या प्रधानमंत्री की सिफारिशपर राष्ट्रपति द्वारा किए जाने पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनकी नियुक्ति से लेकर अन्य सभी आनुशंगिक विषयों के लिए संसद में अधिनियम पारित कराना जरूरी होगा। अपने लंबे भाषण में हरिविष्णु पाटस्कर ने कहा कि डा. अंबेडकर ने यक ब यक सारे अधिकार राष्ट्रपति के नाम से केन्द्र सरकार अर्थात प्रधानमंत्री को दे दिए हैं जबकि मूल प्रस्तावना उपसमितियों में यही थी कि प्रदेषों के लिए प्रादेषिक चुनाव आयोग वहां के राज्यपालों के नाम से गठित किए जाएंगे। इससे संवैधानिक मर्यादाओं का विकेन्द्रीकरण होना जरूरी होगा। केन्द्र को एकाधिकार देते समय सक्सेना ने टोका था कि आज जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं। वे एक आदर्ष डेमोक्रेट हैं। वे अपनी पसंद का चुनाव आयुक्त बहुमत के दम पर नहीं थोपेंगे। आगे कभी ऐसा प्रधानमंत्री आ सकता है जो अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए चुनाव आयोग को बंधुआ मजदूर बना ले और अपनी सियासी सेवाटहल कराने की उम्मीद में हुक्मबजाऊ चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करे। प्रदेशों की पहले प्रस्तावित स्वायत्तता को छीनने का कड़ा विरोध कुलाधर चालिहा ने भी किया। उनका कहना हुआ कि दिल्ली या भारत के अन्य किसी कोने में बैठकर अपना हुक्म चलाने वाले चुनाव आयोग से प्रदेशों के हित की कैसे उम्मीद की जा सकती है? उन्होंने नाम लेकर कहा कि गोविन्दवल्लभ पंत, एन बी खेर और रविशंकर शुक्ल जैसे मुख्यमंत्रियोंं के रहते प्रदेशों के नेतृत्व पर भरेासा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने इस बात पर भी ऐतराज किया कि मुख्य चुनाव आयोग को तो सुरक्षा है कि वह सुप्रीम कोर्ट जज की तरह महाभियोग लाए जाने पर ही सेवा से पृथक किया जा सकता है। बाकी चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्तों के परामर्श ये हटाया जा सकता है। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को सेवा से अलग नहीं कर सकते। द्विसदस्यीय या बहुसदस्यीय बेंच में बैठने पर हर एक जज की राय का बराबर मत होता है। डॉ. अंबेडकर, के. एम. मुंशी, आर. के. सिधवा, नजीरुद्दीन अहमद जैसे सदस्यों की अपनी समझ की जिद के कारण बाकी चुनाव आयुक्तों की वह हालत कर दी गई जैसी मंत्रिपरिषद में बाकी मंत्रियों की होती है। उन्हें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने विवेक से हटा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त होता है और वैसा ही बाकी अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर होता है। तो फिर उनकी अनिश्चित सेवा शर्तें किस तरह संवैधानिक होंगी? यही सवाल हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग संबंधी अपने फैसले में भी दुहराया है।
संविधान सभा में कश्मीर जैसा बहुत महत्वपूर्ण मसला जेरे बहस आया। तब सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे जिम्मेदार लोग हाजिर नहीं थे। श्यामाप्रसाद मुखर्जी को बाद में उनकी मृत्यु के कारण षेरे कष्मीर और षहीद वगैरह के संबोधन ढूंढे गए। कश्मीर की बहस में उन्होंने हाजिरी देकर उस वक्त क्यों कुछ नहीं कहा। जवाब संविधान सभा की फाइलों में दर्ज नहीं है। केन्द्र सरकार, प्रधानमंत्री और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त आदि के एकतरफा एकाधिकार की संभावित पक्षधरता के खिलाफ कुछ संविधान पुरखों ने अपनी सयानी समझ का पोचारा फेरा। उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ भी नहीं कहा। भारत पाक विभाजन की खतरनाक घटना के कारण संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने संविधान को ही केन्द्राभिमुखी बना दिया। उन्हें भय रहा था कि मजबूत केन्द्र के बिना खंडित भारत की अखंडता कैसे बचेगी। नागरिकों के संवैधानिक अधिकार और लोकतंत्र का उद्भव और विकास राजनीतिक दुर्घटनाओं पर निर्भर हो जाएं। तो संविधान की आत्मा की हेठी होती है। तुर्रा यह कि यदि भारत पाक विभाजन हुआ भी तो उसकी अगुवाई की जिम्मेदारी तो केन्द्रीय नेताओं की ही रही है। भारत के प्रदेषों का नेतृत्व इस सिलसिले में हाषिए पर ही रहा है। तब भी प्रदेशों का अधिकार छीनकर केन्द्र को दे दिया गया। इसीलिए पाटस्कर ने याद दिलाया कि अपने पहले प्रस्तावित भाषण में संविधान की रूपरेखा समझाते हुए 4 नवंबर 1948 को अंबेडकर ने कहा ही था कि भारत प्रदेशों का एक फेडरेशन बनेगा। बाद में लगातार अलग अलग विषयों पर विधायन करते हुए राज्यों के अधिकार कम किए जाते रहे और एक मजबूत केन्द्र की अवधारणा के नाम पर लगभग अत्याचारी केन्द्र की हैसियत बना दी गई।
मौजूदा वक्त में मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति संविधान की पीठ पर छुरा भोंकने का वीभत्स उदाहरण है। पंजाब के आईएएस काडर के इस अधिकारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन किया। वे अपने कारणों से नौकरी करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने लगभग उसी दिन मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की अर्जी लगा दी और उनका इस्तीफा भी आनन-फानन में मंजूर हो गया। एक अनिच्छुक नौकरशाह काफी बड़े पद पर इच्छुक मुख्य चुनाव आयुक्त बन गया। संविधान कहता है कि इन्हें बनाया तो प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री और अरुण गोयल की साठगांठ का यह उदारण नहीं तो क्या है? ऐसे में अगले 6 वर्षों तक मुख्य चुनाव आयुक्त की हैसियत में एक पक्षपाती और आत्ममुग्ध व्यक्ति से संविधान और लोकतंत्र क्या उम्मीद करेंगे? प्रधानमंत्री की चुप्पी तो किसी रहस्य महल या भुतहा महल की कहानियों जैसी अवाम विरोधी कथा ही तो कहलाएगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तभी लागू होगा जब मौजूदा चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल खत्म हो जाए। ऐसा भी क्यों हो? जब नियुक्ति करने वाले अधिकारी अर्थात प्रधानमंत्री का विवेक ही प्रदूषित सिद्ध हो जाए। तो उसके उत्पाद अपनी कुर्सियों पर क्यों बैठे रहें। अन्यथा कुछ वर्षों का समय बीत जाने पर केन्द्र सरकार बहुमत की ताकत के कारण कोई न कोई जुगत बिठाना चाहेगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का यह बहुचर्चित फैसला ठंडा पड़ जाए। संविधान सभा में कई मौकों पर सबसे बड़ेे नेताओं की चुप्पी संविधान के लोकयष के लिए मतिभ्रम पैदा करती रही है। आदिवासी अधिकारों को लेकर भी डॉ. अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बहस के दिन ही पूरा ड्रॉफ्ट बदल दिया और आदिवासी अधिकारों में बेतरह कटौती हो गई। तब भी सबसे बड़ेे नेता जवाहलाल नेहरू आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े सेनापति भी थे। वे मौन रहे। ऐसे और भी उदाहरण हैं। इसलिए भारतीय लोकतंत्र की मौजूदा पीढ़ी भक्तिभाव में अभिभूत होकर वैज्ञानिक सच को नहीं समझ पाएगी। लोकतंत्र की बुनियाद नेता, सरकार या राष्ट्रपति और उनके द्वारा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारी नहीं हैं। हम भारत के लोग अर्थात नागरिक बुनियाद का पत्थर हैं। हम पर लोकतंत्र के भवन की मजबूती निर्भर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक कहा जाता है। भले ही वह परिणाम ऐतिहासिक नहीं भी हो। वह चुनाव सुधारों के लिए एक कोशिश के रूप में जरूर दर्ज होगा। पहले चुनाव आयुक्त रहे टी. एन. शेषन और बाद में डॉ. एम. एस. गिल ने कई सुझाव दिए थे। वे सुप्रीम कोर्ट तक गए थे लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने भी टालमटोल किया। वरना तब ही ऐसे सवाल हल किए जा सकते थे। विख्यात संविधानविद जस्टिस वी. आर. कृष्ण अय्यर ने तो इस संबंध में काफी लिखा है। अन्य कई विचारकों का भी इसमें योगदान है। यह तो पिछले 70 वर्षों में एक के बाद एक प्रधानमंत्रियों ने इस मुद्दे की अनदेखी की। वे चाहे जैसे रहे हों लेकिन नरेन्द्र मोदी नाम के प्रधानमंत्री ने संविधान की एक-एक आयत का कचूमर निकालने में अपने अनोखे अभियान का परिचय दिया है। यदि वह कायम रहा तो आगे पूरे संविधान का क्या होगा? उसकी भयावहता केवल उनको हो सकती है जो संविधान का तटस्थ और वस्तुपरक मूल्यांकन करने में भरोसा करते हैं।



.jpg)
.jpg)