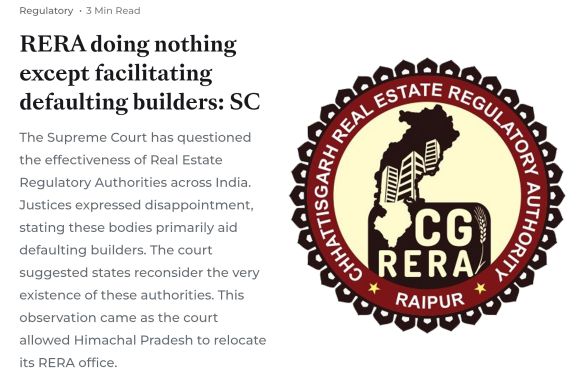संपादकीय

हर दिन आसपास अनगिनत घटनाएं दिल दहला रही हैं। उन्हें खबरों में छापना भी आसान नहीं है, और उन पर यहां लिखने का भी दिल नहीं कर रहा है। आज अपने आसपास के शहर-कस्बों की खबरें हैं कि टोनही के शक में पड़ोसी की जान ले ली। दूसरी खबर है एक आदमी ने अपने ही पांच बरस के बेटे की दोनों आंखें चाकू से फोड़ दीं, परिवार ने बताया कि किसी ने उसे फोन पर ऐसा करने कहा और उसने तुरंत कर दिया। एक अलग खबर है कि एक महिला की संपत्ति हथियाने के लिए उसके बेटे-बहू ने उसका कत्ल कर दिया। एक अलग खबर है कि खाना न बनाने पर एक पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी मारकर मार डाला। दो दिन पहले एक खबर आई थी कि बीवी से दारू के लिए पैसा नहीं मिला तो इसी इलाके में एक आदमी ने अपने डेढ़ बरस के बेटे को मारकर पेड़ पर टांग दिया। ये खबरें मेहनत से बनाई गई लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक नजर में दिखी खबरें हैं। इन सबमें एक बात एक सरीखी है कि ये सब परिवार के भीतर की हिंसा हैं, या अधिक से अधिक पड़ोस की। हर दिन परिवार के भीतर एक या अधिक बलात्कार की खबरें आती हैं, और रिश्तेदारों के साथ-साथ बाप भी अपनी बेटी से बलात्कार करते पकड़ा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन सब मामलों की पुलिस में रिपोर्ट अब अधिक हो रही है, ऐसे मामले हो ही अधिक रहे हैं। इन पर कोई चर्चा भी इसलिए नहीं होगी कि पुलिस रिपोर्ट के बाद गिरफ्तारी हो जाती है, और अदालतों में बरसों तक मुकदमे चलते रहते हैं। लेकिन क्या पुलिस और कोर्ट ही ऐसे मामलों के लिए काफी कार्रवाई है?
किसी भी जनकल्याणकारी सरकार को अपने देश-प्रदेश में लोगों के बीच पनपती हिंसक भावनाओं का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे तनाव की बहुत सी वजहें हो सकती हैं जिनके बढ़ते-बढ़ते लोग मरने-मारने पर उतारू हो जाएं। घर के भीतर जब इस दर्जे की हिंसा होने लगती है तो सोचना चाहिए कि लोगों के दिल-दिमाग पर कौन-कौन से तनाव हैं? गरीब तबके में गरीबी सबसे बड़ा तनाव रहती है, और वह सौ किस्म के गलत काम करवाती है। जब जिंदा रहने, खाने, और इलाज करवाने में ही लोगों का दम टूटने लगता है, तो शायद उनकी जिंदगी के नीति-सिद्धांत भी टूटने लगते हैं। भूखे के लिए रोटी से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं होता। लोगों को जिंदगी से ऐसी निराशा भी होने लगती है कि वे कोई जुर्म करके बाकी पूरी जिंदगी जेल में गुजारने का खतरा उठाने से भी नहीं हिचकते। ऐसा तब और अधिक होने लगता है जब जेल के बाहर की जिंदगी की तकलीफें इतनी बढ़ जाती हैं, कि लोगों को लग सकता है कि जेल के भीतर इससे और बुरा क्या होगा? जब हालात ऐसे हो जाएं तो खयालात भी वैसे ही होने लगते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, नौकरी न मिलने या चली जाने की तकलीफ, अपनी मर्जी से प्रेम न कर पाने की कुंठा, हिन्दुस्तानी समाज के बड़े हिस्से में ये तमाम तनाव आम हैं।
समाज में जब लोग लूट-डकैती के बिना, बिना किसी फायदे के, जब परिवार के भीतर जान लेने लगते हैं, तो यह समझ पड़ता है कि उनकी निजी निराशा पारिवारिक ढांचे से मिलने वाली ताकत से भी कम नहीं हो पा रही है। लोग आमतौर पर परिवार के लिए बहुत से सही-गलत काम करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब परिवार का ढांचा भी उनमें कोई उम्मीद नहीं जगा पाता, जब परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उनको तोड़ देता है, तो वैसे में कौन सी एक चिंगारी उनके भीतर की अहिंसा को हिंसा में तब्दील कर देती है, यह समझना आसान नहीं है। किसी भी अच्छी सरकार को यह चाहिए कि वह समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों की ऐसी एक कमेटी रखे जो कि पारिवारिक हिंसा के ऐसे मामलों की जानकारी जुटाकर यह समझने की कोशिश करे कि कौन सी वजहें लोगों की हिंसा से हिचक खत्म कर देती हैं, और वे पूरी जिंदगी जेल में गुजारने की कीमत पर भी हत्या, बलात्कार जैसे जुर्म घर के भीतर अपनों पर ही करने लगते हैं। पुलिस अपनी जांच के दौरान इन पहलुओं पर गौर नहीं कर सकती क्योंकि वह जुर्म के कानूनी और अदालती पहलुओं को ही देखते हुए थकी रहती है। इसके लिए पुलिस और वकीलों से परे अध्ययन और शोध में दिलचस्पी रखने वाले जानकार लोग चाहिए। सरकार चाहे तो ऐसी रिसर्च के लिए कुछ फैलोशिप भी दे सकती है, और संबंधित विषयों के शोधकर्ता ऐसे मामलों की जानकारी जुटाकर उनके दस्तावेजीकरण का काम कर सकते हैं, ताकि समाज को तनाव से निकालने के लिए उस तनाव की शिनाख्त तो हो सके, उसके पीछे की वजहें देखी जा सकें।
जिन छोटे कस्बों और गांवों से ऐसे जुर्म की खबरें आ रही हैं, उनसे साफ है कि यह शहरीकरण के असर में होने वाले जुर्म नहीं हैं। यह जरूर हो सकता है कि गांव-कस्बों में भी अब परिवार टूट रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था कमजोर हो रही है, और लोगों पर आसपास का दबाव भी कम हो रहा है। ऐसे में किसी के भीतर हिंसक इरादों का विस्फोट होने के पहले उसका अंदाज लगाकर कोई उसे रोक सके, इसकी गुंजाइश कम दिख रही है। आसपास के उठने-बैठने वाले लोग जरूर हिंसक सोच को समय रहते रोकने की संभावना रखते हैं, लेकिन लोग इन दिनों शायद रूबरू रिश्तों के मुकाबले ऑनलाईन रिश्तों में अधिक उलझे रहते हैं, और उसका एक नतीजा यह भी हो सकता है कि वे आसपास के लोगों के तनाव से या तो नावाकिफ हों, या उसकी तरफ से फिक्रमंद न हों।
जो भी है सरकारों को सामाजिक सोच की समस्याओं की पहचान भी करनी चाहिए। यह काम वोट दिलाने जैसा लुभावना काम नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सरकार चुनावी मोड से परे काम करने की सोच रखती हो, तो वह जरूर इस बारे में सोचेगी।