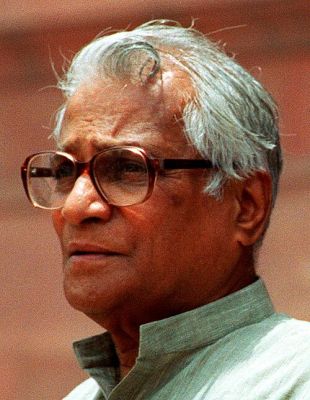विचार / लेख
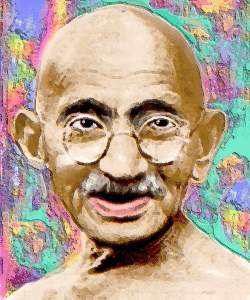
-मयूरेश कोण्णूर
मध्य प्रदेश की एक जनसभा में गुरुवार को सनातन धर्म के विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के बारे में कहा कि, ‘जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया।’
प्रधानमंत्री मोदी का ये दावा करना कि सनातन धर्म ने महात्मा गांधी को छुआछूत प्रथा के खिलाफ लडऩे की प्रेरणा दी, सनातन को लेकर उस तर्क के ठीक उलट है, जो डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने दिया था।
सनातन धर्म के विवाद को गांधी से जोडक़र प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को सियासी तौर पर और धारदार बना दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सनातन धर्म ने जाति के पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दिया था? या फिर, सनातन धर्म ने सामाजिक सुधारों की प्रेरणा दी थी?
हाल ही में आई किताब ‘कास्ट प्राइड : बैटल्स फ़ॉर इक्वॉलिटी इन हिंदू इंडिया’ के लेखक, मनोज मिट्टा कहते हैं कि वैसे तो महात्मा गांधी ने ‘रूढि़वादिता से मुकाबला करने के लिए खुद को सोच समझकर एक सनातनी के तौर पर पेश किया था।’ लेकिन, इस दावे पर सवाल जरूर उठ सकते हैं कि छुआछूत के खिलाफ मुहिम चलाने की प्रेरणा उनको सनातन धर्म से मिली थी।
मनोज मिट्टा बताते हैं कि 1920 में जब कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में अस्पृश्यता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, तो इसमें महात्मा गांधी की बड़ी भूमिका रही थी।
‘गांधी ने समाज के एक तबक़े को अछूत बनाने के पीछे पुरातन पंथियों को कठघरे में खड़ा किया था।’
छुआछूत के खिलाफ कांग्रेस का वो ऐतिहासिक प्रस्ताव इन शब्दों के साथ शुरू हुआ था कि, ‘हिंदू समाज की अगुवाई करने वालों से अपील है कि ‘वो हिंदू धर्म को अछूत प्रथा से निजात दिलाने के लिए विशेष तौर से प्रयास करें।’
उस समय प्रचलित जातिगत भेदभाव की भयावह तस्वीर पेश करते हुए, वो प्रस्ताव इन शब्दों के साथ खत्म हुआ था कि कांग्रेस, ‘पूरे सम्मान के साथ धार्मिक गुरुओं से अपील करती है कि वो समाज के दबे कुचले वर्गों के साथ होने वाले बर्ताव में सुधार की बढ़ती ख्वाहिश को पूरा करने में मदद करें।’
भले ही अस्पृश्यता को लेकर महात्मा गांधी की सोच बिल्कुल साफ रही हो। लेकिन, मनोज मिट्टा सुबूतों के साथ बताते हैं कि गांधी अपने सियासी करियर के एक बड़े हिस्से तक जाति व्यवस्था के मूल यानी वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते रहे थे।
गांधी ने 1924-25 के वायकोम विद्रोह को सिर्फ इसलिए समर्थन दिया था कि उसमें अछूतों के लिए मंदिर की तरफ जाने वाली सडक़ें खोलने की मांग की गई थी, न कि मंदिर में प्रवेश की मांग की गई थी।
गांधी और मालवीय की तीखी तकरार
मनोज मिट्टा की नजर में, ‘मंदिरों में दलितों को प्रवेश करने का अधिकार देने को लेकर गांधी के विचार तब बदले, जब 1932 में उन्होंने पूना का समझौता किया था। इस समझौते के तहत अछूतों ने अलग निर्वाचन व्यवस्था का अधिकार छोड़ दिया था। जबकि ये अधिकार उन्होंने लंबी लड़ाई के बाद हासिल किया था। इसके बाद ही गांधी को लगा कि बदले में उन्हें भी अछूतों के लिए कुछ करना चाहिए।’
तब भी गांधी ने अछूतों के लिए धीरे-धीरे ही आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोलने का प्रस्ताव अलग अलग मंदिरों के हिसाब से लागू किया जाना चाहिए। और, इसका फैसला स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच जनमत संग्रह के बाद किया जाना चाहिए, न कि इसे दलितों को अधिकार देने का मामला माना जाए।
मनोज मिट्टा कहते हैं कि जब गांधी ने दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार देने के विधायी सुधार का समर्थन किया, तो उनकी मदन मोहन मालवीय से तीखी तकरार हुई थी।
मदन मोहन मालवीय मंदिर में प्रवेश के मामले में किसी भी तरह की सरकारी दखलंदाजी के खिलाफ थे।
वैसे तो गांधी के समर्थन वाले विधेयक में आखिरी फैसला तब भी सवर्ण हिंदुओं के हाथ में ही छोड़ा गया था। लेकिन, मदन मोहन मालवीय ने 23 जनवरी 1933 को वाराणसी में ‘सनातन धर्म महासभा’ बुलाकर इस विधेयक के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया था।
उदयनिधि स्टालिन के बयान से छिड़ी बहस
सनातन धर्म को लेकर हालिया बहस उस वक़्त शुरू हुई, जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता का विरोधी है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी।
उदयनिधि के इस बयान को लेकर बीजेपी और विपक्षी नेताओं के बीच सियासी बयानबाज़ी शुरू हो गई। सवाल ये है कि क्या सनातन धर्म जाति व्यवस्था में विश्वास रखता है, और वो समानता के खिलाफ है?
सनातन धर्म को लेकर चल रहे विवाद के बारे में वरिष्ठ भाषा वैज्ञानिक और मानवशास्त्री डॉक्टर गणेश नारायणदास देवी (जी।एन। देवी) का कहना है कि समय के साथ, सनातन धर्म की परिकल्पना बदलती रही है।
वो इसे समझाते हुए बताते हैं, ‘18वीं सदी की शुरुआत में बंगाल क्षेत्र में एक बहस की शुरुआत हुई। इस बहस के दो पक्ष थे। एक तरफ तो ‘नूतन’ वर्ग था और दूसरी ओर ‘सनातन’ समर्थक थे। नूतन वर्ग की तमाम मांगों में अंग्रेजी में पढ़ाई कराने, सती प्रथा और बाल विवाह की प्रथाएं खत्म करने की मांगें भी शामिल थीं। वहीं ‘सनातन’समर्थकों का कहना था कि इन सभी सुधारों से समाज दूषित हो जाएगा।’
वे कहते हैं, ‘बंगाल में ये बहस करीब तीन दशक तक चलती रही थी, जिसके बाद बंगाल में पुनर्जागरण के युग की शुरुआत हुई। तो, 18वीं सदी में जहां सनातन शब्द का इस्तेमाल प्राचीन परंपराओं के लिए किया जाता था वहीं उसके बाद के दौर में इसमें तरह तरह की परंपराएं शामिल हो गईं। इनमें वेद, उपनिषद, धर्मग्रंथ और धर्म से जुड़े तमाम तरह के रिवाज शामिल हो गए।’
जी एन देवी कहते हैं कि सनातन की परंपराएं करीब डेढ़ हजार साल पुरानी हैं। लेकिन, सनातन किसी एक परंपरा या व्याख्या में यकीन रखने वाला विचार नहीं था। लेकिन, 18वीं सदी में इनमें से एक परंपरा यानी जाति व्यवस्था को पकडक़र उसे पूरी मजबूती से सनातन से जोड़ दिया गया।
सनातन धर्म, जाति व्यवस्था और 19वीं-20वीं सदी में उथल-पुथल
सनातन धर्म को लेकर छिड़ी बहस के केंद्र में उदयनिधि स्टालिन का वो बयान है, जिसमें उन्होंने सनातन को सामाजिक न्याय और बराबरी के अधिकार का विरोधी करार दिया था।
उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के दौरान जब समाज सुधार के आंदोलनों ने जोर पकड़ा, तो कुछ समुदायों के बीच से ऐसे समूह उभरे, जो ख़ुद को सनातन या फिर सुधारक कहते थे। डॉक्टर गणेश देवी के विश्लेषण से पता चलता है कि आधुनिक युग की इन परिचर्चाओं का एक प्रमुख मुद्दा जाति व्यवस्था और इसकी वजह से पैदा होने वाली गैर-बराबरी थी। अलग अलग इलाकों में इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिशें भी अलग-अलग तरह की रहीं।
चेन्नई की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका वी। गीता सामाजिक आंदोलनों के ऐतिहासिक संदर्भों पर रिसर्च की विशेषज्ञ हैं। वो कहती हैं कि सनातन धर्म असल में जाति आधारित व्यवस्था है। ये कोई ऐसा धर्म या आस्था नहीं है, जिसका अस्तित्व जाति व्यवस्था के बगैर भी बना रहे। ऐसा भी नहीं है कि सनातन धर्म का जाति व्यवस्था से कोई संबंध ही नहीं है।
वी. गीता इसी बात को बढ़ाते हुए कहती हैं, ‘सनातन शब्द ही अपनी सच्चाई खुद-ब-खुद बयान कर देता है। सनातन का मतलब है, शाश्वत, स्थायी। उन्नीसवीं सदी में सनातन की परिकल्पना को उस वक्त नई ताकत मिली, जब पुरानी हिंदू परंपराओं में लोगों की दिलचस्पी काफी जग गई थी। पूरे देश में सनातन धर्म सभाओं की स्थापना की गई थी।’
‘ये सारे संगठन पुराने और रुढि़वादी नजरिए के समर्थक थे और जाति आधारित असमानता को वाजिब ठहराकर किसी न किसी रूप में जाति व्यवस्था का समर्थन किया करते थे। ये सनातन सभाएं हिदू धर्म की एक ही छवि पेश करती थीं। जिसका मतलब था कि वो ख़ुद को दूसरे धर्मों के बरक्स खड़ा करते थे, खासतौर से उत्तर भारत में इस्लाम के खिलाफ। लेकिन, दक्षिणी भारत में सनातन शब्द कुछ बौद्धिक ब्राह्मणों के बीच ही लोकप्रिय था।’
डॉक्टर गणेश देवी कहते हैं कि वैदिक युग में सनातन धर्म में वर्ण आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई थी। ये वर्ण व्यवस्था आज की जाति व्यवस्था से अलग थी। जाति व्यवस्था तो बाद में मध्यकाल में विकसित हुई थी।
डॉक्टर देवी कहते हैं, ‘जाति और वर्ण की परिकल्पनाएं बिल्कुल अलग हैं। सनातन युग में लिखे गए प्राचीन ग्रंथों में वर्ण को स्वीकार किया गया था। वर्ण का मतलब वर्ग है, जाति नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था एक छद्म आध्यात्मिक आधार पर सामाजिक वर्गीकरण की कोशिश थी, जो पुनरावतार की परिकल्पना पर आधारित थी। हालांकि जाति व्यवस्था पेशे पर आधारित थी, और इसका कोई आध्यात्मिक आधार नहीं था। इसे कोई दैवीय, वैदिक या उपनिषद से मान्यता नहीं मिली थी।’
जैसे-जैसे जाति व्यवस्था विकसित हुई, इसमें जड़ता आती गई और इससे समाज में बहुत असमानताएं फैल गईं। इसका विरोध किया जाने लगा, क्योंकि, इस व्यवस्था में कुछ जातियों ने खुद को समाज में ऊंचा दर्जा दे दिया था और दूसरों पर जुल्म ढाने लगे थे।
जाति आधारित व्यवस्था के खिलाफ समानता का हक़ मांगने के आंदोलन देश के हर क्षेत्र में उभरे थे। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में वराकरी परंपरा ने आध्यात्मिक क्षेत्र में समानता स्थापित करने की कोशिश की। उन्नीसवीं सदी से जाति व्यवस्था के विरोध ने सामाजिक आंदोलन का स्वरूप ले लिया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जाति पर आधारित गैर-बराबरी के विरोध में मजबूती से आवाज़ उठाई और, ‘सार्वजनिक सत्यधर्म’ को इसके विकल्प के तौर पर पेश किया। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी।
वैसे तो जाति व्यवस्था और जाति के आधार पर भेदभाव का ज़ोरदार तरीके से विरोध किया जाता रहा है। लेकिन, सवाल ये भी है कि सनातन धर्म जाति व्यवस्था का समर्थन करता है, इस दावे को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या कहना है।
राज्यसभा सांसद और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार की जीवनी लिखने वाले डॉक्टर राकेश सिन्हा इस दावे को ग़लत बताते हैं कि सनातन धर्म, जाति व्यवस्था का समर्थन करता रहा है। वो कहते हैं कि, ‘सनातन तो सतत प्रगतिवादी प्रक्रिया है। समानता, सौहार्द और विविधता, सनातन धर्म के मूलभूत तत्व हैं।’
राकेश सिन्हा कहते हैं, ‘समाज के भीतर तमाम संप्रदाय, जीवन शैलियां और विविधताएं लगातार विकसित होती रहती हैं। और कोई भी इसका विरोध नहीं करता। इसलिए, सनातन और हिंदू धर्म के बीच अंतर करना बुनियादी तौर पर गलत है। क्योंकि, हिंदू धर्म का मूल तत्व सनातन धर्म ही है।’
आरएसएस का रुख क्या है?
हालांकि, राकेश सिन्हा भले ये कह रहे हों कि सनातन धर्म में समानता का विचार निहित है। लेकिन, ऐसा लगता है कि आरएसएस ने ‘सनातन धर्म’ की अपनी व्याख्या और इसको लेकर उठे हालिया विवाद के बीच जाति की सच्चाई को स्वीकार कर लिया है।
जब सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान को लेकर हंगामा बरपा हुआ था, तब सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सात सितंबर को नागपुर में अपने एक भाषण में कहा था, ‘हमने अपने साथी मनुष्यों को दो हज़ार वर्षों तक दबाकर रखा था। जिस समाज के कुछ वर्गों ने दो हजार वर्षों तक अन्याय को झेला हो, वहां पर हम दूसरों को उनके लिए दो सौ वर्षों तक थोड़ा कष्ट सहन करने के लिए क्यों नहीं कह सकते हैं।’
राजनीति वैज्ञानिक सुहास पलशिकर, मोहन भागवत के बयान को विरोधाभास के तौर पर देखते हैं। इसे समझाते हुए वो कहते हैं, ‘जो लोग बहुत बढ़-चढक़र सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, उनको उस समय बहुत परेशानी हुई जब उदयनिधि ने सनातन धर्म का कड़ा विरोध किया। वो सनातन धर्म के पक्ष में तो बोलते हैं। लेकिन वो जाति व्यवस्था की वजह से समाज पर थोपी गई असमानता को भी स्वीकार करते हैं। उनके पास मौजूदा जाति व्यवस्था का कोई समाधान है नहीं। यही वजह है कि मोहन भागवत, एक तरफ तो जाति के आधार पर आरक्षण की वकालत करते हैं। वहीं दूसरी ओर वो सनातन धर्म का भी समर्थन करते हैं।’
सनातन धर्म को लेकर छिड़ी ये बहस, निश्चित रूप से तीन राज्यों में होने वाले चुनावों में बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच सियासी तकरार का बड़ा मुद्दा बनेगी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी मध्यप्रदेश के चुनावों से पहले इस मुद्दे को हवा दे दी है। इससे ये तय हो गया है कि अब चुनावी रैलियों और भाषणों में ये मुद्दा छाया रहने वाला है। (bbc.com/hindi)