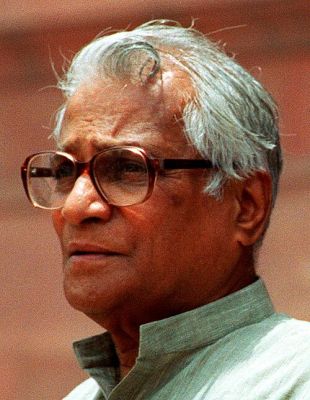विचार / लेख

अनुघा पाठक
‘तो इसका मतलब मेरी शादी मान्य नहीं है?’ मेरी सहेली गायत्री ने मुझसे सवाल किया?
उसने ये सवाल हिंदू विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बारे में पढऩे के बाद किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू विवाह एक 'संस्कार' है और ये एक समारोह के जरिये सही तरीके से पूरा होना चाहिए।
हिंदू विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ही मान्यता मिलती है।
गायत्री 35 साल की आधुनिक महिला हैं, जिन्होंने अपनी शादी में कन्यादान की रस्म नहीं होने दी थी। क्योंकि उनका मानना था कि वो कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे दान में दिया जाए।
हमारी बातचीत से मुझे ये याद आया कि मेरी दोनों बहनों की शादी में हमने वो समारोह नहीं किया था, जिसमें वर पक्ष के मेहमानों के पांव धोए जाते हैं।
तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए ये शादियां अमान्य हैं?
इसका फौरी ज़वाब है- नहीं। लेकिन इसका विस्तार से जवाब आपको इस लेख को पढऩे के दौरान मिलेगा।
आइए पहले उस केस के बारे में जानते हैं, जिससे ये बहस शुरू हुई।
अदालत की बहस और हिंदू विवाह
अदालत उस महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कहा था कि उसकी तलाक की याचिका को बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट से झारखंड के रांची कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत महिला और उनके पूर्व पार्टनर ने संयुक्त रूप से एक याचिका दायर कर कहा था कि वो अपनी असहमतियों का निपटारा कर लेना चाहते हैं।
उन्होंने कहा था कि चूंकि उनकी शादी में परंपरागत रस्मों-रिवाजों का पालन नहीं हुआ था इसलिए उनकी शादी को अमान्य करार दिया जाए।
अदालत ने उनकी याचिका मंजूर कर ली और उनकी शादी को अमान्य घोषित कर दिया।
अदालत ने फैसला देते वक्त कुछ टिप्पणियां की। इनमें से एक थी कि जहां हिंदू शादी उपयुक्त रस्मों और समारोहों से नहीं हुई वहां कानून की नजर में ये हिंदू शादी के तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी की रस्मों के एक उदाहरण के तौर पर सप्तपदी का नाम लिया गया था।
इसे समझने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 114 का जि़क्र करना होगा जिसमें शादी की ‘धारणा’ की बात की गई है।
वीणा गौड़ा महिलावादी वकील हैं और मुंबई में रहती हैं। वो कहती हैं, ‘अदालत हमेशा शादी की धारणा के पक्ष में झुका होता है। मसलन, अगर आप किसी के साथ लंबे समय तक रह रहे हैं और आपने समाज में इसे इस तरह पेश किया है कि आप दोनों पति-पत्नी हैं तो कानून भी ये मानेगा कि आप विवाहित है, जब तक कि कोई पक्ष इसे चुनौती न दे।’
वो कहती हैं कि अगर कोई शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होती है तो कुछ रस्मों-रिवाजों को करना ही होगा। साथ ही शादी के सर्टिफिकेट के लिए ऐसे समारोहों का प्रमाण भी देना होगा।’
वीणा कहती हैं, ‘विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन ही अपने आप में शादी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में निकाहनामा ही आपकी शादी हैं। वहीं क्रिश्चियन कानून के तहत शादी होने पर चर्च सर्टिफिकेट देता है। इन सभी शादियों में मैरिज सर्टिफिकेट या इसका रजिस्ट्रेशन अपने आप में शादी का हिस्सा है। हालांकि हिंदू कानून में शादी के रजिस्ट्रेशन की कोई अवधारणा नहीं है। यह कानून में बाद में शामिल किया गया।’
वो कहती हैं, ‘हिंदू कानून में शादी समारोह की अवधारणा है और इसे दोनों पक्ष में किसी के भी रीति-रिवाज और परंपराओं के तहत करना पड़ता है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन शादी का प्रमाण नहीं हो सकता। इसलिए कानून के जरिये से देखें तो कोर्ट ने जो कहा वो एक हद तक सही है।’
सप्तपदी, कन्यादान या मंगलसूत्र पहनाने को अक्सर पिछड़ी और ब्राह्वणवादी पितृसत्ता मान्यताओं का समर्थन करना माना जाता है क्योंकि ये मानती हैं कि महिलाएं दूसरी को सौंपी जाने वाली संपत्ति है।
कानून क्या कहता है?
कानून इस मामले में स्पष्ट है। ये किसी कर्मकांड या समारोह का जिक्र नहीं करता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 कहती है कि हिंदू विवाह वर-वधू में से किसी भी पक्ष के पारंपरिक अनुष्ठानों और समारोहों के जरिये हो सकता है।
वीणा एक उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं, ‘कर्नाटक के कुछ समुदायों में लोग कावेरी नदी को साक्षी मान कर शादी करते हैं। कुछ शादियों में सूर्य को साक्षी माना जाता है। कई तरह के समारोह और अनुष्ठान होते हैं। कानून किसी खास अनुष्ठान या समारोह के बारे में नहीं कहता है कि इन्हें ही किया जाना चाहिए। ये सिर्फ ये कहता है कि शादी वर या वधू में से किसी भी पक्ष की परंपरा के मुताबिक समारोह करके शादी पूरी हो सकती है।’
हिंदू विवाह अधिनियम का धारा 3 में रीति-रिवाजों का परिभाषा दी गई है। यहां रीति-रिवाज और इनका पालन करने से मतलब ऐसे नियमों को पालन करना है जो लंबे समय से लगातार उसी रूप में माने जाते रहे हैं। और ये परंपराएं किसी समुदाय, जाति, समूह या परिवार में कानून का बल (यानी कानूनी मान्यताएं) हासिल कर चुकी हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट समेत भारतीय अदालतें सप्तपदी जैसी रस्मों पर इतना जोर क्यों दे रही है?
डॉ. सरसु थॉमस नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं और जिनकी फैमिली लॉ और जेंडर कानून में विशेषज्ञता हासिल है। वो मानती हैं कि ‘सभी शादियां ब्राह्मण परंपराओं और रीति-रिवाजों के मुताबिक़ नहीं होती हैं। लेकिन ये सही है कि अदालतें ब्राह्मण परंपराओं और रीति-रिवाजों को ही देख रही हैं।’
वो कहती हैं, ‘मैं समझती हूं कि जहां-जहां कोर्ट ने सप्तपदी या होम करने पर जोर दिया है वो कुछ मामलों में ठीक नहीं है। कुछ लोग ये मान सकते हैं कि मंगलसूत्र बांधना सप्तपदी के बराबर का अनुष्ठान या परंपरा नहीं है।’
हालांकि वो कहती हैं, ‘अगर वर या वधू में से किसी पक्ष के अनुष्ठान,परंपरा या रीति-रिवाज के साथ शादी की जाती है तो शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी मानी जाएगी।’
अदालतों का ये रुख भी
कुछ मामलों में अदालतों ने दूसरा रुख अपनाया है।
उदाहरण के लिए हाल के एक केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तहत कन्यादान कोई अनिवार्य अनुष्ठान नहीं है।
पुणे में रहने वाली रमा सरोद महिला अधिकारों की विशेषज्ञ वकील हैं। उनका कहना है कि भारतीय अदालतों को प्रगतिशील रुख अपनाना चाहिए।
वो कहती हैं, ‘सुप्रीम कोर्ट को आवश्यक कर्मकांडों और समारोहों के परिभाषा को विस्तार देने की जरूरत है। उसे ये बताना होगा कि इसके दायरे में क्या आते हैं। हिंदू विवाह कानून 1955 में आया था। ये सही है कि ये कर्मकांड, रीति-रिवाज, परपराएं उस समय अहम थीं लेकिन अब हमें इन नियमों की व्याख्या आधुनिक समय के हिसाब से करनी होगी।’
रमा कहती हैं, ‘बदलती विचारधाराओं और समारोहों,अनुष्ठानों की जगह होनी चाहिए। लोगों को वही समारोह करने चाहिए जो वो समझते हैं कि ये ठीक है। उन्हें उसी के हिसाब से अपनी शादियों के रजिस्ट्रेशन का अधिकार देना चाहिए। एक वकील के तौर पर मैं ये मानती हूं कि शादी का रजिस्ट्रेशन बेहद अहम है।’ लेकिन सवाल बरकरार है। अगर कोई प्रगतिशील हिंदू उन पुराने रीति-रिवाजों का पालन न करना चाहे तो क्या होगा, भले ही शादी संपन्न होने के लिए ये जरूरी हो।
क्या नए कानून की जरूरत है?
डॉ. सरसु कहती हैं, ‘नए कनून की कोई जरूरत नहीं है।’ वो कहती हैं, ‘अंत में महिलाओं का ही परेशान होना है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी परंपरा के हिसाब से शादी करेंगे। अब अगर इन परंपराओं को मान्यता न दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं की शादियां मान्य नहीं हैं।’
वो कहती हैं, ‘मेरे हिसाब से कानून ठीक है। प्रगतिशील जोड़ों के पास हमेशा से स्पेशल मैरिज एक्ट का विकल्प खुला है। लेकिन नए अनुष्ठानों, समारोहों के लिए कोई नया कानून बनाना ठीक नहीं है। हालांकि कानून ये कह सकता है शादी मान्य होने के लिए रजिस्ट्रेशन पर्याप्त सुबूत है।’
वीणा का कहना है कि अदालत को प्रगतिशील रुख अपनाना चाहिए। उन्हें ऐसी परंपराओं को नामंजूर करना चाहिए जो लैंगिक आधार पर बने हैं। साथ ही उन्हें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि शादी नाम की संस्था कितनी प्रासंगिक है और इसके तहत महिलाओं के अधिकारों की क्या स्थिति है।
वो कहती हैं, ‘भारतीय कानून के तहत मैरिटल रेप पर विचार नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि शादी के तहत पति की ओर से किया गया अप्राकृतिक यौनाचार अपराध नहीं है। शादी में सहमति की कोई अवधारणा नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप यौन संबंध को लेकर असहमत हैं तो भी शादी करने पर इस पर आपकी सहमति मानी जाती है। ये वो चीजें हैं जिन पर मैं मानती हूं कि ज्यादा प्रगतिशील नजरिये से विचार करने की जरूरत है।’
वीणा मुझे कुछ सवालों पर सोचने को मजबूर कर देती हैं। वो कहती हैं, ‘ये कहना आसान है शादी बराबरी के आधार पर होती है। लेकिन क्या कानून महिला को बराबरी का पार्टनर बनने देता है।’
जहां तक मुझे याद है हम महिलाओं को ये कहा जाता है कि कब शादी करो किससे शादी करो और जहां तक इस बहस का सवाल है तो कैसे शादी करो।
इन सब चीजों के बीच हमारी बराबरी की लड़ाई कहां है। (bbc.com/hindi)