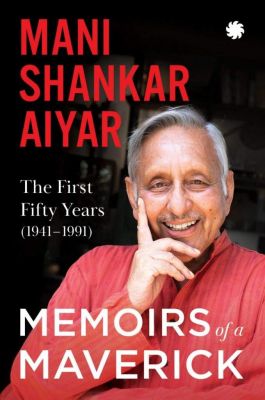संपादकीय
विधानसभा चुनाव सामने है और राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के तरीके ढूंढते ही रहते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर विपक्ष को एक कल्पनाशीलता का मौका दे रही है, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति, और नफरत के मुद्दों ने कल्पनाशीलता को खत्म कर दिया है। राजधानी में कांग्रेस का महापौर है, और शहर की सडक़ों पर गड्ढों को लेकर भाजपा ने कल विरोध दर्ज कराया है। कहने के लिए यह राजधानी आए दिन प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, और देशी-विदेशी मेहमानों की आवाजाही से घिरी हुई है, लेकिन सडक़ों का हाल इतना भयानक है जितना कि पिछले 50 बरस में कभी नहीं था। तकरीबन हर सडक़ खुदी पड़ी है, कहीं पाईप तो कहीं केबल के लिए सडक़ों को खोदा गया है, और बाकी जगहों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। नतीजा यह है कि हड्डी-पसली की किसी तकलीफ वाले मरीज को लेकर कहीं से कहीं नहीं जाया जा सकता। इन गड्ढों में गाडिय़ां रोज पलट रही हैं, कांक्रीट की सडक़ें बनाई जाती हैं, और कुछ महीनों के भीतर उन्हें खोद दिया जाता है। जाहिर है कि यह कंस्ट्रक्शन-माफिया की मर्जी से चलने वाला काम है जो कि कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन इस बार जो हालत है, वह आधी सदी में इस राजधानी में कभी नहीं रही।
अब दो महीने के भीतर यहां चुनाव होने हैं, और भाजपा को विरोध करने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं को दुपहियों पर राजधानी की चार सीटों के वोटरों को शहर घुमाने ले जाना चाहिए, और घंटे भर अगर कोई दुपहिए या चौपहिए पर इन सडक़ों पर घूम ले, तो वे न सिर्फ इस चुनाव बल्कि अगले कुछ चुनाव भी सत्तारूढ़ पार्टी को वोट न दे। भाजपा के पास पर्याप्त कार्यकर्ता हैं, और वे अभी अपने-अपने इलाके के वोटरों को गणेशोत्सव दिखाने के लिए ले जा सकते हैं। बिना भाजपा या कमल छाप का नाम लिए यह सबसे बड़ा प्रचार हो सकता है कि कांग्रेस के राज वाली म्युनिसिपल ने शहर का क्या हाल कर रखा है। यह त्यौहारों और बाजार की खरीददारी का मौसम है, और इस वक्त कदम-कदम पर जिस तरह गड्ढे हैं, जिनमें लोग रात-दिन गिर रहे हैं, वह देखना भी भयानक है।
भाजपा के सामने प्रचार का एक और मौका हो सकता है। शहर के कई इलाकों में जिस अंदाज में दुकानों के बाहर सडक़ों पर अवैध कब्जे करके कारोबार किया जा रहा है, भाजपा को राजधानी की चारों सीटों के वोटरों को इन बस्तियों का दौरा भी करवाना चाहिए ताकि वे देख लें कि शहर के कुछ हिस्सों का क्या हाल है और वहां किस तरह कोई भी कानून लागू नहीं होता है। लेकिन बात घूम-फिरकर फिर इसी पर आती है कि जब तक भाजपा किसी को उम्मीदवार घोषित न करे, रोज दसियों हजार रूपए का पेट्रोल ऐसे मतदाता पर्यटन पर कौन खर्च करे? और जब उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, तो उस वक्त ऐसे काम के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के पास वक्त नहीं रहेगा। भाजपा को चाहिए कि वह परंपरागत बयानबाजी के बेअसर धंधे को छोड़े, और वोटरों को उन्हीं के शहर की बदहाली दिखाने का ठोस काम शुरू करे। प्रदेश में अलग-अलग जगहों से निकली हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा चार दिन बाद राजधानी रायपुर पहुंचने वाली है, और उसकी सबसे बड़ी तैयारी यही हो सकती है कि तब तक इन चारों विधानसभा सीटों के अधिक से अधिक वोटरों को सडक़ों के धक्के खिला दिए जाएं, और कुछ चुनिंदा बाजारों और बस्तियों की अराजकता शाम से देर रात तक कभी भी ले जाकर दिखा दी जाए। इससे अधिक मजबूत चुनाव प्रचार भाजपा के लिए और कुछ नहीं हो सकता है।
छत्तीसगढ़ में ऐसा लगता है कि दोनों बड़ी पार्टियों के बीच अभी कोई मुकाबला ही नहीं है। कांग्रेस रात-दिन हर मिनट चुनाव प्रचार में लगी है, वह जनधारणा गढऩे में लगी है, और जनधारणा प्रबंधन में भी। दूसरी तरफ भाजपा दिल्ली की तरफ देखते हुए बैठी है कि वहां से आकाशवाणी पर कौन सा आदेश आता है, कब आता है। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं में खुद पहल करके कुछ करने का उत्साह दिख नहीं रहा है, और जिस तरह केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आना दो-दो बार रद्द हो चुका है, उससे भी राज्य के भाजपा नेता और अधिक दुविधा में आ गए हैं कि उन्हें कुछ करना चाहिए या चुप घर बैठना चाहिए। हर गुजरता हुआ दिन भाजपा की इस दुविधा के साथ उसे किसी भी संभावना से दूर धकेल रहा है। पर्दे के पीछे और जमीन के नीचे इस पार्टी की तैयारियों की बड़ी-बड़ी कहानियां सुनाई पड़ती हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखता।
चुनाव तैयारी के मामले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी भाजपा से कोसों आगे चल रही है, वह सत्ता पर भी है, इसलिए उसका बहुत सा चुनाव प्रचार तो सरकारी कार्यक्रमों से भी होते रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद के उपचुनावों में कांग्रेस और भाजपा के बीच जिस तरह का फासला हो चुका है, उसे पाट पाना वैसे भी बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में दिल्ली से नियंत्रित होती छत्तीसगढ़ भाजपा जिस तरह टूटे मनोबल के साथ हिचकती और झिझकती हुई दिख रही है, वह जंग के मुहाने पर खड़ी सेना जैसी बिल्कुल नहीं है। किसी पार्टी की जीत या हार से हमारा कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन अगर किसी शहर या प्रदेश की बदहाली महीनों से चली आ रही है, तो उसका इस्तेमाल विपक्ष को इसलिए भी करना चाहिए कि हो सकता है कि जनता की दिक्कतें उसे एक आक्रामक चुनावी मुद्दा बनाने से दूर हो सकें।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
भारत और कनाडा के रिश्तों पर मानो गाज गिर गई। कनाडा भारतवंशी लोगों से भरा हुआ है, और दोनों देशों के बीच बड़े कारोबारी रिश्ते हैं। इनकी वजह से दोनों के बीच संबंध ठीक रहने थे, लेकिन हिन्दुस्तान के एक आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, खालिस्तान को लेकर दोनों देशों के रिश्ते फिलहाल तो तबाह दिखते हैं। मोदी सरकार के 9 बरसों में यह पहली बार दिख रहा है कि कोई बड़ा पश्चिमी देश भारत पर कत्ल का इल्जाम लगाते हुए उसके एक राजनयिक को देश से निकाल दे। जवाब में भारत ने भी ऐसा ही किया है, लेकिन इस जवाबी कार्रवाई से यह तनातनी खत्म नहीं हो जाती क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री ने वहां की संसद में औपचारिक घोषणा करते हुए यह साफ-साफ कहा है कि कनाडा की जमीन पर, एक कनाडाई नागरिक का कत्ल किया गया, और जांच में ऐसे तथ्य मिल रहे हैं कि इसके पीछे भारत है। यह बात साफ है कि कनाडा में खालिस्तानी आंदोलन को बड़ी छूट मिली हुई है, और कुछ महीने पहले लोग यह देखकर हक्का-बक्का रह गए थे कि सिक्खों के एक बड़े कार्यक्रम में इंदिरा गांधी की हत्या की एक झांकी निकाली गई थी। भारत में उस मौके पर भी, और उसके पहले भी दर्जनों बार कनाडा से खालिस्तानी आंदोलन के मुद्दे पर विरोध दर्ज किया था, और कहा था कि भारत में आतंकी और अलगाववादी कार्रवाई करने वाले खालिस्तानी आंदोलनकारी कनाडा की जमीन पर बढ़ावा पा रहे हैं।
भारत के कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि खलिस्तानी आंदोलन का हिन्दुस्तान में कोई अस्तित्व नहीं है, और ऐसे नामौजूद आंदोलन में अपनी भागीदारी बताकर भारत के कई सिक्ख पश्चिमी देशों में राजनीतिक शरण मांगते हैं कि भारत में उन पर खतरा है। दूसरी तरफ भारत ने अभी यह कहा है कि कनाडा में खालिस्तानी आंदोलनकारियों को बढ़ावा देकर वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी कमजोर स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक हकीकत है कि पश्चिमी देशों में राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाकी दुनिया के लिए परेशानी या असहमति का सबब रहती है। इस मामले में भी कुछ हद तक ऐसा ही है कि कनाडा वहां की सिक्ख आबादी के खालिस्तानी-जनमतसंग्रह करते हैं, और पश्चिम के देश ऐसे आंदोलनों को तब तक गैरकानूनी करार नहीं देते, जब तक कि वे हिंसक न हो जाएं। हालांकि कनाडा में खालिस्तानी आंदोलनकारियों में से कुछ ने बड़ी हिंसा भी की है, और लोगों को याद होगा कि कनाडा के इतिहास का सबसे बुरा आतंकी हमला 1985 में एयर इंडिया के एक प्लेन को बम लगाकर उड़ा देने का था, और 1985 के इस खालिस्तानी हमले में सवा तीन सौ से ज्यादा लोग मारे गए थे जिनमें से अधिकतर कनाडा के थे। इसके बाद भी वहां बसी हुई सिक्ख आबादी संख्या में बहुत बड़ी है, राजनीति में सक्रिय है, और वहां मंत्रिमंडल में ऐसे सिक्ख भी रहते आए हैं जो कि खालिस्तानी आंदोलन के आरोपी रहे हैं।
लेकिन इनमें से कोई भी बात बिल्कुल ताजा नहीं है, ये अधिकतर तनाव काफी अरसे से चले आ रहे थे, और ऐसे में जब भारत और कनाडा के प्रधानमंत्री अभी-अभी जी-20 के दौरान रूबरू मिले थे, तब भी कनाडा में हुई इस हत्या की बात ट्रूडो ने मोदी से की थी, लेकिन बात किसी किनारे पहुंची नहीं। एक अभूतपूर्व तनातनी के बीच ट्रूडो कनाडा लौटे, और उन्होंने वहां संसद में भारत पर यह खुला आरोप लगाया और उसके खिलाफ राजनयिक निष्कासन की कार्रवाई की। इस तनातनी में पश्चिम के कई विकसित और ताकतवर देशों के सामने एक परेशानी खड़ी कर दी है कि आज जब वे एक तरफ तो यूक्रेन के मोर्चे पर उलझे हुए हैं, चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय मुकाबला चल ही रहा है, ऐसे में इन दोनों ही मुद्दों पर भारत के साथ के जरूरी होने पर वे किस तरह कनाडा का भी साथ दें? अमरीका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कनाडा ने अपनी कार्रवाई का खुलासा किया है कि वह अपनी जमीन पर अपने नागरिक का कत्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसने इन देशों को अपनी नजर में कत्ल के सुबूत पेश भी किए हैं। आज ये तमाम देश कनाडा के साथ भी बने रहना चाहेंगे, और भारत को भी साथ रखना चाहेंगे। इसलिए भारत और कनाडा दोनों के लिए यह नौबत अंतरराष्ट्रीय असुविधा खड़ी करने की भी है।
फिर कनाडा में लाखों भारतीय छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं, और भारतीय मूल के लाखों लोग वहां बसे हुए हैं। ऐसे में बड़े कारोबारी रिश्तों के अलावा भारतीयों और भारतवंशियों की हिफाजत भी एक बड़ी बात है, और इस मोर्चे पर कोई भी नया तनाव खड़ा होने पर वह भारत के लिए एक परेशानी रहेगी। इन दोनों ही देशों के लिए आज यह माना जा रहा है कि यह कूटनीतिक असफलता है जब दोनों देशों के पीएम दिल्ली में मिल-बैठकर भी इस मुद्दे को नहीं सुलझा पाए, तो फिर अब नीचे के स्तर पर इसका कोई आसान समाधान जल्द हो जाए ऐसा दिखता नहीं है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि खालिस्तानी मुद्दे पर अगर भारत को यह साख मिल रही है कि उसने कनाडा में एक खालिस्तानी को मार गिराया है, तो उससे हिन्दुस्तान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समर्थकों और प्रशंसकों के बीच उनके लिए तारीफ के सिवाय कुछ नहीं होगा। राष्ट्रवादी सोच आतंकियों से सरहद पर या विदेशों में कड़ाई से निपटने की वकालत करती है। दुनिया के कुछ और देश भी अपने विरोधियों के साथ इस किस्म की ‘कार्रवाई’ करने के लिए जाने जाते हैं। यह अलग बात है कि देशों से उम्मीद की जाती है कि वे रंगे हाथों न पकड़ाएं। अब कनाडा हिन्दुस्तान के खिलाफ जिन सुबूतों का हवाला दे रहा है, उनके सामने आने पर ही कोई बात साबित हो सकती है, लेकिन उससे मोदी को भारत के भीतर आबादी के एक बड़े हिस्से में एक मजबूत नेता की शोहरत मिलेगी, जिसे इसमें भी मोदी है तो मुमकिन है ही देखने मिलेगा।
फिलहाल हम इसे दोनों देशों के सर्वोच्च स्तर पर कूटनीतिक नाकामयाबी मानते हैं, और कनाडा इस हद तक पहुंचा, या उसे इस हद तक जाना पड़ा कि वह संसद में भारत को औपचारिक रूप से हत्या का जिम्मेदार कहे, तो यह किसी भी तरह की बातचीत की पूरी ही असफलता है। इस नौबत से पश्चिम के देशों में बसे हुए खालिस्तान-समर्थकों को एक नई ताकत मिलेगी कि कम से कम कनाडा की सरकार इस हद तक उसके लिए और उसके साथ खड़ी है। आने वाला वक्त बताएगा कि इन दोनों बड़े और ताकतवर देशों के रिश्ते किस तरफ बढ़ते हैं क्योंकि दोनों के आपसी हित बहुत व्यापक हैं, और दोनों के साझा दोस्त भी इस तनाव से परेशान हैं। फिलहाल तो यह लगता है कि इस ताजा तनाव से भारत और कनाडा दोनों के प्रधानमंत्रियों को अपनी-अपनी जमीन पर, अपने-अपने लोगों के बीच एक नई ताकत मिली है, और अपने-अपने विपक्षियों का समर्थन भी मिला है।
अगले कुछ दिन दुनिया में कोई बहुत बड़ी अनहोनी न हो जाए, तो हिन्दुस्तान के भीतर चर्चा और बहस के लिए महिला आरक्षण अकेला मुद्दा होना चाहिए। चौथाई सदी से चली आ रही कोशिशों को कल मोदी सरकार ने एक बार फिर एक विधेयक की शक्ल में संसद में पेश किया है, और इस बार सत्तारूढ़ पार्टियों से परे भी देश का प्रमुख विपक्षी दल, कांग्रेस इसके साथ है, और कई और पार्टियां भी यूपीए-2 के शासन काल के मुकाबले अब महिला आरक्षण का साथ देंगी। कांग्रेस की एक मुखिया सोनिया गांधी ने अभी कुछ मिनट पहले लोकसभा में इस बिल पर अपनी बात शुरू करते हुए पहला ही वाक्य इसका समर्थन करने का कहा है। उसके साथ ही उन्होंने दो-तीन और बातें कही हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह बात कही जा रही है कि और छह-आठ बरस भारतीय महिला अपने हक का इंतजार करे। उन्होंने मांग की कि इस बिल को तुरंत ही अमल में लाया जाए, और उसके बाद जाति जनगणना करवाकर अनुसूचित जाति, जनजाति, और ओबीसी की महिलाओं के हक सुनिश्चित किए जाएं। जाहिर है कि वे लोकसभा की मौजूदा सीटों के भीतर आज के दलित और आदिवासी आरक्षण के तहत ही महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने की वकालत कर रही हैं, और हमारा मानना है कि संसद के मौजूदा आरक्षण के तहत एक बड़ा सीधा-सरल आरक्षण आज लागू हो सकता है, जो कि आने वाले पांच विधानसभा चुनावों के पहले भी किया जा सकता है। आज संसद में अनारक्षित, और दलित, आदिवासी, ऐसी तीन किस्म की सीटें हैं। इन तीनों तबकों के भीतर 33 फीसदी आरक्षण तुरंत ही लागू हो सकता है, और एनडीए और कांग्रेस मिलकर ही देश के आधे राज्यों में ऐसे संशोधन को पास करने के लिए काफी हैं।
भारत की जनगणना, और लोकसभा, विधानसभा सीटों के डी-लिमिटेशन का काम बड़ा जटिल है। कुछ लोगों का हिसाब है कि कल के विधेयक के बाद खबरों में आई यह जानकारी सही नहीं है कि महिला आरक्षण 2029 में लागू हो जाएगा। राजनीति और चुनावों के एक जानकार योगेन्द्र यादव ने लिखा है कि 2001 में संशोधित आर्टिकल 82 इस बात की स्पष्ट मनाही करता है कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के पहले डी-लिमिटेशन किया जाए। इसका मतलब यह है कि डी-लिमिटेशन 2031 में ही हो सकेगा। योगेन्द्र यादव का कहना है कि डी-लिमिटेशन कमीशन आमतौर पर तीन से चार साल लेता है, पिछले आयोग ने तो पांच बरस लिए थे। इसके अलावा आने वाला डी-लिमिटेशन का काम बड़े बखेड़े वाला हो सकता है क्योंकि (उत्तर और दक्षिण) की आबादी के अनुपात में बड़ा फेरबदल हुआ है। इसलिए हम 2037 या उसके बाद ही इस आरक्षण की संभावना देखते हैं जो कि 2039 में ही लागू हो पाएगा। कई और लोगों ने भी इसी तरह का हिसाब-किताब सामने रखा है।
इसीलिए हम यहां सोनिया गांधी की बात से एकदम ही सहमत हैं कि इस बिल को बिना वैसी किसी देरी के तुरंत ही लागू करना चाहिए, और इस संविधान संशोधन को दो हिस्सों में भी किया जा सकता है। सोनिया ने इसे तुरंत लागू करने कहा है, और वे इस बात को जानती है कि पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव अभी सामने हैं। जब वे संसद में कुछ बोल रही हैं, तो उनके कहे हुए ‘तुरंत’ का मतलब उनकी पार्टी भी अच्छी तरह समझती है जिसकी कि चार राज्यों में खुद की सरकार है। और ये सरकारें एनडीए की सरकारों के साथ मिलकर आधे राज्यों से संविधान संशोधन पास करवाने की जरूरत पूरी कर सकती हैं। अभी भी अगर कांग्रेस आज इस बात की जिद करे, और अपने राज्यों से इसे पास करवाने का जिम्मा ले, तो 15 दिन बाद की चुनाव घोषणा के पहले शायद यह काम हो सकता है। राज्यों में मौजूदा विधानसभा सीटों का लॉटरी से आरक्षण निकालना भी कुल एक दिन का काम है, और महिला आरक्षण लागू होते ही चुनाव आयोग उसे भी कर सकता है। यह याद रखने की जरूरत है कि सोनिया गांधी की कांग्रेस ने ही यूपी चुनाव में 40 फीसदी टिकटें महिलाओं को दी थीं। अब उसे अपने उस वैचारिक फैसले के साथ ईमानदारी से डटकर खड़े रहना चाहिए। आज देश में जो माहौल बन रहा है कि अगले दस-पन्द्रह बरस के बाद ही महिला आरक्षण लागू हो सकेगा, उस माहौल के बीच सोनिया की यह मांग बड़ी अहमियत रखती है, और डी-लिमिटेशन के बाद के आरक्षण तक मौजूदा सीटों पर एक तिहाई आरक्षण महिलाओं को एक बड़ी संभावना तुरंत ही दे सकता है। मोदी सरकार ने जो विधेयक रखा है, उसे सैद्धांतिक रूप से पहले कदम के रूप में अभी तुरंत लागू करना चाहिए। फिर ऐसे आरक्षण से चाहे जिस पार्टी को, चाहे जिस प्रदेश में फायदा मिलना हो, वह मिलता रहे। वह फायदा आखिर उन पार्टियों की महिलाओं को भी तो मिलेगा, जो पहले तो उम्मीदवार बन सकेंगी, और फिर जीत भी सकेंगी।
महिला आरक्षण चौथाई सदी से ज्यादा समय से बार-बार संसद के दरवाजे खटखटा रहा था, और कम से कम चार अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के वक्त इसे लेकर कोशिश हुई थी। आखिर में जाकर मामला महिला आरक्षण के भीतर अलग से ओबीसी आरक्षण पर आकर रूक गया था, जो कि एक फिजूल का तर्क था। ओबीसी आरक्षण तो आज संसद और विधानसभाओं में किसी भी जगह पर नहीं है, तो जब पुरूषों को ही ओबीसी आरक्षण नहीं है, और संसद और विधानसभाएं चल रही हैं, तो इसी व्यवस्था में महिलाओं के जुड़ जाने से कौन सी नई बेइंसाफी होने जा रही थी? ऐसा लगता है कि कुछ पार्टियां, जिनमें लालू-मुलायम की पार्टियां आगे थीं, वे किसी भी तरह महिला आरक्षण को रोकना चाहते थे, उन्होंने संसद और विधानसभाओं में ओबीसी आरक्षण के बिना ही सिर्फ महिलाओं के भीतर ओबीसी की मांग करके 2010 में विधेयक को पटरी से उतार दिया था। अब सोनिया गांधी की यह बात सही है कि पहले इसे तुरंत लागू किया जाए, और उसके बाद फिर जातीय जनगणना करवाकर उसे दलित, आदिवासी, और ओबीसी सभी के लिए लागू किया जाए। उन्होंने साफ-साफ कहा कि इस बिल को लागू करने में देरी भारतीय महिला के साथ बेइंसाफी होगी।
यह एक बात विवाद की हो सकती है कि जनगणना करवाई जाए, या कि जातीय जनगणना करवाई जाए जिसके कि भाजपा खिलाफ रही है। फिर यह भी एक नया विवाद हो सकता है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए या नहीं। फिर यह भी आरक्षण हो सकता है कि उत्तर भारत में आबादी अंधाधुंध बढऩे की वजह से वहां डी-लिमिटेशन में सीटें बढ़ जाएंगी, और दक्षिण के जिम्मेदार राज्यों ने आबादी पर काबू रखा, तो उनकी सीटें घट जाएंगी। ऐसे कई विवाद आगे जनगणना, जातीय जनगणना, डी-लिमिटेशन को लेकर आएंगे। इसलिए आज यही सबसे समझदारी की बात है कि बिना किसी अगले विवाद में उलझे हुए जो तुरंत आसानी से मुमकिन है, वह हक महिला को अभी दे दिया जाए, ताकि दो महीने बाद के चुनाव में वह एक तिहाई सीटों पर जीतकर विधानसभाओं में पहुंच सके, 2024 में संसद की शक्ल भी बदल सके।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जो लोग बारीकी से देखते आ रहे हैं उन्हें मालूम है कि मोदी का मिजाज एक जादूगर किस्म का है, और वे बार-बार अपने हैट में हाथ डालकर खरगोश निकालकर दिखाते हैं। उनके कई फैसले नोटबंदी दर्जे के आत्मघाती रहे, लेकिन उनके कुछ फैसले ऐतिहासिक महत्व के भी रहे। और ऐसा ही एक फैसला महिला आरक्षण को दुबारा लाने का है। यह फैसला कांग्रेस सरकार के लाए हुए एक विधेयक का किसी तरह का विस्तार होगा जिसे कि यूपीए सरकार खुद पास नहीं कर पाई थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की बिल को बहुमत से पारित करा लिया था। उस वक्त यूपीए का समर्थन करने वाले लालू-मुलायम ने सरकार से समर्थन वापिस लेने की धमकी दी थी, और बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया था। ये दोनों पार्टियां महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी के लिए अलग से कोटे की मांग कर रही थीं, क्योंकि उनका मानना था कि इससे संसद में सिर्फ शहरी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
अब पुराने इतिहास बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, और यह माना जाना चाहिए कि नये संसद भवन में लोकसभा के हॉल में बढ़ी हुई सीटों के साथ अब महिला आरक्षण कई तरह से होना मुमकिन है, जिनमें मौजूदा सीटों में एक तिहाई पर आरक्षण तो एक जरिया हो सकता है, दूसरा यह भी हो सकता है कि लोकसभा की मौजूदा सीटों में एक तिहाई अतिरिक्त सीटें जोड़ दी जाएं। कल इसे मोदी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, और आज-कल में संसद के इस चार दिनों के सत्र में इस विधेयक के विवरण सामने आ जाएंगे। यह जाहिर है कि महिला आरक्षण पर काफी हद तक काम कर चुकी कांग्रेस पार्टी इस विधेयक के इतिहास को लेकर अपना योगदान गिनाएगी, और मोदी सरकार भी नई पैकिंग में पुराना माल पेश करने के बजाय कुछ नया तरीका ईजाद कर सकती है कि महिला आरक्षण को सिर्फ मोदी के नाम से याद रखा जाए।
अब जिस वक्त हम यह बात लिख रहे हैं उस वक्त तक यह विधेयक पेश नहीं हुआ है, इसलिए इसकी अलग-अलग कई किस्म की संभावनाओं पर ही लिखा जा सकता है। हम उन बारीकियों पर जाना नहीं चाहते जो कि इस विधेयक में चौंकाने के अंदाज में आ सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर इससे देश में जो फर्क पड़ेगा, हम अभी इस पल उसी पर लिख रहे हैं। आज किसी समय संसद में यह विधेयक रख दिया जाएगा, और ऐसा अंदाज है कि एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, 33 फीसदी आरक्षण की पुरानी कोशिश अब कामयाब होगी, चौथाई फीसदी बाद जाकर महिलाओं को उनके हक से काफी कम मिलने की बात किसी किनारे पहुंच पाएगी। महिलाओं की आधी आबादी है, और यह आरक्षण भी एक अहसान की तरह उन्हें एक तिहाई सीटें देने वाला हो सकता है। आज देश में संसद और विधानसभाओं में महिलाएं बहुत कम हैं, और 33 फीसदी आरक्षण से भी यह संख्या दुगुनी हो सकती है।
अब अगर ‘इंडिया’ गठबंधन में पार्टियों के बीच इसे लेकर मतभेद बढ़ता है, तो उससे गठबंधन की मजबूती पर आंच आ सकती है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी सत्तारूढ़ चतुराई से इस गठबंधन पर तरह-तरह के दबाव खड़े कर रहे हैं, पहला दबाव वन-नेशन-वन इलेक्शन को लेकर हुआ, जिसे लेकर ‘इंडिया’ गठबंधन के दलों के बीच मतभेद सामने आए, और एक पखवाड़े के भीतर ही यह दूसरा मामला उन्होंने पेश कर दिया है। यह भी हो सकता है कि संसद में पार्टियों के मौजूदा रूख और उनके सदस्यों की गिनती लगाकर लालू-मुलायम की पार्टियों को यह समझ आ जाए कि उनका विरोध कारगर नहीं होगा, और वे शहादत के अंदाज में इसका विरोध न करें। लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर संसद में विधेयक पास करने जितना बहुमत मोदी सरकार जुटा लेती है, तो भी वाहवाही तो मोदी सरकार की ही होगी। यूपीए सरकार के पास भी महिला आरक्षण करने के लिए पूरे दस बरस थे, और वह अगर अपने साथी दलों को इसके लिए सहमत नहीं करा पाई थी, तो यह उसकी नाकामयाबी थी।
खैर, हम अगर आज की हकीकत पर आएं, तो ऐसा लगता है कि पंचायत और म्युनिसिपलों में महिला आरक्षण से अगर कोई सबक इस संसद-विधानसभा महिला आरक्षण को मिलेगा, तो ऐसा लगता है कि महिला आरक्षित सीटें हर पांच या दस बरस में रोटेशन से बदलती रहेंगी। और ऐसा होने पर देश की हर विधानसभा और लोकसभा सीट पर पार्टियों को महिला लीडरशिप तलाशनी होगी, उन्हें तैयार करना पड़ेगा, और अगर वे खुद होकर तैयार हैं, तो उनके मौके बढ़ते रहेंगे। हमारा तो यह भी मानना है कि इस देश में इस कानून को ऐसा गतिशील बनाना चाहिए कि हर पांच बरस में महिला आरक्षण पांच फीसदी बढक़र 50 फीसदी तक पहुंचाया जाए, और वही सामाजिक न्याय होगा। इतना लंबा वक्त मर्द नेताओं को मिलने से वे भी धीरे-धीरे अपनी मर्दानगी के दूसरे तरह के गैरचुनावी इस्तेमाल सोच सकेंगे, और एक पीढ़ी गुजरने तक, अगले 20 बरस में यह सामाजिक न्याय पूरी तरह शक्ल ले सकेगा।
अब इस विधेयक की जानकारियां कुछ घंटों में सामने रहेंगी, और ऐसा लगता है कि इसे खारिज करने का खतरा आमतौर पर कोई भी पार्टी नहीं उठाएगी, क्योंकि उसे अपनी महिला समर्थकों को यह समझाना मुमकिन नहीं होगा कि उसने महिला आरक्षण का विरोध क्यों किया। तथाकथित समाजवादी, कुनबापरस्त हिन्दीभाषी इलाकों की पार्टियों के लिए भी शायद इसे खारिज करना मुश्किल होगा, और महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी आरक्षण का उनका तर्क इसलिए निहायत खोखला और फिजूल है कि आज तो संसद और विधानसभाओं में किसी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं है, और जब ओबीसी के मर्द ऐसे आरक्षण के बिना चल सकते हैं, तो महिला आरक्षण बिना ओबीसी आरक्षण के क्यों नहीं हो सकता?
आज एक दूसरा बड़ा सवाल यह है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव एकदम सामने है, और क्या इन तीन दिनों में संसद में पास हो जाने पर यह विधेयक मौजूदा सीटों पर सीधे-सीधे लागू हो जाएगा, और इसी चुनाव को प्रभावित करेगा, या फिर यह आगे की किसी तारीख पर लागू होगा? अभी जो खबरें आ रही हैं उनसे ऐसा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि यह लोकसभा और विधानसभा की सीटों के डीलिमिटेशन से भी जोड़ा जाएगा, और अगली जनगणना से भी। ऐसा कुछ भी होने पर यह विधेयक अभी सैद्धांतिक रूप से पारित होगा, और इस पर अमल आने वाली तारीखों से बाकी पहलुओं के हिसाब से होगा।
अभी हम विधेयक को देखे बिना यह चर्चा कर रहे हैं, महिला आरक्षण के कई अलग-अलग तरीके मुमकिन हैं, उन पर चर्चा भी चल रही है, लेकिन जादूगर मोदी पिटारे से क्या निकालेंगे, यह अभी इस पल तो हमारे सामने नहीं है। फिर भी देश में महिला लीडरशिप के विकास में इससे जमीन-आसमान का एक फर्क आएगा, जो कि चौथाई सदी पहले से संसद में इंतजार कर रहा था, और भारतीय राजनीति से मर्दों का दबदबा भी इससे कुछ हद तक घटेगा, हालांकि सरपंच पति या पार्षद पति की तरह विधायक पति और सांसद पति का खतरा भी कुछ चुनावों तक रह सकता है, लेकिन यह सोच भी कौन सकते हैं कि हिन्दुस्तानी महिला को उसका कोई भी हक आसानी से मिल जाएगा। यह बिना अधिक जानकारी लिखी गई एक प्रारंभिक बात है, और हम कल इसी जगह शायद इसी मुद्दे के बाकी नए सामने आने वाले पहलुओं पर फिर से लिखेंगे।
कांग्रेस को शायद काफी देर से यह बात समझ आई, लेकिन हैदराबाद में हुई पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी सहित दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल जैसे नेताओं ने कहा कि तमिलनाडु के डीएमके नेता के बयान से शुरू हुए सनातन के बयानबाजी से पार्टी को बचना चाहिए। वहां से निकली खबरें बताती हैं कि कांग्रेस के बहुत से नेताओं का यह कहना था कि पार्टी को बीजेपी के एजेंडा में नहीं फंसना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने नेताओं को पार्टी लाईन से परे निजी बयान देने से कड़ाई से मना किया है। कुल मिलाकर पांच राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को कई हिसाब से चौकन्ना कर दिया है, और वह जो परंपरागत चूक करती है, अब उसका नुकसान पार्टी को समझ आ रहा है। लेकिन औपचारिक चर्चाओं से परे अभी भी बहुत सी बातें हैं जो कि इन खबरों में नहीं आई हैं, और हो सकता है कि उन पर कार्यसमिति की बैठक में चर्चा हुई हो, या न भी हुई हो।
कांग्रेस एक बड़ी पुरानी पार्टी है, और इसका धर्मनिरपेक्षता का इतिहास रहा है। लेकिन हाल के बरसों में इसने यह बात समझ ली कि मुस्लिमों, दलितों, आदिवासियों, या दूसरे अल्पसंख्यकों के मुद्दों को उठाने का नुकसान शायद उसे झेलना पड़ता है। पता नहीं यह बात सच है, या फिर कांग्रेस के भीतर के कुछ कम धर्मनिरपेक्ष, कुछ अधिक हिन्दू लोगों का ऐसा सोचना है। जो भी हो, हाल के बरसों में कांग्रेस ने बड़ी खुलकर हिन्दुत्व की राजनीति की है, और शायद उसने यह भी मान लिया है कि मुस्लिमों के पास भाजपा के खिलाफ अगर कांग्रेस को जिताने का स्पष्ट विकल्प होगा, तो वह कांग्रेस को छोडक़र कहीं जा नहीं सकती, और अगर उसके पास कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ऐसा विकल्प है जो कि भाजपा के खिलाफ जीत की संभावना वाला है, तो वह कांग्रेस से लगाव खत्म भी कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के काफी नेता अल्पसंख्यकों की अनदेखी की राजनीति कर रहे हैं, ताकि बहुसंख्यक हिन्दुओं को पार्टी हिन्दू-विरोधी, या मुस्लिमपरस्त न लगे। पता नहीं यह कांग्रेस का सोचा-विचारा फैसला है, या इसके क्षेत्रीय छत्रप अपने स्तर पर ऐसी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यह तो बहुत जाहिर है कि एक-एक करके बहुत से प्रदेशों में कांग्रेस हिन्दुत्व बी टीम के रूप में अपनी पहचान बना रही है, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में वह भाजपा को पीछे छोड़ चुकी बताई जाती है।
जब देश के मतदाताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा धर्मनिरपेक्षता की लंबी परंपरा और राजनीतिक चेतना को पूरी तरह खोकर धार्मिक ध्रुवीकरण में गर्व पाने लगा है, तो वैसे में चुनावी राजनीति में किस पार्टी को क्या करना चाहिए, इस बारे में हमारे पास कोई समाधान नहीं है। हम अपनी परंपरागत सोच के मुताबिक इतना ही कह सकते हैं कि हर पार्टी को धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए, और वैसा ही दिखना भी चाहिए। लेकिन सत्ता की राजनीति में यह हर पार्टी की अपने प्रति जिम्मेदारी बनती है, और उसका हक बनता है कि वह साम्प्रदायिकता फैलाए बिना, धर्मान्धता को अपनाए बिना, बहुसंख्यकों के धर्म को बढ़ावा देकर अपनी जमीन तैयार करे। पता नहीं मोदी की अगुवाई में भाजपा के रहते हुए ऐसा हिन्दुत्व कांग्रेस को किसी किनारे पहुंचा पाएगा या नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अलग-अलग कुछ प्रदेशों मेें ऐसा ही करते दिख रही है। अभी कांग्रेस कार्यसमिति के कुछ नेताओं के जो बयान बाहर आए हैं, उनमें भाजपा जैसी हिन्दूवादी पार्टी के जाल में फंसने के खिलाफ पार्टी के नेताओं को आगाह किया गया है। ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के मुद्दे पर डीएमके नेताओं ने अपना जो परंपरागत रूख सामने रखा है, उसमें नया कुछ नहीं है, सिवाय भाजपा के उसे दुहने के। भाजपा ने तुरंत ही देश के चुनावी माहौल के बीच इसे सनातन धर्म और हिन्दू धर्म पर हमला करार दिया है, और इंडिया-गठबंधन में डीएमके के साथ रहने पर कांग्रेस को भी इस हमले में शामिल बताया है। चुनावी राजनीति में इतनी तोहमत बहुत हैरान करने वाली नहीं है, लेकिन वोटरों की कमअक्ली के बीच कांग्रेस के किसी भी बड़बोले नेता का बयान पार्टी के लिए बड़ी फजीहत बन सकता है, और हैदराबाद में यही फिक्र सामने आई है, और इसकी तरफ से सावधान रहने की बात कही गई है।
लेकिन कांग्रेस में नासमझी कई अलग-अलग स्तरों पर होती है। जब हिन्दू धर्म से जुड़े हुए कोई मुद्दा या विवाद खबरों में आते हैं, तो कई बार कांग्रेस के कोई मुस्लिम प्रवक्ता उस पर बयान देते दिखते हैं। यह लापरवाही आत्मघाती है, और भारत में हिन्दू-मुस्लिम तनातनी की हकीकत को अनदेखा करना भी समझदारी नहीं है। जब पार्टी के पास आधा दर्जन बड़े-बड़े हिन्दू प्रवक्ता भी हैं, तो पार्टी के मुस्लिम प्रवक्ता या नेता का उस पर कुछ कहना जरूरी तो नहीं रहता। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कई बार होते आया है। अब जाकर अगर पार्टी को धार्मिक संवेदनशीलता समझ में आ रही है, तो उसे सबसे पहले अपने नेताओं को उनके धर्म से परे के धर्मों पर बयानबाजी से दूर रहने को कहना चाहिए। लेकिन एक दूसरी बात यह भी है कि हाल के बरसों में कुछ प्रदेशों में कांग्रेस ने जिस आक्रामक अंदाज में हिन्दुत्व के मुद्दे पर लीड लेने की कोशिश की है, उससे जनता के बीच हिन्दुत्व को लेकर भावनात्मक उभार आया है। उसका नतीजा यह निकल रहा है कि आज हिन्दू-मुस्लिम, या हिन्दू-ईसाई जैसे किसी भी छोटे से तनाव के खड़े होने पर भी बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय का एक तबका तुरंत ही झंडा-डंडा लेकर सडक़ों पर रहता है। हम छत्तीसगढ़ में कई घटनाओं के बाद ऐसा तनाव देख चुके हैं। चूंकि हिन्दुओं को हिन्दुत्व के मुद्दे पर जगाने के काम में भाजपा के अलावा कांग्रेस भी पूरी ताकत से लगी हुई है, इसलिए अब ‘जागे हुए’ जरा से भी किसी गैरहिन्दू मुद्दे पर तुरंत ही उत्तेजित हो जाते हैं। इसलिए हिन्दूवादी पार्टियों और संगठनों की दशकों से फैलाई गई ‘हिन्दू चेतना’ को जब कांग्रेस ने भी बढ़ावा दिया है, तो अब इस नई बढ़ी हुई चेतना के चलते ध्रुवीकरण और अधिक रफ्तार से होने का एक नया खतरा सामने आया है। अब बहुसंख्यक धर्म के लोगों को भी अपने धर्म का अहसास पहले से बहुत अधिक होने लगा है, क्योंकि कांग्रेस भी रात-दिन राम-राम कर रही है।
देश में यह नई धार्मिक उत्तेजना चुनाव में किस पार्टी के कितने काम आएगी इसका कोई अंदाज हमें नहीं है, लेकिन ऐसी उत्तेजना से कौन से नए खतरे खड़े हो रहे हैं, उसका अंदाज लगाना बहुत मुश्किल भी नहीं है। ऐसा लगता है कि हिन्दुत्व को लेकर कांग्रेस कार्यसमिति के भीतर एक सावधानी की बात तो हुई है, भाजपा के जाल में फंसने से बचने की बात तो हुई है, लेकिन पार्टी के अपने आक्रामक हिन्दुत्व के लिए किसी लक्ष्मणरेखा की बात हुई हो ऐसा कम से कम खबरों में नहीं आया है, और अधिक संभावना इस बात की है कि ऐसी कोई चर्चा भी नहीं हुई होगी। यह बात इस देश की गौरवशाली धर्मनिरपेक्ष परंपराओं का हौसला पस्त करने वाली हो सकती है, लेकिन कांग्रेस शायद यह मान रही है कि धर्मनिरपेक्षता की अधिक चर्चा करना उसके लिए नुकसान की बात है। हम देश के राजनीतिक माहौल के बारे में कई तरह की सलाह दे सकते हैं, लेकिन जब बात कांग्रेस के चुनावी नफे-नुकसान की आती है, तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए हमसे अधिक समझदार है, और जिस देश में मुकाबला भाजपा जैसी पार्टी से हो, मोदी जैसे नेता से हो, वहां पर हमारी राय कांग्रेस या किसी और पार्टी के चुनावी फायदे की हो नहीं सकती। इसलिए क्या सही है और क्या गलत, इस पर चर्चा तो हम कर सकते हैं, अपने इस कॉलम में अक्सर ही करते हैं, लेकिन कौन सी बात किस पार्टी के फायदे की हो सकती है, उस पर चर्चा करना हमारे बस से परे की बात है। ऐसे में हम जनता से ही सीधे बात कर सकते हैं, कई राजनीतिक दलों को कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कांग्रेसी मेयर ने यह बताया है कि शहर के बीचोंबीच म्युनिसिपल की पुरानी बिल्डिंग की जगह पर 16 मंजिल इमारत बनाई जाएगी। यह इमारत कारोबारी होगी, और भी मनोरंजन के दूसरे कारोबार यहां चलेंगे। कहा गया है कि सौ करोड़ रूपए से ज्यादा की लागत से यह इमारत शहर के सबसे व्यस्त इलाके में बनाई जाएगी। यह इलाका आज इस कदर व्यस्त रहता है कि कहीं एक दुपहिया खड़ा करने की जगह नहीं रहती, और आसपास के चौराहे, सामने की सडक़ पर ट्रैफिक उफनते रहता है। दशकों से कई बार इस सडक़ पर गाडिय़ों को बंद करवाया गया, सडक़ के एक हिस्से में एक दिन और दूसरे हिस्से में दूसरे दिन ट्रैफिक किया गया, सौ तरह के प्रयोग करने के बाद भी यहां पर आना-जाना मुहाल रहता है। लेकिन चूंकि जगह म्युनिसिपल के पास है, इसलिए अब शहर के इस सबसे व्यस्त हिस्से में 16 मंजिल कारोबारी इमारत बनाने के लिए सौ करोड़ का कर्ज लेकर काम आगे बढ़ाने की योजना है। जाहिर है कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नेता, अफसर, और ठेकेदार, सबको बहुत सुहाता है।
हम ऐसे किसी एक मामले पर अधिक लिखना नहीं चाहते, क्योंकि अब सत्ता की पहुंच में जमीन का जो टुकड़ा है, उसके भयानक बाजारूकरण की बात आम हो गई है। ऐसे टेंडर, ऐसे ठेके, भयानक भ्रष्टाचार से भरे रहते हैं, और सत्ता को इससे ज्यादा कुछ पसंद नहीं आता। इसलिए न सिर्फ म्युनिसिपल, बल्कि सरकार के सभी विभाग और सभी निगम-मंडल, हर किसी में जमीनों के दोहन और शोषण का गलाकाट मुकाबला चलते रहता है, और हमने तो सरकार के ही दो हिस्सों में बाजारू संभावनाओं वाले जमीन के ऐसे टुकड़ों के लिए लड़ाई देखी है।
लेकिन आर्थिक भ्रष्टाचार हमारी आज की बात का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस जमीन पर न सही, किसी और जमीन पर, म्युनिसिपल न सही कोई और, भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत तो खड़ी होकर रहेगी, और उसे कोई रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इस जमीन को लेकर हमें यह फिक्र होती है कि क्या म्युनिसिपल और प्रदेश सरकार तमाम किस्म की कानूनी और सामाजिक जवाबदेही से परे हो चुकी हैं? इनकी नजरों में देश के कानून का, शहर की जरूरत का कोई भी सम्मान रह गया है या नहीं? शहर का सबसे व्यस्त इलाका जहां चारों तरफ कुछ किलोमीटर तक सिर्फ ट्रैफिक जाम रहता है, और शहर का सबसे बड़ा प्रदूषण जहां रहता है, वहां पर लाखों वर्गफीट का यह नया निर्माण बनाना किसकी जरूरत है? कम से कम इस शहर के फेंफड़े की जरूरत नहीं है, जनता की जरूरत नहीं है, और पैसों से लबालब भरे हुए, रात-दिन फिजूलखर्ची और बर्बादी करते हुए, तालाब पाटते, और मैदान काटते हुए म्युनिसिपल को तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस योजना को एक गौरव की तरह पेश किया जा रहा है, और मीडिया के मन में इसे लेकर बुनियादी जिम्मेदारी के कोई सवाल भी नहीं हैं।
किसी शहर में खुली हवा को बने रहने देना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसी कोई भी दैत्याकार फौलादी योजना सबसे पहले घने इलाके में सांस लेना और मुश्किल करेगी, लेकिन जब शहरीकरण के फैसले योजनाशास्त्रियों और विशेषज्ञों की जानकारी के बिना राजनेता करते हैं, और उन्हें मंजूरी उनके ऊपर बैठे हुए राजनेता देते हैं, तो सवाल उठता है कि इस देश में किसी भी विशेषज्ञता की क्या जरूरत है? हर प्रदेश में सत्तारूढ़ नेता, और निर्वाचित स्थानीय नेता अगर अपनी मर्जी से तमाम विशेषज्ञ फैसले ले सकते हैं, तो फिर स्वास्थ्य मंत्री को भी एमआरआई मशीन का इंतजार किए बिना अपने लैटरपैड पर कैंसर और दूसरी बीमारियों का इलाज लिखना चाहिए। शहर के सबसे घने इलाके में 16 मंजिल की यह निहायत गैरजरूरी इमारत भ्रष्टाचार, मनमानी, और शहर के फेंफड़ों में छेद करने वाली रहेगी, और चूंकि कोई जनसंगठन इस पर आवाज उठाने वाले नहीं हैं, और तकरीबन तमाम भ्रष्ट-निर्माणों पर चूंकि सत्ता और विपक्ष दोनों अघोषित रूप से भागीदार हो जाते हैं, इसलिए शहर के अब तक खाली बचे टुकड़ों का हिंसक बाजारूकरण एक आम बात हो गई है। हम छत्तीसगढ़ राज्य में इस एक राजधानी में ही कई दर्जन ऐसी खुली जगहों को देख रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल खुला रखना जरूरी है, लेकिन उनके आसपास के इलाकों का पर्यावरण अध्ययन करवाए बिना भी उन पर दानवाकार योजनाएं बनाई जा रही हैं, और शहर की बेहतरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जा रहा है।
मध्यप्रदेश के समय में हमने पढ़ा-सुना था कि इंदौर में कोई एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट पति-पत्नी सरकार की जनविरोधी नीतियों और योजनाओं के खिलाफ आवाज उठाते थे। अब अधिकतर प्रदेशों में यह मुमकिन इसलिए नहीं रह गया है कि अधिकतर आर्किटेक्ट या इंजीनियर सरकारी योजनाओं से जुड़े रहते हैं, और ऐसी आवाज उठाना उनके लिए हितों का टकराव रहेगा। फिर भी हमारा यह मानना है कि जनता के बीच से कुछ लोग ऐसे निकल सकते हैं जो कि हाईकोर्ट जाकर ऐसी योजनाओं के खिलाफ पीआईएल लगाएं, और उस पीआईएल के लिए मजबूत जमीन तैयार करने को पहले से ऐसी योजनाओं वाली सरकारी संस्थाओं को नोटिस भेजना शुरू करें, सूचना के अधिकार में जानकारी मांगें, और उनमें खामियां निकालकर, उन्हें जनहित के खिलाफ साबित करते हुए अदालत जाएं। निर्वाचित कुर्सियों पर अच्छे या बुरे कैसे लोग पांच बरस के लिए आते हैं, और उन्हें किसी शहर या प्रदेश को हमेशा के लिए बर्बाद करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ की इस राजधानी में राज्य सरकार का इंजीनियरिंग कॉलेज तो है ही, केन्द्र सरकार का एनआईटी भी है। हमारा यह भी मानना है कि बिना किसी राजनीतिक नीयत के सिर्फ छात्र-छात्राओं और प्राध्यापकों के ज्ञान और उनकी समझ के लिए इस शहर की तमाम सार्वजनिक खाली जगहों का एक अध्ययन होना चाहिए कि वहां शहर और समाज की भलाई में क्या बनना चाहिए, और क्या-क्या नहीं बनना चाहिए। वैसे तो राज्य सरकार अगर जिम्मेदार हो, तो उसे ऐसी किसी भी दैत्याकार और विनाशकारी सोच के पहले जानकारों से राय लेनी चाहिए। इस देश के आईआईटी और आईआईएम के लोग पूरी दुनिया में जाकर वहां की सबसे कामयाब कंपनियां चलाते हैं, लेकिन लगता है कि हिन्दुस्तान को उनकी विशेषज्ञता की कोई जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के बाद से अब तक खनिज कमाई की वजह से इसमें जरूरत से ज्यादा पैसा रहा, और राजधानी बन गए इस शहर में जरूरत से अधिक भ्रष्ट योजनाएं बनती ही रहीं। अब यह समय आ गया है कि जागरूक लोगें के किसी जानकार संगठन को जिनका कि सरकार से कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें सार्वजनिक हित के ऐसे मुद्दों पर सरकार के सामने विरोध दर्ज करना चाहिए, और फिर जैसी कि उम्मीद है, उसके अनसुने रहने पर अदालत जाना चाहिए। किसी भी शहर या प्रदेश के लोग अपनी आने वाली पीढिय़ों को दमघोंटने वाला धुआं विरासत में देकर जाएं, तो उन्हें 25-50 बरस बाद लिखे जाने वाले इतिहास में गैरजिम्मेदार मुजरिम ही लिखा जाएगा। जब लोगों के पास शिकायत करने और अदालत तक जाने का विकल्प है, तब तक सत्ता की ऐसी दानवाकार मनमानी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।
‘इंडिया’ गठबंधन के एंकर-बहिष्कार की खबर देश के मीडिया की सबसे बड़ी खबर है। इस पर कल हम अपने यूट्यूब चैनल पर खासा बोल चुके हैं, लेकिन अखबार पढऩे वाले लोगों के लिए इस पर लिखना भी जरूरी है। देश के टीवी-समाचार उद्योग ने इस विपक्षी बहिष्कार को लोकतंत्र पर हमला कहा है, और इसकी निंदा की है। लोकतंत्र में किसी भी नागरिक की तरह टीवी-समाचार उद्योग को भी यह हक है कि वह अपना धंधा अपनी मर्जी से चलाए, और जब सरकार उस पर मेहरबान रहे, सरकार का चेहरा देखकर चलने वाला कारोबार उस पर मेहरबान रहे, तो फिर उसे विपक्ष की कोई फिक्र होनी भी क्यों चाहिए? आज ऐसा लगता है कि जिन 14 नामी-गिरामी (?) एंकरों का सार्वजनिक बहिष्कार किया गया है, वे एक तरफ तो विपक्ष के इस फैसले का विरोध करते हुए अपने आपको पत्रकार साबित करने में भी लग गए हैं, इसके अलावा सत्ता के साथ अपनी बातचीत में वे इसे अपनी शहादत का सुबूत भी बता रहे होंगे कि सत्ता का साथ देने की वजह से उनकी कुर्बानी दी जा रही है। टीवी-समाचारों के बहुत से लोगों को यह मलाल हो रहा होगा कि इस फेहरिस्त में उनका नाम नहीं है जबकि वे भी पूरी ताकत से नफरत फैलाने में लगे रहते हैं, वे भी आपस में और विपक्ष के दोस्तों से यह सवाल पूछ रहे होंगे कि उनकी तपस्या में क्या कमी रह गई थी?
यह बहिष्कार इसलिए हुआ है कि ये कुख्यात एंकर लगातार नफरत की बातें फैला रहे थे, सरकार के पक्ष में, और विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए एक एजेंडा चला रहे थे, पड़ोसी पाकिस्तान के साथ युद्धोन्माद का एक एजेंडा बढ़ा रहे थे, देश के भीतर अलग-अलग तबकों के बीच बहुत बुरी तरह टुकड़े-टुकड़े कर रहे थे। इनका बहिष्कार काफी पहले से कर दिया जाना चाहिए था, पता नहीं राजनीतिक दलों को इस फैसले पर पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा। दूसरी तरफ यह बड़ा और कड़ा फैसला ‘इंडिया’ की मजबूती की एक और परख रहा कि 26 पार्टियों ने यह फैसला लिया है। हमारे हिसाब से बिना गठबंधन बने भी ऐसे किसी मुद्दे पर विपक्ष को एक साथ होना चाहिए था क्योंकि देश के टीवी-समाचार मीडिया का जितना संगठित कार्यक्रम विपक्ष को नीचा दिखाने का चल रहा था, उसका एक अहिंसक विरोध पहले ही होना था। जो समाचार-टीवी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से 9 बरस में भी एक सवाल भी नहीं कर पाए, सत्ता से असुविधा के कोई सवाल करने की जिनकी हिम्मत नहीं है, वे सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के एक प्रकोष्ठ की तरह विपक्ष पर टूटे पड़े रहते हैं, इसलिए विपक्षी पार्टियों को पहले ही ऐसी संगठित साजिश का शिकार बनने से इंकार कर देना था।
हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम इसी जगह लगातार यह बात लिखते आए हैं कि देश के अखबारों को अपने पुराने नाम, प्रेस, पर लौट जाना चाहिए, और देश की आज की मीडिया नाम की विशाल छतरी के नीचे से हट जाना चाहिए। अखबारों और टीवी-समाचारों का चरित्र बिल्कुल अलग है, काम के तौर-तरीके, रीति-नीति, परंपराएं, सब कुछ एकदम अलग है। ऐसे में सबको एक साथ मीडिया बुलाया जाना अखबारों की इज्जत के खिलाफ है जिनके बीच कुछ अखबार जरूर गोदी मीडिया का दर्जा पा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से अखबार ईमानदारी से निकलते हैं। अखबारों का मिजाज ऐसा है कि वहां ईमानदार बने रहने की संभावना कुछ हद तक तो चलती है। एक वक्त था जब अखबारों को प्रेस नाम से ही जाना जाता था, और आज फिर उसी चीज की पहल करनी चाहिए। कल टीवी-समाचार उद्योग के संगठन का जो बयान सामने आया, जिसमें विपक्ष के बहिष्कार के फैसले को अलोकतांत्रिक बताया गया, और चैनलों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ कहा गया, वह बयान अपने आपमें इस बात का सुबूत है कि टीवी-समाचार उद्योग जिस हद तक लोकतंत्र-विरोधी हो चुका है, साम्प्रदायिक हो चुका है, उसका एजेंडा जिस तरह युद्धोन्मादी है, उसने इनमें से किसी भी बात की परवाह नहीं की है, और न इनमें से किसी बात को माना है। ऐसे में जिस तरह देश के और कोई भी कारोबारी संगठन अपने लोगों को बचाने के लिए एकजुट रहते हैं, उसी तरह की एकजुटता टीवी-समाचार उद्योग में दिख रही है। इसका पत्रकारिता के किसी नीति-सिद्धांत से कोई लेना-देना नहीं है, और न ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। आज जब देश का सुप्रीम कोर्ट बार-बार यह कह रहा है कि टीवी किस तरह एक तनाव खड़ा कर रहे हैं, बार-बार चेतावनी दे रहा है, तो उस पर ऐसे एसोसिएशन ने कुछ भी नहीं किया। आज जब दर्जन भर से अधिक लोगों के बहिष्कार का गांधीवादी फैसला लिया गया है, तो उसे टीवी-समाचार उद्योग ज्यादती करार दे रहा है।
हमारा यह मानना है कि न सिर्फ टीवी, बल्कि अखबारों में भी, वेबसाइटों पर भी जो लोग लगातार और स्थाई रूप से बेईमानी करते हैं, उनसे बात करने से लोगों को मना करना चाहिए। ऐसा बहिष्कार किसी भी तरह से उन माध्यमों के किसी अधिकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि लोगों के अपने अधिकारों के तहत लिया गया फैसला है। आज अगर कहीं पर कोई शराब पार्टी होती है, और किसी व्यक्ति को शराबियों के बीच बैठने से परहेज है, और वह उस न्यौते पर वहां जाने से इंकार कर देता है, तो यह शराबियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला नहीं है। ‘इंडिया’ गठबंधन ने न तो और लोगों से इन एंकरों की बहिष्कार की बात कही है, और न ही इन एंकरों के चैनलों का अभी बहिष्कार किया है। यह इन पार्टियों का बुनियादी हक है कि वे किन कार्यक्रमों में जाएं, और किनमें नहीं। कल के दिन वे कुछ चैनलों का भी बहिष्कार करते हैं, तो भी वह अलोकतांत्रिक नहीं होगा। हमारा तो यह मानना है कि देश में लगातार साम्प्रदायिक हिंसा भडक़ाने में लगे हुए कुछ ऐसे चैनल हैं जिनका पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए, जो कि ‘इंडिया’ गठबंधन ने अभी नहीं किया है। ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने वाले चैनलों पर कोई भी कार्रवाई करना नहीं चाहती है, जबकि उसके कानून बहुत कड़े बने हुए हैं। ऐसे में लोगों की उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है कि वह सीधे-सीधे इन चैनलों के लाइसेंस कैंसल करे, इनके प्रसारण पर रोक लगाए, इनकी सम्पत्ति जब्त करके साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार लोगों के बीच बांटे। लोकतंत्र के तहत अगर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, तो उसका मतलब उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल लोकतंत्र को खत्म करना नहीं हो सकता। यह बात एकदम ही साफ रहनी चाहिए कि इस तरह के जितने अधिकार हैं ये लोकतंत्र रहने तक ही हैं, और अगर इनका इस्तेमाल समाज में नफरत फैलाने में किया जा रहा है, देश की राजनीति में एक झूठा संतुलन दिखाने में किया जा रहा है, तो किसी गठबंधन से परे देश के कानून को भी इसका नोटिस लेना चाहिए।
दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लडऩे पर रोक की एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, और उसके नियुक्त किए गए न्यायमित्र वकील विजय हंसारिया ने कोर्ट को सुझाया है कि अदालत से सजा पाने पर सिर्फ एक सीमित समय के लिए चुनावी रोक को ताउम्र करना चाहिए। उन्होंने अदालत को कहा है कि चुनाव लडऩे की अयोग्यता को सीमित करने का कानून संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए समानता के अधिकार के खिलाफ है। अदालत में यह जनहित याचिका ऐसे बहुत से दूसरे मामले दायर करने वाले एक चर्चित वकील अश्वनी उपाध्याय ने लगाई हुई है, इस याचिका में एमपी-एमएलए के आपराधिक मुकदमों की जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। अदालत ने अपनी मदद के लिए एक सीनियर वकील विजय हंसारिया को न्यायमित्र बनाया है जो कि इस मामले में जजों को अपनी राय देते रहते हैं, उनके माध्यम से जजों को इस मुद्दे को बेहतर समझने में आसानी होती है। वे इस मामले में डेढ़ दर्जन से ज्यादा रिपोर्ट दे चुके हैं, और अभी उन्होंने देश भर में एमपी-एमएलए अदालतों में चल रहे मामलों का अध्ययन करके बताया है कि इन मामलों में होने वाली प्रगति की रिपोर्ट हर महीने हाईकोर्ट में जमा होनी चाहिए, और हाईकोर्ट यह निगरानी करें कि सुनवाई तेजी से हो। आज इस वक्त सुप्रीम में इस मामले की सुनवाई चल रही होगी, लेकिन हम अदालत के रूख को जाने बिना इस मुद्दे पर अपनी राय लिख रहे हैं।
हिन्दुस्तान की राजनीति जुर्म से इस बुरी तरह लदी हुई है कि सांसदों-विधायकों के जुर्म पर अगर कोई कड़ी रोक लगाई जाए तो उसका समर्थन करना चाहिए। अब इस रोक को लगाते हुए यह भी याद रखना होगा कि कुछ लोगों को यह सांसदों और विधायकों के संवैधानिक या लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ लगेगा। हमारा यह मानना है कि भ्रष्टाचार या किसी संगीन जुर्म के मामलों में तो जिंदगी भर की रोक लगाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर किसी सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान कोई जुर्म दर्ज होता है, या कि राहुल गांधी किस्म के किसी मानहानि मामले में कोई सजा होती है, तो उसमें जिंदगी भर चुनाव लडऩे पर रोक जायज नहीं होगी। हत्या, बलात्कार, संगठित व्यापक भ्रष्टाचार, सरकारी ओहदे का बेजा इस्तेमाल, मनी लॉंड्रिंग जैसे मामलों में जिंदगी भर की रोक लगाना नाजायज नहीं होगा। अगर भारतीय लोकतंत्र से मुजरिमों को कम करना है, तो कड़ी कार्रवाई के बिना यह मुमकिन नहीं है। आज तो यह जाहिर तौर पर दिखता है कि जो बलात्कारी दिख रहे हैं, उनका भी देश की विधानसभाओं और संसद में सम्मान होता है, और वे आज भी एक सांसद के विशेषाधिकार भंग होने के हक के हकदार बने हुए हैं।
संगीन जुर्म के मुजरिमों पर अगर जिंदगी भर चुनाव लडऩे पर रोक लगती है, तो उससे भी वे अपनी पार्टी के नेता तो बने ही रह सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई कानूनी रोक नहीं है कि सजायाफ्ता लोग राजनीतिक दलों में न रहें। यह पार्टियों की अपनी पसंद है कि वे कितने मुजरिम अपने पर लादना चाहती है, अपनी गोद और अपने सिर पर बिठाना चाहती है। अभी इस समाचार को हम देख रहे हैं तो न्यायमित्र ने अदालत को बताया है कि बलात्कार, ड्रग्स, या आतंकी गतिविधियों या भ्रष्टाचार के मामलों में भी सजा होने पर चुनाव लडऩे पर रोक रिहाई के बाद कुल 6 साल के लिए है। ऐसे मामलों की शिनाख्त की जानी चाहिए, जुर्म की कुछ धाराओं को तय करना चाहिए, और गंभीरता के आधार पर इस रोक को आजीवन किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास ऐसे संगीन जुर्म के बाद चुनाव लडऩे से परे और भी बहुत काम हो सकते हैं, और पार्टियों के पास भी अपने चहेते और पसंदीदा मुजरिमों के अलावा और बहुत से लोग चुनाव लडऩे लायक हो सकते हैं। हर पार्टी को अपने गैरमुजरिमों को मौका देना चाहिए, क्योंकि पार्टी के नेताओं और सदस्यों में से चुनाव लडऩे के मौके तो गिने-चुने लोगों को ही मिल पाते हैं। जिस व्यक्ति को एक बार कोई संगीन जुर्म करने की फुर्सत रहती है, उसे चुनाव न लड़ाकर कुछ और वक्त देना चाहिए ताकि वे लोग दूसरे काम कर सकें, और चाहें तो कोई और जुर्म भी कर सकें। इस बात को पार्टियों से परे मुजरिमों की निजी जिंदगी तक भी ले जाना चाहिए कि वे निर्दलीय उम्मीदवार होकर भी चुनाव न लड़ सकें।
अभी अदालत में चल रही इस याचिका की सारी संभावनाएं हमें ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के नियम भी ऐसे बनाने चाहिए कि ऐसे सजायाफ्ता लोग उसके ओहदों पर न रह सकें। अभी शायद ऐसी रोक नहीं है। सजायाफ्ता मुजरिमों पर रोक बढऩी चाहिए। और अगर वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो ऐसी सजा के बाद उन्हें संसद या विधानसभाओं से मिलने वाली पेंशन भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि जुर्म की कमाई अगर उनकी बाकी जिंदगी के लिए काफी है, तो जनता का पैसा उन पर क्यों बर्बाद किया जाए। हमने देश के अलग-अलग हिस्सों से, खासकर उत्तर भारत से ऐसे गैंगस्टरों के मामले अभी देखे हैं जो अलग-अलग कई पार्टियों से चुनाव लडक़र संसद और विधानसभाओं में पहुंचते रहे। उनका जुर्म का साम्राज्य देखकर लगता है कि उन्हें मुम्बई में दाऊद के मुकाबले कोई गिरोह चलाना था। लेकिन ऐसे लोग अलग-अलग पार्टियों से अलग-अलग वक्त पर सांसद और विधायक बनते रहे हैं। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। राजनीति का आपराधिकरण बढ़ते-बढ़ते अपराध का राजनीतिकरण हो चुका है। अधिकतर पार्टियों को अपने ताकतवर, जीतने वाले, और इलाकों में दबदबा रखने वाले मुजरिमों से कोई परहेज नहीं दिखता। इसलिए अदालत को ही दखल देकर चुनावी पात्रता, और पार्टियों में ओहदों पर रोक लगानी होगी। यह किस तरह के जुर्म पर किस सीमा तक लगे, यह आगे बहस के लायक है, और यह जाहिर भी है कि अदालत में तमाम पहलू सामने आएंगे, हमने तो आज इस मुद्दे पर सिर्फ अपनी मामूली समझ सामने रखी है, जो कि अब तक की जानकारी पर आधारित है।
आज हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है, और लोगों की भावनाएं सोशल मीडिया पर बिखर रही हैं। शायद स्कूल-कॉलेज में इस मौके पर हिन्दी के गुणगान के बहुत से कार्यक्रम होंगे, और अखबारों में पूरे-पूरे पन्ने हिन्दी की सेवा, हिन्दी की महिमा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा जैसी शब्दावली के साथ छपे हैं। भाषा को लेकर साल में एक दिन भावनात्मक होने के बाद अगले दिन से अधिकतर लोग उस भाषा के मनचाहे इस्तेमाल में जुट जाते हैं जिनमें हो सकता है कि भाषा के गर्व के लायक कुछ न हो। सोशल मीडिया पर इसी हिन्दी का इस्तेमाल करके जब महिलाओं का चरित्र हनन किया जाता है, बलात्कार और कत्ल की धमकी दी जाती है, जब क्रिकेट खिलाडिय़ों के बच्चों से बलात्कार की बातें लिखी जाती हैं, जब साम्प्रदायिक नफरत के तमाम बुलबुले हिन्दी में ही बने रहते हैं, और उफनते रहते हैं, तो वह किसी भाषा के मूल्यांकन का अधिक सही मौका रहता है। हिन्दी की सेवा करने वाले लोग सेवा की बात करते हुए अमूमन सरकारी या किसी संस्था के मेवे पर नजर रखते दिखते हैं कि किसी कार्यक्रम में मौका मिल जाए, और भाषा की साख बाकी लोगों की हरकतों से चौपट होती रहती है।
हिन्दी को मातृभाषा बताने वाले लोग इसकी कितनी सेवा करते हैं यह उन मौकों पर साबित होता है जब वे मां-बहन की गालियां इसी भाषा में देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आपकी मातृभाषा वही होती है जो कि आप सडक़ पर गाली बकने की हसरत रहने पर मन के भीतर, या कई बार जुबान से भी, दूसरों को देते हैं। किसी भाषा का गौरव इन दिनों दुनिया की सडक़ और उसका फुटपाथ बने हुए सोशल मीडिया पर तय होते चलता है जहां किसी भाषा में उसे भी सही न लिखने वाले लोग नफरत का सैलाब फैलाते चलते हैं। फिर भाषा का गौरव तय होने की कुछ और जगहें भी रहती हैं। जब कुछ नेताओं, अफसरों, शराब कारोबारी-समाजसेवियों, पत्रकारों के सम्मान और अभिनंदन में एक अनोखी शब्दावली का इस्तेमाल होता है। ऐसे-ऐसे विशेषणों का इस्तेमाल होता है जिन पर खुद सम्मान के पात्र को भरोसा न हो, खुद उसे लगे कि यह तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो भाषा के वैसे इस्तेमाल से भी भाषा का सम्मान तय होता है। तथाकथित पढ़े-लिखे, और तथाकथित जागरूक लोगों की जुबान से जब समाज के कमजोर लोगों, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों, आरक्षित वर्ग के लोगों, और वकील न कर पाने वाले जानवरों के लिए अपमान की बातें निकलती हैं, तो उससे भी उनकी भाषा का सम्मान तय होता है।
इस तरह किसी भाषा का कोई दिन मनाना एक किस्म का पाखंड है, अगर उस भाषा के सम्मान और उसकी सेवा का दावा करने वाले लोग उस भाषा में चल रहे भाषा के अन्याय, और उस भाषा के हिंसक इस्तेमाल के खिलाफ आवाज न उठाएं। किसी भाषा में, सौ फीसदी शुद्धता के साथ मां-बहन की गाली दी जा सकती है, तो क्या उससे भाषा की शुद्धता का सम्मान बढ़ जाता है, किसी भाषा में दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को काटकर फेंक देने के फतवे दिए जा सकते हैं, और उनका व्याकरण सही भी हो सकता है, लेकिन क्या उससे भाषा का सम्मान बढ़ता है? ऐसे हजार सवाल हैं। हमारा यह देखा हुआ है कि हिन्दी भाषा में सैकड़ों बरस से चले आ रहे कहावत-मुहावरों में सामाजिक अन्याय भरा पड़ा है, हिंसा ही हिंसा है, घोर जातिवाद है जो कि मनुवाद के मुताबिक तय किया गया है, लेकिन इसके खिलाफ कोई सोच आंदोलन नहीं बन पाती हैं। आज भी जब लोग इसकी सेवा करने, और इसे मां बताने में लगे हुए हैं, तब भी भाषा को लेकर सामाजिक चेतना और जागरूकता पर कोई चर्चा नहीं होती। जब तक भाषा की हिंसा पर बात नहीं होगी, भाषा में गहरे बैठी हुई सामाजिक असमानता पर बात नहीं होगी, क्या भाषा का कोई सम्मान हो सकता है? ऐसे पढ़े-लिखे लोग भी भला किस काम के जो कि अपनी पसंदीदा भाषा की हिंसा को मानने, और फिर उसे हटाने में दिलचस्पी न रखते हों? ऐसे लोग नवरात्रि के नौ दिनों में देवीपूजा के बाद असल जिंदगी में कन्या भ्रूण हत्या करने वाले लोग सरीखे होते हैं। ऐसे लोगों से तो वे अनपढ़ लोग बेहतर हैं जिन पर किसी भाषा की हिंसा हटाने की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। अपने आपको भाषा का सेवक कहने वाले लोग, उस भाषा के प्रेमी, मातृभाषा की संतान बनने वाले लोग अगर उस भाषा में भरे हुए कलंक को हटाने में दिलचस्पी नहीं रखते, तो वे उस भाषा का कोई भला नहीं करते, वे सिर्फ एक सालाना पाखंड करते हैं।
आज हिन्दुस्तान के तथाकथित हिन्दी प्रेमियों के बीच अंग्रेजी को लेकर सबसे अधिक चिढ़ या जलन दिखती है कि अदालत, सरकार, और उच्च शिक्षा से लेकर कारोबार तक अंग्रेजी का बोलबाला है। अब तो अंग्रेजों को कोसना बंद हो जाना चाहिए क्योंकि आजादी मिले पौन सदी हो चुकी है। इस दौरान अगर हिन्दी भाषा को चाहने वाले लोगों ने अपने आपको दुनिया के मुकाबले तैयार नहीं किया है, तो इसकी कोई तोहमत हिन्दी पर तो डाली नहीं जा सकती। हिन्दी का इस्तेमाल करने वाले लोग इसे बढ़ाने की बात को एक नारे की तरह तो लगाते हैं, लेकिन फिर पूरी दुनिया की संभावनाओं को देखते हुए अंग्रेजी की तरफ बढ़ जाते हैं। सत्ता चला रहे लोगों को यह मालूम है कि आज अंतरराष्ट्रीय संपर्क की भाषा अंग्रेजी है, कम्प्यूटरों पर काम, विज्ञान और टेक्नालॉजी की भाषा अंग्रेजी है। जिस तरह दुनिया के बहुत से गैरअंग्रेजी देश अपनी भाषाओं में हर काम करने लगे हैं, उस तरह का हिन्दुस्तान में मुमकिन इसलिए नहीं है कि हिन्दी इस देश की ही अकेली भाषा नहीं है। इस देश में हिन्दीभाषियों के मुकाबले गैरहिन्दीभाषी आबादी अधिक कामयाब है, वह कारोबार में, उच्च शिक्षा और विज्ञान में अधिक सफल है। बाहर की दुनिया में जाकर कामयाब होना भी हिन्दी वालों के मुकाबले गैरहिन्दी वालों के लिए अधिक आसान है क्योंकि उनके मन में अंग्रेजी के लिए वैसी कोई नफरत नहीं है जैसी कि बहुत से कट्टर हिन्दीप्रेमियों के मन में रहती है। नतीजा यह निकलता है कि हिन्दीभाषी लोग अपनी भाषा की सीमित संभावना को थामकर बैठे हैं, उसकी शुद्धता के लिए उतने ही कट्टर हुए बैठे हैं जैसी कट्टरता शुद्धता को लेकर हिटलर की थी, और इसीलिए दुनिया में ऐसे शुद्धतावादियों के लिए एक शब्द लिखा जाने लगा है, ग्रामर-नाज़ी। रक्त शुद्धता के दुराग्रही लोगों की तरह लोग भाषा शुद्धता पर भी उतारू रहते हैं, और उन्हें यह समझ ही नहीं पड़ता कि हर बरस दुनिया भर के अलग-अलग भाषाओं के हजारों शब्दों को अपनी डिक्शनरी में मिला लेने वाली अंग्रेजी कहां से कहां पहुंच गई है।
आज अगर अंतरराष्ट्रीय संबंध और कारोबार, विज्ञान और टेक्नॉलॉजी, उच्च शिक्षा और राजनीति की भाषा अगर अंग्रेजी रह गई है, तो हिन्दी पर टिके रहने की जिद कई पीढिय़ों की संभावनाओं को खत्म कर चुकी है, और करती रहेगी। लोगों को भाषा की सेवा करने की जिद छोड़ देनी चाहिए, भाषा को किसी सेवा की जरूरत नहीं रहती। वह महज एक औजार रहती है, और उसमें लिखी किताब को अगर नोबल पुरस्कार मिलता है, तो उसका सम्मान बढ़ता है, और उसमें लिखी सोशल मीडिया पोस्ट पर अगर मां-बहन की गालियां लिखी जाती हैं, तो ऐसी मातृभाषा का भी सम्मान खत्म होता है। जिनको मातृभाषा की सेवा करने की जिद है, उन्हें अपनी भाषा से हिंसा और बेइंसाफी को खत्म करने के लिए सार्वजनिक रूप से, सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आना होगा, वरना मातृभाषा को मां-बहन की गालियां पड़ती रहेंगी।
राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध इन्हें लेकर कोई भी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं रहता। इन दोनों की अजीब खूबियां और खामियां रहती हैं, और हैरतअंगेज हमबिस्तर बनते रहते हैं। अब यह किसने सोचा था कि सोते-उठते जो बाल ठाकरे कांग्रेस को गालियां देते थे, उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाएगी। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के मुद्दे पर कांग्रेस छोडऩे वाले एनसीपी के नेता कांग्रेस के करीबी हो जाएंगे। ऐसे ही अभी जब अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन वियतनाम पहुंचे, और वियतनामी राष्ट्रपति वो वान थुओंग के साथ उन्होंने बड़े रणनीतिक समझौते पर दस्तखत किया तो लोगों को याद आया कि अमरीका के साथ सबसे लंबी जंग तो इसी वियतनाम की हुई थी, इसी वियतनाम को अमरीकी फौजों ने बरसों तक रौंदा था, उस दौरान वियतनाम चीन के करीब था, और आज अमरीका और वियतनाम का यह रणनीतिक समझौता एक किस्म से चीन की फौजी ताकत के मुकाबले खड़े किए जा रहे एक अमरीकी मोर्चे का हिस्सा है। आज की पीढ़ी को यह बात याद नहीं होगी कि किस तरह 1954 से 1975 तक वियतनाम पर अमरीकी हमला हुआ था और अमरीका ने इसे वियतनाम के उत्तर और दक्षिण हिस्सों के बीच जंग की तरह दिखाया था। वियतनामी जमीन पर इन दोनों हिस्सों के पीछे चीन और अमरीका थे। बीस बरस चली इस जंग के बाद वियतनामी समाज में एक ऐसी पूरी पीढ़ी ही खड़ी हो गई थी जो कि वियतनामी लड़कियों से अमरीकी सैनिकों के जबर्दस्ती या मर्जी के रिश्तों से पैदा हुई थी। लोगों को याद होगा कि वियतनाम युद्ध की वह भयानक तस्वीर अमरीकी नापाम बम के हमले से बिना कपड़ों के भागती हुई बच्ची की थी। लेकिन उन तमाम यादों से उबरकर आज अमरीका और वियतनाम के बीच यह ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसी तरह हिन्दुस्तानी राजनीति में कई ऐसे समझौते हो रहे हैं, होते रहते हैं जिन्हें कहने वाले अनैतिक कह सकते हैं, लेकिन वे सत्ता पर आने के लिए, सत्ता पर काबिज रहने के लिए किए जाते हैं, और उनके साथ किसी तरह की नैतिकता जुड़ी नहीं रह गई है। नैतिकता दरअसल भारतीय राजनीति, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जंजीरों से बांधकर पीछे के कमरे में कैद कर दी गई है।
अमरीकी राष्ट्रपति अभी जी-20 सम्मेलन में दिल्ली आए, तो कई दिनों तक यह खबर रही कि वे भारत में मीडिया के सवालों का जवाब देना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने इससे पूरी तरह असहमति जताई, और ऐसे सवाल-जवाब नहीं हो पाए। इसके तुरंत बाद यह खबर भी आई कि जो बाइडन वियतनाम पहुंचते ही मीडिया से बात करेंगे, जो कि किसी भी पश्चिमी या विकसित लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य बात सरीखी है। मीडिया से लगातार और बार-बार बात करना ही लोकतंत्र के जिंदा होने का पहला संकेत माना जाता है। भारत सरकार की तरफ से अमरीकी सरकार की कही गई बातों का कोई खंडन भी नहीं किया गया कि उसने जो बाइडन को मीडिया से बात करने से नहीं रोका था। ऐसे में यही माना जाना चाहिए कि खबरें सही थीं, और पहला मौका लगते ही हनोई पहुंचते ही उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया जिनमें भारत में मीडिया की आजादी, और दूसरे कई किस्म की स्वतंत्रता के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इन मुद्दों पर बात की है, जैसी कि वे दुनिया में सभी जगह करते हैं। दूसरी तरफ अमरीका की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि उसने वियतनाम के दौरे के बाद जो बयान जारी किया है उसके 26 सौ शब्दों में कुल 112 शब्द वियतनाम में मानवाधिकारों के बारे में हैं। वियतनाम में मानवाधिकार का बुरा हाल बताया जाता है, और वहां सरकार के आलोचकों को धमकी, प्रताडऩा, और जेल तक का सामना करना पड़ता है। हर किस्म के मीडिया पर सरकार का काबू है, लेकिन जो बाइडन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। जाहिर तौर पर इसलिए कि वियतनाम से समझौते के बाद अमरीका चीन के एक सबसे करीबी रहे देश के साथ भागीदारी कर रहा है, और चीन के एकदम पड़ोस में भी पहुंच गया है। दुनिया के इस हिस्से में यह एक फौजी कामयाबी है, और इसे नैतिकता के किसी भी पैमाने की वजह से नहीं रोका जाता।
हमने कुछ अरसा पहले यह लिखा भी था कि देशों के विदेश मंत्रालयों में बाहर एक तख्ती लगी रहती है कि नैतिकता बाहर छोडक़र आएं। वही होता भी है। जिस यूक्रेन को बड़ी उम्मीद थी कि जी-20 सम्मेलन में उस पर रूसी हमले के खिलाफ कोई मजबूत बात होगी, उसने अपनी निराशा जाहिर की है, लेकिन उस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। देश, जिनमें चीन से लेकर अमरीका तक शामिल हैं, उनमें से कोई भी अभी यूक्रेन के साथ जी-20 के बयान में नहीं थे। जबकि अमरीका नाटो के हिस्सेदार के रूप में रूस के खिलाफ हमलावर है, और चीन अंतरराष्ट्रीय मंच पर रूस का हिमायती माना जा रहा है। लेकिन जी-20 जैसे कोई भी दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन देशों के बीच की जमीनी हकीकत किसी भी नैतिकता को दूर रखती है।
ठीक ऐसे ही भारत जैसे देश की राजनीति को देखें तो पार्टियों और नेताओं को अपनी नैतिकता, नीति और सिद्धांत, गठबंधन की बैठकों में बाहर रखकर आने के लिए कहा जाता है। कल के दुश्मन आज दोस्त हो जाते हैं, और आज के दोस्त कल दुश्मन। इसीलिए कुछ समझदार लोग कहते हैं कि नेताओं के कार्यकर्ताओं को आपसी रिश्ते बर्बाद नहीं करने चाहिए क्योंकि उनके बीच गठबंधन तो कभी भी हो जाते हैं, और कार्यकर्ता कटुता ढोते रह जाते हैं। भारत में आज इंडिया नाम के विपक्षी गठबंधन की सीटों पर तालमेल की पहली बैठक है। यहीं से इस गठबंधन की अग्निपरीक्षा शुरू होने जा रही है, क्योंकि बंदरगाह पर बंधे जहाज तो हर जगह महफूज दिखते हैं, जब समंदर की लहरों और तूफानों से उनका सामना होता है, तभी उनकी मजबूती पता लगती है। ‘इंडिया’ की मजबूती और उसकी संभावनाएं आज की इस बैठक के बाद ही परखना शुरू होगा, और आज से ही इस गठबंधन में दरार पडऩे का एक खतरा भी खड़ा हो सकता है। एक साथ बैठकर लंच और डिनर करना अलग बात होती है, उसमें तो कांग्रेस और केजरीवाल सब भाई-भाई दिखते रहे, आज जब चुनावी सीटों के बीच बंटवारे की बात आएगी, तो हो सकता है कि सुई की नोंक जितनी जमीन देने के बजाय महाभारत शुरू हो जाए। आगे-आगे देखें होता है क्या।
सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी या उसके ऊपर के अफसर के खिलाफ कोई जुर्म कायम करने या कार्रवाई करने के लिए उसे सरकार से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। पहले सरकार में बैठे बड़े अफसरों ने अपने-आपको सीधी कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए इस तरह की व्यवस्था करवा रखी थी, और अभी आए इस फैसले में पांच जजों की बेंच ने यह साफ किया है कि 2003 में दिए गए ऐसे आदेश के बाद कार्रवाई से बचे हुए तमाम लोगों पर भी यह अदालती फैसला लागू होगा। इस तरह यह कड़ा फैसला न सिर्फ अफसरों से एक नाजायज हिफाजत छीन रहा है बल्कि सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के हाथ मजबूत कर रहा है। अफसरों ने सरकार से अपने लिए ऐसी हिफाजत का नियम 2003 में करवा लिया था, वही रद्द कर दिया गया है।
हम सिर्फ इस फैसले को लेकर लिखना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि सरकारों के भीतर अपने पसंदीदा लोगों के भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह का व्यापक और मजबूत बर्दाश्त आम हो चला है, उसके खिलाफ लिखना चाह रहे हैं। आज चारों तरफ केंद्र से लेकर प्रदेश सरकारों तक, और स्थानीय संस्थाओं से लेकर अद्र्धशासकीय संस्थाओं तक सत्ता के मन में अपने चहेते भ्रष्ट लोगों के लिए इतनी मोहब्बत है जितनी कि अनारकली के लिए सलीम के दिल में भी नहीं थी। जब हजारों में से दो-चार मामले उजागर हो ही जाते हैं, और संसद या विधानसभा में सरकार को मजबूरी में जांच के लिए हामी भरनी पड़ती है, या किसी अदालती आदेश से जांच करवानी पड़ती है, तो सरकारें अपने चहेते भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने पर आमादा दिखती हैं। यह जगह-जगह देखने में आता है कि जो पूरी तरह भ्रष्ट लोग हैं, उनको बचाने के लिए सरकारें जांच एजेंसियों के साथ मिलकर साजिश करती हैं, मामलों को कमजोर करती हैं, और भ्रष्ट अफसरों को ऊंची से ऊंची कुर्सियों पर बैठाती हैं, और उन्हें रिटायर होने के बाद भी तमाम नियमों को तोड़ते हुए फिर तरह-तरह से कुर्सी पर बनाए रखती है। केंद्र सरकार का काम करने का तरीका राज्यों से कुछ अलग रहता है, वहां पारदर्शिता और कम रहती है, और वहां नीतिगत फैसलों में चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के काम उतनी जल्दी उजागर नहीं होते, जितनी जल्दी राज्यों में सामने आ जाते हैं। शायद भारत सरकार के काम में पारदर्शिता उतनी अधिक नहीं रहती है जितनी राज्यों में रहती है। अभी जिस दर्जे के अफसरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने अपने-आपको आम सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के ऊपर एक अलग दर्जा बनाकर उसमें हिफाजत से बिठा रखा था, यह सवर्ण किस्म की सोच भी इस फैसले से खत्म होती है।
हमारा तो अनुभव यह भी रहा है कि सरकार के परले दर्जे के संगठित भ्रष्टाचार की साजिश में शामिल मुजरिम अफसरों पर मुकदमे की नौबत जब आ भी जाती है, तब भी सरकार मुकदमे की इजाजत देने से कन्नी काटते रहती हैं, और भ्रष्ट अफसर की जिंदगी पहले खत्म हो जाती है, इजाजत तब तक नहीं आती। यह जनता के पैसों की लूट के अलावा और कुछ नहीं है। न तो सरकार से किसी जांच की इजाजत की जरूरत रहनी चाहिए, और न ही मुकदमा चलाने के लिए। आज ऐसे कई स्तरों पर मामलों को अटकाया जाता है, और सबसे भ्रष्ट लोग सबसे ताकतवर कुर्सियों पर बैठकर राज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल का यह फैसला चाहे भारत सरकार के संयुक्त सचिव और ऊपर के अफसरों को लेकर आया हो, लेकिन यह बात समझने की जरूरत है कि इस फैसले की भावना इसके शब्दों से ऊपर जाकर देश भर में सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होती है, और देश भर की अदालतों को इस फैसले को समझना भी चाहिए जहां पर दसियों हजार सरकारी अधिकारी और कर्मचारी तरह-तरह की तकनीकी आड़ लेकर अपने खिलाफ कार्रवाई रूकवाकर बैठे हैं। चूंकि यह संविधान पीठ का फैसला है इसलिए इसे आसानी से चुनौती भी नहीं दी जा सकती, और यह खुद सुप्रीम कोर्ट के अब तक के छोटी बेंचों के दिए गए प्रतिकूल फैसलों पर भी लागू होगा।
हमारा मानना है कि कई जगहों पर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष इन दोनों की मेहरबानी भ्रष्ट लोगों पर रहती है, और दोनों की गिरोहबंदी भ्रष्ट अफसरों को बचाने में लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की संभावनाओं को देखकर देश के जनसंगठनों और आरटीआई एक्टिविस्ट को चाहिए कि अपने-अपने इलाके के भ्रष्ट लोगों पर सरकारी मेहरबानियों के खिलाफ सवाल करें, और जनहित याचिका के माध्यम से अदालतों का ध्यान खींचें। नेता और अफसर भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के लिए इस हद तक एक हो गए हैं कि उनकी भागीदारी को तोडऩा बड़ा मुश्किल है। फिर भी इस देश का इतिहास बताता है कि जब कभी कुछ ईमानदार लोगों ने कमरकसी है तो इस गठजोड़ को वे तोड़ भी पाए हैं। लोगों को याद रखना चाहिए कि देश के कई राज्यों में भ्रष्टाचार के मामलों में मुख्यमंत्रियों को भी हटना पड़ा है, और राजनारायण नाम के एक जिद्दी नेता की कोशिशों से इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध करार हुआ था। इसलिए लोगों को हौसला नहीं छोडऩा चाहिए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेताओं और अफसरों की गिरोहबंदी के खिलाफ अदालतों का इस्तेमाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखकर उसकी व्यापक संभावनाओं को टटोलना चाहिए।
देश की एक सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएंडटी के मुखिया अनिल मणिभाई नाइक इस कंपनी में 58 बरस काम करने के बाद अब 81 बरस की उम्र में यहां से हट रहे हैं। न तो यह कंपनी अधिक चर्चा में रहती, और न ही अनिल नाइक का नाम अधिक जाना हुआ है। लेकिन उनके बारे में कुछ बातें जानना हिन्दुस्तान के उन लोगों के लिए दिलचस्प हो सकता है जो किसी मामूली कामयाबी के बाद शान-शौकत की जिंदगी जीने लगते हैं। गुजरात में एक शिक्षक पिता के घर पैदा होने के बाद उन्होंने परिवार में गांधी के आदर्शों पर चलना सीखा। इंजीनियर बनने के बाद मुम्बई आकर लार्सन एंड टुब्रो कंपनी में काम करना शुरू किया। पिछले 21 बरस में उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, हर दिन 15 घंटे काम किया। कुछ लोगों के लिए यह जानना दिलचस्प हो सकता है कि उनके कार्यकाल में ही इस कंपनी का मार्केट कैप चार हजार करोड़ से बढक़र 4.1 लाख करोड़ रूपए हो गया। 670 रूपए महीने पर नौकरी शुरू करने वाले नाइक को अभी महज छुट्टियां न लेने के एवज में 19 करोड़ रूपए मिले हैं। अभी उनकी संपत्ति चार सौ करोड़ से ज्यादा है, और 2016 में उन्होंने अपनी 75 फीसदी संपत्ति दान दे दी थी। 2022 में 142 करोड़ रूपए दान दिए थे। और निजी जिंदगी की सादगी ऐसी है कि वे कंपनी की बोर्ड मीटिंग में भी टी-शर्ट पहनकर चले जाते हैं, उनके पास कुल आधा दर्जन शर्ट, 3 सूट, और दो जोड़ी जूते हैं। उन्होंने जिंदगी में कभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया, और कोई डिजिटल भुगतान नहीं किया। अपने दादा और पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए वे अधिक से अधिक दान देने में भरोसा करते हैं। कंपनी में उनका उतना सम्मान है कि वे आने वाले कई बरस तक इस कंपनी के मझले दर्जे के लोगों के मार्गदर्शक और सलाहकार का काम करते रहेंगे। कारोबारी दुनिया में कंपनी की साख इतनी अच्छी है कि अनिल नाइक को पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया था।
किसी कारोबारी के बारे में इस कॉलम में लिखने के अधिक मौके नहीं आते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में कई ऐसे बड़े कामयाब कारोबारी हैं जिन्होंने कानून तोड़े बिना बड़ी कमाई की है, और उसका बड़ा हिस्सा दान भी किया है। अनिल नाइक एलएंडटी में वेतनभोगी मुखिया रहे, और जाहिर है कि अडानी-अंबानी जैसे लोगों के मुकाबले वे दौलत के मामले में कुछ भी नहीं थे, लेकिन अपनी कुछ सौ करोड़ की जायदाद का एक तीन चौथाई हिस्सा दान में देकर उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है। देश में कुछ और ऐसे उद्योगपति-कारोबारी रहे। एचसीएल के संस्थापक शिव नाडर ने 2022 में 1161 करोड़ रूपए दान दिए। विप्रो के अजीम प्रेमजी ने 484 करोड़ रूपए दान दिए। मुकेश अंबानी ने 411 करोड़ और कुमार मंगलम बिड़ला ने 242 करोड़ दान दिए। इसके बाद सुष्मिता और सुब्रत बागची (213 करोड़), राधा और एनएस पार्थ सारथी (213 करोड़), गौतम अडानी (190 करोड़), अनिल अग्रवाल (165 करोड़), नंदन निलेकेणि (159 करोड़), और अनिल नाइक (142 करोड़) दानदाताओं की टॉपटेन की लिस्ट में आते हैं।
न सिर्फ अधिकांश संपत्ति को दान दे देना, बल्कि सादगी से जीना, यह एक बड़ी और अलग किस्म की मिसाल है। आज पैसे कमाने के मामले में अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, और धोनी अनिल नाइक के मुकाबले कई गुना बड़े होंगे, लेकिन उनका दान अमूमन सुनाई नहीं देता। अडानी और अंबानी का जितना बड़ा साम्राज्य है, उसके मुकाबले उनका दान भी ऊंट के मुंह में जीरे सरीखा है। ऐसे में अमरीका के कुछ उद्योगपतियों की याद आती है जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और वारेन बफे जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आधी संपत्ति दान करने की घोषणा की है, और उसे वे तरह-तरह की समाजसेवा में करते चल रहे हैं। बहुत से कामयाब कारोबारियों का यह मानना है कि दौलत कमाने का अपना एक मजा रहता है लेकिन एक सीमा के बाद उस दौलत को दूसरों में बांटने का एक मजा रहता है। अभी भारत में आर त्याग राजन की एक खबर सामने आई जिन्होंने श्रीराम फाइनेंस नाम से भारत के ट्रक-ट्रैक्टर, और दूसरी गाडिय़ां खरीदने वाले लोगों को बिना किसी गारंटी फाइनेंस करना शुरू किया था, और अब 86 बरस की उम्र में वे अपना घर और एक कार छोडक़र बाकी सारी कंपनी कर्मचारियों के बीच बांट दे रहे हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी कमजोर तबके के लोगों को लोन दिया, और अब 6 हजार करोड़ से अधिक की कंपनी वे कर्मचारियों में बांट दे रहे हैं। गारंटी न दे पाने वाले छोटे लोगों को लोन देने का उनका तजुर्बा हमेशा अच्छा रहा, और उनकी कंपनी भी लगातार आगे बढ़ती चली गई। 1974 में शुरू यह कंपनी अपने क्षेत्र की एक सबसे कामयाब कंपनी है, और बहुत अमीर परिवार में बड़े होने के बाद भी वे वामपंथी-समाजवादी सोच के साथ छोटे लोगों को खतरा उठाकर लोन देने का कारोबार करते रहे। वे पूरी जिंदगी बड़ी सादगी से रहे, और अभी भी उनका कहना है कि उनके कोई अधिक खर्च नहीं है। वे एक छोटे से घर में रहते हैं, 6 लाख रूपए की मामूली कार में चलते हैं। वे एक मोबाइल फोन भी नहीं रखते। उनकी कंपनी में आज एक लाख से अधिक कर्मचारी हैं, और बिना गारंटी वाले लोगों को कारोबारी गाडिय़ों के लिए कर्ज देना जारी है, और श्रीराम समूह में अब 30 अलग-अलग कंपनियां हैं।
इन कुछ मिसालों को सामने रखने का एक मतलब यह भी है कि जो लोग अंधाधुंध खर्च और शान-शौकत के पीछे भागते हैं, वे यह बात भी समझ लें कि जिंदगी में शान-शौकत का महत्व एक हद तक ही रहता है, और असल शान की बात सादगी में रहकर लोगों के काम आना है। जिन लोगों के पास दूसरों को दान करने लायक नहीं है, वे भी सादगी में रहकर दूसरों के कुछ न कुछ काम तो आ ही सकते हैं। दूसरी तरफ जिनके पास कुछ है, वे अनिल नाइक या अजीम प्रेमजी से अपनी तुलना किए बिना अपनी क्षमता से लोगों के काम आ सकते हैं। बात सोच की रहती है, आकार की नहीं। किसी जायदाद का आकार बहुत बड़ा हो, लेकिन दान की नीयत बहुत छोटी हो, और वह भी सिर्फ पीएम केयर्स जैसे फंड के लिए पैदा होती हो, तो फिर यह आज की यह बात उन लोगों के लिए नहीं है। यह बात उनके लिए है जो आज की अपनी सीमित क्षमता के बीच भी दूसरे जरूरतमंद लोगों की छोटी-छोटी मदद कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चाम्पा इलाके में शराब पीने से एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल अभी पीडि़त परिवार से मिलने पहुंचे तो वहां की खबर के साथ उनकी तस्वीर भी है। आधा दर्जन लोगों के साथ वे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, सामने बोतल बंद पानी रखा है, और पीडि़त परिवार के सिर मुंडाए लोग सामने खड़े हैं। चूंकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का एक दर्जा होता है, इसलिए आधा दर्जन पुलिस वाले भी आसपास खड़े दिख रहे हैं। वैसे तो इस खबर और तस्वीर में लोगों को कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा, लेकिन जरा सी संवेदनशीलता से इसे देखें तो गमी में शरीक होने पहुंचे नेता जांच कर रहे पुलिस अफसरों के अंदाज में कुर्सियों पर जमकर बैठे हैं, और मृतक परिवार के लोग मुजरिमों की तरह दीनहीन सामने खड़े हैं। अगर यह चुनाव का मौका नहीं भी रहता, तो भी यह नजारा हमें अटपटा लगता कि जो नेता जनता के वोटों पर जिंदा रहते हैं, उनकी जनता की गरिमा और उनकी भावनाओं के लिए जरा भी संवेदनशीलता क्यों नहीं रहती। और अभी तो चुनाव का दौर चल रहा है, नारायण चंदेल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े भाजपा नेता हैं, शायद वे खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ें, और उनका यह अंदाज बहुत सी पार्टियों के बहुत से नेताओं का आम अंदाज है। ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी, और हिन्दुस्तान की सबसे संपन्न पार्टी, और हिन्दुस्तान के इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी, इन दोनों के नेताओं को जनता के साथ मिलने-जुलने, बात करने के तौर-तरीके सिखाने का एक कोर्स होना चाहिए।
पिछले कुछ बरसों से इन दोनों पार्टियों के अलावा और भी कई पार्टियों के नेता छांट-छांटकर दलितों के घर खाने को जाने लगे हैं, और वहां भी उनके लिए अलग से चौकियां लगने लगी हैं, कई जगह सुनाई पड़ता है कि खाना भी बाहर से लाया जाता है। यह सिलसिला दलितों का सम्मान बढ़ाने का नहीं है, उनके राजनीतिक इस्तेमाल का सिलसिला है। दलितों, आदिवासियों, और गरीबों के सबसे हिमायती नेताओं को इस तरह के किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। गरीब के साथ खाना, गरीब जैसा खाना, इसके बजाय अधिक जरूरी यह है कि गरीब के रोज के खाने को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, यह देखना चाहिए। गरीब की जिंदगी देखना हो, तो जिस तरह राहुल गांधी विदर्भ के खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों तक बिना किसी लाव-लश्कर के, बिना किसी मुनादी के पहुंचे थे, उस तरह जाकर देखा जा सकता है। लेकिन जब किसी गरीब दलित परिवार में दर्जन भर बड़े नेताओं के लिए दर्जन भर चौकियों पर कपड़ा ढांककर कई तरह का खाना खिलाया जाता है, तो वह दलित-हमदर्दी नहीं रह जाती, वह दलित-पर्यटन हो जाता है। यह पाखंड खत्म करना चाहिए।
हम फिर छत्तीसगढ़ की उसी बात पर लौटें जिसकी वजह से आज इस मुद्दे पर लिख रहे हैं, तो जब लोग किसी परिवार के दुख में शरीक होने पहुंचें, किसी बीमार को देखने अस्पताल पहुंचें, तो उन्हें कैमरे साथ नहीं ले जाना चाहिए। परिवार का अपना दुख है, नेता वहां जाकर उसका नगदीकरण क्यों करवाएं? इसी तरह जब नेता किसी बीमार को देखने पहुंचते हैं तो उन्हें बीमार के बिस्तर तक ले जाने का सिलसिला पूरी तरह बंद होना चाहिए। अपने कई साथियों और चापलूसों के साथ नेता किसी वार्ड में या किसी बीमार के बिस्तर पर पहुंचकर उसे संक्रमण के खतरे के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। ऐसे में भी नेता फोटोग्राफर ले जाना नहीं भूलते, और अस्पतालों के ऐसे प्रचार-पर्यटन को भी खत्म करना चाहिए। यह बात अकेले हमारे लिखे अमल में नहीं आएगी, सोशल मीडिया पर लोग जब जहां ऐसी तस्वीर देखें, उसके नीचे इतना लिखें कि नेताओं को यह समझ आ जाए कि उन्हें नाम कम मिल रहा है, बदनामी अधिक हो रही है। जब नेता जनता के दुख के प्रति संवेदनशील न रहें, तो यह जनता की ही जिम्मेदारी हो जाती है कि उन्हें झिंझोडक़र याद दिलाएं कि संवेदनाओं के महज प्रदर्शन के लिए न आएं, बल्कि संवेदनशील होकर भी रहें।
बहुत से नेताओं को हमने देखा है कि किसी मिजाजपुर्सी या किसी गमी में जाने पर वहां भी मीडिया के बात करने पर वे हजार किस्म की राजनीतिक बातें करते हैं। ऐसी खबरों और तस्वीरों पर भी लोगों को जमकर लिखना चाहिए कि किसी एक जगह को तो छोड़ दो, गिद्ध भी पशुओं की लाश खाते हुए कैमरों पर बाईट नहीं देते, कोई बयान जारी नहीं करते, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, और सिर्फ वही करते हैं। चूंकि एक-एक करके अधिकतर राजनीतिक दल संवेदनाशून्य हो चुके हैं, इसलिए जनता को ही इस चुनौती को मंजूर करना पड़ेगा कि वह सार्वजनिक मंचों पर, सोशल मीडिया में इस बात को उठाए कि गिद्धों को भी अपने काम से काम रखना चाहिए, और बीमार या विचलित को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
लोकतंत्र को सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच किस मैच का सामान मान लेने वाली जनता अगर खुद को स्टेडियम के चारों तरफ बैठे दर्शक ही मान लेती है, तो फिर उसे उसी किस्म की सरकार मिलती है। उसे पांच बरस राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के कीचड़ फेंकने का मैच देखने मिल सकता है, लेकिन अपनी असल जिंदगी की तकलीफों का कोई इलाज नहीं मिल सकता। इसलिए जनता को नेताओं के आरोपों के सैलाब में भी अपनी बुनियादी जरूरतों और अपनी मुद्दों को जिंदा रखना चाहिए, और इसके लिए उसे किसी मीडिया पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो कि अपने खुद के अस्तित्व के लिए नेताओं और सरकारों का मोहताज रहता है। जनता को आज सोशल मीडिया पर मुफ्त में मिली जगह का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, और नेताओं, पार्टियों, और सरकारों के लिए लगातार दिक्कत खड़ी करनी चाहिए।
देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव पर दिल्ली में चल रहे जी-20 सम्मेलन का कुछ साया पड़ा हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उसी में लगे हुए हैं, और इन राज्यों में भाजपा उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर तमाम पार्टियां इन पांचों राज्यों में चुनाव की तैयारियों में लगी हैं, और वक्त रहते सबके उम्मीदवार आ भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बसपा और आम आदमी पार्टी ने 9-9 सीटों पर, और भाजपा ने 21 सीटों पर नाम घोषित कर दिए हैं, और कांग्रेस भी इसकी बैठकों में लगी हुई है। लेकिन इन सबके बीच जनता, जनहित, और जनचेतना कहां हैं?
आज हालत यह हो गई है कि छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, और राजस्थान जैसे राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के बीच तथ्यों और तर्कों पर बातचीत खत्म हो चुकी है, और सिर्फ भावनात्मक, भडक़ाऊ, धार्मिक, और साम्प्रदायिक जुबान में बातें चल रही हैं। गरीबी के ग पर बात होने के बजाय इन पार्टियों के बीच बहस गाय, गोबर, गणेश, गोमूत्र जैसी बातों पर टिकी हुई है। ऐसे में कुछ जनसंगठनों की जरूरत है जो कि पार्टियों और नेताओं के नारों से परे उनकी हकीकत का विश्लेषण करें, और जनता के सवाल तैयार करें। बहुत से मुद्दों पर हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े ऐसे मामले हैं जो पिछली दूसरी पार्टी की सरकार के वक्त से चले आ रहे हैं, और जिन्हें मौजूदा सरकारों ने पांच बरस में छुआ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियों के बीच कुछ चुनिंदा भ्रष्ट लोगों के लिए एक अघोषित आम सहमति बन जाती है, और फिर उनका कुछ नहीं बिगड़ता। जो बहुत छोटी पार्टियां हैं उनसे जरूर उम्मीद की जाती है कि बड़ी पार्टियों की ऐसी अघोषित गिरोहबंदी के खिलाफ वे अलग रहकर भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करेंगी, लेकिन उनकी अपनी क्षमता बहुत सीमित रहती है, और वे भी इस काम को नहीं कर पातीं। देश में ऐसे संगठन जरूर हैं जो कि पूरे ही समय यह विश्लेषण करते रहते हैं कि किस राज्य के चुनाव में किस पार्टी के कितने मुजरिम किन-किन जुर्मों वाले हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, और विधानसभा या संसद में कितने करोड़पति या अरबपति पहुंच रहे हैं, महिलाओं को कितनी जगह मिल रही है। लेकिन ऐसे एक-दो संगठन सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों का विश्लेषण करके ऐसे निष्कर्ष सामने रखते हैं, लेकिन आयोग में दाखिल ऐसे तथ्यों से परे वे जनमुद्दों को नहीं उठा पाते। इसके लिए जमीन पर काम करने वाले जनसंगठनों की जरूरत है, और उसके बिना लोकतांत्रिक जनचेतना की कोई संभावना नहीं दिखती।
एक किस्म से खबरदार-मतदाता, या खबरदार-नागरिक जैसे कुछ संगठन रहने चाहिए जो किसी भी तरह की राजनीतिक प्रतिबद्धता से परे हों, और जो प्रदेश स्तर पर या चुनाव क्षेत्र के स्तर पर नेताओं और पार्टियों से सवाल करें। कायदे से तो यह काम मीडिया का होना चाहिए, लेकिन मीडिया चुनाव के वक्त जिस तरह प्रायोजित परिशिष्टों से लदा रहता है, और चुनाव में चर्चित पैकेज की ताक में रहता है, उससे अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती। मीडिया अगर कुछ पार्टियों और नेताओं के खिलाफ कुछ छापते या दिखाते दिखता भी है, तो यह मानकर चलना चाहिए कि वह असली नुकसान पहुंचाने वाला मसाला नहीं रहता, बस सतही चोट पहुंचाने, और अपनी साख बचाने का नाटक अधिक रहता है। ये पांच चुनाव भी आ चुके हैं, और ये निकल भी जाएंगे, लेकिन पार्टियों और नेताओं से जो खरे सवाल किए जाने चाहिए, शायद उन्हें न तो विरोधी पार्टियां करेंगी, और न ही मीडिया करेगा। इसलिए लोकतंत्र में तथाकथित स्वघोषित चौथे स्तंभ से परे एक ऐसे जनमंच की जरूरत है जिसके लोग पूरे पांच बरस रिसर्च करते रहें, अध्ययन और विश्लेषण करते रहें, और चुनाव के पर्याप्त पहले वोटरों के सामने वे मुद्दे और सवाल रखें जो उन्हें आने वाले नेताओं और उनकी पार्टियों से पूछने चाहिए। बिना ऐसी जनचेतना के जो चुनाव होंगे वे सिर्फ चुनाव आयोग की तकनीकी औपचारिकता पूरी करने वाले, और पार्टियों और नेताओं से उपकृत होने वाले मतदाताओं के जलसे सरीखे होंगे, उनसे किसी तरह का ईमानदार लोकतांत्रिक चयन नहीं हो सकेगा।
लोकतंत्र एक तंत्र के रूप में ऐसा झांसा देता है कि वह लोक से चलने वाला तंत्र है, जबकि हकीकत यह है कि यह तंत्र के शिकंजे में फंसे हुए लोगों की व्यवस्था हो गई है। लोग इस बात को लेकर खुश रहते हैं कि वे सरकार बनाते हैं, जबकि सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर उन्हें एक किस्म से बेवकूफ बनाते हैं। ये दोनों ही अपने गलत कामों को छुपाते हैं, तरह-तरह के गलत लोगों को उम्मीदवार बनाते हैं, और असुविधा खड़ी करने वाले सवालों को न खड़े होने देने के लिए मीडिया को गोद में भी बिठाते हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो इसके तीन घोषित स्तंभों, और चौथे अघोषित स्तंभ मीडिया से परे जनसंगठनों की जरूरत है जो कि किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता के बिना सिर्फ जनहित में मुद्दे उठाने और सवाल पूछने का काम करें। अब जब मीडिया का बहुत सारा हिस्सा उसी तरह से सवाल पूछता है जिस तरह कई बरस पहले संसद में सवाल पूछने के लिए सांसदों को खरीदा गया था, इसलिए अब सवाल तो कहीं और से ही आ सकते हैं, उन लोगों से ही आ सकते हैं जो कि प्रायोजित परिशिष्टों से लदे हुए नहीं हैं, चुनावी पैकेज पाए हुए नहीं हैं। आज स्वतंत्र मीडिया के कुछ लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो अपने कारोबार की जरूरतों से मुक्त हों, बहुत कम लागत से मीडिया का काम कर रहे हों, और जनता के बीच भरोसा पैदा करके अपनी पहुंच बना चुके हों। आज वेबसाइट, यूट्यूब, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे स्वतंत्र पत्रकार काम कर रहे हैं, जो कि किसी कारोबारी दबाव से मुक्त हैं, और राजनीतिक खरीद-फरोख्त के लिए उपलब्ध नहीं हैं। जनता के राजनीतिक शिक्षण और जनचेतना के विकास का रास्ता ऐसे ही लोगों से निकलेगा। सरकार और कारोबार इन दोनों का गठजोड़ सरोकार को सिर नहीं उठाने देता, इसलिए सरोकारी लोगों और जनसंगठनों को लगातार काम करना चाहिए, यह काम सिर्फ चुनाव के पहले नहीं किया जा सकता, इसके लिए पूरे पांच बरस तैयारी करनी होगी, और चुनावों के वक्त मतदाता को सोचने पर मजबूर करने वाले तथ्य, तर्क, और सवाल सामने रखने होंगे।
एक देश एक चुनाव के विवादास्पद मुद्दे पर बिजली की रफ्तार से काम शुरू हो गया है। पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसके लिए बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, और कई प्रमुख लोगों को कमेटी में रखा गया है जिसकी पहली बैठक कोविंद के निवास पर हुई है। इसमें अलग-अलग ओहदों पर काम कर चुके कानून के जानकार लोगों को रखा गया है, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति के ढांचे से ही असहमति जताते हुए इसमें रहने से मना कर दिया है। इस तरह अब यह समिति किसी विपक्षी असहमति के दबाव से मुक्त होकर काम करेगी, यह एक अलग बात है कि एक पूर्व राष्ट्रपति को किसी कमेटी में रखे जाने को लेकर लोगों में हैरानी है, और उससे भी अधिक हैरानी लोगों में यह है कि एक विवादास्पद मुद्दे पर विचार करने, और रिपोर्ट देने के काम को एक पूर्व राष्ट्रपति ने मंजूर किया है जिन्हें कि परंपरा के मुताबिक किसी भी काम से परे रहना चाहिए था। लोकतंत्र में हर बार यह तर्क इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि कानून में इसकी कोई मनाही नहीं है। एक स्वस्थ और विकसित लोकतंत्र न सिर्फ कानूनों के मुताबिक चलता है, बल्कि कई किस्म की गौरवशाली परंपराओं का भी ध्यान रखता है। एक पिछले मुख्य न्यायाधीश ने बहुत बुरी तरह विवादास्पद कार्यकाल के बाद सरकार को सुहाने वाले फैसले देने के बाद जिस तरह राज्यसभा में सत्ता के भेजे जाना तय किया, उसे भी बहुत बुरी मिसाल माना गया। हमने पहले ही दिन रामनाथ कोविंद के इस चयन, और उनकी इस सहमति, इन दोनों को ही खराब करार दिया था, और आज भी हम उस पर कायम हैं।
लोकतंत्र बहुमत के बाहुबल का नाम नहीं होता, वह बहुमत और अल्पमत के बीच एक समावेशी व्यवस्था होती है जिसमें सहमति जरूरी न होने पर भी सहमति के लिए कोशिश की जाती है। एक आम सहमति, या व्यापक सहमति किसी फैसले को अधिक लोकतांत्रिक सम्मान दिलाती है, और बेहतर लोकतंत्र हमेशा ही इसकी कोशिश करते हैं। हिन्दुस्तान में या इसके अलग-अलग प्रदेशों में जहां सदनों में अनुपातहीन बहुमत से सत्ता बनती है, वहां किसी भी तरह की सहमति की फिक्र करना अवांछित काम मान लिया जाता है। संसदीय फैसले इस तरह लिए तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसे फैसलों को इज्जत नहीं दिलाई जा सकती। एक देश एक चुनाव के लिए बनी कमेटी में रहने से इंकार करना कांग्रेस का सही फैसला है या गलत उस पर हम अभी कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन कई विपक्षी पार्टियों और नेताओं ने ऐसी कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति को रखने का विरोध किया है, और वह अपने आपमें इस कमेटी का बहिष्कार करने के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए।
हमने अपने अखबार में इसी जगह बहुत लंबे समय से एक देश एक चुनाव की वकालत की है। और आज जब मोदी सरकार इसी के लिए एक अभियान चला रही है, और देश के अधिकतर मोदी विरोधी इसके खिलाफ हैं, तो भी हम सैद्धांतिक रूप से इस सोच के साथ हैं। हर बरस कहीं न कहीं होने वाले चुनाव तरह-तरह की सत्तारूढ़ या प्रमुख विपक्षी पार्टियों से कई किस्म के लुभावने वायदे करवाते हैं, और इनसे देश का एक योजनाबद्ध विकास प्रभावित होता है। आदर्श स्थिति यही होगी कि लोकसभा, विधानसभा, और स्थानीय संस्थाओं के चुनाव एक साथ हों, और लोग वोट डालकर सत्ता पर आने वाली पार्टियों को पांच बरस बिना किसी मतदाता-दबाव के काम करने दें। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि हर बरस कहीं न कहीं होने वाले चुनाव राजनीतिक दलों को मनमानी करने से रोकते हैं, और जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखते हैं। इस तर्क पर हमारा अधिक भरोसा नहीं है क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही सामान्य कार्यकाल में होनी चाहिए, पूरे कार्यकाल में होने चाहिए, और न कि चुनाव के वक्त होनी चाहिए। आम चुनाव, राज्यों के विधानसभा चुनाव, और जगह-जगह होने वाले उपचुनाव, म्युनिसिपल और पंचायतों के चुनाव ये अगर बिखरे रहेंगे, तो पार्टियां गैरजरूरी समझौतों में लगी रहेंगी, और मतदाताओं को रुझाने का काम जनता के पैसों को ही बर्बाद करने की कीमत पर होगा। अब आज देश में मोदी के नाम का जो बोलबाला दिख रहा है, उसे देखते हुए अगर कई पार्टियों को इनसे देश में एक अलग तरह का खतरा दिखता है, तो हम ऐसे व्यक्तिकेन्द्रित विरोध का समर्थन नहीं करते। जब देश के पहले चार चुनाव हुए थे, तो पहले तीन चुनावों में तो जवाहरलाल नेहरू ही देश के सबसे बड़े नेता थे, और उनकी लोकप्रियता की वजह से ऐसा तो हुआ नहीं था कि लोगों ने चुनावों को अलग-अलग करने की मांग की हो।
हमारा तो यह भी सोचना है कि मोदी की लोकप्रियता से लोकसभा चुनावों में उन्हें बहुमत मिल रहा है, लेकिन कई राज्यों में भाजपा चुनाव हारी भी है। अगर वहां विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए रहते, तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब जैसे कई राज्यों में विधानसभा जीतने वाली पार्टियों का असर लोकसभा पर भी हुआ रहता, और हो सकता है कि वहां भाजपा या एनडीए की सीटें घटी होतीं। फिलहाल हमारा इतना ही कहना है कि सरकार को सिर्फ बहुमत से असहमति को नहीं कुचलना चाहिए, और इस मुद्दे पर एक व्यापक बहस होने देना चाहिए। वैसे भी लोगों का यह कहना है कि इसके लिए कई किस्म के संविधान संशोधन लगेंगे, और वे तमाम राज्यों की सहमति के बिना नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक देश एक चुनाव से सहमत और असहमत लोगों को सार्वजनिक रूप से भी अपने तर्क लोगों के सामने रखने चाहिए, ताकि आने वाले चुनावों के वक्त लोग ऐसे फैसलों के नफे-नुकसान ध्यान में रखकर वोट डाल सकें।
हरियाणा के गुरूग्राम की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग के वीडियो को तोड़-मरोडक़र प्रसारित करने के मामले में 8 पत्रकारों के खिलाफ कई आपराधिक आरोप तय किए हैं। ये पत्रकार देश के चर्चित टीवी जर्नलिस्ट हैं, और इन पर पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए गए हैं जो कि बच्चों के अश्लील इस्तेमाल का कानून है। यह करीब दस साल पहले से चले आ रहा मामला था, और एक खबर में बताया गया है कि एक परिवार में आसाराम (बापू) के पहुंचने पर परिवार के लोगों ने उनसे आशीर्वाद लिया था, और उसकी वीडियो भी बनाई गई थी। बाद में जब आसाराम का बलात्कारकांड हुआ तो कई टीवी चैनलों ने जो रिपोर्ट बनाई उनमें इस परिवार के साथ उनके आशीर्वाद के वीडियो को भी गलत तरीके से जोडऩे का आरोप है, और इस घर को अश्लीलता का अड्डा बताया गया था। अब बड़े नामी-गिरामी और चर्चित पत्रकारों पर पॉक्सो के तहत चार्जफ्रेम हो गए हैं, तो उनके लिए कुछ परेशानी हो सकती है।
इस मामले से एक सबक तो यह मिलता है कि कानून के तहत मीडिया को जो सावधानी बरतनी चाहिए, उसमें बड़े-बड़े, अनुभवी पत्रकार भी गलती कर सकते हैं। खासकर बच्चों और महिलाओं के मामले में, दलितों और आदिवासियों के मामले में कानून बड़ा साफ है, और बड़ा कड़ा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बिजली सरीखी रफ्तार के चलते, और एक-दूसरे से गलाकाट मुकाबला होने की वजह से टीवी चैनलों से गलतियां कुछ अधिक होती हैं, हालांकि अखबार भी इससे अछूते नहीं रहते। दूसरी तरफ बड़ी लागत से चलने वाले टीवी चैनलों के पास तो चीजें को जांचने-परखने के लिए एक ताकत रहती है, लेकिन इन दिनों डिजिटल मीडिया के नाम पर कोई अकेले व्यक्ति भी एक वेबसाइट बनाकर उस पर समाचार-विचार, फोटो और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, करते हैं, और फिर इसके लिंक तरह-तरह के मैसेंजरों से आगे बढ़ाते हैं। इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेस से जुड़े हुए कानून पढ़े नहीं हैं, और जिन्हें पत्रकारिता की लंबी सीख से गुजरने का कोई मौका नहीं मिला है, उसकी अब जरूरत भी नहीं रह गई है। अब सिर्फ एक वेबसाइट, और एक कम्प्यूटर होना काफी रहता है, और वीडियो-कैमरों की कमी को मोबाइल फोन भी पूरा कर देता है। फिर इससे भी एक कदम आगे बढक़र यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, जिनमें वेबसाइटों और न्यूजपोर्टलों की तरह किसी संपादक की नजर से कुछ गुजरना जरूरी नहीं होता है, और लोग जो चाहे वह पोस्ट करते हैं, विवाद होने पर उसे हटाकर यह मान लेते हैं कि विवाद खत्म हो गया है, जबकि इन दिनों हटाई गई पोस्ट भी जांच एजेंसियों को पूरी तरह हासिल रहती हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं जहां पर आम लोग भी कई किस्म की आपत्तिजनक, और हिंसक बातें पोस्ट करते हैं।
ऐसा लगता है कि जब केन्द्र और राज्य सरकारें डिजिटल मीडिया को विज्ञापनों के लिए भी मान्यता दे रही हैं, और उन्हें पत्रकारों में शामिल भी कर रही हैं, पत्रकारों को मिलने वाली सहूलियतों और हिफाजत का फायदा ऐसे डिजिटल स्वघोषित पत्रकारों को भी मिल रहा है। ऐसे में यह सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि वह देश के कानून की जानकारी तमाम ऐसे स्वघोषित पत्रकारों को देने का कोई इंतजाम करे ताकि देश में बदअमनी न फैले। अखबारों में संपादक नाम की एक संस्था होती थी, जो अपने अनुभव से बाकी लोगों के काम को कुछ या अधिक हद तक जांच ही लेते थे। लेकिन अब एक सैनिक की फौज सरीखे बहुत से डिजिटल समाचार-विचार माध्यम प्रचलन में हैं, और खुद उनके भले के लिए यह जरूरी है कि सरकार उनके प्रशिक्षण का कोई इंतजाम करे।
उत्तरप्रदेश जैसे राज्य ने अभी सभी तरह के मीडिया को जांचने-परखने का एक सरकारी फैसला लिया है जिसमें यह इंतजाम भी किया गया है कि अगर उनमें कोई गलत जानकारी आती है, तो उन्हें इसकी सूचना दी जाए। इसे कई लोग मीडिया पर नजर रखने की बात कह रहे हैं, लेकिन बहुत से प्रदेशों ने, और केन्द्र सरकार के मीडिया संस्थान पीआईबी ने भी फैक्ट चेक का एक औपचारिक ढांचा खड़ा किया है, और आए दिन बहुत सी खबरों को झूठ का ठप्पा लगाकर सबके सामने रखा भी जाता है। हमारा यह मानना है कि सरकार की ऐसी जांच से किसी जिम्मेदार मीडिया को नहीं डरना चाहिए। और फैक्ट चेकिंग का काम तो सरकारों से परे कई जिम्मेदार वेबसाइटें भी कर रही हैं, और कुछ बड़े मीडिया संस्थान भी अपनी और दूसरों की खबरों का फैक्ट चेक करते ही रहते हैं।
किसी अदालत तक मामला पहुंचने, और सजा पाने से पहले हर मीडिया संस्थान के पास यह मौका रहता है कि अपनी जानकारी गलत होने की खबर लगने पर वे उसमें सुधार करें, और जरूरत रहे तो माफी मांगें। ऐसा करने के बाद अदालती खतरा घट जाता है। लेकिन हमारा लंबा तजुर्बा यह कहता है कि अधिकांश मीडिया संस्थान अपनी गलती, या अपने गलत काम के उजागर हो जाने के बाद भी माफी न मांगकर अपने अहंकार पर टिके रहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह कि बहुत से नेता अपने अपमानजनक बयानों पर टिके रहते हैं। हमारा अपना नजरिया इस बारे में बड़ा साफ है। अगर हम अपने प्रकाशित किसी समाचार में कोई गलती पाते हैं, या उसके खिलाफ कोई आपत्ति आती है जो कि जायज दिखती है, तो हम तुरंत ही उसका खंडन या स्पष्टीकरण छापते हैं, और गलती रहती है तो माफी भी मांगते हैं। हमारा मानना है कि लोग जब अपनी गलतियां मानने को तैयार रहते हैं, तो यह शर्मिंदगी उन्हें आगे गलती करने से बचाती भी है। अपनी गलतियों पर अड़े रहकर लोग आगे और गलतियों का रास्ता खुला रखते हैं। किसी भी जिम्मेदार पत्रकार या मीडिया संस्थान को ऐसा नहीं करना चाहिए। हिन्दुस्तान में कम से कम एक अखबार, द हिन्दू की मिसाल सबके सामने है कि किस तरह उसने अपने अखबार के बाहर से एक स्वतंत्र व्यक्ति को जिम्मेदारी देकर उसकी खुली सूचना अपने पन्नों पर छापी कि ये व्यक्ति इस अखबार के लिए ओम्बुड्समैन रहेंगे, और पाठक या संबंधित व्यक्ति अखबार के किसी भी हिस्से के बारे में उन्हें शिकायत भेज सकते हैं, और उनका जो भी फैसला रहेगा, उसे अखबार मानेगा। ऐसा हौसला किसी अखबार की इज्जत को बढ़ाता ही है। और अब चूंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तकनीक, और संचार क्रांति की वजह से समाचार-विचार की सुनामी ही हर दिन रहती है, इसलिए ऐसी पहल और जरूरी है। कहने के लिए तो इस देश में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसा संवैधानिक अधिकार प्राप्त इंतजाम किया गया है, लेकिन उसके अधिकार नहीं के बराबर हैं, इसलिए उसका कोई असर भी मीडिया पर नहीं दिखता। लेकिन अब चूंकि मीडिया नाम के इस कारोबार के आकार में एक विस्फोट सा हुआ है, इसलिए राज्य और केन्द्र सरकारों को इस बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। आज जिस तरह अखबारों की प्रसार संख्या, टीवी चैनलों की टीआरपी, और वेबसाइटों की हिट्स के आधार पर सरकारें इश्तहार देती हैं, वह एक बहुत ही गैरजिम्मेदारी का काम है। सिर्फ आंकड़ों से मीडिया के महत्व को तय करना इस देश को बहुत ही गैरजिम्मेदार मीडिया ही दे सकता है।
हर दिन आसपास अनगिनत घटनाएं दिल दहला रही हैं। उन्हें खबरों में छापना भी आसान नहीं है, और उन पर यहां लिखने का भी दिल नहीं कर रहा है। आज अपने आसपास के शहर-कस्बों की खबरें हैं कि टोनही के शक में पड़ोसी की जान ले ली। दूसरी खबर है एक आदमी ने अपने ही पांच बरस के बेटे की दोनों आंखें चाकू से फोड़ दीं, परिवार ने बताया कि किसी ने उसे फोन पर ऐसा करने कहा और उसने तुरंत कर दिया। एक अलग खबर है कि एक महिला की संपत्ति हथियाने के लिए उसके बेटे-बहू ने उसका कत्ल कर दिया। एक अलग खबर है कि खाना न बनाने पर एक पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी मारकर मार डाला। दो दिन पहले एक खबर आई थी कि बीवी से दारू के लिए पैसा नहीं मिला तो इसी इलाके में एक आदमी ने अपने डेढ़ बरस के बेटे को मारकर पेड़ पर टांग दिया। ये खबरें मेहनत से बनाई गई लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक नजर में दिखी खबरें हैं। इन सबमें एक बात एक सरीखी है कि ये सब परिवार के भीतर की हिंसा हैं, या अधिक से अधिक पड़ोस की। हर दिन परिवार के भीतर एक या अधिक बलात्कार की खबरें आती हैं, और रिश्तेदारों के साथ-साथ बाप भी अपनी बेटी से बलात्कार करते पकड़ा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन सब मामलों की पुलिस में रिपोर्ट अब अधिक हो रही है, ऐसे मामले हो ही अधिक रहे हैं। इन पर कोई चर्चा भी इसलिए नहीं होगी कि पुलिस रिपोर्ट के बाद गिरफ्तारी हो जाती है, और अदालतों में बरसों तक मुकदमे चलते रहते हैं। लेकिन क्या पुलिस और कोर्ट ही ऐसे मामलों के लिए काफी कार्रवाई है?
किसी भी जनकल्याणकारी सरकार को अपने देश-प्रदेश में लोगों के बीच पनपती हिंसक भावनाओं का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे तनाव की बहुत सी वजहें हो सकती हैं जिनके बढ़ते-बढ़ते लोग मरने-मारने पर उतारू हो जाएं। घर के भीतर जब इस दर्जे की हिंसा होने लगती है तो सोचना चाहिए कि लोगों के दिल-दिमाग पर कौन-कौन से तनाव हैं? गरीब तबके में गरीबी सबसे बड़ा तनाव रहती है, और वह सौ किस्म के गलत काम करवाती है। जब जिंदा रहने, खाने, और इलाज करवाने में ही लोगों का दम टूटने लगता है, तो शायद उनकी जिंदगी के नीति-सिद्धांत भी टूटने लगते हैं। भूखे के लिए रोटी से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं होता। लोगों को जिंदगी से ऐसी निराशा भी होने लगती है कि वे कोई जुर्म करके बाकी पूरी जिंदगी जेल में गुजारने का खतरा उठाने से भी नहीं हिचकते। ऐसा तब और अधिक होने लगता है जब जेल के बाहर की जिंदगी की तकलीफें इतनी बढ़ जाती हैं, कि लोगों को लग सकता है कि जेल के भीतर इससे और बुरा क्या होगा? जब हालात ऐसे हो जाएं तो खयालात भी वैसे ही होने लगते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, नौकरी न मिलने या चली जाने की तकलीफ, अपनी मर्जी से प्रेम न कर पाने की कुंठा, हिन्दुस्तानी समाज के बड़े हिस्से में ये तमाम तनाव आम हैं।
समाज में जब लोग लूट-डकैती के बिना, बिना किसी फायदे के, जब परिवार के भीतर जान लेने लगते हैं, तो यह समझ पड़ता है कि उनकी निजी निराशा पारिवारिक ढांचे से मिलने वाली ताकत से भी कम नहीं हो पा रही है। लोग आमतौर पर परिवार के लिए बहुत से सही-गलत काम करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब परिवार का ढांचा भी उनमें कोई उम्मीद नहीं जगा पाता, जब परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उनको तोड़ देता है, तो वैसे में कौन सी एक चिंगारी उनके भीतर की अहिंसा को हिंसा में तब्दील कर देती है, यह समझना आसान नहीं है। किसी भी अच्छी सरकार को यह चाहिए कि वह समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों की ऐसी एक कमेटी रखे जो कि पारिवारिक हिंसा के ऐसे मामलों की जानकारी जुटाकर यह समझने की कोशिश करे कि कौन सी वजहें लोगों की हिंसा से हिचक खत्म कर देती हैं, और वे पूरी जिंदगी जेल में गुजारने की कीमत पर भी हत्या, बलात्कार जैसे जुर्म घर के भीतर अपनों पर ही करने लगते हैं। पुलिस अपनी जांच के दौरान इन पहलुओं पर गौर नहीं कर सकती क्योंकि वह जुर्म के कानूनी और अदालती पहलुओं को ही देखते हुए थकी रहती है। इसके लिए पुलिस और वकीलों से परे अध्ययन और शोध में दिलचस्पी रखने वाले जानकार लोग चाहिए। सरकार चाहे तो ऐसी रिसर्च के लिए कुछ फैलोशिप भी दे सकती है, और संबंधित विषयों के शोधकर्ता ऐसे मामलों की जानकारी जुटाकर उनके दस्तावेजीकरण का काम कर सकते हैं, ताकि समाज को तनाव से निकालने के लिए उस तनाव की शिनाख्त तो हो सके, उसके पीछे की वजहें देखी जा सकें।
जिन छोटे कस्बों और गांवों से ऐसे जुर्म की खबरें आ रही हैं, उनसे साफ है कि यह शहरीकरण के असर में होने वाले जुर्म नहीं हैं। यह जरूर हो सकता है कि गांव-कस्बों में भी अब परिवार टूट रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था कमजोर हो रही है, और लोगों पर आसपास का दबाव भी कम हो रहा है। ऐसे में किसी के भीतर हिंसक इरादों का विस्फोट होने के पहले उसका अंदाज लगाकर कोई उसे रोक सके, इसकी गुंजाइश कम दिख रही है। आसपास के उठने-बैठने वाले लोग जरूर हिंसक सोच को समय रहते रोकने की संभावना रखते हैं, लेकिन लोग इन दिनों शायद रूबरू रिश्तों के मुकाबले ऑनलाईन रिश्तों में अधिक उलझे रहते हैं, और उसका एक नतीजा यह भी हो सकता है कि वे आसपास के लोगों के तनाव से या तो नावाकिफ हों, या उसकी तरफ से फिक्रमंद न हों।
जो भी है सरकारों को सामाजिक सोच की समस्याओं की पहचान भी करनी चाहिए। यह काम वोट दिलाने जैसा लुभावना काम नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सरकार चुनावी मोड से परे काम करने की सोच रखती हो, तो वह जरूर इस बारे में सोचेगी।
हिन्दुस्तानी बच्चों को स्कूल में निबंध लिखना सिखाते हुए यह लिखवाया जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सच तो यह है कि भारत एक धर्म प्रधान देश है, और खासकर पिछले दस बरस में कृषि और दूसरे रोजगार लोगों का पार्टटाईम जॉब हो गए हैं, और उनका मूल रोजगार धर्म हो गया है। यही वजह है कि फलते-फूलते धर्म को देखकर लोग संतुष्ट हैं, उनके पेट भर जाते हैं, और किसी को भी इस बात का अफसोस नहीं है कि रोजगार कम हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, कारोबार मंदा है, और महंगाई कमरतोड़ है। ऐसे में धर्म लोगों के सिर चढक़र बोल रहा है क्योंकि अकेला धर्म ही है जो सिर चढ़ी हुई महंगाई और बेरोजगारी को ढांक सकता है, इसलिए लोग उसे भी सिर चढ़ाकर रख रहे हैं। फिर धर्म के साथ-साथ राष्ट्रवाद और राजनीति इन दो का गठजोड़ भी हो गया है, और नतीजा यह है कि त्रिवेणी संगम पर तीन नदियों के पानी के मिलने की तरह धर्म, राजनीति, और राष्ट्रवाद का संगम देश में चल रहा है।
ऐसे में जब इंडिया नाम के गठबंधन के भागीदार एक दल, तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जब सनातन धर्म के उन्मूलन की बात कही, तो भाजपा ने इसे तुरंत लपककर इंडिया से सवाल किया कि क्या यह गठबंधन इसीलिए बना है? डीएमके तमिलनाडु में दलितों की राजनीति करने वाली पार्टी है, और हिन्दू धर्म के पीछे की सनातनी, जातिवादी सोच का वह हमेशा से विरोध करते आई है। इसमें कोई नई बात नहीं है। तमिलनाडु में पेरियार सरीखे महान दलित नेता हुए हैं, जिन्होंने समाज में जाति व्यवस्था की हिंसा का विरोध किया, और दलित चेतना के लिए बड़ा काम किया। इसलिए तमिलनाडु एक दलित राजनीतिक चेतना वाला राज्य है, और वहां पर हिन्दू धर्म के पाखंड वाले हिस्से का विरोध करने में कोई दबी-छुपी जुबान इस्तेमाल नहीं होती। इसी के चलते उदयनिधि स्टालिन ने वामपंथी लेखक-कलाकार संघ के इस सनातन उन्मूलन सम्मेलन में कहा कि सम्मेलन का नाम बहुत अच्छा है, और सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन बेहतर सोच है। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों का विरोध काफी नहीं है, उन्हें खत्म करना होगा, उन्होंने कहा कि हम मच्छर डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस का विरोध नहीं करते हैं (उनका उन्मूलन करते हैं)। उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है, उन्होंने देश की कुछ राजनीतिक ताकतों की तरफ इशारा करते हुए कहा फासीवादी ताकतें हमारे बच्चों को पढऩे से रोकने के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही हैं। सनातन की नीति यही है कि सबको नहीं पढऩा चाहिए। नीट इम्तिहान इसकी एक मिसाल है।
भाजपा ने उदयनिधि के इस बयान को लेकर इंडिया नाम के गठबंधन और कांग्रेस पार्टी से कई किस्म के सवाल किए, भाजपा के नेताओं ने उदयनिधि के खिलाफ दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट की। और आज की खबर यह है कि उत्तर भारत में किसी साधू सरीखे नाम और हुलिए वाले व्यक्ति ने कैमरे के सामने उदयनिधि की तस्वीर को तलवार से चीरते हुए यह घोषणा की कि उनका सिर काटकर लाने वाले को दस करोड़ रूपए का ईनाम दिया जाएगा। ईनाम की इस घोषणा पर अभी तक किसी जिले की पुलिस या सरकार ने कोई जुर्म दर्ज नहीं किया है। इस बीच राजद के सांसद और प्रवक्ता प्रो.मनोज झा ने कहा है कि उदयनिधि के बयान के प्रतीकों और मुहावरों के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई लोगों का मानना है कि सनातन में कई विकृतियां हैं। उन्होंने पूछा कि क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? उन्होंने कबीर के एक दोहे का जिक्र करते हुए कहा कि इस देश में कबीर ने कई दोहे कहे, क्या आप उन्हें फांसी पर चढ़ा देंगे?
लोकतंत्र में किसी भी धर्म की मान्यताएं और सोच अगर संविधान को कुचलने वाले हों, तो उन्हें बदलने की जरूरत है। अभी मोदी सरकार ने ही मुसलमानों के तीन तलाक को एक कानून बनाकर खत्म किया है। तो क्या इस पर कोई मुस्लिम नेता सिर काटने का फतवा करने लगे? जब राजस्थान में सतीप्रथा को कानून बनाकर बंद करना पड़ा, तो उसे भी कई लोगों ने धार्मिक परंपरा को कुचलना कहा था, आज अगर वह प्रथा जारी होती, तो ताजमहल के मुकाबले अधिक बड़ी संख्या में पश्चिमी पर्यटक उसे देखने आते। समाज सुधार के लिए धर्म में कई किस्म के बदलाव लाए जाते हैं, अभी भी देश में यूनीफॉर्म सिविल कोड की बात चल ही रही है। इससे भी बहुत से धर्मों के रिवाजों पर असर पड़ेगा। आज अगर तमिलनाडु के दलित यह मानकर चल रहे हैं कि सनातन धर्म की नसीहतें जातिवादी हैं, नीची करार दी गई जातियों के खिलाफ हिंसक हैं, और इसलिए सनातन का उन्मूलन होना चाहिए, तो यह दलितों की तकलीफ अधिक है, यह किसी सनातनी को मारने की बात नहीं है। लेकिन आज भारत की राजनीति में किसी बात को तोड़-मरोडक़र एक झूठी तोहमत लगाने का जो फैशन चल रहा है, वह अपनी पूरी हिंसा के साथ उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सामने आई है। यह कहा गया कि उदयनिधि ने हिन्दुओं की सफाये की बात कही है, हिन्दुओं के उन्मूलन की बात कही है। यह बात तो उदयनिधि के शब्दों से भी नहीं निकलती, और न ही शब्दों की भावना से। यह बात कुछ उसी तरह की है जो कि जवाब में उदयनिधि ने कही है। उन्होंने याद दिलाया कि नरेन्द्र मोदी बार-बार कांग्रेसमुक्त भारत की बात कहते हैं, तो क्या वे कांग्रेसियों के सफाये की बात करते हैं? ठीक उसी तरह सनातन के उन्मूलन की बात सनातनियों को मारने की बात नहीं है, इस धर्म या सोच में जो भेदभाव है, बेइंसाफी है, उसके उन्मूलन की बात है।
इंडिया गठबंधन को घमंडिया से लेकर ठगबंधन तक बुलाते हुए भाजपा के नेताओं का गला सूखने लगा है। इस एक नाम से जरूरत से कुछ अधिक दहशत फैल गई लग रहा है। इसलिए इस गठबंधन के एक भागीदार, डीएमके के नौजवान नेता की कही इस बात का कोई तर्कसंगत जवाब देने के बजाय उसके शब्द और उसकी भावना दोनों को तोड़-मरोडक़र भडक़ाने का काम हो रहा है। लोगों में इतनी समझ बाकी रह गई है या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन अगर लोकतांत्रिक समाज में लोगों को ऐसी तोड़-मरोड़ समझ नहीं आती है, तो फिर वे कैसी सरकार के हकदार हैं, इसे बोलने की जरूरत हमें नहीं है। उदयनिधि स्टालिन ने एक बुनियादी सवाल खड़ा किया है, और सनातनी धर्म के भीतर हिंसा के सबसे बुरे शिकार दलितों की ओर से बात की है। अगर भारत में हिन्दू समाज के आंकड़े देखें, तो तकरीबन 77 फीसदी लोग दलित, आदिवासी, ओबीसी हैं। एक चौथाई से कम सवर्ण आबादी का एक बहुत छोटा सा सनातनी हिस्सा अपने धर्म को हमेशा से, हमेशा के लिए, और अपरिवर्तनीय बताता है। इस सवर्ण हिस्से से अधिक आबादी तो देश में दलित-आदिवासियों की है, बल्कि सारे सवर्णों जितने 23 फीसदी तो अकेले दलित ही हैं। ऐसे में इस आबादी को कुचलते हुए संख्या में इतनी ही सवर्ण आबादी के एक बड़े छोटे सनातनी हिस्से के भेदभाव को लोकतंत्र में कब तक जारी रखा जाएगा? और इस भेदभाव और हिंसा पर सवाल उठाने वालों का सिर काटने पर ईनाम रखा जा रहा है। उदयनिधि ने जो कहा उस पर तो कोई जुर्म नहीं बनता है, लेकिन उनका सिर काटने पर ईनाम रखने वाले की गिरफ्तारी में देर करना तो सुप्रीम कोर्ट के हेट-स्पीच आदेश के सीधे-सीधे खिलाफ है।
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आकर यहां की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बहुत कुछ बोलकर गए हैं। उन्होंने एक बड़ी मोटी सी पुस्तिका की शक्ल में आरोप पत्र जारी किया, और काफी तीखे शब्दों में राज्य सरकार को भ्रष्ट करार दिया। इसी दिन राजधानी रायपुर में ही राहुल गांधी का भी कार्यक्रम था, जिसमें कि जाहिर है कि राज्य सरकार की तारीफ की गई, और केन्द्र सरकार और भाजपा की आलोचना की गई। इसके पहले कांग्रेस भाजपा का काला चिट्ठा नाम से एक दस्तावेज जारी कर चुकी थी जिसमें पिछली रमन सरकार के कार्यकाल की कुछ बातें, और मोदी सरकार की कुछ बातों के खिलाफ कई आरोप लगाए गए थे।
लेकिन जब राजनीतिक आरोपों से परे ठोस बातों को देखें, तो ऐसा लगता है कि इनके बीच असल भ्रष्टाचार, और असल जुर्म कहीं दबकर न रह जाए, कहीं ऐसा न हो जाए कि जुर्मों की चर्चा सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित रहे, और चुनावों के साथ ही केन्द्र और राज्य की जांच एजेंसियां भी ठंडी पड़ जाएं। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा है कि राज्य में महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ कार्रवाई यहां की सरकार ने की है, पैसे भी जब्त किए हैं, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक किस्म से अमित शाह से ही यह सवाल किया कि महादेव ऐप बंद कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, या केन्द्र सरकार? उन्होंने अमित शाह से पूछा कि अगर इसे बंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या कारण है? भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस सट्टेबाजी ऐप का न सिर्फ पैसा जब्त किया, बल्कि इसके उपकरण भी जब्त किए, लुक आउट सर्कुेलर जारी किया, केन्द्र सरकार ने क्या किया? उन्होंने तो यह तक कहा कि केन्द्र सरकार इसकी जांच किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को दे दे।
महादेव ऐप नाम का आनलाईन सट्टेबाजी का हजारों करोड़ का कारोबार छत्तीसगढ़ से ही पनपा है, और ऐसी चर्चा है कि दुर्ग-भिलाई इलाके के इसके संचालक अब दुबई जा बसे हैं। किसी फिल्मी कहानी की तरह ऐसी कतरा-कतरा खबरें आती हैं कि बड़े-बड़े अफसर, बड़े-बड़े नेता, दुबई में जुर्म की दुनिया काबू करने वाला दाऊद इब्राहिम, इन सबका इस धंधे में दखल है। ईडी ने छत्तीसगढ़ में इस सिलसिले में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार, और कांग्रेस के राज्य के सबसे बड़े रणनीतिकार विनोद वर्मा सहित कई लोगों पर छापे डाले, और उनसे बयान लेना भी जारी है। मुख्यमंत्री का यह कहना सही है कि राज्य पुलिस ने इस सट्टेबाजी से जुड़े बहुत से लोगों पर कार्रवाई की है। लेकिन ईडी ने अदालत को बताया है कि राज्य के बड़े-बड़े आईपीएस और गैरआईपीएस पुलिस अधिकारी इस धंधे से लगातार पैसा पाते थे, और यह पैसा नेताओं तक भी पहुंचता था। ऐसे में हम ईडी के अदालत में कहे हुए के मुकाबले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अमित शाह को दी गई सार्वजनिक चुनौती को अधिक वजनदार मानते हैं कि केन्द्र सरकार इस ऑनलाईन सट्टेबाजी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इसे बंद क्यों नहीं कर रही है, उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि केन्द्र सरकार तो ऑनलाईन सट्टेबाजी पर 28 फीसदी जीएसटी लगा चुकी है।
भूपेश बघेल और ईडी इन दोनों के सामने रखे गए तथ्य एक-दूसरे के ठीक खिलाफ हैं। ऐसे में जब राज्य के मुख्यमंत्री केन्द्रीय गृहमंत्री को कार्रवाई की चुनौती देते हैं, तो इस पर भरोसा करना चाहिए। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह इस सट्टेबाजी ऐप को बंद करे, जो कि साइबर कानून के तहत उसके लिए पल भर का काम है। दूसरी बात यह कि यह सट्टेबाजी देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों से चल रही थी, और इन सब जगहों पर कार्रवाई करना भी केन्द्र सरकार के एजेंसियों के हाथ है, फिर चाहे इसके खिलाफ एफआईआर किसी एक राज्य में ही क्यों न दर्ज की गई हो। केन्द्र सरकार के पास दूसरे देशों में जांच करने का भी अधिकार है, और वही अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल से ऐसी कार्रवाई कर सकती है। केन्द्र सरकार की ईडी ने छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के सिलसिले में कई लोगों पर छापे मारे हैं, और कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। ये सारे आरोप बहुत भयानक हैं, राज्य की पुलिस के अफसरों और कर्मचारियों के बारे में ईडी ने जो कुछ कहा है, उसे या तो अदालत में साबित करना चाहिए, या फिर चुनावी राजनीति से परे ऐसे आरोप बंद होने चाहिए। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केन्द्र की मोदी सरकार के साथ तनातनी के संबंध हैं। मुख्यमंत्री के आसपास के दर्जनों लोगों को ईडी ने अपने निशाने पर रखा हुआ है, और बहुत से लोग महीनों से जेल में हैं। ऐसे में जब भूपेश बघेल केन्द्र सरकार को कार्रवाई की चुनौती दे रहे हैं, तो यह जिम्मा अब केन्द्र सरकार की एजेंसियों का है कि वे सारी सच्चाई सामने रखें। राज्य का चुनाव सामने है, और ऐसे में अगर ईडी की कार्रवाई के सुबूत अगर सामने नहीं आते हैं, सिर्फ अदालत में दाखिल उसके आरोप ही हवा में तैरते रहते हैं, तो वह मतदाताओं के साथ ज्यादती होगी। अगर केन्द्र की एजेंसियों के पास कोई सुबूत हैं, तो उन्हें खुलकर सामने रखना चाहिए, उनके आधार पर जो कार्रवाई की जा सकती है वह करनी चाहिए, वरना इसे राजनीतिक आरोप का सामान बनाना ज्यादती होगी।
पिछले दो दिनों से राज्य में यह भी चर्चा है कि ईडी के दर्ज किए गए एक मामले में जेल में बंद, कोयला उगाही माफिया सूर्यकांत तिवारी का नाम भी भाजपा के मोटे आरोप पत्र में नहीं लिखा गया है। अगर ऐसा है तो आरोप पत्र बनाने वाले लोगों को यह जवाब देना चाहिए कि इस माफिया सरगना कहे जाने वाले सूर्यकांत तिवारी का नाम क्या इसलिए छोड़ा गया है कि उसके रमन सरकार के तमाम लोगों के साथ बड़े अंतरंग संबंध थे, और सबके साथ उसकी तस्वीरों के एलबम उसकी गिरफ्तारी के समय से सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। जब कोई आरोप लगाया जाता है, तो लगाने वाले लोग कई बातों के लिए जवाबदेह भी हो जाते हैं। आज भूपेश बघेल के जवाबी हमले के बाद भाजपा की ओर से अमित शाह को ही इन सब बातों का जवाब देना होगा क्योंकि उन्होंने केन्द्र सरकार की एजेंसियों के दायर किए गए मुकदमों के आधार पर आरोप लगाए हैं, और भूपेश बघेल ने उन्हें कार्रवाई करने की चुनौती दी है। लोकतंत्र और छत्तीसगढ़ की जनता के हित में यही होगा कि इन मामलों पर गोलमोल आरोपों के बजाय ठोस सुबूत जनता के सामने रखा जाए, और जनता उसके आधार पर अपना फैसला ले सके।
हमने केन्द्र और राज्य सरकारों की कई जांच एजेंसियों की कार्रवाईयों को ठंडे बस्ते में जाते देखा है, आरोपियों और मुजरिमों के दलबदल से मामले खत्म होते देखा है, अपने पसंदीदा मुजरिमों के खिलाफ मामले को पटरी से उतारते हुए भी देखा है, और ऐसा लगता है कि इस देश में जुर्म की जांच का काम राजनीति का एक विस्तार होकर रह गया है। ऐसे में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को चाहिए कि अब तक जांच में मिले हुए तथ्यों को जनता की समझ में आने लायक भाषा में उसके सामने रखा जाए, ताकि जनता छोटा मुजरिम छांट सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी भाजपा नेताओं पर आरोप वाले कई मामले दर्ज कर रखे हैं, उसे भी तथ्य जनता के सामने रखना चाहिए। अभी दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे के खिलाफ काला चिट्ठा सामने रखा है, हमारा कहना है कि ये दोनों ही पार्टियां जनता के सामने श्वेत पत्र रखें, जिनमें जांच एजेंसियों की सार्वजनिक की गई बातों को सरल भाषा में समझाया जाए, और जनता को फैसला लेने में मदद की जाए। मोटे-मोटे काले कागजों में छपे अभी के ये आरोप पत्र बहुत काम के नहीं हैं, जांच एजेंसियों के अदालत में पेश आरोप पत्र, उनके सुबूत, पुलिस में दर्ज मामलों की स्थिति, इन सब पर दोनों पार्टियों को श्वेत पत्र निकालने चाहिए, जो कि पतले अखबारी कागज पर सस्ते छपे हुए रहें, लेकिन अधिक लोगों तक पहुंच सकें। ऐसा करके कांग्रेस और भाजपा जनता के लोकतांत्रिक अधिकार मजबूत कर सकेंगी।
राखी की शाम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे हुए मंदिर हसौद में मोटरसाइकिल से आ रहे तीन लोगों को शराबियों ने रोका, नौजवान को चाकू की नोक पर रखा, और साथ की दोनों युवतियों को सडक़ के पास खुले में ले जाकर दस लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया। इस खबर के आने के बाद मीडिया और सोशल मीडिया में लोग सहमे हुए दिख रहे हैं, और इस घटना के मुजरिमों को कड़ी सजा देने की मांग शुरू हो गई है, जिसकी जिंदगी दो-चार दिन रह सकती है। उसी इलाके के दस नाौजवानों को पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार कर लिया है, और कहा जा रहा है कि वे ही बलात्कारी थे। दो दिन बाद ही केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी के रायपुर में बड़े कार्यक्रम थे, इसलिए भी उसके ठीक पहले की यह बदनामी शासन-प्रशासन को हिला रही थी। राखी बांधकर लौट रही एक युवती अपने मंगेतर और अपनी छोटी नाबालिग बहन के साथ थी, और शाम के वक्त ही वे इस तरह से सामूहिक बलात्कार की शिकार हुईं। जब उन्हें सडक़ पर रोककर परेशान किया जा रहा था, उसी वक्त पास से और लोग आ-जा रहे थे, लेकिन किसी ने दखल नहीं दी थी।
ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस ने अपने बुनियादी काम की समझ खो दी है। राखी के दिन पूरे प्रदेश में लोग मोटरसाइकिलों पर बहन या बीवी को लेकर आते-जाते हैं, साथ में बच्चे भी रहते हैं, बहुत सी जगहों पर तो लड़कियां अकेले भी दुपहियों पर आती-जाती हैं। जाहिर है कि ऐसे मौके पर छेडख़ानी का खतरा अधिक रहता है। लेकिन पुलिस ने अपने-अपने इलाकों में किसी गश्त का इंतजाम किया हो, ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि पुलिस तथाकथित वीआईपी कार्यक्रमों को जिंदगी का मकसद मानकर चलती है। इस बीच इलाके के गुंडों को ऐसी नौबत माकूल बैठती है, और वे तरह-तरह के जुर्म करते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, छत्तीसगढ़ में पुलिस का जो हाल महादेव ऑनलाईन सट्टेबाजी ऐप के मामले में सुनाई दे रहा है, उससे यह समझ में आता है कि हर महीने 50-50 लाख रूपए तक रिश्वत पाने वाले लोग लाख-पचास हजार की तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी में जान तो नहीं दे देंगे। पूरे प्रदेश का यह हाल सुनाई पड़ता है कि कहीं अवैध रेत खदानों से, कहीं कोयले की चोरी और ट्रांसपोर्ट से, कहीं चोरी के कबाड़ के धंधे से पुलिस अफसरों ने संगठित मुजरिमों के टक्कर का काम शुरू कर दिया है। बहुत से जिलों से यह पुख्ता जानकारी आती है कि किस तरह बड़े पुलिस अफसरों ने मुजरिमों के गिरोह ही अपने कब्जे में ले लिए हैं, और मुजरिम अब उनके सब एजेंट की तरह काम करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में अब यह आम चर्चा चलने लगी है कि किस जिले में पुलिस की कितनी कमाई है, और खासकर बड़ी कुर्सियों की कमाई कितनी है। यह एकदम नई बात भी नहीं है, क्योंकि पिछली रमन सिंह सरकार के समय उनके एक ताकतवर मंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में ही राजधानी रायपुर के उस वक्त के आईजी के बारे में कहा था कि उसकी पांच करोड़ रूपए महीने की कमाई है। यह सिलसिला पहले भी था, लेकिन अब यह आसमान से ऊपर निकलकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक पहुंच गया है। एक तरफ पुलिस राजनीतिक नाराजगी से बचते हुए, सत्तारूढ़ नेताओं और बड़े अफसरों की खुशामद करते हुए अपनी कुर्सी पर बने रहना चाहती है, या अधिक कमाऊ कुर्सी पर जाना चाहती है। दूसरी तरफ वह अपने लिए, और अपने से ऊपर के लोगों के लिए जिस बड़े पैमाने पर संगठित जुर्म कर रही है, उसमें बलात्कार जैसे मामूली जुर्म रोकने के लिए उनके पास वक्त न होना समझ आता है।
आज ही छत्तीसगढ़ के एक बड़े अखबार में यह रिपोर्ट है कि किस तरह राजधानी रायपुर में थानों से महिला डेस्क गायब हो गई है, और महिलाओं के नाम पर बनाए गए संवेदना कक्ष भी बंद हो गए हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि कई थानों महिला आरक्षक भी नहीं है। एक दूसरी खबर जो बहुत से अखबारों में है, वह बताती है कि एक मुस्लिम लडक़ी ने वीडियो बनाकर यह शिकायत की है कि किस तरह उसके घर के बाहर गुंडे परेशानी कर रहे हैं, और जब इसकी शिकायत की गई, तो उस इलाके में प्रशिक्षु आईपीएस ने उसे धमकाया है। यह मामला उसी दिन का बताया जा रहा है जब राजधानी रायपुर अमित शाह से लेकर राहुल गांधी तक की मेजबानी कर रहा था। इन तमाम बातों को मिलाकर देखें तो लगता है कि पुलिस की प्राथमिकता संगठित अपराधों में भागीदारी करने, या उनको खुद चलाने की रह गई है। ऐसा भी लगता है कि प्रदेश की राजनीतिक ताकतों को पूरे प्रदेश में पुलिस के ऐसे रूख से कोई शिकायत नहीं है। इनमें से कई बातें पिछली सरकार के समय भी दिखती थीं, लेकिन अब वे सिर चढक़र बोल रही हैं।
आम बोलचाल की भाषा में दशकों से यह चले आ रहा है कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, या अपराधियों का राजनीतिकरण। अब छत्तीसगढ़ में पुलिस के हाल को देखकर यह लगता है कि पुलिस का माफियाकरण हो चुका है, और शायद बहुत ही कम जिलों में पुलिस वर्दीधारी गुंडा नहीं होगी। लोगों को याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज, जस्टिस अवध नारायण मुल्ला ने यह ठीक ही कहा था कि यूपी की पुलिस दुनिया की सबसे बड़ी अपराधी-गिरोह है। फर्क सिर्फ यही हुआ है कि अब पुलिस का वैसा हाल बहुत से प्रदेशों में हो गया है, और महादेव ऐप जैसे संगठित अपराध की ईडी जांच-रिपोर्ट से आगे बढक़र आम जनता को यह अधिक मालूम है कि पुलिस किस तरह इस जुर्म में भागीदार थी, शायद अब भी है, और दर्जनों पुलिस अफसर सिर्फ इसी एक जुर्म से करोड़पति बन चुके हैं।
जब पुलिस संगठित अपराधों को रोकने से परे हटकर उनमें भागीदार बनने लगी है, और अब खुद करने लगी है, तो फिर आम जनता के साथ बलात्कार पर अधिक चौंकना नहीं चाहिए। मुजरिमों को अपने ही पेशे के लोगों से कोई डर तो रह नहीं गया होगा, और हम इसका सबसे बड़ा नमूना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखते हैं जहां हर दिन सडक़ों पर चाकूबाजी होती है, हर दिन छेडख़ानी होती है, आए दिन छेडख़ानी करने वाले गुंडे रोकने वालों को या लडक़ी के परिवार को घर घुसकर मारते हैं। आज पुलिस की कामयाबी सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल फोन टेक्नालॉजी की मदद से दिखती है। लेकिन इन दो औजारों से पकड़े जाने वाले जुर्म अगर छोड़ दें, तो राजधानी भी बाकी तमाम किस्म के जुर्म और गुंडागर्दी की गवाह है। पुलिस के कुछ बेहतर अफसरों का यह मानना है कि राज्य में पुलिसिंग का जितना पतन हो गया है, अगले कई बरस उसको सुधारना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में प्रदेश की तमाम लोकतांत्रिक ताकतों को यह भी सोचना चाहिए कि सरकार के सबसे ताकतवर इस वर्दीधारी महकमे को अगर सबसे बड़ा मुजरिम भी बनने दिया गया, तो फिर प्रदेश में किसी भी जुर्म को रोकना तभी हो पाएगा, जब उससे पुलिस को कोई संगठित वसूली और उगाही होते नहीं दिखेगी। अब इस नौबत में लोगों को बलात्कार और छेडख़ानी को रोकने की जितनी उम्मीद करना ठीक लगे, वे करते रहें, लोकतंत्र में हर किसी को खुशफहमी में जीने का पूरा हक है।
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। उन्होंने अपनी आत्मकथा के पहले हिस्से के विमोचन समारोह में यह कहकर खलबली मचा दी कि अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने कहा कि भाजपा के पहले पीएम पी.वी.नरसिम्हाराव थे। अब इतिहास तो नरसिम्हाराव को कांग्रेस पीएम के रूप में दर्ज करता है, लेकिन मणिशंकर अय्यर का मंच और माईक से यह कहना लोगों को हैरान कर गया। उन्होंने कहा कि यह बात वे पहले अपनी एक दूसरी किताब में लिख चुके हैं, और इस ताजा किताब में उन्होंने यह नहीं लिखा है, लेकिन वे उस बात पर आज भी अटल हैं कि नरसिम्हाराव भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे। अपनी बात के पीछे का तर्क बताते हुए उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने के वक्त पीएम नरसिम्हाराव जिस शांति से अपने कमरे में पूजा कर रहे थे, उससे जाहिर था कि वे भाजपा के पीएम थे। उन्होंने याद किया कि कैसे जब वे (मणिशंकर) राम-रहीम यात्रा निकाल रहे थे तो नरसिम्हाराव ने उन्हें फोन किया था और कहा था कि उन्हें इस यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे धर्मनिरपेक्षता की मणिशंकर की परिभाषा से असहमत थे। राव का यह कहना था कि मणिशंकर इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि यह हिन्दू देश है। मणिशंकर अय्यर ने इस घटना के बारे में विमोचन समारोह में कहा कि भाजपा बिल्कुल यही कहती है (कि यह हिन्दू देश है), इसलिए भाजपा के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी नहीं नरसिम्हाराव थे।
मणिशंकर अय्यर लिखने-पढऩे वाले हैं, और राजनीति के हिसाब से कुछ असुविधाजनक और तीखी जुबान बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुए उन्होंने कई मौकों पर इतने तीखे विशेषणों का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। अभी भी नरसिम्हाराव के बारे में मणिशंकर अय्यर के बयान के खिलाफ भाजपा ने उन्हें गांधी परिवार का चापलूस करार दिया है कि वे इस परिवार को खुश करने के लिए नरसिम्हाराव की आलोचना कर रहे हैं। यह बात पहले भी चर्चा में रही है कि नरसिम्हाराव के गुजरने पर किस तरह उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उनके शव को श्रद्धांजलि और दिल्ली में अंतिम संस्कार से परिवार को रोका था। ऐसा भी माना जाता है कि सोनिया गांधी नरसिम्हाराव को अधिक पसंद नहीं करती थीं, और नरसिम्हाराव ने विद्याचरण शुक्ल के मार्फत बोफोर्स के मामले को कुरेदने का काम किया था ताकि वह मीडिया में बने रहे, और सोनिया गांधी को शर्मिंदग झेलती रहनी पड़े। खैर, वह बात पार्टी के भीतर की थी जिस पर नरसिम्हराव के परिवार का कोई औपचारिक बयान अभी याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन मणिशंकर अय्यर जो बात कहते हैं वह बात तो कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत से दूसरे नेता भी मानते हैं कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने को प्रधानमंत्री की मौन सहमति थी जिन्होंने तथाकथित साधू-संतों और यूपी के उस वक्त कट्टर हिन्दू सीएम कल्याण सिंह के तथाकथित वायदों पर भरोसा किया। उस वक्त भी अर्जुन सिंह सरीखे भाजपा-संघ के विरोधी, और कुछ वामपंथी रूझान वाले नेताओं ने नरसिम्हाराव को आगाह किया था कि वे गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, और ऐसे लोग खतरा बन सकते हैं। फिर भी नरसिम्हाराव ने हिन्दू संगठनों और ताकतों की बात सुनी थी जिसका नतीजा बाबरी विध्वंस की शक्ल में सामने आया था। अब उस दौर का कांग्रेस पार्टी और केन्द्र सरकार का इतिहास देखा जाए, तो कुछ लोगों ने भीतर से भी नरसिम्हाराव का विरोध किया था, लेकिन वह बहुत दूर तक जा नहीं पाया था। खुद अर्जुन सिंह बाबरी मस्जिद गिराए जाने में नरसिम्हाराव की संदिग्ध भूमिका के खिलाफ इस्तीफा देने का हौसला नहीं जुटा पाए थे।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि मणिशंकर अय्यर जो बात नरसिम्हाराव के बारे में बोल रहे हैं, वह आज भी कांग्रेस के बहुत से नेताओं पर लागू हो रही है। वैसे भी कांग्रेस का इतिहास बताता है कि उसके भीतर हिन्दूवादी ताकतों का एक बड़ा जमावड़ा सर्वोच्च स्तर पर था, और मदन मोहन मालवीय से लेकर राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद तक बहुत से लोग नेहरू की असहमति के बावजूद हिन्दू रीति-रिवाजों को औपचारिक बढ़ावा देते रहते थे। आजादी के तुरंत बाद का वह दौर कुछ अलग इसलिए था कि उस वक्त नए भारत के निर्माण की चुनौती थी, और लोग तरह-तरह की विचारधाराओं के साथ भी तालमेल बिठाने के आदी थे। गांधी और नेहरू कांग्रेस के भीतर भी कई किस्म की असहमति और विरोध झेलते थे, जिसमें कट्टर हिन्दूवादी नेता भी थे।
1992 में प्रधानमंत्री पी.वी.नरसिम्हाराव पर यह तोहमत लगी थी कि उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने को मौन सहमति दी थी। आज भारत के कई प्रदेशों में कांग्रेस के नेता जिस हद तक हिन्दुत्ववादी हो गए हैं, आज अगर 6 दिसंबर 1992 का दिन आए, तो कांग्रेस नेता घर नहीं बैठे रहेंगे, उनमें से बहुत से अयोध्या में सब्बल-कुदाली लिए हुए दिखेंगे। देश की राजनीति में भाजपा जिस फौलादी पकड़ से हिन्दुत्व को जकडक़र रखना चाहती हैं, वैसे ही फौलादी हाथों से बहुत से कांग्रेस नेता धर्मनिरपेक्षता को दूर धकेल भी रहे हैं। देश के कई बड़े कांग्रेस नेता इस बात में भी कामयाब हो गए हैं कि वे प्रियंका गांधी सरीखी प्रमुख कांग्रेस नेता को पूरी तरह से हिन्दुत्व की छत्रछाया में ले जा चुके हैं। अब भाजपा से चुनावी मुकाबले की यह हिन्दूवादी रणनीति कितनी कामयाब होती है, यह आने वाले चुनावों के नतीजों के विश्लेषण से पता चलेगा, लेकिन आज मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के भीतर गिने-चुने नेताओं में से रह गए हैं जो कि साम्प्रदायिकता के खिलाफ खुलकर बात करने से परहेज नहीं करते। हो सकता है कि भाजपा के लिए वे कांग्रेसी कैम्प में एक पसंदीदा काम कर रहे हों, लेकिन हमारा यह भी मानना है कि चुनावी जीत-हार से परे बुनियादी मुद्दों पर नेताओं और पार्टियों की सोच सार्वजनिक रहनी चाहिए, और पारदर्शी रहनी चाहिए। अगर वोट पाने के लिए झूठ बोलना और सच को छुपाना जरूरी हो, तो हम उसके हिमायती नहीं हैं। मणिशंकर अय्यर आज 1992 के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के बारे में जो बोल रहे हैं, वो आज के किन कांग्रेस नेताओं के बारे में 25 बरस बाद बोला जाएगा, यह सोचने की बात है।
देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करने के लिए मोदी सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद होंगे। देश में शायद यह पहला ही मौका होगा कि एक भूतपूर्व राष्ट्रपति को कोई काम दिया जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र की हमारी बहुत मामूली सी समझ यह कहती है कि राष्ट्रपति बनते ही लोग अपनी पार्टी से परे के, गैरराजनीतिक व्यक्ति हो जाते हैं, और कार्यकाल खत्म होने के बाद तो वे पूरी तरह से रिटायर्ड जिंदगी जीते हैं, जिसका खर्च सरकार उठाती है। किसी भूतपूर्व राष्ट्रपति की कोई ऐसी जिंदगी इसके पहले की ऐसी याद नहीं पड़ती है जिसमें उन्होंने सरकार के लिए कोई काम किया हो। लेकिन रामनाथ कोविंद को एक देश एक चुनाव की तैयारी के लिए बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष बनाकर मोदी सरकार ने विपक्षी दलों के सामने भी शिष्टाचार की एक दिक्कत खड़ी कर दी है कि एक भूतपूर्व और दलित राष्ट्रपति से कितनी असहमति जाहिर की जाएगी, कितना विरोध किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि रामनाथ कोविंद के एक बयान की चर्चा की जा रही है कि उन्होंने संसद के एक संयुक्त सत्र में एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। अब यह बात बड़ी बुनियादी समझ की है कि राष्ट्रपति के तमाम औपचारिक भाषण केन्द्रीय मंत्रिमंडल से मंजूर होते हैं। और संसद में उनके दिए गए भाषण केन्द्र सरकार द्वारा लिखे गए रहते हैं, जिन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल पास करके राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति के पास बस इतनी आजादी रहती है कि उस भाषण के किसी पैरा को पढऩा वे छोड़ सकते हैं, लेकिन वह भी लिखित भाषण में तो बंटता ही है। इसलिए संसद में उन्होंने जो भाषण दिया था वह सरकार का ही लिखा हुआ था, और अब उसे उनके विचार बताकर उन्हें ऐसी किसी कमेटी का मुखिया बनाना, यह सब कुछ बड़ा सोचा-समझा लगता है। रामनाथ कोविंद में जाने क्या सोचकर अपनी रिटायर्ड जिंदगी में यह विवाद मोल लिया है, और इसने संविधान के जानकार लोगों को बड़ा निराश भी किया है।
लेकिन केन्द्र सरकार ने एक और राष्ट्रपति का इसी तरह का इस्तेमाल अभी किया है। मौजूदा आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ से लगे हुए ओडिशा की हैं, और छत्तीसगढ़ अभी चुनाव से गुजर रहा है। यहां के आदिवासी इलाकों में आदिवासियों के ईसाई बनने का मुद्दा बहुत बड़ा है, और उसका हिन्दूवादी संगठन जमकर विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ आना, और यहां एक के बाद दूसरे मंदिर में जाना, और एक तथाकथित आध्यात्मिक संगठन में जाना जो कि हिन्दू धर्म से ही जुड़ा हुआ है। दो दिनों में उनके इन तमाम कार्यक्रमों को देखें तो ऐसा लगता है कि वे अपने आदिवासी होने के साथ-साथ अपने हिन्दू होने की बात को भी स्थापित कर रही हैं। यह पूरा कार्यक्रम केन्द्र सरकार की सहमति से बनता है, और इससे आदिवासियों के बीच आदिवासियों के हिन्दू होने की एक बात बिना कहे हुए ही चली जाती है। छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी हिस्से ओडिशा से लगे हुए हैं, और द्रौपदी मुर्मू का नाम वहां पर उनके राष्ट्रपति बनने के वक्त से ही अच्छी तरह जाना-माना है। तमाम आदिवासियों के बीच द्रौपदी मुर्मू के मंदिरों में जाने की तस्वीरें, उसके वीडियो पहुंचे हैं, और उनका जो भी असर हो सकता है, वह हो रहा है।
देश के अलग-अलग राज्यों में मतदान के दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कभी नेपाल के मंदिरों का दौरा करते रहते हैं, तो कभी बांग्लादेश के मठ-मंदिरों का। भारत में तो चुनाव कानूनों की वजह से उन राज्यों में किसी तरह का चुनाव प्रचार नहीं हो सकता, लेकिन मोदी के ऐसे मंदिर भ्रमण हिन्दुस्तानी टीवी चैनलों पर दिनभर छाए रहे, और चुनावी भाषण बिना भी उन्होंने चलते मतदान के बीच चुनाव प्रचार का काम किया। अब मुम्बई में विपक्षी गठबंधन, इंडिया, की बैठक के बीच जिस तरह से संसद के विशेष सत्र की घोषणा हुई, उससे इस गठबंधन की पार्टियों के बीच बात आगे बढऩे के बजाय इन मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई जो कि संसद के विशेष सत्र में सरकार ला सकती है। जिस तरह से मीडिया में चार-पांच गिने हुए मुद्दे एक साथ छा गए, और सरकार की कोई घोषणा तक नहीं हुई है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से ही किसी ने ऐसे संभावित मुद्दों की जानकारी मीडिया तक दी जिससे विपक्षी गठबंधन के बीच खलबली मचे। यह बात जाहिर है कि महिला आरक्षण, या महिला सीटों को बढ़ाना, एक देश-एक चुनाव करवाना जैसे मुद्दों पर विपक्षी गठबंधन की पार्टियां बहुत मजबूती से एकजुट नहीं रह पाएंगी। उनके बीच सैद्धांतिक मतभेद भी होंगे, और क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी क्षेत्रीय मजबूरियां भी होती हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि बिना कोई एजेंडा घोषित किए संसद के इस विशेष सत्र की घोषणा से, और इसके संभवित एजेंडा की उठ खड़ी हुई चर्चा से खबरें गठबंधन से हट गईं, और संसद के होने वाले सत्र पर जा टिकीं।
इन तमाम बातों को मिलाकर देखने की जरूरत है कि एक दलित पूर्व राष्ट्रपति को उसके एक ऐसे भाषण के हवाले से एक कमेटी का मुखिया बनाने का अभूतपूर्व काम किया गया, जो भाषण खुद केन्द्र सरकार का लिखा हुआ था। एक आदिवासी राष्ट्रपति को चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में हिन्दू मंदिरों के दौरे पर भेज दिया गया, और इस राज्य में एक तिहाई आबादी आदिवासियों की हैं। विपक्षी गठबंधन की बैठक के बीच संसद के विशेष सत्र की घोषणा कर दी गई, और किसी एजेंडा की घोषणा के बिना देश का मीडिया इस विशेष सत्र को मास्टर स्ट्रोक और सर्जिकल स्ट्राईक लिखने लगा है। इन तमाम बातों के पीछे मोदी सरकार का एक विशाल जनधारणा प्रबंधन दिखता है। हिन्दुस्तानी लोकतंत्र में शायद ही किसी प्रधानमंत्री और सरकार ने खुद ऐसे अवसर गढ़े, और उनका भरपूर दोहन भी किया। विपक्षी गठबंधन को अगर मोदी से पार पाना है, तो मोदी के परसेप्शन मैनेजमेंट का अध्ययन करने के लिए उसे अपनी एक अघोषित कमेटी बनानी चाहिए।
मोदी सरकार ने 18 सितंबर से संसद का पांच दिनों का एक विशेष सत्र आयोजित किया है जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन लोगों का अंदाज है कि सरकार की तरफ से कुछ बड़े फेरबदल वाले संसदीय काम इस सत्र में करवाए जा सकते हैं। इसके लिए विशेष कानून बनाना हो, या मौजूदा कानून में कोई फेरबदल करना हो तो वह सब इन पांच दिनों में हो सकता है। सत्तारूढ़ गठबंधन का जो बाहुबल है, उसके चलते लोकसभा में उसे विपक्ष के किसी समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ राज्यसभा में उसका समर्थन करने के लिए कुछ गैरएनडीए, गैर-इंडिया पार्टियां मौजूद हैं, और सरकार को संसदीय बहुमत जुटाने में वहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली के जानकार राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि देश में सारे चुनाव एक साथ करवाने का एक विधेयक लाया जा सकता है, और इसकी बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तो बरसों से करते ही आए हैं। उनके पहले से भी यह बात कई दूसरे लोग भी बोल चुके हैं कि संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसके अलावा म्युनिसिपल और पंचायतों के चुनाव भी इन्हीं के साथ करवाए जा सकते हैं, ताकि चुनाव का खर्च घटे, और वोटर पांच बरस में एक बार वोट डालने जाए। देश में आजादी के बाद चार आम चुनाव ऐसे थे जिनमें लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ हुए। उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने का सिलसिला चला, और वहां राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद जब दुबारा चुनाव हुए तो उन सदनों का पांच बरस का कार्यकाल दूसरे राज्यों से अलग हो गया। अब देश में हर बरस कुछ राज्यों में चुनाव चलते ही रहते हैं। इसलिए पहले भी यह मांग उठी थी, बहुत अलग-अलग पार्टियों के बहुत से लोग इसके पक्ष में थे, और हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हमने भी इसी जगह पर देश में एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया था।
इसकी कई वजहें हैं, जो कि आज मोदी की आक्रामक छवि और उनकी अभूतपूर्व लोकप्रियता के सामने दब जाती हैं। आज जब मोदी यह बात करते हैं तो लगता है कि वो पूरे देश के चुनावों को प्रभावित करने के लिए अपना चेहरा पोस्टरों पर रखना चाहते हैं, फिर चाहे वह संसद का चुनाव हो, या विधानसभा का। लेकिन लोकतंत्र में सिद्धांत और कानून किसी व्यक्ति को देखकर तय करना ठीक नहीं है। यह बात सही है कि आज मोदी बाकी पार्टियों के नेताओं के मुकाबले वोटरों के बड़े तबके में अधिक लोकप्रिय हैं, लेकिन देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं नेताओं के चले जाने के बाद भी कायम रहती हैं। नेहरू सबसे लोकप्रिय थे, लेकिन 1964 में वे भी चले गए थे, और उनके बाद भी लोकसभा-विधानसभा के चुनाव साथ में हुए। इंदिरा गांधी द्वारा विधानसभाओं को भंग करने की वजह से यह सिलसिला टूटा। फिर जिन लोगों को यह डर लगता है कि मोदी की तस्वीर राज्यों से भी बाकी पार्टियों को बेदखल करने में कामयाब हो जाएगी, उन्हें याद रखना चाहिए कि देश में कई ऐसे चुनाव हुए जिसमें एक दिन एक मतदान केन्द्र पर लोगों को दो बैलेट दिए गए, उन्होंने राज्य के लिए एक पार्टी को चुना, और केन्द्र के लिए किसी दूसरी पार्टी को। गैरभाजपाई पार्टियों को यह भी सोचना चाहिए कि आज जिन राज्यों में भाजपा हारी थी, वहां भी लोकसभा चुनाव में मोदी का एकतरफा बोलबाल था। ऐसे में अगर साथ में चुनाव होते, तो हो सकता है कि राज्य में लोकप्रिय पार्टी का कुछ असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता।
लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से खर्च में कटौती तो एक बात है, राजनीतिक दलों पर से मतदाताओं को खुश करने का दबाव भी इससे घटेगा, और उससे भी लुभावने राजनीतिक कार्यक्रमों को सरकारी खर्च से पूरा करने का सिलसिला थमेगा। आज चुनाव तो पांच राज्यों में विधानसभा के होने हैं, लेकिन केन्द्र सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए चाहे-अनचाहे रसोई गैस के दाम घटाए। ऐसे और भी कई कार्यक्रमों, कई रियायतों की घोषणा अभी हो सकती है, और हर बरस के किसी न किसी चुनाव को देखते हुए देश भर में ऐसी कई रियायतें दी जाती हैं। रियायतों से जनकल्याण होने की बात तक तो ठीक है, लेकिन अगर उन्हें सिर्फ लुभाने के लिए दिया जा रहा है, तो इससे देश की आर्थिक योजना प्रभावित होती है। एक साथ चुनावों से देश और प्रदेशों की सरकारें लंबे पांच बरसों के कार्यकाल के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकेंगी, उन पर अधिक गंभीरता से अमल कर सकेंगी।
अगर लोकसभा में, राज्यसभा में विचार-विमर्श और बहस का माहौल रहेगा, तो इस बारे में भी वहां बहस होगी, और अलग-अलग पार्टियों के तर्क भी सामने आएंगे। यह एक दिलचस्प मामला है। और केन्द्र सरकार के एक फैसले ने इसे और दिलचस्प बना दिया है। मोदी सरकार की तरफ से खबर आई है कि उसने एक देश एक चुनाव पर एक कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। यह कुछ हैरानी की बात है। हमारी मोटी समझ यह कहती है कि राष्ट्रपति रिटायर होने के बाद एक सम्माननीय नागरिक होकर रह जाते हैं, उनके किसी तरह के सरकारी या संवैधानिक काम नहीं हो सकते। ऐसे में उन्हें ऐसी किसी कमेटी का अध्यक्ष बनाना कुछ हैरान करता है, क्योंकि इस कमेटी में कई राजनीतिक दलों और दूसरे तबकों की असहमति भी आ सकती है, वहां पर गर्मागर्म बहस भी हो सकती है जो कि किसी भूतपूर्व राष्ट्रपति के लिए शायद शोभनीय न हो। फिर भी केन्द्र सरकार ने अगर ऐसा किया है तो उसकी सोच को जानना भी दिलचस्प होगा।
एक देश एक चुनाव का पहला असर यह देखने मिल सकता है कि पांच राज्यों के चुनावों के साथ लोकसभा के चुनाव समय के पहले हो जाएं, या फिर विधानसभाओं के चुनाव कुछ देर से हों। ऐसी चर्चा है कि मोदी का जादू घट रहा है, और वह एक सीमा से अधिक घट जाए, उसके पहले भाजपा अगला चुनाव चाहती है। हो सकता है ऐसी भी कोई नीयत ऐसे किसी संविधान संशोधन, या नए कानून के पीछे हो। इसके साथ-साथ कुछ और मामलों पर भी इस सत्र में चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है, जिनमें संसद की सीटें बढ़ाकर उन्हें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की भी बात सुनाई पड़ रही है, लेकिन उस बारे में एक लंबी चर्चा अलग से।
सोशल मीडिया राखी के मौके पर भाई-बहनों की फोटो से भरा हुआ है। छोटे-छोटे बच्चों की तस्वीरें देखना तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़े लोगों की तस्वीरें देखते हुए कुछ हैरानी होती है कि क्या बालिग हो चुके भाई जिन सगी बहनों से राखी बंधवा रहे हैं, क्या उन्हें बाप की जायदाद में बराबरी का हक दे रहे होंगे? और राखी का तो पारंपरिक मतलब ही यही है कि बहन की रक्षा करना। बहन-भाई को राखी बांधती है ताकि वह हर हालत में उसकी रक्षा करे। अभी हम कुछ देर के लिए इस परंपरागत मतलब की लैंगिक असमानता को किनारे रख रहे हैं, और यह मान रहे हैं कि भारतीय समाज में हिफाजत की जरूरत एक लडक़ी और महिला को ही अधिक है, और इसके लिए राखी की यह परंपरा शुरू हुई होगी, जो अब तक चल रही है। एक छोटा हिस्सा ऐसे भाई-बहन का भी हो सकता है जिसमें भाई कमजोर हालत में हो, और बहन उसकी मददगार हो, वैसे मामलों में यह भी कहा जा सकता है कि उस भाई को अपनी बहन को राखी बांधनी चाहिए ताकि वह भाई की रक्षा कर सके। अभी दो दिन पहले राखी के मौके पर एक खबर आई थी कि किस तरह दोनों खराब किडनी वाले एक आदमी को उसकी बहन अपनी किडनी दे रही है। हमारे पास इसके कोई आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन ऐसा अंदाज जरूर है कि अंगदान करने वाले लोगों में महिलाएं ही अधिक रहती होंगी, फिर वे चाहे पति, भाई, पिता, या पुत्र को अंग देती हों। जाहिर तौर पर भाई-बहनों के बीच बहन ही अधिक काम आती होगी, और भाई की जिंदगी बचाने की सोच और जिम्मेदारी उसी पर रहती होगी।
लेकिन आमतौर पर बिना मेडिकल-जरूरत के जिन परिवारों में भाई-बहन के बीच रिश्ते तभी तक बहुत अच्छे रहते हैं जब तक बहन बाप की दौलत में अपना हक नहीं मांगती। भारत के कानून में लडक़ी को बराबरी का हक दिया गया है, और आमतौर पर लड़कियां भाई, और उसके पास रहने वाले बूढ़े माता-पिता के दिमागी सुख-चैन के लिए अपने हक को छोडक़र चुप रहती हैं, और संपत्ति पर दावा नहीं करती हैं। भारतीय, कम से कम हिन्दू समाज में उससे यही उम्मीद भी की जाती है, और समाज खुद होकर यह मान लेता है कि चूंकि लडक़ी की शादी में खर्च किया गया था, दहेज दिया गया था, इसलिए उसे अब आगे और कुछ देने की जरूरत नहीं है। यह बात पूरी तरह फर्जी रहती है क्योंकि शादी का खर्च और दहेज इन दोनों को परिवार अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, न कि लडक़ी के हक की तरह। कानून और अदालतों ने बार-बार यह साफ किया है कि इन चीजों को लडक़ी का हक मानकर आगे हाथ खींच लेना कानूनी नहीं है। लेकिन हिन्दू समाज ने इसका एक तोड़ निकाल लिया है, और पैसे वाले परिवारों की बेटियां जब शादी होकर बाहर जाती हैं, तो उनसे यह लिखवा लिया जाता है कि उसे पिता की संपत्ति में से कुछ नहीं चाहिए। यह सिलसिला पूरी तरह खत्म होना चाहिए, और लडक़ी को ऐसे हित त्याग करने का कोई हक नहीं रहना चाहिए क्योंकि उस लडक़ी की शादी के बाद भी उसे मां-बाप की दौलत में से जो मिलना है उस पर उसके बच्चों का भी हक रहता है, और उन बच्चों के हक त्याग करने का उसे कोई हक नहीं है।
राखी के मौके पर हम इसकी चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि साड़ी, लिफाफा, घड़ी, मोबाइल फोन, या कोई छोटा-मोटा गहना देकर भाई-भाभी इस बात की गारंटी चाहते हैं कि बहन बाप की दौलत में हक का बखेड़ा खड़ा न करे। आज राखी की प्रथा या परंपरा का कोई भी मतलब अगर है, तो वह यही है कि भाई बहन की हर तरह की हिफाजत करे। यह हिफाजत बाहर के गुंडों से बहन को बचाने तक सीमित नहीं है, यह उसके कानूनी हक पर डाका डालने वाले भाई पर भी लागू होती है, जिससे बहन को बचाने की जिम्मेदारी उसी डकैत भाई पर आती है। आज हालत यह है कि हिन्दू समाज में कोई भी लडक़ी अगर कानूनी हक की बात करेगी, तो भाई-भाभी तो दूर की बात रहे, मां-बाप भी उसके भावनात्मक शोषण में जुट जाएंगे, और उसे मरने-मारने की धमकी देने लगेंगे। मां-बाप जान देने पर उतारू दिखें, तो तमाम लड़कियां अपने हक छोडऩे के लिए तैयार हो जाएंगी। इसलिए इस बारे में कानून को ही कुछ करना होगा।
हमारा यह मानना है कि देश में ऐसा कानून बनना चाहिए कि कम से कम आयकरदाता परिवार के लिए यह बंदिश हो जाए कि लडक़ी की शादी के साथ ही अगले बरस के इंकम टैक्स रिटर्न, या किसी और टैक्स कागजात में उस परिवार को लडक़ी के हक देने की जानकारी देना जरूरी हो जाए, जमीन-जायदाद का ट्रांसफर एक या दो बरस के भीतर हो जाए, और ऐसे तमाम कागजात सरकार के किसी विभाग में दाखिल करने की मजबूरी हर परिवार पर लाद दी जाए। समाज में कई किस्म के सुधार बिना कड़े कानूनों के लागू नहीं हो सकते। समाज और परिवार तो बाल विवाह करवाने पर उतारू रहते थे, और हिन्दू समाज कन्या भ्रूण हत्या के लिए भी कुख्यात रहा है। जब तक पूरे के पूरे ससुराल को जेल भेजने के कानून पर कड़ाई से अमल नहीं होने लगा, तब तक दहेज-हत्याएं आए दिन की बात थीं, और कड़े कानून के साथ-साथ उस पर कड़े अमल की कानूनी बंदिश की वजह से परिवारों ने बहू को जलाकर मारना, या प्रताडि़त करके आत्महत्या को मजबूर करना बंद किया है। ऐसा ही कड़ा कानून लडक़ी के हक को लेकर बनाने की जरूरत है।
आज सोशल मीडिया पर जितने लोग रक्त संबंध वाली सगी बहन से राखी बंधवाते हुए तस्वीरें पोस्ट करते हैं, उनसे यह भी पूछना चाहिए कि बालिग और शादीशुदा बहन के हक तो उन्होंने जरूर ही दे दिए होंगे, और अगर नहीं दिए होंगे तो राखी की जिम्मेदारी का यह तकाजा है कि वे जल्द से जल्द बहन को यह हक दिलवाएं, मां-बाप न भी चाहें, तो भी वे उनसे लडक़र बहन को जायदाद में बराबरी का हक दिलवाएं। भारत की अदालतों का जो हाल है, उसमें यह साफ है कि लडक़ी मां-बाप और भाई के खिलाफ अदालत पहुंचकर इंसाफ पाने की लड़ाई आसानी से नहीं लड़ सकती। उस पर सामाजिक दबाव भी रहेगा। इसलिए कानून के साथ-साथ सामाजिक दबाव की नौबत भी बदलनी होगी, और जिस समाज में जो सुधार की बात करने वाले लोग हैं, उन्हें लड़कियों के कानूनी हक की बात भी उठानी चाहिए।
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। उन्होंने अपनी आत्मकथा के पहले हिस्से के विमोचन समारोह में यह कहकर खलबली मचा दी कि अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने कहा कि भाजपा के पहले पीएम पी.वी.नरसिम्हाराव थे। अब इतिहास तो नरसिम्हाराव को कांग्रेस पीएम के रूप में दर्ज करता है, लेकिन मणिशंकर अय्यर का मंच और माईक से यह कहना लोगों को हैरान कर गया। उन्होंने कहा कि यह बात वे पहले अपनी एक दूसरी किताब में लिख चुके हैं, और इस ताजा किताब में उन्होंने यह नहीं लिखा है, लेकिन वे उस बात पर आज भी अटल हैं कि नरसिम्हाराव भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे। अपनी बात के पीछे का तर्क बताते हुए उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने के वक्त पीएम नरसिम्हाराव जिस शांति से अपने कमरे में पूजा कर रहे थे, उससे जाहिर था कि वे भाजपा के पीएम थे। उन्होंने याद किया कि कैसे जब वे (मणिशंकर) राम-रहीम यात्रा निकाल रहे थे तो नरसिम्हाराव ने उन्हें फोन किया था और कहा था कि उन्हें इस यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे धर्मनिरपेक्षता की मणिशंकर की परिभाषा से असहमत थे। राव का यह कहना था कि मणिशंकर इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि यह हिन्दू देश है। मणिशंकर अय्यर ने इस घटना के बारे में विमोचन समारोह में कहा कि भाजपा बिल्कुल यही कहती है (कि यह हिन्दू देश है), इसलिए भाजपा के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी नहीं नरसिम्हाराव थे।
मणिशंकर अय्यर लिखने-पढऩे वाले हैं, और राजनीति के हिसाब से कुछ असुविधाजनक और तीखी जुबान बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुए उन्होंने कई मौकों पर इतने तीखे विशेषणों का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। अभी भी नरसिम्हाराव के बारे में मणिशंकर अय्यर के बयान के खिलाफ भाजपा ने उन्हें गांधी परिवार का चापलूस करार दिया है कि वे इस परिवार को खुश करने के लिए नरसिम्हाराव की आलोचना कर रहे हैं। यह बात पहले भी चर्चा में रही है कि नरसिम्हाराव के गुजरने पर किस तरह उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उनके शव को श्रद्धांजलि और दिल्ली में अंतिम संस्कार से परिवार को रोका था। ऐसा भी माना जाता है कि सोनिया गांधी नरसिम्हाराव को अधिक पसंद नहीं करती थीं, और नरसिम्हाराव ने विद्याचरण शुक्ल के मार्फत बोफोर्स के मामले को कुरेदने का काम किया था ताकि वह मीडिया में बने रहे, और सोनिया गांधी को शर्मिंदग झेलती रहनी पड़े। खैर, वह बात पार्टी के भीतर की थी जिस पर नरसिम्हराव के परिवार का कोई औपचारिक बयान अभी याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन मणिशंकर अय्यर जो बात कहते हैं वह बात तो कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत से दूसरे नेता भी मानते हैं कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने को प्रधानमंत्री की मौन सहमति थी जिन्होंने तथाकथित साधू-संतों और यूपी के उस वक्त कट्टर हिन्दू सीएम कल्याण सिंह के तथाकथित वायदों पर भरोसा किया। उस वक्त भी अर्जुन सिंह सरीखे भाजपा-संघ के विरोधी, और कुछ वामपंथी रूझान वाले नेताओं ने नरसिम्हाराव को आगाह किया था कि वे गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, और ऐसे लोग खतरा बन सकते हैं। फिर भी नरसिम्हाराव ने हिन्दू संगठनों और ताकतों की बात सुनी थी जिसका नतीजा बाबरी विध्वंस की शक्ल में सामने आया था। अब उस दौर का कांग्रेस पार्टी और केन्द्र सरकार का इतिहास देखा जाए, तो कुछ लोगों ने भीतर से भी नरसिम्हाराव का विरोध किया था, लेकिन वह बहुत दूर तक जा नहीं पाया था। खुद अर्जुन सिंह बाबरी मस्जिद गिराए जाने में नरसिम्हाराव की संदिग्ध भूमिका के खिलाफ इस्तीफा देने का हौसला नहीं जुटा पाए थे।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि मणिशंकर अय्यर जो बात नरसिम्हाराव के बारे में बोल रहे हैं, वह आज भी कांग्रेस के बहुत से नेताओं पर लागू हो रही है। वैसे भी कांग्रेस का इतिहास बताता है कि उसके भीतर हिन्दूवादी ताकतों का एक बड़ा जमावड़ा सर्वोच्च स्तर पर था, और मदन मोहन मालवीय से लेकर राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद तक बहुत से लोग नेहरू की असहमति के बावजूद हिन्दू रीति-रिवाजों को औपचारिक बढ़ावा देते रहते थे। आजादी के तुरंत बाद का वह दौर कुछ अलग इसलिए था कि उस वक्त नए भारत के निर्माण की चुनौती थी, और लोग तरह-तरह की विचारधाराओं के साथ भी तालमेल बिठाने के आदी थे। गांधी और नेहरू कांग्रेस के भीतर भी कई किस्म की असहमति और विरोध झेलते थे, जिसमें कट्टर हिन्दूवादी नेता भी थे।
1992 में प्रधानमंत्री पी.वी.नरसिम्हाराव पर यह तोहमत लगी थी कि उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने को मौन सहमति दी थी। आज भारत के कई प्रदेशों में कांग्रेस के नेता जिस हद तक हिन्दुत्ववादी हो गए हैं, आज अगर 6 दिसंबर 1992 का दिन आए, तो कांग्रेस नेता घर नहीं बैठे रहेंगे, उनमें से बहुत से अयोध्या में सब्बल-कुदाली लिए हुए दिखेंगे। देश की राजनीति में भाजपा जिस फौलादी पकड़ से हिन्दुत्व को जकडक़र रखना चाहती हैं, वैसे ही फौलादी हाथों से बहुत से कांग्रेस नेता धर्मनिरपेक्षता को दूर धकेल भी रहे हैं। देश के कई बड़े कांग्रेस नेता इस बात में भी कामयाब हो गए हैं कि वे प्रियंका गांधी सरीखी प्रमुख कांग्रेस नेता को पूरी तरह से हिन्दुत्व की छत्रछाया में ले जा चुके हैं। अब भाजपा से चुनावी मुकाबले की यह हिन्दूवादी रणनीति कितनी कामयाब होती है, यह आने वाले चुनावों के नतीजों के विश्लेषण से पता चलेगा, लेकिन आज मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के भीतर गिने-चुने नेताओं में से रह गए हैं जो कि साम्प्रदायिकता के खिलाफ खुलकर बात करने से परहेज नहीं करते। हो सकता है कि भाजपा के लिए वे कांग्रेसी कैम्प में एक पसंदीदा काम कर रहे हों, लेकिन हमारा यह भी मानना है कि चुनावी जीत-हार से परे बुनियादी मुद्दों पर नेताओं और पार्टियों की सोच सार्वजनिक रहनी चाहिए, और पारदर्शी रहनी चाहिए। अगर वोट पाने के लिए झूठ बोलना और सच को छुपाना जरूरी हो, तो हम उसके हिमायती नहीं हैं। मणिशंकर अय्यर आज 1992 के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के बारे में जो बोल रहे हैं, वो आज के किन कांग्रेस नेताओं के बारे में 25 बरस बाद बोला जाएगा, यह सोचने की बात है।