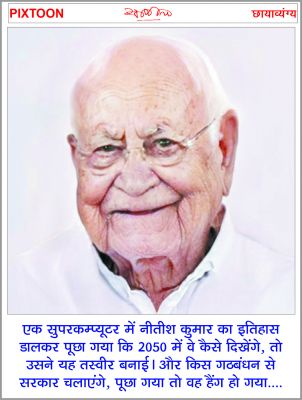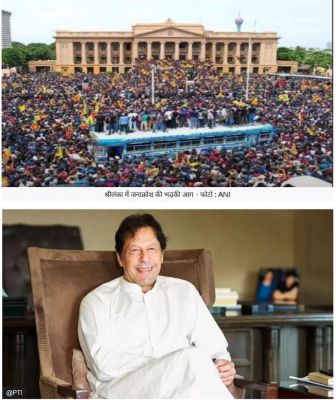संपादकीय
यह बात सुनने में कुछ हैरान कर सकती है कि अदना सी दवा की टेबलेट पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बताया गया है कि पिछले दो दौर की कोरोना महामारी के दौरान बुखार और बदन दर्द में काम आने वाली पैरासिटामॉल टेबलेट के एक खास ब्रांड डोलो-650 की बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी ने डॉक्टरों को रिश्वत दी, ताकि वे इसे अंधाधुंध लिखें। अदालत में यह जनहित याचिका फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दायर की है, जिसका कहना है कि इस कंपनी ने डॉक्टरों को रिश्वत देने पर हजार करोड़ रूपये खर्च किए हैं। कंपनी ने इस खर्च को गलत बताया है और कहा है कि यह कोरोना के दौरान का खर्च नहीं है, यह पिछले कई बरसों का मार्केटिंग का खर्च है। अभी यह मामला अदालत में चलना है, और जज भी इसे गंभीरता से ले रहे हैं। अदालत ने उपहारों के नाम पर डॉक्टरों को दी गई रिश्वत पर कंपनी से जानकारी मांगी है। कुछ समय पहले आयकर विभाग ने भी यह दवा बनाने वाली कंपनी के 9 राज्यों के 36 ठिकानों पर छापा मारा था।
लेकिन हम आज की बात को इसी एक दवा पर शुरू और खत्म करना नहीं चाहते, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पर सुनवाई कर ही रही है, और वहां से कोई न कोई नतीजा सामने आएगा। हम चिकित्सा और दवा कारोबार में फैले हुए भारी भ्रष्टाचार की बात जरूर करना चाहते हैं जो कि बहुत ही संगठित है, इस कारोबार से जुड़े लोगों की नजरों में हैं, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं होती है। बड़े-बड़े कामयाब कारोबारी-अस्पताल और डॉक्टर मरीज लेकर आने वाले दलालों को कमीशन देते हैं, मरीज भेजने वाले छोटे डॉक्टरों को इलाज के बाद की निगरानी के नाम पर चेक से भुगतान करते हैं। इसके अलावा तरह-तरह की जांच करने वाले जो मेडिकल सेंटर हैं, वे भी अपने को मरीज भेजने वाले लोगों को संगठित तरीके से कमीशन देते हैं। यह पूरा कारोबार चिकित्सकों के संगठनों की नीतियों के खिलाफ है, वहां से कई बार नोटिस जारी होते भी हैं, लेकिन जिंदगी से जुड़े इस पेशे और कारोबार से इस गंदगी को दूर करने की कोई ठोस कोशिश दिखाई नहीं देती है।
दरअसल चिकित्सा से जुड़ा हुआ यह पूरा कारोबार निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में होने वाले पूरी तरह से संगठित भ्रष्टाचार से शुरू होता है, और सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए दी जाने वाली रिश्वत पर खत्म होता है। फिर एक बात यह भी है कि इलाज के तौर-तरीके, जांच का फैसला, और दवाओं की पसंद, इन सबमें अलग-अलग डॉक्टरों की अलग-अलग सोच हो सकती है, और किसी को भी तेजी से तब तक खारिज नहीं किया जा सकता, जब तक उनके इन फैसलों को किसी रिश्वत से प्रभावित साबित न किया जा सके। अभी सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो संगठन कंपनी और डॉक्टरों के बीच बेईमान रिश्ते का आरोप लेकर पहुंचा है, वह एक जागरूक संगठन है, और वह समय-समय पर कंपनियों की बेईमानी के खिलाफ लड़ते भी रहता है। हिन्दुस्तान में मरीजों का तो कोई संगठन न है, और न बन सकता, लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का संगठन ही दवाओं की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ हर समय आवाज उठाते रहता है, और दवा उद्योग के दूसरे नाजायज तौर-तरीकों का भांडाफोड़ भी करता है। इसलिए ऐसे संगठन की कोशिशों का साथ देने की जरूरत है ताकि वह मरीजों के हित के लिए लड़ सके, और दवा कंपनियों और डॉक्टरों के अनैतिक गठबंधन के खिलाफ भी।
आज हिन्दुस्तान में निजी चिकित्सा कारोबार लगातार बढ़ते चल रहा है, और केन्द्र और राज्य सरकारें भी मरीजों को दिए जाने वाले स्वास्थ्य बीमा कार्ड को इन अस्पतालों से जोड़ते जा रही हैं। नतीजा यह है कि आज सरकारी अस्पताल लगातार उपेक्षित हो रहे हैं, और निजी चिकित्सा कारोबार बढ़ते ही जा रहा है। जब गरीब बीमार होते हैं, तो अगर सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड उस खर्च को नहीं उठा पाता, तो लोग गहने और मकान बेचकर भी इलाज करवाते हैं। ऐसे में उनके साथ अगर दवाओं के रेट को लेकर बेईमानी होती है, गैरजरूरी जांच करवाई जाती है, जांच में कमीशन लिया जाता है, तो इन सबका भांडाफोड़ होना चाहिए। लोगों को याद होगा कि कुछ बरस पहले जब कई अस्पतालों ने अपने दलालों के मार्फत यह पाया कि लोगों के स्वास्थ्य बीमा कार्ड पर अभी और इलाज करवाने लायक रकम बाकी है, तो कुछ अस्पतालों ने गांव के गांव की महिलाओं को उठवा लिया, और उनकी उम्र देखे बिना भी उनके गर्भाशय निकाल दिए गए थे। अस्पतालों ने तो छप्पर फाडक़र कमाई कर ली थी, लेकिन बाद में जब यह पूरी धोखाधड़ी उजागर हुई तो कई डॉक्टरों और अस्पतालों को ब्लैकलिस्टेड किया गया था, और उनका कारोबार रोका गया था। इसलिए सरकारी स्वास्थ्य बीमा जहां सबसे गरीब लोगों के लिए मुफ्त इलाज का एक जरिया है, वहीं गैरजरूरी इलाज करके गरीबों के बदन का नुकसान भी किया जाता है, और सरकार को चूना भी लगाया जाता है। लोगों को याद होगा कि कुछ अरसा पहले मेडिकल कॉलेजों के दाखिलों को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ाया था, और मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने वाली कमेटी एमसीआई में भी फेरबदल किया गया था। आज जरूरत यही है कि जिस तरह दवा प्रतिनिधियों के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट तक पहल की है, बाकी सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी चिकित्सा कारोबार की बाकी गड़बडिय़ों के खिलाफ पहल करनी चाहिए, और जरूरत हो तो स्टिंग ऑपरेशन भी करना चाहिए। देश की राजधानी में यह बात आम प्रचलित है कि निजी मेडिकल कॉलेजों से लेकर निजी अस्पतालों, और दवा कंपनियों तक के खेमे सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में करने की अपार ताकत रखते हैं। ऐसी लॉबियों की मर्जी के खिलाफ कुछ कर पाना सरकारों के लिए भी आसान नहीं रहता है। ऐसे में सुबूतों और स्टिंग ऑपरेशनों के साथ अदालतों तक जनहित याचिका लेकर जाना एक असरदार तरीका हो सकता है।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
हिन्दुस्तान के हजारों बरस पुराने कहे जाने वाले कई किस्म के धर्म और दूसरे ग्रंथों में महिलाओं के खिलाफ जितनी हिंसक बातें लिखी गई हैं, जिनका हिन्दुस्तान में खुलकर इस्तेमाल भी होता है, उन बातों ने हिन्दुस्तान की अदालतों के जजों के दिल-दिमाग पर बहुत गहरा असर किया हुआ है। और यह असर कभी-कभार किसी एक मामले में दिखता है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसी सोच वाले लोग अगर फैसले कर रहे हैं, तो वे फैसले किस कदर महिला-विरोधी होंगे। केरल के एक जिले कोझीकोड के एक जज ने यौन उत्पीडऩ के एक मामले में अभियुक्त को जमानत दे दी क्योंकि उसका यह तर्क था कि शिकायतकर्ता महिला ने उस वक्त उत्तेजक कपड़े पहन रखे थे। मतलब यह कि अगर किसी महिला के कपड़े उत्तेजक हैं, तो वह महिला बलात्कार के लायक है। यह जज एस. कृष्णकुमार इसके दस दिन पहले यौन उत्पीडऩ के एक दूसरे मामले में भी आरोपी को जमानत दे चुका है, और उसने लिखा था- यह मानना विश्वास से बिल्कुल परे है कि अभियुक्त ने यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि पीडि़ता दलित है, उसे छुआ होगा।
इन दो आदेशों ने इस जज की सोच भयानक स्तर पर महिला-विरोधी भी है, और दलित-विरोधी भी है। वह महिला के कपड़ों की पसंद के आधार पर उसे एक किस्म से बलात्कार के लायक पा रहा है, और दूसरी तरफ एक दलित महिला के बारे में कह रहा है कि उसे दलित जानते हुए भी कैसे कोई छू सकता है? जज का नजरिया तालिबानों सरीखा दिखता है जो कि महिला की पोशाक तय कर रहे हैं। लेकिन यह अकेला जज ऐसा नहीं है, अभी हफ्ते भर पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट की एक महिला जज प्रतिभा एम.सिंह के एक बयान के खिलाफ बहुत सी महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर बयान दिया था जिसमें इस जज ने मनुस्मृति की वजह से भारतीय महिला को सम्मानजनक स्थान मिलने की बात कही थी। मनुस्मृति की चर्चा हिन्दुस्तान में महिलाओं को नियंत्रित करने वाली सोच की तरह होती है, और उसमें महिलाओं के लिए बहुत ही अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं। ऐसे में अगर हाईकोर्ट की एक जज मनुस्मृति से प्रभावित है तो जाहिर है कि उसके फैसले इस सोच से प्रभावित होंगे। मनुस्मृति के मुताबिक एक महिला को पुरूष द्वारा सुरक्षित किया जाता है। जब वह बालिका है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उसके पिता की है, शादी के बाद वह अपने पति की जिम्मेदारी है, और अगर वह विधवा हो जाए तो वह उसके पुत्र की जिम्मेदारी है। मनुस्मृति महिलाओं के न करने के छह काम गिनाती है जिनमें से एक शराब पीना है। महिलाओं को बिना काम के इधर-उधर घूमने की मनाही की गई है। महिलाओं को बेवक्त और देर तक सोने की मनाही की गई है। मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखा गया है कि वे हमेशा दूसरे मर्दों को आकर्षित करने और संभोग के लिए आतुर रहती हैं। वे अपने पति के प्रति भी वफादार नहीं रहतीं। लेकिन इस तरह की अनगिनत भेदभाव की बातें उसमें महिलाओं के खिलाफ हैं, और इसके साथ-साथ मनुस्मृति बहुत बुरी तरह ब्राम्हणवादी और पुरूषवादी सोच भी है। इसमें शूद्रों को नीच माना गया है, और कहा गया है कि अगर कोई शूद्र ब्राम्हण को धर्मउपदेश दे, तो राजा को उसके मुंह और कानों में खौलता हुआ तेल डलवा देना चाहिए। शूद्रों के पास सम्पत्ति होने का भी विरोध किया गया है, शूद्र अगर ब्राम्हण या उसकी जाति का नाम बदतमीजी से ले, तो उसके मुंह में दस अंगुल लंबी लोहे की दहकती हुई कील डाल देना चाहिए।
हिन्दुस्तान में निचली अदालतों के जजों को लिखित इम्तिहान के मुकाबले से छांटा जाता है, और उनकी राजनीतिक-सामाजिक सोच के बारे में कभी सोचा भी नहीं जाता है। नतीजा यह होता है कि उनका दलित-विरोधी, महिला-विरोधी पूर्वाग्रह सिर चढक़र बोलता है, और उन अदालतों से इन तबकों को किसी इंसाफ की गुंजाइश भी नहीं रहती है। हमारा तो ख्याल यह है कि लिखित परीक्षा में कामयाब होने के बाद ऐसे उम्मीदवारों को सामाजिक कार्यकर्ताओं के सवालों का सामना करना चाहिए या लिखित परीक्षा में ही सामाजिक सोच के बारे में पूछना चाहिए, और उस आधार पर उनका मूल्यांकन करना चाहिए। अब सवाल यह भी उठेगा कि ऐसा मूल्यांकन कौन करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को यह काम दिया जाएगा उनकी अपनी सोच पुरूषवादी और दलित-विरोधी होने का पूरा खतरा रहेगा। पिछले एक दशक में हिन्दुस्तान में मनु के प्रशंसकों, और भारत की हजारों साल पुरानी सोच के प्रशंसकों के दिन निकल आए हैं। यही वजह है कि दलितों को देश भर में तरह-तरह से मारा जा रहा है, और बलात्कारियों का तरह-तरह से अभिनंदन हो रहा है।
केरल के इस जज की सोच के खिलाफ तो वहां लोगों की आवाज उठने लगी है। कुछ रिटायर्ड जजों ने यह भी कहा है कि इस जज की टिप्पणियों के खिलाफ ऊपर की अदालत में जाने की जरूरत है। आज हिन्दुस्तान में सामाजिक न्याय के आंदोलनकारियों के बीच इस सक्रियता की जरूरत है कि अदालतों की बेइंसाफ बयानबाजी, और उनके फैसलों के खिलाफ एक सामाजिक जागरूकता फैलाई जाए। जब तक ऐसे जजों के खिलाफ सार्वजनिक और सामाजिक सवाल नहीं उठेंगे, तब तक उनका ऐसा ही रूख जारी रहेगा। इसलिए जब कभी ऐसा कोई अपमानजनक बयान या फैसला किसी अदालत का आता है, तो तुरंत उसका विरोध करने की जरूरत है। केरल के एक जिले के इस जज की टिप्पणियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर खूब लिखा जा रहा है, और इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
सुप्रीम कोर्ट में अभी इस बात पर बहस चल रही है कि हिंदुस्तान के चुनावों में राजनीतिक दल मुफ्त के तोहफों के जो वायदे करते हैं, क्या उन पर रोक लगाई जानी चाहिए? यह मामला चुनाव आयोग के सामने भी आया था, और देश के कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इस आधार पर ऐसी घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग की थी कि उनसे राज्यों के बजट पर गैरजरूरी बोझ बढ़ता है, और विकास कार्य के लिए रकम नहीं बचती है। पिछले कुछ दशकों में हिंदुस्तानी चुनावों में ऐसा हुआ भी है कि राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे से आगे बढक़र ऐसी लुभावनी घोषणाएं की हैं कि जिनसे सत्ता पर पहुंचने से पहले ही वे बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर चुके होते हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से ही कहा है कि वह एक संवैधानिक संस्था है, और सुप्रीम कोर्ट चुनावी तोहफों को लेकर जो विशेषज्ञ पैनल बना रहा है, उससे आयोग को बाहर रखा जाए। आयोग का यह मानना है कि यह तय करना अदालत का काम होना चाहिए कि चुनावी घोषणाओं में क्या-क्या कहा जा सके और क्या-क्या नहीं कहा जा सके। सुप्रीम कोर्ट में यह बहस चल ही रही है कि इस दौरान संसद में मोदी सरकार के मंत्रियों ने जनता को दिए जाने वाले अनाज को मुफ्त का तोहफा करार देकर यह बहस शुरू कर दी है कि जिंदा रहने के लिए जनता का जो बुनियाद हक है, उसे मुफ्त का कैसे कहा जा सकता है? विपक्ष के बहुत से नेताओं ने इस पर संसद के भीतर और बाहर, दोनों जगह आपत्ति की है कि इसे मुफ्त कहना देश की जनता के हक का अपमान है।
अब सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए विशेषज्ञ पैनल के लोग यह तय करेंगे कि चुनावी घोषणापत्र में राजनीतिक दल जनता से किन चीजों का वायदा कर सकते हैं, और किन चीजों का नहीं? इस बात में जागरूक और जानकार सामाजिक कार्यकर्ता एक बड़ी खामी देखते हैं कि देश के तथाकथित विशेषज्ञ एक अलग ही दुनिया में जीते हैं, और वे देश के सबसे गरीब लोगों की जरूरतों का अहसास ही नहीं रखते। ऐसे सामाजिक आंदोलनकारियों का यह मानना है कि अपने-आपको अर्थशास्त्र का जानकार समझने वाले ये लोग आमतौर पर सरकारों की पूंजीवादी सोच का साथ देते हैं, और जिंदा रहने के लिए जो न्यूनतम जरूरतें आम जनता को चाहिए, ये उन्हें भी रियायत या राहत की तरह देने के खिलाफ रहते हैं। लोगों को याद होगा कि किस तरह बड़े-बड़े सरकारी अर्थशास्त्री मनरेगा जैसी योजना के खिलाफ थे, जो कि आज हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी को जिंदा रखने का सबसे बड़ा जरिया साबित हो रही है। किस तरह सरकारी अर्थशास्त्री रियायती राशन या स्कूलों में दोपहर के भोजन के खिलाफ थे जिनकी वजह से आबादी के एक बड़े हिस्से का पोषण आहार संभव हो सका, और करोड़ों बच्चों का विकास बेहतर हो सका। सामाजिक विकास के पैमानों को अगर तात्कालिक आर्थिक विकास और उत्पादकता से जोडक़र देखा जाएगा, तो वह एक गड़बड़ अनुमान ही सामने रखेगा। सरकार की ऐसी जनकल्याणकारी योजनाओं का दीर्घकालीन फायदा होता है, और कुछ दशक इनके चलते रहने के बाद इनका फायदा पाने वाली आबादी की औसत उम्र में भी बेहतरी दिखेगी, और इनकी उत्पादकता में भी। अब पूरे देश में यह बात निर्विवाद रूप से मान ली गई है कि देश की करीब आधी आबादी को रियायती या नि:शुल्क अनाज देना जरूरी है, और उसे पाना उनका बुनियादी हक है।
लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की इस अतिरिक्त दिलचस्पी को लेकर भी उसकी कड़ी आलोचना की है कि उसके सामने देश की राजनीति को साफ करने के लिए दर्जनों जलते-सुलगते मामले खड़े हैं, लेकिन वह उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, बल्कि चुनावी लुभावनी घोषणाओं का विश्लेषण करने में लगी है जो कि संसद और विधानसभाओं का काम होना चाहिए। लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार का यह हक रहता है कि वह संविधान के दायरे के भीतर अपनी मर्जी से बजट के मुद्दे तय करे। अगर वह गलत फैसले लेती है तो पांच बरस बाद उसे फिर जनता के बीच जाना पड़ता है, और उसका हिसाब-किताब जनता ही चुकता करती है। जहां तक लुभावनी घोषणाओं पर सरकारों का दीवाला निकल जाने के खतरे की बात है, तो उसके लिए भी देश-प्रदेश में विपक्ष भी है, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के सलाह-मशविरे भी हैं, मीडिया भी है, और जनता के बीच से भी आवाज उठती है। इसलिए अगर कोई विशेषज्ञ कमेटी बुनियादी लोकतांत्रिक मुद्दों को तय करेगी, तो उसका सोचने का नजरिया गरीबों के खिलाफ होने का एक बहुत बड़ा खतरा है।
यहां पर तमिलनाडु के वित्त मंत्री पीटीआर का कल का एक टीवी इंटरव्यू देखने लायक है जिसमें उन्होंने सवाल पूछ रहे उत्साही चैनल-मुखिया को बेजवाब कर दिया। प्रधानमंत्री ने जनता को दिए जाने वाले रियायती सामानों को लेकर या दूसरी छूट को लेकर रेवड़ी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, और इस बारे में तमिल वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों से किस आधार पर प्रधानमंत्री अपनी नीतियां बदलने को कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि या तो कोई संवैधानिक आधार होना चाहिए तो आप जो कहेंगे उसे हम सब सुनेंगे, या फिर आपकी कोई ऐसी विशेषज्ञता होनी चाहिए, आपके पास अर्थशास्त्र में दोहरी पीएचडी होनी चाहिए, या फिर आपको नोबेल पुरस्कार मिला होना चाहिए, या फिर कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो बताए कि आप हमसे बेहतर हैं। या आपका काम का रिकॉर्ड ऐसा हो जो बताए आपने अर्थव्यवस्था को आसमान पर पहुंचा दिया है, या कर्ज को जमीन पर ला दिया है, या प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी है, या रोजगार खड़े कर दिए हैं। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने कहा कि जब इनमें से कोई बात सच नहीं है तो हम उनके नजरिए से क्यों देखें? उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने बहुत से पैमानों पर केंद्र सरकार से बेहतर काम किया है, ऐसे में यह राज्य प्रधानमंत्री के कहे अपनी नीतियां क्यों बदले? उन्होंने कहा कि क्या यह स्वर्ग से आ रहा कोई संविधानेतर हुक्म है? तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके सुप्रीम कोर्ट गई है और उसने इस मामले में फ्रीबीज (बोलचाल की जुबान में रेवड़ी) की परिभाषा तय करने की मांग की है, और कहा है कि जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए और आर्थिक न्याय के लिए लिए जाने वाले फैसले फ्रीबीज नहीं कहे जा सकते।
अभी यह बहस अगले कुछ हफ्ते या कुछ महीने चलती रहेगी, और सुप्रीम कोर्ट शायद ही सरकार से यह पूछ सकेगी कि देश के बड़े कारोबारियों को बैंकों से दिए गए कर्ज का दस-दस लाख करोड़ रुपया डूब जाना किस आकार की रेवड़ी कहलाएगा? और यह भी कि राष्ट्रीय सूचना आयोग के बार-बार के आदेश के बाद भी देश के राजनीतिक दल उन्हें मिले चंदे का हिसाब देने को तैयार क्यों नहीं हैं? क्या बड़े कारोबारियों से उन्हें मिलने वाला मोटा देशी और विदेशी चंदा भी रेवड़ी कहलाएगा, या कुछ और?
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों में एक मुस्लिम युवती बिलकिस बानो के परिवार पर हमला हुआ था, भीड़ ने इस पांच महीने की गर्भवती युवती की तीन साल की बेटी को मार डाला था, परिवार के सात लोगों का कत्ल कर दिया था, और बिलकिस के साथ गैंगरैप किया था। 2002 के इस मामले पर प्रदेश के बाहर हुई सुनवाई में 2008 में सीबीआई कोर्ट ने मुंबई में ग्यारह लोगों को उम्रकैद सुनाई थी जिसे कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कायम रखा था। इसके बाद पन्द्रह बरस कैद काटने के बाद इन्होंने सजा माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और अदालत ने राज्य सरकार को इस पर विचार करने कहा। राज्य सरकार की एक कमेटी ने इन सारे लोगों को पन्द्रह अगस्त को उस वक्त रिहा किया जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कुछ घंटे पहले ही लालकिले पर से महिलाओं के सम्मान की अपील करके हटे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की सजा माफी करने को नहीं कहा था, उस पर विचार करने कहा था, और यह गुजरात सरकार का अपना फैसला है, जिसे वह आज सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर बचने की कोशिश कर रही है। इस एक खबर ने प्रधानमंत्री की एक बड़ी घोषणा को पल भर में खोखला साबित कर दिया क्योंकि गुजरात की राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपनी ही है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि वह राज्य सरकार अपनी पार्टी और अपने गृहमंत्री, प्रधानमंत्री को बताए बिना इतना नाजुक फैसला ले। यह भी समझने की जरूरत है कि केन्द्र सरकार के ऐसे बहुत से निर्देश पहले से हैं, 2014 की एक सजामाफी नीति भी है जिसमें साफ लिखा है कि बलात्कार जैसे भयानक अपराधों के मुजरिमों को माफी नहीं दी जाएगी। गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद जानकार वकीलों का कहना है कि राज्य का यह फैसला केन्द्र की इसी नीति के तहत होना था।
लोगों को याद होगा कि कुछ महीने पहले भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी में अदालतों से विचाराधीन कैदियों को जल्द छोडऩे के बारे में कुछ कहा था। यह मामला विचाराधीन कैदियों का तो नहीं है, लेकिन यह राज्य सरकार के विवेक का मामला जरूर है जो कि सजा का एक वक्त पूरा हो जाने के बाद सजामाफी की अपील पर विचार कर सकती है। अब जब गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री की हाल ही में कैदियों की रिहाई के बारे में कही गई बातों को देखें तो ऐसा लगता है कि क्या वे गुजरात की इस कार्रवाई के पहले एक जमीन तैयार कर रहे थे?
स्वतंत्रता दिवस के दिन जब इन कैदियों को रिहा किया जा रहा था तो जिस तरह से उन्हें मालाएं पहनाई गईं, उनकी आरती उतारी गई, उससे भी देश बहुत विचलित है। प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर देश भर में यह विवाद चल ही रहा था कि देश में उनके समर्थक और प्रशंसक महिलाओं पर सबसे अधिक ओछे हमले करने के लिए जाने जाते हैं, और खुद प्रधानमंत्री ने पिछले बरसों में महिलाओं के बारे में बहुत से आपत्तिजनक बयान दिए थे। इसके ठीक बाद जब गुजरात में हत्यारों और बलात्कारियों की रिहाई ऐसे दिन को छांटकर की गई, तो उसकी तस्वीरें और उसके वीडियो देखकर लोग हक्का-बक्का रह गए। यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि चार महीने बाद दिसंबर में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और वहां के पिछले कई चुनाव हिन्दू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक आक्रामक ध्रुवीकरण करके भाजपा ने जीते थे, और 2014 के पहले तक तो नरेन्द्र मोदी ही वहां के कई बार के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में अभी हिन्दुस्तान के इतिहास के सबसे चर्चित साम्प्रदायिक हमले के इन ग्यारह गुनहगारों को जिस तरह जेल से छोड़ा गया है, जिस तरह उनका स्वागत हुआ है, उससे लगता है कि यह चुनाव के ठीक पहले का एक ऐसा सरकारी फैसला है जिसका निशाना तात्कालिक ध्रुवीकरण पर है। देश के सबसे मुखर मुस्लिम नेता, असदुद्दीन ओवैसी ने कल से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा, और गुजरात की भाजपा सरकार पर बड़ा तीखा हमला शुरू कर दिया है, और कल ही विश्व हिन्दू परिषद ने उसका बड़ा लंबा आक्रामक जवाब दिया है। मतलब यह कि यह नूरा कुश्ती अगले कुछ महीनों में चुनाव का एक अखाड़ा बनाने में लग गई है। ओवैसी को हम पहले भी भाजपा के चुनाव अभियान में शामियाना खड़ा करने वाला लिख चुके हैं, और आज वे जितने अधिक हमलावर तेवर दिखाएंगे, वह दिसंबर के चुनाव में भाजपा के उतने ही अधिक काम आएगा। जाहिर है कि इस रिहाई से गुजरात की मुस्लिम बिरादरी बहुत बुरी तरह विचलित रहेगी, और गुजरात का इतिहास बताता है कि विचलित मुस्लिम बिरादरी हिन्दुओं के ध्रुवीकरण का काम करती है। इस बात को कुछ हफ्ते पहले उन दो लोगों की गिरफ्तारी से न जोडऩा ठीक नहीं होगा जिन्हें गुजरात दंगों के बाद मोदी सरकार के खिलाफ बागी तेवरों वाला माना गया था क्योंकि वे मुस्लिमों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, या दंगों में मोदी सरकार के रूख को लेकर जिन्होंने बयान दिए थे। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, और एक रिटायर्ड आईपीएस पुलिस अफसर आर.बी. श्रीकुमार को गिरफ्तार किया गया, और जिला अदालत से उन्हें जमानत देने से मना कर दिया गया है। दिसंबर के चुनावों के पहले कुछ महीने पहले की इन घटनाओं को चुनाव से न जोड़ऩा मुमकिन नहीं है, खासकर तब, जब मोदी की भाजपा चुनाव के वक्त के एक-एक दिन को अपने पक्ष में तय करने की चतुराई रखती है। वह हिन्दुस्तान के किसी मतदान के दिन नरेन्द्र मोदी को नेपाल के मंदिरों में घूमता दिखाती है, तो किसी और मतदान के दिन बांग्लादेश के मंदिरों में। टीवी पर दिन-दिन भर मंदिरों में छाए हुए मोदी भारत की किसी चुनावी आचार संहिता से भी बचे रहते हैं। इसलिए अभी गुजरात में हक्का-बक्का कर देने वाली यह रिहाई पूरी तरह से कानून की भावना के खिलाफ है, केन्द्र सरकार की 2014 की नीतियों के खिलाफ है, और चुनावी ध्रुवीकरण की गारंटी करने वाली है।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
मद्रास हाईकोर्ट ने चार दिन पहले राज्य के बड़े पुलिस अफसरों के घरों पर तैनात किए गए पुलिस के निचले दर्जे के कर्मचारियों को गुलामीप्रथा करार देते हुए फटकार लगाई है। अदालत इसके खिलाफ पहले भी कड़ा आदेश कर चुकी है, लेकिन इसका कोई असर सरकार और अफसरों पर नहीं हुआ। सरकारी वकील ने कहा कि अदालत के पिछले आदेश के बाद 19 पुलिस कर्मचारियों को अर्दली ड्यूटी से मुक्त किया गया है, लेकिन जज ने कहा कि इसके बाद भी बड़ी संख्या में छोटे स्तर के पुलिस कर्मचारी बड़े अफसरों के बंगलों पर तैनात हैं। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा करके ये बड़े पुलिस अफसर पुलिस फोर्स में अनुशासन लागू करने का अपना नैतिक अधिकार खो देते हैं। अदालत ने इसे इस देश के संविधान और लोकतंत्र पर तमाचा कहा है, और यह भी कहा कि यह अंग्रेजों के वक्त की गुलामीप्रथा की जारी परंपरा है।
तमिलनाडु में अदालत पहुंचे इस मामले से परे देश के अधिकतर राज्यों में पुलिस के निचले कर्मचारियों का यही हाल है। बड़े पुलिस अफसरों के बंगलों पर अविश्वसनीय संख्या में सिपाही तैनात कर दिए जाते हैं। वे घरेलू कामकाज करते हैं, कुत्तों और बच्चों को साफ करते हैं, उन्हें घुमाते हैं, बंगला बड़ा हो तो डेयरी और सब्जी-भाजी का बगीचा भी देखते हैं। एक प्रदेश की राजधानी में बैठे हुए जानकार लोग बतलाते हैं कि अफसर की अपनी मोटी तनख्वाह से कई गुना अधिक तनख्वाह कर्मचारियों की उन बंगलों पर खर्च होती है जो अपने आपमें अंग्रेजी राज का प्रतीक हैं। सरकार को बंगलों और नौकर-चाकर का यह इंतजाम खत्म करना चाहिए, और इसके लिए एक भत्ता अफसरों को देना चाहिए, या मकान भत्ता तो उन्हें मिलता ही है। यह बात सिर्फ आईपीएस अफसरों के साथ नहीं है, जंगल विभाग के आईएफएस अफसरों के पास रोजी पर मजदूर रखने के अनगिनत काम रहते हैं। ऐसे में अफसरों के बंगलों पर बहुत से रोजी वाले लोग तैनात रहते हैं जिनका सरकारी भुगतान होता है। आईएएस अफस चूंकि इन दोनों से ऊपर माने जाते हैं, इसलिए उनके बंगलों पर हर तरफ से कर्मचारी बुलाए जाते हैं, और भेजे जाते हैं।
यह बात सरकार के फिजूलखर्च से अधिक खतरनाक है। जिन लोगों को पुलिस की ड्यूटी के लिए नौकरी पर रखा जाता है, जिन्हें पुलिस के काम की ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे घरेलू काम लेकर उनका मनोबल तोड़ दिया जाता है। कुछ बरस किसी बंगले पर गुलामी करने के बाद ये सिपाही किसी चुनौतीपूर्ण या खतरनाक मोर्चे के लायक रह भी नहीं जाते। रसोई में काम करते हुए, ट्रे थामे हुए, चाय-पानी परोसते हुए, जानवर नहलाते हुए, बच्चों का पखाना धोते हुए किस इंसान का मनोबल मुजरिमों को पकडऩे, आतंकियों से लडऩे, अराजक लोगों को रोकने के लायक रह जाएगा? यह बात पूरी तरह से अमानवीय भी है कि नियम-कायदों के खिलाफ, सरकारी सेवा शर्तों के खिलाफ मातहत लोगों को उनकी ड्यूटी से हटाकर इस तरह गुलाम बनाकर रखा जाए। हम पहले भी इसी जगह इस बात की वकालत कर चुके हैं कि ऐसे गुलाम-कर्मचारियों को अपने ऐसे मालिकों के खिलाफ बगावत करनी चाहिए, उन्हें गुलामी के वीडियो बनाकर शिकायत करनी चाहिए, उन्हें चारों तरफ फैलाना चाहिए। इससे कुछ लोगों की नौकरी पर खतरा आ सकता है, लेकिन वर्दीधारी कर्मचारियों के ऐसे अपमानजनक इस्तेमाल के सिलसिले को खत्म करने के लिए कुछ लोगों को तो ऐसा खतरा उठाना ही होगा। यह एक अकेली वजह हमें पुलिस कर्मचारियों की यूनियन बनाने के लिए काफी लगती है। कुछ प्रदेशों में ऐसी यूनियन है, और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में सरकारों ने बड़ी कोशिश करके पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को भी संगठित होने से रोका है। उन्हें रोक तो दिया गया है, लेकिन उनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई है।
तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट के इस मामले की मिसाल देते हुए, उससे सबक लेते हुए बाकी प्रदेशों में भी सरकारी कर्मचारियों को अर्दलियों की तरह अफसरों और नेताओं के बंगलों पर इस्तेमाल करने के खिलाफ कानूनी पहल करनी चाहिए। यह बात छोटे सरकारी कर्मचारियों के मानवीय अधिकारों के खिलाफ भी है, और पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और गैरकानूनी तो है ही। एक-एक बड़े अफसर और सत्तारूढ़ नेता पर लाखों रूपये महीने की तनख्वाह छोटे कर्मचारियों की भी लगती है, और यह पूरी तरह से अघोषित खर्च है जो कि गरीब जनता के ही सिर पर आता है। सरकारों को बड़े-बड़े सरकारी बंगलों का इंतजाम पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। एक-एक परिवार के लिए बड़े-बड़े बंगले, और जनता पर उनका खर्च, पूरी तरह नाजायज है। अफसरों को अपनी तनख्वाह के अलावा जिस मकान भत्ते की पात्रता रहती है, उस भत्ते पर जो मकान उन्हें मिलेगा, उसमें कर्मचारियों की फौज की जरूरत भी नहीं रहेगी।
पुलिस कर्मचारी चूंकि वर्दीधारी हैं, और उनके संघ को छूट नहीं है, इसलिए किसी न किसी को यह बात उठानी होगी। कोई जनसंगठन भी इस मुद्दे को लेकर मानवाधिकार आयोग जा सकते हैं, या अदालत में जनहित याचिका लगा सकते हैं।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
आज जब पूरा हिन्दुस्तान तिरंगे झंडे को लहराते हुए घूम रहा है, और कल आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा है, उस वक्त राजस्थान के जालौर में इंटरनेट बंद किया गया है। आमतौर पर साम्प्रदायिक घटनाओं को लेकर देश में जगह-जगह ऐसी नौबत आती है, लेकिन जालौर में तो हिन्दुओं के बीच ही ऐसी नौबत आई है। वहां के एक निजी स्कूल में 9 बरस के एक दलित बच्चे ने मास्टर छैलसिंह की अलग रखी हुई मटकी से पानी पी लिया, तो मास्टर ने उसे मार-मारकर जख्मी कर दिया, और तीन हफ्ते बाद इन्हीं जख्मों की वजह से अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मास्टर की मार से इस दलित बच्चे के चेहरे और कान बुरी तरह जख्मी हुए थे, और इन जख्मों से वह उबर ही नहीं पाया। अब वहां के तनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने वहां इंटरनेट बंद किया है।
आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रही भारत सरकार के जलसे के बीच यह एक बुरी खबर है जो कि हिन्दुस्तान में उस दलित तबके की हकीकत बताती है जो कि आज देश पर राज कर रही सोच के पांवों तले जी रहा तबका है। आज इस देश में हाईकोर्ट की एक जज उस मनुस्मृति को महिमामंडित कर रही है जिसमें दलितों के खिलाफ तमाम किस्म की हिंसक बातें लिखी गई हैं, जहां महिलाओं को तिरस्कार के लायक पाया गया है। जिस हिन्दू सोच के मुताबिक दलित के कानों में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाने पर उसमें पिघला हुआ सीसा भर देने की व्यवस्था है, उस सोच के तहत इस मास्टर ने तो दलित बच्चे को महज पीटा ही था, और यह तो उसके दलित बदन का कुसूर था कि वह मास्टर की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और चल बसा।
राजस्थान, मध्यप्रदेश, और उत्तर भारत के कुछ दूसरे हिस्से दलितों के साथ ऐसे जुल्म करने की परंपरा की गिरफ्त में हैं। हिन्दुस्तान के जिन लोगों को यह लगता है कि अब जाति व्यवस्था खत्म हो चली है, और अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, उन लोगों को सीमेंट और डामर की सडक़ों से कुछ नीचे उतरकर देखना चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है। मध्यप्रदेश के कई इलाकों में दलित चप्पल पहनकर सवर्णों की बस्ती से नहीं गुजर सकते, और जो लोग भारत के गांवों के परंपरागत ढांचों के जानकार हैं, उनका कहना है कि आम गांवों में ऊंचे इलाकों में सवर्ण बसते हैं, और वहां से नालियों का पानी जिस तरफ बहता है, वहां ढलान की तरफ दलित बसते हैं, ताकि दलितों की नालियों का पानी कभी भी सवर्ण बस्तियों की तरफ न आ सके। हर बरस दर्जनों ऐसी खबरें आती हैं कि दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढक़र बारात में निकलने के लिए पुलिस की हिफाजत मांगनी पड़ी, और पुलिस की मौजूदगी में भी उन पर हमले हुए। कहीं दलितों को मूंछ रख लेने पर मारा जाता है, तो कहीं संगीत जोर से बजाने पर। देश को आजाद हुए पौन सदी हो गई है, लेकिन दलितों के लिए सवर्ण नफरत में कोई कमी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की धारदार वक्ता महुआ मोइत्रा ने कुछ दिन पहले ही यह कहा था कि हिन्दुस्तान में जब तक मुस्लिम हैं, तभी तक हिन्दू हिन्दू हैं। जब मुस्लिम खत्म हो जाएंगे तो हिन्दू नहीं रह जाएंगे, उनकी जगह ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत बच जाएंगे। यह बात सौ फीसदी सही है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जो दलित जाति व्यवस्था में पैरों से पैदा हुए माने जाते हैं, और अछूत समझे जाते हैं, जिन्हें इंसानी हकों का दावा करते ही मार दिया जाता है, वे दलित भी उन्हीं सवर्ण हिन्दुओं के देवी-देवताओं की पूजा करने के लिए मरे पड़े रहते हैं, जिन देवी-देवताओं ने इन दलितों को कभी नहीं बचाया। हिन्दू धर्म की व्यवस्था में मंदिर प्रवेश, और ईश्वर की उपासना का अधिकार मांगने का मतलब ही ब्राम्हणवादी सवर्ण व्यवस्था को मजबूत करना है। इन दलितों को हिन्दू समाज के ऐसे जातिवादी ढांचे से बाहर निकलकर अपना खुद का ईश्वर ढूंढने या बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन सदियों की गुलाम मानसिकता उन्हें मंदिर प्रवेश का एक ऐसा अधिकारों का सपना दिखाती है जिसे हासिल करना उन्हें बहुत बड़ी बात लगती है। जिस दिन दलित समुदाय एकमुश्त हिन्दू समाज के ढांचे के बाहर निकल आएंगे, बचे हुए गैरदलित हिन्दुओं की अकल ठिकाने आ जाएगी। सवर्ण हिन्दुओं का यह दंभ, और उनकी यह हिंसा, तभी तक कायम हैं, जब तक दलित 21वीं सदी में भी गुलाम मानसिकता के शिकार बने हुए हैं, और मंदिर-प्रवेश को एक अधिकार का दावा मानकर चल रहे हैं।
ऐसी व्यवस्था को धिक्कारकर, लानत भेजकर दलितों को हिन्दू व्यवस्था को ही खारिज करना चाहिए जिसने कि उन्हें शोषण का सामान बनाकर रखा है। यह तो इस देश में दलितों और आदिवासियों के साथ जुल्म और ज्यादती करने पर एक अलग कानून का इंतजाम है, उसके बाद भी सवर्ण तबका धड़ल्ले से हिंसा करते रहता है, क्योंकि उसे भारत की जांच और न्याय व्यवस्था पर अपनी बिरादरी के कब्जे पर अतिआत्मविश्वास है। यह सिलसिला खत्म करना चाहिए, और राजस्थान, मध्यप्रदेश सरीखे राज्यों में कानून के कड़ाई से इस्तेमाल से हालात सुधारने चाहिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, और तैनात अफसरों में अगर दलितों की बराबरी का सम्मान नहीं है, तो उन्हें चुनावों से दूर करना चाहिए, और उनकी नौकरी खत्म करनी चाहिए। यह इस देश के लिए आजादी की सालगिरह के इस मौके पर शर्म से डूब मरने की एक बात है कि एक दलित बच्चे को इसलिए मार डाला गया कि उसने गैरदलित का पानी छू लिया था। जहां तक इस सालगिरह को आजादी का अमृत महोत्सव करार देने की भाषा का सवाल है, तो यह भाषा अपने आपमें उसी हिन्दू धर्म से निकली हुई है जिसमें समुद्र मंथन से निकले अमृत पर देवताओं का हक तय किया गया था। यह भाषा आज भी इस देश में उसी धर्म व्यवस्था को मजबूत करती है, और किसी के लिए अमृत और किसी के लिए विष की सोच आगे बढ़ाती है।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
भारत में जन्मे और पश्चिम में बसे विख्यात लेखक सलमान रुश्दी पर कल अमरीका के न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के मंच पर एक नौजवान ने जाकर चाकू से हमला किया, और बुरी तरह जख्मी कर दिया। रुश्दी लंबे समय से मुस्लिम या इस्लामी आतंकियों के निशाने पर थे। उनकी एक किताब ‘सैटेनिक वर्सेज’ पर 1988 में ईरान ने उनकी मौत का फतवा जारी किया था, जो कि ईरान के सत्तारूढ़ धार्मिक मुखिया की तरफ से सार्वजनिक रूप से दिया गया था। इस किताब को मोहम्मद पैगंबर का अपमान करार दिया गया था, और रुश्दी के कत्ल पर दसियों लाख डॉलर का ईनाम भी रखा गया था। एक विश्लेषण यह कहता है कि ईरान और इराक के बीच आठ साल चली लड़ाई खत्म हुई ही थी, और ईरान के हर घर में किसी न किसी शहीद की तस्वीर टंगी थी, देश का बुरा हाल था, सिर्फ कब्रिस्तान पनपे हुए थे, ऐसे में वहां के धार्मिक नेता अयातुल्ला खुमैनी को रुश्दी की शक्ल में एक दुश्मन खड़ा करके लोगों के दुख-दर्द को भुलवाने का एक जरिया सूझा था, और उन्होंने ईरानियों को इस धार्मिक कट्टरता के उन्माद में झोंक दिया था। इसका एक असर यह भी हुआ था कि बात की बात में दुनिया के दर्जनों देशों में मुस्लिमों के बीच बिना इस किताब को पढ़े हुए उसका लेखक ईशनिंदक साबित हो गया था, और उसके कत्ल की मांग करते हुए चारों तरफ जुलूस निकलने लगे थे। दशकों से रुश्दी कुछ हमदर्द देशों की हिफाजत के घेरे में जी रहे थे, लेकिन धार्मिक उन्माद और नफरत को जानने वाले यह भी जानते थे कि यह दिन एक न एक दिन आना ही था। इस हमले के बाद रुश्दी अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं, धर्मान्ध लोग खुशियां मना रहे हैं, और समझदार लोग इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि एक धर्म के हत्यारों की कामयाबी से दूसरे धर्म के कट्टर लोगों को भी हत्यारा बनने का हौसला मिलता है।
यह हमला एक इंसान या एक लेखक पर नहीं है, यह सोच की आजादी पर हमला है। एक लेखक अपने काल्पनिक लेखन में कुछ किरदार गढ़ता है और उन्हें अपनी आस्था का अपमान मानते हुए कुछ कट्टर और धर्मान्ध लोग उसके कत्ल का फतवा जारी कर देते हैं। यह तो रुश्दी पश्चिमी देशों की सरकारी हिफाजत में जी रहे थे, वरना यह हमला कब का हो चुका रहता। लोगों को याद रखना चाहिए कि फ्रांस की एक व्यंग्य पत्रिका में मोहम्मद पैगंबर पर बनाए गए कार्टूनों का विरोध इस कदर हिंसक हुआ था कि पेरिस में हथियारबंद लोगों ने इसके दफ्तर पर हमला करके दर्जन भर लोगों को मार डाला था, और दर्जन भर दूसरे लोग घायल कर दिए गए थे। इन कार्टूनों के खिलाफ योरप के दूसरे देशों में भी जगह-जगह तरह-तरह के हमले हुए थे, और इसने योरप में बसे हुए मुस्लिमों, और वहां पहुंचने वाले मुस्लिम शरणार्थियों की जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया था। यह बात समझने की जरूरत है कि किसी धर्म के नाम पर जो हमला होता है, वह बहुत बार तो सबसे बड़ा नुकसान उसी धर्म को मानने वाले लोगों को करता है। आज जो लोग इस्लाम को मानते हुए भी अलग-अलग देशों में वहां के कानून को भी मानते हुए अमन-चैन से जी रहे हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह की दहशत आज चारों तरफ फैलेगी, और दूसरे धर्मों के कुछ कट्टर लोग हो सकता है कि मुस्लिमों पर हिंसक या आर्थिक किसी तरह के हमले भी करें।
यह बात सिर्फ ईरान की नहीं है, बल्कि उन तमाम देशों की है जहां पर किसी एक धर्म, या कई धर्मों के लोग अपनी आस्था को देश और दुनिया के कानून से ऊपर मानकर हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। आज अगर इस्लामिक आतंक को देखा जाए, तो उसके सबसे अधिक शिकार दुनिया के मुस्लिम ही हैं। आज जिस सलमान रुश्दी को लेकर यह बात हो रही है वह मुम्बई में एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में ही पैदा हुए थे, और मुम्बई की एक ईसाई स्कूल में पढ़े थे। वे कुछ अरसा पाकिस्तान में भी अपने परिवार के साथ रहे थे, और अब वे इस्लामी आतंकियों के निशाने पर हैं। पिछले दशकों में रुश्दी दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक प्रतीक की तरह भी बन गए थे, और उन्होंने अपने विचारों को नहीं छोड़ा था। अभी से कुछ घंटे पहले हुआ यह हमला दुनिया में हर किस्म की कट्टर ताकतों को मजबूती देगा, और कई दूसरे आतंकी गिरोह और धर्मान्ध लोग इस बात को लेकर हीनभावना के शिकार हो जाएंगे कि वे इस काम को नहीं कर पाए।
हिन्दुस्तान जैसे लोकतंत्र के लिए ऐसी कट्टरता एक बहुत बड़ा खतरा इसलिए है कि यहां बीते दशकों में अलग-अलग मुद्दों को लेकर अलग-अलग लोगों के खिलाफ जुबान काट देने और सिर काटकर लाने के फतवे दिए गए, ऐसी हिंसा पर ईनाम रखा गया। हिन्दुस्तान के सभी तरह के धार्मिक आतंकियों को रुश्दी पर हमले से एक प्रेरणा मिलेगी, और मुस्लिमों के खिलाफ कट्टरता की जो बात कही जाती है, उसे एक मजबूती मिलेगी। यह सिलसिला किसी एक व्यक्ति या किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, यह संक्रामक रोग की तरह है, और समाज के बीच धार्मिक कट्टरता, और साम्प्रदायिकता को बढ़ाते चलने वाला है। हिन्दुस्तान उन देशों में से था जिसने दुनिया के इस्लामिक और मुस्लिम देशों से भी पहले रुश्दी की इस किताब पर रोक लगा दी थी, और वह आज भी जारी है। भारत की बड़ी मुस्लिम आबादी को देखते हुए राजीव गांधी की सरकार ने यह रोक लगाई थी, और उसने बहुत से लोगों को हैरान भी किया था कि ऐसी तेज रफ्तार प्रतिक्रिया तो किसी इस्लामिक देश की भी नहीं थी। इतिहास बताता है कि भारत पहला देश था जिसने इस उपन्यास को बैन कर दिया था, इसके बाद फिर पाकिस्तान और दूसरे इस्लामी देशों ने रोक लगाई।
यह मौका इस बात को भी समझने का है कि क्या किसी सरकार को इस रफ्तार से रोक लगानी चाहिए, या अपने देश के लोगों को उदारता की बात भी समझानी चाहिए। जब सरकार ही तेजी से धर्मान्धता को मान्यता देती है, तो फिर समाज के भीतर किसी उदारता की अधिक गुंजाइश बचती नहीं है। इस हमले के बाद लोगों में बड़े पैमाने पर चर्चा शुरू हो चुकी है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नए सिरे से दुबारा बात बढऩी चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
आजादी की 75वीं सालगिरह पर भारत सरकार ने हर घर तिरंगा नाम का एक अभियान शुरू किया है, और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर भी अधिक से अधिक घरों में तिरंगा पहुंचाने की घोषणा के साथ कुछ कोशिश कर रही है। रेलवे के करोड़ों कर्मचारियों को बाजार भाव से काफी अधिक दाम पर अनिवार्य रूप से तिरंगा झंडा खरीदने के लिए कहा जा रहा है, जिसे लेकर विरोध भी हो रहा है, और लोग यह हिसाब भी पोस्ट कर रहे हैं कि ठेकेदार को इससे कितने करोड़ की कमाई होने जा रही है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा की राशन दुकानों के ऐसे वीडियो पोस्ट हो रहे हैं जहां पर राशन दुकानदार ही यह बता रहा है कि उसे ऊपर से हुक्म मिला है कि जो लोग बीस रूपये का झंडा खरीदें, उन्हें ही राशन देना है। अब सीमित आय वाले जो लोग राशन कार्ड लेकर गिने-चुने नोट लेकर राशन दुकान पहुंच रहे हैं, वहां उन्हें पता लग रहा है कि पहले बीस रूपये तो झंडे के देने होंगे। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस से भी झंडा बेचा जा रहा है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर यह पढऩे मिला कि वह गलत तरह से छपा हुआ झंडा है जिसमें अशोक चक्र एक तरफ खिसका हुआ है, और यह पढक़र जब इस अखबार ने पोस्ट ऑफिस से झंडा खरीदकर मंगवाया तो अशोक चक्र बीच के बजाय एक तरफ बहुत बुरी तरह खिसका हुआ छपा था। झंडे को लेकर ही यह विवाद भी हुआ कि सरकार ने झंडा कानून बदलकर अब सिंथेटिक कपड़ों के तिरंगे झंडे को भी छूट दे दी है, जबकि खादी के कपड़ों से बनने वाले परंपरागत झंडे कपास उगाने वाले किसानों से लेकर बुनकरों तक को रोजगार देते थे, वह पूरा काम अब खत्म सा हो गया।
लेकिन बात अगर महज झंडे तक सीमित रहती, तो भी ठीक था। झंडों के साथ जिस तरह राष्ट्रवाद का उन्माद फैलाया जा रहा है, और एक सकारात्मक राष्ट्रवाद से परे जाकर जिस तरह बिना झंडे वाले लोगों को देशद्रोही और गद्दार करार देने की पहल शुरू हो रही है, वह भयानक है। इस देश में अब देशप्रेमी होना काफी नहीं है, एक खास विचारधारा को देशप्रेम के जो प्रतीक पसंद हैं, उन प्रतीकों को अनिवार्य रूप से मानना, दिखाना, और प्रदर्शित करना भी जरूरी है। उत्तराखंड के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेश भट्ट ने एक आमसभा में कहा कि जो लोग तिरंगा अभियान के दौरान अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाते, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा जिनके घर में तिरंगा नहीं लगेगा, हम उन्हें विश्वास की नजर से कभी नहीं देख पाएंगे। उन्होंने कहा मुझे उस घर का फोटो चाहिए जिस घर में तिरंगा न लगा हो।
पिछले बरसों में हिन्दुस्तान ने ऐसे बहुत से प्रतीकों का प्रदर्शन देखा है जिन्हें मोदी की स्तुति के रूप में देखना तो ठीक था, लेकिन जो उस प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, उन्हें देश का गद्दार करार देना लोकतंत्र के मुताबिक तो बहुत बड़ी ज्यादती थी। हर किसी के देशप्रेम के तौर-तरीके अलग-अलग होते हैं। हर धर्म और संस्कृति, इलाके और जुबान में देशप्रेम के नारे अलग हो सकते हैं, मातृभूमि की परिभाषा अलग-अलग हो सकती है, देशप्रेम के गाने अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन पिछले बरसों में इस देश ने जिस तरह-हिन्दुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, या, हिन्दुस्तान में रहना है तो जयश्रीराम कहना होगा जैसे नारे लगाए गए, जो कि किसी के सम्मान में कम थे, धमकी अधिक थे। ऐसे में अलग धर्म और अलग संस्कृति वाले लोगों को तेजी से देशद्रोही करार देकर पाकिस्तान भेजने की बात भी कुछ बरस चली थी, फिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने फतवों के आधार पर वीजा देना बंद कर दिया, और सारे ‘देशद्रोही’ लोग इसी देश पर बोझ बने हुए यहीं कायम हैं।
राष्ट्रीयता और देशप्रेम को कुछ खास प्रतीकों से अनिवार्य रूप से जोडक़र उन्हें हर किसी पर लादकर इस तरह का उन्माद खड़ा करना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक तबके को ऐसे उन्माद में मजा आ सकता है, लेकिन इसके तौर-तरीकों से असहमत दूसरे कहीं अधिक बड़े देशप्रेमी लोगों को यह सजा भी लग सकती है कि उस पर कोई बात थोपी जा रही है। लोकतंत्र ऐसे प्रतीकों का नाम नहीं हो सकता जिन्हें सरकारी खर्च पर, राजनीतिक फतवों से, धमकी-चमकी और दबाव से, लोगों का अनाज रोककर उन पर लादा जाए, और उसे आजादी का अमृत महोत्सव कहा जाए। हरियाणा की जिन राशन दुकानों पर बेबस गरीब महिलाओं का आक्रोश निकल रहा है, उनके बीस रूपये में खरीदे झंडों से क्या उनके घर पर आजादी का जश्न मनेगा, या वे लोग जश्न के इस जबरिया तौर-तरीके को कोसेंगे? जिस आजादी के नाम पर यह जलसा मनाया जा रहा है, उसी आजादी को कुचलते हुए यह खुली राजनीतिक धमकी दी जा रही है कि जो लोग झंडा नहीं फहराएंगे उनके घरों की तस्वीरें भेजी जाएं, उन पर यह देश कभी भरोसा नहीं कर सकेगा।
विविधता से भरा हुआ यह देश अपनी राजनीतिक और सामाजिक विविधताओं की वजह से ही आजाद दिखता है, और माना जाता है। अगर सारी आबादी की पोशाक, खानपान, राजनीतिक विचारधारा, और सांस्कृतिक तौर-तरीके सभी को एक सरीखा किया जाए, और तभी उन्हें देशप्रेमी माना जाए, तो यह तो आजादी के ठीक खिलाफ होगा। लोगों को आज तिरंगा झंडा अच्छा लग सकता है, लेकिन घरों पर इसे फहराना उन्हीं लोगों को अच्छा लगेगा जिनके मन में ऐसा करने की बात है। नसबंदी बहुत अच्छी बात थी, और हिन्दुस्तान की बढ़ती आबादी को घटाने में कारगर भी हो सकती थी, लेकिन जब इमरजेंसी में संजय गांधी नाम के एक तानाशाह ने पूरे देश पर नसबंदी को जबरिया थोप दिया था, तो अगले चुनाव के वक्त लोगों ने इसे याद रखा था। कोई अच्छी चीज भी लोकतंत्र में दूसरों पर जबरिया कैसे थोपी जा सकती है? और आज जिस तरह सार्वजनिक धमकी देते हुए ऐसे लोगों को अविश्वसनीय करार दिया जा रहा है, जो घरों पर झंडा नहीं फहराएंगे, ऐसे नेता यह तो बताएं कि देश का कौन सा संविधान उन्हें किसी को अविश्वसनीय करार देने का हक देता है?
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
मुम्बई फिल्म उद्योग के एक बहुत ही औसत दर्जे के अभिनेता मुकेश खन्ना का नाम बच्चों के लिए बनाए गए शक्तिमान नाम के एक किरदार से जुड़ा हुआ था, और एक वक्त था जब छत्तीसगढ़ में स्कूलों का जाल बिछाने वाले, और साथ-साथ अखबार चलाने वाले एक जालसाज ने मुकेश खन्ना को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर दसियों हजार मध्यमवर्गीय मां-बाप को लूटा था। ऐसे मुकेश खन्ना ने अभी एक गंदा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है- कोई भी लडक़ी अगर किसी लडक़े को कहे कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूं तो वो लडक़ी लडक़ी नहीं है, वो धंधा कर रही है। इस तरह की निर्लज बातें कोई सभ्य समाज की लडक़ी नहीं करेगी, और अगर वो करती है तो वो सभ्य समाज की नहीं है, उसका धंधा है ये, उसकी भागीदार मत बनिये। मुकेश खन्ना के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, और लोग सोशल मीडिया पर ही उन्हें जमकर धिक्कार भी रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस भेजकर इस बारे में जानकारी मांगी है, एफआईआर की कॉपी भेजने कहा है, और इस पर की गई कार्रवाई के बारे में बताने कहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाती मालीवाल ने इस चिट्ठी को ट्वीट करते हुए कहा है कि महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों पर एफआईआर दर्ज करवाने हेतु दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
दरअसल महिलाओं को बर्दाश्त कर पाना आसान बात नहीं होती है। सोशल मीडिया पर कई लोग इस बात को लिखते हैं कि लोगों को कामयाब महिलाएं दूर से तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उनसे रूबरू सामना होता है, तो मर्द उन्हें पसंद नहीं कर पाते। ऐसा शायद इसलिए भी होता है कि कामयाबी किसी भी महिला में एक आत्मविश्वास पैदा करती है, और महिला का आत्मविश्वास आदमी में हीनभावना पैदा करता ही है। अपने आपको बच्चों के बीच एक आदर्श किरदार की तरह पेश करने वाले इस अभिनेता की बकवास में आदमियों की कोई जगह नहीं है कि अगर कोई आदमी किसी औरत से ऐसी बात कहे तो वह आदमी भी क्या पेशा करने वाला होगा? इक्कीसवीं सदी के दो दशक निकल चुके हैं, लेकिन हिन्दुस्तानी आदमी, और खासे पढ़े-लिखे और सार्वजनिक जीवन के कामयाब लोग, सार्वजनिक रूप से भी अठारहवीं सदी की ऐसी दकियानूसी बात करते हैं।
और मुकेश खन्ना तो फिर भी एक छोटा सा आदमी है, इस देश के कई मुख्यमंत्री और कई केन्द्रीय मंत्री एक से बढक़र एक घटिया और अश्लील बातें महिलाओं के बारे में कहते आए हैं। इनमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरीखे लोग भी शामिल हैं, और इनको सहूलियत यह भी रहती है कि इनके ऐसे महिलाविरोधी बयानों के बाद भी न तो ये चुनाव हारते, और न ही इनकी पार्टी चुनाव हारती। मतलब यह है कि जनता के एक छोटे और मुखर तबके को ऐसे बयान खटकते हैं, लेकिन ऐसे बयान वोट नहीं बिगाड़ पाते जबकि वोटरों में आधी महिलाएं हैं। जब तक वोटरों की जागरूकता नहीं बढ़ेगी, और महिलाओं के बीच एक तबके के रूप में स्वाभिमान नहीं जागेगा, तब तक महिलाओं के खिलाफ खाप पंचायतों से लेकर देश की संसद और विधानसभाओं तक बकवास चलती रहेगी, और उनके साथ बेइंसाफी जारी रहेगी।
लोगों को खाप पंचायतों की इन बातों को नहीं भूलना चाहिए जो कि लड़कियों के जींस पहनने पर पाबंदी लगाती हैं, उनके मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी लगाती हैं। अभी-अभी हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में सोना जीतकर आने वाली निखत जरीन को बॉक्सिंग के कपड़े पहनने के लिए मुस्लिम समाज के भीतर से लगातार चेतावनी दी जाती थी। कुछ ऐसा ही सानिया मिर्जा को भी झेलना पड़ता था। और जब इनकी कामयाबी आसमान पर पहुंची तब जाकर इनके खिलाफ ओछे हमले बंद हुए, वरना इन्हें भी अपने कपड़ों के लिए मर्दों के वैसे ही हमले झेलने पड़ते थे जैसे हमले घर से बाहर निकलने वाली लड़कियों को योगियों और मनोहरलालों के झेलने पड़ते हैं।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा इन मामलों में जागरूक हैं, और देश की राजधानी में बैठे हुए वे बहुत से मामलों में जागरूकता दिखाती हैं। अगर और योजना आयोग, बाल आयोग, या महिला आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करते, तो बकवास पर कुछ लगाम लग सकती थी। लोगों को याद होगा कि उत्तरप्रदेश के बड़बोले समाजवादी नेता आजम खान ने जब बलात्कार की शिकार बारह बरस की एक बच्ची की शिकायत को राजनीतिक साजिश कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी थी, और इस बड़बोले नेता को अदालत में माफी मांगनी पड़ी थी। हिन्दुस्तान में आज जरूरत ऐसी ही कार्रवाई की है जिससे हिंसक और अश्लील बकवास करने वाले लोगों को अदालत तक घसीटा जा सके, और वहां उनकी जुबान पर लगाम लगाई जा सके।
दूसरा एक और तरीका लोकतांत्रिक जागरूकता वाले सभ्य समाज में हो सकता है, लेकिन उसकी गुंजाइश हिन्दुस्तान में कम ही दिखती है। यहां पर अगर ऐसी गंदगी की बात करने वाले लोगों से जुड़े हुए सभी सामानों का बहिष्कार किया जा सकता, तो भी बहुत से लोगों के होश ठिकाने आ जाते। लेकिन एक तरफ तो पश्चिम के जागरूक देशों में तीसरी दुनिया के देशों में बहुत कम मजदूरी देकर, अमानवीय स्थितियों में बनवाए गए सामानों का बहिष्कार किया जाता है, और वैसे बहिष्कार के असर से सामान बनाने वाले इन देशों में मजदूरों की हालत कुछ सुधरती है। भारत जैसे देश में बाल मजदूरों से बनवाए गए कालीनों का दुनिया के दूसरे देश बहिष्कार करते हैं, लेकिन हिन्दुस्तानी घरों में बाल मजदूरों को बंधुआ बनाकर रखा जाता है, और दफ्तरों और बाजारों में बाल मजदूर चाय पहुंचाते हैं, जिनसे किसी को परहेज नहीं होता। दरअसल इस देश और इसके प्रदेशों में संवैधानिक जिम्मेदारियों के आयोगों में राजनीतिक मनोनयन होने से वहां बैठे लोग अपने राजनीतिक आकाओं को असुविधा का कोई काम नहीं करना चाहते, और इस तरह सुधार की संवैधानिक-संभावना खत्म हो जाती है।
आज जरूरत तो यह भी लगती है कि मानवाधिकार आयोग, बाल आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग की कुर्सियों पर राजनीतिक मनोनयन खत्म होना चाहिए, और किसी भी राज्य में इन ओहदों पर राज्य के बाहर की एक राष्ट्रीय फेहरिस्त से लोगों को मनोनीत करने का एक संवैधानिक ढांचा खड़ा करना चाहिए। जब तक राजनीति से संवैधानिक पदों को अलग नहीं किया जाएगा, तब तक समाज के कमजोर तबकों के खिलाफ हिंसक बकवास जारी रहेगी। अभी दिल्ली के करीब यूपी में भाजपा के बताए जा रहे एक नेता ने जिस गंदी जुबान में एक महिला को धमकाया, उस पर भारी जनदबाव के चलते पुलिस कार्रवाई तो हुई है, लेकिन उत्तरप्रदेश में कोई महिला आयोग भी है, ऐसा पता नहीं लगा है। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
बिहार में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह एनडीए को छोडक़र और मुख्य विपक्षी लालू यादव और कांग्रेस से हाथ मिलाकर नई सरकार बनाने का रास्ता बना लिया है, वह पिछले दो दिनों का सबसे बड़ा भूचाल रहा। कांग्रेस ने इस मौके पर पिछली बार के नीतीश के साथ के गठबंधन की तरह बिना शर्त नीतीश का समर्थन करने की घोषणा की है, और हर विधायक के समर्थन के जरूरत आज इस नई गठबंधन सरकार को होगी। लेकिन इसके पहले कि नीतीश कुमार एक बार और शपथ लें, या सरकार बनाएं, उसके पहले ही उनके समर्थकों ने नीतीश कुमार के अगले प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी होने की घोषणाएं शुरू कर दी हैं। और शायद लालू यादव की राजद ने भी इन घोषणाओं को अपना अपमान मानने के बजाय तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना मानकर उनका स्वागत ही किया है। देश में एक दिन के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उम्मीदवारी के खिलाफ विपक्ष की एक बड़ी उम्मीदवारी की उम्मीद बंध गई है। जिन लोगों को यह लगता था कि मोदी चाहे अच्छे न हों, उनके मुकाबले कौन? उन लोगों को अब एक ऐसा विकल्प मिल गया है जो कि कांग्रेस के मुकाबले अधिक पार्टियों को मंजूर हो सकता है। लेकिन जिस कांग्रेस ने आज बिहार की सरकार से भाजपा को बाहर करने के लिए नीतीश का साथ दिया है, वह कल प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए क्या करेगी? क्योंकि देश में आम चुनाव के हिसाब से, और वोटरों की गिनती के हिसाब से कांग्रेस आज भी नीतीश कुमार की जेडीयू से बड़ी पार्टी है, यह एक अलग बात है कि उसके पास नीतीश जितना वजनदार, और अधिक सर्वमान्य कोई नेता नहीं है, राहुल गांधी भी नहीं।
इसलिए बिहार तो आज निपट जाएगा, या कि यह कहना बेहतर होगा कि निपट चुका है, लेकिन अभी से लेकर 2024 के आम चुनाव तक मुद्दा यह रहेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप के मामले में मोदी के एकाधिकार को जो चुनौती नीतीश कुमार दे सकते हैं, उसमें कौन सी पार्टी किस हद तक उनके साथ रहेगी? पल भर के लिए कांग्रेस को किनारे करके बाकी पार्टियों को देखें, तो आरजेडी और वामपंथियों ने बिहार सीएम के लिए तो नीतीश का जिस तरह साथ दिया है, ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री पद के लिए एनडीए विरोधी चेहरा बनाने के लिए वे नीतीश के साथ नहीं रहेंगे। बल्कि मोदी जिस तरह एक टीना फैक्टर (देयर इज नो ऑल्टरनेटिव), कोई विकल्प नहीं है का मजा ले रहे थे, वह मजा रातोंरात खत्म हो गया है। और अब लोगों का अंदाज यह है कि मोदी सरकार के हाथों बुरी तरह जख्मी और प्रताडि़त तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बैनर्जी अपनी सीमित अपील पर दांव लगाना छोडक़र शायद मोदी-विरोधी उम्मीदवार के रूप में नीतीश का साथ देंगी। ऐसा भी दिखता है कि दक्षिण भारत में तेलंगाना के केसीआर से लेकर तमिलनाडु के द्रमुक सीएम स्टालिन तक कई लोग नीतीश के हिमायती हो सकते हैं। फिर महाराष्ट्र में भाजपा से जख्मी शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी अब तक बने हुए हैं, और इन तीनों पार्टियों के अनगिनत लोग मोदी सरकार की मार के शिकार हैं, और महाराष्ट्र में भाजपा के मुकाबले नीतीश की लीडरशिप वाले किसी गठबंधन में ये तीनों पार्टियां शामिल हो सकती हैं। फिर भाजपा से त्रस्त और नष्ट कुछेक और पार्टियां भी हैं, पंजाब में अकाली हैं, कश्मीर में महबूबा हैं, और अलग-अलग जगहों पर कुछ दूसरी पार्टियां हैं। भाजपा से तमाम रिश्तेदारी के बावजूद नीतीश कुमार कई अजीब वजहों से अब तक साम्प्रदायिक तमगे से बचे हुए हैं, मुसलमानों के बीच उनकी ठीकठाक विश्वसनीयता कायम है, और छोटी-छोटी बहुत सी पार्टियां उनका साथ दे सकती हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल अगले आम चुनाव के वक्त कांग्रेस के सामने रहेगा जिसके पास देश में पिछले आम चुनाव के करीब 12 करोड़ वोट थे, और उसके सहयोगियों के पास और भी वोट थे। ऐसे में जेडीयू से बड़ी पार्टी होने के नाते उसकी महत्वाकांक्षा अपने नेता राहुल गांधी पर केन्द्रित हो सकती है, और अपने अस्तित्व को खोकर कांग्रेस किस सीमा तक नीतीश कुमार की अगुवाई मंजूर करेगी, यह अंदाज लगाना आज आसान नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के भाजपा-गठबंधन से बाहर आने से देश में एनडीए विरोधी प्रधानमंत्री की संभावना जितनी बढ़ी है, नीतीश की वजह से ही कांग्रेस के किसी नेता की प्रधानमंत्री-प्रत्याशी होने की संभावना उतनी ही घट गई है। यह कांग्रेस के सामने एक ऐतिहासिक मौका रहेगा कि वह मोदी-विरोधी गठबंधन की नेता बनने के बजाय बेहतर संभावनाओं वाले एक बड़े गठबंधन की भागीदार बने, या न बने। अभी 2024 खासा दूर है, इसलिए कांग्रेस तुरंत ही अपना कोई रूख दिखाने के लिए दबाव में नहीं है, लेकिन नीतीश के आने से भाजपा-विरोधी पार्टियों के भीतर जो उत्साह दिख रहा है, वह इन चर्चाओं को बहुत दबने भी नहीं देगा। यह सिलसिला कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा और नया दबाव भी पैदा करेगा क्योंकि पार्टी आज वैसे भी घरेलू बेचैनी और निराशा से गुजर रही है, अपने संगठन के चुनाव करवाने की हालत में नहीं है, और उसके पास आज कुल दो राज्यों में सरकार रह गई है। कांग्रेस की एक दिक्कत यह भी है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन दोनों ही राज्यों में संगठन के भीतर एक बेचैनी बनी हुई है, और सोनिया परिवार ईडी के दफ्तर में बैठा हुआ तो इन मुद्दों को देख भी नहीं सकता।
कुल मिलाकर बिहार में भाजपा की एक बहुत बड़ी शिकस्त, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आई है, पहले तो उसे 2024 के चुनाव तक अपनी दो राज्य सरकारों को सम्हालना है, संगठन के नेताओं को सम्हालना है, अदालती मामलों और ईडी की जांच को देखना है, और 2024 के किसी संभावित विपक्षी गठबंधन में अपनी जगह को महत्वपूर्ण और सम्मानपूर्ण बनाने की कोशिश भी करनी है। ऐसी किसी भी संभावना के लिए कांग्रेस को अपने आपको मजबूत भी करना होगा, और उसकी मजबूती का सबसे बड़ा सुबूत उसकी दो राज्य सरकारों का मजबूत रहना, और ठीकठाक चलना होगा क्योंकि उसके पास अपनी नीतियों पर अमल की बस यही दो जगहें तो हैं। आने वाला वक्त जितना नीतीश को देखने का रहेगा, उतने का उतना कांग्रेस को भी देखने का रहेगा, क्योंकि अगर किसी विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं रहेगी, वह मैदान में अलग से रहेगी, तो वह मोदी के लिए क्रिकेट की जुबान में वॉकओवर जैसा रहेगा।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
आज 9 अगस्त को दुनिया भर में मूल निवासियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। हिन्दुस्तान में इन्हें आदिवासी कहा जाता है, लेकिन एक राजनीतिक सोच इस शब्द के खिलाफ है, और वह इन्हें वनवासी कहने पर अड़ी रहती है। खैर, आज की चर्चा इस छोटी सोच से परे की है, और आदिवासियों के मुद्दे पर इस सीमित जगह में एक व्यापक बात करने के लिए है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर दुनिया भर में बिखरी आदिवासियों या मूल निवासियों की दुनिया के अस्तित्व को मान्यता देने के हिसाब से, उनका सम्मान करने के हिसाब से 9 अगस्त को यह दिन मनाना तय किया गया। हिन्दुस्तान में भी आदिवासियों की एक बड़ी आबादी है, और आज इस सालाना जलसे में क्या सचमुच उनके लिए खुशी मनाने का कुछ है?
दुनिया के विकसित देशों में पिछले कुछ दशकों में यह जागरूकता पैदा हुई है कि वहां के शहरी शासकों ने लोकतंत्र के नाम पर, और शहरी-संगठित धर्म के नाम पर मूल निवासियों के साथ पीढिय़ों तक जो जुल्म किया, उनके लिए आज की सरकार, और संसद को माफी मांगनी चाहिए। कुछ ऐसा ही कैथोलिक ईसाईयों के मुखिया पोप को भी लगा, और उन्होंने अभी कनाडा जाकर वहां के मूल निवासियों से माफी मांगी कि चर्च ने पीढिय़ों तक उनके साथ उन्हें ‘शहरी और सभ्य’ बनाने के नाम पर जुल्म किए। आज जब हिन्दुस्तान में केन्द्र और राज्य सरकारों की तरफ से आदिवासी समुदाय को बधाई दी जा रही है, तो ऐन उसी वक्त उन पर तरह-तरह के गैरकानूनी, कानूनी, और संवैधानिक जुल्म जारी हैं। लोगों को लग सकता है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में संवैधानिक जुल्म कैसे ढहाए जा सकते हैं, लेकिन इस बात के पुख्ता सुबूत हैं कि इस देश में आदिवासियों पर गैरकानूनी मार जितनी पड़ रही है, उतनी ही मार उन शहरी कानूनों की पड़ रही है जो कि शहरियों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए हैं, और जिन्हें आदिवासियों पर लादा जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में ही आदिवासी इलाके, हसदेव, के सबसे घने जंगल आज केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, और अडानी के निशाने पर हैं, और वहां की प्रकृति का क्या होगा, वहां बसे लोगों का क्या होगा, और छत्तीसगढ़ के इस फेंफड़े का क्या होगा, कुछ भी तय नहीं है। इसी छत्तीसगढ़ के एक दूसरे सिरे पर बस्तर में आदिवासियों के साथ हिंसा का एक लंबा इतिहास है, और पन्द्रह बरस की भाजपा सरकार के वक्त जो जुल्म हुए हैं, आदिवासियों को थोक में मारा गया है, उसकी जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद भी मौजूदा कांग्रेस सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आदिवासियों के मामले में इन दो अलग-अलग पार्टियों के रूख में क्या फर्क समझा जाए? क्या कुछ आदिवासियों को मंत्री बना देने से ही देश-प्रदेश में आदिवासियों को हक मिल जाते हैं? हकीकत तो यह है कि दलित, आदिवासी, या ओबीसी, किसी भी तबके के नेता सत्ता पर पहुंचने के बाद अपने वर्ग-चरित्र को खो बैठते हैं, अपने वर्गहित को इस्तेमाल किए गए कंडोम की तरह फेंक देते हैं, और सत्ता-चरित्र में ढल जाते हैं। इसलिए किसी सरकार की आदिवासी नीति वही मानी जानी चाहिए जो काम उसने किए हैं। आज भारत सरकार का एक फैसला खबरों में अधिक नहीं आया है, खुद आदिवासी समाज के भीतर इस पर अधिक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आदिवासियों के बीच के कुछ जागरूक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बात को उठाया है, और इस बात पर तुरंत ही आगे व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
अंग्रेजों के वक्त हिन्दुस्तान में 1872 से हर दस बरस में की जा रही जनगणना को अगर देखें तो शुरू से लेकर 1941 तक जनगणना में आदिवासियों, या मूल निवासियों के लिए अलग से एक दर्जा था। बाकी धर्मों के लिए अलग कॉलम थे, और आदिवासियों के लिए अलग कॉलम। पूरी दुनिया की तरह हिन्दुस्तान के आदिवासी भी किसी भी आधुनिक, शहरी, और संगठित धर्म से अलग थे, और अंग्रेजों की जनगणना में उन्हें वैसा रखा भी गया था। लेकिन आजादी के बाद 1951 की पहली जनगणना में आदिवासियों का कॉलम हटा दिया गया, और ‘अन्य’ नाम के कॉलम में उन्होंने अपनी जगह पाई। वह सिलसिला भी 2011 तक चलते रहा, जब छह प्रमुख शहरी धर्मों को कॉलम मिले, और आदिवासियों को ‘अन्य’ कॉलम में खड़े रहने की जगह मिली। अभी झारखंड की एक आदिवासी कार्यकर्ता गीताश्री उरांव ने एक इंटरव्यू में इस मुद्दे को उठाया है कि 2021 की जनगणना में इस ‘अन्य’ कॉलम को ही खत्म कर दिया गया है, और इसके साथ ही आदिवासियों की पहचान ही जनगणना में खत्म हो गई है। कोरोना की वजह से यह जनगणना समय पर नहीं हो पाई है, और 2023 में यह होने वाली है। लेकिन आज सवाल यह उठता है कि अगर हाल के तीन हजार बरस में पैदा हुए शहरी धर्मों के बीच दसियों हजार बरस से चले आ रहे आदिवासियों की पहचान को बांटने पर इस देश की सरकार आमादा है, तो फिर आज आदिवासी दिवस मनाने की क्या जरूरत है?
संविधान में आदिवासी इलाकों में से कुछ इलाकों में आदिवासी समुदायों, और गांवों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। उनकी ग्रामसभाओं के फैसलों को शहरी लोकतंत्र भी नहीं कुचल सकता। लेकिन हो इसका ठीक उल्टा रहा है, छत्तीसगढ़ में ही राज्यपाल ने पिछली रमन सिंह सरकार को भी चिट्ठियां लिखी थीं कि आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार अपने अधिकार से बाहर जाकर काम कर रही है। और वैसी ही चिट्ठियां राज्यपाल ने आज की कांग्रेस सरकार को भी लिखी हैं। लेकिन इन चिट्ठियों ने सरकारों को आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में अपने फैसले लादने से नहीं रोका है, और छत्तीसगढ़ के एक के बाद एक कई राज्यपालों ने सरकारों को चिट्ठियां लिखने से अधिक कुछ नहीं किया। राज्यपालों ने तो आदिवासियों की थोक में की गई हत्याओं की जांच रिपोर्ट पर भी कार्रवाई करने को नहीं कहा। यह पूरा सिलसिला अपने आपमें भयानक है, लेकिन यह अधिक भयानक इसलिए है कि देश भर की सरकारें आदिवासियों का भला करने का दावा भी करती हैं, लेकिन उनके बुनियादी मानवाधिकार भी कुचले जा रहे हैं, उनका कत्ल किया जा रहा है।
जब कभी कोई दिन मनाया जाता है, तो उस दिन ये तमाम बातें और तल्खी से सूझती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह कि अभी चार दिन बाद हिन्दुस्तान में आजादी की कमी की बात सूझेगी। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए, और किसी भी तरह के दिवस मनाने का पाखंड भी खत्म होना चाहिए। ऐसे दिन मनाना धर्मों के उन दिनों की तरह है जब अपने किए जुर्म को पाप मानकर उनका प्रायश्चित किया जाता है, और फिर धुली हुई साफ आत्मा पाकर अगले एक साल फिर जुर्म किया जाता है। कुछ ऐसा ही आजादी की सालगिरह पर भी होता है, और आदिवासी दिवस पर भी। हिन्दुस्तान में एक मजबूत किसान आंदोलन ने यह साबित किया है कि बिना हिंसा के लोकतांत्रिक आंदोलनों से हक किस तरह पाया जा सकता है। आज हिन्दुस्तान में ऐसे ही आदिवासी आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की सरकारों की तरह हिन्दुस्तान की सरकारें आदिवासियों से अगले सौ बरस में भी माफी तो मांगने से रहीं। और आदिवासियों को ऐसी किसी माफी का इंतजार भी नहीं करना चाहिए, ऐसा इंतजार मंदिरों के बाहर दाखिले के इंतजार में खड़े दलितों के इंतजार की तरह का होगा जो कि पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आदिवासियों को इस देश में रही-सही अदालती संभावनाओं पर भी काम करना चाहिए, और सडक़ की लड़ाई भी लडऩी चाहिए। आज जब उन्हें संविधान की नोंक पर मजबूर किया जा रहा है कि वे तीन हजार बरस में पैदा हुए धर्मों में से किसी एक को मानें, तो उन्हें संविधान के इस बेजा इस्तेमाल के खिलाफ भी खुलकर लडऩा चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल देश में बलात्कार की घटनाओं पर कहा है कि 2012 में निर्भया गैंगरेप के बाद कानून में हुए बदलाव की वजह से बलात्कार के बाद हत्या के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने कहा कि जब से कानून बदलकर बच्चियों से रेप करने वाले को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है तब से हत्याएं ज्यादा होने लगी हैं। उन्होंने कहा कि बलात्कारी जब देखता है कि पीडि़ता उसके खिलाफ कल गवाह बन जाएगी, तो वो रेप भी करता है, और बच्चियों की हत्या भी कर देता है।
जिस वक्त इस कानून में बदलाव की बात हो रही थी, कानून और समाज के बहुत से और जानकारों की तरह हमने भी इसी जगह पर यह बात लिखी थी कि बलात्कार पर हत्या के बराबर सजा कर देने से बलात्कार की शिकार को मार डाले जाने का खतरा बढ़ जाएगा। लोगों को लगेगा कि जब बलात्कार की सजा भी उतनी ही मिलनी है, तो फिर हत्या करके एक गवाह खत्म कर दिया जाए, और सजा तो उससे भी उतनी ही मिलेगी। कई कानून ऐसे जनदबाव के बीच बनते हैं जब सत्तारूढ़ लोगों, या कि अदालत के जजों को भी फैसले लेते-देते हुए यह ख्याल रहता है कि लोग क्या कहेंगे? जज भी इस दबाव से परे नहीं रह पाते, और लोगों के वोट से जीतने वाले नेता तो लोगों का चेहरा देख-देखकर ही फैसले लेते हैं। इसलिए बहुत से ऐसे मौके रहते हैं जब जनता के आंदोलन के चलते पुलिस किसी बेकसूर को भी पकडक़र अदालत में पेश कर देती है, और वहां से वे छूट जाते हैं। कई बार पुलिस और दूसरे सुरक्षाबल अपने साथियों की बड़ी मौतों के बाद उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए बेकसूर लोगों को या तो मुठभेड़ बताकर मार डालते हैं, या फिर बेकसूरों को पकडक़र उन पर मुकदमा चलाने लगते हैं, जैसा कि हाल ही में बस्तर में 120 से अधिक बेकसूर आदिवासियों की रिहाई से साबित हुआ है। दूसरी तरफ उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में सांप्रदायिक तनाव के चलते सत्तारूढ़ पार्टी अपने को नापसंद लोगों के घर-दुकान पर बुलडोजर चलाने लगती है क्योंकि उसे अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की साम्प्रदायिक हिंसक भावनाओं को शांत करना है, और दूसरे धर्म के लोगों को सबक सिखाना है।
दबाव में किया गया कोई भी काम न्यायोचित नहीं हो पाता है। संसद या विधानसभा में कई बार सत्ताबल के दबाव में ऐसे विधेयक पास हो जाते हैं, और कानून बन जाते हैं जो कि जनविरोधी होते हैं, या जिनके साथ बेजा इस्तेमाल का खतरा अधिक बड़ा होता है, बजाय उनसे फायदा होने के। भारतीय संसद में ऐसे बहुत से कानून बने हैं, जो कि जनदबाव में बने, या जनता को लुभाने के लिए बने, या संसद के भीतर सत्ता के अपार बाहुबल के मुकाबले विपक्ष की सीमित आवाज को कुचलते हुए बने। ये सारे कानून आगे जाकर बड़ी दिक्कत खड़ी करते आए हैं, और उनमें कई किस्म की सुधार की नौबत भी आती है। बच्चियों से बलात्कार पर फांसी की सजा का प्रावधान इसी तरह का एक कानून था जिसे लेकर कम से कम अब केन्द्र और राज्य सरकारों को यह सर्वे करना चाहिए कि क्या ऐसे मामलों में बलात्कार की शिकार बच्चियों की हत्याओं के मामले बढ़े हैं?
अभी बहुत से अलग-अलग ऐसे मामलों के वीडियो सामने आते हैं जिनमें राजनीतिक ताकत से लैस कोई बाहुबली किसी महिला से बदसलूकी कर रहा है, या कि कोई अफसर अपनी मातहत महिला से। ऐसे तमाम मामलों को लेकर कानून में एक संशोधन की जरूरत है कि जब कभी अधिक ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर कोई जुल्म ढाते हैं, उन ताकतवर लोगों को आम लोगों के मुकाबले अधिक कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए, और उनकी संपन्नता के अनुपात में उन पर जुर्माना भी लगाना चाहिए। आज जब अदालत किसी अरबपति पर दो हजार रूपये का जुर्माना लगाती है, और जब किसी मानवाधिकार कार्यकर्ता पर जनहित याचिका लगाने पर पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाती है, तो अदालत के इंसाफ पर से भरोसा उठ जाता है। कल ही देश के एक बड़े वकील, और यूपीए सरकार के समय कानून मंत्री रहे हुए कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट पर से उनका भरोसा उठ गया है। जिस आदमी की पूरी जिंदगी ही कानून के साथ गुजरी हो वह अगर आज सार्वजनिक रूप से मंच से माईक पर यह बात कह रहा है, तो इससे आम गरीब लोगों के कानून पर से भरोसा उठ जाने में कोई हैरानी नहीं रहनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपना सदमा जाहिर करते हुए निराशा में यह बात कही है, लेकिन आज देश के बहुत से लोगों का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी नाजायज आ रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि देश की संसद बहुत से गलत कानून बना रही है। जिन तीन किसान कानूनों को मौजूदा मोदी सरकार ने अपने संसदीय बाहुबल से बना ही दिया था, उन्हें एक बरस से अधिक लगातार चले अभूतपूर्व किसान आंदोलन ने वापिस लेने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अगर उतना लंबा आंदोलन नहीं चला होता तो वे कानून तो देश पर लागू हो ही चुके थे। इसलिए एक बात बिल्कुल साफ है कि संसद या विधानसभा के भीतर असंतुलित ताकत लोकतंत्र को मजबूत करने के काम की नहीं रहती, उससे सत्तारूढ़ पार्टी गलत कानून बनवा सकती है, बनाती है। अब इस एक संदर्भ को छोडक़र बात करें, तो लोगों का यह तर्क भी हो सकता है कि भारतीय लोकतंत्र में जब संसद या विधानसभा में किसी पार्टी या गठबंधन का बाहुबल पर्याप्त नहीं होता है, तो उसके लोगों को तोड़-फोडक़र, खरीदकर सरकार गिराई भी जा सकती है, गिराई जाती है।
आज यहां पर लिखी गई बातें टुकड़ा-टुकड़ा कई मुद्दों को छूती हुई हैं, और इन सब पर अलग-अलग सोचने की जरूरत है, और एक साथ मिलाकर भी।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
लोकतंत्र जब कमजोर होता है, तो कई तरफ से होने वाले हमलों की वजह से कमजोर होता है, किसी एक वजह से नहीं। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान एक ही दिन दो आजाद मुल्क बने थे, और हिन्दुस्तान अभी कुछ बरस पहले तक लोकतंत्र के पैमानों पर एक मजबूत देश माना जाता था। हाल के बरसों में इस देश में लोकतांत्रिक ढांचा बुरी तरह कमजोर हुआ है, लेकिन फिर भी जब कभी पड़ोस के पाकिस्तान से इसकी तुलना की जाती है तो यह एक बेहतर, और एक अधिक विकसित लोकतंत्र दिखता है। दरअसल लोगों की नजरों में आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक विकास के बीच कई बार कोई फर्क नहीं भी रह जाता है। लोग देश के बेहतर ढांचे को बेहतर लोकतांत्रिक विकास भी मान लेते हैं। इस पैमाने से तो तेल की दौलत से रईस बने हुए खाड़ी के देश सबसे अधिक लोकतांत्रिक मान लिए जाने चाहिए क्योंकि वहां आधुनिक सुविधाओं का ढांचा सबसे विकसित है, या उस सिंगापुर को अधिक लोकतांत्रिक मान लेना जाना चाहिए जहां लोगों के नागरिक अधिकार कम हैं। इसलिए भारत के आर्थिक विकास को भारत का लोकतांत्रिक विकास भी मान लेना एक खुशफहमी की बात हो सकती है, जिससे समझदार लोगों को बचना चाहिए।
अब आज इस तुलना और चर्चा की जरूरत इसलिए आ पड़ी है कि ताजा खबर यह है कि पाकिस्तान में पिछले प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी, पीटीआई, के 123 सांसदों के इस्तीफों के बाद किश्तों में मंजूर किए जा रहे इस्तीफों से अब तक ग्यारह सीटें खाली हुई हैं, और इमरान खान ने उनमें से जनरल सभी नौ सीटों पर खुद चुनाव लडऩे की घोषणा की है। वहां की मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी के साथ संसद के भीतर और बाहर चल रही लगातार तनातनी के बीच अपनी पार्टी का बाहुबल दिखाने के लिए इमरान खान ने यह घोषणा की है, पिछली बार भी वे पांच सीटों पर लड़े थे, और कानून के मुताबिक उन्हें जीती गई पांच सीटों में से चार से इस्तीफा देना पड़ा था। इस बार अगर वे सभी ग्यारह सीटों पर जीतते हैं, तो दस सीटों पर उपचुनाव की नौबत आएगी जो कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में कम खर्चीला काम नहीं होता है। पड़ोस के श्रीलंका में सरकार पर से लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है, हर कोई यही मान रहे हैं कि यह चुनाव करवाने का सही मौका है, लेकिन वहां चुनाव करवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए हर उस देश में जहां गरीबी है, यह भी देखना चाहिए कि लोग संवैधानिक अधिकारों का ऐसा बेजा इस्तेमाल न करें जो कि जनता पर ही खर्च बनकर टूट पड़े। हिन्दुस्तान में भी कई बार बड़े-बड़े नेताओं को जब यह आशंका रही कि किसी एक सीट पर उन्हें बुरी तरह हराया जा सकता है, या उनके खिलाफ कोई साजिश की जा सकती है, तो उन्होंने दो सीटों से भी चुनाव लड़ा है। लेकिन इसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, और यह माना जाता है कि यह हौसले की कमी का नतीजा है। इमरान खान के बारे में यह कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ चल रही तरह-तरह की जांच में जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने के लिए वे ऐसी हरकत कर रहे हैं कि बहुत सी सीटों पर जीतकर वे अधिक वजनदार साबित हो सकें, और जांच प्रभावित हो सके। जो भी हो, यह सिलसिला सिरे से गलत है, और हिन्दुस्तान में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सौ चुनिंदा सीटों पर भी लडक़र उनमें से अधिकतर सीटों पर जीत सकते हैं, और बाकी तमाम सीटों पर बाद में एक मिनी आम चुनाव की नौबत आ सकती है। लेकिन इसका खर्च तो देश पर ही आएगा।
हिन्दुस्तान में बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री इस्तीफे की नौबत आने पर बीवी या बच्चों को चुनाव लड़वाकर तब तक सीट भरी रखते हैं, जब तक वे खुद दुबारा चुनाव लडऩे लायक नहीं हो जाते। मध्यप्रदेश में ही कमलनाथ का मामला ऐसा ही था, उन्हें एक विवाद के चलते लोकसभा सीट छोडऩी पड़ी थी, उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाकर जिता दिया, और फिर खुद चुनाव लडऩे की नौबत आने पर पत्नी से इस्तीफा दिलवाकर खुद चुनाव लड़ा, और शायद इस रूख को अहंकारी मानते हुए जनता ने उन्हें उनकी परंपरागत सीट से हरा ही दिया था। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह इमरान पांच सीटों पर लड़े और इस बार ग्यारह सीटों पर लडऩे की मुनादी की है, उसकी तो कोई मिसाल किसी तानाशाही में भी नहीं मिलती। जिस पाकिस्तान में लोकतंत्र ठीक से पनप नहीं पाया है, उसी पाकिस्तान में कोई नेता लोकतंत्र के नाम पर इस दर्जे की तानाशाही और बेशर्मी दिखा सकते हैं।
लेकिन हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और ऐसे दूसरे देशों से भी लोकतंत्र को कुछ सीखते चलने की जरूरत रहती है। जिस तरह हिन्दुस्तान में बहुत से लोकतांत्रिक मूल्य कुचले जा रहे हैं, और लोकतांत्रिक परिपक्वता, राजनीतिक जागरूकता खत्म की जा रही है, वह जरूरी नहीं है कि सिर्फ चुनावों को प्रभावित करे, वह रोज की जिंदगी को भी प्रभावित कर सकती है, और उसका नुकसान राजनीति से परे भी रोज की जिंदगी में देखने मिल सकता है। पाकिस्तान में किसी वक्त फौज को बढ़ावा दिया गया, तो किसी वक्त एक धर्म को देश का राजकीय धर्म बना लिया गया। इससे आगे चलकर लोकतांत्रिक संस्थान कमजोर होते चले गए, और धर्म बढ़ते-बढ़ते धार्मिक आतंकवाद में तब्दील हो गया। वहां अल्पसंख्यक मारे जाने लगे, और अब तो पाकिस्तान की सरकार भी अगर चाहती है कि अल्पसंख्यक न मारे जाएं, तो भी वह रोक पाना सरकार के बस में नहीं रह गया है। जब लोकतांत्रिक संस्थान कमजोर होते हैं तो देश में ताकतवर संस्थाएं भ्रष्ट होने लगती हैं, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह इसका शिकार रहा, वहां के प्रधानमंत्री और फौजी तानाशाह देश छोडक़र दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हुए क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत से मामले रहे। लेकिन आज पाकिस्तान में एक सहूलियत या दिक्कत यह हो गई है कि तकरीबन तमाम पार्टियां भ्रष्ट हैं, और किसी पर इस बात को लेकर बदनामी का कोई खास खतरा नहीं रह गया है। हिन्द महासागर के इस इलाके में ये देश अड़ोस-पड़ोस के हैं, और भारत को अपने इन सरहदी देशों के साथ तजुर्बों से सबक लेना भी सीखना चाहिए। पाकिस्तान और श्रीलंका आज जिस बदहाली में पहुंचे हुए हंै, उसमें धर्मान्धता का खासा हाथ रहा है, अल्पसंख्यकों पर ज्यादती का खासा हाथ रहा है, और इस एक बात का सबक तो भारत को तुरंत ही लेना चाहिए। इन देशों के मुकाबले भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था भारत में लोकतंत्र की बेहतर स्थिति का सुबूत नहीं है, इस धोखे में आने से भी लोगों को बचना चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
एक-एक करके देश के सभी बड़े अखबारों ने इस बात पर रिपोर्ट छाप ली है कि बस्तर में किस तरह करीब सवा सौ बेकसूर आदिवासियों को एनआईए ने नक्सल आरोपों में पांच बरस तक जेल में सड़ाए रखा, और अदालत से उनकी जमानत तक नहीं हो सकी क्योंकि वे सब बहुत गरीब थे। अब जब ये इतने बरस बाद लौटकर जिंदगी का सामना कर रहे हैं, तो रोज कमाने-खाने वाले लोगों के न रहने से परिवारों का जो हाल हुआ है, वह पता लग रहा है। और यह हाल आदिवासी इलाकों से बाहर शहरी इलाकों में और अधिक खराब इसलिए होता है कि वहां लोगों के खर्च कुछ अधिक होते हैं, परिवार की पढ़ाई और इलाज पर भी खर्च लगता है, और बिना कमाऊ सदस्य के परिवार तबाह हो जाते हैं। इस देश में न्याय व्यवस्था का हाल इस कदर खराब है कि बेकसूर को अदालत में बेकसूर साबित होकर छूटने में एक पूरी जिंदगी निकल जाती है, और तब तक परिवार के लोगों की जिंदगी तबाह भी हो जाती है। पिछले दिनों एक ही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश दोनों ने ऐसी नौबत को लेकर फिक्र जाहिर की थी, और देश का अदालती ढांचा सुधारने की अपील मुख्य न्यायाधीश ने की थी ताकि गरीबों के साथ भी इंसाफ हो सके। आज की अदालती हकीकत यह है कि पुलिस से लेकर दूसरी तमाम जांच एजेंसियों तक भ्रष्टाचार की वजह से सबसे दौलतमंद और ताकतवर लोग तो अपनी मर्जी के सुबूत और गवाह पा जाते हैं, अदालतों में उनके महंगे वकील केस को उनकी सहूलियत से तेज या धीमा कर देते हैं, लेकिन गरीब की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है।
प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायााधीश की इन बातों के बाद सोशल मीडिया पर सामाजिक मुद्दों पर लिखने वाले कुछ गंभीर लोगों ने लगातार यह भी लिखा है कि देश में जज सबसे कम काम करते हैं, सबसे अधिक दिन छुट्टियां मनाते हैं, और यह सिलसिला भी बदलना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर लिखे लोगों से परे कल एक और बात हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की एक बेंच ने एक सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार के वकील से कहा कि देश जब अपनी आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है तो केन्द्र सरकार को अदालती हालत सुधारने के लिए लीक से हटकर कुछ करना चाहिए, और सरकारी वकील सरकार को इस बात के लिए राजी करें कि स्वतंत्रता दिवस के पहले ऐसा कुछ किया जाए ताकि जनता तक एक संदेश जाए। यह बेंच अदालती मामलों में होने वाली अंधाधुंध देरी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही थी, और उसमें प्रतीकात्मक रूप से ही सरकार से यह बात कही है। इन जजों ने अदालत में ही कहा कि किसी को बीस या पच्चीस साल सलाखों के पीछे रखने का क्या तुक है? किसी को लंबे समय तक जेल में रखने से उसका सुधार नहीं हो जाता। जजों ने कहा कि जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लंबी मुकदमेबाजी इसका हल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये बेकसूर साबित होते हैं तो इन सालों को कौन लौटाएगा?
हमारे पाठकों को याद होगा कि हम महीने भर में दो बार इसी जगह यह लिख चुके हैं कि अदालत से बेकसूर बरी होने वाले लोग अगर गरीब हैं, तो उन्हें देश की न्यूनतम मजदूरी के मुताबिक उतने दिनों की मजदूरी दी जानी चाहिए। यह तो कम से कम मुआवजा हो सकता है, जो कि बिना देर किए शुरू होना चाहिए। सबसे गरीब परिवारों को इससे थोड़ी सी मदद मिल सकती है, लेकिन परिवारों की पूरी जिंदगी तबाह होती है, और उसके लिए दूसरा ही रास्ता निकालना होगा। आज अदालतों पर मामलों का बोझ किस वजह से इतना बढ़ा हुआ है, यह एक अलग शोध का विषय हो सकता है। हो सकता है कि वकीलों की भी दिलचस्पी मामले को लंबा खींचने में हो, और अदालत के कर्मचारियों की भी, जिन्हें कि हर पेशी पर हर किसी से कुछ न कुछ रिश्वत वसूलने का मौका मिलता है। ऐसे में अदालती ढांचे को बढ़ाना तो एक सीधा-सीधा इलाज दिख रहा है, और प्रदेशों की निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में बहुत सी कुर्सियां खाली रहती हैं, जिन्हें भरा जाना चाहिए ताकि मामलों की सुनवाई तेज हो सके। लेकिन जिस देश के आईआईएम और आईआईटी से निकले हुए लोग आज दुनिया की कई सबसे बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, वैसी काबिलीयत वाले लोगों से योजना बनवाकर भारत की अदालती प्रक्रिया क्यों नहीं सुधारी जा सकती? अदालती कामकाज का कम्प्यूटरीकरण, जेलों से वीडियो कांफ्रेंस पर सुनवाई से काम की रफ्तार बहुत बढ़ सकती है, और सुप्रीम कोर्ट सरकार से सीधे-सीधे यह कह सकती है कि अदालत के काम के सिस्टम को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट और टेक्नालॉजी संस्थानों की मदद ली जाए। आज टेक्नालॉजी जिंदगी के कई दायरों में काम की लागत भी घटा रही है, और हो सकता है कि तरीके बदलने से ही इतनी ही लागत में, इतने ही लोगों से अदालती कामकाज तेज हो जाए। लेकिन जब तक यह पूरा सिलसिला चलता है, तब तक भी अदालतों को कम से कम गरीबों के मामले में यह रूख अपनाना चाहिए कि वे जमानत का इंतजाम करने की ताकत नहीं रखते हैं, और सामाजिक बराबरी तभी हो सकेगी जब उन्हें बिना किसी इंतजाम के जमानत मिल सके। ऐसा करके भी अदालतों पर से एक बड़ा बोझ कम किया जा सकता है, और उस क्षमता का इस्तेमाल बाकी मामलों को तेजी से निपटाने में हो सकता है।
अब कुछ दिन पहले मुख्य न्यायाधीश की कही बातों, और कल सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की इस बेंच की कही बातों के बाद अब गेंद सरकार के पाले में है, और यह उम्मीद बहुत बड़ी नहीं होगी कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त के अपने भाषण में अदालती व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस घोषणा करें। देश भर में तिरंगे झंडे फैलाने जैसे प्रतीकों से बेहतर है कि आज देश भर में जो करोड़ों लोग जेलों में हैं, जिनमें से बहुत बड़ी संख्या में बेकसूर गरीब हैं, उन्हें आजाद कराया जाए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
छत्तीसगढ़ में कल एक बुरा सडक़ हादसा हुआ, जिसमें मौतें तो कुल तीन हुईं, लेकिन उनसे सरकार के इंतजाम की कमजोरी उजागर हुई है। एक नौजवान लडक़े ने अपनी गर्लफ्रेंड को कार का स्टियरिंग थमा दिया जिसे कि कार चलाना आता ही नहीं था। नतीजा यह हुआ कि उसने इलाज के लिए अस्पताल जाते हुए एक बाईक पर सवार तीन लोगों को कार से बहुत बुरी तरह ठोकर मारी, और उसमें तीनों लोगों की मौत हो गई। जख्मी कार सवार लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और कार को जब्त किया है। सडक़ों पर इस तरह की गैरकानूनी बददिमाग हरकत छत्तीसगढ़ के शहरों में बड़ी आम बात है। यहां आबादी के एक छोटे तबके के पास इतना अधिक पैसा है कि वह सिर चढक़र बोलता है। शहरों में महंगी गाडिय़ों पर सवार बददिमागी दूसरों के लिए खतरा बनी हुई दिखती ही रहती है। कहने के लिए पुलिस यह आंकड़े पेश कर सकती है कि उसने पिछले कितने हफ्तों में कितने लोगों पर क्या-क्या चालानी कार्रवाई की है, लेकिन कानून तोडऩे वालों के मुकाबले चालान पटाने वालों का अनुपात बड़ा छोटा सा दिखता है, और यही नतीजा है कि सडक़ों पर दूसरों के हक कुचलते हुए बददिमागी दिखाने वाले लोग कभी कम होते नहीं दिखते हैं। अब हिन्दुस्तानी सडक़ों पर बड़ी से बड़ी गाडिय़ां आम दिखने लगी हैं, और एक-एक शहर में लाखों रूपये से अधिक दाम वाली हजारों मोटरसाइकिलें भी दौड़ती हैं। नतीजा यह होता है कि जेब में रखे क्रेडिट कार्ड की ताकत के साथ जब गाड़ी का हॉर्सपॉवर मिलता है, तो मिजाज नीम चढ़े करेले सरीखा हो जाता है।
आज एक दिक्कत यह भी है कि पुलिस अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को पूरा करने के बजाय हर नौबत में यह तौलने में लगी रहती है कि किसी ऐसे का चालान न हो जाए जो कि उनका ही ट्रैफिक से बस्तर के किसी थाने में तबादला करवाने की ताकत रखता हो। और यह डर छोटे-छोटे सिपाहियों का ही नहीं रहता है, आज इस प्रदेश में बड़े से बड़े पुलिस अफसर लगातार इस तनाव में काम करते हैं कि उनके काम से सत्ता में ताकत रखने वाले कोई लोग नाराज न हो जाएं। नतीजा यह होता है कि सत्तारूढ़ बददिमागी या सत्ता तक पहुंच रखने वाली बददिमागी लोगों को रौंदते चलती है। इस नौबत को सुधारने का एक अच्छा तरीका कुछ हफ्ते पहले केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सुझाया था। उन्होंने बताया था कि ऐसा एक कानून लाया जा रहा है जिसमें ट्रैफिक नियम तोडऩे वाले लोगों के वीडियो बनाकर लोग पुलिस को भेज सकेंगे, और अगर वे चालान करने लायक होंगे, तो जुर्माने का एक हिस्सा वीडियो भेजने वाले लोगों को भी मिलेगा। हमने इसकी तारीफ में इसी जगह लिखा था कि इससे लोगों में नियम का सम्मान बढऩे तक कई लोगों को एक मजदूरी या रोजगार सरीखा भी मिल सकेगा। लेकिन इस पर कई जागरूक लोगों ने यह लिखना शुरू कर दिया था कि सरकार की ऐसी सोच लोगों को आपस में लड़वाने की है। यह लोगों का काम नहीं है कि वे ट्रैफिक सुधारें, सरकार अपने हिस्से का काम लोगों पर डाल रही है। ऐसी सोच पर हमें बड़ा अफसोस हुआ था क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में नियम-कानून लागू करने का काम अकेले सरकार का नहीं होता है, यह पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। और अगर समाज अपनी किसी भी तरह की जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहता है, तो फिर इसकी कीमत उसे बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बढ़ाकर देनी होगी, जिसका आर्थिक बोझ जनता पर ही आएगा। जनता के बीच से अगर ऐसी जागरूकता निकलती है जो कि सडक़ों पर अराजकता करने वाले लोगों को कैमरों पर कैद करके पुलिस को भेजे, और एक ईनाम पाए, तो इससे दोहरा फायदा होगा। जरूरतमंदों को आर्थिक मदद मिलेगी, और नियम तोडऩे वाले लोगों को यह पता होगा कि आसपास पुलिस नहीं दिख रही है तो भी उनके गैरकानूनी काम के सुबूत पुलिस तक पहुंच सकते हैं।
देश भर के बहुत से प्रदेशों में ऐसा हाल होगा कि लोग अपने छोटे बच्चों को गाडिय़ां देकर खुश होते होंगे। लेकिन ऐसे बच्चे सडक़ों पर औरों के लिए बड़ा खतरा बनते हैं। इनके अलावा नशे में गाड़ी चलाने वाले, अंधाधुंध रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले लोग भी कम नहीं हैं। हम तो आसपास यह देखकर थक जाते हैं कि एक चौथाई दुपहिया वाले एक हाथ में मोबाइल पकडक़र, या सिर और कंधे के बीच उसे फंसाकर सामने तिरछा देखते हुए गाड़ी चलाते जाते हैं। अब इस सिलसिले को रोकने की भी जरूरत है, और कड़े नियमों का इस्तेमाल करके इन लोगों की गाडिय़ां भी राजसात करनी चाहिए, और इनके लाइसेंस भी रद्द करने चाहिए। सडक़ों पर नियम तोडऩे का सीधा मतलब दूसरों की जान के लिए खतरा खड़ा करना होता है, और पुलिस या आरटीओ के लोग ऐसे भ्रष्ट और अराजक लोगों को किसी की जिंदगी नहीं देख सकते। हिन्दुस्तान के प्रदेशों को सभ्य और सुरक्षित बनना चाहिए, और नियम तोडऩे वाले लोगों की सुबूत सहित शिकायत पुलिस को करनी चाहिए, यह काम पुलिस की मुखबिरी करने जैसा नहीं है, यह काम अपने आपको सुरक्षित रखने का भी है। रोजाना कई मौतें छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से प्रदेश में भी सडक़ों पर हो रही हैं, और सडक़ से जुड़े सरकारी महकमों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
अभी दुनिया यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद शुरू हुई जंग को ही बड़ी मुश्किल से झेल पा रहा है। इन दो देशों से दूर, धरती के बिल्कुल दूसरी तरफ बसे हुए देशों तक भी इस जंग के धमाकों से अर्थव्यवस्था में दरारें पड़ रही हैं। चारों तरफ पेट्रोलियम और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, अनाज और खाद की कमी हो रही है, और महंगाई से परे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो कि अंतरराष्ट्रीय दान में मिले अनाज पर जिंदा है, और वह हिस्सा भूख से मौत की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि यूक्रेन में जमा अनाज बाहर निकल नहीं पा रहा है। इस जंग में अपनी फौजें न भेजते हुए भी योरप और अमरीका हथियार भेजकर शामिल तो हो ही चुके हैं, लेकिन इस बीच एक नया टकराव एक नई सरहद पर हो रहा है, वह भी दुनिया के लिए रूस-यूक्रेन से बड़ी फिक्र का सामान हो सकता है।
अमरीकी कांग्रेस (संसद) की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी उस ताइवान में पहुंची हुई हैं जिसे चीन अपना एक हिस्सा मानता है। और दशकों से यह तनाव चल रहा है, चीन अपना फौजी बाहुबल दिखाते रहता है, ताइवान किसी टकराव से बचकर एक कामयाब कारोबारी देश बन चुका है। और इस तनाव के बीच अमरीका अपनी पूरी ताकत के साथ ताइवान के पीछे खड़ा दिखता है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो अमरीका उसका जवाब देगा। हालांकि अमरीका की घोषित विदेशनीति में ताइवान की फौजी मदद की घोषणा नहीं है, लेकिन अमरीका की कही बातों का लब्बोलुआब वही रहता है कि वह ताइवान पर किसी भी चीनी हमले के वक्त ताइवान का साथ देगा। अभी जब अमरीकी संसद की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी के ताइवान जाने की खबर आई तो चीन ने जमकर विरोध किया, और उसका यह कहना था कि ताइवान उसी का हिस्सा है, और वहां पर एक प्रमुख अमरीकी नेता का आना चीन बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी सरकार ने यह साफ कर दिया कि संसद की अध्यक्ष सरकार के मातहत नहीं आती, और संसद एक स्वायत्त संस्था है, इसलिए उसकी अध्यक्ष का कार्यक्रम अमरीकी सरकार तय नहीं करती। फिलहाल तनातनी के बीच नैंसी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी हैं, और चीन अपना फौजी बाहुबल दिखाते हुए ताइवान के करीब अपने फाइटर प्लेन उड़ा रहा है, करीब के समंदर में चीन और अमरीका के फौजी जहाज पहुंचे हुए हैं, और यह तनाव का एक नया मोर्चा खुला है।
वैसे तो जब से यूक्रेन पर रूसी हमला हुआ, तभी से यह चर्चा चल रही थी कि क्या इससे प्रेरणा लेकर चीन भी ताइवान पर हमला करेगा? लेकिन यूक्रेन के मुकाबले आज की बाकी दुनिया ताइवान पर अधिक दूर तक टिकी हुई है, और अगर ताइवान किसी जंग में फंसता है, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था इस बुरी तरह गिरेगी कि जिसका अंदाज लगाना भी आज मुश्किल है। दरअसल ताइवान हर किस्म की मशीन और कम्प्यूटर में लगने वाले सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है। अगर किसी वजह से ताइवान में ये कारखाने थमते हैं, तो पूरी दुनिया में मोबाइल फोन से लेकर कार-टीवी तक, और कम्प्यूटरों तक का उत्पादन ठप्प पड़ जाएगा। एक अकेला देश दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक धडक़न को रोकने वाला साबित होगा। ऐसा नहीं कि आज लोगों को इसका अंदाज नहीं है, लेकिन यूक्रेन के तुरंत बाद ताइवान को लेकर एक फिक्र की नौबत इतनी जल्दी आएगी, यह बात किसी को नजर नहीं आ रही थी। फिर लोगों को इस बात पर भी हैरानी हो रही है कि अमरीकी संसद की अध्यक्ष को आज अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच ताइवान का साथ देने के लिए इस तरह वहां पहुंचकर चीन के साथ तनाव बढ़ाने की बात क्यों सूझी? अभी यह बात साफ नहीं है कि अमरीकी सरकार और वहां की संसद-अध्यक्ष के बीच इस मुद्दे पर कितनी सहमति बनी है, या नहीं बनी है। लेकिन इस एक दौरे से, नैंसी पेलोसी के लौटते ही चीन ने ताइवान की फौजी नाकेबंदी कर दी है, और उसके आसपास फौजी कसरत छेड़ दी है। मानो इसके जवाब में अमरीका ने अपना एक सबसे बड़ा जंगी जहाज वहीं पास में पहुंचा दिया है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था ऐसा कोई टकराव झेलने की हालत में नहीं है जिससे कि तमाम देशों के इलेक्ट्रॉनिक कारोबार ठप्प हो जाने का खतरा रहे। इससे दुनिया के कारोबार के सामने यह सोचने का एक सामान भी आ खड़ा हुआ है कि किसी एक नाजुक और जरूरी पुर्जे को लेकर क्या किसी एक देश पर इतना आश्रित रहना समझदारी की बात है?
ताइवान और चीन के बीच ऐतिहासिक तनाव हमेशा से चले आ रहा है, और ताइवान चूंकि चीन की फौजी ताकत के मुकाबले कहीं नहीं टिकता, इसलिए वह बिना टकराव अपनी आर्थिक तरक्की करने में लगे रहता है। अमरीका की कोई अतिरिक्त हमदर्दी ताइवान से हो, ऐसी कोई वजह नहीं है, लेकिन आज दुनिया के फौजी भूगोल में दुश्मन के दुश्मन देश को दोस्त बनाने का जो सिलसिला चलता है, उसी के तहत चीन के दुश्मन अमरीका को, चीन का दूसरा दुश्मन ताइवान सुहाता है। लेकिन ताइवान आज अपने कारोबारी एकाधिकार को लेकर दुनिया पर एक खतरनाक नौबत खड़ी करता है कि अगर उसके कारखाने ठप्प हुए, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप्प हो जाएगी। और यह अर्थव्यवस्था उन कारोबारों की ठप्प होगी जो कि रूस-यूक्रेन जंग से प्रभावित नहीं हैं। दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक कारोबार अगर ठप्प होगा, तो दुनिया भर की सरकारों का टैक्स भी मार खाएगा। इसलिए यह खतरा रूस-यूक्रेन के खतरे से बड़ा हो सकता है।
आज चीन और अमरीका, ये दोनों ही देश अपनी ताकत को बढ़ाने और अपने प्रभाव क्षेत्र को फैलाने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। फिर आज रूस की घेरेबंदी करते हुए पश्चिमी देशों ने रूस के चीन पर आश्रित होने को भी बढ़ा दिया है। दुनिया की महाशक्तियों के बीच संतुलन की यह एक नई नौबत है, और अभी तस्वीर साफ भी नहीं है। इसलिए आने वाला वक्त यह बताएगा कि ताइवान को लेकर अमरीका और चीन के बीच तनाव बढ़ता है, या कि बांहें फडक़ाने के बाद ये दोनों देश चुप बैठेंगे। फिलहाल ऐसे कोई भी अंतरराष्ट्रीय तनाव फिक्र तो खड़ी करते ही हैं क्योंकि दुनिया मौजूदा तनावों से भी उबर नहीं पा रही है।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अभी 11 लोगों को बच्चों के पोर्नो वीडियो इंटरनेट पर डालने और उन्हें फ़ैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। हर कुछ महीनों में इस राज्य में ऐसी गिरफ्तारी हो रही है, और देश में तो हर दिन कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है। बच्चों के पोर्नो का एक मतलब यह भी होता है कि उनका देह-शोषण भी हो रहा है।
दो बरस पहले उत्तरप्रदेश से बच्चों के सेक्स-शोषण का एक भयानक मामला सामने आया था जिसमें सिंचाई विभाग का एक इंजीनियर, रामभवन सिंह, बच्चों को इधर-उधर से जुटाकर उनका यौन शोषण करता था, और उनके वीडियो बनाकर इंटरनेट पर बेचता था। दस साल से वह यह काम करते आ रहा था, लेकिन उसके रिश्तेदारों को भी इसकी भनक नहीं लगी थी। फिर जब किसी सुराग से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तो उसके पास बच्चों के पोर्नो का जखीरा मिला है। अब तक की जांच से पता लगा है कि वह गरीब परिवारों के 5 से 16 बरस तक की उम्र के बच्चों को अपना निशाना बनाता था। उसके पास से इतने डिजिटल सुबूत बरामद हुए थे कि इस मामले में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसकी जांच सीबीआई कर रही थी. यह अफसर बच्चों को मोबाइल पर वीडियो गेम खेलने के बहाने बुलाता था और उनका सेक्स-शोषण करता था।
इसके पहले 2017 में केरल में पुलिस ने लोगों के एक ऐसे समूह को पकड़ा था जो कि आपस में अपने बच्चों के अश्लील वीडियो बनाकर, उनकी नग्न तस्वीरें खींचकर शेयर करते थे, और इस समूह को चलाने वाले ने ऐसे पांच हजार लोगों को जुटा लिया था। यह मुस्लिम नौजवान इस बात की वकालत करता था कि जब तक बच्चियां चार बरस की रहें, उनसे बलात्कार करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इस उम्र की बातें उनको याद नहीं रहती। यह आदमी अपनी ही बच्चियों से बलात्कार करते उनके भी वीडियो पोस्ट करता था। केरल पुलिस ने इन पांच हजार लोगों को पकडऩे की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये लोग मोबाइल फोन के एक ऐसे मैसेंजर, सिग्नल, का इस्तेमाल करते हुए जहां किसी को पकड़ा नहीं जा सक रहा है। इन लोगों ने अपने सरीखे हजारों लोगों के साथ ऐसे वीडियो शेयर करने का काम कर रखा था और इसमें गिरफ्तारियां शुरू हो गई है।
लेकिन इतने बड़े मामलों का भांडाफोड़ होने से इसकी गिरफ्तारी के साथ-साथ अब आगे उन लोगों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए जो कि बच्चों के पोर्नो खरीदते हैं। इंटरनेट के जानकार लोग यह जानते हैं कि इंटरनेट पर आसानी से पकड़ में न आने वाला एक डार्क वेब होता है जिस पर तरह-तरह के मुजरिम काम करते हैं और वहां ऐसे वीडियो की खरीद-बिक्री भी होती है। हिन्दुस्तान में सीबीआई को तलाशते हुए योरप की किसी पोर्नो वेबसाईट पर एक हिन्दुस्तानी बच्चे का ऐसा पोर्नो मिला और वहां से ढूंढते हुए जांच एजेंसी रामभवन तक पहुंची।
इस मामले का भांडाफोड़ होने से हिन्दुस्तान के लोगों की आंखें खुलनी चाहिए कि बच्चों का यौन-शोषण कोई विदेशी सोच नहीं है, यह देशों की सरहदों से परे इंसानों के बीच एक आम बात है, और ऐसे अधिकतर लोग बच्चों का सेक्स-शोषण करने के बाद भी बच निकलते हैं क्योंकि बच्चे अपने घर या स्कूल में अपने शोषण की बात बताते भी हैं तो भी उनके ही लोग उस पर भरोसा नहीं करते। धीरे-धीरे बच्चों में बताने का हौसला खत्म होने लगता है। अब अगर एक अफसर 50 से अधिक बच्चों का शोषण कर चुका है, उसके कब्जे से दर्जनों वीडियो और सैकड़ों तस्वीरें मिली हैं, वह इंटरनेट पर पोर्न साईट्स को ये वीडियो बेच देता था, और बच्चों से सेक्स भी करते रहता था, 10 बरस तक उसका कोई भांडाफोड़ नहीं हो सका, तो यह नौबत भारतीय समाज के एक खतरनाक हाल को बताती है।
दुनिया के बाकी तमाम देशों के साथ-साथ हिन्दुस्तान के समाज को जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि गरीब और बेघर बच्चे, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों की पहुंच के भीतर के बच्चे हमेशा ही खतरे में रहते हैं। हिन्दुस्तान में मां-बाप अपने बच्चों की शिकायतों को इसलिए भी सुनना नहीं चाहते क्योंकि ये शिकायतें कई तरह की असुविधा खड़ी करने वाली रहती हैं, रिश्तेदारों या पहचान वालों से रिश्ते बिगड़ते हैं, पुलिस थाने और कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगते हैं, और जैसे कि आम हिन्दुस्तानी सोच है, सेक्स-हमले के शिकार लोगों के लिए ही यह मान लिया जाता है कि उनकी इज्जत लुट गई है। इस देश में बलात्कारी की इज्जत नहीं लुटती, बलात्कार के शिकार की इज्जत लुटती है। ऐसे देश में शिकायत लेकर किसी बच्चे का सामने आना नामुमकिन सा रहता है।
हिन्दुस्तान अपने डिजिटल विकास पर बड़ा गर्व करता है। लेकिन यहां चारों तरफ साइबर-ठगी चलती रहती है, साइबर-जालसाजी, और साइबर-जुर्म एक बड़ा कारोबार बन चुका है। ये तमाम जुर्म सरकार के काबू के बाहर दिखते हैं। इसी तरह चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सरकार की पकड़ बहुत कम दिख रही है जबकि कई अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियां और दूसरे संगठन लगातार चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर नजर रखकर संबंधित सरकारों को सावधान करने का काम करते हैं। हिन्दुस्तान सरकार को ऐसे डिजिटल औजार विकसित करने चाहिए जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करने वाले लोगों को पकड़े। हाल के महीनों में छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी बहुत से लोग दिल्ली से मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन वॉट्सऐप जैसे तकनीक के चलते लोग दूसरे किस्म के सेक्स-पोर्नो के साथ-साथ बच्चों के सेक्स-पोर्नो भी एक-दूसरे को भेजते रहते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनकी खबरें पढक़र बाकी लोगों को एक सबक मिल सके।
लेकिन बच्चों के सेक्स-शोषण का मुद्दा एक अलग पहलू भी रखता है। छोटे-छोटे सामानों का लालच, कई बार तो बेघर बच्चों के लिए एक रात सिर छुपाने की जगह या कंबल मिल जाना भी उन्हें अपने बदन का समझौता करने पर मजबूर कर देता है। इस देश में जब तक बच्चों की आम हालत नहीं सुधरेगी, जब तक वे बेघर और अनाथ बने रहेंगे, तब तक मोटे तौर पर उनका शोषण नहीं थम सकेगा। इसलिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी का यह मामला बच्चों से बलात्कार के अनगिनत मामलों का एक पुख्ता सुबूत भी है। और सरकार को इस जुर्म का व्यापक प्रचार करके देश के बाकी मां-बाप, समाज के लोगों को सावधान भी करना चाहिए कि उनके इर्द-गिर्द ऐसी कोई हरकत दिखे तो वे तुरंत पुलिस को खबर करें। एक अफसर 10 बरस तक दर्जनों बच्चों का सेक्स-शोषण करते रहा, उसकी रिकॉर्डिंग करते रहा, उसे दुनिया भर में बेचते रहा, और किसी को उसकी खबर नहीं लगी, यह बात भी हैरान करने वाली है।
यह मामला सरकार और समाज दोनों के सावधान और चौकन्ने होने का है।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
मध्यप्रदेश में भोपाल में बीटेक की पढ़ाई करने वाले 21 बरस के एक छात्र, निशांक राठौर की लाश एक पटरी पर कटी हुई मिली, और उसके फोन से उसके पिता को भेजा गया ऐसा मैसेज मिला जो मुस्लिमों द्वारा दी गई धमकी सरीखा लग रहा था। उसमें लिखा था- नबी से गुस्ताखी नहीं, राठौर साहब आपका बेटा बहुत बहादुर था। इस छात्र के इंस्टाग्राम अकाऊंट पर भी ऐसा लिखा मिला- सारे हिन्दू कायरों देख लो, अगर नबी के बारे में गलत बोलोगे तो यही हश्र होगा। इससे अधिक टीवी चैनलों को और क्या लगता था। भडक़ाने वाले पोस्टर बनाकर टीवी समाचार बुलेटिन चलने लगे, और इस घटना को राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड और अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड की अगली कड़ी की तरह पेश किया जाने लगा। अब भाजपा शासित मध्यप्रदेश की पुलिस ने इस मामले की जांच करने के बाद यह पाया है कि इस नौजवान का फोन स्क्रीन लॉक किया हुआ था, और उसे किसी और ने नहीं खोला था। पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि इस छात्र ने कर्ज न चुका पाने की वजह से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी, न कि उसकी हत्या हुई। जांच अफसर ने बताया कि उसने करीब 18 ऑनलाईन ऐप्प से लोन ले रखा था, और दोस्तों से भी कर्ज ले रखा था, और चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उसने आत्महत्या करने के पहले अपने पिता को साम्प्रदायिक किस्म का मैसेज भेजा जिसमें सिर तन से जुदा करने की बात लिखी, ऐसी ही बात उसने अपने इंस्टाग्राम अकाऊंट पर डाली।
लेकिन 24 जुलाई की शाम मिली इस लाश को लेकर 25 जुलाई से ही सोशल मीडिया पर इसे एक हिन्दू पर मुस्लिम हमला बताते हुए, इसे एक साम्प्रदायिक हत्या बताते हुए मुहिम छेड़ दी गई थी, जो कि टीवी चैनलों की मेहरबानी से जंगल की आग की तरह फैल रही थी। यह तो गनीमत है कि यह हादसा एक भाजपा शासित राज्य में हुआ है जहां एक हिन्दू नौजवान की ऐसी मौत का शक मुस्लिमों पर होने के बावजूद पुलिस ने यह पाया है कि इसमें कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं था, और यह आत्महत्या थी। अगर यह मामला किसी गैरभाजपा राज्य का रहता, तो वहां की पुलिस पर मुस्लिमों को बचाने की तोहमत लग सकती थी, कम से कम भाजपा के राज्य में यह तोहमत तो नहीं लग सकती। लेकिन अब ऐसे में सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले लोगों, और देश के टीवी समाचार चैनलों के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि किसी एक घटना की जांच भी पूरी होने के पहले उसे लेकर नफरत का सैलाब फैला देने की इनकी नीयत का क्या किया जाए? अभी चार दिन पहले ही देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने बड़ी तल्खी के साथ देश के टीवी समाचार चैनलों को कोसा था, और सोशल मीडिया को उससे भी अधिक खराब बताया था। सोशल मीडिया तो खैर किसी एक दिमाग से नियंत्रित मीडिया नहीं है, और वहां पर करोड़ों लोग लगातार लिखते रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो मीडिया को मिलने वाले तमाम किस्म के विशेषाधिकार, और पहुंच का इस्तेमाल करता है, और उसके बाद नफरत फैलाने का गैरजिम्मेदार काम, बल्कि बेहतर यह कहना होगा कि जुर्म भी करता है। अब भोपाल की यह घटना इसका एक ताजा सुबूत है कि मुस्लिमों की तरफ इशारा करने वाले ऐसे संदेशों के बीच एक हिन्दू मौत की जांच कर रही पुलिस वैसे ही दुनिया भर के दबाव में रही होगी, और उस पर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हमला होते रहा। यह तो गनीमत है कि पुलिस ने एक हफ्ते की शुरुआती जांच में ही पूरी तरह से यह स्थापित कर दिया कि यह बिना किसी बाहरी हरकत के, सीधी-सीधी आत्महत्या है, वरना अब तक तो सडक़ों पर मुस्लिमों पर हमले होने लगते।
हर कुछ दिनों में ऐसी नौबत आती है जब हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक बड़े हिस्से के बारे में यह बात लिखनी पड़ती है कि भारत सरकार अपने पास सुरक्षित बड़े कड़े अधिकारों पर बैठी हुई क्यों है, और देश में नफरत और साम्प्रदायिकता फैलाकर अपना कारोबार बढ़ाने की ऐसी खुली साजिश के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? देश के मुख्य न्यायाधीश कुछ ही दिन पहले सार्वजनिक भाषण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में दुनिया भर का कहकर जाते हैं, और उसके बाद भी आज ऐसी हरकत जारी है। बल्कि मुख्य न्यायाधीश के बयान के दिन से ही यह ताजा नफरती सैलाब चल रहा है। इस देश में केन्द्र सरकार ने टीवी चैनलों के कामकाज की निगरानी के लिए एक संस्था बना रखी है, दूसरी तरफ पहले से चली आ रही प्रेस कौंसिल है जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज रहते हैं, हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि भोपाल के इस मामले को ही एक नमूना मानकर इस पर टीवी चैनलों के कवरेज की जांच करवाए, और उस पर केन्द्र सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहे। आज टीवी समाचार चैनलों का एक बड़ा हिस्सा देश के किसी भी साम्प्रदायिक संगठन के मुकाबले अधिक साम्प्रदायिक हो चुका है, और वह किसी भी दूसरे साम्प्रदायिक संगठन के मुकाबले अधिक सक्रिय भी है। देश में बनाए गए बड़े कड़े कानून धरे हुए हैं, और हिंसा भडक़ाने की यह हरकतें चल रही हैं जिनके बारे में मुख्य न्यायाधीश यह भी कह चुके हैं कि मीडिया पर मानो एक मुकदमा चलाया जाता है, और उसके दबाव में जजों के लिए भी काम करना मुश्किल हो जाता है। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए, हम आज की बात को खत्म करते हुए एक बार फिर दुहरा रहे हैं कि अखबारों को मीडिया नाम की इस बड़ी छतरी से बाहर निकल जाना चाहिए, और अपने को टीवी से अलग, अपने पुराने नाम प्रेस का इस्तेमाल करना चाहिए। नफरती टीवी मीडिया के खिलाफ एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगनी चाहिए, और देखें कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यकाल के इन आखिरी कुछ हफ्तों में उस पर कुछ करते हैं या नहीं।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में एक मालवाहक गाड़ी में 27 तीर्थयात्रियों को ले जाया जा रहा था, अचानक इस पिकअप वैन में करंट दौड़ा, और 10 लोगों की मौत हो गई, कई लोग करंट से जख्मी हो गए। पुलिस का अंदाज यह है कि इस गाड़ी में डीजे सिस्टम चलाने के लिए जनरेटर लगाया गया था, और उसी की वायरिंग की गड़बड़ी से यह करंट दौड़ा हो सकता है। इस हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोडक़र भाग गया है, और शिवभक्तों के परिवारों को खबर की गई है। ऐसा हादसा हिन्दुस्तान के दो अलग-अलग पहलुओं पर फिक्र खड़ी करता है, एक तो यह कि धर्म का स्वरूप पूरी तरह अराजक हो गया है, वह आत्मघाती होने की हद तक लापरवाह हो गया है, और कई मामलों में हत्यारा होने की हद तक हिंसक भी हो गया है। दूसरा पहलू यह है कि सडक़ों पर हादसों में मरने वाले लोगों में दुनिया में हर दस में से एक हिन्दुस्तान में होते हैं, लेकिन देश-प्रदेशों में किसी को इसकी अधिक फिक्र नहीं दिखती है। धर्म पर आस्था के प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक जगहों पर लोग नियम-कानून के खिलाफ किसी भी हद तक जाते हैं, और यह हादसा उसी का एक नमूना है।
हिन्दुस्तान में आज धर्म तरह-तरह से जानलेवा साबित हो रहा है। अभी चार ही दिन हुए हैं, उत्तर भारत में कांवडिय़ों के एक जत्थे ने एक दूसरे कांवडिय़े को पीट-पीटकर मार डाला जो कि थलसेना का फौजी है, और अपनी आस्था के चलते कांवड़ लेकर जा रहा था। इससे परे भी जगह-जगह आस्थावान लोगों की हिंसा सामने आती रहती है, और अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच टकराव भी होते ही रहता है। फिर मानो एक धर्म के कट्टर और धर्मान्ध प्रदर्शन के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के लोग उससे अधिक बढ़-चढक़र प्रदर्शन में लग जाते हैं। नतीजा यह होता है कि सार्वजनिक जगहें धार्मिक, कट्टर, और बढ़ते-बढ़ते साम्प्रदायिक मुकाबले का मैदान बन जाती हैं, और हर धार्मिक त्यौहार पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आता है। उत्तरप्रदेश जैसे कुछ राज्यों में बहुसंख्यक हिन्दू धर्म को राजकीय धर्म सरीखा अघोषित दर्जा देकर धार्मिक टकराव की नौबत घटा दी गई है, क्योंकि गैरहिन्दुओं, और खासकर मुस्लिमों को यह अच्छी तरह मालूम है कि कांवडिय़ों पर हेलीकॉप्टर से या सडक़ किनारे खड़े होकर फूल बरसाने वाले आला पुलिस अफसरों का रूख उनके प्रति कैसा रहेगा अगर वे सडक़ पर कुछ मिनटों की नमाज पढ़ते दिख जाएंगे। जब प्रदेश का राज इस दर्जे का धार्मिक भेदभाव करने लगता है, तो सत्ता की ताकत के सामने टकराव की नौबत घट जाती है। राज्य-धर्म के मानने वाले लोगों, और दूसरे दर्जे के नागरिकों के बीच टकराव की गुंजाइश नहीं रह जाती है, क्योंकि सरकारी इंसाफ कमजोर तबके को हासिल नहीं रहता है।
जिस धर्म को निजी आस्था का सामान होना चाहिए था, वह राजनीतिक बढ़ावे से विकराल होते चल रहा है। त्यौहारों या तीर्थयात्राओं के मौके पर सडक़ों पर परले दर्जे का उत्पात दिखता है। और यह भी कम इसलिए दिखता है कि अधिकतर सीधे-सरल लोग सडक़ों पर अपना अधिकार भूलकर धार्मिक गुंडागर्दी के सामने खड़े नहीं होते। वे चुपचाप किसी और रास्ते से निकल जाते हैं, और किसी टकराव का खतरा नहीं उठाते। लेकिन सार्वजनिक जीवन में साल भर किसी न किसी तरह से अड़ंगा बनने वाले धर्म लोगों की उत्पादकता को भी कम करते हैं, और उनके जीवन का सुख-चैन भी छीनते हैं। चौबीसों घंटे धार्मिक लाउडस्पीकर बजते हैं, सडक़ों पर शामियाने तानकर कार्यक्रम होते हैं, भंडारे लगाकर चारों तरफ गंदगी छोड़ दी जाती है, विसर्जन से नदियों और तालाबों में अपार कचरा इकट्टा होते जाता है। इन सबसे परे लगातार बढ़ते साम्प्रदायिक तनाव और टकराव से लोगों की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। धार्मिक हिंसा में धर्म से परे चल रहे लोग भी घिर और फंस जाते हैं।
अब इससे जुड़े हुए दूसरे पहलू पर आएं, तो हिन्दुस्तान में सडक़ों पर गाडिय़ां धर्म से परे भी बहुत बुरी तरह बेकाबू हैं। गाडिय़ों से जुड़ा हुआ सारा ही सरकारी अमला संगठित भ्रष्टाचार चलाता है, और सामान ढोने वाली गाडिय़ों में मजदूरों और मुसाफिरों को ढोना रोजमर्रा की एक आम बात है। अब ऐसी गाडिय़ों में किसी हिफाजत का कोई इंतजाम तो हो नहीं सकता, इसलिए इनके हादसों में लोग बड़ी संख्या में मरते हैं। सरकारी नियमों का यह हाल है कि एक तरफ तो केन्द्र सरकार हर कार में आधा दर्जन एयरबैग लगाने का कानून बना रही है, ताकि लोगों की जिंदगी किसी हादसे में भी बच सके, दूसरी तरफ मजदूरों से लेकर तीर्थयात्रियों तक को सामान की तरह ढोने वाले ट्रकों और दूसरे कारोबारी वाहनों पर कोई रोक नहीं है। हालत यह है कि सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए भी सभी तरह की मालवाहक गाडिय़ों में जिंदगियां ढोई जाती हैं। अब देश में ऐसे दोहरे कानून से क्या फायदा जिसमें पैसे वाले लोगों की निजी कारों में भी हर मुसाफिर की जिंदगी बचाने एयरबैग लगाए जाएं, और गरीबों की जिंदगी जानवरों से भी कम कीमती मानी जाए। अगर मालवाहक गाडिय़ों में लोगों को ढोना बंद होगा, ऐसी गाडिय़ों को राजसात किया जाएगा, तो धीरे-धीरे मुसाफिर गाडिय़ां बढऩे लगेंगी। लेकिन नियमों का कोई सम्मान न करने की वजह से आज ऐसी अराजक नौबत है कि सामान या जानवर की तरह ठूंसकर इंसानों को ले जाया जाता है, और उस पर कोई रोक नहीं है। फिर जब ऐसी गाडिय़ों पर धार्मिक लोग सवार रहते हैं, तो उन्हें छूने की हिम्मत किसकी हो सकती है। राजनीतिक दलों का यह चरित्र बीते दशकों में लगातार अधिक उजागर होते चल रहा है कि वे सार्वजनिक-धार्मिक आयोजनों में भीड़ को बढ़ावा देकर अपनी जमीन बनाने की कोशिश करते हैं, और भीड़ अपने मिजाज के मुताबिक अराजकता पर चलते हुए राजनीतिक संरक्षण का अधिक मजा भी लेते चलती है।
लेकिन हर कुछ बरसों में किसी न किसी चुनाव में जाने वाली पार्टियों की हांकी जाती सरकारें कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती हैं। तो क्या अब सरकार की रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के लिए भी लोग अदालत जाएं? और अब तो यह भी खतरा हो गया है कि जनहित याचिका लेकर जाने वाले लोगों पर सुप्रीम कोर्ट पांच लाख रूपये तक का जुर्माना लगा सकता है, कैद सुना सकता है।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है जिसमें मुम्बई के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच से माईक पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा- कभी-कभी मैं यहां लोगों से कहता हूं कि महाराष्ट्र में, विशेषकर मुम्बई और ठाणे से, गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो, तो तुम्हारे यहां कोई पैसा बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो कहलाती है आर्थिक राजधानी, ये आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। वे इन्हीं समुदायों में से एक से जुड़े एक नामकरण समारोह में बोल रहे थे। और जैसी कि उम्मीद की जा सकती है, राज्यपाल के इस बयान के बाद आज विपक्ष में बैठे शिवसेना के उद्धव ठाकरे समेत तमाम लोग राज्यपाल पर टूट पड़े। ठाकरे ने शिवसेना के परंपरागत हमलावर तेवरों के साथ कहा- भगत सिंह कोश्यारी ने भले ही महाराष्ट्र की संस्कृति देखी हो, लेकिन उन्हें कोल्हापुरी जोड़ा भी दिखाना होगा। उल्लेखनीय है कि कोल्हापुरी चप्पलें विश्वविख्यात हैं। ठाकरे ने यह भी कहा कि राज्यपाल ने मराठी लोगों का अपमान किया है, और इसके साथ ही उन्होंने हिन्दुओं को बांटने की कोशिश भी की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने भी राज्यपाल के बयान से असहमति जताई है, और कहा है कि महाराष्ट्र के निर्माण में मराठियों का योगदान सबसे ज्यादा है, और मुम्बई देश की आर्थिक राजधानी सिर्फ मराठियों की मेहनत से बनी है।
भगत सिंह कोश्यारी जिस इतिहास के साथ आते हैं, उसमें इस तरह की अनर्गल बातें कहना अटपटा नहीं समझा जाता। और खासकर जब अलग-अलग तबकों के बीच भेदभाव को बढ़ाने की बात हो, तो उसमें ऐसे लोग अतिरिक्त सक्रियता के साथ जुट जाते हैं। उनका पर्याप्त राजनीतिक अनुभव है, और वे महाराष्ट्र के बाहर के भी हैं। इसलिए वे ऐसी बातों की नजाकत को भी समझते हैं, और इनके खतरों को भी। वे उत्तराखंड विधानसभा, विधान परिषद से होते हुए राज्यसभा और लोकसभा सभी का तजुर्बा रखते हैं, और इसके पहले भी वे महाराष्ट्र के कुछ सबसे सम्मानजनक लोगों के बारे में अनर्गल बातें कर चुके हैं। मार्च में ही उन्होंने सावित्री बाई फुले के बाल विवाह को लेकर उटपटांग बात कही थी जिस पर बड़ा बवाल मचा था। इसके अलावा उन्होंने समर्थ रामदास को छत्रपति शिवाजी का गुरू करार दिया था जो कि ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत बात है और उस समय सत्तारूढ़ कांग्रेस एनसीपी, शिवसेना गठबंधन ने उनके बयानों पर आपत्ति जताई थी, और कहा था कि सावित्री बाई फुले के बाल विवाह का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने जिस तरह हॅंसते हुए हाथों से कुछ इशारे किए थे, वह बहुत शर्मनाक था, गठबंधन ने कहा था कि ये महाराष्ट्र की बदनसीबी है कि उसे ऐसा गवर्नर मिला है। समर्थ रामदास को छत्रपति शिवाजी का गुरू बताने के पीछे भी महाराष्ट्र में यह वैचारिक विवाद चलता है कि ऐसा सुझाना ब्राम्हणों की गैरब्राम्हणों पर प्रभुत्व दिखाने की भावना है।
सार्वजनिक जीवन में जुबान पर लगाम देना किसी भी राजनीतिक दल में एक बुनियादी तालीम होनी चाहिए। जिस तरह प्राइमरी स्कूल में पहाड़ा और अक्षरज्ञान सिखाए जाते हैं, लिखना सिखाया जाता है, उसी तरह राजनीति में जुबान पर लगाम देना सिखाना चाहिए। ये राज्यपाल अकेले ऐसे नहीं हैं, अभी चार दिन पहले ही लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस लापरवाही के साथ राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया, उसने सदन के भीतर और बाहर बड़ी कड़वाहट घोल दी, और देश का मानो एक पूरा संसदीय दिन ही इस बदजुबानी को समर्पित हो गया। जो लोग राजनीति में लंबे समय से रहते हैं, उन्हें बदजुबानी की कोई रियायत नहीं दी जा सकती। और अधीर रंजन चौधरी तो इसके पहले भी मुंह खोलते ही पार्टी के लिए मुसीबत का सामान बनते रहे हैं। बहुत सी पार्टियों में बहुत से नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जुबान से अपनी पार्टी का नुकसान किया है। समाजवादी पार्टी के आजम खान के नाम को याद रखा जा सकता है जिन्होंने बलात्कार की शिकार एक छोटी बच्ची की लिखाई रिपोर्ट को राजनीतिक साजिश करार दिया था, और जिसके लिए उन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट की लताड़ भी पड़ी, और वहां जाकर माफी भी मांगनी पड़ी। ऐसे बयान ममता बैनर्जी से लेकर शरद यादव तक देते आए हैं, और ऐसी गंदगी बाद में दूसरी पार्टियों के लिए अपनी गंदगी के बचाव का तर्क बनती है।
चूंकि हिन्दुस्तान में अदालतों की एक सीमा है, और वैसे तो तमाम आबादी ऐसे बयानों को लेकर अदालत तक जाने के लिए आजाद है, लेकिन पहले से मामलों के बोझ से टूटी कमर वाली अदालतें और कितना बोझ झेल पाएंगी, इसका अंदाज लगाना अधिक मुश्किल नहीं है। इसलिए सार्वजनिक जीवन में बकवासी और मवादी बयान देने वाले लोगों के खिलाफ राजनीति और सार्वजनिक जीवन के लोगों को दूसरी संवैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर महिला आयोग, बाल आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग में जाकर शिकायत करने की गुंजाइश हो, तो वहां शिकायत करनी चाहिए, या फिर सार्वजनिक बयानों के हमले से ओछे और घटिया बयानों का जवाब देना चाहिए। जब तक ऐसे बकवासी लोगों को सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी बकवास जारी रहेगी। राज्यपाल के रूप में कोश्यारी अकेले नहीं हैं, और भी बहुत से राज्यपाल घटिया बातें करते आए हैं, घटिया हरकतें भी करते आए हैं। लोगों को याद होगा कि किस तरह के हालात में नारायण दत्त तिवारी को आन्ध्र का राजभवन छोडऩा पड़ा था, और उन्हें सेक्स वीडियो के विवाद के बीच वहां से निकलकर अघोषित संतान के डीएनए विवाद में आकर फंसना पड़ा था। राजनीतिक पार्टियों को भी अपने-अपने घटिया लोगों को काबू में रखना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से देश के जलते-सुलगते मुद्दे धरे रह जाते हैं, और पार्टियां बकवासी में उलझ जाती हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल एक मिसाल हैं कि राज्यपाल कैसे नहीं होने चाहिए। किसी समझदार ने कहा भी है कि बेवकूफ होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बेवकूफ को बढ़-चढक़र बोलने का शौक हो, तब दिक्कत बड़ी रहती है।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
उत्तरप्रदेश के कल तक के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज की कुछ अटपटी खबर है। आमतौर पर तो यह माना जाना चाहिए था कि शहर को धार्मिक नाम मिलने के बाद वहां का माहौल अधिक धार्मिक या आध्यात्मिक होगा, लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि इस शहर के स्कूली बच्चों में एक अजीब किस्म की हिंसा फैल रही है, जैसी कि बमों के शौकीन पश्चिम बंगाल में भी दिखाई-सुनाई नहीं पड़ी है। पुलिस ने वहां स्कूली बच्चों के कुछ गिरोह पकड़े हैं जो बम बनाकर उन्हें दूसरी स्कूलों के बाहर फोड़ रहे थे। ऐसे 35 स्कूली बच्चे प्रयागराज पुलिस की हिरासत में है, और रिपोर्ट कहती है कि पिछले कई महीनों से वहां पर सरेआम देसी बम मारने की वारदातें हो रही थीं। पुलिस का कहना है कि ये सभी बच्चे प्रयागराज के जाने-माने स्कूलों में पढ़ते हैं, और शुरुआती जांच में पता लगा है कि ओटीटी वेब सीरिज से प्रभावित होकर, उन्हीं के नामों पर इन छात्रों ने तांडव ग्रुप, जैगुआर ग्रुप, इम्मॉर्टल ग्रुप, माया ग्रुप जैसे गिरोह बनाए, इंटरनेट पर यूट्यूब से देखकर घरेलू बम बनाए, और एक दूसरे समूह पर दबदबा कायम करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए ऐसे बम फोड़े, और सोशल मीडिया पर इन वारदातों की शोहरत भी बढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि ऐसे किसी-किसी ग्रुप में तो छात्रों की संख्या सौ से लेकर तीन सौ तक भी है।
यह बड़ी अजीब सी खबर है, और लोगों को याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक शायद नाबालिग लडक़ी ने सडक़ पर एक साइकिल वाले के किनारे न होने पर उसका गला ही काटकर मार डाला, तब भी हमने ऐसी हिंसा के विश्लेषण की जरूरत बताई थी। बाद में आई खबरों में पता लगा कि वह लडक़ी एक गिरोह-सरगना बनना चाहती थी, और वह नशे के कारोबार से भी जुड़ी बताई गई थी। नाबालिग पीढ़ी की हिंसा और उसके जुर्म की बात अधिक बड़ी फिक्र इसलिए खड़ी करती है कि उसे शायद कानूनी जटिलताओं और जिंदगी के खतरों का पूरा अहसास नहीं रहता है। और भारत में नाबालिग बच्चों के किए हुए जुर्म पर उनके सुधार का इंतजाम इतना खराब है कि छत्तीसगढ़ में एक जगह ऐसे सरकारी केन्द्र पर इक_ा बच्चों ने छत पर चढक़र बाहर पुलिस या अफसरों पर गैस सिलेंडर फेंककर हमला करने की कोशिश की थी। जानकार लोगों का यह भी कहना है कि ऐसे सभी बाल सुधारगृह बच्चों को कई नए किस्म के जुर्म करना सिखाकर बिदा करते हैं, और कई तरह के नशे की भी आदत डालकर। हिन्दुस्तान में बच्चों को सुधारने का कोई भी असरदार सरकारी इंतजाम नहीं है, और इसलिए भी ऐसी नौबत आने देने से बचना चाहिए।
आज जब अलग-अलग कमरों में टीवी, या कि हर मोबाइल फोन पर तरह-तरह के वीडियो की सहूलियत, और उसका खतरा, दोनों ही मौजूद हैं, तो मां-बाप को चाहिए कि वे अपने बच्चों की हरकतों पर ध्यान दें, और पहली शिकायत का मौका आने के भी पहले उन्हें लेकर सम्हल जाएं। लोगों को याद होगा कि जो देश का सबसे चर्चित बलात्कार कांड था, उसमें निर्भया से बलात्कार और सबसे खूंखार दर्जे की हिंसा करने वालों में एक नाबालिग भी था। और एक नाबालिग के ऐसी हिंसा में शामिल होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यह बहस भी हुई थी कि क्या नाबालिगों को ऐसे जुर्म में भी उम्र की रियायत देना जायज है? अब दुनिया के अलग-अलग देशों में, और उनके अलग-अलग प्रदेशों में बच्चों की उम्र के पैमाने अलग-अलग हैं। उनके गाड़ी चलाने से लेकर उनके सिगरेट-शराब पीने तक की उम्र अलग-अलग है। जुर्म को लेकर भी, शादी की उम्र को लेकर भी ये नियम अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग हैं। ऐसे में हिन्दुस्तान में मौजूदा नियम-कानून को देखना चाहिए जिसमें किसी नाबालिग से कोई गलती होने पर, या उसके कोई गलत काम करने पर उसे जिस किस्म के सुधारगृह में भेजा जाएगा, वहां से उसका और बुरा मुजरिम होकर निकलना तय रहेगा। लोगों का पैसा, उनकी राजनीतिक पहुंच, और उनकी किसी और किस्म की ताकत उनके बच्चों को हमेशा ही कानून के शिकंजे से नहीं निकाल सकती। पुलिस और न्याय व्यवस्था कितनी भी भ्रष्ट क्यों न हो, आज वीडियो-सुबूतों की वजह से बहुत से नाबालिग भी अदालत में ले जाकर मुजरिम साबित किए जा सकते हैं, और उन्हें कई बरस सुधारगृह में रखा जा सकता है। हर मां-बाप को ऐसे सुधारगृहों के खतरों को बारीकी से समझ लेना चाहिए, और ऐसी नौबत नहीं आने देनी चाहिए कि उनके बच्चे ऐसी जगहों पर भेजे जाएं, और वे वहां से पूरी तरह बर्बाद होकर निकलें। उन्हें यह खतरा भी समझना चाहिए कि आज उनके बच्चे नाबालिग उम्र में सुधारगृह पहुंचेंगे, और फिर 18 बरस के होने पर उन्हें आम जेल भेजा जाएगा, और वहां की जिंदगी के तमाम किस्म के खतरों को यहां पर गिनाना भी मुमकिन नहीं है, लोगों को सिर्फ इतना समझना चाहिए कि इन जगहों से उनके बच्चे बलात्कार के शिकार होकर भी निकल सकते हैं, जो कि इन जगहों पर एक आम बात है।
अब जिस घटना से आज का यह लिखना शुरू किया गया है, उस प्रयागराज में लौटें, तो यह बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ तो उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पुलिस चारों तरफ, हर किस्म की मुठभेड़ भी कर रही है जिसमें जुर्म के आरोपियों को सडक़ पर ही निपटा दिया जा रहा है। यह तरीका ऐसी शोहरत पा चुका है कि अभी कर्नाटक में साम्प्रदायिक हत्या के जवाब में वहां के हिन्दू संगठनों और भाजपा नेताओं ने इसी योगी-शैली का राज कर्नाटक में भी मांगा है, और वहां कल ही एक मंत्री ने यह भरोसा भी दिलाया है कि जरूरत रहेगी तो यूपी से अधिक बड़े पैमाने पर मुठभेड़ कर्नाटक में भी की जाएगी। ऐसी बड़ी कानूनी कार्रवाई वाले उत्तरप्रदेश में धार्मिक नाम वाले प्रयागराज में अगर नामी-गिरामी स्कूलों के बच्चे ऐसे औपचारिक गिरोह बनाकर एक-दूसरे पर सार्वजनिक हमलों का काम कर रहे हैं, तो यह बहुत भयानक नौबत है, यह उत्तरप्रदेश की ताजा समस्या तो है ही, यह बाकी हिन्दुस्तान के लिए भी खतरे की एक घंटी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली हिंसक वेब सिरीज और हिंसक वीडियो गेम्स का असर अगर इस तरह सिर चढक़र बोल रहा है, तो सरकार और समाज दोनों को इसके बारे में सोचना चाहिए। इस ताजा मामले को एक स्थानीय घटना मानने के बजाय नई पीढ़ी पर मंडराते एक व्यापक खतरे की तरह देखना बेहतर होगा, और बाकी जगहों पर ऐसी नौबत आए उसके पहले सबको सम्हल जाना होगा।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
कर्नाटक में आज किसी हिन्दू की, तो चार दिन बाद किसी मुस्लिम का कत्ल चल रहा है। और जाहिर तौर पर ये मामले साम्प्रदायिक हत्या के दिख रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि ये जवाबी हत्याएं हैं। पहले किसी एक सम्प्रदाय के लोगों ने या संगठन ने दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को मारा, तो बाद में दूसरों ने उसका जवाब दे दिया। लोगों को याद होगा कि बीच-बीच में केरल में भी आरएसएस और सीपीएम के लोगों के बीच इस तरह की जवाबी हिंसा चलती रहती है। कर्नाटक में दिक्कत यह है कि वहां भाजपा के एक कार्यकर्ता के कत्ल के बाद लोग अब मुख्यमंत्री से यूपी के योगी-मॉडल की मांग कर रहे हैं। योगी मॉडल कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, यह पुलिस और बुलडोजर की मदद से अल्पसंख्यक तबके के खिलाफ आतंक का एक माहौल बनाने का राजनीतिक मॉडल है, जिसके तहत मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक करार दिया जाता है। अब अगर भाजपा और संघ परिवार के लोग कर्नाटक में भाजपा सरकार रहने के बाद उनके कार्यकर्ता के कत्ल पर योगी मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो एक बरस पहले मुख्यमंत्री बने बासवराज बोम्मई पर एक दबाव पडऩा तो तय है ही। इस दबाव के चलते वे वहां पर पुलिस को और अधिक साम्प्रदायिक नजरिये से काम करने कहेंगे, या योगी के कुछ और असंवैधानिक तौर-तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, यह पता नहीं। लेकिन धर्मान्धता और कट्टरता लोगों को गैरकानूनी हिंसा की तरफ धकेलने का काम करती हैं, और कर्नाटक आज उस खतरे की कगार पर दिख रहा है।
लेकिन इसे कर्नाटक की इस ताजा हिंसा के हमलों से परे भी देखें, तो यह देश के लिए एक अलग फिक्र की बात है। जब सडक़ों पर पूजा या नमाज को लेकर जगह-जगह तनातनी चल रही है, जब मस्जिद के लाउडस्पीकर का जवाब देने के लिए उनके सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, जब पूरे देश की हवा में साम्प्रदायिक जहर घोला जा रहा है, तो कोई कब तक महफूज रहेंगे, यह एक पहेली है। आने वाली पीढ़ी को लोग कितनी हिफाजत या कितने खतरे में छोडक़र जाएंगे, यह तो बहुत दूर की बात है, आज की बात यह है कि साम्प्रदायिक तनाव बढ़ते-बढ़ते अब जगह-जगह कत्ल करवा रहा है। आज केन्द्र सरकार और बहुत से प्रदेशों की सरकारें ऐसे फैसले ले रही हैं कि जिनसे मुस्लिम अल्पसंख्यक अपने को खतरे में महसूस करें, उपेक्षित पाएं, और फिर उनके बीच के कुछ नौजवान कानून पर भरोसा छोड़ दें। पूरा देश इस बात को देख रहा है कि किस तरह किसी भाषण या ट्वीट को लेकर मुस्लिम नौजवान छात्र नेताओं को बरसों तक बिना जमानत जेल में डालकर रखा जा रहा है, और जैसा कि हमने कुछ दिन पहले लिखा था, और उसके कुछ दिनों के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा लगता है कि इस देश में प्रक्रिया को ही सजा बना दिया गया है। अब अगर किसी समुदाय के लोगों को यह लगने लगेगा कि कानून की प्रक्रिया ही उनके खिलाफ सजा की तरह इस्तेमाल की जा रही है, तो उनका भरोसा ऐसे कानून और ऐसे लोकतंत्र पर से उठ जाने में कोई हैरानी नहीं होगी। आज जिन लोगों को यह लगता है कि बहुसंख्यक आबादी के वोटों को अल्पसंख्यक आबादी के वोटों के खिलाफ एक धार्मिक-जनमत संग्रह सरीखे चुनाव में खड़े करके इस देश और प्रदेशों पर अंतहीन राज किया जा सकता है, उन लोगों को ऐसी नौबत के खतरों का या तो अंदाज नहीं है, या वे खुद अपने परिवार को महफूज रखने की ताकत रखते हैं। अगर इस देश में दो समुदायों के बीच हिंसक नफरत को आसमान तक ले जाया जाएगा तो कौन सुरक्षित रह जाएंगे? आज जिस तरह किसी एक समुदाय के दो या चार लोग मिलकर दूसरे समुदाय के किसी एक को मार डाल रहे हैं, वैसी गिनती पूरे हिन्दुस्तान में हर दिन लाखों जगहों पर आ सकती है। लाखों ऐसे मौके हर दिन रहते हैं जब किसी एक समुदाय के चार लोगों के बीच दूसरे समुदाय का कोई एक घिरा हुआ रहे। अगर नफरत के हिंसा बढ़ती चली गई, तो हिन्दू और मुस्लिमों के बीच किसी टकराव को रोकने के लिए पूरे देश की पुलिस और तमाम फौज भी मिलकर कम पड़ेंगी। इन दोनों समुदायों के तमाम लोगों को पूरी हिफाजत दे पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। देश के लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा बना रहेगा, तो ही वे खतरे से बाहर रहेंगे। आज जिस तरह धर्म को लोकतंत्र से बहुत-बहुत ऊपर रखा जा रहा है, और लोगों की धार्मिक भावनाएं पल-पल आहत हो रही हैं, किसी की भी लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय भावनाएं कभी भी आहत नहीं हो रही हैं, यह एक बहुत ही खतरनाक नौबत है।
इस देश के धर्मान्ध और साम्प्रदायिक लोगों को यह बात समझ लेना चाहिए कि उनकी संपन्नता और ताकत की वजह से आज हो सकता है कि उनके परिवार महंगी कारों में बैठकर दूर निकल जाते हों, लेकिन जिस दिन किसी एक समुदाय के लोग हिसाब चुकता करने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों को ठिकाने लगाने लगेंगे, वैसे राज्यों में पुलिस और सरकार के पास सिर्फ ऐसे कत्ल की जांच, और उससे उपजे तनाव को काबू में करने का काम ही रह जाएगा। आज जिस तरह एक-एक कत्ल पूरे-पूरे राज्य को तनाव में डाल रहा है, कहीं कफ्र्यू लगता है, कहीं शहर बंद होता है, जिंदगी और कारोबारी कामकाज ठप्प हो जाते हैं, पढ़ाई-लिखाई बंद हो जाती है, यह सब कुछ देश की बर्बादी का सिलसिला है। लोगों को याद होगा कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, और देश के मुस्लिमों को लगा था कि कानून का राज उनके हक बचा नहीं पा रहा है, तब मुम्बई में आतंकी बम धमाके हुए थे, और सैकड़ों लोग मारे गए थे। इन धमाकों की तोहमत जिन पर है, वैसे दाऊद सरीखे कुछ लोग पाकिस्तान या कहीं और जा बसे हैं, लेकिन उन दंगों में हुए नुकसान की कोई भरपाई तो हो नहीं पाई। इसलिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक तबकों के बीच खाई खोदने के लिए भी, चुनाव जीतने के लिए भी अगर साम्प्रदायिक तनाव की आग को हवा दी जाती है, तो वह आग जंगल की आग की तरह बेकाबू भी हो सकती है, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर सकती है। साम्प्रदायिक नफरत चुनाव तो प्रभावित करती है, लेकिन उससे उपजी हिंसा कारोबार को भी प्रभावित करती है, देश के विकास को भी प्रभावित करती है। कर्नाटक ने पिछले बरसों में लगातार साम्प्रदायिकता देखी है, और देश का यह एक सबसे विकसित राज्य अपनी संभावनाओं से काफी पीछे हो गया होगा। जिन लोगों को साम्प्रदायिक हिंसा से आर्थिक गिरावट का रिश्ता समझ नहीं आता है, उन्हें अपने देश-प्रदेश की संभावनाओं का कोई अंदाज नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस देश में 140 करोड़ आबादी में से अगर 20 करोड़ मुस्लिम हैं, तो हिन्दू और मुस्लिम आबादी के एक-एक फीसदी लोगों के भी साम्प्रदायिक-कातिल हो जाने का खतरा इस मुल्क को तबाह कर सकता है। आज सरकारें हांक रहे कई लोग इस खतरे की कीमत पर भी धार्मिक ध्रुवीकरण करके सत्ता पर निरंतरता चाहते हैं, लेकिन वह किसी श्मशान की चौकीदारी की निरंतरता सरीखी रहेगी।
और इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि जब धर्म के नाम पर कत्ल करने की आदत पड़ जाती है, तो उसके लिए दूसरे धर्म के किसी को मुर्दा बनाना जरूरी नहीं रहता, अभी उत्तराखंड में कांवड़ लेकर जा रहे एक फौजी से बहस होने पर दूसरे कावडिय़ों के एक जत्थे ने उसे लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
ब्रिटेन में इन दिनों अगले प्रधानमंत्री के लिए कंजरवेटिव पार्टी के दो सांसदों के बीच मुकाबला चल रहा है। और इस मुकाबले को देखना हिन्दुस्तान के लोगों के लिए किसी किस्से कहानी सरीखा हो सकता है क्योंकि एक ही पार्टी के दो सांसदों के बीच सार्वजनिक रूप से जैसी बहस चल रही है, उसी पार्टी के सांसदों के बीच कई सांसदों को वोट देकर फिर अधिक वोट पाने वाले लोगों के बीच चुनकर जिस तरह दो आखिरी उम्मीदवार छांटे गए हैं, वह भी देखना दिलचस्प है। खासकर हिन्दुस्तान जैसे चुनावी लोकतंत्र में जहां पर कि किसी भी पार्टी में ऐसे किसी लोकतंत्र की उम्मीद की नहीं जा सकती। आज के ये दोनों ही उम्मीदवार, ऋषि सुनक और लिज ट्रस मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल में शामिल थे, और जब बोरिस जॉनसन को बहुत मजबूरी में हटना ही पड़ा, तो अब ये दोनों अगले कुछ हफ्तों में पार्टी के रजिस्टर्ड वोटरों के बीच मतदान से अगला प्रधानमंत्री तय करवाएंगे। दूसरी तरफ इससे कुछ दूर हटकर देखें तो अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव के पहले दोनों बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार बनने के लिए उन पार्टियों के लोगों के बीच दावेदारी सामने आती है, वे दावेदार देश भर में घूमकर अपनी पार्टी के लोगों के बीच अपनी काबिलीयत के बारे में बताते हैं, और इस तरह देश भर से पहले तो पार्टियां ही अपने अधिकृत उम्मीदवार तय करती हैं, और फिर देश भर के वोटर उनमें से किसी को अगला राष्ट्रपति चुनते हैं। मतलब यह कि पार्टी के भीतर भी देश के सबसे बड़े पद के लिए उम्मीदवार बनने के लिए लोगों को बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, और इन दोनों ही मॉडल्स में पूरी पार्टी की भागीदारी हो जाती है।
अब अगर इस तरह की कोई कल्पना हिन्दुस्तान के बारे में की जाए, तो यहां ऐसा कोई लोकतंत्र मुमकिन नहीं दिखता। पहले तो पार्टी के पदाधिकारियों का चुनाव भी किसी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता, और अधिकतर पार्टियों में एक परिवार के भीतर निपटारा हो जाता है, और भाजपा जैसी पार्टी में कहा जाता है कि संघ परिवार के भीतर निपटारा हो जाता है। हिन्दुस्तान में न तो प्रधानमंत्री, न ही मुख्यमंत्री, और न ही किसी और ओहदे के लिए कोई भी चुनाव होता है। पार्टी के संसदीय दल, या विधायक दल के नेता भी शायद ही कहीं बहुमत से चुने जाते हैं, और पार्टी हांकने वाले लोग बंद कमरों से संगठन और सरकार दोनों का भविष्य तय कर लेते हैं कि किस कुर्सी पर किसे बिठाना है। इसलिए जब कभी संगठन या सरकार की किसी कुर्सी के लिए चुनाव के बारे में सोचना हो, तो ब्रिटेन और अमरीका सरीखे मॉडल पर सोच लेना चाहिए। ये दोनों ही देश बाकी दुनिया के लिए चाहे कितने ही अलोकतांत्रिक क्यों न हों, कितने ही हमलावर क्यों न हों, ये दोनों ही अपने घर के भीतर लोकतांत्रिक सिलसिले को जिंदा रखे हुए हैं।
हिन्दुस्तान ने वैसे तो अधिकतर कुनबापरस्त पार्टियां ही देखी हैं, कांग्रेस से शुरू करके शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, राष्ट्रीय जनता दल, अकाली दल, चौटाला-कुनबा, नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जैसी अनगिनत पार्टियां हैं जिनमें सबसे बड़े फैसले भी परिवार नाश्ते की टेबिल पर ले सकता है, या रात के खाने पर। इनमें किसी संगठन की कोई भूमिका नहीं है। और जब भाजपा की भी बात आती है, तो उसमें भी नीचे से लेकर ऊपर तक किसी भी ओहदे के लिए लोगों का मनोनयन होता है, किसी तरह के चुनाव नहीं होते। अब यह मनोनयन आरएसएस करता है, या हाल के बरसों में नरेन्द्र मोदी और अमित शाह करते हैं, यह तो अंदर की बात है, लेकिन बाहर दिखावे के लिए भी किसी तरह का चुनाव नहीं होता है। अब इस नौबत की पूरी की पूरी तोहमत कांग्रेस की कुनबापरस्ती पर डालना ठीक होगा या नहीं, यह तो पता नहीं। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते, और इस पर एक ही कुनबे का प्रत्यक्ष और परोक्ष कब्जा होने की वजह से भारतीय राजनीति में परिवारवाद के लिए तोहमत तो इसे ही झेलनी पड़ेगी। आज भाजपा मोटेतौर पर लीडर के स्तर पर वंशवाद से मुक्त दिखती है, लेकिन वह आंतरिक लोकतंत्र से कोसों दूर भी है। उसके भीतर के तमाम बड़े फैसले रहस्यमय तरीके से अपने को राजनीति से दूर करार देने वाला एक सांस्कृतिक संगठन लेता है, या अब बदले हुए हालात में मोदी और शाह लेते हैं। और एक-दूसरे पर तोहमत लगाने की जरूरत को अगर छोड़ दें, तो तमाम कुनबापरस्त पार्टियां अपने भीतर मगनमस्त हैं। इनमें से किसी भी पार्टी के भीतर कुनबापरस्ती के खिलाफ कोई बेचैनी नहीं दिखती है, कोई आवाज नहीं उठती है। और तो और एक-दो मिसालें तो भारतीय राजनीति में ऐसी भी हैं कि कुनबे से परे भी नेता ने अपनी प्रेमिका को पार्टी का मुखिया बना दिया, और न सिर्फ संगठन ने, बल्कि जनता ने भी उसे मंजूर कर लिया।
जिन लोगों को घूमने-फिरने का शौक रहता है लेकिन दुनिया भर में जाने की सहूलियत नहीं रहती, वे लोग टीवी के कुछ चैनलों पर अलग-अलग देशों के सैर-सपाटे की डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं, और तसल्ली कर लेते हैं। उसी तरह जब हिन्दुस्तानियों को लोकतंत्र के बारे में कुछ अच्छा पढऩे की जरूरत लगे, लोकतंत्र के बारे में कुछ अच्छा महसूस करने की जरूरत लगे, तो उन्हें ब्रिटेन और अमरीका के ऐसे लोकतांत्रिक मॉडल के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए, और यह मान लेना चाहिए कि हिन्दुस्तान में न सही, दुनिया में और कहीं इस तरह का जिंदा लोकतंत्र कायम तो है। दुष्यंत कुमार ने एक वक्त लिखा था- हो कहीं भी आग लेकिन, आग जलनी चाहिए...। इसी के मुताबिक लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आजाद मीडिया, लोकतांत्रिक पार्टियां, लोकतांत्रिक चुनाव, लोकतांत्रिक मूल्यों की अपनी हसरत पूरी करने के लिए दुनिया के बेहतर लोकतंत्रों की तरफ देखना चाहिए, और उनकी कामयाबी पर खुश हो लेना चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
दुनिया में कैथोलिक ईसाई लोगों के सबसे बड़े धर्मगुरू पोप अभी कनाडा पहुंचे। और जैसा कि पहले से तय था उन्होंने वहां के मूल निवासियों से इस बात के लिए माफी मांगी कि पिछली डेढ़ सदी में कैथोलिक चर्च और उसकी चलाई स्कूलों ने डेढ़ लाख के करीब आदिवासी बच्चों को उनके परिवार से दूर करके उन्हें ‘शहरी, शिक्षित, और सभ्य’ बनाने के लिए उन्हें अपनी स्कूलों में बंधुआ सा रखा। कनाडा के इतिहास में 1870 से 1996 के बीच मूल निवासियों के बच्चों को जबर्दस्ती उनके घरों से ले जाकर इस तरह उनका ‘विकास’ किया जाता था। और एक जांच रिपोर्ट बताती है कि इनमें से तीन हजार बच्चे इन स्कूलों में मर भी गए, जिन्हें इस जांच रिपोर्ट ने मूल निवासियों का सांस्कृतिक-जनसंहार करार दिया था। पोप फ्रांसीस ने आदिवासी समुदाय से ऐसी ही एक आवासीय-स्कूल की जमीन पर आमंत्रित आदिवासियों से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें चर्च के लोगों के इस किए हुए का बहुत दुख है, और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। यहां पर आदिवासी समुदायों के ऐसे लोग मौजूद थे जो कि चर्च की आवासीय-स्कूलों में कैद करके रखे गए थे, और जो आज भी जिंदा हैं। उन लोगों ने पोप की माफी पर तसल्ली जाहिर की, इनमें से कई लोग इस मौके के लिए दूर-दूर से पहुंचे थे। पोप ने कैथोलिक चर्च की तरफ से दुख और शर्मिंदगी का इजहार किया, और कहा कि वह स्कूल प्रथा भयानक गलती थी, और आदिवासियों के खिलाफ बहुत से ईसाई लोगों द्वारा की गई दुष्टता के लिए उन्होंने माफी मांगी। वहां पहुंचे मूल निवासियों में कई लोगों का कहना था कि यह माफी नाकाफी है, और पोप को इससे अधिक कुछ कहना चाहिए।
दुनिया में सभ्यता वही होती है कि लोग अपनी गलतियों, और खासकर अपने किए गलत कामों पर अफसोस जाहिर करना सीखें, और माफी मांगना सीखें। दुनिया का इतिहास ऐसी सभ्य संस्कृतियों से भरा हुआ है। लोगों को याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी शहरी, गोरे, ईसाई लोगों ने वहां के मूल निवासियों के साथ ऐसा ही किया था, और उनके बच्चों को सभ्य बनाने के नाम पर गांव-परिवार से दूर करके शहरी, ईसाई, आवासीय-स्कूलों में उन्हें रखा था जिससे कि वे अपनी संस्कृति से कट गए थे। सदियों के ऐसे शोषण के बाद अभी कुछ बरस पहले ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इन समुदायों के प्रतिनिधियों को सदन के भीतर आमंत्रित किया, और फिर पूरी संसद ने खड़े होकर इनसे समाज की की हुई ज्यादती के लिए माफी मांगी थी। ऑस्ट्रेलिया में इसे स्टोलन जनरेशन कहा जाता था, यानी मूल निवासियों से चुराई गई (उनके बच्चों की) पीढ़ी। दुनिया के इतिहास में ऐसा कई देशों के साथ भी हुआ है जिन पर ज्यादती करने वाले दूसरे देशों ने उनसे माफी मांगी है। लेकिन ऐसी शर्मिंदगी जाहिर करने के लिए, और माफी मांगने के लिए लोगों का सभ्य होना जरूरी होता है।
हिन्दुस्तान के इतिहास को देखें, तो अंग्रेजों ने तो अपने जलियांवाला बाग जैसे जुल्म और जुर्म के लिए भी माफी नहीं मांगी थी, और नतीजा यह हुआ था कि एक हिन्दुस्तानी क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन जाकर जलियांवाला बाग के अंग्रेज खलनायक जनरल डायर को सार्वजनिक रूप से गोली मार दी थी। हिन्दुस्तान के भीतर जो ताकतें, और जो संगठन गांधी की हत्या के पीछे थे, उसके लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने कभी भी उस जुर्म के लिए माफी नहीं मांगी। बल्कि अब तो ये संगठन गोडसे से लेकर सावरकर तक के महिमामंडन में लगे हुए हैं, और उसके लिए भी गांधी स्मृति के प्रकाशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में ऐसे और भी जो-जो ऐतिहासिक जुर्म हुए हैं, उनके लिए माफी मांगने का कोई इतिहास नहीं रहा है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, और उनके बेटे संजय गांधी की असंवैधानिक सत्ता देश को कुचल रही थी। लेकिन आपातकाल की ज्यादतियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कोई सार्वजनिक माफी मांगी हो ऐसा याद नहीं पड़ता। बल्कि इन शब्दों से इंटरनेट पर ढूंढने पर 2015 का कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का यह बयान सामने आता है कि आपातकाल के लिए कांग्रेस को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उनका तर्क है कि इसके बाद लोगों ने इंदिरा गांधी को फिर प्रधानमंत्री चुन लिया था, और अगर हम (कांग्रेस) इसके लिए माफी मांगते हैं, तो देश की जनता को भी माफी मांगनी पड़ेगी कि उसने इसके बाद भी इंदिरा गांधी को क्यों चुना। कांग्रेस के एक बड़े नेता, जो कि एक वकील भी हैं, उन्होंने एक लंबे-चौड़े बयान में कई तरह से इस बात की वकालत की थी कि कांग्रेस को इमरजेंसी पर माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।
माफी तो इंदिरा गांधी के कत्ल के लिए सिक्ख पंथ के उस वक्त के उग्रवादियों की तरफ से भी किसी ने नहीं मांगी थी, बल्कि उसे जीत के जश्न की तरह मनाया गया था। इसके पहले जब स्वर्ण मंदिर से हथियारबंद आतंकियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, तो एक धर्मस्थान पर घुसने के लिए केन्द्र सरकार और कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की गई थी। अनगिनत हत्याएं करके भाग-भागकर स्वर्ण मंदिर में रहने वाले भिंडरावाले के आतंकियों को हटाने के लिए उस वक्त जो कार्रवाई सरकार को मुनासिब लगी थी, उसने की थी, और भिंडरावाले के हत्यारे-आतंक पर चुप रहने वाले सिक्ख नेताओं ने स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई के खिलाफ जुबानी हमला बोल दिया था, और नतीजा इंदिरा गांधी की हत्या तक पहुंचा था। इसके तुरंत बाद देश भर में सिक्ख विरोधी दंगे हुए थे, और यह बात आज तक जारी है कि कांग्रेस ने उस पर पर्याप्त माफी मांगी है या नहीं। जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिक्ख विरोधी दंगों के लिए देश से माफी मांगी थी, जिसे बाद में लीक हुए एक अमरीकी कूटनीतिक संदेश में कहा गया था कि बीस बरस में किसी भारतीय नेता ने ऐसा करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई थी।
हिन्दुस्तान में ऐतिहासिक जुल्म और ज्यादती के और भी मामले हैं, 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, और गिराने वालों ने सामने मंच पर खड़े होकर, माईक से फतवे जारी करके यह काम किया, इसके ठीक पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने मैदान को समतल कर देने जैसी कोई बात सार्वजनिक रूप से कही थी, अडवानी ने इसके पहले रथयात्रा निकाली थी जिसमें उनके साथ आज के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मौजूद थे। लेकिन बाबरी मस्जिद गिराने के लिए किसी ने माफी नहीं मांगी, जिसके बाद कि देश भर में हुए दंगों और आतंकी हमलों में सैकड़ों मौतें हुई थीं। 2002 में गुजरात में हिन्दुओं से भरे रेल डिब्बे जला दिए गए, और उसके बाद मानो इसके जवाब में हिन्दू उग्रवादियों ने छांट-छांटकर हजारों मुस्लिमों को तीन दिनों तक मारा, और मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार दूसरी तरफ मुंह मोड़े बैठी रही। अपनी सरकार के चलते राजधर्म की ऐसी अनदेखी पर मोदी ने कभी माफी नहीं मांगी। बल्कि आज जो संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति पद प्रत्याशी थे, उन यशवंत सिन्हा के नाम के साथ गुजरात दंगे टाईप करके देखें तो पहली हैडिंग 2014 की दिखाई पड़ती है जिसमें यशवंत सिन्हा का बयान है कि गुजरात दंगों के लिए माफी न मांगकर मोदी ने सही किया। आज जरूर यशवंत सिन्हा की हार पर देश के बहुत से लोगों को अफसोस हो रहा है जो कि भाजपा की उम्मीदवार को हराना चाहते थे, लेकिन 2014 में जब यशवंत सिन्हा भाजपा के नेता थे, वे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेन्द्र मोदी के बारे में दमखम से यह बात कह रहे थे, और उन्होंने यह भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर जरा भी विचलित नहीं है कि 2002 में गुजरात में क्या हुआ था, ठीक उसी तरह जिस तरह कि वे भूल गए हैं कि 1984 में सिक्खों के साथ क्या हुआ था।
माफी मांगने के लिए लोगों में लोकतांत्रिक समझ होना जरूरी है, दूसरे लोगों के हक और अपनी जिम्मेदारी की बुनियादी समझ होना जरूरी है। आज भी इस हिन्दुस्तान में संघ परिवार के संगठन उत्तर-पूर्वी राज्यों से आदिवासी परिवारों की बच्चियों को लाकर देश भर में जगह-जगह बनाए गए शबरी आश्रमों में रख रहे हैं, और उनकी संस्कृति, उनके धर्म से उन्हें परे ले जाकर उनका शहरी, हिन्दूकरण कर रहे हैं। यह ठीक उसी तरह का काम है जिसके लिए सैकड़ों बरस बाद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में वहां की संसद, सरकार, और ईसाई धर्मप्रमुख माफी मांग रहे हैं, शर्मिंदगी जाहिर कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में तो बस्तर जैसे आदिवासी इलाकों में आदिवासियों के साथ क्या तो भाजपा सरकार, और क्या तो कांग्रेस सरकार, सबके राज में जिस तरह के जुल्म हो रहे हैं, उसके लिए आदिवासियों से माफी मांगने की सभ्यता इस देश में जाने कब विकसित हो सकेगी। कई मामलों में हिन्दुस्तान पश्चिम से सैकड़ों बरस पीछे चलता है, और 22वीं या 23वीं सदी में हिन्दुस्तान की संसद और सरकार शायद आदिवासियों से माफी मांगने जितनी सभ्य हो सकेंगी।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
आज की दुनिया इन्फर्मेशन ओवरलोड की शिकार है। कोई इंसान एक दिन में जितना पढ़ सकते हैं, सुन या देख सकते हैं, उससे करोड़ों गुना अधिक उनके इर्द-गिर्द इंटरनेट पर तैर रहा है। अधिक सक्रिय और अधिक जुड़े हुए लोगों को वॉट्सऐप जैसे मैसेंजरों पर इतना अधिक आता है कि आम लोगों के लिए यह मुमकिन नहीं रहता कि उसे जांच-परख लें। यह एक और बात है कि अधिकतर लोगों के बीच ऐसे उत्साही इंसान जिंदा रहते हैं जो कि पूरी गैरजिम्मेदारी के साथ चीजों को आगे बढ़ाने को उतावले रहते हैं। नतीजा यह होता है कि लोग झूठी बातों को भी आगे बढ़ा देते हैं, और अक्सर ही यह जानते हुए भी आगे बढ़ा देते हैं कि वह झूठ है। लोगों को संपर्कों के अपने दायरे में यह दिखाने की भी एक हड़बड़ी रहती है कि उनके पास दिखाने को कुछ है। हर किसी को यह साबित करने की चाह रहती है कि उनका भेजा हुआ, या उनका पोस्ट किया हुआ भी लोग देखते हैं, और गैरजिम्मेदारी से उसे पसंद भी करते हैं।
अब अभी कल की ही बात है, योरप की एक बड़ी पर्यावरण आंदोलनकारी छात्रा ग्रेटा थनबर्ग के बारे में एक पोस्टर लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उसने जर्मन रेलगाडिय़ों को भीड़भरा बताया, और अपनी एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह एक डिब्बे में अपने सामान सहित फर्श पर बैठी हुई है। अभी पोस्ट की हुई जानकारी यह भी बताती है कि जर्मन रेलवे ने तुरंत ही यह पोस्ट किया कि ग्रेटा थनबर्ग का फस्र्ट क्लास के डिब्बे में रिजर्वेशन था, और उसके लिए फलां सीट नंबर तय था। इस बात को ग्रेट थनबर्ग के खिलाफ इस्तेमाल किया गया कि पर्यावरण बचाने के नाम पर वह झूठ फैलाती है। अच्छे-खासे, पढ़े-लिखे, विकसित देशों में बसे हुए लोगों ने भी इस पोस्टर का मजा लिया क्योंकि पर्यावरण बचाने की मुहिम छेड़े हुए इस लडक़ी ने दुनिया के बड़े-बड़े नेताओं का जीना हराम किया हुआ है, और अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप जैसे लोग इससे हलाकान थे। लेकिन जब इस पोस्टर की हकीकत ढूंढने की कोशिश की गई, तो दो बातें सामने आईं, एक तो यह कि यह करीब तीन बरस पुरानी बात है। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर जर्मन रेलवे ने यह जानकारी जरूर दी थी। लेकिन ग्रेटा-विरोधियों ने इसके बाद के हिस्से को छुपाकर यह पोस्टर बनाया जिसमें ग्रेटा थनबर्ग ने यह लिखा था कि उसका ट्रेन सफर तीन हिस्सों में था, और इसमें से एक हिस्सा उसने डिब्बे के फर्श पर गुजारा था। उसने यह भी साफ किया कि ट्रेनों को भीड़भरा बताना उसके लिए कोई नकारात्मक बात नहीं थी बल्कि उसने इसे पर्यावरण के लिए एक अच्छी बात की तरह पेश किया था क्योंकि ट्रेनें पर्यावरण का कम नुकसान करती हैं।
इस बात को महज एक घटना की तरह देखना ठीक नहीं है, इसे लोगों के रूझान की तरह देखना ठीक है कि जो लोग जिन्हें पसंद नहीं करते हैं, उनके खिलाफ वे चुनिंदा तथ्यों को लेकर एक झूठ को आगे बढ़ाते हैं, या सच की एक ऐसी शक्ल को सामने रखते हैं जो कि अधूरी रहती है, और एक अलग धारणा बनाती है। पिछले कुछ बरसों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें वे लोगों की उपेक्षा करते दिख रहे हैं। खासकर लालकृष्ण अडवानी के साथ मोदी की एक ऐसी तस्वीर है जिसमें अडवानी हाथ जोड़े हुए बहुत ही बुरी तरह दीन-हीन, गिड़गिड़ाते हुए से दिख रहे हैं, और मोदी सामने एक क्रूर अंदाज में खड़े हैं। यह तस्वीर अपने आपमें गढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन यह एक सेकेंड के भी एक छोटे हिस्से को दिखाती हुई तस्वीर थी, जिसके पहले और बाद के पल जब दूसरी तस्वीरों में सामने आए, तो दिखा कि मोदी उसके पहले या बाद में नमस्कार कर चुके थे। कुछ इसी तरह का एक वीडियो अभी दो दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें जाते हुए राष्ट्रपति उनके विदाई समारोह में एक कतार में खड़े हुए लोगों के सामने से नमस्कार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और वहां खड़े हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर कैमरों को देख रहे हैं, उस पल सामने से हाथ जोड़े हुए गुजरते हुए राष्ट्रपति को भी वे नहीं देख रहे हैं। बाद में इसके जवाब में भाजपा के लोगों ने एक दूसरा वीडियो पोस्ट किया जिसमें इन पलों के पहले के कुछ पल दिखते हैं, और उनमें मोदी राष्ट्रपति को नमस्कार कर चुके हैं, और राष्ट्रपति के सामने-सामने चलते हुए फोटोग्राफरों पर जब उनकी नजर टिकती है, तो फिर वहीं टिकी रह जाती है। अगर शुरू के इन पलों को न देखें, तो तस्वीर ऐसी बनती है कि मोदी ने राष्ट्रपति को देखा ही नहीं, और बस कैमरे देखते रह गए। यह एक अलग बात है कि कुछ पल राष्ट्रपति को देखने के बाद मोदी का ध्यान कैमरों की तरफ ही रह गया, लेकिन उन्होंने शुरू के कुछ पलों में राष्ट्रपति को नमस्ते तो कर लिया था।
आज का वक्त सूचनाओं के सैलाब का वक्त है, और साधारण समझबूझ के इंसानों के लिए यह आसान नहीं रहता कि वे इस सैलाब के बीच संभल पाएं। सुनामी सरीखे सैलाब से जूझते इंसान की तरह आज के लोगों के सामने दिक्कत यह रहती है कि उन्हें अपने संपर्कों के दायरे में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की एक हड़बड़ी रहती है, और उसका दबाव भी रहता है। जिस तरह लोग अपने साथ के लोगों को निराश करने के बजाय उनके साथ सिगरेट या दारू पीने लगते हैं, या जुआ खेलने लगते हैं, ठीक उसी तरह आज लोग अपने गैरजिम्मेदार दायरे की बराबरी करने के लिए उसी के दर्जे की गैरजिम्मेदारी दिखाने में लग जाते हैं। फिर सच को आधे या पूरे झूठ की तरह दिखाने के लिए कुछ गढऩे की जरूरत भी नहीं रहती, चीजों को बस आधा दिखाना, चीजों को गलत वक्त का दिखा देना भी काफी होता है। उमा भारती का एक पुराना वीडियो नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सबसे बुरी बातें कहते हुए इंटरनेट पर मौजूद है। उसे आज मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ मोदी के कहे हुए एक वीडियो को आज मजाक में इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि रूपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा रहता है। अब उमा भारती ने भाजपा से बाहर रहते हुए जो कुछ कहा था उसे आज भी इस्तेमाल करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन जिम्मेदार लोगों को यह समझने की जरूरत जरूर है कि कौन सी बात किस संदर्भ में कही गई थी।
संदर्भ से काटकर जब किसी बात को देखा जाता है, तो सरदार पटेल को नेहरू का विरोधी साबित किया जा सकता है, सरदार पटेल को आरएसएस का हिमायती साबित किया जा सकता है, गांधी, सुभाषचंद्र बोस, और भगत सिंह को संघ के मंच पर सजाया जा सकता है। आज आंखों से जो सच सा दिखता है, उसे भी परख लेने का वक्त है। और इंटरनेट की मेहरबानी से यह बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है। जो जानकारी आपके सामने आ रही है, उसके चुनिंदा शब्दों को इंटरनेट पर सर्च कर देखें, बड़ी संभावना रहेगी कि आप हकीकत की गहराई तक पहुंच जाएं। इससे एक दूसरा फायदा यह भी होगा कि आप झूठ फैलाने से बचेंगे। याद रखें कि आज के वक्त आपकी साख बस उतनी ही है जितनी कि आपकी फैलाई गई बातों की है। इसलिए बदनीयत झूठों की भीड़ के दबाव में आकर उनकी बराबरी करने न उतरें, सच पर बने रहें।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)