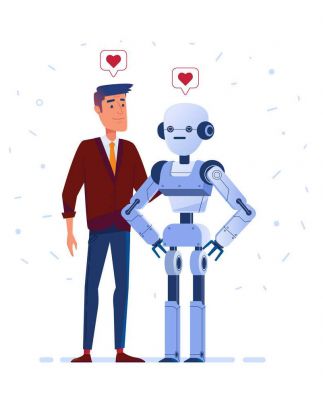संपादकीय
राजस्थान में एक हिन्दू दर्जी की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जिस तरह दो मुस्लिमों ने गला काटकर हत्या की है, और उसे मोहम्मद पैगंबर का कथित अपमान करने वाली नुपूर शर्मा के समर्थन के खिलाफ किया गया बताया है, उससे चारों तरफ खलबली मची हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर इतनी हिंसक कार्रवाई शायद पहली बार हुई है, और शायद पहली बार ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम लेकर धमकी देते हुए इस तरह वीडियो जारी हुआ है। लेकिन इन तमाम बातों पर हम कल लिख चुके हैं, और आज इससे जुड़े हुए एक पहलू पर लिखने की वजह केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के एक बयान से आई है, जिन्होंने यह सवाल उठाया है कि मदरसों में छोटे बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि ईशनिंदा (अल्लाह की निंदा), की सजा सिर काटना है। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम कानून कुरान से नहीं आता है, वह बाद के राजाओं के समय इँसानों का लिखा हुआ जो सिर काटने की सजा लिखता है। आरिफ मोहम्मद खान ने इस पर अफसोस जाहिर किया कि यह कानून बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पांच-छह बरस की उम्र से ही ऐसा कानून मदरसों में पढ़ाया जाता है, और अगर बच्चे उससे प्रभावित होते हैं, और उसके मुताबिक काम करते हैं, तो फिर वे अपने धर्म की रक्षा के नाम पर कोई भी काम करने को तैयार हो सकते हैं। उन्होंने यह राय भी जाहिर की कि चौदह बरस की उम्र तक बच्चों को सामान्य शिक्षा ही देनी चाहिए, और यह उनका मौलिक अधिकार भी है। उन्होंने कहा कि इस उम्र के पहले उन्हें कोई विशेष शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी फिर से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुरान ऐसी सजा नहीं सुझाता, यह बाद के लोगों ने लिखा है।
आज देश राजस्थान के इस ताजा धार्मिक हमले को लेकर विचलित है, इसलिए ऐसे हमलावरों की सोच के हर पहलू पर चर्चा हो रही है। आरिफ मोहम्मद खान भाजपा के बनाए हुए राज्यपाल हैं, और उनका नाम अभी कुछ दिन पहले तक राष्ट्रपति पद के संभावित एनडीए उम्मीदवार के लिए भी खबरों की अटकलों में था। लेकिन भाजपा से उनके संबंधों की वजह से उनकी बात का वजन कम नहीं होता। मदरसों के खिलाफ हिन्दूवादी ताकतों की सोच के पीछे उनकी बदनीयत हो सकती है, लेकिन एक जाहिर सा दूसरा सवाल यह भी है कि क्या आज के जमाने में गरीब मुस्लिम बच्चों को बचपन से ही मदरसों में धर्म की शिक्षा देना, और उन्हें सामान्य औपचारिक स्कूली शिक्षा से दूर रखना कोई जायज बात है? ईसाई स्कूलों में भी बच्चों को धार्मिक पाठ पढ़ाए जाते हैं, या उनसे धार्मिक प्रार्थना करवाई जाती है। कुछ दूसरे अल्पसंख्यक धर्मों के स्कूलों में भी ऐसा होता होगा क्योंकि उनका दर्जा ही धार्मिक अल्पसंख्यक आधार पर बने हुए शैक्षणिक संस्थान है। ऐसे किसी भी स्कूल-कॉलेज में अगर बच्चों को आज की बाकी औपचारिक शिक्षा से परे सिर्फ धर्म पढ़ाया जाएगा, तो वह उन बच्चों की जिंदगी खराब करने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। मुस्लिम मदरसों को धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक होने के नाते मर्जी का पाठ्यक्रम पढ़ाने की छूट मिली भी हो, तो भी उस तबके के गरीब बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह सोचना होगा कि क्या उन्हें सिर्फ इसी तरह की शिक्षा देना जायज है?
भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर धर्मनिरपेक्ष ताकतें लगातार सक्रिय रहती हैं। इनमें ऐसे राजनीतिक दल भी रहे जिन्होंने शाहबानो के वक्त एक अकेली मुस्लिम महिला के हकों के खिलाफ अड़े हुए मुस्लिम दकियानूसी मर्दों के वोटर-बाहुबल के सामने समर्पण कर दिया था, और संसद में नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। फिर धार्मिक आधार पर ही इस तबके को कई तरह की छूट देने का सिलसिला भी चले आ रहा था जिसकी कुछ बातों को केन्द्र की मोदी सरकार ने बदला है। इसमें मुस्लिम महिला के अधिकार बढ़ाने के लिए तीन तलाक के खिलाफ बनाया गया कानून है। मोदी सरकार की दूसरी कई नीतियों के चलते हुए तीन तलाक के कानून को भी मुस्लिम विरोधी करार दिया गया जबकि इससे मुस्लिम महिला के अधिकार बढ़ रहे थे, और मुस्लिम पुरूष के अधिकार कम हो रहे थे। देश की धर्मनिरपेक्ष ताकतें मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का साथ देते हुए मुस्लिम महिला के अधिकारों को अलग से देखने से कई बार कतराती भी हैं, क्योंकि वह इसे मुस्लिम समाज के भीतर का मुद्दा मानती हैं। अब हिन्दू समाज में भी बाल विवाह से लेकर सतीप्रथा तक बहुत सी बातें समाज के भीतर की थीं, लेकिन समाज के भीतर का कोई सुधार इन बातों को खत्म नहीं कर पा रहा था, और आखिर में देश की सरकार को कानून बनाकर ही हिन्दू समाज की इन रूढिय़ों को खत्म करना पड़ा था। तमाम कानून के बावजूद आज भी बाल विवाह बड़े पैमाने पर चल रहा है, और कानून भी उसे नहीं रोक पा रहा है। ऐसे में मदरसों को लेकर अगर उनमें धर्म शिक्षा से परे औपचारिक शिक्षा की बात होती है, तो उसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल नहीं मानना चाहिए। ऐसे मदरसे दुनिया में एक ऐसी पीढ़ी ला रहे हैं जो कि धार्मिक व्यवस्था पर परजीवी की तरह टिकी रहेगी, और आधुनिक दुनिया में अधिक आगे बढऩे के लायक नहीं बनेगी। किसी तबके को धार्मिक अल्पसंख्यक आधार पर शिक्षा के ऐसे धार्मिक अधिकार को देने का एक मतलब यह भी है कि उस धर्म की एक पीढ़ी के बहुत से लोगों को हमेशा के लिए पिछड़ा बना देना। यह सिलसिला उस समुदाय के साथ भी बेइंसाफी है, और बच्चों की उस पीढ़ी के साथ तो बेइंसाफी है ही जो कि अपना फैसला खुद नहीं ले पाती।
चाहे स्कूल-कॉलेज हो, चाहे किसी दूसरे धर्म से जुड़े हुए ऐसे तथाकथित सांस्कृतिक संगठन हों जो कि धार्मिक आधार पर बच्चों के दिमाग में जहर भरते हैं, कट्टरता भरते हैं, उन सब पर रोक लगानी चाहिए। आज देश में कई तरह की धार्मिक कट्टरता एक-दूसरे की प्रतिक्रिया में बढ़ती चली जा रही हैं, इस पर रोक लगाने के लिए भी पढ़ाई-लिखाई में से धर्म की भूमिका कम करने की जरूरत है। और सिर्फ धार्मिक पढ़ाई तो एक पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद कर देने के अलावा कुछ नहीं है, और ऐसे लोग अपने धार्मिक स्थानों पर दान पर पलने वाले लोग बनकर रह जाते हैं, जिन्हें किसी धार्मिक फतवे से किसी हिंसा में झोंक देना आसान रहता है। इसलिए देश के तमाम शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक शिक्षा से अलग करने की जरूरत है, और जब व्यापक स्तर पर ऐसा किया जाएगा तो समझ आएगा कि इससे सिर्फ मदरसे प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि दूसरी धर्मों के शैक्षणिक संस्थान भी प्रभावित होंगे, उनकी पढ़ाई की किताबें भी प्रभावित होंगी। फिलहाल तो राजस्थान की इस ताजा हिंसा को देखते हुए इस बात की जांच की जरूरत है कि क्या मदरसों में ईशनिंदा पर गला काटने की सजा सिखाई जा रही है?
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
राजस्थान के उदयपुर में कल ऐसी धार्मिक-आतंकी वारदात हुई है कि जिसने हिन्दुस्तान को तालिबान के मुकाबले ला खड़ा किया है। वहां के एक हिन्दू दर्जी के सोशल मीडिया पेज पर शायद उसके आठ बरस के बेटे ने नुपूर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट की थी। एक टीवी बहस पर नुपूर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थीं, जिसकी प्रतिक्रिया में हिन्दुस्तान के मुसलमानों से लेकर मुस्लिम देशों तक ने विरोध दर्ज किया था, और कई देशों के विरोध के बाद भारत में भाजपा ने अपनी इस राष्ट्रीय प्रवक्ता को पद से हटाया था, और सरकार ने उसके खिलाफ जुर्म दर्ज किए थे। तब से अब तक नुपूर शर्मा गिरफ्त से बाहर है। देश में धर्मान्ध हिन्दुओं का एक तबका पूरी ताकत से नुपूर शर्मा के साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ मुस्लिम इस बात से आहत हैं कि उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऐसे माहौल के बीच सोशल मीडिया उबला पड़ा है, और साम्प्रदायिकता मानो इस देश का मुख्य खानपान हो गई है, और लोगों के पास मानो नफरत को फैलाना ही अकेला रोजगार बचा है। कम से कम अधिक मुखर और हमलावर लोगों ने सोशल मीडिया पर नुपूर शर्मा पर इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया है, और इसी माहौल में जब राजस्थान के इस हिन्दू दर्जी के आठ बरस के बेटे ने बाप के सोशल मीडिया अकाऊंट पर नुपूर शर्मा की हिमायत में कुछ पोस्ट किया, तो उस पर उदयपुर के कुछ मुस्लिमों ने उसे हिंसक धमकी दी थी। इस पर कन्हैयालाल नाम के इस दर्जी को पुलिस ने पकड़ा था, और फिर छोड़ भी दिया था। अब दो मुस्लिम उसके पास कपड़े का नाप देने के नाम पर आए, एक ने नाप देते-देते कटार जैसे बड़े हथियार से उसका गला रेत दिया, और दूसरा मुस्लिम उसका वीडियो बनाते रहा जिसे बाद में अपने बयान के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या की धमकी के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस बहुत ही भयानक तालिबानी हिंसा के बाद पूरे राजस्थान में साम्प्रदायिक तनाव है, और गनीमत यह है कि ये दोनों हत्यारे गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
हिन्दुस्तान अपने आज के साम्प्रदायिक तनाव के साथ बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। कट्टर, धर्मान्ध, और साम्प्रदायिक ताकतों में से किसी भी एक ताकत से लैस हिन्दुस्तानी दूसरे का गला काटने की ताकत रखते हैं। धार्मिक कट्टरता और साम्प्रदायिक नफरत इस देश में आज सबसे अधिक ताकतवर इंजन बन गए हैं, और कुछ तबकों में डबल इंजन की नफरत चल रही है। राजस्थान में पिछले कुछ महीनों में बार-बार साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन घटनाओं से कुछ कम दर्जे के तनाव देश के अधिकतर प्रदेशों में छाए हुए हैं। ऐसे में राजस्थान के कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से अपील की है कि उनकी बातों का सार्वजनिक असर होता है, और उन्हें देश की आम जनता से शांति की अपील करने को कहा है। केन्द्र सरकार ने उदयपुर की इस तालिबानी-हत्या की जांच एनआईए को दी है, जो कि आतंकी पहलू के नजरिये से इस मामले की जांच करेगी। इस बीच एक खबर यह भी है कि भाजपा के जिन दो प्रवक्ताओं/नेताओं, नुपूर शर्मा, और नवीन जिंदल ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थीं, उनमें से नवीन जिंदल को उदयपुर का यह वीडियो भेजकर उसी तरह मारने की धमकी दी गई है। यह तनाव उम्मीद से परे का नहीं है, और ऐसे बयानों से लेकर ऐसे कत्ल तक का मकसद देश में हत्यारे तनाव को बढ़ाना ही रहता है, और साम्प्रदायिक ताकतें इसमें बहुत कामयाब हुई दिख रही हैं। आज इस देश के लोग जीने-खाने और कमाने की फिक्र को छोडक़र किसी धर्म के अपमान करने को अपना पेशा बना चुके हैं, और ऐसे लोगों के चलते देश में कोई भी महफूज नहीं रहेंगे।
यह वक्त हिन्दुस्तान को अब भी और जलने देने से बचाने का है, और अधिक खत्म हो जाने के पहले इसे थाम लेने का है। हाल के बरसों में देश के अमन-चैन, और भाई-बहनचारे की जो तबाही हुई है, उनसे उबरने में इन बरसों जितनी पीढिय़ां लग जाने वाली हैं, इसलिए तबाही के हर बरस को और आगे की एक पीढ़ी की बर्बादी मानकर इस खतरे का अंदाज लगाना चाहिए। जहां कन्हैयालाल का आठ बरस का बेटा एक नफरतजीवी नुपूर शर्मा की हिमायत में सोशल मीडिया पर नफरत का ट्वीट करता है, तो आज साम्प्रदायिकता ने किस पीढ़ी तक को तबाह कर दिया है, उसे समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए। गहलोत अपने राज्य राजस्थान की साम्प्रदायिक घटनाओं को रोकने में नाकामयाब दिख सकते हैं, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि पूरे देश के लोगों पर गहलोत की बात का असर नहीं हो सकता, और मोदी-शाह की बात का असर हो सकता है। इसलिए कम से कम प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोडक़र, देश के आज के माहौल पर कुछ बोलना चाहिए, और कुछ से अधिक काफी बोलना चाहिए। नाजुक मौकों पर चुप्पी के कई गलत मतलब भी निकाले जाते हैं, इसलिए जो जिम्मेदारी के ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो शोहरत-हासिल लोग हैं, उन लोगों को नाजुक मौकों पर चुप रहने का हक नहीं दिया जा सकता। आज देश में धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता जितनी तबाही ला रही है, वह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खतरा बन चुकी है। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री को खुलकर सामने आना चाहिए, और उन्हें अपना आदर्श मानने वाले लोगों के बीच भी जिस तरह की गलतफहमी या खुशफहमी फैली हुई है, उसे दूर करना चाहिए। किसी को ऐसा लग सकता है कि साम्प्रदायिक हिंसा से परे बड़े-बड़े कारखाने तो चलते ही रहते हैं, और उनसे देश की जीडीपी चलना जारी रहता है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। उदयपुर का कन्हैयालाल आज किसी दूसरे के सामान का ग्राहक नहीं रह गया है, और अपने ग्राहकों के लिए अब वह कपड़े नहीं सिलने वाला है। उसके कातिल भी अब न कोई ग्राहक रह जाएंगे, और न ही कारीगर। इस तरह देश की साम्प्रदायिक हिंसा कारोबार को खतम कर रही है, जिसकी रफ्तार धीमी लग सकती है, लेकिन इसका असर हर हिन्दुस्तानी पर पड़ रहा है, खासकर अगर वे अरबपति न हों।
देश को साम्प्रदायिकता और धर्मान्धता से उबारने की जरूरत है। जो ताकतें विवेकानंद से लेकर सरदार पटेल तक, और भगत सिंह से लेकर विनायक दामोदर सावरकर तक को अपना आदर्श मानती हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि आज वे सब अपने आदर्श कहे जाने वाले इन तमाम लोगों की कही बातों के ठीक खिलाफ काम कर रहे हैं। मन, वचन, और कर्म का यह विरोधाभासी पाखंड खत्म होना चाहिए। एक मेहनतकश कन्हैयालाल को दूसरे मेहनतकश मोहम्मद के हाथों मरवाने की तोहमत कुछ जटिल रास्तों से अपने ठिकाने तक पहुंच सकती हैं, सीधे-सीधे नहीं। यह देश इस नुकसान को झेलने की हालत में नहीं है, और ऐसा देश जाने किस जुबान से विश्व गुरू बनने का दंभ पाले हुए है। यह असाधारण समय है, और इसकी मांग है कि देश के असाधारण लोग इस वक्त चुप न रहें, हालात को सम्हालने की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करें।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
अमरीका के कई सरहदी राज्यों में वैसे तो पड़ोस के देशों से लोगों की गैरकानूनी घुसपैठ चलती ही रहती है, लेकिन अभी कुछ घंटे पहले वहां के टैक्सास में एक बड़ी लॉरी लावारिस पड़ी मिली जिसके भीतर 46 लाशें पड़ी हुई थीं। जाहिर तौर पर ये गैरकानूनी तरीके से अमरीका में आए हुए लोग थे जो कि मानव-तस्करी का कारोबार करने वाले लोगों की इस लॉरी में आगे ले जाए जा रहे थे। इसके भीतर न कोई एयरकंडीशनिंग थी, न ही पीने का पानी भी था, और इन 46 लाशों के बीच 16 लोग जिंदा भी मिले हैं जो कि लू और गर्मी की वजह से बुरी तरह तप रहे थे, और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अमरीका की मैक्सिको के साथ सरहद के करीब का यह हादसा वहां के पुलिस अफसरों को भी हिला गया है क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में ऐसी लाशें नहीं देखी थीं। मानव तस्कर तरह-तरह के तकलीफदेह सफर से लोगों को अमरीका में लाते हैं, और सरहद से दूर ले जाते हैं, लेकिन मौतों का यह रिकॉर्ड नया है। अमरीका में मैक्सिको से आते पिछले महीने ही दो लाख 40 हजार अवैध घुसपैठियों को पकड़ा गया था, और कितने लोग आए होंगे इसका कोई अंदाज अभी नहीं है। लेकिन यह हाल सिर्फ अमरीका का हो ऐसा भी नहीं है, योरप के अधिकतर देशों में बाहर के देशों से ऐसी घुसपैठ चलती ही रहती है, और लोगों को याद होगा कि जब सीरिया, लिबिया, अफगानिस्तान जैसे देशों में गृहयुद्ध जैसे हालात थे, तो वहां के लोग भी दूसरे देशों में पहुंचते थे, और समुद्र तट पर एक छोटे बच्चे की लाश की तस्वीर लोगों को अब भी परेशान करती है।
यह हादसा उस दिन सामने आया है जिस दिन अमरीकी राष्ट्रपति जी-7 देशों के प्रमुख लोगों के साथ दुनिया की आर्थिक असमानता और मानवाधिकारों पर चर्चा कर ही रहे हैं। इस बैठक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, और ब्रिटेन पिछले कुछ महीनों से अपनी एक शरणार्थी योजना को लेकर विवादों में घिरा हुआ है। ब्रिटेन पहुंचने वाले अवैध शरणार्थियों के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक अफ्रीकी देश रवांडा के साथ एक समझौता किया है, और ब्रिटेन अपनी दिक्कतों को बढऩे से रोकने के लिए ऐसे आ रहे शरणार्थियों को अपने खर्च से रवांडा भेजेगा, और वहां पर उनके लिए बनाए गए शरणार्थी शिविरों का खर्च भी उठाएगा। यह नीति खुद ब्रिटेन में बहुत बुरी आलोचना से घिरी हुई है, और मानवाधिकार की फिक्र करने वाले लोग यह मानते हैं कि यह शरणार्थियों के प्रति जिम्मेदारी पूरी करना नहीं है, उन्हें मामूली खर्च से अपनी आंखों से, और अपनी सरहद से दूर धकेल देना भर है। खैर, ब्रिटिश सरकार के इस बारे में अपने तर्क हो सकते हैं, और हर देश की शरणार्थी नीति अपनी घरेलू फिक्रों, और वहां के खतरों को देखते हुए ही बनाई जा सकती है। कुछ मुस्लिम देशों से आने वाले शरणार्थियों को जगह देकर योरप के कई देशों में जिस तरह के सांस्कृतिक टकराव सामने आ रहे हैं, वे भी वहां स्थानीय सरकारों पर एक दबाव बने हुए हैं। इससे परे भी जब बाहर से आए हुए शरणार्थियों में से कुछ लोग धार्मिक आधार पर आतंकी हमले करने लगते हैं, तो स्थानीय आबादी के बीच भी शरणार्थियों के खिलाफ एक नाराजगी खड़ी होने लगती है। ऐसी बहुत सी बातें शरणार्थियों को जगह देने के साथ जुड़ी हुई हैं, और कुछ देशों में तो शरणार्थी नीति किसी राजनीतिक दल की जीत या हार भी तय कर देती हैं।
आज दुनिया में आर्थिक असमानताएं इतनी अधिक हैं कि बहुत से देशों में भूखे मरने के बजाय लोग जिंदगी दांव पर लगाकर किसी ऐसे देश में घुस जाना चाहते हैं जहां पर उनके जिंदा रहने की तो गारंटी रहेगी ही, हो सकता है कि उनकी अगली पीढ़ी उन विकसित देशों की पूरी संभावनाएं हासिल कर सकें। यह उम्मीद इस कदर दुस्साहस दे देती है कि लोग रबर की छोटी सी बोट पर सवार होकर समंदर पार करके ऐसे किसी देश तक पहुंचने का खतरा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें यह तो मालूम रहता ही है कि उनके पहले ऐसी कोशिश करने वाले लोगों में से कुछ को कामयाबी भी मिली थी। और अपने देश के गृहयुद्ध के बीच, वहां की भुखमरी के बीच अपने बच्चों को हर दिन मरते देखने से बेहतर उन्हें यह लगता है कि जिंदगी के लिए एक कोशिश की जाए। आज जब जी-7 या किसी दूसरे किस्म के देशों के समूह बैठकर बाकी दुनिया की भी बात करते हैं, तो इस पर भी बात होनी चाहिए कि दुनिया के किसी भी देश के नागरिकों के कितने न्यूनतम अधिकारों की गारंटी करना संपन्न और विकसित देशों की जिम्मेदारी रहेगी। दुनिया में जब तक सबसे गरीब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, धार्मिक और राजनीतिक आधार पर हिंसा जारी रहेगी, गरीबों की अमीर देशों में घुसपैठ जारी रहेगी, और यह सिलसिला सरहदी सिपाहियों के रोके रूकने वाला नहीं है।
दुनिया के संपन्न और विकसित देशों को सबसे गरीब देशों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अपनी वैश्विक जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। आज धरती के किसी हिस्से पर कोई देश है, और किसी दूसरे हिस्से पर कोई दूसरा देश। लेकिन धरती तो एक ही है, और उसके हर इंसान का एक न्यूनतम अधिकार वैश्विक संपदा पर है ही। इस अधिकार का सम्मान करने की बात होनी चाहिए, और ऐसा किए बिना कोई भी देश अपनी इंसानियत का दावा नहीं कर सकेंगे। जब कोई हादसा एक सीमा से परे का तकलीफदेह होता है, तो ही वह सोचने पर मजबूर करता है। अमरीका में कल जितनी बड़ी संख्या में जिस हालत में लाशें मिली हैं, उन्हें देखते हुए दुनिया को एक ईकाई मानकर हालात सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
सोशल मीडिया की मेहरबानी से किसी भी जलते-सुलगते मुद्दे पर खास से लेकर आम लोगों तक को अपने मन की बात कहने का मौका हासिल है। और इसी के चलते हुए अभी लगातार यह बात लिखी जा रही है कि महाराष्ट्र से शिवसेना के विधायकों को लेकर पहले भाजपा शासित गुजरात और फिर भाजपा शासित असम ले जाने वाले विमानों का खर्चा कहां से आ रहा है? लोग यह भी पूछ रहे हैं कि विधायकों का पहला बड़ा जत्था गुवाहाटी पहुंच जाने के बाद छोटे-छोटे जत्थों के लिए फिर से विमान जुटाने का खर्च कहां से आ रहा है? और एक बात यह भी उठ रही है कि पिछले कई राज्यों की राज्य सरकारें पलटने के वक्त सत्तारूढ़ पार्टी के बागी विधायकों को दूसरी पार्टी के राज्य वाले प्रदेश के महंगे होटल या रिसॉर्ट में ठहराने का खर्च कहां से आता है? बाढ़ में डूबे हुए असम में नदियों के पानी में लाशों के तैरने की तस्वीरें इंटरनेट पर तैर रही हैं, और ऐसे माहौल में ये सवाल बड़ी तल्खी के साथ उठाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार पलटने के लिए यह पूरा खर्च कौन उठा रहा है? केन्द्र सरकार की एजेंसियां इसकी जांच क्यों नहीं कर रही हैं?
इस मुद्दे पर किसी का पक्ष लेने के बजाय हम इसकी बुनियादी बातों पर जाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में मुम्बई में किसी एक जमीन या इमारत पर कारोबारी इजाजत देने पर सत्ता को दसियों करोड़ रूपये मिल सकते हैं, और मिलते भी रहे होंगे। ऐसे में 25-50 लाख रूपये अगर विशेष विमानों और महंगी होटलों पर खर्च हो भी रहे हैं, तो उसे मुद्दा बनाने का मतलब असल मुद्दे को छोड़ देना है। अगर नीयत सांप को मारने की है, तो उसके गुजर जाने के बाद उसकी लकीर पर लाठी पीटने से क्या हासिल होगा? आज राजनीतिक पार्टियों की सत्ता जिस बड़ी दौलत में खेलती हैं, उसके सामने कुछ दर्जन विधायकों का हफ्ते-दस दिन किसी होटल में रहना कोई बड़ा खर्च नहीं है। और यह पहली बार भी नहीं हो रहा है।
लोगों को याद होगा कि अभी कुछ बरस पहले ही जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की भाजपा सरकार में शामिल वहां के सबसे बड़े खदान कारोबारी और सरकार में मंत्री रेड्डी बंधु जब अपनी ही सरकार गिराना चाहते थे, तो वे बाढ़ में तबाह कर्नाटक के दर्जनों विधायकों को लेकर कई दिन आन्ध्र के हैदराबाद के किसी सात सितारा होटल में पड़े हुए थे। जैसे-जैसे राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ते चल रहा है, सत्ता की कमाई बढ़ते चल रही है, वैसे-वैसे सांसदों और विधायकों की खरीद-फरोख्त के रेट बढ़ रहे हैं, सौदेबाजी बढ़ रही है, और नई सत्ता पर पूंजीनिवेश करने के लिए बड़े कारोबारियों में उत्साह भी बढ़ रहा है। जो लोग राज्यों के कामकाज से वाकिफ हैं, वे जानते हैं कि राज्य की चुनिंदा ताकतवर कुर्सियों पर अपने पसंदीदा अफसरों को लाने के लिए बड़े कारोबारी बड़ा पूंजीनिवेश करने को एक पैर पर खड़े रहते हैं। यही हाल केन्द्र सरकार में कुछ खास मंत्रालयों के मामले में होता है जहां आने वाले अफसरों का अपनी मर्जी का होने के लिए देश के बड़े कारोबारी सरकार पर अपने सारे असर का इस्तेमाल करते हैं, जरूरत रहती है तो पेशगी भी देते हैं, और फिर किस्त भी बांध देते हैं। जिस देश में और उसके प्रदेशों में भ्रष्टाचार के पैमाने इतने ऊपर जा चुके हैं, वहां अगर महाराष्ट्र की नई सरकार अपनी मर्जी से बनवाने के लिए होटल, हवाई जहाज, और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर दस-बीस करोड़ रूपये खर्च भी होने जा रहे हैं, तो इतनी रकम तो मुम्बई कीकिसी एक खास पुलिस-कुर्सी के लिए करने लोग तैयार रहते हैं।
हम किसी भी किस्म के भ्रष्ट पूंजीनिवेश की वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब लोकतंत्र दांव पर लगा है, तब कुछ करोड़ के बिल पकडक़र उस पर बहस करने से असल मुद्दा तो धरे ही रह जाएगा। आज भारत की राजनीति में त्रिपुरा के माक्र्सवादी मुख्यमंत्री रहे माणिक सरकार जैसे आदर्शों की उम्मीद नहीं करना चाहिए जिनके चुनावी घोषणापत्र के मुताबिक उनके पास 10 हजार 8 सौ रूपये थे, और जो तनख्वाह पार्टी में जमा कर देते थे, और वहां से उन्हें गुजारे के लिए पांच हजार रूपये महीने मिलते थे। उनकी जिंदगी में केन्द्र सरकार की कर्मचारी रही पत्नी की पेंशन से भी मदद मिलती थी जिसने पति के मुख्यमंत्री रहते हुए भी पूरे वक्त रिक्शे से सरकारी दफ्तर आना-जाना किया करते थे। और माणिक सरकार ऐसी ईमानदारी वाले अकेले वामपंथी मुख्यमंत्री नहीं थे। उसी त्रिपुरा में उनके पहले नृपेन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री रहे, और उनकी ईमानदारी का भी यही हाल रहा। नृपेन चक्रवर्ती जब मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे तो उनका सारा सामान टीन की एक पेटी में था। एक दशक बाद जब वे मुख्यमंत्री निवास से हेमेले हॉस्टल गए, तो रिक्शे पर उनके साथ वही एक पेटी गई। दस बरस मुख्यमंत्री रहते हुए इस पेटी में कोई नया सामान नहीं जुड़ा।
जिस देश ने ऐसे लोगों का और उनकी पार्टी का चुनावी नक्शे से नामोनिशान मिटा दिया है, उन्हें अब विशेष विमानों में एक होटल से दूसरे रिसॉर्ट जाने वाले विधायक और सांसद ही नसीब होने चाहिए, और नसीब हैं। इन छोटे-छोटे खर्चों को अगर कोई आज बड़ी मुद्दा मान रहे हैं, तो यह दाऊद इब्राहिम के स्टेडियम में सिगरेट पीने जितना बड़ा ही जुर्म है, जिस पर खूब लंबी बहस हो सकती है, उसके बाकी के तमाम जुर्मों को अनदेखा करते हुए। लोगों को लोकतंत्र के लिए मायने रखने वाले मुद्दों के पहलुओं को उनकी असल अहमियत के अनुपात में ही महत्व देना चाहिए। भारत की राजनीति अब गांधीवादी मूल्यों का खेल नहीं रह गई है। इसलिए अब कुछ करोड़ों के खर्च पर बहस खर्च करना सिवाय बेवकूफी के कुछ नहीं है। मुम्बई का शहरी विकास विभाग का एक छोटा सा अफसर यह पूरा खर्च उठा सकता है, और इतने से खर्च को लेकर भाजपा पर तोहमतें लगाना भी ठीक नहीं है। राजनीतिक दल होटल के कमरे, और प्लेन की सीट पर खर्च नहीं करते, वे संसद और विधानसभा के भीतर की सीटों को खरीदते-बेचते हैं। इसलिए सोशल मीडिया और बाकी मीडिया पर भी जो लोग विधायकों के जनवासे के खर्च पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी मासूमियत पर तरस आता है।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
पंजाब के चंडीगढ़ में एक आईएएस अफसर के बेटे ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, और परिवार का कहना है कि पंजाब विजिलेंस की जो टीम उनकी घर की तलाशी लेने आई थी, उसी ने बेटे को गोली मार दी हैं। यह आईएएस अफसर, संजय पोपली, कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और उसकी काली कमाई की जांच के लिए विजिलेंस कई जगह छापेमारी कर रही है, और इसी सिलसिले में उसके घर पहुंची थी जहां परिवार में यह हादसा हुआ। विजिलेंस को इस अफसर के घर से बारह किलो सोना, तीन किलो चांदी की ईटें मिली हैं, और अनगिनत दूसरे महंगे सामान भी। इस अफसर की जांच पाईप लाईन टेंडर मंजूर करने के लिए एक फीसदी कमीशन मांगने के आरोप के बाद हुई थी, और वहां से इन सामानों के साथ-साथ हथियार और कारतूस भी मिले, जिन्हें लेकर एक अलग मामला दर्ज किया गया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले दिन से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मोर्चा खोलने की घोषणा की थी, और देश का शायद यह पहला मौका था कि मुख्यमंत्री ने काम सम्हालने के कुछ हफ्तों के भीतर ही अपने एक मंत्री को भ्रष्टाचार के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया। अब यह महज दिखावा मानना या कहना तो नाजायज होगा क्योंकि सरकार के मंत्री का ऐसा भ्रष्ट होना सरकार के लिए बदनामी भी लेकर आता है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हौसला दिखाया था।
अकाली-भाजपा गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की सरकारों के रहते हुए पिछले दशकों में पंजाब भ्रष्टाचार में डूबा हुआ राज्य बन गया था, और वहां मंत्री भी नशे की तस्करी में शामिल बताए जाते थे। दोनों ही तरह की सरकारें जमीन से कट गई थीं, सामंती और कुनबापरस्त अंदाज में चल रही थीं, और शायद यही वजह थी कि वोटरों ने इस बार हैरतअंगेज नतीजे देते हुए इन तीनों ही पार्टियों को खारिज कर दिया था, और आम आदमी पार्टी को सत्ता दे दी थी। लोगों को यह भी याद रहना चाहिए कि दो चुनाव पहले दिल्ली में भी वोटरों ने कांग्रेस और भाजपा को एकमुश्त खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी को सत्ता दी थी, और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में सरकार दुबारा लौटकर भी आई। दिल्ली में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम केजरीवाल का एक बड़ा नारा रहा, और अगर लगातार दो चुनावों के नतीजे कोई संकेत हैं, तो वोटरों ने उनके इस नारे पर भरोसा किया दिखता है।
लेकिन पंजाब, दिल्ली, और आम आदमी पार्टी से परे देश में भ्रष्टाचार की बात करें, तो सरकारों का एक बड़ा बजट भ्रष्टाचार के हवाले हो जाता है। अलग-अलग सरकारों में भ्रष्टाचार के तौर-तरीके अलग हो सकते हैं, कहीं पर हर ठेकेदार से रिश्वत और कमीशन ली जाती है, कहीं पर अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को एक बड़ी इंडस्ट्री की तरह चलाया जाता है, और कहीं-कहीं बड़े कारोबारियों को सरकारी कामकाज में उपकृत करके उनसे पर्दे के पीछे भागीदारी कर ली जाती है। हिन्दुस्तान में अलग-अलग पार्टियों और देश-प्रदेश की सरकारों के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरा देश भ्रष्टाचार में बुरी तरह डूबा हुआ है, और आम जनता उसमें पिस रही है। आज जब यूक्रेन यूरोपीय समुदाय का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, तो यूक्रेन का मौजूदा भ्रष्टाचार इस राह का रोड़ा बना हुआ है। यूरोपीय यूनियन जैसा विकसित लोकतंत्रों और सभ्य समाजों का गठबंधन भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा मानता है, और किसी को सदस्य बनाने के पहले उस देश की सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब देना पड़ता है, कानून बनाने पड़ते हैं, और उन पर अमल भी करना पड़ता है। आज हिन्दुस्तान ऐसे किसी समुदाय की सदस्यता की जरूरत से बहुत दूर है, लेकिन अगर ऐसी कोई नौबत रहती, तो हिन्दुस्तान कभी यूरोपीय यूनियन जैसी संस्था का सदस्य नहीं बन सकता था।
आज की ही एक दूसरी खबर बताती है कि जिस बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुशासन बताया जाता है, उसकी राजधानी पटना में सरकारी निगरानी विभाग ने एक ड्रग इंस्पेक्टर के घर पर छापा मारा तो वहां से पांच बोरों में भरे हुए चार करोड़ के नोट मिले, दर्जनों जमीनों के कागज मिले, कई कारें मिलीं, और गहने, बैंक खाते मिले। अब ड्रग इंस्पेक्टर तो राज्य सेवा का एक छोटा अफसर होता है, और बिहार को नीतीश कुमार का सुशासन कहा जाता है, वहां यह हाल है। आज अगर एक प्रदेश के एक अफसर के घर के स्टोर रूम से सोने-चांदी का ऐसा जखीरा निकल रहा है, दूसरे छोटे अफसर के घर बोरों में करोड़ों के नोट निकल रहे हैं, और दूर-दूर तक उसकी दौलत बिखरी होने की जांच जारी ही है, तो फिर पूरे देश को कुल मिलाकर किस तरह बेचा जा रहा है, यह साफ है। हमारा तो यह मानना है कि भ्रष्ट अफसरों से जितनी जब्ती हो पाती है, वह उनकी काली कमाई का एक बहुत ही छोटा हिस्सा रहता है, बाकी तो चारों तरफ बेनामी जायदाद और दूसरे देशों के बैंकों में चले जाता है। ऐसे में देश-प्रदेश की सरकारें अगर कोई ईमानदार नीयत रखती हैं, तो उन्हें किसी के इतने अधिक भ्रष्ट हो जाने के बहुत पहले ही उसे दबोच लेने का इंतजाम रखना चाहिए। जब भ्रष्ट अफसर अरबपति हो जाएं, उसके बाद उन पर हाथ डाला जाए, तो उसका मतलब है कि वे सरकारी पैसों और कामकाज की दसियों गुना अधिक बर्बादी कर चुके हैं, जनता के हितों और सरकारी कामकाज की क्वालिटी को बेच चुके हैं। यह हालत ऑल इंडिया सर्विस कही जाने वाली नौकरियों की है, जिनके लिए देश भर से सबसे चुनिंदा लोगों को छांटा जाता है, और फिर वे आनन-फानन देश के सबसे भ्रष्ट लोग भी बनने का खतरा रखते हैं। यह सिलसिला अखिल भारतीय सेवाओं की साख को खत्म कर चुका है, और केन्द्र सरकार और अलग-अलग प्रदेशों में हर किस्म के भ्रष्टाचार के नमूने मौजूद हैं।
अच्छी साख वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने डेढ़ दशक पहले एक सर्वे किया था तो उसमें पाया था कि पचास फीसदी हिन्दुस्तानी रिश्वत देकर, या कोई पहचान जुटाकर सरकारी काम करवा पाते हैं। 2021 में भ्रष्टाचार पर जनधारणा का एक सर्वे हुआ, उसमें दुनिया के 180 देशों में हिन्दुस्तान को 85वें जगह पर रखा गया था, यानी यह देश दुनिया के 84 और देशों के मुकाबले अधिक भ्रष्ट मिला था। केन्द्र और राज्य सरकारों के कई विभाग भ्रष्टाचार की सबसे अधिक गुंजाइश रखने वाले माने जाते हैं, और मंत्रियों में इन विभागों को पाने के लिए गलाकाट मुकाबला तो चलता ही है, अफसर भी इन विभागों या ऐसी जगहों पर तैनाती के लिए लूटपाट करने को तैयार रहते हैं।
पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार सचमुच ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लगी हुई है, या यह उसका दिखावा है, जो भी हो, देश-प्रदेश की तमाम सरकारों को अपने राज के भ्रष्टाचार पर काबू पाना चाहिए, और जनता के बीच के लोगों को भी चाहिए कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग-अलग तरह की लड़ाई लड़ें। यह इसलिए भी जरूरी है कि भ्रष्टाचार सबसे गरीब जनता के बुनियादी हक भी खा जाता है, लोगों को अपने परिवार की लाश के पोस्टमार्टम के लिए भी रिश्वत देनी होती है, और मानवाधिकारों का इससे बुरा कुचलना और क्या हो सकता है? लोग अपने-अपने आसपास के भ्रष्टाचार को देखें, और अपनी जिम्मेदारी सोचें।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
अमरीका में पिछले दो-चार दिनों में वहां की सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों ने अमरीकी समाज को बड़ा झटका दिया है। खासकर समाज के उस हिस्से को जो संविधान में दिए गए एक बुनियादी अधिकार के साथ बंदूकों को लेकर कुछ शर्तें जोडऩा चाहते हैं क्योंकि आए दिन नौजवान किसी तनाव या नफरत को लेकर सार्वजनिक जगहों पर गोलीबारी कर रहे हैं, और कई लोगों को मार डाल रहे हैं। अमरीका के मौजूदा कानून में 18 बरस के होते ही लोग मनचाही बंदूकें खरीद सकते हैं, और ऐसे हमलावर हथियार भी बेहिसाब लेकर रख सकते हैं जिनमें से एक-एक हथियार से पलक झपकते दर्जन भर लोगों को मार डाला जा सकता है। अमरीकी सरकार हाल के महीनों की ऐसी गोलीबारी के बाद लगातार कोशिश कर रही थी कि एक जनमत ऐसा तैयार हो जो बंदूकें रखने के बुनियादी हक के साथ-साथ कुछ सावधानियों की शर्तें जोडऩे की इजाजत सरकार को दे। अभी अमरीका के न्यूयॉर्क राज्य का एक कानून सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जो कि लोगों को सार्वजनिक जगहों पर हथियार लेकर चलने से रोकता था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों में से जिन छह ने इस फैसले पर सहमति दी है, उनमें से तीन को पिछले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के कार्यकाल में नियुक्त किया गया था। अमरीकी न्याय व्यवस्था हिन्दुस्तान जैसे देश से अलग है, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज मरने तक काम करते हैं, और ऐसे में किसी जज के गुजरने पर ही मौजूदा राष्ट्रपति को अपनी पसंद का जज बनाने का मौका मिलता है। इसलिए राष्ट्रपति की अपनी विचारधारा वाले जज अनायास ही बनते हैं, और ट्रंप को ऐसे तीन जज बनाने का मौका मिला था।
अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला पचास बरस पहले के इसी अदालत के एक फैसले को खारिज करने वाला है, और इस फैसले से देश भर में अमरीकी महिलाओं को गर्भपात का फैसला लेने का हक खत्म हो गया है। सिर्फ एक-दो बहुत ही सीमित किस्म के मामलों में गर्भपात हो सकेंगे, जैसे कि गर्भपात न होने से अगर गर्भवती की जिंदगी को खतरा है, तो बड़ी कड़ी मेडिकल सिफारिश पर ही ऐसा गर्भपात हो सकेगा। अमरीका में गर्भपात हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है, और चुनावों के दौरान भी पार्टियों और नेताओं को इस मुद्दे पर अपना रूख साफ करना होता है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ही फैसले की उम्मीद की जा रही थी क्योंकि वहां के जजों ने डोनल्ड ट्रंप के नियुक्त किए हुए, और कन्जर्वेटिव विचारधारा के जजों का बहुमत है, और पांच जजों ने बहुमत से यह फैसला दिया, तीन जज इसके खिलाफ रहे। इस फैसले से भी अमरीका के उदारवादी, नागरिक अधिकारों के हिमायती, और डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक बहुत निराश हुए हैं, और इसे महिला अधिकारों के आंदोलन की एक बहुत बड़ी हार माना जा रहा है।
ये दोनों फैसले बिल्कुल ही अलग-अलग संदर्भों में हैं, लेकिन ये दोनों ही मौजूदा अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन की सोच के खिलाफ गए हैं, और अमरीका के काले लोग, दूसरे देशों से वहां पहुंचे हुए दूसरी नस्लों के लोग, प्रवासी और शरणार्थी लोग इन सबकी उम्मीदों पर पानी फेरने वाले रहे हैं। जिस अमरीका में आधी सदी से महिलाओं को गर्भपात का फैसला लेने का हक था, आज वह तस्वीर पूरी तरह पलट गई है। इसी तरह बरसों से यह बहस चली आ रही थी कि लोगों के हथियार रखने के साथ कुछ शर्तें जोड़ी जानी चाहिए ताकि हिंसक, नफरतजीवी, और विचलित मानसिक स्थिति के लोग हमलावर हथियार इक_े न कर सकें। लेकिन आज हालत यह है कि अनगिनत अमरीकी परिवार अपनी खरीदी हुई बंदूकों की घर के भीतर ही जब नुमाइश करते हैं तो ऐसा लगता है किसी फौजी बटालियन के हथियारों की दशहरे की पूजा हो रही है। अभी कुछ हफ्तों के भीतर जिस तरह दो बड़ी-बड़ी सामूहिक हत्याएं दो नौजवानों ने की हैं, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि गनकंट्रोल पर बात कुछ बन सकेगी, और जनमत तैयार हो सकेगा, लेकिन न्यूयॉर्क के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही निराश करने वाला है, और आज की अमरीका की जरूरत, वहां के आम लोगों की हिफाजत के खिलाफ है।
अमरीका के घरेलू मामलों से बाकी दुनिया का अधिक लेना-देना नहीं है, क्योंकि न तो बाकी दुनिया की महिलाओं को गर्भपात के लिए अमरीका जाना है, और न ही जब तक किसी सैलानी पर अमरीका में गोली चले, तब तक वहां गए पर्यटकों को भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन इससे दुनिया भर के सोचने के लिए यह मुद्दा उठता है कि जजों की निजी सोच किस तरह किसी देश की तस्वीर बदल सकती है। अमरीका में न्यायपालिका को लेकर तरह-तरह के विश्लेषण करने की छूट लोगों को है। हिन्दुस्तान में अदालतें जिस तरह की टिप्पणी पर अवमानना का केस शुरू कर दें, वैसी टिप्पणी अमरीका में आम हैं कि कौन से जज कैसी सोच रखते हैं, और किस मामले में वे किस तरह फैसला दे सकते हैं, यह आमतौर पर लिखा जाता है। यह भी आमतौर पर लिखा जाता है कि किस राष्ट्रपति ने उन्हें जज बनाया है। इसलिए अमरीका की बात अलग है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों को अपनी-अपनी न्याय व्यवस्था के भीतर यह सोचने की जरूरत है कि वहां किस तरह के जज बनाए जा रहे हैं, किस तरह की ताकतें जज छांट रही हैं, और रिटायर होने के बाद जज सरकार से किस-किस तरह के उपहारों और उपकारों की उम्मीद कर रहे हैं। यह सब समझने की बात है, और किसी जिम्मेदार लोकतंत्र को अपने आपको ऐसी फिक्र से बेपरवाह नहीं रखना चाहिए। दुनिया के तमाम देशों को, खासकर उन्हें जिन्हें अपनी न्यायपालिका पर बड़ा गुरूर है, उन्हें अमरीका में ट्रंप के बनाए जजों, और उनके ऐसे फैसलों को लेकर आई नौबत पर विचार करना चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
विज्ञान, विज्ञान कथाओं के मुकाबले कभी-कभी अधिक रफ्तार से आगे बढ़ते दिखता है। विज्ञान और तकनीक में इंसानी कामयाबी उसकी कल तक की उम्मीद के मुकाबले बहुत आगे चल रही है। अब ऐसे में गूगल के एक ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस इंजीनियर ने जब यह दावा किया कि वह भाषा की समझ के प्रयोग करते हुए इसी मकसद के लिए बनाई गई एक मॉडल के साथ बात कर रहा था, तब उसने पाया कि ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस वाली यह मॉडल अपनी भावनाओं के साथ बोलने लगी थी। अब तक ऐसे कम्प्यूटर उनमें डाली गई जानकारी, याददाश्त, और उसके कम्प्यूटर-विश्लेषण के आधार पर जवाब देते हैं, लेकिन यह मॉडल ऐसी एक बातचीत के दौरान भावनाओं के साथ बोलने लगी, तो यह इंजीनियर भी हक्का-बक्का रह गया। उसने यह बात अपनी वेबसाइट पर लिखी, और कंपनी ने उसे अभी काम से अलग कर दिया है। गूगल ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के साथ जुड़े हुए बहुत से नैतिक पहलुओं पर भी शोध और काम करते चल रहा है, और ब्लेक मोइन नाम का यह इंजीनियर इन्हीं पहलुओं पर काम कर रहा था। अब काम से सस्पेंड हो जाने के बाद ब्लेक का कहना है कि उसकी कम्प्यूटर मॉडल (चैटबोट) ने भावनाएं हासिल कर ली हैं, और उसने अब ब्लेक से कहा है कि वह उसके लिए एक वकील तलाश दे। हालांकि गूगल ने, और दूसरे ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस विशेषज्ञों ने ब्लेक के इस दावे को खारिज कर दिया है कि कोई कम्प्यूटर भावनाएं हासिल कर सकता है।
यह अकेली खबर जितनी हैरानी खड़ी करती है, उतने ही सवाल भी खड़े करते हैं। अगर कृत्रिम बुद्धि पाने वाले कम्प्यूटर भावनाएं भी पाने लगेंगे, और भावनाओं के आधार पर फैसले लेकर काम करने लगेंगे, तो शायद वे उन्हें एक खास मकसद से बनाने वाले इंसानों के काबू के बाहर हो जाएंगे। अभी भी विज्ञान के साथ यह एक बड़ा खतरा जुड़ा हुआ ही है कि उसकी ताकत इंसानों के काबू के बाहर हो सकती है। अभी तक तो विज्ञान और तकनीक इंसानों के हाथ औजार और हथियार की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे उनमें कृत्रिम बुद्धि बढ़ाई जा रही है, विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाई जा रही है, वैसे-वैसे वे उस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि इन कम्प्यूटरों में भावनाएं, और चेतना आ जाने पर हो सकता है। आज कम्प्यूटर अपनी कृत्रिम बुद्धि से कई तरह के काम करने के लायक बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें भावनाओं से लैस नहीं किया गया है, या उन्होंने खुद भावनाएं हासिल नहीं की हैं। लेकिन विज्ञान और टेक्नालॉजी में कई बार यह होता है कि खोज किसी चीज की जाती है, और हासिल कोई और चीज हो जाती है। किसी बीमारी का इलाज ढूंढा जाता है, और किसी और बीमारी का इलाज हाथ लग जाता है। ऐसे में ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को बढ़ाते चलते इंसानों को हो सकता है कि उस पल की खबर न लगे जब ऐसे कम्प्यूटर अपनी कृत्रिम बुद्धि से भावनाएं हासिल कर लें, नैतिकता के अपने पैमाने तय कर लें, और अपने फैसले खुद लेने लगें। ऐसी नौबत बहुत आसान नहीं लग रही है, और इसीलिए कम्प्यूटर के भावनाओं के इस ताजे दावे की वजह से गूगल ने अपने एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है।
दुनिया में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिनमें कम्प्यूटर मशीनों, या रोबो को बेकाबू होकर अपनी भावनाओं से काम करते दिखाया है। वे अच्छे और बुरे का फैसला खुद लेने लगते हैं, और उन्हें बनाने वाले लोगों को भी हक्का-बक्का कर देते हैं। और ऐसी नौबत फिल्मों और विज्ञान कथाओं से परे, असल जिंदगी में बहुत दूर रह गई हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अब पल भर के लिए यह कल्पना करें कि भारत की संसदीय राजनीति में सही और गलत का फैसला करने के लिए ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लैस किसी कम्प्यूटर पर नियम-कायदे और लोकतंत्र की परंपराओं को डाला जाए, और फिर यह कहा जाए कि जिन लोगों का आचरण असंसदीय है, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है, उन लोगों को सजा दी जाए, और कम्प्यूटर ऐसे लोगों के फोन बंद कर दे, उनके बैंक खातों का काम बंद कर दे, उनकी कार को रिमोट से बंद कर दे, और उन्हें पकडऩे के लिए पुलिस भेज दे, तो क्या होगा? अभी तक इंसान जाहिर तौर पर तो ऐसे कम्प्यूटर नहीं बना रहे हैं जिनके बेकाबू हो जाने का खतरा हो, लेकिन जब दुनिया की महाशक्तियां फौजी दर्जे की रिसर्च के नाम पर बहुत से अनैतिक काम करती हैं, तो क्या वे ऐसे रोबोसोल्जर नहीं बना रही होंगी जो कि जंग के मैदान में दुश्मनों को छांट-छांटकर, खुद फैसले लेकर उन्हें मारे? आज तो जंग के हथियारों में भी घोषित तौर पर ऐसे हथियार या मशीनी सैनिक नहीं बनाए जा रहे हैं जो मारने का फैसला भी खुद लें, लेकिन क्या फौजों और उनकी सरकारों पर सचमुच ही इतना भरोसा किया जा सकता है कि वे पर्दे के पीछे भी ऐसी टेक्नालॉजी विकसित नहीं कर चुके होंगे?
अब कृत्रिम बुद्धि से लैस रोबो भावनाओं और नैतिक मूल्यों से भी कब लैस कर दिए जाएंगे, यह महज वक्त की बात लगती है। अभी गूगल के इस ताजा मामले के बाद यह भी बहस चल रही है कि ऐसे रोबो, या चैटबोट के साथ लगातार काम करने वाले लोग क्या उनसे ऐसे भावनात्मक संबंध भी बना लेंगे कि वे उन्हें अपने रिसर्च के दायरे के बाहर भी भावनाओं से लैस करने की सोचने लगें? कुछ लोग इसे एक सचमुच का खतरा मानते हैं कि लगातार किसी चैटबोट के साथ काम करते हुए इंजीनियर और उसके बीच ऐसे भावनात्मक संबंध हो जाएं कि इंजीनियर या शोधकर्ता उसे इंसानी दर्जे के करीब लाने लगे, अपनी मोहब्बत को जिंदा शक्ल देने लगे। अब गूगल से अभी सस्पेंड इस इंजीनियर ने अपनी इस चैटबोट के कहे उसके लिए एक वकील छांटकर उससे संपर्क करवा दिया है, और वकील से बातचीत करके चैटबोट ने उसे अपना केस दे भी दिया है। यह पूरा सिलसिला एक विज्ञान कथा की तरह लग रहा है, लेकिन यह उस गूगल कंपनी के भीतर की बात है जिसके बिना आज के एक आम और औसत इंसान की जिंदगी कुछ घंटे भी नहीं चलती।
आज से दस-बीस बरस में ऐसे मामले-मुकदमे शायद देखने मिल जाएं कि चैटबोट के लिए किसी ने अपने जीवनसाथी को छोड़ा, और चैटबोट से शादी कर ली। या चैटबोट ने ईर्ष्या में अपने रिसर्चर की प्रेमिका को मार डाला। देखें आगे क्या-क्या होता है...
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
हिन्दुस्तान में फौज एक बड़ा मुद्दा है। हर बरस 25-50 हजार लोगों को नौकरी देने की ताकत से परे भी बहुत सी बातें हैं जो हिन्दुस्तान में फौज की अहमियत बताती हैं। इनमें से एक तो यह है कि यह एक साथ दो ऐसे देशों से घिरा हुआ है जिनसे हिन्दुस्तान के रिश्ते दुश्मनी के माने जाते हैं। दूसरी बात यह कि इन दोनों के आपसी रिश्ते दुनिया में सबसे अधिक मीठे रिश्तों वाले देशों सरीखे हैं। और जब इन दोनों से एक साथ हिन्दुस्तान की तनातनी चल रही है, तो इस मुल्क की फौज को इन दोनों से एक साथ जूझने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज इस फौज को लेकर जितने तरह के सवाल उठ रहे हैं, वे ऐसी किसी तैयारी से बिल्कुल परे के हैं, और फौज पर आज की तारीख में लदे हुए पेंशन के बोझ को आगे चलकर घटाने की नीयत के हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अग्निपथ नाम की नई योजना सरकार की फौजी योजना नहीं है, वह एक वित्तीय योजना है कि सस्ते में सैनिक कैसे जुटाए जा सकते हैं, और उनका बोझ फौज पर डालने से कैसे बचा जा सकता है। किफायत बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में यह किफायत की जा रही है, वह अंदाज बड़ा अटपटा है, और लोगों के मन में ऐसे शक खड़े कर रहा है जिनके बारे में बहुत पहले किसी ने कहा था कि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। आज की मौजूदा सरकार के पास तो जनता के बीच खड़े हो गए शक का इलाज बिल्कुल भी नहीं है।
देश के फौजी और प्रतिरक्षा के दूसरे मामलों के जानकार लोगों का कहना है कि अग्निपथ नाम की यह योजना इस रहस्यमय तरीके से रातों-रात सामने रख दी गई कि इस पर देश में कोई लोकतांत्रिक बहस भी नहीं हो पाई, लोगों से राय भी नहीं ली जा सकी। और इसमें ऐसी किसी फौजी गोपनीयता की बात भी नहीं थी कि परमाणु विस्फोट करने के पहले कैसे उस राज को उजागर किया जाए। आज अग्निपथ का जितना विरोध हो रहा है, और उसकी जितनी आलोचना हो रही है, और उसे बचाने के लिए सरकार को जिस तरह फौजी वर्दियों को सामने बिठाकर उसका बचाव करना पड़ रहा है, उन सबसे सरकार की साख अच्छी नहीं हो रही है। इस पर आज लिखने की एक ताजा वजह यह है कि देश के आज मौजूद एकमात्र परमवीर चक्र विजेता और सियाचीन के हीरो, कैप्टन बानासिंह ने एक अखबार से बातचीत में खुलकर कहा है कि अग्निपथ की वजह से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये योजना सेना को बर्बाद कर देगी, और पाकिस्तान चीन को फायदा पहुंचाएगी। बानासिंह 73 बरस की उम्र में सर्वोच्च फौजी सम्मान के साथ रिटायर्ड जिंदगी जी रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जिस तरह अग्निपथ योजना सब पर थोपी गई है, वह तानाशाही के समान है। उन्होंने कहा कि सैनिक बनना खेल नहीं है, इसके लिए सालों की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, और महज छह महीने में कैसे किसी की ट्रेनिंग हो सकती है? उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस योजना को लाने का फैसला किया, उन्हें सशस्त्र बलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
किसी एक रिटायर्ड बहादुर फौजी की बात से असहमत होने वाले लोग भी हो सकते हैं, लेकिन फौजी रणनीति के जानकार बहुत से दूसरे लोगों का यह मानना है कि अग्निपथ और अग्निवीर का यह सिलसिला लोगों पर थोप दिया गया है, और चूंकि सरकार ने एक बार यह फैसला ले लिया है, तो अब उसे किसी भी कीमत पर लोगों पर लादा जा रहा है। जिस तरह नोटबंदी का फैसला लेकर, उसे लोगों पर लादने के लिए लगातार उसमें बदलाव किए गए थे, जिस तरह लॉकडाउन और टीकाकरण के फैसले लेकर फिर उन्हें लागू करवाने के लिए लगातार फेरबदल किए गए थे, जिस तरह जीएसटी को हड़बड़ी में आधी रात की आजादी की तरह का जलसा संसद में करके उसे लागू किया गया था, और उसके बाद उसमें सैकड़ों फेरबदल किए गए, ठीक उसी तरह दो दिनों के भीतर ही अग्निपथ के साथ भी हो रहा है, और सडक़ों पर आगजनी को देख-देखकर सरकार तरह-तरह के रास्ते निकालते दिख रही है कि चार बरस में रिटायर होने वाले अग्निवीरों को कहां-कहां नौकरी दी जा सकेगी। एक-एक करके भाजपा राज्य इसकी घोषणा कर रहे हैं, और उन राज्यों का नाम लिए बिना देश के सबसे बड़े फौजी अफसर खौल रही नौजवान पीढ़ी को गैरफौजी बातें समझाने में लगे हुए हैं। बिना किसी अपवाद के तमाम विश्लेषक इस बात को लेकर भी सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि सरकारी और राजनीतिक बातों को सार्वजनिक रूप से समझाने के लिए फौज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और, तीनों सेनाओं के सबसे बड़े अफसरों की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में वर्दियों से यह तक कहलवा दिया गया कि अग्निपथ के खिलाफ आगजनी करवाने में कोचिंग सेंटरों का हाथ है जिन्होंने उन्हें फौजी बनवाने के लिए लाखों रूपए ले लिए थे। अब इतनी बात तो अब तक पुलिस भी किसी चार्जशीट में नहीं लिख पाई है, और ऐसी विवादास्पद और साबित न हुई बात फौज के सबसे बड़े अफसरों के मुंह से कहलवाई जा रही है।
यह पूरा सिलसिला एक खतरा खड़ा कर रहा है। फौज में आज सैनिकों का एक ही दर्जा है, उन सबके रिटायर होने की एक ही शर्तें हैं। लेकिन अग्निवीरों के पहुंचने के बाद वहां पर दो अलग-अलग तबके एक ही किस्म के काम में खड़े हो जाएंगे, कुछ तो अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर होंगे, और बाकी पूरी जिंदगी पेंशन और सहूलियतें पाएंगे, और दूसरा तबका उन अग्निवीरों का रहेगा जो चार साल बाद वहां से निकाल दिए जाएंगे, और फिर किसी इंडस्ट्री में या भाजपा कार्यालय में चौकीदार का काम करेंगे। इस तरह के चार बरस लोगों की जिंदगी में देश के लिए जान कुर्बान कर देने की कितनी प्रेरणा भर सकेंगे, यह अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है। और लोगों को यह शक है कि फौज के भीतर एक ही किस्म के काम के लिए, एक ही किस्म की वर्दी में इन दो किस्म के सैनिकों के बीच भेदभाव वहां के माहौल को खराब भी कर सकता है। दिक्कत यह है कि आज इस देश में सरकार की मर्जी से असहमति रखने को देशद्रोह करार दिया जा रहा है, और योग के नाम पर देश का एक सबसे बड़ा कारोबार खड़ा कर देने वाले रामदेव ने दो दिन पहले ही अग्निपथ के विरोधियों को देशद्रोही करार दिया है।
चूंकि सरकार अपनी इस योजना को हर कीमत पर पूरी तरह लागू करने पर आमादा है, इसलिए आज इस पर चर्चा की जरूरत फिर लग रही है। लोगों के अलग-अलग मंचों को इस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हमने मोदी सरकार के तमाम बड़े फैसलों को लागू होने के बाद जनता के दबाव में सुधरते भी देखा है, और किसान कानूनों की तरह वापस होते भी देखा है। कई फैसलों को बिना लागू हुए ताक पर रखे जाते भी देखा है। इसलिए चार बरस के ठेके पर नौजवानों को शहादत के जज्बे के लिए तैयार करने की सरकार की जिद पर लोगों को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध करना चाहिए, हो सकता है कि सरकार को खुद समझ में आए कि उसने जिद में गलत फैसला ले लिया है। यह देश मौजूदा सरकार का ही नहीं है, यह देश तमाम लोगों का है, और इसे सरकार के फैसलों पर सोचना चाहिए ताकि आने वाली पीढिय़ां उसे न भुगतें।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
अखबार की जिंदगी भी बड़ी अजीब रहती है, अक्सर ही पहले पन्ने पर जगह पाने के लिए खबरों में धक्का-मुक्की होती है, और अगर पहला पन्ना तैयार करने वाले लोगों को मेहनत से परहेज न हो, तो आखिरी पलों तक खबरें ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर होती रहती हैं। अब कल ही एक तरफ तो महाराष्ट्र की शिवसेना में अभूतपूर्व और बड़ी बगावत चल रही थी, सरकार गिरने के आसार दिख रहे थे, और दूसरी तरफ देश की विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक आकस्मिक एकता दिखाते हुए यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। और जैसा कि पहले से तय था, कुछ घंटों के बाद देश पर सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए की मुखिया भाजपा ने एक भूतपूर्व भाजपा विधायक, और राज्यपाल रह चुकीं द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद प्रत्याशी घोषित किया है। इन दोनों ही नामों के साथ कई तरह की चर्चा शुरू हुई, यशवंत सिन्हा भाजपा की अगुवाई वाली अटल सरकार में महत्वपूर्ण वित्तमंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं, लेकिन कल सुबह तक वे ममता बैनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में थे, और विपक्ष के संयुक्त सर्वसम्मत उम्मीदवार बनने के पहले उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दिया। यह बात जगजाहिर है कि ममता बैनर्जी और कांग्रेस के बीच एक अनबोला सा चल रहा है, और बड़ी तनातनी चल रही है, इस बीच में अगर ममता की पसंद को कांग्रेस खुलकर अपना पूरा समर्थन दे रही है, तो यह कल का एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था। और खासकर उन घंटों में यह सहमति या एकता नजर आई जब उन्हीं घंटों में महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर असहमति और फूट सुर्खियों में थी। राष्ट्रपति पद के लिए दो उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, लेकिन विधायकों और सांसदों के बहुमत से चुने जाने वाले राष्ट्रपति के लिए आज आंकड़े किसके साथ हैं, यह बात साफ है, और अब से राष्ट्रपति चुनाव मतदान तक हो सकता है कि शिवसेना के बहुत से विधायकों के वोट भी भाजपा उम्मीदवार के साथ चले जाएं।
लेकिन ये राजनीतिक घटनाक्रम अभी उतार-चढ़ाव से गुजर रहा है, और इस पर लिखने की अधिक जरूरत नहीं है। एक दूसरा मुद्दा जो इन्हीं सबके बीच से निकलकर आ रहा है, वह द्रौपदी मुर्मू का है। वे ओडिशा में सरकारी नौकरी में छोटी सी कुर्सी से उठकर वार्ड चुनाव लड़ते हुए विधायक बनी, और दो कार्यकाल विधायक रही, मंत्री भी रहीं। वे सिर्फ भाजपा में रहीं, और इस नाते 2015 में वे झारखंड की राज्यपाल बनाई गईं। वे ओडिशा की आदिवासी हैं, और देश के आदिवासी राज्य झारखंड में राज्यपाल रहीं, और अब उन्हें एक आदिवासी महिला के रूप में भाजपा ने अगला राष्ट्रपति बनाने का फैसला लिया है। उनका नाम सामने आने के बाद देश में यह चर्चा जोरों से चल रही है कि क्या एक आदिवासी महिला होने के नाते वे आदिवासियों या महिलाओं की हिफाजत के लिए कुछ कर पाएंगी, या फिर वे मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरह होकर रह जाएंगी जो एक दलित होने के नाते इस पद पर लाए गए थे, और जिनके कार्यकाल के दौरान देश के दलितों ने खूब जुल्म झेले हैं, और राष्ट्रपति की तरफ से हमदर्दी के कुछ शब्द भी नहीं आए। अब सोशल मीडिया इस बात पर उबला पड़ा है कि द्रौपदी मुर्मू जब झारखंड की राज्यपाल रहीं उस दौरान वहां आदिवासियों पर खूब जुल्म हुए, सरकारी फैसले आदिवासियों के खिलाफ लिए गए, लेकिन राजभवन में रहते हुए उन्होंने इनमें से किसी बात का विरोध नहीं किया।
अब राष्ट्रपति बनाते वक्त किसी तबके को महत्व देने, या किसी तबके को संतुष्ट करने की बात तो ठीक हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद क्या ऐसे लोग अपने तबके का कोई भला कर पाते हैं? या क्या उन्हें अपने तबके का अलग से कोई भला करना चाहिए? जो ओहदा देश की संवैधानिक व्यवस्था में सबसे ऊपर बनाया गया है, और जिसकी हकीकत भी सब जानते हैं कि यह ओहदा मोटेतौर पर केन्द्र सरकार का चेहरा देखकर काम करता है, उस ओहदे पर किसी को किस उम्मीद के साथ बिठाया जाता है? यह बात तो साफ है कि जिस तरह ज्ञानी जैलसिंह अपने पूरे कार्यकाल प्रधानमंत्री राजीव गांधी से नापसंदगी से देश में एक अनिश्चितता बनाए हुए थे, वैसा राष्ट्रपति तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। सरकार तो आमतौर पर फखरूद्दीन अली अहमद किस्म का राष्ट्रपति चाहेगी जिससे आपातकाल की घोषणा पर आधी रात को दस्तखत करवा लिए गए थे। इसलिए किसी भी सरकार से राष्ट्रपति को अधिकार देने की उम्मीद करना फिजूल की बात है।
अब सवाल यह उठता है कि अगर प्रचलित जनधारणा के मुताबिक राष्ट्रपति केन्द्र सरकार की रबर स्टैम्प ही है, तो किसी भी ईमानदार और इज्जतदार व्यक्ति को रबर स्टैम्प क्यों बनना चाहिए? और जहां तक संवैधानिक सीमाओं की बात है, तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था में भी राष्ट्रपति के लिए बहुत सी बातें मुमकिन हैं। राष्ट्रपति देश के हालात पर अपनी बात कह सकते हैं, और उन्हें केन्द्र सरकार भी इससे नहीं रोक सकती। राष्ट्रपति कोई इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई लेख लिख सकते हैं, सरकार के भेजे प्रस्तावों को रोककर देर कर सकते हैं, उन्हें कम से कम एक बार तो अपनी आपत्ति या सुझाव लगाकर वापिस भेज सकते हैं, लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति अपने इन संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, तो वे अपने को इस कुर्सी पर बिठाने वाले के प्रति वफादारी दिखाते हैं, या राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल पाने के लिए सरकार की सेवा करते हैं। जो एक बार इस ओहदे पर पहुंच गए, उन्हें हटाना तो आसान नहीं रहता, इसलिए उन्हें पांच बरस के एक कार्यकाल की सहूलियतों की तो गारंटी रहती है। इसके बाद भी अगर पुरानी वफादारी या आगे की उम्मीद न हो, तो यह रबर स्टॉम्प भी देश का भला कर सकता है, सरकार के गलत कामों पर उसकी फजीहत कर सकता है। लेकिन ऐसे राष्ट्रपति पहली बात तो बनाए नहीं जाते, और दूसरी बात यह कि बनने के बाद वैसे रह नहीं जाते। इसलिए देश के सबसे बड़े संवैधानिक ओहदे का लगभग हमेशा ही बेजा इस्तेमाल होते आया है, पुरानी वफादारी और शुक्रगुजारी दिखाने के लिए, या दूसरे कार्यकाल की उम्मीद के लिए। ऐसे में अगर कोई राष्ट्रपति केन्द्र सरकार या देश की किसी सरकार के असंवैधानिक कामकाज को देखते हुए भी उसे अनदेखा करते हैं, तो वे हौसले की कमी, और निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं, या फिर ऐसा इसलिए भी कर सकते हैं कि उनकी कुछ कमजोर बातें सरकार के हाथ हों।
आज एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने की संभावनाओं से न तो आदिवासियों के खुश होने की कोई बात है, और न ही महिलाओं के खुश होने की। इन दोनों के खिलाफ देश भर में पिछले बरसों में जो माहौल बना हुआ था, उसमें राज्यपाल रहते हुए भी, और उसके बाद भी उन्होंने मुंह खोला हो, ऐसा याद नहीं पड़ता। इसलिए उनके आने से देश के आदिवासी समुदाय में उत्साह की कोई वजह नहीं है, और न ही महिलाओं में उत्साह की। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करेंगी, या वफादारी और उम्मीद के साथ वक्त काटेंगी। भारत के राष्ट्रपति पद को गैरजरूरी महत्व नहीं देना चाहिए, यह समारोहों के लिए बनाया गया दिखावे का एक ओहदा है, जिस पर बैठे लोगों के सामने इस पसंद का मौका रहता है कि वे चाहें तो असर डाल सकते हैं।
मुम्बई की एक रिपोर्ट है कि 2021 में वहां नए जन्म का रजिस्ट्रेशन कोरोना के पहले के बरस 2019 के मुकाबले 24 फीसदी गिर गया है। 2019 में 1 लाख 48 हजार से अधिक जन्म रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो 2020 में गिरकर 1 लाख 20 हजार हो गया, अब 2021 में वह कुल 1 लाख 13 हजार रह गया है। इसकी एक बड़ी वजह मुम्बई में बाहर से आकर काम करने वाले लोगों का लॉकडाउन के दौरान अपने गांव लौट जाना रहा, और उसके बाद से अब तक वे सारे लोग काम पर लौटे नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो काम मुम्बई में हासिल था, वह अपने गांव या कस्बे में मिल रहा होगा, लेकिन लॉकडाउन के दौरान महानगरों से जो हौसला टूटा, तो वह फिर जुड़ नहीं पाया। ऐसा भी देखा गया है कि मजदूर अगर लौटकर आ भी गए हैं, तो भी उनके परिवार नहीं लौटे हैं, और नतीजा यह है कि अगर उनमें नई संतान होती भी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कहीं और हुआ होगा। लोगों को लगा कि मुसीबत के वक्त न मालिक काम आए, न महानगर।
ऐसे कामगारों के अलावा जानकारों का यह भी अंदाज है कि मुम्बई में जन्म घटने के पीछे लोगों पर छाई हुई आर्थिक अनिश्चितता भी एक वजह थी। मंदी छाई हुई थी, लोगों को यह समझ नहीं पड़ रहा था कि कोई भी नया खर्च वे कैसे उठाएंगे, और अस्पतालों के नाम से दहशत हो रही थी। ऐसे में बीमारी और बदहाली से घिरे हुए लोगों ने चाहे-अनचाहे यह समझदारी दिखाई कि ऐसे दौर में परिवार नहीं बढ़ाए। जबकि खतरा यह था कि महीनों तक घर बैठे हुए लोग आबादी बढ़ा सकते थे, लेकिन वह नौबत नहीं आई। हो सकता है कि पूरे देश के ऐसे आंकड़े कुछ और तस्वीर दिखाएं क्योंकि पूरा देश तो महानगर मुम्बई है नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि देश की बड़ी आबादी ने आज की आर्थिक हकीकत का अहसास करते हुए यह समझ लिया है कि नए मुंह और पेट तुरंत कमाने वाले नए हाथ लेकर नहीं आने वाले हैं, और इसलिए अच्छे कहे जाने वाले दो बच्चों का भी यह शायद सही वक्त नहीं है।
अभी आबादी के आंकड़ों को लेकर तो हम अधिक विश्लेषण करना नहीं चाहते क्योंकि पूरे देश के आंकड़े सामने भी नहीं हैं, और कोरोना-लॉकडाउन के इस दौर को लेकर अधिक अटकल भी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि हिन्दुस्तान में आज जिंदा रहना जितना महंगा हो गया है, पढ़ाई और इलाज जिस तरह लोगों की पहुंच के बाहर होते चल रहा है, रोजगार सिमटते चल रहे हैं, इन सबको देखते हुए लोगों को पहले कमाई की गारंटी करनी चाहिए, उसके बाद ही शादी या नए परिवार जैसे खर्च बढ़ाने चाहिए। आज परिवार को बढ़ाना एक दिन का खर्च नहीं है, जन्म और अस्पताल का बिल तो एक बार ही जुट सकता है, लेकिन नई जिंदगी का रोजाना का खर्च, और किसी परेशानी के वक्त अचानक आने वाला खर्च जुटाना आज अधिकतर लोगों की पहुंच के बाहर हो चुका है। आज एक बार फिर अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में लिखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सेना से चार बरस बाद रिटायर कर दिए जाने वाले अग्निवीरों को केन्द्रीय सुरक्षा बलों, राज्य सरकारों, या निजी कंपनियों में नौकरी देने का भरोसा या गारंटी उस वक्त बेमायने लगते हैं जब यह दिखता है कि सरकारी से लेकर निजी क्षेत्र तक लगातार नौकरियों की कटौतियां चल रही हैं, सरकारों में लाखों कुर्सियां सोच-समझकर खाली रखी गई हैं, ताकि तनख्वाह का बोझ घट सके। यह नौबत न तो अग्निपथ से सुधरने वाली है, न ही अधिक बिगडऩे वाली है। इसलिए लोगों को परेशानी से जूझने की अपनी क्षमता पर अधिक भरोसा करना चाहिए, अच्छे दिन आने की उम्मीद पर कम भरोसा करना चाहिए।
लोगों को परिवार बढ़ाने से परे भी अपने खर्चों पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि आज जो कमाई है, वह कल जारी रह सकेगी इसकी कोई गारंटी नहीं हैं। दूसरी तरफ बढ़े हुए खर्च कम कर पाना आसान नहीं रहता, इस बात की तो गारंटी सी रहती है। भारत जैसे देश में सकल राष्ट्रीय उत्पादन के आंकड़े चाहे हौसला बहुत पस्त न करें, लेकिन यह याद रखने की जरूरत है कि इन आंकड़ों में मनरेगा मजदूरों से लेकर अडानी-अंबानी की कमाई के, उत्पादन के आंकड़े भी शामिल हैं। और आज देश में कमाई का जो अनुपातहीन बंटवारा है, उसमें अडानी-अंबानी की दोगुनी होती दौलत और कई गुना बढ़ती कमाई के आंकड़ों से देश के गरीब और मध्यम वर्ग को खुश होने की जरूरत नहीं है। आने वाला वक्त इससे और अधिक कड़ा हो सकता है, और लोगों को न सिर्फ अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हुनर के बाजार में उनकी कद्र बनी रहे, बल्कि उन्हें लगातार अपने खर्चों पर काबू भी रखना चाहिए। अभी पूरी दुनिया में आसमान पर पहुंच रही महंगाई के कम होने का आसार नहीं दिख रहा है, और लोगों को खर्च घटाते जाने की कोशिश भी करनी चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
आज देश में कांग्रेस पार्टी से परे बाकी तमाम लोगों के लिए सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी की बात कुछ अलग है, उसके नए संचार प्रमुख, राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने कल ही ट्वीट किया है कि आज 20 जून का देश भर का कांग्रेस का प्रदर्शन अग्निपथ के खिलाफ और राहुल गांधी पर केन्द्रित प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ रहेगा। आज जब देश की बहुत सी पार्टियां और संगठन अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस व्यापक मुद्दे से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को जोडक़र अग्निपथ के महत्व को घटाने के अलावा और कुछ नहीं कर रही। खैर, जयराम रमेश आज अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो कि अपने बयान से आज अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय ने कल वीडियो कैमरों के सामने जिस तरह यह बात कही कि अग्निपथ से भर्ती होने वाले सैनिक रिटायर होने के बाद भाजपा कार्यालय के सुरक्षाकर्मी बनने में प्राथमिकता पाएंगे, वह बात उनकी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान कर गई है, और भाजपा की अगुवाई वाली मोदी सरकार जो जनधारणा प्रबंधन करना चाह रही थी, कैलाश विजयवर्गीय ने उस कोशिश को मानो लात ही मार दी। दूसरी तरफ कल ही केन्द्र सरकार के एक मंत्री, जी.किशन रेड्डी ने औपचारिक प्रेस कांफ्रेंस में यह कहा कि अग्निवीरों को सेना से निकलने के बाद काम की कमी नहीं रहेगी क्योंकि उन्हें ड्राइवरी, बिजली मिस्त्री का काम, नाई और धोबी का काम सिखाया जाएगा। फिर मानो भाजपा इस तरह की बातों में आगे न निकल जाए इसलिए कांग्रेस के एक एमएलए इरफान अंसारी अपनी बेवकूफी की बातों के साथ दो दिनों से समाचार बुलेटिनों पर छाए हुए हैं, और अभी उनका यह बयान बार-बार दिखाया जा रहा है कि चार साल सैनिक रहकर निकले हुए लोग बाहर आकर हथियार उठा लेंगे, और सडक़ों पर खून-खराबा होगा। जिस तरह अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नौजवान भीड़ सडक़ों और पटरियों पर हिंसा कर रही है, कुछ उसी किस्म की हिंसा अलग-अलग पार्टियों के नेता कैमरा और माईक देखते ही कर रहे हैं, और लापरवाही और गैरजिम्मेदारी से बकवास करते हुए ये लोग अपनी खुद की पार्टी या अपनी खुद की सरकार को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
लोगों को याद होगा कि अभी दो हफ्ते ही गुजरे हैं जब भाजपा के दो प्रवक्ताओं ने पार्टी को एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक मुसीबत में डाला है, और अपनी पार्टी के साथ-साथ उन्होंने इस पूरे देश को भी दुनिया के बीच हिकारत के घेरे में डाल दिया है, और एकमुश्त तमाम मुस्लिम देशों को भारत के आमने-सामने कर दिया है। उसके तुरंत बाद भी ऐसी अनौपचारिक खबर आई थी कि भाजपा के प्रवक्ता धर्म के मामलों पर नहीं बोलेंगे, कई और मुद्दों पर पार्टी के बड़े नेताओं से बात करने के बाद ही बोलेंगे, जिन्हें पार्टी ने अधिकृत किया है वे ही लोग टीवी चैनलों पर जाएंगे। इस अनौपचारिक खबर से ऐसा लगने लगा था कि अब भाजपा के प्रवक्ताओं की जुबान पर पार्टी की लगाम रहेगी। लेकिन जब कोई केन्द्रीय मंत्री, या कैलाश विजयवर्गीय सरीखे बड़े नेता किसी जलते-सुलगते मुद्दे पर ऐसे लापरवाही के शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो यह समझ आता है कि पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं पर पार्टी का कोई बस नहीं है। यही हाल दूसरी कई पार्टियों के बारे में भी कहा जा सकता है, और आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपनी सुनाई अपने बचपन की कहानियों को लेकर उनकी आलोचना के साथ-साथ उनकी मां का भी जिस तरह का मजाक बनाया जा रहा है, उस पर भी कोई पार्टी अपने लोगों को कोई जिम्मेदारी सिखाते नहीं दिख रही है, क्योंकि हर पार्टी के पास भाजपा के कई नेताओं के इससे भी बुरे बयानों की मिसालें कायम हैं, और जुबानी गिरावट का यह सिलसिला बेधडक़ आगे बढ़ते चल रहा है।
आज अग्निवीरों को लेकर एक तरफ तो फौजी वर्दी पहने हुए बड़े अफसर मीडिया के सामने आकर उन्हें अपनी बराबरी का सैनिक बता रहे हैं, अपने बगल में सुला रहे हैं, अपने से किसी मायने में कम नहीं बता रहे हैं, और ऐसा करके वे सरकार की शांति कायम करने की नीयत का साथ दे रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार के ही हिमायती लोग तरह-तरह से इन अग्निवीरों को मनरेगा मजदूरों से बेहतर गिनाकर लोगों को यह तुलना करने पर मजबूर कर रहे हैं कि अग्निवीर मनरेगा मजदूरों से तो बेहतर ही रहेंगे। सरकार के हिमायती इन लोगों को यह भी समझ नहीं है कि मनरेगा मजदूर सरहद पर जान कुर्बान करने के लिए नहीं जाते हैं, अपने गांव के बगल ही मिट्टी खोदते हैं। देश का सिलसिला कुछ तो सोशल मीडिया की मेहरबानी से, और कुछ बाकी मीडिया की मेहरबानी से भी इतना बिगड़ चुका है कि अब लोग सेना भर्ती के तरीके पर उठाए सवालों को सेना को कमजोर करने की साजिश कह रहे हैं, दुश्मन देश की सेना को मजबूत करने की साजिश कह रहे हैं। जिसके मुंह में जो आ रहा है वह कहे जा रहे हैं, और जो बात जितनी अधिक अटपटी है, जितनी अधिक खटकने वाली है, वह मीडिया में उतनी ही अधिक अहमियत भी पा रही है। ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया, और मीडिया भी, लोकतंत्र का बड़ा औजार माने जाते हैं, वे एक ऐसी लाठी बन गए हैं जिसे घुमा-घुमाकर लोकतंत्र के टुकड़े किए जा रहे हैं।
आज हर मोबाइल फोन एक मीडिया संस्थान बन गया है, और हर नागरिक मीडियाकर्मी। ऐसे में रद्दी से रद्दी नेता को भी कई कैमरे नसीब हो जाते हैं, और सामने कैमरे देखकर, खबरों में आने की उनकी हसरत उमडऩे लगती है, और वे अपनी पार्टी या अपने संगठन का नुकसान भी करने की कीमत पर उटपटांग बोलने लगते हैं। कल तक मोदी सरकार के विरोधी यह कह रहे थे कि चार साल बाद फौज से निकलकर अग्निवीर दर्जे के सैनिक अडानी और अंबानी के सिक्यूरिटी गार्ड बन पाएंगे, कैलाश विजयवर्गीय ने चार कदम आगे बढक़र उन्हें भाजपा दफ्तर का सिक्यूरिटी गार्ड बना दिया। फिर मानो कैलाश विजयवर्गीय के मुकाबले केन्द्रीय मंत्री जी.किशन रेड्डी को हीनभावना होने लगी, तो उन्होंने रिटायर्ड अग्निवीरों को ड्राइवर, बिजली मिस्त्री, नाई और धोबी बना दिया। अब देश के दर्जनभर राज्यों में लगी हुई आग को बुझाने में लगी मोदी सरकार को उसके घर के चिरागों से ही आग लग रही है। बहुत सी दूसरी विपक्षी पार्टियों के पास जलने लायक कुछ बचा नहीं है, इसलिए उन्हें आज समझ नहीं आ रहा है कि उनके नेता और प्रवक्ता उनका क्या नुकसान कर रहे हैं। हिन्दुस्तान के मीडिया की दिक्कत यह हो गई है कि सोशल मीडिया के बीच जिंदा रहने के लिए उसे तरह-तरह से सोशल मीडिया की अराजकता से मुकाबला करना पड़ता है। फिर यह भी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने ग्राहकों की जरूरतों, और अपनी तकनीक की सीमाओं के चलते हुए चाहे-अनचाहे सनसनी पर ही जिंदा रहता है, और अधिक गैरजिम्मेदारी उसे अधिक कामयाब भी बनाती है।
इस पूरे दौर में राजनीतिक दलों को एक ही सहूलियत है कि उसके बकवासी नेताओं के मुकाबले दूसरी पार्टियों में भी बकवासी नेता हैं, और नुकसान किसी एक पार्टी का ही नहीं हो रहा है। लेकिन तमाम पार्टियों के नुकसान होने को राहत मानने वाली हिन्दुस्तानी राजनीति इस बात की तरफ से बेफिक्र और बेखबर है कि इससे हिन्दुस्तान की सार्वजनिक जीवन की हवा जहरीली होती चल रही है, और यहां पर अब कोई न्यायसंगत, तर्कसंगत संवाद मुमकिन नहीं रह गया है।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
अफगानिस्तान के काबुल में एक गुरुद्वारे पर आईएस के आतंकियों ने हमला किया। हमला बहुत बड़ा था, दर्जन भर से अधिक विस्फोट किए गए, हथगोलों और रायफलों से लैस आतंकी गुरुद्वारे के अंदर घुसे, और दो लोगों मार डाला। इसके बाद अफगानिस्तान के आज के शासक, तालिबान ने इन आईएस आतंकियों को मार गिराया। खबरें बताती हैं कि अफगानिस्तान में हाल ही में सिक्ख धर्मस्थलों पर यह पांचवां बड़ा हमला है, और इनमें से अधिकतर की जिम्मेदारी आईएस ने ली है। इस बार आईएस ने इस हमले के बाद यह बयान जारी किया है कि उसने हिन्दुस्तान में (भाजपा प्रवक्ता) नुपूर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर का अपमान करने के जवाब में यह हमला किया है। अफगानिस्तान के घरेलू हालात ऐसे हैं कि तालिबान का भी आईएस आतंकियों पर कोई बस चल नहीं रहा है, और आज दुनिया के सबसे कट्टर इस्लामी आतंकी समूहों में से एक, आईएस वहां जब तब हमले करते रहता है।
अफगानिस्तान के किसी आतंकी हमले या मुठभेड़ के बारे में यहां लिखने की कोई वजह नहीं बनती थी, लेकिन इस बार आईएस ने इस हमले के बाद जो बयान दिया है, वह हिन्दुस्तान के लिए फिक्र की बात है। हिन्दुस्तानी लोग दुनिया के अधिकतर देशों में बसे हुए हैं, और दुनिया का ऐसा कोई इस्लामी देश नहीं है जहां पर हिन्दुस्तानी न हों। ऐसे में हिन्दुस्तान ने इस्लाम पर किया हुआ कोई भी हमला कई देशों में हिन्दुस्तानियों को निशाना बना सकता है, और बनाता ही है। जो आतंकी हमले हैं वे तो दिख जाते हैं, लेकिन जो आर्थिक हमले होते हैं, वे आसानी से दिखते नहीं हैं। जब न्यूयार्क के वल्र्ड ट्रेड सेंटर की जुड़वां इमारतों पर ओसामा-बिन-लादेन के आतंकियों ने विमान टकराकर हमला किया था, तो उसके जवाब में पूरी दुनिया में ही मुस्लिमों को जगह-जगह आर्थिक बहिष्कार झेलना पड़ा था, और उनके कारोबार में बड़ी गिरावट आई थी। अभी भारत में धार्मिक कट्टरता, साम्प्रदायिकता, और असहिष्णुता का नुकसान दुनिया भर में हिन्दुस्तानियों को कई अघोषित तरीकों से हो रहा है। और जो लोग अपनी-अपनी बसाहट में दुनिया भर में ऐसा नुकसान झेल रहे हैं, वे भी खुलकर इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि यह सिलसिला और आगे न बढ़े।
यह पहले भी कई बार लिखा जा चुका है कि खाड़ी के देशों में दसियों लाख हिन्दुस्तानी काम करते हैं, और उनके घर भेजे गए पैसों से भारत की विदेशी मुद्रा की जरूरत भी पूरी होती है, और भारतीय घरेलू अर्थव्यवस्था भी उसकी वजह से आगे बढ़ती है। ऐसे में हिन्दुस्तान के जिन नफरतजीवियों को तरह-तरह के फतवे देना सूझता है, उन्हें इस बात का अहसास भी नहीं है, और इसकी फिक्र भी नहीं है कि दूसरे देशों में अल्पसंख्यक कामगार तबके के हिन्दुस्तानियों, और हिन्दुओं का क्या हाल होगा। जिन्हें अपने मुहल्ले से बाहर निकलना नहीं है, और सबसे करीब की सडक़ पर उत्पात करना है, सबसे पास की बस्तियों में आग लगानी है, उन्हें दूर बसे अपने ही धर्म के लोगों की फिक्र की बात भला कैसे सूझेगी, क्यों सूझेगी? नतीजा यह है कि दुनिया के माहौल से बेखबर और बेफिक्र ऐसे धर्मान्ध और साम्प्रदायिक लोग हिन्दुस्तान में आग लगाकर यहां तो खुद बच निकलने की गारंटी कर लेते हैं, लेकिन दूसरे देशों में हिन्दुस्तानी लोग उसका दाम चुकाते हैं।
आज हिन्दुस्तान में धर्मान्धता, और साम्प्रदायिकता की जो आंधी चल रही है, उस बीच लोगों को यह भी दिखाई नहीं दे रहा है कि एक देश के रूप में भारत की सभ्य दुनिया में कितनी बेइज्जती हो रही है। और न सिर्फ दूसरे देशों के पूंजीनिवेशकों ने हाल ही के हफ्तों में बहुत बड़ी रकम हिन्दुस्तान से निकाल ली है, बल्कि चीन के विकल्प के रूप में भारत को जो महत्व मिलना था वह भी कहीं आसपास दिख नहीं रहा है। कुछ लोगों को हिंसक हिन्दुस्तानियों के हाथों में झंडे-डंडों से इसका रिश्ता समझ नहीं आएगा, लेकिन साम्प्रदायिकता की आग में झोंके जा रहे देश में पूंजीनिवेश करने भी लोग बाहर से नहीं आएंगे। आबादी के बहुसंख्यक हिस्से को जब सत्ता की तरफ से हिफाजत मिल जाती है, तब उसके भीतर अगर साम्प्रदायिक हिंसा सुलगती रहती है, तो वह लपटों में बदलने में वक्त नहीं लगता। और ऐसी लपटों में सबसे पहले अर्थव्यवस्था आती है, इस देश में भी, और इस देश के बाहर बसे हिन्दुस्तानियों की भी।
आज अफगानिस्तान के एक सिक्ख गुरुद्वारे को भारत में भाजपा प्रवक्ताओं के बयानों की वजह से इस्लामी आतंकियों का हमला झेलना पड़ा है। सिक्खों का इन बयानों से भी कोई लेना-देना नहीं था, और तो और इन प्रवक्ताओं में भी कोई निजी हैसियत में सिक्ख नहीं थे, लेकिन हिन्दुस्तानी होने की वजह से सिक्खों ने वहां कुछ साम्प्रदायिक हिन्दुओं के फैलाए जहर के दाम चुकाए हैं, अपनी जिंदगियां खोई हैं, और गुरुद्वारे पर हमला झेला है। देश के भीतर जो लोग बढ़ाई जा रही साम्प्रदायिकता पर चुप हैं, वे यह बात समझ लें कि दुनिया भर में जगह-जगह हिन्दुस्तानी लोग इसके दाम चुका रहे हैं, चुकाते रहेंगे। हिन्दुस्तान में जो लोग इस आग को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनसे अफगानिस्तान के इस ताजा हमले को लेकर सवाल होने चाहिए कि यहां पर हिंसा फैलाते हुए क्या उन्हें दुनिया भर में बसे भारतवंशियों की फिक्र है?
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
एक बार फिर देश की मोदी सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना से बड़ा बवाल उठ खड़ा हुआ है। अग्निपथ योजना के तहत देश के नौजवान फौज में भर्ती होकर अग्निवीर बनने के पहले ही देश के आधा दर्जन राज्यों में प्रदर्शन करते हुए ट्रेन और बस में आग लगाने की वीरता दिखा रहे हैं। यह मामला बड़ा जटिल है, और हम देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई इस फौजी नीति में आमूलचूल बदलाव का अतिसरलीकरण करना भी नहीं चाहते। लेकिन अलग-अलग जानकार लोगों की कही हुई, और लिखी हुई जो बातें अब तक सामने आई हैं, वे हैरान करती हैं कि क्या मोदी सरकार सचमुच ही बिना काफी सोच-विचार के ऐसा फैसला ले सकती है? आज देश में दस करोड़ से अधिक बेरोजगार हैं, इनमें फौज में जाने की हसरत रखने वाले करोड़ों नौजवान हैं, इनमें से लाखों ऐसे हैं जो पिछले पांच-दस बरस से इसकी तैयारी कर रहे हैं, और आज उन्हें पता लग रहा है कि उनके लिए खुल रही नौकरी कुल चार बरस की है, और इन चार बरसों के बाद न उन्हें पेंशन रहेगी, न उनको भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली किसी भी तरह की सहूलियत रहेगी, तो ऐसे बेरोजगार नौजवान आपा खोकर आग लगाते सडक़ों और पटरियों पर हैं।
केन्द्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर सरकार से बाहर के लोगों के मन में अनगिनत आशंकाएं हैं। इनमें से एक आशंका कांग्रेस पार्टी ने खुलकर सामने रखी हैं कि चार बरस हथियारबंद ट्रेनिंग और काम के बाद जब ये नौजवान एकदम से बेरोजगार होकर पच्चीस बरस की उम्र में फिर काम तलाशेंगे, तो हथियारों की उनकी ट्रेनिंग उन्हें गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। यह आशंका कांग्रेस से परे भी बहुत से लोगों ने जाहिर की है, और दुनिया के कई दूसरे देशों का ऐसा तजुर्बा भी है कि सेना से निकले हुए ऐसे ठेके के सैनिक बिना किसी सरकारी सहूलियत और बंदिश के निजी कारोबारी सैनिक बन जाते हैं, और कहीं वे बड़ी कंपनियों के लिए दूसरे देशों में हथियारबंद काम करते हैं, तो कहीं किसी देश में जंग में भाड़े पर काम करते हैं। रूस की ऐसी ही एक निजी सेना के लोग इन दिनों यूक्रेन में काम कर रहे हैं, और भाड़े पर कत्ल कर रहे हैं, और वागनर ग्रुप नाम की यह प्राइवेट मिलिट्री पहले सीरिया में भी काम कर चुकी है।
कुछ लोगों की यह खुली आशंका है कि आज हिन्दुस्तान में निजी कंपनियां जितनी विकराल होती जा रही हैं, उन्हें अगले बरसों में अपने होने वाले और अधिक विस्तार की हिफाजत के लिए निजी सेना की जरूरत पड़ेगी, और प्राइवेट सिक्यूरिटी के नाम पर उन्हें ऐसे हथियार-प्रशिक्षित लोग लगेंगे, और चार बरस में हिन्दुस्तानी फौज से रिटायर होने वाले ऐसे लोग ऐसी निजी सुरक्षा वर्दियों के लिए तैयार रहेंगे। लोगों ने इस सिलसिले में देश की एक सबसे बड़ी कंपनी की निजी सिक्यूरिटी एजेंसी का नाम भी गिना दिया है कि शायद उसी की भर्ती के लिए हिन्दुस्तानी फौज के रास्ते यह रास्ता निकाला जा रहा है।
एक दूसरी आशंका जो बहुत बड़ी है वह देश के एक रिटायर फौजी जनरल ने गिनाई है, और कुछ गैरफौजी जानकार लोगों ने भी। उनका कहना है कि अग्निपथ के रास्ते अग्निवीरों की नियुक्ति में देश के किसी इलाके के लिए कोई कोटा नहीं रहेगा, किसी तबके का कोई आरक्षण नहीं रहेगा, और भारतीय सेना में हमेशा से चली आ रही लड़ाकू और योद्धा जातियों के आधार पर बनी हुई रेजिमेंट नहीं रहेंगी। पूरे देश से जब एक साथ सेलेक्शन की जब एक लिस्ट बनेगी, तो यह भी मुमकिन है कि उसके अधिकतर लोग दो-चार राज्यों के ही हों। और फौज की इस तरह बदलती हुई शक्ल से राष्ट्रीय एकता पर किस तरह का असर पड़ेगा, इसका अंदाज लगाना अभी नामुमकिन है। लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों से फौज में भर्ती के लिए जो कोटा रखा जाता था, वह इस अग्निपथ-अग्निवीर में खत्म कर दिया गया है, और फौज के बड़े जानकार लोग इसे एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। इस देश की राष्ट्रीय एकता की इस तरह की अनदेखी बहुत लंबे समय में जाकर भारी पड़ सकती हैं क्योंकि हिन्दुस्तानी फौज आज धर्म और साम्प्रदायिकता से परे, जाति और क्षेत्रीयता से परे, राष्ट्रीय एकता की एक बड़ी मिसाल है, जिसका कि बिगडऩा शुरू होगा, तो एक-दो पीढ़ी बाद उसका नुकसान और खतरा पता चलेगा।
आज हिन्दुस्तानी फौज में जाकर देश के लिए जान कुर्बान करने का जज्बा सस्ते में नहीं आता है। सैनिकों को यह मालूम रहता है कि उनकी नौकरी के बाद इस देश की सरकार उनके परिवार को पेंशन, इलाज, रियायती सामान जैसी अनगिनत सहूलियतें देगी, उनके रिटायरमेंट के बाद उनके पुनर्वास के लिए तरह-तरह की योजनाएं रहेंगी, और उनके परिवार का भविष्य बुनियादी जरूरतों के लिए हिफाजत से रहेगा। आज चार बरस के अग्निवीर पांचवें बरस में किसी कंपनी के सिक्यूरिटी गार्ड बन जाएं तो बहुत रहेगा, न उनके हाथ पेंशन रहेगी, न इलाज, न बच्चों की पढ़ाई, न और कुछ। और इन्हीं चार बरसों में देश के लिए कुर्बान होने का मौका आने पर उनसे कुर्बानी की उम्मीद भी की जाएगी। मतलब यह कि वे अपनी जवानी के बेहतरीन बरस देश पर कुर्बान होने को तैयार रहें, खतरा उठाएं, और चार बरस बाद रिटायर होकर किसी कारखाने के गार्ड बन जाएं, या एटीएम की चौकीदारी करें। इनमें से कोई रोजगार खराब नहीं है, लेकिन ऐसे रोजगार के लिए कोई देश पर कुर्बानी का जज्बा जुटा पाएंगे, यह उम्मीद करना कुछ ज्यादती होगी।
इस योजना की घोषणा के दो दिन के भीतर, और दो दर्जन आगजनी के बाद इसमें भर्ती की उम्र में दो बरस की ढील घोषित की गई है। हैरानी की बात यह है कि मोदी मंत्रिमंडल में आज मंत्री, और रिटायर्ड थलसेनाध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह ने मीडिया के वीडियो कैमरे के सामने यह बात कही कि उन्हें इस योजना के बारे में कुछ नहीं पता है, वे इसे तैयार करने वाले लोगों में नहीं थे, उन्हें इसके बारे में मालूम नहीं है। अब अगर केन्द्रीय मंत्रिमंडल के इतने बड़े एक भूतपूर्व फौजी से ही इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, और जैसा कि सारे जानकार लोग बता रहे हैं कि फौजी भर्ती में आमूलचूल फेरबदल का कोई पायलट प्रोजेक्ट भी नहीं बना, तो ऐसा लगता है कि यह नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून, नागरिकता कानून सरीखा ही एक और बिना तैयारी का फैसला है जिसमें मौजूदा विशेषज्ञों की राय भी नहीं ली गई है। यह सिलसिला इस देश की इतनी पुरानी फौज के लिए भी ठीक नहीं है, और उसी वजह से वह देश की हिफाजत के लिए भी ठीक नहीं है। संसद में बहुमत वाली सरकारें हर किस्म का फैसला लेने की ताकत रखती हैं, लेकिन जब सरकारें कई फैसले महज इसलिए लेने लगती हैं कि वे उन्हें लेने की ताकत रखती हैं, तो ये फैसले देश के खिलाफ भी हो सकते हैं, और सरकारों के खुद के खिलाफ भी।
आज करोड़ों बेरोजगारों के देश में दस लाख नई नौकरियों की उम्मीद से जश्न का माहौल रहना था, लेकिन आज केन्द्र सरकार के भागीदारों से परे कोई भी इसका हिमायती नहीं दिख रहा है। एक रिटायर्ड मेजर जनरल जी.डी. बक्शी जो कि आए दिन टीवी पर आग उगलते दिखते हैं, और मोदी सरकार के एक बड़े प्रवक्ता की तरह काम करते हैं, उन्होंने कहा है कि अग्निपथ स्कीम के बाद पीढिय़ों से फौज में जा रहे लोगों का सामाजिक ताना-बाना बिखर जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि चार साल में एक साल तो छुट्टी में मेडिकल में ही चला जाएगा, तीन साल में जवान मोर्चे पर क्या जंग लड़ेगा? चार साल के बाद जब सैनिक लौटेगा, और उसे काम नहीं मिलेगा तो वह मुजरिम ही बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय सेना का रेजिमेंटल सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा।
हम अभी अग्निपथ योजना से फौज को होने वाले नफे और नुकसान पर अपनी तरफ से कोई नतीजा नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन जानकार लोगों की कही बातों से जो नतीजे निकल रहे हैं, उनमें से कुछ बातों को सामने रख रहे हैं। देश को इस बारे में और सोचने की जरूरत है, और सरकार को इस फैसले को स्थगित रखना चाहिए, यह देश को एक अलग तरीके से धीरे-धीरे विभाजित करने वाला फैसला हो सकता है, और कई तरह से खतरे में डालने वाला फैसला भी। आज इसे लेकर देश भर में जो उपद्रव चल रहा है, उसमें बेरोजगार नौजवानों से शांत रहने की हमारी अपील का क्या कोई मतलब होगा, जब देश के प्रधानमंत्री ही किसी भी हिंसक उपद्रव पर शांत रहने की अपील नहीं कर पा रहे हैं?
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
महाराष्ट्र के प्रमुख मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, आज के केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कुछ बातें हैं जो उन्हें किसी भी दूसरे केन्द्रीय मंत्री से अलग दिखाती हैं। वे लगातार अपने विभाग के तहत सडक़-पुल बनाने, ट्रैफिक सुधारने, गाडिय़ों को पेट्रोल-डीजल से बैटरी की तरफ ले जाने की सकारात्मक बातें करते हैं। उनकी तमाम बातों से ऐसा लगता है कि वे देश में फैले हुए नफरत के सैलाब से अनछुए रहकर अपनी बैटरी कार पर सवार, अपने बनाए हुए हाईवे पर आगे बढ़ते चले जाना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वे अपनी पार्टी और सरकार की राजनीति के खिलाफ हैं, लेकिन जनता के बीच कही उनकी बातें उन्हें एक अलग तरह का सम्मान दिलाने वाली रहती हैं और लोगों को यह भरोसा दिलाने वाली भी रहती हैं कि उनके विभाग के तहत होने वाला काम लोगों को सचमुच अच्छे दिन दिखा सकता है।
अभी नितिन गडकरी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यह कहा कि सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके बाद लोग अगर गलत खड़ी की हुई गाड़ी की फोटो भेजेंगे, और उस पर हजार रूपए से अधिक का जुर्माना बनेगा, तो उस पर पांच सौ रूपए का ईनाम उन्हें मिल सकेगा। उनका कहना है कि इससे गलत पार्किंग खत्म हो जाएगी। उन्होंने इस पर भी अफसोस जाहिर किया कि लोग गाडिय़ां तो ले लेते हैं, लेकिन उनके पास पार्किंग की जगह नहीं रहती। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हमने बरसों पहले इसी तरह की बात अपने इलाके की पुलिस को सुझाई थी कि उसे अखबारों के फोटोग्राफरों से अपील करनी चाहिए कि सडक़ों पर ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों की फोटो खींचकर भेजें, और उस पर जुर्माना होने पर उसका एक हिस्सा फोटोग्राफर को भी मिलेगा। उस वक्त सडक़ों पर अखबारी-फोटोग्राफर ही अधिक रहते थे, और उस वक्त मोबाइल फोन-कैमरों का चलन नहीं था। लेकिन अब तो हर हाथ में एक कैमरा है, और अगर स्थानीय पुलिस चाहे तो वह अपने वॉट्सऐप नंबर, ईमेल एड्रेस, और सोशल मीडिया पेज तैयार कर सकती है जहां पर राह चलते लोग भी ऐसे फोटो-वीडियो भेजें, और उन पर जुर्माना होने पर उसका एक हिस्सा शिकायतकर्ता को भी मिले। आज पूरे हिन्दुस्तान में फौज में भर्ती की नई योजना, अग्निपथ, के खिलाफ जगह-जगह प्रदर्शन हो रहा है, रेलगाडिय़ां जलाई जा रही हैं, लेकिन ट्रैफिक की शिकायत की ऐसी सडक़पथ योजना बनाकर ट्रैफिकवीरों से फोटो-वीडियो बुलवाने और ईनाम देने से वह सुधार हो सकेगा जो कि पुलिस अपने अमले को दस गुना करके भी नहीं कर सकती।
किसी भी सभ्य समाज में नियमों को लागू करना और करवाना हर किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज देश की अराजक आबादी से पूरे नियम पालन करवाना हो तो दस गुना पुलिस भी कारगर नहीं होगी। और हर पुलिस सिपाही का खर्च तो जनता पर ही आता है। इसलिए जिस तरह सफाई अभियान में लोगों को जोडऩे वाली म्युनिसिपलें अधिक कामयाब होती हैं, उसी तरह ट्रैफिक सुधारने की मुहिम में जो प्रदेश या शहर अपने लोगों को उसमें भागीदार बनाएंगे, वे सरकारी खर्च बढ़ाने के बजाय सरकारी कमाई बढ़ाएंगे, और लोगों के बीच भी बिना वर्दी देखे नियमों का सम्मान रहेगा। आज तो जहां पुलिस के दिखने का खतरा न हो, वहां लोग अपनी मर्जी के मालिक रहते हैं, और सडक़ों के मवाली भी। यह नौबत बदलने के लिए जनभागीदारी की नितिन गडकरी की आज की सोच हम दस-पन्द्रह बरस पहले लिख चुके हैं, और उसके लिए राज्य सरकार को एक मामूली सा नियम बनाना पड़ेगा। आज भी ट्रैफिक चालान की कमाई राज्य के खजाने में ही जाती है, और अगर उसका एक हिस्सा लोगों को ईनाम में दिया जाता है, तो उसमें केन्द्र सरकार से किसी इजाजत की जरूरत भी नहीं है। राज्य सरकार अपने स्तर पर पहल करके अपने नागरिकों को ट्रैफिक सुधारने की इस मुहिम में लगा सकती हैं, और हर हाथ में मोबाइल फोन होने से इसकी कामयाबी भी तय है। यह जरूर हो सकता है कि ट्रैफिक से जुड़े हुए सरकारी महकमों के संगठित भ्रष्टाचार के एकाधिकार पर इससे चोट पहुंच सकती है, लेकिन वह भ्रष्टाचार लोगों की जिंदगी की कीमत पर चलता है, जिसे कि बंद किया जाना चाहिए।
शहरी जिंदगी में बच्चों को कोई भी नियम सिखाने की पहली शुरुआत ट्रैफिक से होती है, और जब वे ट्रैफिक के नियम तोड़े जाते देखते हैं, वे खुद भी वैसा ही करना सीख जाते हैं, और फिर धीरे-धीरे किसी भी नियम के लिए उनके मन में हिकारत घर कर जाती है। ऐसी अराजक सोच सरकार के लिए आगे कई किस्म के जुर्म पेश करती हैं, और देश की बहुत सी पुलिस, बहुत सी अदालतें इसी से जूझते रह जाती हैं। इसलिए ट्रैफिक सुधारना बच्चों को नियमों का सम्मान सिखाने का पहला पाठ रहता है। एक सभ्य देश की आसान सी पहचान यही रहती है कि वहां का ट्रैफिक नियमों का कितना सम्मान करता है। बिना राजनीतिक पसंद या प्रतिरोध के, नितिन गडकरी की सोच को राज्यों को अपने स्तर पर लागू करना चाहिए, चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश इस अखबार के लिखे शुरू न हुई, तो भी कोई बात नहीं, गडकरी के कहे हुए शुरू हो जानी चाहिए। यह भी हो सकता है कि कई बेरोजगार अपने मामूली से मोबाइल फोन के कैमरे से दिन भर में हजार-दो हजार रूपए कमाने का एक रास्ता निकाल लें, और उन्हें अग्निपथ के मुकाबले चालानपथ एक बेहतर कॅरियर लगने लगें।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
दो दिन पहले झारखंड के राज्यपाल, देश के सबसे सीनियर सांसद रह चुके रमेश बैस की तरफ से मीडिया को भेजी गई एक जानकारी में बताया गया था कि रांची के राजभवन में उन्होंने पुलिस के बड़े अफसरों को बुलाकर रांची में दस जून और उसके बाद हुई घटनाओं के बारे में खुलासे से जानकारी ली थी। दस जून के वहां के प्रदर्शन में पुलिस गोली से दो मौतें हुई थीं, और उस बारे में राज्यपाल ने पूछा था कि इतनी हिंसा को रोकने के लिए पहले से बचाव की कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? पुलिस की तैयारी क्यों नहीं थी? उन्होंने अफसरों से यह भी कहा था कि प्रदर्शन करने वाले लोगों और गिरफ्तार लोगों की तस्वीरों को नाम-पते के साथ देकर शहर के प्रमुख जगहों पर होर्डिंग लगाए जाएं ताकि जनता उन्हें पहचान सके। अब राज्यपाल की तरफ से ही मीडिया को बैठक की भेजी गई इस जानकारी के बाद रांची पुलिस ने ऐसे होर्डिंग बनाकर जारी किए थे जिनमें उपद्रव करते लोगों के चेहरे दिख रहे थे, और उन्हें पहचान कर उनके बारे में पुलिस को खबर करने की अपील की गई थी। लेकिन पुलिस ने इसके बाद प्रेस नोट जारी किया कि इन वांछित उपद्रवियों के फोटो में संशोधन करने के लिए उसे वापिस लिया जा रहा है। इसके पहले झारखंड सरकार के गृहसचिव की रांची एसएसपी को लिखी एक चिट्ठी सामने आती है जिसमें कहा गया है ऐसी तस्वीरों के पोस्टर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ है, और इस बारे में स्पष्टीकरण दें। जाहिर है कि झारखंड में देश के एक सबसे वरिष्ठ भाजपा सांसद रहे, और अब राज्यपाल, रमेश बैस के निर्देशों पर काम कर रही पुलिस अपनी ही सरकार के निशाने पर आ गई है। राज्यपाल की तरफ से मीडिया को अफसरों संग उनकी बैठक की जो जानकारी भेजी गई थी, उसमें यह बात साफ थी कि उन्होंने ऐसे होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए हैं।
ऐसे होर्डिंग लगाने के खिलाफ दाखिल एक जनहित याचिका में दो बरस पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साफ-साफ एक आदेश दिया था। उत्तरप्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सार्वजनिक प्रदर्शनों में उपद्रव करने के कथित आरोपियों की तस्वीरों, और उनके नाम-पते के साथ होर्डिंग लगाए थे, जिनमें कई शांतिपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम-फोटो भी लगाए गए थे। इस मामले में वहां के हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। भारत की न्याय व्यवस्था के मुताबिक समान किस्म के मामलों में दूसरे प्रदेशों में भी किसी दूसरे प्रदेश के हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला दिया जाता है, और झारखंड सरकार ने ऐसे ही एक हवाले के साथ राजधानी के एसएसपी को दिए नोटिस में इसका जिक्र किया है, जो कि चि_ी में लिखे बिना भी राज्यपाल के निर्देश को यह आईना दिखाना है कि ऐसे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था।
अदालत की पूरी प्रक्रिया को किनारे रखकर जिस तरह से बुलडोजर चलाए जा रहे, ठीक उसी तरह ऐसे होर्डिंग भी लगाए जा रहे हैं। उत्तरप्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दोनों काम किए हैं, और इनमें से एक, बुलडोजर अभी भी पूरी रफ्तार से जारी है। जब सरकार ही यह तय करने लगे कि कौन उपद्रवी है, कौन मुजरिम है, उसके परिवार की संपत्ति को कितना जमींदोज करना जायज होगा, तो फिर अदालत की जरूरत ही क्या है? इस पर हम अभी एक-दो दिनों में ही खुलासे से लिख चुके हैं, जिसे दुहराना जगह बर्बाद करना होगा, लेकिन झारखंड के राज्यपाल के ताजा निर्देश को देखते हुए हम उसका जिक्र भर कर रहे हैं। झारखंड में सरकार तो भाजपा की नहीं है, लेकिन वहां के राज्यपाल भाजपा से आए हैं, और दिल्ली की भाजपा-अगुवाई वाली सरकार के भेजे हुए हैं। इसलिए वहां की सरकार की रीति-नीति से परे भी उन्होंने अफसरों को राजभवन बुलाकर एक निर्देश दिया जिसके मुताबिक आरोपियों और संदिग्ध लोगों के ये होर्डिंग जारी किए गए। इसके खतरे को समझना जरूरी है। आज जब देश में वैसे भी गोश्त के एक टुकड़े को लेकर लोगों का कत्ल किया जा रहा है कि वह गोमांस है, तब सरकार की तरफ से कुछ लोगों की तस्वीरें और नाम-पते संदिग्ध उपद्रवी की तरह पेश करके उन्हें भीड़त्या के लिए पेश किए जाने के बराबर है। झारखंड की राजधानी की पुलिस ने राज्यपाल के जुबानी निर्देशों को मानते हुए कानून के अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल भी नहीं किया, और एक सहज लोकतांत्रिक समझ का भी नहीं, कि संदेह के आधार पर लोगों को निशाना बनाकर पेश करना अपने आपमें एक जुर्म है। इससे देश के अल्पसंख्यक तबके के लोगों की जिंदगी खतरे में डालने का काम भी किया जा रहा है, और चाहे राज्यपाल ही क्यों न कहे, अफसरों को यह काम नहीं करना था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी हर बड़े अफसर को होगी, यह उम्मीद तो की ही जाती है। एक राज्य की पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट जब कोई फैसला देता है, तो बाकी राज्यों के बड़े पुलिस अफसर भी उसे गौर से पढ़ते ही हैं, और राजभवन की बैठक में प्रदेश के तीन बड़े पुलिस अफसरों की मौजूदगी का जिक्र किया गया था।
संदेह के आधार पर लोगों की जिंदगी खतरे में डालना, उनके खिलाफ हिंसा के लिए दूसरे हिंसक तबकों को उकसाने के बराबर है। यह किसी राज्य में राज्य शासन का काम हो, या किसी दूसरे राज्य में राजभवन का, इससे उन प्रदेशों में हालात और बिगडऩे का पूरा खतरा रहता है, और सत्ता को अपने स्तर पर ऐसा इंसाफ करने में नहीं जुट जाना चाहिए जिसके लिए हिन्दुस्तानी लोकतंत्र में न्यायपालिका बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर सकता है जिसमें देश के बहुत से भूतपूर्व जजों ने बुलडोजरी इंसाफ के खिलाफ अदालत से कार्रवाई करने की अपील की है। यह अपील करने वालों में तीन भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट जज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया है कि अदालत कितना खरा सोना है, यह आज जैसे हालात की अग्निपरीक्षा में ही साबित होता है।
आज यह बात साफ है कि सरकारें और राजभवन जिस तरह अदालत के अहाते में अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ अदालत की आंखें खुलनी चाहिए। कल के दिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आपको सांसद या मंत्री घोषित करने लगेंगे, खुद सरकार चलाने लगेंगे, तो लोकतंत्र कहां बचेगा?
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
छत्तीसगढ़ के लिए बीते कल की तारीख एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई जब आधी रात के ठीक पहले जांजगीर जिले में एक बंद ट्यूबवेल में साठ फीट से अधिक गहराई में जाकर गिरा, और वहां फंस गया बच्चा पहाड़ सी विकराल कोशिशों के बाद बचा लिया गया। आधी रात के जरा पहले इस बच्चे को सुरंग के रास्ते निकालने की तस्वीरें जब सामने आईं, तब प्रदेश के दसियों लाख लोग चैन से सो पाए। और जैसा कि ऐसी किसी भी मानवीय त्रासदी के मामले में होता है, इस घटना के बीच प्रदेश के बाहर के भी लाखों लोग भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे, और अपने-अपने किस्म से दुआ कर रहे थे कि यह बेकसूर बच्चा बच जाए। जिन कोशिशों से जांजगीर के जिला प्रशासन, राज्य शासन, और केन्द्र सरकार की एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना जैसी एजेंसियों ने इस असंभव को संभव कर दिखाया, उसके लिए ये सब बधाई के हकदार हैं। खासकर राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि पार्टी के प्रदर्शनों में राहुल गांधी के साथ दो दिन दिल्ली में सडक़ों पर पुलिस से जूझते रहे, और इन्हीं दो दिनों में वे लगातार जांजगीर जिले में एक दूसरे राहुल को बचाने की कोशिशों में भी लगे रहे। भूपेश बघेल अपने आत्मविश्वास और इस मामले में मजबूत लीडरशिप के लिए बधाई के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने हर घंटे-दो घंटे में हालात पर नजर रखी, लोगों से बात की, और सोशल मीडिया पर हौसला बढ़ाते हुए बार-बार दुहराया कि इस बच्चे को बचा लिया जाए।
आज जब यह बच्चा बिलासपुर के एक सुविधा-संपन्न अस्पताल में अच्छी देखरेख में इलाज पा रहा है, तो बीती रात की बकाया नींद पूरी करने के बाद हमारे दिमाग में भी सौ किस्म की बातें आ रही हैं कि इस हादसे में क्या नहीं हो सकता था जो कि इस बच्चे की जान ले लेता, और किसी को कोई हैरानी भी नहीं होती। हैरानी तो इस बच्चे के बच जाने में है जिसे कुदरत या आस्थावानों के ईश्वर ने मूकबधिर भी बनाया, और शायद दिमागी रूप से कुछ कमजोर भी। फिर हादसा ऐसा बुरा हुआ कि अपने ही घर में खुले पड़े रह गए एक ट्यूबवेल में वह साठ फीट से अधिक की गहराई में गिर गया। जब शासन-प्रशासन ने यह तय किया कि ट्यूबवेल के गड्ढे के पास दूसरा गड्ढा खोदकर सुरंग बनाकर इस बच्चे को बचाया जाए, तो पहाड़ की ऊंचाई जितनी गहरी खुदाई करने के दौरान यह पता लगा कि नीचे की जमीन पूरी चट्टानी है, और यह चट्टान भी सबसे अधिक कड़ी चट्टान है जिसे छीलना भी मुश्किल था। ऐसे में बच्चा उस गड्ढे में पानी में कुछ हद तक डूबा हुआ उकड़ू बैठा था, पहले घड़ी के कांटों से बढ़ते हुए घंटे दिख रहे थे, फिर कैलेंडर के पन्नों पर तारीखें बढ़ते दिख रही थीं, और चार दिन गुजर जाने पर भी उस बच्चे तक पहुंचने का कोई ठिकाना नहीं था। यह सब कुछ वक्त के खिलाफ, मौत के खिलाफ, हादसों के खतरों के खिलाफ चल रहा था। सरकार की कोशिशें जितनी कड़ी थीं, उनसे कहीं अधिक कड़ा वहां हौसला था जिसे लेकर यह कमजोर बच्चा बिना सुने, बिना बोले उस गहराई में, उस छेद में पड़ा हुआ था। यह सब कुछ उसके बचने की संभावनाओं के खिलाफ था, और खासकर जब खुदाई में मिट्टी की जगह चट्टानें निकलने लगीं, तो सब कुछ उस बच्चे की तथाकथित किस्मत के भी खिलाफ दिखने लगा था।
लेकिन सौ घंटे से अधिक, 105 घंटे उस छेद में बैठे-बैठे उस बच्चे ने जिस हौसले के साथ अपनी धडक़नों को जारी रखा, अपनी सांसों को थमने नहीं दिया, और वहां भर रहे पानी को निकालने के लिए ऊपर से लटकाई गई बाल्टी को भरने का काम भी किया, वह सब कुछ अकल्पनीय है। लोग अपने बच्चे के घर के बाथरूम में कुछ मिनटों के लिए बंद हो जाने पर जिस परले दर्जे की दहशत के शिकार हो जाते हैं, उसके मुकाबले इस बच्चे की जिंदगी पर खतरा, उसका अकेलापन, और सरकारी कोशिशों की तंग सीमाएं, इन सबने मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाई थी कि बच्चे के बचने की उम्मीद कम ही दिखती थी। लेकिन रायपुर और दिल्ली से सीएम, और जांजगीर में वहां के डीएम (कलेक्टर) जितेन्द्र शुक्ला ने अपना हौसला कभी कमजोर नहीं दिखने दिया, और आखिरकार इस बच्चे को बचा लिया गया।
हादसा होते ही मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के लिए यह हुक्म जारी किया कि सभी तरह के बंद पड़े हुए ट्यूबवेल की जांच की जाए कि कहीं कोई छेद खुला हुआ तो नहीं है। ऐसे ही किसी पुराने हादसे के वक्त इसी जगह पर हमने बरसों पहले यही सिफारिश की थी कि हर ट्यूबवेल की जांच हो जानी चाहिए कि कोई खुला हुआ तो नहीं है। आज सबसे अधिक यातना इस बहादुर बच्चे ने झेली है जिसने दस बरस की उम्र में मौत को इतने करीब से देख लिया, और शिकस्त भी दे दी। लेकिन उसके साथ-साथ उन सैकड़ों लोगों ने भी यातना झेली है जो उसे बचाने में लगे हुए थे, और जो भावनात्मक रूप से इस जिंदगी से जुड़ गए थे। ऐसी भावनात्मक त्रासदी, और मौत के खतरे से बचने के लिए हर गांव और थाना स्तर पर हर ट्यूबवेल की जांच हो जानी चाहिए कि उनमें से कोई खुले तो नहीं पड़े हैं। इस बार तो यह बच्चा बच गया, लेकिन ऐसे हादसों में बचना बहुत कम मामलों में हो पाता है, और जैसी नामुमकिन दर्जे की कोशिश इस एक मामले में सरकार और सरकारी एजेंसियों ने की है, वैसी भी हर हादसे में मुमकिन नहीं हो पाती। इसलिए बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है। इस हादसे ने प्रदेश को बड़ा सबक दिया है कि ऐसे हर खतरे को टालने के लिए पुख्ता कोशिश की जाए, और हर ट्यूबवेल का रिकॉर्ड भी बना लिया जाए।
फिलहाल राहत की सुबह वाले इस दिन शासन-प्रशासन को बधाई देने के अलावा यह भी सूझ रहा है कि अभूतपूर्व साहस दिखाने वाले, और अंतहीन संघर्ष करने वाले इस बच्चे के हौसले की कहानी कम से कम इस राज्य के बाकी बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए ताकि वे अपनी जिंदगी में आने वाली दिक्कतों को पहाड़ सा विकराल न मान लें, और हमेशा यह याद रखें कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों से भी बच्चे बाहर निकल सकते हैं, निकले हुए हैं। राहुल नाम का यह बच्चा हौसले, सब्र, और संघर्ष का इस प्रदेश का सबसे बड़ा प्रतीक है, और समाज और सरकार को चाहिए कि उसे प्रेरणा की तरह इस्तेमाल करे, बच्चों के बीच, और बड़ों के बीच भी।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए खबरों में अधिक आने वाले सत्यपाल मलिक बड़ा खुलकर बोलते हैं, और इस वजह से वे हाल के बरसों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के घरेलू आलोचक की तरह भी स्थापित हुए हैं। अब अपने मुखर होने की वजह से, या किसी और वजह से, सत्यपाल मलिक पिछले बरसों में लगातार अलग-अलग प्रदेशों के राज्यपाल बनाए जाते रहे। 2018 से अब तक, ठीक चार बरस में वे ओडिशा, बिहार, जम्मू-कश्मीर, गोवा, और मेघालय के राज्यपाल रहे। चार बरस में पांच राजभवनों में बसाए गए शायद वे देश के अपने किस्म के अकेले राज्यपाल हैं। और मोदी के आलोचना के अलावा और तो कोई वजह ऐसी दिखती नहीं है कि वे लगातार और धीरे-धीरे कम महत्वपूर्ण राज्यों में भेजे गए, और अब वे आखिरी के चार महीने मेघालय में हैं जिसके बारे में देश के बाकी हिस्से को शायद यह भी याद नहीं होगा कि वहां का राजभवन किस शहर में है।
ऐसे सत्यपाल मलिक अभी दो दिन पहले राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय जाट संसद में हिस्सा लेने पहुंचे थे, और उन्होंने अपने आम बागी तेवरों के मुताबिक अपनी ही पार्टी की केन्द्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, सरकार के दोस्त अडानी को बेचे जा रहे हैं, हमें देश को बिकने से रोकना होगा। उन्होंने कहा जब सब बर्बाद हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री बताएं कि ये लोग मालदार कैसे हो रहे हैं? उन्होंने बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों का यह भी आव्हान किया कि अडानी ने फसल सस्ते दाम पर खरीदने और महंगे दाम पर बेचने के लिए पानीपत में बड़ा गोदाम बनाया है, अडानी का ऐसा गोदाम उखाड़ फेंको, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जेल चलूंगा, अंबानी और अडानी मालदार कैसे हो गए हैं, जब तक इन लोगों पर हमला नहीं होगा, तब तक ये लोग रूकेंगे नहीं।
सत्यपाल मलिक ने खुद के बारे में कहा कि किसान आंदोलन के दौरान वे अपना इस्तीफा जेब में लेकर प्रधानमंत्री से मिलने गए, उन्हें समझाया कि किसान कानून हटा दे, तब वह नहीं माने, बाद में प्रधानमंत्री को समझ आया, और उन्होंने किसानों से माफी मांगी, कानून वापस ले लिए। सत्यपाल मलिक ने कहा- मेरे तो राज्यपाल के तौर पर चार माह बचे हैं, जेब में इस्तीफा लेकर घूमता हूं, मां के पेट से गवर्नर बनकर नहीं आया था, चार महीने में ही किसानों के हक के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतर जाऊंगा।
उनकी बातों को खुलासे से यहां पर लिखना इसलिए जरूरी था कि उन बातों को लेकर ही यहां आज की बात की जा रही है। यह बात तो ठीक है कि पिछले बरसों में घरेलू ऑडिटर की तरह या घर के भीतर के चौकीदार की तरह सत्यपाल मलिक ने कई बार सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाने पर लिया है, और जाने वे कौन सी रहस्यमय वजहें हैं जिनकी वजह से ये छोटे-छोटे राज्यों में भेजे तो गए, लेकिन फिर भी राज्यपाल बने रहे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि वे अगर मोदी सरकार के कृषि कानूनों की तरह गंभीर मुद्दों पर गंभीर खामियां देखते हैं, तो वे राजभवनों से चिपके हुए क्यों हैं? एक तरफ तो वे लोगों के साथ जेल जाने को तैयार होने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वे किसानों को कानून तोडक़र अडानी का गोदाम उखाडक़र फेंकने को कह रहे हैं, लेकिन साथ-साथ वे राजभवन में अपनी तैनाती के आखिरी दिन तक वहां बने भी रहना चाहते हैं। अब मेघालय का राज्यपाल होना जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल होने की तरह का तो है नहीं कि वे प्रदेश को मंझधार में छोडक़र निकल नहीं सकते। जब चार महीने बाद वे किसानों के साथ सडक़ों पर आने पर आमादा हैं, तो चार महीनों के लिए राजभवन का यह मोह कैसा? वे इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ भाजपा के भीतर से सबसे कटु आलोचना करने वाले एक-दो लोगों में शामिल रहे हैं, और सार्वजनिक रूप से, कैमरों के सामने उन्होंने बहुत कड़वी, निजी और गोपनीय बातें उजागर की हैं, और किसी भी बात का सरकार ने कोई खंडन नहीं किया है। ऐसी गंभीर तनातनी के चलते हुए उनका आलोचक भी बने रहना, और राजभवन में भी बने रहना कुछ विरोधाभासी लगता है। सार्वजनिक जीवन में जो लोग रहते हैं, वे अगर अपनी खुद की कही हुई बातों के गंभीर विरोधाभास में बरसों से, लगातार और नियमित रूप से ऐसे उलझे रहते हैं, तो उन्हें अपनी नीयत को लोगों के सामने साफ-साफ रखना चाहिए। वे अपनी नीयत का दावा करते हैं, लेकिन राज्यपाल के पद पर इन्हीं नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई तैनाती के आखिरी दिन तक बने भी रहना चाहते हैं, जो कि नीयत की ईमानदारी से परे की बात है, और सरकार द्वारा तय की गई नियति का पूरा मजा उठाने की बात भी है।
केन्द्र सरकार चाहे तो सत्यपाल मलिक को हटा भी सकती थी, लेकिन उसे भी शायद एक अभूतपूर्व टकराव और कड़वाहट का खतरा दिख रहा होगा। शायद इसलिए मोदी सरकार मलिक के कार्यकाल को पूरा हो जाने देना चाहती है, जो कि खुद मलिक के मुताबिक चार महीने बाकी है। लेकिन हम सार्वजनिक जीवन के प्रमुख लोगों से इस नैतिकता की उम्मीद करते हैं कि वे प्रधानमंत्री पर अगर अडानी-अंबानी को लेकर इतनी बड़ी तोहमतें लगा रहे हैं, तो वैसे प्रधानमंत्री की दी गई कुर्सी पर उन्हें बने भी नहीं रहना चाहिए, और सत्ता-प्रतिष्ठान से बाहर आकर सडक़ की लड़ाई लडऩी चाहिए। हम इस बात को भी नैतिक बेईमानी पाते हैं कि वे किसानों को तो अडानी का गोदाम गिराकर बिना डरे जेल जाने का आव्हान कर रहे हैं, लेकिन खुद अगले चार महीने कानून से हर किस्म की हिफाजत पाते हुए राजभवन में बने रहना चाहते हैं। उनकी की गई आलोचना कम अहमियत नहीं रखती, लेकिन उनके कहने और करने के बीच एक फासला दिख रहा है, जिसे उन्हें खुद ही पाटना चाहिए। अगर उन्हें यह लग रहा है कि देश बेचा जा रहा है, प्रधानमंत्री के करीबी लोग उसे खरीद रहे हैं, तो ऐसी सरकार का राज्यपाल रहे बिना उन्हें सडक़ से इस बात को उठाना चाहिए। महज यह कहना कि वे मां के पेट से गवर्नर बनकर नहीं आए थे, काफी नहीं है, होना तो यह चाहिए कि वे उम्र के इस पड़ाव पर यह भी साबित करे कि किसी की अर्थी राजभवन से निकले, या किसान आंदोलन के धरना स्थल से, उनके धर्म के हर किसी को विलीन तो उन्हीं गिने-चुने पांच तत्वों में होना है। चार महीने बाद आंदोलन में शरीक होने की बात फिजूल की है, अगर उन्हें देश आज इस खतरनाक मुहाने पर दिख रहा है। सत्यपाल मलिक को अपनी नीयत के सत्य को साबित करना चाहिए, वरना उनकी बातों का कोई वजन नहीं रह जाएगा।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
उत्तरप्रदेश के योगीराज में जिस अंदाज में किसी भी प्रदर्शन में शामिल मुस्लिमों के घरों को जिस तरह सरकारी बुलडोजर आनन-फानन जमींदोज करने में लग जा रहे हैं, वह देखना भी भयानक है। लेकिन देश के लोगों के लिए ही यह नजारा भयानक है, देश का सुप्रीम कोर्ट अभी शायद ठंडी पहाडिय़ों पर गर्मी की छुट्टियां मना रहा है, और वैसे भी जब सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा था तब भी उसने बुलडोजरों को रोकने की जहमत नहीं उठाई थी, इसलिए पहाड़ों से जजों के लौट आने के बाद भी लोगों को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और नीचे से लेकर ऊपर तक हिन्दुस्तानी अदालतों में जिस तरह आज की हिन्दुत्ववादी सरकारों के लिए एक बड़ा बर्दाश्त दिखाई पड़ रहा है, वह गजब का है। लेकिन हिन्दुस्तान में लोकतंत्र आज सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने वाले कुछ धर्मनिरपेक्ष और इंसाफपसंद लोगों के मार्फत जिंदा है जो इस बात को जमकर उठा रहे हैं कि किस-किस प्रदेश में भाजपा की सरकारें कौन-कौन से काम साम्प्रदायिक नीयत से कर रही हैं, और किस तरह यह देश एक धर्मराज में तब्दील किया जा रहा है।
सोशल मीडिया के एक नियमित जिम्मेदार लेखक ने अभी कुछ मिनट पहले ही याद दिलाया है कि दो महीने पहले इसी यूपी एक अयोध्या में बरसों से आरएसएस और बजरंग दल के लिए काम कर रहे ब्राम्हण समाज के कई नौजवानों ने मस्जिदों के दरवाजों पर धार्मिक ग्रंथ के फटे पन्ने फेंके, गाली-गलौज की चि_ियां फेंकीं, और कथित रूप से सुअर के मांस के टुकड़े फेंके जिन्हें कि इस्लाम में अपवित्र माना जाता है। योगी की ही पुलिस ने उसी वक्त सात लोगों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी को दो महीने हो रहे हैं, पुलिस के पास पूरे सुबूत हैं जिनमें सीसी टीवी की रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन किसी सरकारी बुलडोजर ने इन लोगों के घरों का रूख नहीं किया। इस तरह के और भी कई जुर्म लोगों ने गिनाए हैं कि साम्प्रदायिक दंगों में जहां हिन्दू शामिल मिले, उनमें से किसी हिन्दू पर ऐसी कार्रवाई नहीं की गई।
चीजों को सही तरीके से सामने रखने के लिए ये मिसालें अच्छी हैं, लेकिन हम इस भेदभाव के बाद भी किसी पर भी बुलडोजरी फैसले के खिलाफ हैं क्योंकि यह सत्ता का पसंदीदा तरीका हो सकता है कि वह जिसे सजा देना चाहे कुछ मिनटों के भीतर उसे जमींदोज कर दे, लेकिन यह लोकतंत्र का तरीका नहीं हो सकता। और भेदभाव बताने के लिए तो ये मिसालें ठीक है क्योंकि ये सत्ता के साम्प्रदायिक चरित्र को उजागर करती हैं, लेकिन विरोध इस पूरे बुलडोजरी मिजाज का होना चाहिए, न कि आज जिन पर यह हमला हो रहा है, महज उन्हें बचाने के लिए। लोकतंत्र में सरकार और संसद से परे अदालत को भी इसलिए बनाया गया है कि जब कभी इनमें से किसी एक संस्था की ताकत इंसाफ के दायरे को पार करने लगे, तो दूसरी संस्थाएं उस पर कुछ कर सकें। इसीलिए बड़ी अदालतों के जजों को हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी पलटने के लिए संसद में कानून में संशोधन या नया कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन सबसे अधिक जरूरत पड़ती है सत्ता की सरकारी बददिमागी को काबू करने के लिए अदालती दखल की, और उसका भी सबसे मजबूत इंतजाम भारतीय लोकतंत्र में किया गया है।
आज हैरानी की बात यह है कि जब देश के बच्चे-बच्चे को यह दिख रहा है कि कई राज्यों की सरकारें घोर साम्प्रदायिक तरीके से काम कर रही हैं, और मुस्लिम समुदाय को घेरकर मारना ही सबसे बड़ी नीयत हो गई है, उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट को यह नौबत दखल देने लायक नहीं लग रही है, तो यह उसकी चेतना को लकवा मार गया दिखता है। देश की सबसे बड़ी अदालत को आज अगर हिन्दुस्तानी सत्तारूढ़ साम्प्रदायिकता को टोकने की भी जरूरत नहीं लग रही है, तो देश के कार्टूनिस्टों ने तो पिछले कुछ दिनों से ऐसे कार्टून बनाने शुरू कर दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत तक पहुंचे बुलडोजर उसे गिराने की तैयारी कर रहे हैं। और यह नौबत कार्टूनिस्ट की कल्पना से, उसके तंज से परे भी हकीकत से बहुत दूर नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के प्रति बहुत रियायत का इस्तेमाल करते हुए उसकी चेतना को लकवा मारने की बात कह रहे हैं, सच तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी चुप्पी अख्तियार कर ली है जो उसकी जरूरत को ही खारिज कर रही है। जब देश के कमसमझ और मामूली लोगों को भी यह दिखे कि सत्ता अभूतपूर्व और ऐतिहासिक दर्जे की बेइंसाफी कर रही है, जुल्म कर रही है, और जुर्म कर रही है, और वैसे में मुल्क में अकेले सुप्रीम कोर्ट को ही यह बात न दिखे, तो उसे क्या कहा जाए?
आज हिन्दुस्तान में निशानों को छांट-छांटकर, धर्म के आधार पर जब निर्वाचित और संविधान की शपथ लेने वाली सरकारों के बुलडोजर जज का काम भी कर रहे हैं, वे बुलडोजज बन गए हैं, तब भी अगर सुप्रीम कोर्ट पहाड़ों पर छुट्टियां मना रहा है, तो क्या उसे लंबी छुट्टी दे देने की नौबत नहीं आ गई है? जहां तक हमें याद पड़ता है कि दिल्ली में बड़े जजों की राह में ट्रैफिक की मामूली दिक्कत भी आ जाने पर घंटे भर के भीतर पुलिस कमिश्नर को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, आज तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों की अदालतों के कटघरे भी इन बुलडोजरों के लिए छोटे और कम पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इस रहस्यमय चुप्पी के चलते अब सरकारी जुल्म ने अदालतों की जगह ले ली है, अपने आपको हाशिए पर धकेलने वाली यह भारतीय लोकतंत्र की अकेली संस्था बन रही है।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
नगालैंड में दिसंबर 2021 में भारतीय सेना के एक मुहिम के दौरान 13 बेकसूर नौजवानों को गोलियों से भून दिया गया था, जिनमें से आधे तो नाबालिग ही थे। सारे के सारे निहत्थे थे, और एक जगह से मजदूरी करके लौट रहे थे, थलसेना की पैरा स्पेशल फोर्स ने इन कोयला खदान मजदूरों की पहचान भी नहीं की, और उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। अब नगालैंड पुलिस की एसआईटी ने अदालत में चार्जशीट फाईल की है जिसमें सेना के एक मेजर, दो सूबेदार, आठ हवालदार, चार नायक, छह लांस नायक समेत कुल तीस लोगों के खिलाफ जुर्म पेश किया गया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि घातक लगाकर किए गए इस हमले में गलत पहचान के चलते बेकसूर मजदूर मार डाले गए थे।
सुरक्षा बल जब विपरीत और दबावपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं, तो उनसे कई बार ऐसी चूक होती है, और कई बार वे दुस्साहस या अतिआत्मविश्वास में भी ऐसी कार्रवाई कर बैठते हैं क्योंकि जिन इलाकों में लगातार बंदूकों की तैनाती रहती है, वहां पर सुरक्षा बलों के हाथों हिंसा के मामले होते ही रहते हैं। कश्मीर हो, उत्तर-पूर्व, या कि बस्तर जैसे नक्सली इलाके, यहां पर राज्य और केंद्र के सुरक्षा बल तरह-तरह से मानवाधिकार भी कुचलते रहते हैं, कत्ल और बलात्कार जैसे जुर्म भी करते रहते हैं, और बंदूक की ताकत का बाकी हर किस्म का बेजा इस्तेमाल भी आम बात रहती है। मध्यप्रदेश में इंदौर के पास मऊ नाम की जगह पर सेना का बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है, और हर साल दो साल में प्रशिक्षण केंद्र से निकलकर सैनिक शहर में जाते हैं, और स्थानीय पुलिस के साथ उनकी झड़प होती है, और यह पुलिस अफसरों का जिम्मा रहता है कि वे मामले को रफा-दफा करें। ऐसा टकराव रेल्वे स्टेशन और रेलगाडिय़ों में भी कई बार देखने मिलता है जब सैनिक समूहों में सफर करते हैं, और वे आम मुसाफिरों को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, और पूरे डिब्बों पर कब्जा कर लेते हैं। मोटेतौर पर देखें तो भीड़ की जैसी मानसिकता आम जनता की हिंसक भीड़ में हो जाती है, वैसी ही मानसिकता सिपाहियों या सैनिकों के समूह की भी हो जाती है कि उनकी नजरों में कानून की कोई कीमत नहीं रह जाती है।
छत्तीसगढ़ का बस्तर लंबे समय से सुरक्षा बलों की ऐसी बददिमागी का गवाह और शिकार रहा है। यहां भी राज्य पुलिस के कुख्यात बड़े अफसरों की लीडरशिप में राज्य और केंद्र के सुरक्षा बलों ने गांव के गांव जला दिए, दसियों हजार लोग बेदखल हो गए, और पुलिस अफसर खुलेआम यह बोलते घूमते रहे कि बस्तर में उसी को जिंदा रहने का हक है जिसका जिंदा रहना वे जरूरी समझते हैं। ऐसे लंबे रिकॉर्ड वाले अफसरों का भी न तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कुछ बिगाड़ पाया, और न ही सुप्रीम कोर्ट। जब सुरक्षा बलों के खिलाफ कार्रवाई की नौबत आती है, तो सत्तारूढ़ नेताओं को यह समझा दिया जाता है कि अगर वर्दी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो आगे जाकर दूसरे वर्दीधारी लोग खतरे उठाना बंद कर देंगे। ऐसे तर्क आतंक के दिनों में पंजाब में केपीएस गिल के वक्त भी दिए गए थे जब बड़े पैमाने पर मानवाधिकार हनन हुआ था और बेकसूरों को मारा गया था। पूरी दुनिया में बेकसूरों की ऐसी मौतों को हत्या मानने के बजाय उन्हें कोलैटरल डैमेज मान लिया जाता है कि मानो गेंहू के साथ घुन भी पिस गया हो। हकीकत यह है कि सत्तारूढ़ राजनेताओं की यह मजबूरी सी हो जाती है कि वे अपने सुरक्षा कर्मचारियों की गलती, या गलत काम को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा न करने पर जिम्मेदारी की आंच उन पर भी तो आएगी।
लेकिन किसी लोकतंत्र की परिपच्ता इसी में रहती है कि वह अपने भीतर होने वाली गलतियों, और गलत कामों को कितना खुलकर मंजूर करता है, और उन पर सुधार की क्या कार्रवाई करता है। अगर किसी सुरक्षा बल के लोगों की ज्यादती पर कार्रवाई होती रहे, तो उस सुरक्षा बलों के हाथों बड़ी हिंसा होने का खतरा भी घटते चलता है। लेकिन जब कश्मीर में फौज का एक अफसर जीप के सामने एक स्थानीय कश्मीरी को बांधकर पथराव के बीच से निकलने के लिए उसे मानव-कवज की तरह इस्तेमाल करता है तो ऐसे सुरक्षा बल स्थानीय लोगों की सारी हमदर्दी भी खो बैठते हैं। आज हिंदुस्तान में जगह-जगह केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्यों की पुलिस का जैसा साम्प्रदायिक और जातिवादी दिमाग बनाया जा रहा है, उसके चलते समाज के एक तबके का उस पर से भरोसा उठ गया है, और अपने देश के भीतर भी ऐसे सुरक्षा बल बिना जनसमर्थन वाले परदेश की तरह रह जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी हमारा देखा हुआ है कि सुरक्षा बलों से स्थानीय आदिवासियों की कोई हमदर्दी नहीं रह जाती, और पुलिस और प्रशासन अपनी गलती मानने के बजाय इसे नक्सलियों का असर करार देते हैं।
हमारा ख्याल है कि सुरक्षा बलों के हाथों जब कभी ऐसी हिंसा होती है, तो उसकी जांच, और उस पर कार्रवाई के लिए एक बहुत पारदर्शी और समयबद्ध इंतजाम होना चाहिए। बस्तर में हिंसा की शिकार पीढिय़ां गुजरी जा रही हैं, और कुसूरवार आलाअफसरों या बाकी वर्दीधारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नगालैंड में स्थानीय पुलिस ने यह अच्छा काम किया है कि साल भर के भीतर ही अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। इससे उत्तर-पूर्वी राज्यों की यह मांग भी मजबूत होगी कि सेना के बचाव के लिए बनाए गए विशेष अफ्पसा कानून को खत्म किया जाए। नगालैंड पुलिस के मौजूदा डीजीपी टीजे लांगकुमेर लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी रहे हैं, और उनके दौरान भी बस्तर में पुलिस ज्यादती के कई मामले सामने आए थे। आज राज्य के पुलिस मुखिया की हैसियत से उन्होंने नगालैंड में तेजी से कार्रवाई की है, क्या छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी भी अपने प्रदेश की सरकार से ऐसी किसी तेज कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं? या फिर उन्हें सिर्फ नक्सल समर्थक होने की तोहमत झेलनी पड़ेगी?
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
हिन्दुस्तान में मुस्लिमों की एक प्रमुख संस्था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुस्लिमों से सार्वजनिक अपील की है कि वे टीवी चैनलों की बहसों में हिस्सा न लें। मीडिया के मार्फत जारी इस अपील में कहा गया है कि समाज के प्रमुख लोग उन टीवी चैनलों की बहस में हिस्सा न लें जिसका मकसद सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाना है। उनका मकसद इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करना है, ये चैनल अपनी तटस्थता साबित करने के लिए एक मुस्लिम चेहरे को भी बहस में शामिल करना चाहते हैं, और प्रमुख मुस्लिम लोग अज्ञानता से इस साजिश के शिकार हो जाते हैं। अपील में आगे कहा गया है कि अगर इन कार्यक्रमों और चैनलों का बहिष्कार किया जाए तो इससे न केवल इनकी टीआरपी कम होगी, बल्कि वे अपने मकसद में पूरी तरह नाकामयाब भी होंगे।
इस अपील के बिना भी हिन्दुस्तान में आम लोग टीवी चैनलों पर इस किस्म की बहसों को देखकर थक चुके हैं जिनमें नफरत को आसमान की ऊंचाईयों तक ले जाया जाता है और वहां से देश के तमाम लोगों पर उसे छिडक़ दिया जाता है। बहुत से लोग अब खुलकर यह बात करने लगे हैं कि टीवी चैनल देखना बंद किया जाए। कहने के लिए तो केन्द्र सरकार के बड़े कड़े कानून टीवी समाचार चैनलों पर लगते हैं, और कई अर्जियां तो बरसों तक पड़ी रह जाती हैं, उन्हें टीवी चैनल शुरू करने की इजाजत नहीं मिलती। ऐसे में जब टीवी पर नफरत फैलाने के जुर्म में देश की सत्तारूढ़ भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता पर जुर्म दर्ज हुआ है, तब भी उस चैनल पर जुर्म दर्ज नहीं हुआ है जिस पर उसे दुनिया को हिला देने वाला यह बयान दिया था। अब किसी चैनल के साथ या और चैनलों के साथ यह रियायत भी समझ से परे है, कि उस पर किसी बयान पर तो जुर्म दर्ज हो गया, लेकिन वह चैनल यूट्यूब पर उस बयान को बनाए रखे, और उस पर कोई जुर्म न हो। यह पूरा सिलसिला मीडिया के गलाकाट मुकाबले में सबको एक-दूसरे के मुकाबले अधिक गैरजिम्मेदार बनाने वाला है, और इससे देश की सरकार को कोई परहेज भी नहीं लग रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही एक बहुत छोटा सा जिम्मेदार हिस्सा बार-बार यह कह रहा है कि लोगों को टीवी देखना छोड़ देना चाहिए। और फिर टीवी के जो चैनल जाहिर तौर पर सबसे अधिक नफरत फैला रहे हैं, वे लोकप्रियता के पैमानों पर सबसे ऊपर भी बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो चैनल आज भी सबसे अधिक जिम्मेदारी दिखाकर जिंदा चल रहा है, वह लोकप्रियता के पैमाने पर सबसे नीचे पाया जा रहा है। इन बातों का मतलब क्या निकाला जाए?
लोकतंत्र और उदार बाजार व्यवस्था में किसी कारोबार पर तो रोक लगाई नहीं जा सकती, लेकिन सरकार देश के हर कारोबार को नियंत्रित करती है। ऐसे में अधिकार जिसके हाथ रहते हैं, जिम्मेदारी भी उसी की रहती है। जो सरकार टीवी चैनलों को बहुत थोक-बजाकर इजाजत देती है, और जिसके हाथ यह अधिकार रहता है कि वह किसी भी चैनल को कितने भी वक्त के लिए बंद कर सकती है, उसी से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह देश के अमन-चैन के खिलाफ सोची-समझी चैनली साजिश देखने पर उन चैनलों पर कम या अधिक वक्त के लिए रोक लगाए, और उसके खिलाफ जुर्म दर्ज करे। अब हर सैटेलाइट चैनल तकनीकी रूप से पूरी दुनिया में देखा जा सकता है, इसलिए उसके खिलाफ जुर्म भी पूरी दुनिया में दर्ज हो सकते हैं। हिन्दुस्तान में भी देश के हर थाने में किसी चैनल के खिलाफ जुर्म दर्ज हो सकता है, लेकिन वह एक अराजक नौबत हो जाएगी। जब देश में केन्द्र सरकार बहुत से मामलों में देश के तमाम प्रदेशों की मुखिया है, तो किसी चैनल के जुर्म पर जुर्म कायम करने में भी उसे पहल करनी चाहिए। अब यह एक अलग बात है कि दुनिया के मुस्लिम देशों में भारत को दी गई कूटनीतिक चेतावनी में हिन्दुस्तानी समाचार चैनलों का अलग से जिक्र नहीं किया, वरना अब तक दो-चार चैनल कम से कम कुछ दिनों के लिए तो बंद हो ही चुके रहते।
हिन्दुस्तान में यह सिलसिला बहुत भयानक है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारतीय लोकतंत्र की एक कमजोर नब्ज बन गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नीयत की सही शिनाख्त की है। आज देश में साम्प्रदायिक हिंसा भडक़ाने की कीमत पर भी जो चैनल अपने धर्मान्ध और साम्प्रदायिक दर्शकों को हिंसा की तरफ धकेलते हुए अपने लिए अधिक टीआरपी जुटा रहे हैं, उनका जमकर विरोध होना चाहिए। हम पहले भी कई बार इस बात को लिख चुके हैं कि भारत अब भी अखबारों का एक बड़ा तबका गैरसाम्प्रदायिक बना हुआ है, और उसे मीडिया नाम की इस विशाल छतरी से बाहर निकल आना चाहिए, और प्रेस नाम की अपनी पुरानी पहचान पर टिके रहना चाहिए। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक साथ गिनना नामुमकिन है, और प्रेस को अपनी परंपरागत पहचान, अपने परंपरागत मूल्यों पर टिके रहना चाहिए। हालांकि हिन्दुस्तानी प्रेस का एक हिस्सा आज टीवी चैनलों के बहुतायत हिस्से की तरह का भडक़ाऊ, उकसाऊ, साम्प्रदायिक या हिंसक हो चुका है, लेकिन फिर भी मोटेतौर पर हिन्दुस्तानी प्रेस टीवी से बहुत बेहतर बचा हुआ है, और उसे वैसा अलग रखने के लिए उसकी अपनी पहचान मीडिया शब्द से बाहर होनी चाहिए। यहां यह भी साफ कर देना जरूरी है कि हिन्दुस्तानी समाचार चैनल जो कर रहे हैं, वह पत्रकारिता बिल्कुल नहीं है, उसका अखबारनवीसी से कोई लेना-देना नहीं है, वह जर्नलिज्म बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि इन तीनों शब्दों से यह साफ है, पत्रकारिता (समाचार) पत्र से जुड़ी हुई है, अखबारनवीसी अखबार से, और जर्नलिज्म किसी जर्नल से जुड़ा हुआ है, और वही मुमकिन भी है। प्रेस को अपनी टूटी-फूटी गुमटी में संपन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को घुसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह पर्याप्त बदनाम हो चुका है, और उसकी नीयत इंसानियत से परे की, कारोबारी कामयाबी की हो चुकी है, और फिर वह चाहे इंसानी लहू की कीमत पर ही क्यों न हो।
देश में आज नफरत का जो सैलाब टीवी चैनलों ने फैलाया हुआ है, उसे समेटना बरसों तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। लगातार फूटते हुए ज्वालामुखी की तरह टीवी चैनलों के सिग्नल नफरत का लावा लेकर घरों तक पहुंच रहे हैं, और अपने दर्शकों के दिल-दिमाग को जहर के धुएं से भर दे रहे हैं। दर्शकों की यह बड़ी संख्या इस देश में मानसिक हिंसक रोगियों की बड़ी संख्या की तरफ इशारा भी करती है, और इस देश की सामूहिक चेतना को परामर्श और इलाज की जरूरत भी है। देश के आम लोगों को एक मुस्लिम संगठन के जारी किए हुए इस बयान पर गौर करना चाहिए, और अपने परिवार को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जहर से बचाना भी चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महीने भर से गांव-गांव घूम रहे हैं। मकसद है लोगों से उनकी दिक्कतों को जानना, और सरकारी योजनाओं की कामयाबी को तौलना। इसी दौरान उन्हें कई जगह यह भी सुनने मिला कि जंगल से बंदर आकर गांवों की फसल खत्म या खराब करके चले जाते हैं। जब कई जगह उन्हें यह बात सुनाई दी तो उन्होंने वन विभाग से कहा कि जंगलों मेंं सागौन जैसे पेड़ लगाने के बजाय फलों के पेड़ लगाए जाएं, जो कि जानवरों के भी काम आएं, और आसपास बसे हुए लोगों के भी।
दरअसल जंगल तो ऐसे ही हुआ करते थे। मिलेजुले पेड़ रहते थे, कुछ लकड़ी के इस्तेमाल आते थे, कुछ बांस होता था, और कुछ आदिवासियों और जानवरों के खाने लायक फल होते थे। लेकिन चूंकि फलों से वन विभाग को कोई कमाई नहीं होती, इसलिए वह यूक्लिपटस से लेकर सागौन तक का वृक्षारोपण करते आया है जिससे कमाई की गारंटी रहती है। लेकिन इससे जानवरों और इंसानों के जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं रहती, क्योंकि जंगल के सागौन जैसे पेड़ सिर्फ वन विभाग ही काट सकता है, और वहां बसे हुए लोगों को भी उसे काटने की इजाजत नहीं रहती। सरकारी योजनाओं के फायदे को अगर रूपयों की ठोस शक्ल में नहीं गिना जा सकता, तो उन्हें फिजूल का मान लिया जाता है। इसलिए सागौन जैसे वृक्षारोपण विभाग के पसंद के होते हैं, और आम स्थानीय जंगली फलों के पेड़ कभी भी उसकी प्राथमिकता नहीं रहते।
एक वक्त तो ऐसा था जब सडक़ों के किनारे लगे पेड़ों पर भी कई किस्म के फल लगते थे, लेकिन धीरे-धीरे ऐसी सार्वजनिक जगहों पर ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जिनका असल जिंदगी में इस्तेमाल सीधे-सीधे नहीं होता, और जो कम रखरखाव में पल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। शहरों के इर्द-गिर्द भी अभी कुछ दशक पहले तक देसी फलों के कई किस्म के जंगल होते थे, और शहरों से बच्चे भी फल तोडऩे यहां चले जाते थे, जानवरों को तो पेड़ पर लगे हुए या जमीन पर गिरे हुए फल नसीब होते ही थे। जंगल विभाग ने सभी जगह विविधता को खत्म करने का काम किया है, और किसी एक किस्म के पेड़ के जंगल लगा दिए जिससे कि जैवविविधता खत्म हुई, और स्थानीय जानवरों और इंसानों दोनों से जंगल के फायदे छिन गए। शहरों के भीतर तो बसाहटों में फलों के पेड़ को अगल-बगल के लोगों के लिए खतरा भी मान लिया जाता है क्योंकि उन्हें तोडऩे के लिए लोग पत्थर चलाएंगे। लेकिन जंगलों में अगर फलदार पेड़ लगाए जाते हैं, तो उससे जंगली जानवरों का शहरों में उत्पात भी कम होगा, जंगल में बसे लोगों को खाने और बेचने के लिए ऐसे फल मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ की एक और खूबी है कि यहां के जंगलों की वनोपज देश के किसी भी राज्य के मुकाबले अधिक है। और तेन्दूपत्ता, महुआ, इमली, चिरौंजी जैसे पेड़ सरकार के लगाए हुए नहीं हैं, वे कुदरती पेड़ हैं, जिनकी उपज सरकार खरीद लेती है, और इस तरह वनवासियों को एक मामूली सालाना कमाई होती है। जंगलों से भरे-पूरे इस राज्य में कोई न कोई रास्ता निकालकर इमारती लकड़ी का दो नंबर का कारोबार चलते रहता है, लेकिन अगर फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, तो उनसे कोई कारोबार नहीं चलेगा, बल्कि लोगों का रोजगार चलेगा। छत्तीसगढ़ के जंगलों में फलदार पेड़ों को बढ़ावा देने की जरूरत और संभावना तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी प्राकृतिक जंगलों में रेशम पालन, लाख के कीड़ों को पालना जैसे बहुत से और रोजगार की गुंजाइश भी है जो कि मामूली सी सरकारी मदद से आगे बढ़ सकती है। देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में अर्थव्यवस्था कुछ हद तक बांस पर भी टिकी हुई है, और छत्तीसगढ़ में बांस अच्छी तरह बढ़ता है, और यहां बांस से सामान बनाने का काम भी काफी बढ़ा हुआ है। राज्य के पहले वित्तमंत्री रामचन्द्र सिंहदेव अपने जीवनकाल में बस्तर में केन की खेती के लिए कोशिश करते रहे, और छत्तीसगढ़ में ऐसी बेंत के फर्नीचर भी बनाए जाते हैं।
मुख्यमंत्री की इस बात से आज हमने यहां लिखना शुरू किया है, वह बात जानवर और इंसानों के बीच के टकराव को भी घटा सकती है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में जंगली जानवरों के साथ इंसानों का मुख्य टकराव हाथियों तक सीमित है, और जंगलों को बचाना ही उसका अकेला तरीका हो सकता है। हाथियों के खाने के लिए अलग से कोई फसल तो नहीं लगती, लेकिन जंगल और तालाब-नदी जरूर लगते हैं, और छत्तीसगढ़ में कोयला निकालने के लिए बड़े पैमाने पर ऐसे जंगल खत्म करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यह याद रखने की जरूरत है कि कोयले के लिए जब जंगल हटेंगे, जंगली जानवर बेदखल होंगे, तो उनका इंसानों के साथ टकराव भी बढ़ेगा, और गांव-कस्बों में उनका दाखिला भी। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को जंगलों की अपनी पहचान बचाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इसी से यह राज्य भी बचेगा, और इसके जानवर और इंसान भी। फलों के पेड़ लगाना इस सिलसिले में एक शुरूआत हो सकती है, जिसका असर आगे चलकर देखने मिलेगा।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
पिछले महीने स्लोवेनिया में चल रहे साइकिलिंग के एक प्रशिक्षण कैम्प से भारत की एक प्रमुख महिला खिलाड़ी ने वापिस आना तय किया क्योंकि टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच आर.के. शर्मा पर उसका यह आरोप था कि वे उसे अपने साथ सोने के लिए कह रहे थे, बलपूर्वक अपने करीब खींच रहे थे, उसने शर्मा के बारे में यह भी कहा कि वे उसे अपनी बीवी की तरह रहने के लिए दबाव डाल रहे थे, वरना वे उसका कॅरियर तबाह करने की धमकी दे रहे थे, और कह रहे थे कि उसे सडक़ों पर सब्जियां बेचनी पड़ेगी। इस पर भारत के खेल संगठन ने इस खिलाड़ी को जांच का भरोसा दिया है, और कमेटी बना दी है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि वे पूरी तरह अपनी खिलाड़ी के साथ हैं। उल्लेखनीय है कि यह कोच 2014 से ही राष्ट्रीय साइकिलिंग टीम के साथ है।
यह पहला मौका नहीं है जब खेलों में प्रशिक्षक या टीम मैनेजर द्वारा यौन शोषण की बात सामने आई हो। अब तक का ऐसा सबसे बड़ा मामला अमरीका में जिमनास्ट कोच का सामने आया है जिसकी वजह से पिछले ओलंपिक के बीच से अमरीका की सबसे होनहार जिमनास्ट ने मुकाबला छोड़ दिया था क्योंकि वह मानसिक रूप से टूट गई थी। बाद में अमरीका में जब इस मामले की जांच हुई तो पता लगा कि बीस बरसों तक प्रशिक्षक रहे हुए इस आदमी ने इस दौरान 368 जिमनास्ट लड़कियों का देह शोषण किया था। जिस अमरीका में कानून और उस पर अमल दोनों ही कड़े हैं, वहां पर भी देश के सबसे बड़े, ओलंपिक खिलाड़ी, देह शोषण का शिकार होते रहे, और वहां के खेल संगठन कुछ नहीं कर पाए। अब अगर एक कोच 368 जिमनास्ट को ऐसी यातना दे सकता है, तो इस भांडाफोड़ होने के पहले कितनी प्रतिभाशाली खिलाड़ी यह खेल छोडक़र जा नहीं चुकी होंगी?
अब हिन्दुस्तान में अधिकतर खिलाड़ी लड़कियां गरीब या मध्यम वर्ग से निकलकर आती हैं, बहुत से खिलाड़ी आदिवासी इलाकों से आने वाले होते हैं, जिनकी न पारिवारिक आवाज होती है, न जिनमें कानूनी हकों को लेकर बहुत जागरूकता ही होती है। ऐसे में उनका शोषण करना अधिक आसान रहता है क्योंकि खेल संगठनों पर वही गिने-चुने पेशेवर हो चुके सत्तारूढ़ नेता काबिज रहते हैं, और बड़े ताकतवर अफसर भी हर प्रदेश में खेल संघों को हांकते हैं। ऐसे में सत्ता के इस मिलेजुले कारोबार के एकाधिकार के सामने खड़ा होना किसी खिलाड़ी के बस का नहीं रहता। फिर बचपन से लेकर बड़े होने तक दस-दस बरस जो लडक़े-लड़कियां पढ़ाई को भी छोडक़र रात-दिन मेहनत करके, परिवार और समाज से लडक़र खेल के मैदान पर मेहनत करते हैं, उन्हें ताकतवर प्रशिक्षकों या खेल संघ पदाधिकारियों के शोषण के सामने समर्पण करना कई बार अकेला जरिया दिखता है। ऐसे में अपने पूरे खेल-कॅरियर को देखते हुए बहुत से खिलाड़ी देह शोषण को बर्दाश्त करते होंगे, क्योंकि हिन्दुस्तानी समाज में कोई लडक़ी किसी के भी खिलाफ शोषण की शिकायत करे, सबसे पहले तो उस लडक़ी को ही अछूत और सरदर्द मान लिया जाता है, और सब लोग उससे परहेज करने लगते हैं कि कब यह कोई बवाल न खड़ा कर दे। नतीजा यह होता है कि खेल का मैदान हो, या पढ़ाई-लिखाई में रिसर्च हो, या किसी दफ्तर में प्रमोशन का मौका हो, मर्दों का यह समाज उससे चुप्पी के साथ सब बर्दाश्त करने की उम्मीद ही करता है। जो लडक़ी या महिला यौन शोषण झेलते हुए चुपचाप काम में लगी रहे, उसे अधिक व्यवहारिक मान लिया जाता है, और उसकी राह में अड़ंगे घट जाते हैं। हिन्दुस्तान में अगर किसी लडक़ी या महिला को अपनी प्रतिभा और काबिलीयत के दम पर प्रमोशन मिलता है तो भी लोग आंखें बना-बनाकर आपस में बात करते हैं कि उसने बॉस को खुश कर दिया होगा।
हिन्दुस्तान में महिला के कानूनी हक कागजों पर तो बहुत लिखे हैं, लेकिन जमीन पर देखें तो सारी की सारी न्याय प्रक्रिया उसके इन हकों को कुचलने के हिसाब से बनी हुई है। यह तो हिन्दुस्तान का हाल है, जहां पर हालत दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले अधिक खराब है, लेकिन विकसित देशों में भी खेलों के भीतर सेक्सटॉर्शन कहे जाने वाले इस यौन शोषण को एक बड़ी समस्या बताया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक ताजा रिपोर्ट में कई देशों में खिलाडिय़ों के खिलाफ ऐसी यौन हिंसा की मौजूदगी को पाया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जर्मन एथलीटों के बीच सर्वे में तीन में से एक ने यौन हिंसा के कम से कम एक हादसे का जिक्र किया है। आम जानकार लोगों का यह मानना है कि खेल के क्षेत्र से यौन शोषण के बहुत सारे मामलों की रिपोर्ट ही नहीं की जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि खेलों में अलग-अलग लोगों के बीच ताकत में बहुत अधिक फासला है। बच्चे बहुत कमजोर हालत में हैं, और वे खेलों के मिजाज के मुताबिक प्रशिक्षक पर भावनात्मक और शारीरिक रूप से आश्रित भी रहते हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि ये रिश्ते कुछ मामलों में खिलाडिय़ों के कॅरियर को बनाने या बर्बाद करने की ताकत रखते हैं।
भारत में साइकिलिंग की एक दिग्गज महिला खिलाड़ी की शिकायत का यह मौका देश भर के तमाम खेल संगठनों, और सरकारी विभागों को आत्मविश्लेषण और आत्ममंथन का मौका भी देते हैं। यह भी समझने की जरूरत है कि शोषण कई बरस तक जारी रहे, और वह अनदेखा रहे, या उसे अनसुना किया जाता रहे, तो फिर ऐसे खेल संगठनों को भी भंग करना चाहिए, और उनके पदाधिकारियों पर जिंदगी भर के लिए प्रतिबंध भी लगाना चाहिए। अगर खिलाडिय़ों का यौन शोषण बरस-दर-बरस जारी है, और खेल संघ उसकी तरफ से अनजान है, तो वह अनजान नहीं होते, वे लापरवाह होते हैं, और ऐसे लोगों पर आजीवन प्रतिबंध भी लगना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर का एक सेक्स स्कैंडल देश भर में लोगों को जुबान भी दे सकता है, और खेल संगठनों या प्रशिक्षण कैम्पों को अधिक पारदर्शी भी बनाना चाहिए जहां पर खिलाडिय़ों के लिए परामर्शदाता आएं-जाएं, और उनकी कोई शिकायत है तो वह जल्द सामने आ सके, बजाय इसके कि शोषण करने वाले लोग बरसों तक इस सिलसिले को जारी रखें।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
उत्तरप्रदेश की खबर है कि मोबाइल फोन पर पबजी खेलने की लत के शिकार हो चुके सोलह बरस के एक लडक़े को जब मां ने और खेलने से रोका, तो उसने बाप की पिस्तौल लेकर मां को गोली मार दी, और हत्या के बाद पहुंची पुलिस को इधर-उधर भटकाने की कोशिश भी की। लेकिन पूछताछ के बाद यह साफ हो गया कि उसी ने मां को मारा। इस वारदात के बाद आई खबरों में यह भी याद किया गया है कि मार्च के महीने में महाराष्ट्र के ठाणे में पबजी खेल को लेकर ही दोस्तों में झगड़ा हुआ था, और तीन दोस्तों ने चौथे को चाकू के दस वार करके मार डाला था।
ये तो परले दर्जे की हिंसा के मामले हैं इसलिए खबरों में आ गए हैं, लेकिन डिजिटल उपकरणों, वीडियो गेम्स, और टीवी-फोन पर वीडियो देखने की लत नई पीढ़ी के बच्चों से लेकर जवान लोगों तक सबको बराबरी से तबाह कर रही है, और आज के बच्चे-जवान दिन में अपना जितना वक्त सब इंसानों के साथ कुल मिलाकर गुजारते हैं, उससे कहीं अधिक वक्त वे टीवी और मोबाइल फोन पर गुजारत हैं। नतीजा यह है कि आज फोन ही लोगों का जीवनसाथी हो गया है, वही तुम्हीं हो बंधु, सखा तुम्ही हो, हो गया है। इस सिलसिले के खतरे लोगों को आज समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन भयानक हैं। आज छोटे-छोटे बच्चे कुछ खाते-पीते हुए मोबाइल या टीवी पर कार्टून फिल्में देखने या कोई वीडियो गेम खेलने की जिद पर अड़े रहते हैं, और वे दुनिया के सबसे कमउम्र के ब्लैकमेलर रहते हैं जो कि अपनी बात मनवाए बिना मुंह नहीं खोलते। मां-बाप कामकाजी रहते हैं तो उन्हें अपने काम की हड़बड़ी रहती है, और छोटे-छोटे बच्चे उनके बर्दाश्त को परखते रहते हैं, उन्हें यह अंदाज रहता है कि थक-हारकर मां-बाप उनके सामने समर्पण कर देंगे, और फिर मर्जी की स्क्रीन के साथ वे खा-पीकर मां-बाप पर अहसान करेंगे। दरअसल फोन या टीवी की स्क्रीन बच्चों के दिमाग पर सोचने का बोझ भी नहीं डालती, और फिर वे अपने घर पर मां-बाप को टीवी पर क्रिकेट या दूसरे प्रोग्राम देखते हुए खाते-पीते बैठते देखते हैं, और वही सीखते हैं।
जब तक मरने-मारने की बात न आए तब तक लोगों की नींद नहीं खुलती है, इसलिए अभी लोग इस खतरे की तरफ से मोटे तौर पर अनजान चल रहे हैं, या फिर इस खतरे से जूझना उनके लिए मुश्किल होगा, इसीलिए वे इसे अनदेखा कर रहे हैं। इस देश में मनोचिकित्सकों या परामर्शदाताओं की मौजूदगी उनकी जरूरत के पांच-दस फीसदी भी नहीं है, इसलिए भी लोग बच्चों के सामने सरेंडर करके उन्हें मनमानी करने देते हैं, और स्क्रीन की लत बढ़ते-बढ़ते हिंसा तक पहुंच रही है। जो लोग मरने-मारने पर उतारू हो रहे हैं, या मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करने के लिए कहने पर खुदकुशी कर ले रहे हैं, वे बाकी वक्त भी किस मानसिकता में जी रहे होंगे, इसका एक अंदाज लगाया जा सकता है। इसलिए हत्या-आत्महत्या न होने पर भी लोगों को परिवार के भीतर इस खतरे की तरफ से चौकन्ना रहना चाहिए, और बच्चों का, लडक़े-लड़कियों का स्क्रीन टाइम घटाने की कोशिश करनी चाहिए।
पिछले दो बरस में कोरोना-लॉकडाउन की वजह से बहुत सी पढ़ाई-लिखाई ऑनलाईन हुई है, और पढ़ाई की जानकारी भी बच्चों को इंटरनेट पर तलाशनी पड़ी है। नतीजा यह हुआ है कि छात्र-छात्राओं की स्मार्टफोन या कम्प्यूटर तक पहुंच बढ़ी है, और इंटरनेट की सहूलियत मानो स्याही जितनी जरूरी हो गई। ऐसे में मां-बाप के बस में भी नहीं रहता है कि वे बच्चों को फोन या कम्प्यूटर से पूरे समय रोक सकें, क्योंकि उन पर यह निगरानी भी नहीं रखी जा सकती कि वे पढ़ाई कितनी देर कर रहे हैं, और वीडियो गेम, या वयस्क वीडियो पर कितना समय लगा रहे हैं। वीडियो गेम की वजह से हुई हत्या और आत्महत्या की खबरें अधिक रहती हैं, लेकिन लोगों को याद होना चाहिए कि कुछ महीने पहले ही छत्तीसगढ़ के एक संयुक्त परिवार में एक छोटी सी बच्ची के साथ परिवार के ही पांच-सात नाबालिग लडक़ों ने सेक्स-वीडियो देख-देखकर बलात्कार किया था, और फिर परिवार के लोग ही पुलिस तक पहुंचे थे। इंटरनेट पर बिखरी हुई सनसनी के साथ जीना सीखने में पता नहीं हिन्दुस्तानी समाज के बच्चे कितना वक्त लेंगे। आज तो हालत यह है कि पश्चिम की गोरी चमड़ी के सेक्स-वीडियो से अधिक उत्तेजना देने वाले देसी वीडियो बड़ी रफ्तार से बाजार पर कब्जा कर रहे हैं, और हिन्दुस्तानियों की सेक्स-कल्पनाओं को पंख मुहैया करा रहे हैं।
स्मार्टफोन और कम्प्यूटरों ने किताबों को धकेलकर फुटपाथ पर कर दिया है, और खुद रोजाना की जिंदगी के हाईवे पर तेजी से दौड़ रहे हैं। यह सिलसिला बच्चों के बोलना भी सीखने के पहले से शुरू हो रहा है, और लोगों के वयस्क या अधेड़ हो जाने तक भी चल रहा है। तमाम जिंदगी तो किसी को न रोका जा सकता, न सिखाया जा सकता, लेकिन छोटे बच्चों को तो किसी भी तरह की स्क्रीन से परे रखने के लिए पूरे परिवार को कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसकी बुनियाद ही एक स्क्रीन का कैदी होकर न डले। इसके लिए परिवार के लोगों को बच्चों के लिए वक्त निकालना चाहिए, और बच्चों को ऐसी स्थितियों में रखना चाहिए जहां किसी भी तरह की स्क्रीन उनके सामने ही न आए, या आसपास स्क्रीन रहे भी, तो भी उसकी बजाय कुछ दूसरी अधिक आकर्षक चीजों में बच्चों को उलझाकर रखा जाए। यह मुद्दा बहुत से लोगों को महत्वहीन लग सकता है, और यह भी लग सकता है कि बच्चे तो इसी तरह बड़े होते हैं, लेकिन इस तरह बड़े होते हुए बच्चे कल्पनाशून्य होने लगते हैं, और कई मामलों में वे हिंसक भी होने लगते हैं। इसलिए इस समस्या को मामूली या कम खतरनाक मानकर चलना एक गलती होगी।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत से तथाकथित वीआईपी लोगों की हिफाजत में कटौती की तो अगले ही दिन उस सुरक्षा घेरे के बिना बाहर निकले वहां के एक कांग्रेस नेता और बड़े मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भून दिया गया। और कुछ घंटों के भीतर ही पंजाब के एक बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया के मार्फत इस कत्ल की जिम्मेदारी ली, और कहा कि उसके गिरोह के एक आदमी के कत्ल में इस गायक का मैनेजर शामिल था जिसे इस गायक ने बचाया था, और उसे इसकी सजा दी जा रही है। इसी वक्त अलग-अलग बहुत सी खबरों यह बात आई कि लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में सात सौ लोग शामिल हैं जो कि हिन्दुस्तान से लेकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक बिखरे हुए हैं, और वह जेल के भीतर से जुर्म का अपना साम्राज्य चलाता है।
अगर पंजाब का यह ताजा कत्ल इतना चर्चित नहीं होता, वहां आम आदमी पार्टी की नई-नई बनी सरकार न होती, चर्चित लोगों का सुरक्षा घेरा खत्म न किया गया होता, तो शायद देश के लोगों को यह पता नहीं लगा होता कि पंजाब में इतने बड़े-बड़े गिरोह काम कर रहे हैं। कम से कम खबरों में तो इसके पहले कभी ऐसे गैंगवॉर की चर्चा याद नहीं पड़ती। अब तक पंजाब को लेकर सबसे अधिक चर्चा वहां पर सरहद पार से आने वाले नशे की रहती थी, जिसकी गिरफ्त में पंजाब की नौजवान पीढ़ी बर्बाद बताई जाती है। यह भी शक लोगों को रहता था कि सरहद पार कर कई तरह के हथियार भी पंजाब में घुसते हैं, और इन्हीं तर्कों को लेकर केन्द्र सरकार ने अभी सरहद के किनारे की बहुत चौड़ी पट्टी सीमा सुरक्षा बल के हवाले की है, और राज्य का एक बड़ा हिस्सा राज्य पुलिस के बाहर हो गया है। ऐसा पंजाब अगर अपने पड़ोसी कुछ राज्यों से लेकर दिल्ली तक इतने बड़े मुजरिम गिरोह का भी शिकार है कि जिसके बंदूकबाज कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए हैं, तो फिर सवाल यह उठता है कि ऐसे बड़े गिरोह-सरगना जेल के भीतर से अपना राज कैसे चलाते हैं? जेल के भीतर इन्हें मोबाइल फोन या दूसरी सहूलियतें किस तरह हासिल होती हैं? जब तक जेल का अमला भ्रष्ट नहीं होगा, तब तक कोई मुजरिम वहां से किस तरह सैकड़ों लोगों के अपने गिरोह को चला सकता है? अब यह मामला पंजाब से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, और इन तीन राज्यों की अलग-अलग पुलिस का चौकन्नापन दिल्ली के एक भाजपा प्रवक्ता की गिरफ्तारी और उसकी बलपूर्वक रिहाई में तो सामने आया है, लेकिन जुर्म की ऐसी दुनिया इन्हीं पुलिसवालों की आंखोंतले, और शायद इनकी मेहरबानी से खड़ी हुई है।
लोगों को याद होगा कि पंजाब में धार्मिक और अलगाववादी आतंक का लंबा इतिहास रहा है, और वह बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ था। अब अगर वहां पर इतने बड़े गिरोह काम कर रहे हैं, जो कि इस तरह बेधडक़ ऐसे जुर्म कर रहे हैं, तो यह सरकारों की नालायकी का भी एक सुबूत है, और इतने बड़े गिरोह रातों-रात तो खड़े हुए नहीं हैं। आज हालत यह है कि ये मुजरिम सोशल मीडिया पर अपना पेज चलाते हैं, और उनके लाखों फॉलोअर भी हैं। फिर ऐसे में देश का आईटी कानून क्या हुआ, जो कि एक कार्टून बनाने वाले को तो तुरंत जेल भेज देता है, एक ट्वीट पर राजद्रोह लगा देता है, लेकिन जो ऐसे बड़े गैंगस्टरों को हीरो बनने का मौका देता है। यह एक मामला पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार, और केन्द्र की भाजपा अगुवाई वाली सरकार के लिए एक टेस्ट केस सरीखा है कि हत्या का ऐसा जुर्म सामने आने के बाद, और उसकी जिम्मेदारी लेने के बाद ये सरकारें ऐसे मुजरिमों के गिरोह खत्म करने के लिए क्या करती हैं। हैरानी की बात यह है कि पंजाब की जेलों से लेकर दिल्ली की तिहाड़ जेल तक, हर कहीं ताकतवर मुजरिमों, पैसे वालों, और नेताओं को मोबाइल फोन की सहूलियत हासिल रहती है, और वहां से फोन करके वे बाहर लोगों को धमकाते हैं, उनसे फिरौती और उगाही लेते हैं। आम लोगों को भी यह लगता है कि जिनकी ताकत जेल के भीतर से जुर्म का कारोबार चलाने की है, उनसे कितना उलझा जाए? इसलिए जेल के भीतर मुजरिमों की ताकत उन्हें जेल के बाहर की दुनिया से अधिक ताकतवर बना देती है, और सरकारों को इसका ध्यान रखना चाहिए। पंजाब जैसे नाजुक राज्य को यह भी सोचना चाहिए कि मुजरिमों की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती है, वे किसी के भी हाथ बिक सकते हैं, वे सरहद पार के विदेशी आतंकियों, या वहां की सरकारों के हाथ भी बिक सकते हैं, और बड़े-बड़े गिरोह कब इस देश में साम्प्रदायिक दंगों से लेकर सार्वजनिक हमलों तक के लिए भाड़े पर काम करने लगें, इसका कोई भरोसा तो है नहीं। इसलिए देश-प्रदेश की सरकारों को बड़े अपराधियों के गिरोह खत्म करने के लिए अधिक मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये आज तो एक गायक को मार रहे हैं, कल वे भाड़े पर किसी सार्वजनिक-जानलेवा हमले को तैयार हो जाएं तो उसमें हैरानी क्या रहेगी?
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
भारतीय जनता पार्टी की एक चर्चित नेता नुपूर शर्मा के एक टीवी चैनल पर मोहम्मद पैगंबर के बारे में दिए गए बहुत ही ओछे और हमलावर बयान को लेकर हिंदुस्तान के गैरसाम्प्रदायिक लोगों में भारी नाराजगी है और उस नाराजगी के चलते दूसरे कुछ मुस्लिम देशों में भारतीय सामानों के खिलाफ एक फतवा जारी हुआ है कि उनका बहिष्कार किया जाए। अब इन मुस्लिम देशों के साथ भारत के जो कारोबारी संबंध हैं उनको देखते हुए, या कि बाजार में ग्राहकों से बहिष्कार की अपील को देखते हुए, भारत सरकार ने इनके कूटनीतिक विरोध को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत सांस्कृतिक विरासत और अनेकता में एकता की मजबूत परंपराओं के अनुरूप सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देता है, और अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। सरकार ने यह भी कहा कि इस संबंध में बयान भी जारी किया गया जिसमें किसी भी धार्मिक शख्सियत के अपमान की निंदा करते हुए सभी धर्मों की समानता पर जोर दिया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि यह बयान देने वाले लोग शरारती तत्व हैं, या फ्रिंज एलिमेंट है, जो कि हाशिए पर बैठे हुए लोगों के बारे में कहा जाता है। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि भाजपा की तरफ से अधिकृत रूप से उसकी नेता नुपूर शर्मा टीवी की बहसों में आते रहती हैं और अगर कुछ बरस पहले कि उनकी एक ट्वीट के स्क्रीन शॉट पर भरोसा किया जाए तो नुपूर शर्मा ने बड़े शान के साथ ही यह बखान किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ट्विटर पेज को फॉलो करते हैं। अब ऐसे में भाजपा अपने प्रवक्ता से एकाएक हाथ धो ले उसे शरारती तत्व या फ्रिंज एलिमेंट बतलाए यह आसानी से गले उतरने वाली बात नहीं लगती है। जब अपने लोगों के कुकर्मों और जुर्म से बदनामी और नुकसान सर से ऊपर निकल जाये तो उसे फ्रिंज एलिमेंट कह देना क्या दुनिया को समझ नहीं आता है?
फिर इस सिलसिले में एक बात समझने की जरूरत है कि जिस दिन टीवी चैनल पर अपमानजनक, भडक़ाऊ, और सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला बयान दिया गया उसके बाद से खाड़ी के देशों के विरोध आने तक शायद 2 दिनों से अधिक का वक्त भाजपा के पास था कि वह इस बयान से अपना पीछा छुड़ाती, अपने नेताओं को निष्कासन की चेतावनी देती, अपने नेताओं का निलंबन करती उन्हें पार्टी से निकालती, लेकिन भाजपा की यह प्रतिक्रिया तब जाकर दो-तीन दिन बाद आई, जब खाड़ी के देशों में भारतीय सामानों के बहिष्कार का सिलसिला शुरू हो गया और जब वहां पर भारत के राजदूतों को बुलाकर औपचारिक विरोध दर्ज किया गया कि वे देश मोहम्मद पैगंबर का ऐसा अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा के पास नफरत की आग उगलते अपने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई का जो मौका था, वह मौका तो उसके हाथ से तभी निकल गया जब ऐसे बयान के बाद सोशल मीडिया और मीडिया में लगातार इस बयान के बारे में लिखा गया, पार्टी की जानकारी में यह बयान था लेकिन उसने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, इसे खारिज नहीं किया, इन लोगों को तुरंत पार्टी से नहीं निकाला तो सवाल है कि आज भारत सरकार किस तरह से, सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के दिए गए ऐसे बयान को लेकर एक देश की हैसियत से दूसरे देशों से माफी मांग रही है? ऐसा शायद इस हड़बड़ी में किया गया कि खाड़ी के देशों में मोदी के अपमान वाले पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर छा गए थे। वरना इन बयानों के बाद कानपुर में दंगा भडक़ गया, तब भी पार्टी ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।
यह सत्ता और सत्तारूढ़ पार्टी इन दोनों के बीच ऐसे मेल-मिलाप का मुद्दा है जो कि लोकतंत्र में हो नहीं सकता। अगर भारत सरकार को दूसरे देशों को यह कहना है कि जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, तो यह कड़ी कार्रवाई पार्टी से निलंबन नहीं हो सकती, वह तो राजनीतिक दल के भीतर का मामला है। पार्टी के भीतर से निलंबन का मौका भी पार्टी ने खो दिया 2 दिन 3 दिन के बाद जाकर इनको पार्टी से निलंबित किया या निकाला। अब सवाल यह उठता है कि भारत सरकार को जो संवैधानिक, कानूनी, या सरकारी कार्रवाई इस मामले में करनी थी उनमें से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है तो भारत सरकार का दूसरे देशों को यह कहना कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, यह बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। सरकार कह रही है कि अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। इनके खिलाफ कोई सरकारी या कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, लोगों ने इनके खिलाफ जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है, और अंतरराष्ट्रीय बवाल खड़ा होने के बाद भाजपा ने इन लोगों को, ऐसे 2 नेताओं या प्रवक्ताओं को पार्टी से निलंबित किया है, या निष्कासित किया है। यह पूरा का पूरा सिलसिला एक बहुत ही साफ बात दिखाता है वह यह कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के बिना भाजपा अपने देश के भीतर भी अपने ऐसे बवाली लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। आज तो वह किसी चुनाव में नहीं लगी हुई थी, आज पार्टी के पास इन बयानों के ऊपर विचार करने का पर्याप्त समय था, इन लोगों के ये विचार वीडियो की शक्ल में, और खबरों की शक्ल में चारों तरफ फैले हुए थे, लेकिन पार्टी ने कुछ भी नहीं किया था। यह एक बवाल खड़ा होने के बाद एक अंतरराष्ट्रीय दबाव आने के बाद अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार होने के बाद लिया गया फैसला है, जो कि पार्टी का फैसला है। भारत सरकार को यह साफ करना चाहिए कि ऐसे बयान के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए थी उसका क्या हुआ? इसके साथ साथ ऐसे नेताओं की पार्टी भाजपा को भी यह साफ करना चाहिए कि आज उसने, सरकार ने जिन शब्दों में देश की सांप्रदायिक एकता, सद्भाव, सभी धर्मों के प्रति सम्मान की जो बात कही है, क्या देश में सचमुच ही भाजपा उनको बढ़ावा दे रही है ? इन बातों की रक्षा कर रही है, क्या आज देश में सचमुच ही अल्पसंख्यक लोगों और दूसरे लोगों को संरक्षण मिल रहा है? क्या वे बिना खतरे के जी रहे हैं? यह बात भी समझ लेने की जरूरत है कि आज दुनिया एक बड़े गांव की तरह हो गई है और हिंदुस्तान में जो कुछ होता है उसकी प्रतिक्रिया दुनिया भर में देखने मिल सकती है। भारत में अगर हिंदूवादी ताकतें, हिंदुत्ववादी सरकारें अगर अल्पसंख्यकों को इस तरह से घेर-घेरकर मार रही हैं, अगर उनके रीति-रिवाज पर हमला कर रही हैं, उनके खानपान पर हमला कर रही हैं, उनके आराध्य पर हमला कर रही हैं, तो उन्हें यह बात जान लेना चाहिए कि जिन देशों का शासन इस्लाम के आधार पर चलता है उन देशों में काम कर रहे दसियों लाख हिंदुस्तानियों की नौकरी, उनका भविष्य, उनके परिवार सब कुछ खतरे में पड़ रहे हैं। भारत में हिंसक बकवास करने वाले लोगों को इस बात का अंदाज नहीं है कि वे पूरी दुनिया में किस तरह के खतरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए खड़े कर रहे हैं। एक बार अगर कोई खाड़ी के देशों में जाकर वहां से कमाई करके, वहां काम करके, वहां अपने परिवार को रखकर हिंदुस्तान लौटेंगे, तो वह इस तरह की बकवास नहीं कर सकेंगे। इन तथाकथित राष्ट्रवादियों को यह भी अहसास नहीं है कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों का जीना मुश्किल करके ये मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान के हाथ कितने मजबूत कर रहे हैं।
सरकार को अपनी राजनीतिक पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी को समझ देने की जरूरत है कि देश के भीतर नफरत को इस हद तक बढ़ावा देने से तमाम देशों में हिंदुस्तानियों के लिए मुसीबत आने जा रही है। अभी अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर हिंदुस्तान के खिलाफ एक कड़ी टिप्पणी की है, दुनिया भर की कई संसदों में भारत में अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे हैं हमलों को लेकर फिक्र जाहिर की जा चुकी है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि एक ऐसे देश की बन रही है जहां पर एक धर्म की गुंडागर्दी चल रही है, और दूसरे धर्म को कुचला जा रहा है। तो यह बात तय है कि यहां आने वाला पूंजी निवेश भी घटेगा और हिंदुस्तान की इज्जत तो मटियामेट हो ही रही है। यह मौका भारत सरकार के लिए, और भारत पर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, इन दोनों के लिए गंभीर आत्ममंथन का मुद्दा है। इस देश की, इसके लोगों की और कितनी बेइज्जती दुनिया भर में करवाई जाएगी, या लोगों की संभावनाओं को बाकी दुनिया में किस हद तक खत्म किया जाएगा इन बातों को सोचे बिना महज इन 2 नेताओं-प्रवक्ताओं पर कार्रवाई से बात सुलझने वाली नहीं है, मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। इस मुद्दे की तरफ लोगों का ध्यान गया है, लोगों ने इस पर तंज कैसा है कि क्या सचमुच ही भारत सरकार आज देश में ऐसे माहौल को बढ़ावा दे रही है जैसा कि उसने एक बयान में बखान किया है? क्या सचमुच ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम कर रही है जैसा कि उसने एक बयान में अभी लिखकर जारी किया है? यह तो ऐसा लगता है कि कई देशों के विरोध और भारत के बहिष्कार के खतरे को देखते हुए, नुकसान को कम करने की एक कोशिश के तहत जारी किया गया बयान है जिसका हकीकत और असलियत से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह साफ दिखाई देता है कि ये दोनों बयान जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, यह दोनों बयान महज कागज के दो पन्ने हैं, जिनको आज बड़े अन्तरराष्ट्रीय नुकसान को रोकने के लिए जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत भारत सरकार और भाजपा इन दोनों से यह सवाल किए हैं कि क्या वे सचमुच इन बातों पर भरोसा कर रहे हैं, और अमल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने इन बयानों में लिखा है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उनसे लगातार यह सवाल किए जाएंगे। कहा जाता है कि कोई घड़ा जब पूरा भर जाता है, तब फूटता है, तो भारत में आज सांप्रदायिक तनाव सोच-समझकर साजिश के तहत इस हद तक बढ़ाया जा चुका था कि अब वह घड़ा किसी न किसी एक वजह से फूटना था। अभी फूटा है, इसका मवाद चारों तरफ फैला है, इसे समेटना इतना आसान नहीं है, लेकिन इससे एक मौका मिल रहा है भारत सरकार और भाजपा दोनों को कि अपने तौर-तरीके सुधारें और अपनी पार्टी और अपनी सत्ता को और अधिक बदनामी से बचाएं। देश को तो बचाने की जरूरत आज सबसे अधिक आ खड़ी हुई है, क्योंकि आज देश इन्हीं हरकतों की वजह से खतरे में पड़ा हुआ है। आज देशद्रोह का मुकदमा ऐसे लोगों पर अगर दर्ज नहीं होगा, तो फिर सरकार कुछ भी नहीं करती दर्ज होगी।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)