अंतरराष्ट्रीय

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन डर्मेटोलॉजी की किताबों में नस्लीय प्रतिनिधित्व की कमी साफ तौर पर दिखती है. यह समस्या सिर्फ श्वेत आबादी वाले देशों में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में है.
 डॉयचे वैले पर क्लेयर रोथ की रिपोर्ट-
डॉयचे वैले पर क्लेयर रोथ की रिपोर्ट-
सीये एबिम्बोला 2000 के दशक की शुरुआत में नाइजीरिया में डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे. उस समय उनकी किताबों में त्वचा से जुड़ी जितनी भी तस्वीरें दी गई थीं सबका रंग गोरा था. उनकी ज्यादातर किताबें अमेरिका या ब्रिटेन से आई थीं, जहां चिकित्सा से जुड़ी तस्वीरों में गोरी नस्ल को दिखाया जाता है. जब डर्मेटोलॉजी की बात आई, तो एबिम्बोला पेज पर दिख रही तस्वीरों को हकीकत से नहीं जोड़ पा रहे थे. नाइजीरिया की लगभग पूरी आबादी अश्वेत है. वह, उनके सहपाठी और उनके शिक्षक सभी अश्वेत थे.
एबिम्बोला ने डॉयचे वेले को बताया, "इसके बाद मैंने भारतीय किताबें खरीदीं, क्योंकि मैं यह बात नहीं समझ पा रहा था कि गोरी त्वचा में कोई जख्म कैसा दिखता है और वह काली त्वचा में कैसा दिखता है. इसे लेकर उस किताब में कोई खास जानकारी नहीं दी गई थी. भारतीय किताब के जरिए इस बात को आसानी से समझा जा सकता था. हालांकि, मैंने उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था."
अफ्रीका में एक जैसा अनुभव
दक्षिण अफ्रीका और युगांडा के त्वचा विशेषज्ञों को भी पढ़ाई के दौरान इसी तरह का अनुभव हुआ. दक्षिण अफ्रीका की डर्मेटोलॉजिस्ट नकोजा डलोवा भी जब पढ़ाई कर रही थीं, तो उनकी किताबों की भी ज्यादातर तस्वीरों में गोरी त्वचा दिखाई गई थी. दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त होने के कुछ समय बाद ही 1990 के दशक के अंत में डलोवा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की. वह देश की पहली अश्वेत त्वचा विशेषज्ञ बनीं.
वह कहती हैं, "उन तस्वीरों के जरिए पूरी बात को समझना हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि हमारे ज्यादातर मरीज अश्वेत हैं. अगर हमें बताया जाता है कि किसी व्यक्ति को सोरायसिस (त्वचा से जुड़ी बीमारी) है और उसके शरीर पर सैल्मन के रंग वाला धब्बा हो गया है, तो हमें आश्चर्य होगा. हमें तो पता भी नहीं कि यह धब्बा कैसा दिखता है. हमारे यहां आने वाले अश्वेत रोगियों में सोरायसिस की बीमारी होने पर ऐसा नहीं दिखता है. यह तस्वीर हमारे यहां के रोगियों के हिसाब से सही नहीं है."
वह आगे कहती हैं, "काली त्वचा से जुड़ी कीलॉइड और रंगहीनता जैसी सामान्य समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था. जब उनके बारे में किताबों में जानकारी दी भी गई, तो काफी कम. यह इतनी कम जानकारी थी कि उसके सहारे किसी का इलाज करना भी संभव नहीं था."
दक्षिण अफ्रीका की एक अन्य डर्मेटोलॉजिस्ट सेबी सिबिसी ने भी पढ़ाई करते समय कुछ इसी तरह का अनुभव किया. वह कहती हैं कि उनकी किताबों में दिखाई गई 95 फीसदी तस्वीरें गोरी त्वचा की थीं. वह डॉयचे वेले को बताती हैं, "अश्वेत लोगों को हाइपरपिंग्मेंटेशन (त्वचा पर काले धब्बे) की काफी समस्या होती है. हमारे यहां लगभग हर दिन ऐसे मरीज आते हैं जो चेहरे के धब्बे, जांघ के नीचे गहरे काले धब्बे जैसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इनका इलाज कैसे करना है. हमें इसके बारे में विश्वविद्यालय में कभी बताया ही नहीं गया."
कम प्रतिनिधित्व और शोषण
वर्ष 2021 के सितंबर महीने में एक जर्मन अध्ययन प्रकाशित हुआ है. इसके लिए जर्मन डॉक्टरों द्वारा पिछले चार वर्षों में जर्मन भाषा में प्रकाशित की गईं डर्मेटोलॉजी की 17 किताबों में छपीं 5,300 तस्वीरों का मूल्यांकन किया गया. जर्मन डॉक्टरों ने इन किताबों के जरिए त्वचा के अलग-अलग रंग के बारे में जानकारी देने के लिए फिट्जपैट्रिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया है.
अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि 91 फीसदी तस्वीरों में गोरी त्वचा, 6 फीसदी में मध्यम या जैतून के रंग की त्वचा, और 3 फीसदी से भी कम में भूरी त्वचा दिखाई गई है. टाइप 6 वाले सबसे गहरे रंग की त्वचा वाली सिर्फ एक तस्वीर मिली. 2021 में एक अमेरिकी किताब का भी विश्लेषण किया गया था. उसके नतीजे भी इसी से मिलते-जुलते हैं. उसमें भी सिर्फ 14 फीसदी तस्वीरें गहरे रंग की त्वचा की थी.
डलोवा कहती हैं कि उन्होंने पढ़ाई करते समय शायद ही अपनी किताबों में गहरे रंग की त्वचा की कोई तस्वीर देखी थी. उन्होंने कहा कि यौन संचारित रोगों के बारे में पढ़ाई करते समय भी उनके लिए यह असामान्य बात नहीं थी. ये रोग भी सबसे पहले त्वचा को ही प्रभावित करते हैं.
सिफलिस यौन संचारित रोगों में से एक है. यह बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है जो यौन संपर्क की वजह से फैलता है. इस रोग को लेकर हुए अमेरिकी शोध के दौरान अश्वेत लोगों का शोषण किया गया था. 1930 के दशक में अमेरिकी सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों ने इस बीमारी के बारे में जानने के लिए सैकड़ों अश्वेत पुरुषों पर प्रयोग किया. उस समय तक इस बीमारी के उपचार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. इस अध्ययन को बाद में कुख्यात ‘टस्केगी सिफलिस एक्सपेरिमेन्ट' नाम दिया गया.
अगले 15 वर्षों में शोधकर्ताओं ने पाया कि पेनिसिलिन को सिफलिस के इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अश्वेत पुरुषों को पेनिसिलिन की खुराक नहीं दी गई. डॉक्टर देखना चाहते थे कि यह बीमारी किस तरह इंसानों को मौत के मुंह में ले जाती है. 1970 के दशक की शुरुआत में एक रिपोर्टर ने इस प्रयोग का खुलासा किया. तब तक दो दर्जन से अधिक पुरुषों की मौत हो गई थी. कई अन्य पुरुष अपने परिवार के लोगों को भी इस बीमारी से ग्रसित कर चुके थे.
सिस्टम का असर
ऑस्ट्रेलिया में सिडनी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्वास्थ्य प्रणाली के शोधकर्ता और वरिष्ठ व्याख्याता एबिम्बोला ने कहा कि 1940 के दशक के अंत में अमेरिका में टस्केगी एक्सपेरिमेन्ट पर काम चल रहा था. इसी दौरान अंग्रेजों ने नाइजीरिया में पहला मेडिकल स्कूल स्थापित किया था.
एबिम्बोला ने डीडब्ल्यू को बताया, "उस समय औपनिवेशिक शासन था. स्कूल की स्थापना करने वालों ने अपने मुताबिक पाठ्यक्रम तैयार किया. वे चाहते थे कि इस स्कूल से पढ़ाई करने वाले डॉक्टर ब्रिटेन में प्रैक्टिस करें." इसका साफ मतलब था कि डॉक्टरों को नाइजीरिया के बजाय ब्रिटेन में होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए तैयार किया गया था.
एबिम्बोला कहते हैं, "आप 1948 के नाइजीरिया और ब्रिटेन की कल्पना कर सकते हैं. आपको यह तय करना होगा कि आप डॉक्टर को किस लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं. अगर आप उन्हें ब्रिटेन में इलाज करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि आप नहीं चाहते कि वे नाइजीरिया में रोगियों का इलाज करें." उन्होंने कहा कि 1960 में देश को आजादी मिलने के बाद भी, नाइजीरियाई मेडिकल स्कूल में किस तरह ट्रेनिंग और पढ़ाई हो, इस तर्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
स्थानीय विशेषज्ञ की जरूरत
एक बार यूरोपीय डर्मेटोलॉजिस्ट से मुलाकात के दौरान डलोवा ने देखा कि उस डर्मेलॉजिस्ट को अफ्रीका के लोगों की त्वचा से जुड़ी सामान्य समस्याओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है. उसके पास कांगो का एक मरीज इलाज के लिए गया था. वहां का कर्मचारी इलाज के सिलसिले में मरीज का बायोप्सी करना चाहता था.
डलोवा ने इस बीमारी की पहचान तुरंत कर ली. वह बीमारी थी सारकॉइडोसिस. यह एक गंभीर बीमारी है जिससे त्वचा पर लाल या बैंगनी रंग के धब्बे उभर आते हैं. इससे त्वचा पर जख्म होने का खतरा बढ़ जाता है और त्वचा के नीचे दाना भी हो सकता है. डलोवा ने उनसे कहा, "यह सारकॉइडोसिस है. आपको बायोप्सी करने की जरूरत नहीं है."
डलोवा ने कहा कि मेडिकल जर्नल को त्वचा से जुड़ी इन समस्याओं के बारे में लिखने के लिए अफ्रीका के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना चाहिए. वह कहती हैं, "उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए जिसे इन सब के बारे में जानकारी नहीं है. उन्हें अमेरिकन या यूरोपीय डर्मेटोलॉजिस्ट की जगह इन बीमारियों के बारे में पूरी तरह जानकारी रखने वाले अफ्रीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए."
जब डलोवा, एबिम्बोला और सिबिसी मेडिकल स्कूल में थे, उस समय की तुलना में चीजें अब बदलने लगी हैं. डलोवा ने 2017 में ‘डर्मेटोलॉजी: अ कॉम्प्रिहेंसिव हैंडबुक फॉर अफ्रीका' नामक पुस्तक प्रकाशित की. साथ ही, वह ऐसे अंतरराष्ट्रीय दल का हिस्सा भी रह चुकी हैं जिसने 2019 में ऐसे जीन की खोज की जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि अश्वेत महिलाओं के बाल क्यों झड़ते हैं.
नाइजीरियाई मेडिकल छात्र चिडीबेरे इबे की एक तस्वीर दिसंबर 2021 में वायरल हुई थी. इस चित्र में मां के गर्भ में अश्वेत बच्चे को दिखाया गया था. दुनिया भर के लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी त्वचा के रंग को चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली तस्वीर में देखा.
पिछले महीने इबे ने घोषणा की कि उन्होंने डर्मेटोलॉजी की ऑनलाइन किताब ‘माइंड इन गैप' की तस्वीरें बनाने की योजना बनाई है. इस किताब को 2020 में यूके में लॉन्च किया गया था. यह किताब ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर उपलब्ध उन संसाधनों में से एक है जिसमें पूरी तरह काली त्वचा से जुड़ी जानकारी दी गई है. (dw.com)



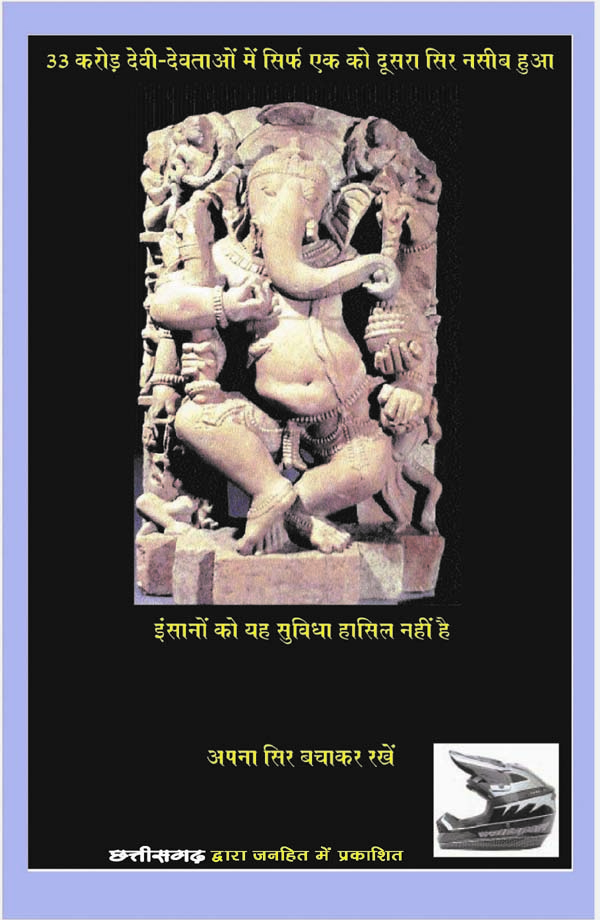




.jpg)




.jpg)












.jpg)
.jpg)
.jpg)















.jpg)

.jpg)



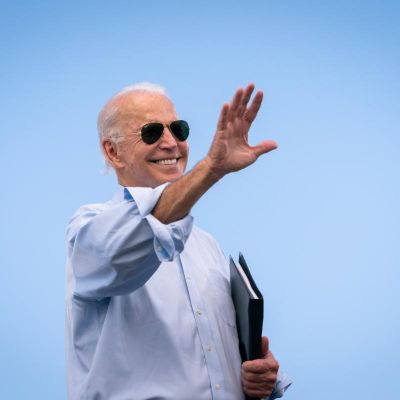
.jpg)











