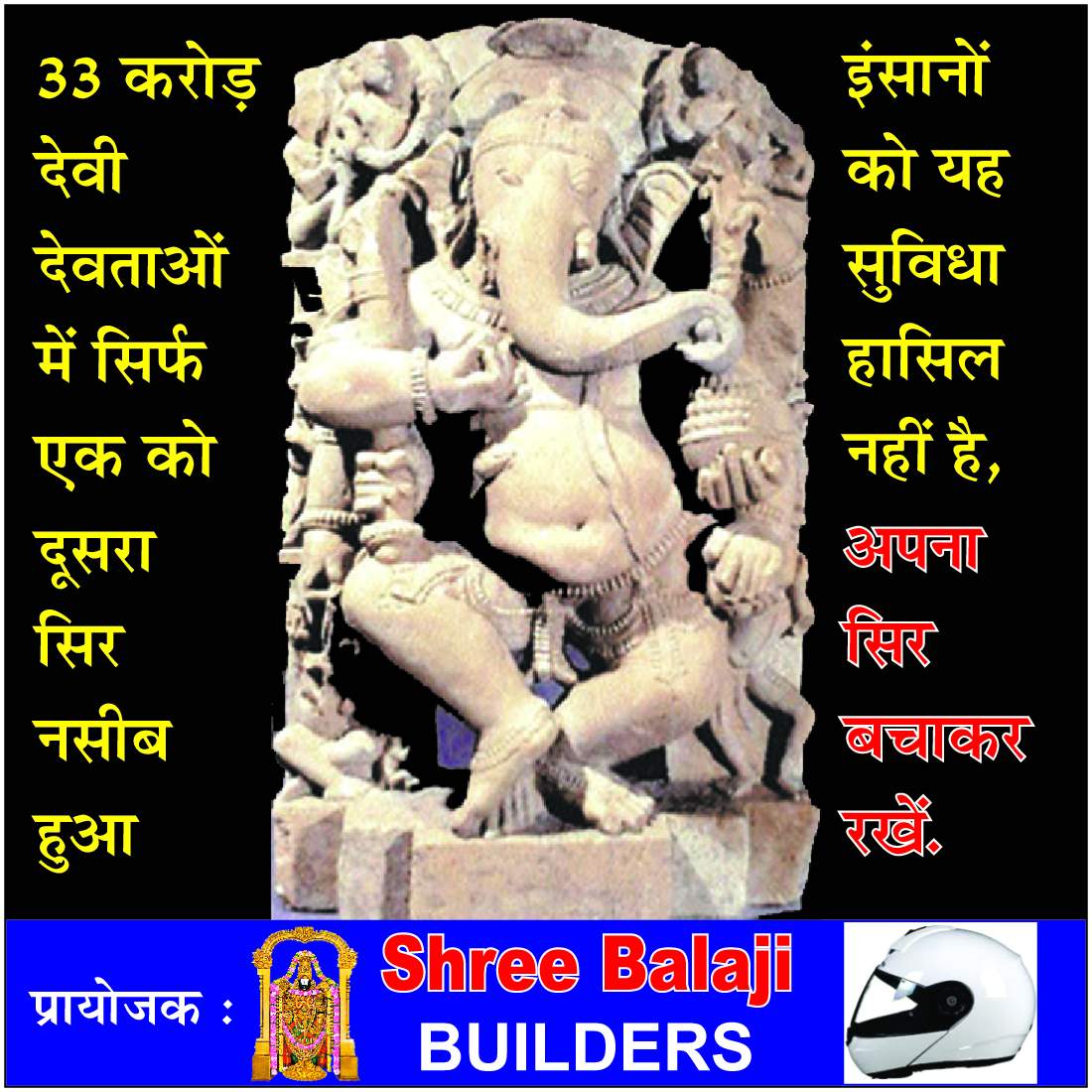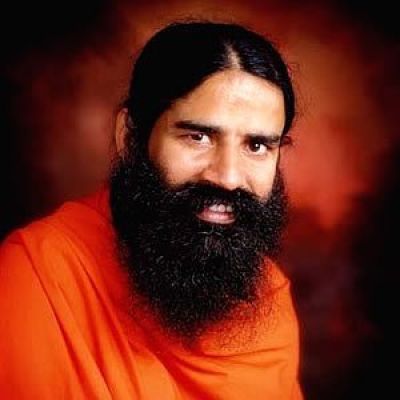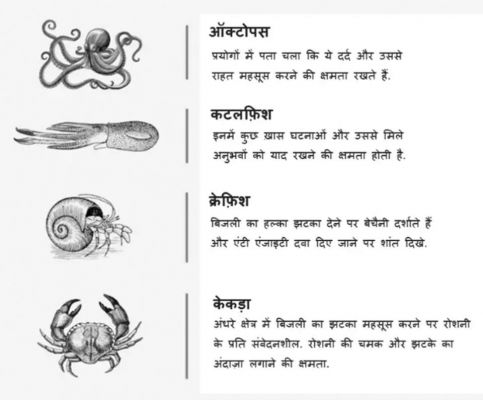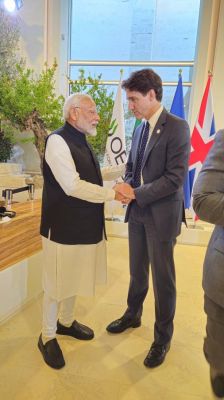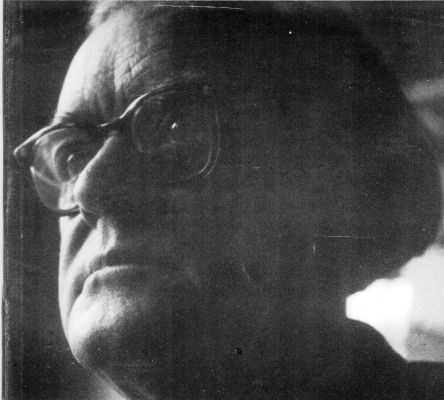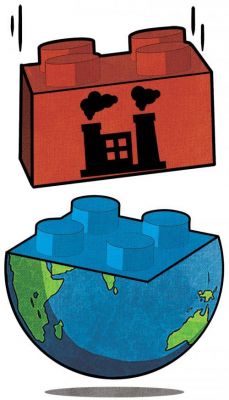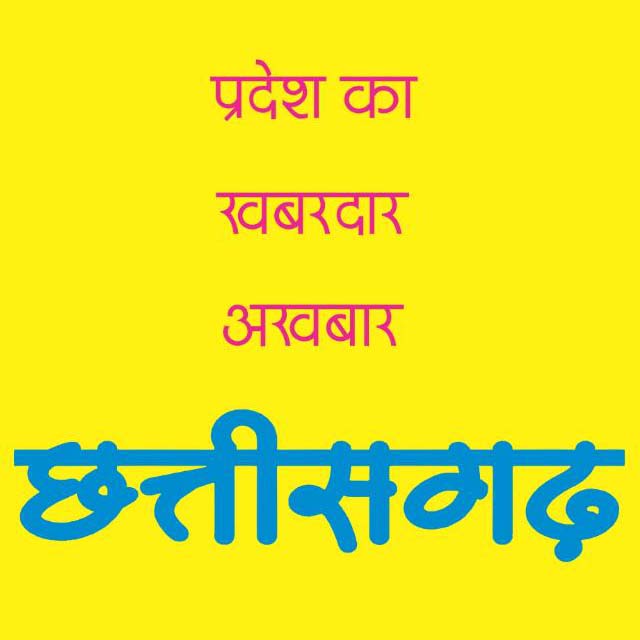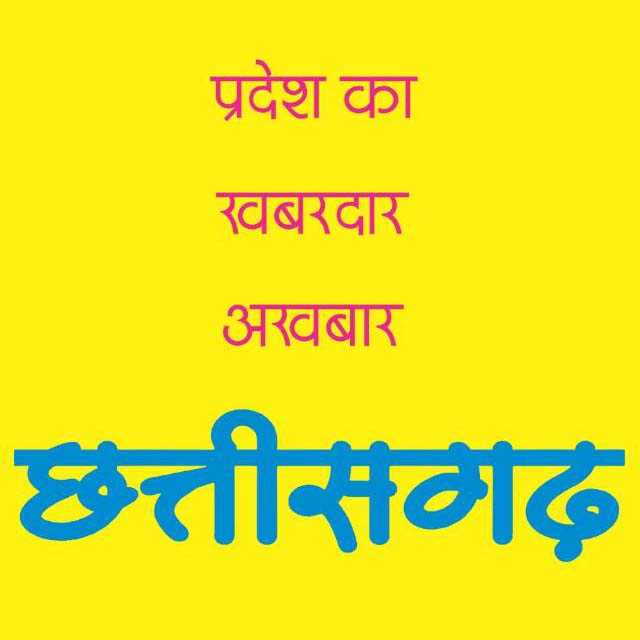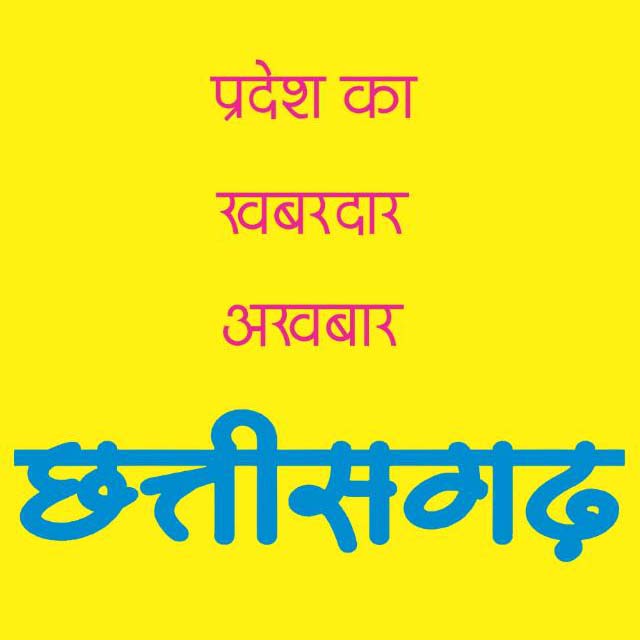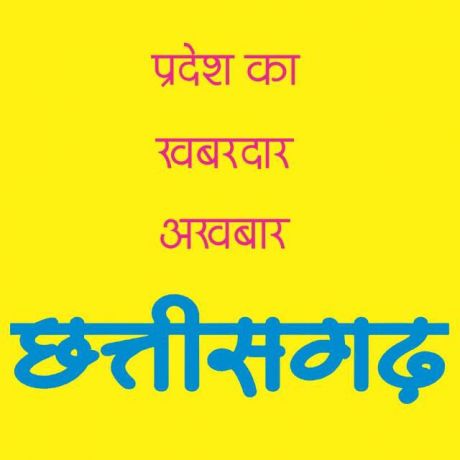विचार / लेख

photo : KIMSHI LHAINEIKIM
-इमरान कुरैशी
भारत के पूर्वोत्तर राज्य नगालैंड के एक शख़्स दक्षिण भारत के केरल में स्वास्थ्य सुविधाओं के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ये शख़्स हैं डॉ. विसाज़ो कीची, जिनका मलयालम में बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
विभिन्न उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडरों के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं है कि वो अपने वीडियो को कई स्थानीय भाषाओं में डब करते हैं। लेकिन नगालैंड की राजधानी कोहिमा के रहने वाले 29 साल के डॉ. विसाज़ो कीची का मामला कुछ अलग है। वे धाराप्रवाह मलयालम बोलते हैं। हालांकि वो यह भी मानते हैं कि ये बहुत कठिन भाषा है।
कीची ने बीबीसी हिंदी से कहा, ‘अगर आप डॉक्टर हैं तो ये मजबूरी हो जाती है क्योंकि आपको अपने मरीजों से बात करने के लिए भाषा सीखनी पड़ती है।’
जब अगस्त 2013 में डॉ. कीची कोझिकोड पहुंचे तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने वाले वो पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति थे। इसके दो साल बाद ही पूर्वोत्तर से लोगों का वहां आना शुरू हुआ। कई लोगों के लिए ये ‘दूसरा घर’ बन गया है।
केरल में प्रवासी मजदूर
केरल के बारे में उनकी हिचक तब गायब हो गई जब उनके अध्यापक और सहपाठी बहुत मददगार साबित हुए, जैसा कि कोहिमा में उनके मलयाली पड़ोसी ने उन्हें आश्वस्त किया था।
डॉ. कीची ने कोझिकोड में अपना एमबीबीएस कोर्स पूरा किया और तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सर्जरी की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में दाखिला लिया। उनके लिए केरल शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में मॉडल राज्य है।
वे कहते हैं, ‘अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो भी अस्पताल में बेधडक़ जा सकता है और राज्य कि विभिन्न योजनाओं के तहत अपना इलाज करा सकता है।’
लेकिन जो बात डॉ। कीची को ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, वो है केरल का ख़ुद को एक ऐसे राज्य के रूप में दिखाने का दृढ़ संकल्प जहां ‘किसी भी भारतीय के पढऩे, काम करने और रहने का स्वागत है।’
जैसा कि एक अधिकारी ने कहा, यह राज्य बार-बार साबित करना चाहता है कि यह ‘ईश्वर का अपना देश है’, जो कि राज्य की लोकप्रिय टैगलाइन भी है।
‘सभी का स्वागत’
एक्सपर्ट केरल सरकार के इस नीतिगत फैसले के पीछे कई कारण बताते हैं।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन प्रवासी मज़दूरों को मेहमान वर्कर बताते हैं। सभी के स्वागत वाला बोर्ड लगाना राज्य की मजबूरी है ताकि राज्य से बाहर जाने वाली मलयाली मजदूरों की आबादी के साथ यहां आने वाले प्रवासी मजदूरों का संतुलन बिठाया जा सके।
केरल से लोग, खासतौर पर 20 से 40 साल की उम्र वाले, दूसरे देशों में रोजग़ार के लिए जाते हैं और वहां से वो पेट्रोडॉलर या अन्य विदेशी मुद्राएं भेजते हैं जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था चलती है और यह सालाना एक लाख 10 हजार करोड़ रुपये की राशि है।
केरल में उनके परिवारों को घर बनाने, बिजली के काम करने, बढ़ई, खेत और औद्योगिक मजदूर आदि के रूप में मानव संसाधन की जरूरत है।
1980 के दशक से 2000 की शुरुआत तक केरल में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूर आते थे। बीते दो दशक से यहां बंगाल, असम, बिहार, पूर्वोत्तर और उत्तरी राज्यों के लोग आने लगे हैं।
सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड इन्क्लूसिव डेवलपमेंट के डायरेक्टर बेनॉय पीटर ने बीबीसी हिंदी से कहा, ‘दिहाड़ी मज़दूरों में 40 प्रतिशत बंगाल से और 20 प्रतिशत असम से आते हैं जबकि बाकी ओडिशा और अन्य पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय आदि से आते हैं।’
हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर जजाति के पारिदा बताते हैं कि क्यों अन्य राज्यों से कुशल और अकुशल मजदूर केरल आ रहे हैं।
वे कहते हैं, ‘उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जो लोग कृषि में रोजगार खो रहे हैं, वे ही प्रवास कर रहे हैं।’
‘वे केरल में मजदूरी को लेकर भी आकर्षित हो रहे हैं। अगर ओडिशा की बात करें तो वहां के मुकाबले केरल में करीब-करीब चार से पांच गुना मजदूरी है।’
अन्य राज्यों से अधिक मजदूरी
पारिदा ने कहा, ‘अगर ओडिशा में 200 रुपये दिहाड़ी है तो केरल में 800 रुपये है। बड़े पैमाने पर मजदूरों के यहां आने की प्रमुख वजह यही अंतर है। केरल की अर्थव्यस्था में उनका बड़ा योगदान है। उनके बिना, केरल की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।’
पारिदा ने केरल प्लानिंग बोर्ड के सदस्य डॉ. रवि रमन के साथ मिलकर 2021 में एक अध्ययन ‘ऑन माइग्रेशन, इनफॉर्मल एम्प्लायमेंट एंड अरबनाइजेशन इन केरला’ का सह लेखन किया।
पारिदा ने कहा कि अध्ययन दिखाता है, ‘बहुत कम जगहें हैं जहां औसत आमदनी थोड़ी बहुत कम थी। कुछ जगहें ऐसी थीं जहां स्थानीय लोगों का बर्ताव प्रवासी मज़दूरों के साथ अच्छा नहीं था लेकिन कुल मिलाकर संबंध अच्छे थे। चंद जगहों पर स्थानीय लोगों को प्रवासी मज़दूर स्थानीय मजदूरों के मुक़ाबले अधिक बेहतर लगे। प्रवासी मज़दूर 30 मिनट ज़्यादा काम करते थे जबकि स्थानीय मज़दूर इनकार कर देते थे।’
पीटर ने कहा कि 2017-18 में केरल में 31 लाख प्रवासी मज़दूर थे। 17.5 लाख प्रवासी मजदूर निर्माण में, 6.3 उद्योग में, 3 लाख खेती और उससे जुड़ी सेवाओं में, 1.7 लाख सेवा क्षेत्र में, एक लाख रिटेल या होलसेल व्यापार में और 1.6 लाख अन्य नौकरियों में थे।
अध्ययन के मुताबिक, ‘औसतन भुगतान की सूचनाओं के आधार पर अनुमान है कि केरल से हर साल 7.5 अरब रुपये अन्य राज्यों को जाता है।’
लेकिन पीटर केरल सरकार के ताजा प्रस्ताव से असहमति जताते हैं, ‘ऐसी खबरें हैं कि पुलिस प्रवासी मजदूरों से उनके राज्य से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट चाहती है। ये सिर्फ इसलिए कि बमुश्किल एक या दो प्रतिशत लोग अपराध में संलिप्त होते हैं। केरल को ये नहीं करना चाहिए। उसे दुनिया को दिखाना चाहिए कि बाकी जगहों पर मलयालियों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए।’
प्रवासी स्टूडेंट
जब बीती तीन मई को मणिपुर में हिंसा शुरू हुई तब भी केरल सरकार ने ‘सबका स्वागत’ वाली नीति को जारी रखा।
एंथ्रोपोलॉजी (मानव शास्त्र) के 25 साल की पीएचडी स्डूडेंट किमशी लहैनीकिम ने मणिपुर की राजधानी इम्फ़ाल में ‘भयावह अनुभव’ के बाद एक महीने पहले ही कन्नूर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
उन्होंने बीबीसी को बताया, ‘जब हिंसा शुरू हुई उस समय मैं एक किराए के कमरे में रहती थी जबकि मेरे माता पिता चुराचांदपुर में थे। हमने ऐसे नारे सुने कि सभी कुकी को मार डालो। चार मई को हम डीजीपी के घर पहुंच गए। हम 300 लोग थे और इसके बावजूद हम पर दिनदहाड़े हमला हुआ। शाम को जब डीजीपी लौटे, हम सभी को मणिपुर राइफल्स कैंप में भेज दिया गया।’
किमशी ने बताया, ‘बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को विदाई देना शुरू कर दिया क्योंकि हमें यकीन नहीं था कि हम भीड़ के हाथों बच पाएंगे।’
किमशी और उनके दूसरे साथी किसी तरह 9 मई को इम्फाल से निकलने में कामयाब होकर दिल्ली पहुंचे जहां उन्होंने नौकरी तलाश करनी शुरू कर दी।
उन्होंने बताया, ‘मुझे एक कॉल सेंटर में नौकरी भी मिल गई। कुकी स्टूडेंट आर्गेनाइजेशन की अपील पर केरल पहला राज्य था जिसका जवाब आया। बिना दोबारा सोचे मैं अपना अध्ययन पूरा करने कन्नूर चली आई। मैंने कभी सुना था कि मेरे हाईस्कूल के कुछ टीचर यहीं के थे।’
किमशी और 34 अन्य छात्रों को उनके मोबाइल पर मौजूद दस्तावेजों के आधार पर एडमिशन दे दिया गया, ‘फीस अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे।’
किमशी को जो सबसे अच्छी बात लगी कि यहां के लोग ‘बहुत सरल और मेहमानवाज़ हैं। और हम यहां सुरक्षित महसूस करते हैं। केरल सरकार और विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों ने जो हमें मौके मुहैया कराए हम उसके बहुत आभारी हैं। यहां के लोगों ने जो प्यार बरसाया, उसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं।’
राज्य में 81 प्रतिशत प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा मिलती है। हाल के महीनों में पायल कुमारी ने प्रवासी समुदाय का नाम ऊंचा किया जब उन्होंने कुछ महीने पहले डिग्री परीक्षा में पहला रैंक हासिल किया। अर्नाकुलम में एक पेंट शॉप में सेल्समैन का काम करने वाले की बेटी पायल का जन्म बिहार में हुआ और पालन पोषण केरल में हुआ क्योंकि उनके पिता यहीं बस गए थे।
पायल ने बीबीसी हिंदी को बताया, ‘जब पत्रकारों ने मेरा साक्षात्कार लिया तो वो ये देख कर हैरान हुए और खुश हुए कि मैं मलयालम बोल लेती हूं। एक बार आपको मलयालम आ गई तो आप यहां स्वीकार लिए जाते हैं।’
पायल का भाई एक एनजीओ में फ़ाइनेंस अधिकारी है और उनकी बहन पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही है। पायल इस समय सिविल सेवा की तैयारी कर रही हैं।
डॉ.कीची ने कहा, ‘मैं हमेशा कहता हूं कि केरल को अनुभव करने के लिए आपको यहां की संस्कृति और भाषा सीखनी पड़ेगी।’ अगले महीने भारतीय रेलवे में नौकरी जॉइन करने के लिए वो वडोदरा, गुजरात जा रहे हैं। (bbc.com/hindi)