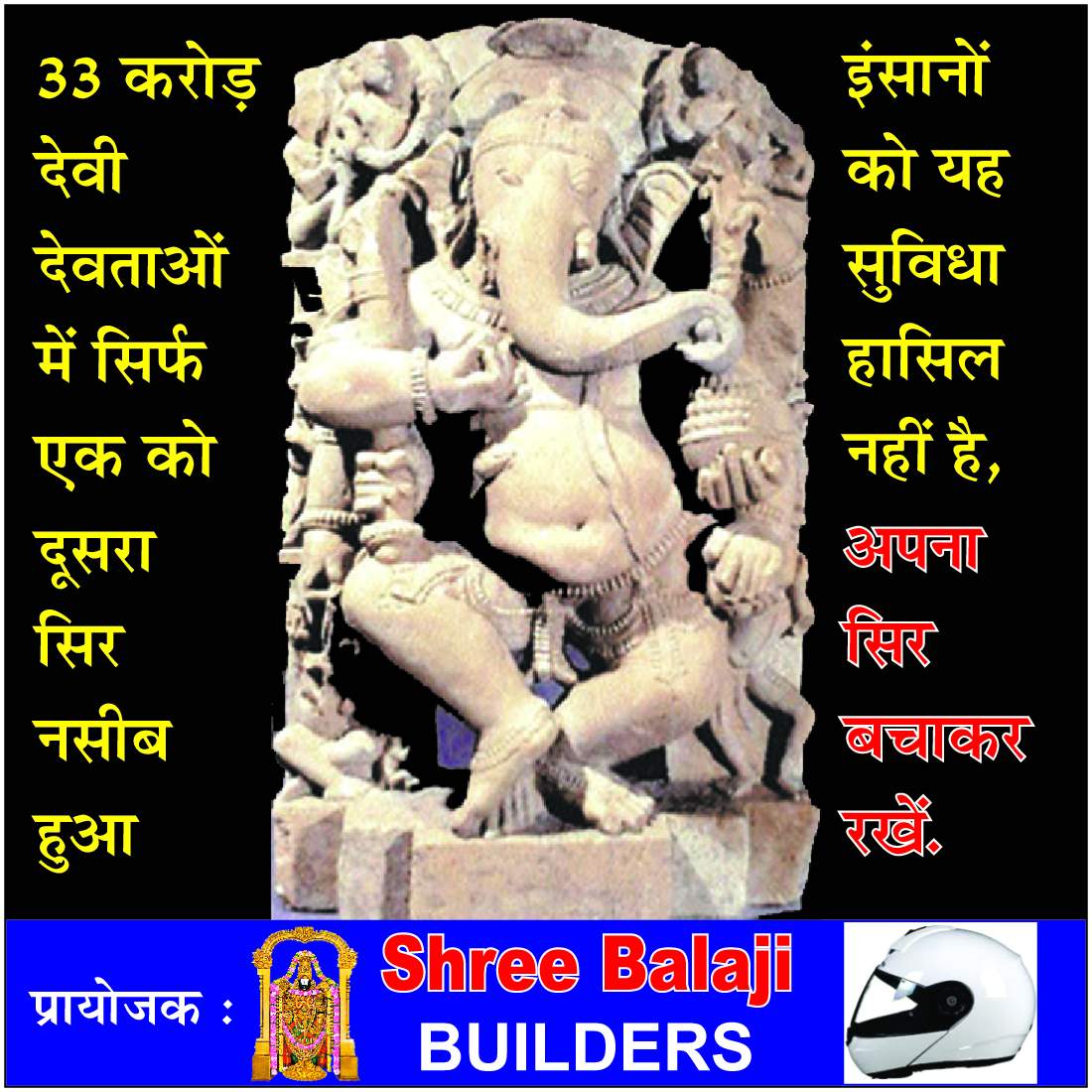संपादकीय
मुम्बई में कल आई तेज आंधी से एक पेट्रोल पंप के करीब बड़ा सा होर्डिंग गिरा, और उसके नीचे दबकर 14 मौतें हो गईं, इनके अलावा करीब 60 लोग जख्मी हो गए हैं जिनमें से 43 अस्पताल में भर्ती हैं। अब यह सब हो जाने के बाद बड़े पैमाने पर बचाव चल रहा है क्योंकि इसके नीचे बड़ी संख्या में लोग और गाडिय़ां दब गए थे। मुख्यमंत्री रात में हादसा देखने मौके पर पहुंचे और कहा कि मुम्बई में जितने भी होर्डिंग हैं उसका स्पेशल स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा। इस हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का जुर्म भी दर्ज किया जा रहा है। किसी भी बड़े शहर में होर्डिंग अंधाधुंध कमाई का जरिया रहती है, और एक-एक होर्डिंग का दसियों लाख रूपए महीने का भाड़ा रहता है। स्थानीय म्युनिसिपल से लेकर सडक़ किनारे की जगहों की मालिक राज्य सरकार, और पुलिस जैसे कई विभाग होर्डिंग के कारोबार में दखल रखते हैं, और इनमें भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहता है। हम अपने ही शहर, राजधानी रायपुर में देखते हैं जहां हजारों होर्डिंग अवैध लगी हुई हैं, और हर कुछ बरस में म्युनिसिपल उनको नोटिस देने की बात करती है, लेकिन बाद में मामला रफा-दफा हो जाता है।
देश और दुनिया में किसी एक जगह ऐसी ठोकर लगे जैसी दहलीज दूसरी जगहों पर भी है, तो बाकी लोगों को ठोकर लगने के पहले सावधान हो जाना चाहिए। अधिकतर शहरों में जब तूफान आता है तो होर्डिंग बिजली के तारों पर गिरते हैं। तेज आंधी-तूफान में बहुत से पेड़ भी बिजली के तारों पर गिरते हैं, खंभे गिर जाते हैं, तार टूट जाते हैं, और मानो इतनी तबाही काफी नहीं रहती, होर्डिंग उसमें और इजाफा कर देते हैं। होर्डिंग का फ्लैक्स फटकर तारों से लिपट जाता है, और कई तरह के खतरे खड़े करता है। लेकिन वैध और अवैध ऐसे होर्डिंग जिन खंभों पर लगे रहते हैं, जिन छतों पर उन्हें खड़ा किया जाता है, उनकी मजबूती का कोई ठिकाना नहीं रहता, और बहुत मामूली समझ वाले म्युनिसिपल-इंजीनियर इन्हें सर्टिफिकेट दे देते हैं। जबकि मौसम की मार हर बरस अधिक तेज होती जा रही है, अधिक बार होती जा रही है, और कितने आंधी-तूफान के हिसाब से ये होर्डिंग खड़े किए जाते हैं, वे बिजली के तारों से कितने दूर रखे जाते हैं, और उनके टूटकर गिरने या उडऩे से वे कितनी दूर तक खतरा खड़ा कर सकते हैं, इसका हिसाब शायद ही म्युनिसिपल के इंजीनियर लगाते होंगे। राज्य सरकारों को चाहिए कि मुम्बई के इस हादसे को देखते हुए अपने-अपने शहरों में इस कारोबार की हिफाजत की जांच कर लें। हमें तो पहली नजर में ही यह दिखता है कि अनगिनत होर्डिंग ऐसे हैं जो अगर गिरे तो बिजली के तारों में उलझेंगे, और किसी प्राकृतिक विपदा की हालत में मुसीबत को और कई गुना बढ़ा देंगे।
होर्डिंग के पूरे धंधे को देखें, तो इसमें कुछ भी जनहित का, और जनसहूलियत का नहीं है। यह एक विशुद्ध कारोबार है जिसे सार्वजनिक जगह पर, जनसुरक्षा के पैमानों पर कोई रियायत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हालत यह है कि इस धंधे में लगे हुए हजारों अवैध होर्डिंग खुद सरकारें भाड़े पर लेती हैं, और इनसे अवैध होर्डिंग्स को भी एक किस्म की हिफाजत मिल जाती है। यह सिलसिला खत्म करना चाहिए, और हर म्युनिसिपल के अफसरों को, या निर्वाचित नेताओं को यह देखना चाहिए कि अपने इलाके में वे इस निहायत गैरजरूरी कारोबार से तबाही का खतरा कैसे घटा सकते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
अमरीका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने 30 बरस तक चला एक लंबा अध्ययन किया और इसमें एक लाख से अधिक बालिग लोगों के खानपान को देखा गया। ये तमाम वे लोग थे जो बाजार में बने या पके हुए प्रोसेस्ड फूड खाते थे, और इनमें इस्तेमाल होने वाले नमक, शक्कर, फैट, और रसायनों की वजह से उन पर मौत का खतरा ऐसा खानपान न करने वाले लोगों के मुकाबले 9 फीसदी अधिक मिला। यह आंकड़ा कम नहीं होता है क्योंकि बाकी पैमाने बराबर रहने पर भी अगर ऐसे खानपान से तकरीबन 10 फीसदी अधिक मौतें हुई हैं, तो मौत से परे के दूसरे खतरों को भी देखा जा सकता है। अमरीकी बाजार में जिसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है, वहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उसे नियमित रूप से खाते रहता है। बहुत से कामकाजी लोग, और घर के बाहर खाने वाले लोग इसी तरह की चीजों को खाकर जिंदा रहते हैं, इनके अलावा अनगिनत अमरीकी परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में नाश्ते से लेकर खाने तक इसी तरह कारखानों में बने सामान इस्तेमाल होते हैं, और वे स्वाद को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के रसायनों की साजिश वाले तो रहते ही हैं, वे अपने पैकिंग में तरह-तरह की जालसाजी से उसमें इस्तेमाल हानिकारक चीजों को या उनकी मात्रा को छुपाते हैं। यह बात तो अमरीका और यूरोप के विकसित और जागरूक देशों में भी होती हैं, भारत जैसे कारोबारी-दबाव वाले देश में बहुत ही बुरा हाल है।
हम समय-समय पर बाजारू खानपान के बारे में सावधान करते रहते हैं। आज छोटे-छोटे बच्चों के दूध पावडर, और घरेलू दलिया के उनके बाजारू विकल्प में अंधाधुंध शक्कर मिली पाई गई है। यह भी पाया गया है कि यही कंपनी अमरीका और योरप में ऐसी गड़बड़ी नहीं करती, क्योंकि कानून वहां कड़ा है। हिन्दुस्तान को तो मानो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी मनमानी का अड्डा बना लिया है क्योंकि यहां की भ्रष्ट सरकारों से किसी भी तरह की बाजारू छूट ले लेना बड़ा आसान है। यहां पर खानपान के सामानों की पैकिंग पर चेतावनियां उस तरह से नहीं लिखी जातीं जिस तरह किसी भी विकसित और जागरूक लोकतंत्र में यही कंपनियां करती हैं। कायदे की बात तो यह है कि सेहत की सावधानी एक जगह सुझाने और दूसरे जगह न सुझाने को मासूम नहीं माना जा सकता, और ऐसी कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी, और इसके साथ-साथ जनता की सेहत को खतरा खड़ा करने के जुर्म में भी अदालत में घसीटना चाहिए।
दुनिया में सबसे अच्छा खाना घर पर बना हुआ, घरेलू या आम सामानों से पकाया हुआ खाना रहता है। लेकिन अब तो हिन्दुस्तान के कस्बाई शहरों तक में घर पर खाना पहुंचाने वाली कंपनियों का कारोबार इतना फैल चुका है कि चटपटा और रासायनिक-जायकेदार खाना मंगाकर खाने का चलन बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर लोग इतना खर्च उठा पाते हैं, तो वे पकाने की जहमत से बच भी जाते हैं। इन सबके चलते हुए बाजार का पका खाना, और बाजार से डिब्बाबंद आने वाले सामानों को बड़ा साफ-सुथरा और सेहतमंद मान लिया गया है। बचपन से ही दूध पावडर से लेकर बेबी फूड तक का इस्तेमाल डॉक्टर और सरकार दोनों की चेतावनियों के बावजूद अंधाधुंध किया जाता है। जिन बच्चों को मां की दूध पर ही रहना चाहिए, उन्हें भी बाजार के हवाले कर दिया जाता है। हालत इतनी खराब हो गई है कि गरीब मजदूरों के बीच भी अपने बच्चों के लिए बाजार में मिलने वाले नमकीन या मीठे सामानों के पैकेट खरीदकर बच्चों को चुप करवाना अधिक सहूलियत का काम हो गया है, क्योंकि उन्हें भूख लगने पर उनके लिए उसी वक्त समय निकाल पाना हर मजदूर मां के लिए मुमकिन नहीं होता है। एकदम बचपन से ही बाजार के अतिरिक्त शक्कर-नमक पर टिके रहने वाले बच्चे हिन्दुस्तान में कमउम्र में डायबिटीज होने का खतरा उठा रहे हैं, और यह बड़ी संख्या में बढ़ते चल रहा है।
कारखानों में बने हुए तरह-तरह के सामानों को संपन्न तबका संपन्नता की सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बना लेता है, और आने-जाने वाले मेहमानों के सामने परंपरागत घरेलू नाश्ता पेश करने के बजाय सब कुछ बाजारू पेश करने को रईसी माना जाता है। नतीजा यह होता है कि इस वक्त मौजूद बच्चे भी अतिरिक्त स्वाद वाले ऐसे सामान खाते हैं, और बाद में उन्हीं से बंधे रह जाते हैं। आज दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक अध्ययन इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर चुके हैं कि इस तरह का खानपान अधिक करने वाले लोग दिल की बीमारियों, डायबिटीज, किडनी, और फेंफड़े की बीमारियों का, कैंसर का खतरा अधिक विकसित कर लेते हैं, और घरेलू खानपान करने वाले के मुकाबले कमउम्र में बुरी मौत मरते हैं। ये जब तक जिंदा रहते हैं, तब तक भी ये बीमारियों से घिरे रहते हैं, एक तरफ तो जुबान पर बस गया बाजारू खानपान महंगा पड़ता है, दूसरी तरफ उसकी वजह से कपड़ों पर खर्च अधिक होता है, इलाज पर खर्च अधिक होता है, इलाज का बीमा महंगे में मिलता है, और लोग कमउम्र में चल बसते हैं। इसलिए खानपान की किसी भी किस्म की बाजारू चीज को बीमारी मानकर चलना ही ठीक है।
जो लोग इस तरह के खानपान में पड़ते हैं, वे अपने बच्चों में भी इसकी आदत पडऩे का बहुत बड़ा खतरा पालकर चलते हैं, और फिर यही खतरा डीएनए से लेकर मिजाज तक, सभी तरह बढ़ते चलता है। इसलिए ऐसी नुकसानदेह और खतरनाक विरासत छोडक़र जाना ठीक नहीं है, विरासत में मकान-दुकान चाहे न छोड़ें, खानपान की बुरी आदत, तम्बाकू और सिगरेट की लत जैसी चीजों तो बिल्कुल ही नहीं छोडऩा चाहिए। फिर इस बात को भी समझना चाहिए कि खानपान के घरेलू सामानों के किसी भी तरह के बाजारू विकल्प धरती पर अधिक प्रदूषण भी खड़ा करते हैं, उनकी पैकिंग का प्रदूषण बहुत से मामलों में हजारों बरसों का रहता है। इसलिए जेब की रकम और धरती को, सेहत को और डीएनए को बर्बाद करने के बजाय लोगों को परांपरागत घरेलू खानपान की तरफ लौटना चाहिए, और अगर आपके मेहमान समझदार हैं, तो वे बाजारू चीजों के मुकाबले घर की बनी चीजों को अधिक बड़ा सम्मान मानेंगे।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में नाना के घर आए हुए 14 बरस के एक लडक़े से जब परिवार ने वीडियो गेम की लत छुड़वाने के लिए मोबाइल छीना, तो वह घर छोडक़र निकल गया, और अब नदी से उसकी लाश निकली है। ऐसा माना जा रहा है कि उसने खुदकुशी कर ली। इसके पहले भी जब उसे वीडियो गेम की लत छुड़ाने की कोशिश की गई तो वह एक बार घर छोडक़र चला गया था, और एक बार पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुका था। अब जब दुनिया में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है, और मां के त्याग की महिमा का गुणगान चल रहा है, उस दिन यह मां अपने किशोर बेटे से वीडियो गेम का यह नशा छुड़वाने की कोशिश करते उसे खो चुकी है। आज कम या अधिक हद तक यह बीमारी घर-घर तक बिखर चुकी है कि छोटे-छोटे बच्चे मोबाइल पर कार्टून फिल्में देखने के ऐसे आदी हो चुके हैं कि वे मां-बाप को खाने-पीने के लिए एक किस्म से ब्लैकमेल करने लगते हैं, और जब तक मोबाइल न मिले, या टीवी का रिमोट उनके हाथ न आए, तब तक वे खाना शुरू नहीं करते। उसके बाद वे अधिक से अधिक वक्त तक स्क्रीन देखने के चक्कर में बहुत धीरे-धीरे खाने लगते हैं, ताकि उसे फोन या टीवी न छीना जाए। इसका क्या इलाज हो सकता है, यह सोचना बड़ा मुश्किल है।
दुनिया में कुछ समझदार लोग ऐसे कार्टून पोस्ट करते हैं जिनमें मां-बाप किताबें पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ बैठे उनके बच्चे भी किताबें पढ़ रहे हैं। अब अगर घर के तमाम बड़े लोग बहुत सा वक्त मोबाइल या लैपटॉप-कम्प्यूटर पर गुजारने लगते हैं, तो बच्चों के साथ बात करने और खेलने का वक्त भी किसी के पास नहीं रहता, न ही कोई कहानी की किताबों में उनको व्यस्त रख सकते, न बाहर ले जा सकते, और नतीजा यह होता है कि वे भी बड़ों की तरह किसी न किसी स्क्रीन में उलझकर रह जाते हैं। वीडियो गेम खेलने में तो कुछ हद तक दिमाग लगता है, लेकिन उसकी चुनौतियों से जूझते हुए बच्चे उसमें और डूबते चले जाते हैं, और अधिक स्कोर पाने की उनकी कोशिश कभी खत्म ही नहीं होती है। दूसरी तरफ जो बच्चे कार्टून फिल्में देखने के आदी हो जाते हैं, उन्हें अपने दिमाग और अपनी कल्पना का कोई भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, और महज आंख-कान से ही वे ऐसे वीडियो देख लेते हैं। इन दोनों ही मामलों में बच्चों के मानसिक, और शारीरिक भी, विकास का सिलसिला बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। और यह वह उम्र रहती है जब उनका दिमागी और भावनात्मक विकास होना चाहिए, और इसी उम्र में वे बिना किसी कल्पना के, बस वीडियो देखते रह जाते हैं।
एक दूसरी बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि बच्चों को बचपन में और जितने किस्म के सामाजिक विकास की जरूरत रहती है, स्क्रीन के चलते उसकी गुंजाइश घटती चली जाती है। अभी एक बड़े जानकार मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि दुनिया के तमाम प्राणियों में सिर्फ के इंसान के बच्चे हैं जिनकी जिंदगी का इतना लंबा हिस्सा बचपन में गुजरता है। बाकी तमाम प्राणियों के बच्चे बहुत जल्द बड़े हो जाते हैं। ऐसा शायद इसलिए हैं कि इंसान के बच्चों को सामाजिकता की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है, परिवार, परंपरा, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति जैसी बहुत सी चीजें रहती हैं जिन्हें बड़े होने के साथ-साथ बच्चे सीखते चलते हैं, और इसीलिए इंसान के बच्चों का बचपन उतना लंबा खिंचता है। अब अगर ऐसे में बच्चे मोबाइल फोन, वीडियो गेम, कार्टून फिल्में, सोशल मीडिया पर उलझकर रह जाते हैं, तो उन्हें बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं लगती है, और नतीजा यह होता है कि वे विकास के इस क्रम से कुछ या अधिक हद तक अछूते रह जाते हैं। इसलिए बच्चों से किस तरह उनका स्क्रीन टाईम लिया जा सकता है, इस बारे में समाज और परिवार दोनों को गंभीरता से सोचना चाहिए।
और यह बात तो हमेशा से ही स्थापित है कि बच्चों को कुछ समझाने के लिए उनके सामने उसी काम को करके जो मिसाल रखी जाती है, उसका सबसे अधिक असर होता है। ऐसे में परिवार के बाकी लोगों को यह देखना चाहिए कि किस तरह वे बच्चों को बाहर के खेल में, सैर पर, दूसरे बच्चों के साथ खुले में रहने, और किताबें पढऩे जैसे कामों में लगा सकते हैं। इसके लिए उनके साथ अगर परिवार के किसी बड़े को रहना है, तो उन्हें भी उतनी देर तक अपने मोबाइल फोन से परे रहना पड़ेगा। हम कई बार सोशल मीडिया पर इस बात को लिखते हैं कि अगर आप एक बच्चे के साथ हैं, और मोबाइल फोन के भी साथ हैं, तो फिर आप बच्चे के साथ नहीं हैं। जरूरत रहे तो परिवार के लोगों को बच्चों की जिम्मेदारी का वक्त बांटना चाहिए कि किस-किस वक्त घर के कौन से लोग बच्चे या बच्चों के साथ रहेंगे। उतने वक्त उन्हें खुद फोन या टीवी से, कम्प्यूटर या अपने किसी दूसरे काम से मुक्त रहना चाहिए।
यह तो एक बच्चे की खुदकुशी से आज इस मुद्दे पर लिखे बिना रहा नहीं गया, लेकिन हम पहले भी इस बात को लिखते आए हैं कि बच्चों का विकास बाजार के फैक्ट्री-बंद खानपान से, बैट्री या बिजली से चलने वाले किसी भी उपकरण से, आसपास के किसी के बीड़ी-सिगरेट के धुएं से, या बचपन में ही उन पर लाद दिए गए धर्म से बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। इसके पहले कि यह नौबत बच्चों के घर छोडक़र जाने, या खुदकुशी की कोशिश तक पहुंचे, और लोगों को पेशेवर मनोचिकित्सकों या परामर्शदाताओं तक जाना पड़े, लोगों को खुद होकर अपनी सामान्य समझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने बच्चों के लिए बिना उपकरणों के समय निकालना चाहिए। इसके लिए किसी परमाणु तकनीक जैसी जटिल समझ की जरूरत नहीं है, लोग बच्चों के साथ रहते हुए किस तरह अधिक से अधिक वक्त बिना गैजेट्स के रह सकते हैं, वह सोचना चाहिए। यह नौबत बहुत ही खतरनाक है कि वीडियो गेम से परे रखने पर कोई बच्चा खुदकुशी कर ले। दुनिया में इतने किस्म की चीजें मौजूद हैं जिनमें बच्चों को व्यस्त रखा जा सकता है, उनका ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, उनका विकास बेहतर किया जा सकता है, परिवार को इस बारे में गंभीर कोशिश करनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, और अपने आसपास के दूसरे परिवारों से भी इस बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि बच्चे घर पर इन चीजों से परे रखे जाने पर दूसरे घरों में जाते ही वहां इनमें उलझ सकते हैं, इसलिए सावधानी आसपास भी फैलनी चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
एक महिला सरपंच का पति से झगड़ा हुआ तो गुस्से में वह बेटे-बेटी के साथ घर छोडक़र मायके जाने निकल गई। रास्ते में अचानकमार टाइगर रिजर्व एरिया पड़ा, और वहां यह महिला बच्ची को पहाड़ी पर छोडक़र आ गई। उससे पड़ोसियों को जानकारी मिली, फिर पति साथियों सहित जंगल में बच्ची को ढूंढने निकला, और तीन दिन बाद यह बच्ची भूख और प्यास से मरी हुई मिली। छत्तीसगढ़ का यह मामला देश भर में शादीशुदा जोड़ों के बीच चल रही तनातनी, और उससे उपजी हिंसा के अनगिनत मामलों में से एक है। हर दिन कई ऐसे मामले हो रहे हैं जिनमें महिला बच्चों सहित खुदकुशी कर रही है। पिता के साथ ऐसे तनाव की नौबत आती है तो वह पूरे परिवार को मारकर मरता है, लेकिन महिला के दिमाग में शायद यह बात रहती है कि उसके छोडक़र जाने के बाद बच्चों का जितना बुरा हाल होगा उससे बेहतर तो बच्चों को मारकर फिर खुद मरना है। लेकिन पारिवारिक हिंसा इतनी अधिक गंभीर होने पर भी परिवार के बाकी लोग, पड़ोसी, और यार-दोस्त बीच-बचाव करके हिंसा की नौबत आने से रोक क्यों नहीं पाते? क्या लोगों की पारिवारिक और सामाजिक जवाबदेही पुराने जमाने के मुकाबले अब कमजोर हो गई है, और अब लोग अधिक आत्मकेन्द्रित हो गए हैं? एक महिला सरपंच तो एक आम महिला के मुकाबले अधिक ताकतवर होनी चाहिए थी, लेकिन उसका निर्वाचित सरपंच होना, राजनीतिक ताकत, इन सबका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया, और तनाव के बीच वह पति को छोडक़र निकल जाने के बजाय बेटी को जंगल में छोडक़र आ गई। होना तो यह चाहिए था कि अगर पति के साथ रहना मुमकिन नहीं था, तो एक महिला सरपंच बच्चों के साथ अलग भी रह सकती थी।
भारत में तलाक के मामले तो पश्चिमी देशों के मुकाबले कम दिखते हैं, लेकिन पारिवारिक हिंसा वहां के मुकाबले बहुत अधिक है। पहले तो सिर्फ महिलाएं ही परिवार में हिंसा की शिकार होती थीं, लेकिन अब कई मामलों में यह भी सुनाई देता है कि कोई पत्नी भी पति को खत्म कर रही है, खुद अकेले, या किसी प्रेमी के साथ मिलकर। यह पहले के मुकाबले कुछ नई और अनोखी बात है। लेकिन चाहे जिस किस्म की हो, पारिवारिक हिंसा पूरे परिवार को खत्म कर देती है, किसी का कत्ल हो जाता है, और कोई उम्रकैद के लिए जेल चले जाते हैं। ऐसी किसी भी नौबत में बच्चे सबसे अधिक तकलीफ पाते हैं, और बाकी रिश्तेदारों या पड़ोसियों, या सरकारी इंतजाम में उनकी जिंदगी तबाह हो जाना तय सरीखा रहता है।
ऐसी पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए कोई नाटकीय कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन जैसे-जैसे भारत में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, समाज में बिना पति रहने वाली महिला के लिए कामकाजी हॉस्टल सरीखा सुरक्षित इंतजाम रहेगा, वैसे-वैसे हिंसा की नौबत आने के पहले महिला अलग हो सकेगी। आज भी कुछ गिनी-चुनी घटनाओं को अगर छोड़ दें, तो पारिवारिक हिंसा में आमतौर पर महिलाएं ही हिंसा की शिकार होती हैं। इसलिए उनकी आत्मनिर्भरता उन्हें परिवार के भीतर बेहतर सम्मान और जगह दिला सकती है, साथ ही समाज में अपने दम पर कमाने-खाने, और सुरक्षित रहने की संभावना भी दिला सकती है। जहां कहीं परिवारों में औरत और मर्द की ताकत में बहुत बड़ा फर्क होगा, वहां इन दोनों में से कमजोर पर हिंसा का खतरा अधिक रहेगा, जो कि भारत में महिला पर ही रहता है।
आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक दूसरा जरिया भी होता है। शादीशुदा महिला के मायके के लोग अगर किसी मुसीबत की नौबत में उसके साथ खड़े रहते हैं, तब भी वह हिंसा झेलने के बजाय हिंसक पति-परिवार को छोडक़र निकल सकती है। इसके लिए मां-बाप और भाईयों को पिछले कुछ महीनों में दो अलग-अलग खबरों को देखना चाहिए जिनमें ससुराल में प्रताडि़त बेटी को पिता गाजे-बाजे के साथ बारात की शक्ल में अपने घर लेकर आए। अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महिला का मां-बाप की संपत्ति में वैसे भी बेहतर हक स्थापित हो चुका है, इसलिए भाईयों को भी हिंसा से बचकर आई बहन को जगह देने में तंगदिली नहीं दिखानी चाहिए। भारतीय समाज में तलाक को लेकर जितनी बुरी सोच है, उसे भी बदलने की जरूरत है। अगर साथ रहना, साथ रहकर जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, तो बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करने, खुद मरने-मारने के बजाय अलग रहना बेहतर है। ऐसे में लडक़ी का परिवार, समाज की सोच, और सरकार का कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल सरीखा इंतजाम, ये सब मिलकर हिंसक-रिश्ते में फंस गई महिला को वहां से निकलने में मदद कर सकते हैं। और आर्थिक आत्मनिर्भरता तो इन सबसे ऊपर है ही।
भारत में तलाक और अलग रहने के बजाय यह परंपरागत सोच अधिक चली आ रही है कि लडक़ी की डोली पिता के घर से उठती है, और उसकी अर्थी पति के घर से उठनी चाहिए। इस पुरानी सोच को समाज के अधिकतर लोग इतनी गंभीरता से ले लेते हैं कि फिर चाहे उसकी अर्थी भरी जवानी में ही छोटे-छोटे बच्चों को छोडक़र या मारकर ही क्यों न निकल जाए। इस सोच को बदलने की जरूरत है। सरकारें महिलाओं के खातों में नगद रकम डालने से लेकर दूसरी कई किस्म की योजनाएं उनके लिए लागू करती रहती हैं। ऐसे में ही शहरों और कस्बों तक कामकाजी महिला हॉस्टल का विस्तार होना चाहिए, ताकि परेशानी में फंसी महिला पूरा मकान किराए पर लेने से बचे, और किसी अकेले मकान में रहने से वह पति की हिंसा के खतरे से भी परे रहे। ऐसा इंतजाम भारत में परिवार व्यवस्था को तोडऩे को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि महिला को तोडऩे की भारतीय पुरूषवादी सोच का खतरा घटाएगा, महिलाओं को नागरिक के रूप में बहुत बुनियादी हक देने के लिए ऐसा इंतजाम करना जरूरी है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
इंसानों के बीच किसी भी तरह के मुमकिन जुर्म में से बलात्कार एक सबसे भयानक जुर्म होता है। देश में जगह-जगह बलात्कार को लेकर जिस तरह की राजनीति चल रही है, वह भयानक है। अभी कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल के संदेशखाली नाम की एक जगह से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर स्थानीय महिलाओं ने बलात्कार के आरोप लगाए थे। उस मामले को भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया था, और लोकसभा चुनाव प्रचार के चलते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी ममता बैनर्जी सरकार और तृणमूल पार्टी पर खूब हमले किए थे, और उन्होंने भाषणों में कहा था कि संदेशखाली से उठा तूफान पूरे बंगाल में तृणमूल सरकार का अंत कर देगा। उन्होंने कहा था कि संदेशखाली की महिलाओं की नाराजगी वहीं तक सीमित नहीं रहेगी। उस वक्त जिस तरह से संदेशखाली की तथाकथित हिंसा का प्रचार हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वहां के तृणमूल नेता एक किस्म का जंगल राज चला रहा थे। अब एक के बाद एक, बलात्कार की शिकायत करने वाली कम से कम दो ऐसी महिलाओं ने यह खुलासा किया है कि उनके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ था, और भाजपा नेताओं ने उनसे कोरे कागजों पर दस्तखत कराकर पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई थी। उन्होंने बाद में मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना बयान दर्ज कराया है। इसमें से एक महिला ने कहा कि अभी जब उन्होंने यह शिकायत वापिस ली है, तो उन्हें मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक दूसरी महिला ने रिपोर्ट वापिस लेते हुए कहा है कि उसने भाजपा की स्थानीय महिला नेता को मनरेगा की बकाया रकम न मिलने की शिकायत की थी, तो उससे कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए गए थे, और फिर पुलिस में रेप की शिकायत कर दी गई थी। एक महिला का यह भी कहना है कि उसके नाम पर एक दूसरी महिला को ले जाकर राष्ट्रपति से मिलवा दिया गया था। अब बंगाल से दूर बैठे हुए हमारे लिए यह अंदाज लगाना मुश्किल है कि बलात्कार की शिकायत सही थी, या उसका यह खंडन सही है। लेकिन अभी वीडियो-कैमरों के सामने महिलाएं यह कहते दिख रही हैं कि किस तरह उनके नाम से बलात्कार की झूठी रिपोर्ट करवाई गई थी।
दूसरी तरफ कर्नाटक में जहां देवेगौड़ा कुनबे के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर सैकड़ों महिलाओं से जबरिया सेक्स करने, और उसके वीडियो भी बनाने के आरोप लगे हैं, और कई महिलाएं कर्नाटक पुलिस में रिपोर्ट लिखा चुकी हैं, और इसी मामले में इन्हीं हरकतों के लिए इसके बाप विधायक एच.डी.रेवन्ना को गिरफ्तार भी किया गया है, और प्रज्वल शायद देश के बाहर फरार हो गया है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नाटक पुलिस में दर्ज मामलों के ठीक खिलाफ एक बयान जारी किया है, और कहा है कि उसके सामने कर्नाटक की कोई भी महिला प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने नहीं आई है, और कुल जमा एक महिला यह रिपोर्ट दर्ज कराने आई है कि उसे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ फर्जी शिकायत के लिए मजबूर किया गया था। इस मामले में एक तरफ तो कर्नाटक में सार्वजनिक रूप से 2976 सेक्स-वीडियो मौजूद हैं, और बाप-बेटे के खिलाफ शिकायत करने वाली महिलाएं भी। साथ-साथ यह भी है कि महिलाओं से जबरिया सेक्स करके उसके वीडियो बनाने के आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना देश छोडक़र भाग भी गया है। अब केन्द्र के भाजपा अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए की कर्नाटक की भागीदार जेडीएस के उम्मीदवार के साथ अगर यह मामला चल रहा है, तो केन्द्र सरकार के मनोनीत किए गए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की महिला अध्यक्ष एक किस्म का यह रियायती बयान दे रही है जो कि सैकड़ों बलात्कारों के आरोप से घिरे हुए भाजपा के भागीदार उम्मीदवार को बचाने वाला दिख रहा है। ऐसा महिला आयोग भी किस काम का जो बलात्कार के ऐसे भयानक मामले में बलात्कारी का हिमायती बने रहने के लिए ओवरटाईम कर रहा है? दुनिया के इतिहास में कर्नाटक सेक्सकांड जैसा मामला पहले कभी नहीं आया था जिसमें एक निर्वाचित नेता सैकड़ों महिलाओं के साथ जबरिया सेक्स के हजारों वीडियो में अच्छी तरह दर्ज हो, और उसके बाद भी राष्ट्रीय महिला आयोग उसे बचाने में जुट गया हो।
हमने अभी-अभी बरेली की एक अदालत का एक फैसला अपने यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल, पर सामने रखा था कि एक नाबालिग लडक़ी ने एक बालिग लडक़े पर बलात्कार का आरोप लगाया था, और वह नौजवान चार बरस से अधिक, 1653 दिनों से जेल में था। अब बालिग हो चुकी इस शादीशुदा लडक़ी ने अदालत में खुद माना है कि उसने झूठा बयान दिया था, तो जिला अदालत के जज ने उसे 1653 दिन कैद काटने का फैसला दिया है, और इतने ही दिन की सरकारी रेट से मजदूरी उस नौजवान को देने का जुर्माना भी सुनाया है। लोकतंत्र में लोग शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, और बाद में उसे वापिस भी ले सकते हैं, या अपना बयान भी बदल सकते हैं। लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि ऐसे गंभीर जुर्म का आरोप झूठा लगने पर किसी की जिंदगी किस हद तक खराब हो सकती है, और ऐसे झूठे आरोप पर क्या सजा होनी चाहिए? हम बरेली के जज की सुनाई सजा से कई वजहों से असहमत हैं, लेकिन अगर बलात्कार की झूठी शिकायत लडक़ी या महिला खुद दर्ज करा रहे हैं, या फिर कोई और उनसे धोखे में, या दबाव डालकर ऐसी रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, तो इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे किसी और को ऐसी साजिश का हौसला न हो सके। राजनीतिक दल अगर बलात्कार की शिकायत को एक औजार या हथियार की तरह इस्तेमाल करके राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने का काम करते हैं, तो वह सिलसिला खत्म होना चाहिए, कानून को कड़ाई बरतनी चाहिए। बरेली के जज ने बेकसूर नौजवान की कैद जितनी लंबी ही सजा उस लडक़ी को सुनाई है जो कि शिकायत करने के दिन नाबालिग थी, मां के दबाव में उसने रिपोर्ट लिखाई थी। लेकिन जो बालिग महिलाएं किसी साजिश के तहत ऐसी रिपोर्ट लिखाती हैं, या राजनीतिक या दूसरे किस्म की ताकतें किसी साजिश में लड़कियों और महिलाओं को शतरंज की बिसात के प्यादों की तरह इस्तेमाल करती हैं, तो सभी लोगों को कड़ी सजा होनी चाहिए। बलात्कार को औजार या हथियार की तरह इस्तेमाल करने से जो सचमुच ही बलात्कार की शिकार होंगी, उनकी जायज शिकायत की विश्वसनीयता भी घट जाएगी। इसलिए आम लोगों, और बलात्कार की शिकार लड़कियों और महिलाओं को इंसाफ मिलने के लिए भी यह जरूरी है कि ऐसे आरोपों वाली झूठी शिकायतों की तुरंत जांच करके साजिश का भांडाफोड़ करना चाहिए।
अमरीका में बसे हुए कांग्रेस से जुड़े एक नेता, सैम पित्रोदा ने अपने ताजा बयान से एक बार फिर बवाल खड़ा कर दिया है। कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक और बयान दिया था जिसे कांग्रेस पार्टी को उनका निजी बयान बताना पड़ा था। उन्होंने अमरीका में विरासत-टैक्स की चर्चा की थी, और कहा था कि किसी अतिसंपन्न के गुजरने पर उसकी संपत्ति का खासा हिस्सा टैक्स के रूप में देश को मिलता है जो कि पूरे समाज को काम आता है। अभी सैम पित्रोदा ने भारत के लोगों की जेनेटिक विविधता की बात करते हुए कहा कि यहां पूर्व के लोग चीनियों जैसे, पश्चिम के लोग अरब जैसे, उत्तर के लोग गोरों जैसे, और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। उन्होंने कहा कि यही वह भारत है जिसमें मैं विश्वास करता हूं, यहां हर कोई एक-दूसरे के लिए थोड़ा-बहुत समझौता करते हैं। जब इस बयान को लेकर बवाल हुआ, और खासकर नरेन्द्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जोडक़र हमले किए, तो शाम तक ही सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से कांग्रेस को आम चुनाव के मतदान के बीच होने वाला नुकसान तो नहीं थमा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने रिकॉर्ड के लिए अपने आपको इस बयान से अलग कर लिया, और इसकी निंदा की है।
जैसा कि सैम पित्रोदा का ओहदा था, वे विदेशों में बसे हुए भारतीयों के बीच कांग्रेस संगठन के मुखिया थे, और जाहिर है कि वे दूसरे देश में बसे हुए हैं, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जहां की सांस्कृतिक सहनशीलता एक अलग दर्जे की रहती है। वे पश्चिम के देशों में लगातार रहते हुए उसी स्वतंत्रता के आदी हैं, और वहां पर किसी वैचारिक बात पर ऐसा बवाल खड़ा नहीं होता है कि लोग उसे संपत्ति को छीनकर दूसरों में बांट देने का नारा बना दें। सैम पित्रोदा की न पिछली बात में एक विचार-विमर्श के स्तर पर कुछ गलत था, और न ही इस बार भारत की विविधता को लेकर कही हुई उनकी बात में कोई नाजायज बात है। उन्होंने अभी भारत के अलग-अलग इलाकों के लोगों के रूप-रंग को लेकर जो कहा है, वह तो जेनेटिक शोध में अच्छी तरह स्थापित बात है। जिन लोगों को वैज्ञानिक शोध पर आधारित ऐसे नतीजों को पढऩा है वे भारत के एक पत्रकार टोनी जोसेफ की लिखी हुई किताब अर्ली इंडियंस पढ़ सकते हैं जो कि डीएनए सुबूतों के आधार पर लिखी गई है। उन्होंने इसमें 65 हजार साल पहले का इतिहास बताया है जब आधुनिक मानव के पूर्वज होमो सेपियंस के एक समूह ने अफ्रीका से आकर भारतीय उपमहाद्वीप में पैर रखे थे। यही सबसे पहले भारतीय हुए। इसके बाद ईसा के 37 सौ बरस पहले ईरान के किसान उस वक्त के भारत में आए, और उनका डीएनए यहां मिला। यह पूरी किताब वैज्ञानिक निष्कर्षों पर आधारित है, और यह किसी देश या जाति के गौरव की धारणा के साथ मेल नहीं खाती। यह किताब कई तरह के असुविधा पैदा करने वाले तथ्य सामने रखती है, जिससे कई जातियों का गुरूर टूटता है। इस किताब को आए कुछ बरस हो चुके हैं, और उसके बाद इसका अधिक जानकारी का नया संस्करण भी आ गया है, लेकिन उसे लेकर कोई बवाल नहीं हुआ, अब जब चुनाव के बीच सांप-नेवले जैसी दुश्मनी वाले कांग्रेस और भाजपा के बीच यह बात निकली, तो इसका विवाद दूर तक जाना ही था। सैम पित्रोदा की बात को देखें तो वह भारत की विविधता में एकता वाली बात है जो कि भारत का सम्मान करने की है, लेकिन भारत के कुछ राजनीतिक दलों में हर बात को अपना अपमान साबित करने की अपार क्षमता है, और उसी ताकत से सैम पित्रोदा की कही बात पर इतना बवाल हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने ही उन्हें इस्तीफा देने का एक मौका दे दिया।
आज दुनिया में वंशावली बनाने की दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए ऐसी कई वेबसाइटें हैं जो कि उनके पुरखों को ढूंढ निकालती हैं, और उनकी मौजूदा पीढिय़ों के लोगों के साथ उनका मेल कराती हैं। भारत में भी दुनिया के बहुत से देशों का डीएनए आया हुआ है, और तरह-तरह के विदेशी खून की वजह से इस देश के अलग-अलग प्रदेशों के लोगों के रूप-रंग में, कद-काठी में कई तरह का फर्क साफ दिखता है। लोगों को अपनी जड़ों को लेकर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। किसी भी इंसान के लिए यह पसंद की कोई बात तो होती नहीं कि वे किस मां-बाप से पैदा हों, किस नस्ल, रंग, जाति, धर्म, या राष्ट्रीयता के हों। भारत में आज रक्त शुद्धता को लेकर जिस तरह का दुराग्रह चल रहा है, वह पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। डीएनए विज्ञान साफ-साफ बताता है कि मोहन जोदड़ो के वक्त से किस तरह अफ्रीका से आए हुए दक्षिण भारत में बसे हुए लोग ईरान और योरप से आए हुए लोगों से मिले, और फिर एक मिलीजुली नस्ल उत्तर भारत में बिखरी। उत्तर-पूर्व के राज्यों के लोगों का डीएनए, चीन के लोगों के डीएनए से दसियों हजार साल पहले कहीं न कहीं मिलता-जुलता रहा है, और उस वक्त तो देशों की सरहद नहीं थी, और भौतिक आवाजाही से डीएनए फैलता था। ऐसे में सैम पित्रोदा की कही बात को लेकर उनकी राजनीतिक भीड़त्या कर देना आसान बहुत है, यह बात लुभावनी भी बहुत है, और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करने की हालत में भी नहीं है, लेकिन उनकी कही बात पर वैज्ञानिक विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों से बात करके देखा जाए, तो समझ पड़ेगा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, और उन्होंने मानो भारतीय पत्रकार टोनी जोसेफ की लिखी किताब की कुछ पंक्तियां ही पढ़ी हैं जो कि बिना किसी विवाद के हिन्दुस्तान में बिक रही है।
राजनीति जिंदगी की तमाम दूसरी बातों को बुरी तरह से कुचल चुकी है। विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, इनमें से कतरा-कतरा उठाई गई जिन बातों से लोगों को चुनावी उकसावे में लाया जा सकता है, आज उन्हीं का बाजार रह गया है। आज देश के सबसे अच्छे इतिहासकार, वैज्ञानिक, या दुनिया के तरह-तरह के विशेषज्ञ हिन्दुस्तान में सच बोलने पर जूते खाने का खतरा रखते हैं। भारत में इतने किस्म की नस्लीय और रक्त विविधता के लोग अगर आजादी के बाद की आधी-पौन सदी तक एक-दूसरे से मिलजुलकर रहते आए थे, और इसी को अनेकता में एकता कहा जाता था, तो आज सैम पित्रोदा की कही हुई उसी बात पर उनकी खुद की पार्टी भी चुनावी नुकसान का खतरा देखते हुए उससे किनारा कर ले रही है, और भाजपा के हाथ तो तेल लगा हुआ एक लट्ठ लग ही गया है, हाथ को तोडऩे के लिए। यह सिलसिला बहुत खतरनाक है कि किसी की भी बात को तोड़़-मरोडक़र नफरत का सामान बनाने की गुंजाइश को ही राजनीति बना लिया जाए। आज सैम पित्रोदा को गालियां देना बहुत आसान है, लेकिन यह करते हुए लोग अपनी अगली पीढ़ी को विज्ञान के इतिहास, इतिहास के विज्ञान के ज्ञान से दूर कर ले रहे हैं। आज हिन्दुस्तान में वैज्ञानिक तथ्यों को खारिज करने, और अवैज्ञानिक बातों को स्थापित करने की अपार राजनीतिक ताकत और संस्कृति स्थापित हो चुकी हैं, और ऐसे में सच के मारे जाने का पूरा खतरा खड़ा है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में बोर्ड इम्तिहान की उत्तर पुस्तिकाओं की हिफाजत की ड्यूटी पर लगाए गए राज्य पुलिस के एक हथियारबंद जवान ने नशे की हालत में जगह-जगह गोलियां चलाईं, इसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। ऐसा कुछ अरसा पहले राजधानी रायपुर के पुलिस मुख्यालय में तैनात एक पुलिस जवान ने भी किया था जो बस्तर के नक्सल मोर्चे को लेकर चिल्लाए जा रहा था, और गोलियां चलाए जा रहा था। इन दोनों ही मामलों में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन लोगों के मरने में कोई कसर भी नहीं रह गई थी। किसी तरह के तनाव या नशे की हालत में ऐसी गोलीबारी से बहुत से साथियों या दूसरे लोगों को मार डालने के मामले दुनिया भर में सामने आते हैं। खासकर अपने नागरिकों की संख्या से अधिक निजी हथियारों वाले अमरीका में तो स्कूल, कॉलेज, और मॉल जैसी सार्वजनिक जगहों पर अंधाधुंध गोलीबारी से लोगों को मारने की वारदात होती ही रहती है। हिन्दुस्तान में निजी हथियारों का वैसा जमावड़ा नहीं है, और यहां सुरक्षा बलों के जवान ही मानसिक तनाव या नशे में ऐसा करते मिलते हैं। चूंकि चुनाव से लेकर नेताओं की हिफाजत तक, और इम्तिहानों से लेकर बड़े अफसरों की सुरक्षा तक कई किस्म की ड्यूटी ऐसे हथियारबंद लोग करते हैं, इसलिए इनके बारे में सरकारों को समय रहते कोई नीति बनाना चाहिए, ताकि नशा या तनाव हथियार के साथ मिलकर एक जानलेवा मेल न बन जाए।
एक तो पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों में तनाव की घटनाएं बहुत होती हैं, और खासकर अपने शहर और प्रदेश से दूर रहने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों के जवानों में खुदकुशी की भी बहुत सी घटनाएं होती हैं, और उनके पीछे सबसे बड़ी वजह पारिवारिक जरूरत के समय उन्हें छुट्टी न मिलना बताया जाता है। एक वजह कई खबरों में यह भी आती है कि लंबे समय तक परिवार से दूर रहने के बाद जब वे घर लौटते हैं तो उन्हें स्थानीय सरकार से अपने मामले सुलझते नहीं दिखते, और वे उसे लेकर भी तनाव में रहते हैं। इन दिनों हर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी के पास लगातार कई गोलियां दागने वाले ऑटोमेटिक हथियार रहते हैं, और ऐसे में हर हथियार एक खतरा रहता है, उस जवान के लिए भी, उसके आसपास के लोगों के लिए भी। इंदिरा गांधी को जिस तरह उनके हथियारबंद निजी अंगरक्षकों ने ही धार्मिक आधार पर मार डाला था, वैसा एक भयानक खतरा तो देश में हर बड़े नेता पर मंडरा सकता है जिससे किसी धर्म के लोगों को शिकायत हो, और धार्मिक प्रताडऩा के वैसे मामले किसी सुरक्षाकर्मी के सिर चढक़र बोलने लगें। यह नौबत बहुत भयानक हो सकती है, और सिर्फ सरकारें इस आखिरी नौबत को काबू में नहीं कर सकतीं, देश में सद्भावना का माहौल अगर रहेगा, तो ही ऐसे खतरे टल सकते हैं, वरना ये किसी भी दिन जानलेवा साबित हो सकते हैं।
फिलहाल सुरक्षा बलों के मुखिया देश का माहौल तो नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ बुनियादी सुधार जरूर कर सकते हैं जिससे कि खतरे कम हो सकें। पहली बात तो यह कि हथियारबंद पुलिस या दूसरे सुरक्षाकर्मियों की एक निश्चित संख्या के अनुपात में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता नियुक्त होने चाहिए जो कि तैनाती की जगह पर ही साथ में रहें। खून-खराबा होने के पहले भी तनाव कई और किस्म से नुकसान पहुंचाता है, और ऐसे परामर्शदाता उस नुकसान को कम कर सकते हैं, और खूनी मंजर को टाल सकते हैं। हर हथियारबंद कर्मी को खुद के लिए और दूसरों के लिए एक खतरा मानते हुए इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए, और मानसिक रूप से सेहतमंद हथियारबंद लोग ही आसपास के लोगों के लिए बिना खतरे के हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि हथियारबंद सुरक्षा कर्मचारियों के नशे की आदत को लेकर सरकार को गंभीरता से कुछ करना चाहिए। ऐसे कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह नशा करने की छूट नहीं पा सकते। और अगर सरकार को भर्ती नियमों में फेरबदल भी करना पड़े, तो भी जिसके पास जब तक हथियार है, तब तक उसके नशे पर रोक का एक सिद्धांत बनाकर उसे कड़ाई से लागू करना चाहिए। कुछ सुरक्षा एजेंसियों में संस्था की तरफ से ही कर्मचारियों को रियायती शराब मुहैया कराई जाती है, यह सिलसिला भी काबू में रखना चाहिए, या बेहतर हो कि इसे बंद कर देना चाहिए। आज देश में बेरोजगारी इतनी अधिक है कि ऐसे संवेदनशील और हथियारबंद मोर्चों के लिए शराब पीने वालों के मुकाबले शराब न पीने वालों को नौकरी में प्राथमिकता देकर इन जगहों से नशाखोरी खत्म की जा सकती है। बड़े-बड़े जानलेवा ऑटोमेटिक हथियार नौकरी के तनाव के साथ जब नशे से भी जुड़ जाते हैं, तो फिर बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। हमारे हिसाब से यह खतरा खत्म किया जाना चाहिए, और अगर हथियारबंद ड्यूटी वालों के लिए नशा न करने की शर्त जोडऩा पड़े, तो वह भी किसी के मानवाधिकार के खिलाफ नहीं होगी, उसे कड़ाई से बनाना चाहिए, और लागू करना चाहिए। जब नशे में कोई व्यक्ति कहीं पर भी हथियार या गोलियां छोडक़र चले जा रहा है, या सार्वजनिक जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, तो ऐसे खतरों को बढऩे से तुरंत ही रोकना चाहिए।
शराब पीना किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन सरकार अपनी नौकरियों के लिए ऐसी शर्तें जोड़ सकती है कि नौकरी देने के पहले ही यह बात साफ रहे कि इस नौकरी में नशे की गुंजाइश नहीं रहेगी। आज भी फौज से लेकर पुलिस तक, और अर्धसैनिक बलों तक यूनियन न बनाने, हड़ताल न करने जैसी कई शर्तें जुड़ी ही रहती हैं। हम देश में खतरनाक हथियारों की बढ़ती मौजूदगी के साथ ऐसी किसी हिफाजत को न जोडऩे को आम और खास, हर किस्म के लोगों पर खतरा मानते हैं, और इससे बचाव का इंतजाम सरकार की ही जिम्मेदारी है।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी में एक नया बवाल मीडिया का काम देखने वाले उसके लोगों के बीच हुआ। दिल्ली से आई पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा ने रोते हुए ये गंभीर आरोप लगाए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने उनसे बदसलूकी की, और उनकी शिकायतों पर पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर दिल्ली के बड़े कांग्रेस नेताओं तक किसी ने भी कुछ नहीं किया। ऐसी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के पहले से यह टकराव चल रहा था, और छत्तीसगढ़ में मतदान के बीच आधे से अधिक सीटों पर बाकी मतदान के पहले राधिका खेड़ा ने यह बम फोड़ा है, और इसके पीछे भाजपा हो सकती है। अब आज अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर यह बवाल हो रहा है, तो सबसे पहले तो कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं जिन्हें 6 महीने पहले से टकराव मालूम था, और उन्होंने इसे नहीं निपटाया। आज जब पूरा देश राम से अधिक भाजपा का नाम लेने के माहौल से गुजर रहा है, उस वक्त अपने घर की आग के लिए कांग्रेस भाजपा पर तोहमत लगाए, इससे कुछ अधिक हासिल नहीं होना है। लेकिन इस विवाद से कुछ बातें उठी हैं, और उन पर कांग्रेस पार्टी, और उसे छोड़ देने वाली राधिका खेड़ा दोनों को जवाब देना चाहिए। हम किसी महिला की की हुई शिकायत को पहली नजर में गलत नहीं मानते हैं, लेकिन दोनों तरफ की महज जुबानी तल्खी की शिकायतों का हल वह निकल सकता है जो सुशील आनंद शुक्ला ने सुझाया है, उन्होंने कहा है कि वे नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, और उससे इन आरोपों को भी कसौटी पर चढ़ाया जा सकेगा जिनके मुताबिक राधिका खेड़ा अपने साथ कई किस्म की बदसलूकी की बात कहती हैं, रात में होटल के कमरे के दरवाजे पीटने की बात कहती हैं, और शराब पीने के प्रस्ताव का आरोप भी लगाती हैं। नार्को टेस्ट ऐसे विवाद का एक अच्छा हल हो सकता है जिसके अधिक सुबूत नहीं हैं, और जिनके पीछे गहरी राजनीति होने के संदेह या आरोप हैं। सार्वजनिक जीवन में जब बात चाल-चलन पर आती है, तो नार्को टेस्ट की बात पर राधिका खेड़ा को भी हॉं कहना चाहिए।
चूंकि यह मामला कई दिनों से खबरों में बना हुआ है, और अब कांग्रेस पार्टी पर उसे छोड़ते हुए उसकी एक बड़ी प्रवक्ता ने यह आरोप लगाया है कि चूंकि वे रामलला के दर्शनों को अयोध्या गई थीं, इसलिए हिन्दूविरोधी कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उन्होंने अपने इस्तीफे में बार-बार राम का जिक्र किया है, और अभी कुछ दिन पहले तक मीडिया से बात करते हुए वे बार-बार इस बात का जिक्र कर रही थीं कि कांग्रेस पार्टी हिन्दूविरोधी नहीं हैं, और उसने उनके (राधिका के) अयोध्या जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं की थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संचार विभाग के साथ अपने टकराव के चलते हुए भी एक बार भी अयोध्या का जिक्र नहीं किया था, पार्टी के रामविरोधी या हिन्दूविरोधी होने की चर्चा नहीं की थी। अब एकाएक उन्होंने राम का नाम लेकर जितने गंभीर आरोप लगाए हैं, वे कांग्रेस पार्टी के इस घोषित रूख के ठीक खिलाफ हैं कि उसके नेता-कार्यकर्ता, सदस्य अपनी मर्जी से अयोध्या जाना तय करें। पार्टी ने इसे संगठन का मुद्दा नहीं बनाया था, और लोगों की अपनी पसंद या विवेक पर इसे छोड़ दिया था। अब राधिका खेड़ा उसके ठीक खिलाफ यह बात कह रही हैं। राम के नाम पर अगर इतना बड़ा विवाद हो रहा है, तो नार्को टेस्ट जैसी अग्नि परीक्षा से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। चूंकि बदसलूकी की अधिक शिकायत राधिका खेड़ा को है, इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता का नार्को टेस्ट होना बेहतर होगा, और उन्होंने खुद ही इसका प्रस्ताव भी रख दिया है।
लेकिन इस विवाद में कुछ दूसरी चीजें सामने आई हैं जिनकी भी जांच हो जानी चाहिए। एक आरोप यह आया है कि राधिका खेड़ा की मां की एक कंपनी है जो कि फिल्में बनाती है, और छत्तीसगढ़ में सरकार या कांग्रेस पार्टी से उसे फिल्म बनाने का काम मिला था, और उसके भुगतान का भी कोई विवाद चल रहा है। अगर ऐसा है तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कांग्रेस संगठन के लोग अपनी घरेलू कंपनियों को लेकर संगठन या पार्टी की सरकार को किस तरह दुहते हैं, और क्या इस बारे में पार्टी की कोई नीति है? यह विवाद इसलिए भी सुलझाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अभी एक ऐसा एग्रीमेंट सामने आया था जिसके मुताबिक तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को कांग्रेस पार्टी से पांच-छह करोड़ रूपए दिए गए थे। इसके अलावा यह बात भी जगजाहिर है कि विनोद वर्मा की कुछ दूसरी कंपनियां भूपेश सरकार का कई तरह का काम कर रही थीं। यह चर्चा भी आम रहती हैं कि कांग्रेस हाईकमान के आसपास के कई बड़े नेता अपनी कुछ बेनामी कंपनियों के नाम से विज्ञापन, चुनाव सर्वे, और रणनीति जैसे कामों के नाम पर पार्टी से मोटी रकम ले लेते हैं। अब अगर राधिका खेड़ा के मामले में ऐसा हुआ है, तो उसका भी खुलासा होना चाहिए, और नार्को टेस्ट होने पर तो तमाम बातों का खुलासा हो सकता है।
हम भारत जैसी, गटर के पानी से भी गंदी हो चुकी, राजनीति में नार्को टेस्ट को फिटकरी की तरह का देखते हैं जो कि गंदे पानी को साफ करने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रही है। न सिर्फ कांग्रेस के इस मामले में, बल्कि सत्ता पर बैठे तमाम लोगों का कार्यकाल खत्म होने पर अगर उनका अनिवार्य रूप से नार्को टेस्ट करवाया जाए, और उनके बारे में हवा में चल रहे तमाम विवादों पर सवाल किए जाएं, तो हो सकता है कि यह आधुनिक फिटकरी राजनीति से गंदगी कुछ दूर तक तो कम कर दे। ऐसा होने पर जनता का भी अधिक भरोसा राजनीति, और कुल मिलाकर लोकतंत्र पर लौट सकता है। आज जनता सरकार को टैक्स देने से इसलिए भी बचना चाहती है क्योंकि उसे मालूम है कि सरकारें बहुत भ्रष्ट रहती हैं, और उसके दिए हुए टैक्स जनता के काम कम आते हैं, भ्रष्टाचार में अधिक जाते हैं। आज का मुद्दा वैसे तो कांग्रेस संगठन के भीतर के विवाद से शुरू हुआ था, लेकिन इसका विस्तार नार्को टेस्ट के व्यापक इस्तेमाल तक करने के बारे में जनमत तैयार करने के लिए होना चाहिए। वैसे भी जो लोग संविधान की शपथ लेकर पांच बरस अप्सरा की तरह रिझाने वाली सत्ता पर सवार रहते हैं, उन्हें इतना त्याग तो करना ही चाहिए कि सत्ता की शानदार इनिंग के बाद वे नार्को टेस्ट को उसी तरह तैयार रहें जिस तरह कि ओलंपिक में शामिल होने तमाम खिलाड़ी नशे की जांच के लिए तैयार रहते हैं। और राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से दिए इस्तीफे में जितने दर्जन बार राम का नाम लिया है, उसे देखते हुए उन्हें भी सुशील आनंद शुक्ला के साथ-साथ नार्को टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, आखिर अग्निपरीक्षा गौरवशाली भारतीय परंपरा रही है, और राम के युग से ही इसका चलन भी रहा है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
छत्तीसगढ़ की बाकी लोकसभा सीटों के साथ देश में सौ से जरा कम, 95 सीटों पर 7 मई को वोट डलने जा रहे हैं। इनमें 12 राज्यों और केन्द्र प्रशासित प्रदेशों की सीटें हैं। ये राज्य इतने बिखरे हुए हैं कि इनमें किसी एक पार्टी या गठबंधन का बोलबाला नहीं दिख रहा है लेकिन खेमों में बंटा हुआ मीडिया, और सोशल मीडिया इसके पहले के दो दौर के मतदान का अपने-अपने हिसाब से विश्लेषण करते हुए, अपने पसंदीदा लोगों की जीत की मुनादी कर रहा है। दुनिया के 60 देशों में इस बरस चुनाव हो रहे हैं, और दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस विशेषज्ञ यह मान चुके हैं कि इस बार चुनावों को प्रभावित करने की कोशिशों में एआई के इस्तेमाल को रोक पाने का वक्त अब जा चुका है, और अब दुनिया की यह ताकत नहीं है कि चुनावों को इस प्रभाव से बचा सके। 60 देशों का मतलब दुनिया के चुनाव-आधारित देशों में से करीब एक तिहाई देश होता है, और अगर इनमें घरेलू पार्टियां, या विदेशी सरकार-कारोबार एआई की ताकत से वोटरों को प्रभावित करते हैं, तो जाहिर है कि चुनकर आने वाले लोकतंत्र बड़ी ताकतों की मर्जी के रहेंगे, और शायद बड़ी ताकतों के पांव दबाएंगे।
भारत में भाजपा को छोड़ बाकी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के अपने परंपरागत तरीकों से निकल ही नहीं पा रहे हैं। भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसने अंतरराष्ट्रीय बाजार में मौजूद हर किस्म के औजार और हथियार का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार में किया है, और लोकतंत्र इसकी इजाजत भी देता है। भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए, और देश की बाकी राजनीतिक पार्टियों के बीच दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर गैरबराबरी के हालात हो सकते हैं, शायद हैं भी, लेकिन कल्पनाशीलता और उसके आधार पर चुनावी तैयारी करने से तो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी दूसरी पार्टियों को रोक नहीं सकती है। इस मामले में भी भारत का विपक्ष बुरी तरह पिछड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ-साथ देश की चुनाव आयोग सरीखी संवैधानिक संस्थाओं से लेकर देश की जांच एजेंसियों तक का जैसा अभूतपूर्व और असाधारण इस्तेमाल आज की मोदी सरकार कर रही है, वह भी अब तक सुप्रीम कोर्ट की नजरों के सामने लोकतांत्रिक-संवैधानिक सीमाओं और संभावनाओं के लचीलेपन का ऐतिहासिक इस्तेमाल है। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर ऐसे इस्तेमाल के खिलाफ देश का विपक्ष और बाकी लोकतांत्रिक ताकतें सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर गुहार नहीं लगा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अकेले तो विपक्ष की भूमिका निभा भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नापसंद आने वाले बहुत से फैसले पिछले कई महीनों में दिए हैं, इसलिए यह मानने की कोई वजह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग जैसी सत्ता-प्रतिबद्ध संस्था बन चुका है। अदालत के कई फैसले मोदी सरकार के लिए खासी दिक्कतें खड़ी कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दुनिया की बुरी से बुरी विपरीत परिस्थिति से भी उबर जाने की अपनी क्षमता का सुबूत गुजरात के वक्त से देते आए हैं, और आज वह जारी भी है। ऐसे में देश में हाल के हफ्तों तक बिखरे, कमजोर, और असंगठित विपक्ष को लेकर अगर जनता में उत्साह कुछ कम दिखा है, तो यह भी सत्तारूढ़ पार्टी की कामयाबी रही है।
लेकिन अचानक ही मतदान शुरू होने के बाद इस देश में इन कुछ हफ्तों में मोदी की अगुवाई में भाजपा के चुनावी एजेंडा में जो फेरबदल देखने मिल रहा है, वह लोगों को मतदाताओं के रूझान में एक फेरबदल सुझा रहा है। ऐसा है या नहीं, इसे परखने का हमारे पास कोई सर्वे नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि पिछले कुछ हफ्तों में मोदी और उनकी पार्टी ने दस साल की अपनी कामयाबी के दावों को छोडक़र जिस तरह बहुत ही सतही और खूंखार मुद्दों को उठाया है, उससे लोगों को हैरानी हो रही है। आमतौर पर जो लोग मोदी के लिए हमदर्दी और तारीफ रखते हैं, वे भी कुछ हैरान दिख रहे हैं कि मुस्लिम से लेकर मंगलसूत्र तक जैसे गैरमुद्दों को सच से एकदम परे जाकर क्यों उठाया जा रहा है? क्या सरकार की सरकारी और निजी एजेंसियां देश में हवा के रूख के बदलने का इशारा कर रही हैं?
मतदाताओं का रूझान और हवा का रूख, ये बातें बड़ी अमूर्त रहती हैं। इनका न चेहरा-मोहरा होता, न कद-काठी होती, ये सिर्फ कल्पना की बातें रहती हैं। इसलिए हम इनके आधार पर कल के मतदान के लिए लोगों को कुछ नहीं सुझा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मतदाताओं को अधिक से अधिक वोट डालने के लिए जरूर कहना चाहते हैं। हमारा ख्याल है कि घर बैठने वाले वोटरों में से एक चौथाई भी अगर घंटे भर का वक्त निकालकर वोट डालने चले जाएंगे, तो नेताओं के कपड़े गीले हो जाएंगे। आज हर तरह की राजनीतिक अटकलबाजी, योजना, और चुनावी रणनीति पिछले चुनावों में वोटरों की गिनती पर आधारित रहती है। अगर वह गिनती ही दस-पन्द्रह फीसदी बदल जाएगी, तो नेताओं और पार्टियों के होश उड़ जाएंगे। लोकतंत्र में जनता को सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि हर किसी को वोट डालने निकलना चाहिए, फिर चाहे वह वोट नोटा को ही क्यों न जाए।
दूसरी बात यह है कि लोगों को अपने और अपनी अगली पीढ़ी के भले के लिए देश के असल मुद्दों को पहचानना सीखना चाहिए। किसी नाटक में मुखौटे लगाए हुए लोगों को देखना, उस प्रदर्शन के वक्त तक ही ठीक रहता है, उससे परे लोग अगर उन मुखौटों को ही हकीकत मान लेते हैं, तो इससे उनका नुकसान छोड़ और कुछ नहीं होता। लोगों को जिस नेता और पार्टी को वोट देना हो, उन्हें अपना फैसला जिंदगी और देश-प्रदेश के असल मुद्दों के आधार पर करना चाहिए। धर्म, जाति, अंधभक्ति, नफरत और हिकारत से लोकतांत्रिक फैसले नहीं करने चाहिए। अपने बच्चों को मकान की दीवारें चाहे कमजोर देकर जाएं, लोकतंत्र मजबूत देकर जाना चाहिए। भारत दुनिया का एक इतना बड़ा देश है कि यहां एक अच्छी या बुरी सरकार का बनना इस देश से परे, दुनिया को भी बहुत प्रभावित कर सकता है। इसलिए लोगों को पूरी धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारी देखते हुए, देश के मुद्दों को देखते हुए, लोकतंत्र की बुनियादी समझ को ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए। आज के वक्त यह कहना भी जरूरी है कि हिन्दुस्तान में चुनावों को ही लोकतंत्र मान लेना गलत है। चुनाव सिर्फ एक औजार है जो कि देश की अगली सरकार बनाने में काम आता है, लोकतंत्र तो सरकार से भी बहुत ऊपर होता है, दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाओं से भी ऊपर होता है, वह बहुत ही व्यापक और अमूर्त होता है। ऐसे बेचेहरा लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव की शक्ल में पहचानना सही नहीं होगा। सही तो यह होगा कि लोग चुनाव नाम के औजार का इस्तेमाल करने के पहले अपने देश के असल मुद्दों के बारे में सोचें, और उसके बाद वोट दें। जिंदगी की हकीकत, और उसके असल मुद्दों की फिक्र करने वाले तमाम लोगों को इस, और अगले कई चुनावों के लिए हमारी शुभकामनाएं।
छत्तीसगढ़ में पिछली भूपेश सरकार के दौरान हुए कई किस्म के बड़े-बड़े भ्रष्टाचार में से एक अभी सामने आया है जिसमें केन्द्र सरकार की भारतीय संचार सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आए एक अफसर को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से धान खरीदती है, और फिर राईस मिलों से उसकी मिलिंग करवाकर उसे एफसीआई को देती है, या केन्द्र और राज्य की किसी दूसरी योजना में इस्तेमाल करती है। अभी दो बरस पहले तक यह मिलिंग रेट 40 रूपए क्विंटल था, और कहा जाता था कि राज्य सरकार की संस्था मार्कफेड इस काम में 20 रूपए क्विंटल का कमीशन लेती थी। इसके बाद भूपेश मंत्रिमंडल ने एक दिन अचानक राईस मिल एसोसिएशन की एक चिट्ठी के आधार पर 40 रूपए की इस रेट को तीन गुना बढ़ा दिया, और 120 रूपए कर दिया। इसके बाद मार्कफेड के एमडी रहे मनोज सोनी नाम के भारतीय संचार सेवा से आए अफसर ने 60 रूपए क्विंटल की वसूली की। जाहिर है कि एक अफसर अपने खुद के भ्रष्टाचार के लिए न तो राज्य में चले आ रहे किसी रेट को कैबिनेट में तीन गुना करवा सकता था, और न ही सौ-दो सौ करोड़ जैसी बड़ी रकम वसूल सकता था। पिछली सरकार के वक्त सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल थे, जो पुराने राईस मिल कारोबारी हैं, और कारोबारियों के संगठन में बड़े पदाधिकारी भी रहे हैं। अभी वे साल भर से ईडी के शिकंजे से बचने के लिए फरार चल रहे हैं, लेकिन उनके कोषाध्यक्ष रहते यह तो हो भी नहीं सकता था कि उनके धंधे से उनकी पार्टी की सरकार में उनकी जानकारी के बिना इतनी संगठित उगाही हो जाए। साधारण समझबूझ तो यही कहती है कि रामगोपाल अग्रवाल जैसे जानकार व्यक्ति ने ही ऐसी योजना बनाई होगी क्योंकि पार्टी फंड आना तो उन्हीं के पास था। आज हालत यह है कि मार्कफेड के एमडी रहे दो-दो लोग जेल में हैं। यह एक अलग बात है कि इन दोनों के ठीक पहले किरण कौशल नाम की जो आईएएस अफसर इस कुर्सी पर थी, उन्होंने सत्ता के अंधाधुंध दबाव के बाद भी गलत भुगतान करने से मना कर दिया था, और भूपेश सरकार ने उन्हें तुरंत वहां से हटाया था। अगले दो एमडी उगाही में जुट गए, और अब ईडी की गिरफ्तारी के बाद जेल में पड़े हुए हैं।
कारोबारियों से सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार के लोग उगाही करें, इसमें कुछ भी नया या असाधारण नहीं है। ऐसा हमेशा ही होता है। लेकिन सरकार के खर्च को जिस तरह तीन गुना करके चावल की कस्टम मिलिंग से उगाही की गई थी, वह छुपने लायक जुर्म नहीं था। सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिरकर, और भागीदारी की वजह से भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों की जो मिसालें छत्तीसगढ़ में सामने आई हैं, वैसा इस प्रदेश में तो पहले कभी नहीं हुआ था। यह एक अलग बात हो सकती है कि केन्द्र सरकार की जांच एजेंसियां सिर्फ कांग्रेस सरकारों और नेताओं के भ्रष्टाचार पकड़ रही हैं, लेकिन इनमें किसी मासूम या ईमानदार के फंसने की आशंका अभी भी नहीं लगती है। लोगों को पहली नजर में यह दिखता है, और मालूम है कि यह सब भ्रष्टाचार सचमुच ही हुआ था। चावल हो, शराब, या कोयला ट्रांसपोर्ट, इन सबमें जो संगठित भ्रष्टाचार हुआ था, उसने आईएएस-आईपीएस अफसरों की साख को चौपट कर दिया क्योंकि वे खुलकर इस माफिया-कारोबार में भागीदार हो गए थे। यही वजह है कि साल भर बाद भी ऐसे बड़े अफसरों को जमानत भी नहीं मिल पा रही है। कारोबारियों से राजनीतिक चंदा शिष्टाचार के दायरे में हमेशा से चले आ रहा था, लेकिन उसे चाकू की नोंक पर, कारखाने बंद करवा देने की धमकी देकर, या गिरफ्तारी का डर दिखाकर इस भयानक अंदाज में कभी नहीं वसूला गया था। इसलिए अब जब ईडी दिलचस्पी लेकर भूपेश सरकार के वक्त के जाने कितने ही मामलों में कार्रवाई कर रही है, तो संबंधित कारोबारियों से प्रदेश के प्रमुख और जानकार लोगों को तो यह जानकारी मिल ही रही है कि सचमुच ही ऐसा भ्रष्टाचार हुआ था।
यूपीएससी के चुने हुए ऐसे अफसरों का संगठित माफिया की तरह नेताओं के साथ मिलकर जबरिया उगाही का धंधा चलाना बताता है कि भारत में ऐसी अखिल भारतीय सेवाएं भ्रष्टाचार का एक ढांचा बन चुकी है। इन सेवाओं के अफसर अंधाधुंध ताकत के ओहदे पाते हैं, और उनके सौ किस्म के गलत काम जांच से परे रह जाते हैं। अब भारत सरकार और राज्यों के सामने विचार-विमर्श का एक यह मुद्दा रहना चाहिए कि अखिल भारतीय सेवाओं का क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, या किस तरह उनके कामकाज को बदला जाए ताकि वे केन्द्र और राज्य सरकारों के नाजायज दबाव झेल सकें। आज देश भर में इंकम टैक्स विभाग ने जिस तरह करदाताओं के मामले कम्प्यूटर से बिना पसंद-नापसंद छांटकर पर्ची निकालने के अंदाज में देश में किसी भी राज्य में भेज देना चालू किया है, और करदाता और अफसर एक-दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते, क्या उसी तरह का कुछ काम अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों की राज्यों में तैनाती को लेकर हो सकता है? या राज्यों के भीतर अफसरों को अलग-अलग जिम्मेदारी मिलने के वक्त कुछ ऐसा किया जा सकता है कि नेताओं की पसंद पर किसी अफसर को कोई कुर्सी न मिले? हमारी समझ इस मामले में बड़ी सीमित है, और इसलिए सत्ता के संगठित भ्रष्टाचार को रोकने की कौन सी तरकीबें हो सकती है, इस पर और अधिक जानकार लोग शायद कुछ बेहतर सुझा सकते हैं। देश के बेदाग भूतपूर्व अफसरों से भी राय लेनी चाहिए कि यह देश नौकरशाही के संगठित भ्रष्टाचार, और नेताओं से भागीदारी से छुटकारा कैसे पा सकता है? जब टेलीफोन सेवा का कोई अफसर राज्य में धान की मिलिंग का बहुत बदनाम और बहुत कमाऊ दफ्तर पा सकता है, और वहां बैठकर लूटमार कर सकता है, तो फिर इस व्यवस्था को सुधारने या बदलने की जरूरत है। और बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की नहीं है, बहुत से प्रदेशों में दूसरी पार्टियों की भी बहुत सी सरकारें कमोबेश इसी तरह का काम करती हैं, और पूरे देश को जनता के पैसों की इस लूटमार को रोकने का रास्ता तलाशना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक सेक्स करने के आरोपी पति को बरी कर दिया है। पत्नी ने यह रिपोर्ट लिखाई थी, और अदालत ने यह मान लिया है कि पत्नी के साथ किसी भी तरह का सेक्स अपराध नहीं है। जिसे अप्राकृतिक कहा जाता है, और जो धारा 377 के तहत अपराध है, वह भी पत्नी के मामले में पुरूष पर लागू नहीं होता। जस्टिस जी.एस.अहलूवालिया ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर एक वैध पत्नी विवाह के बाद पति के साथ रह रही है, तो उसके द्वारा किया गया कोई भी सेक्स जुर्म नहीं माना जा सकता, अगर पत्नी 15 बरस से छोटी नहीं है। जज ने कहा कि शादीशुदा जोड़ों में रेप को अभी तक कानूनी रूप से नहीं माना गया है, इसलिए यह मामला रद्द किया जा रहा है। पत्नी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि पति ने उसके साथ कई बार अप्राकृतिक सेक्स किया, और किसी को बताने पर तलाक की धमकी भी दी थी।
अब यहां पर कई सवाल खड़े होते हैं, जो कि कानून को लेकर भी हैं, बड़ी अदालतों द्वारा कानून की व्याख्या को लेकर भी हैं, और कानून बनाने वाली संसद को लेकर भी हैं। क्या सचमुच ही आज 21वीं सदी के हिन्दुस्तान में महिला के इतने भी हक नहीं हैं कि वह पति द्वारा जबर्दस्ती करके किए जा रहे अप्राकृतिक सेक्स का विरोध कर सके? क्या संविधान की व्याख्या करने वाले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज के वक्त में भी भारतीय महिला को एक इंसान की तरह देखने से इंकार कर सकते हैं? क्या मौजूदा कानूनों की इतनी संकुचित व्याख्या की जा सकती है जो कि महिला के बुनियादी इंसानी हकों को भी नकार दे? अगर भारतीय संवैधानिक अदालतों की सोच महिला को मनुस्मृति के नजरिए से देखती है, तो यह लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाती। हमारा ख्याल है कि यह मामला जबलपुर हाईकोर्ट के बाद अगर किसी तरह सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाएगा, और वहां पर इसकी संवैधानिक व्याख्या के लिए कोई संविधानपीठ बैठेगी, तो वह महिला के अधिकारों की एक बेहतर व्याख्या करेगी। अभी जबलपुर हाईकोर्ट के जज ने भारतीय पति को जो खुली छूट दी है, उसने भारतीय शादीशुदा महिला को हर किस्म के बलात्कार का सामान करार दिया है। यह फैसला दिल दहलाता है, और महिला अधिकारों के लिए लडऩे वाले कुछ वकीलों को खुद होकर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जाना चाहिए क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ कोई राय जाहिर नहीं करेगी, तब तक इस हाईकोर्ट का यह फैसला एक नजीर की तरह निचली अदालतों में इस्तेमाल किया जाता रहेगा।
ऐसा लगता है कि भारत में शादीशुदा जोड़ों के बीच बलात्कार की बात को मानने से कानून जिस तरह इंकार करता है, उस पर भी एक बार और गौर करने की जरूरत है, फिर चाहे इस देश की सरकारें, राजनीतिक दल, और सुप्रीम कोर्ट भी अब तक पत्नी की बलात्कार की शिकायत को किसी सजा के लायक नहीं मान रहे हैं। पुरानी चली आ रही सामाजिक व्यवस्था में फेरबदल आसानी से नहीं होता है। सतीप्रथा से लेकर बाल विवाह तक के खिलाफ कानून आसानी से नहीं बन पाए थे, और उन पर अमल तो और भी मुश्किल से हो पाया था, और आज दशकों बाद भी हम अपने आसपास गांव-कस्बों के मामले देखते हैं जहां पुलिस और प्रशासन जाकर बाल विवाह को रोकते हैं। इसलिए जिस देश में हाईकोर्ट के कई जज बहुत से फैसलों में औपचारिक रूप से मनुस्मृति का हवाला देते हैं, वहां महिला अधिकार की बात करना आसान नहीं है। जहां बड़ी अदालतें अपने लिखत फैसलों में महिलाओं के अधिकार कुचलने में जरा भी लिहाज नहीं करती हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर शादीशुदा महिला की रेप की शिकायत को किसी लायक नहीं माना है, तो उसमें हैरानी नहीं होती है। यह बात सिर्फ हिन्दुस्तान की नहीं है, हम अमरीका की बात करें तो वहां सदियों के लोकतंत्र के बाद भी 1920 तक तो महिलाओं को वोट डालने का हक नहीं मिला था, जबकि इसके पहले आधी सदी से देश भर में इसके लिए संघर्ष चल रहा था। दुनिया के बाकी देशों का इतिहास भी अलग-अलग दर्जों का तालिबानी इतिहास रहा है, जो कि आज हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं। और जब जजों का यह हाल रहता है कि वे महिला के किसी बुनियादी अधिकार के बारे में नहीं सोचते हैं, तो उनके नीचे के, कानून की और इंसाफ की कुछ कमसमझ रखने वाले वकील और अफसर और क्या सोच सकते हैं? नतीजा यह होता है कि थाने से लेकर हाईकोर्ट तक महिला के हक अलग-अलग कई तरह के बूटों से कुचले जाते हैं। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट भी महिलाओं को बराबरी के नागरिक अधिकार और मानवाधिकार देते हुए नहीं दिख रहा है, और राजनीतिक दल और संसद तो दकियानूसी रहते ही हैं। सुधारवादी, प्रगतिशील, और न्यायप्रिय नजरिया जब किसी तबके का नहीं रहता, तो महिला को अपनी लड़ाई खुद ही लडऩी पड़ती है। हाईकोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद इसकी जरूरत और अधिक लग रही है कि महिला को सेक्स के सामान की तरह इस्तेमाल किए जाने पर रोक कैसे लग सकती है।
लोगों को याद होगा कि कुछ देशों में आईएसआईएस, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों ने इस्लाम की एक किसी बहुत ही तंगनजरिए की व्याख्या करते हुए महिलाओं को सेक्स-गुलाम बनाने को भी जायज ठहराया था। ऐसे सैकड़ों मामले मीडिया में बड़ी बारीकी से दर्ज हैं जिसमें इस्लामिक स्टेट नाम के आतंकी संगठन ने हजारों महिलाओं को सेक्स-गुलाम बनाया, और औपचारिक रूप से उसे धर्म के अनुरूप भी कहा। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का और हिजाब लादकर रखा जाता है, जो कि सीधे-सीधे उन्हें समाज के भीतर दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का काम है। इसके अलावा चार शादियां, तीन तलाक जैसे और रिवाज भी हैं जो कि महिलाओं के इंसानी हकों के खिलाफ हैं। इसलिए लड़ाई सिर्फ किसी एक धर्म की महिला की अपनी सामाजिक व्यवस्था, या अपने देश के कानून से लड़ाई की नहीं है, उसे कदम-कदम पर संघर्ष करना रहता है, और जबलपुर हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी भारत की महिलाओं को संघर्ष करना रहेगा। अभी हम मौजूदा कानूनों की बेहद तकनीकी व्याख्या करके महिला की शिकायत को खारिज करने पर अधिक कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन प्राकृतिक न्याय की हमारी बड़ी साधारण समझ यह कहती है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिकपीठ में टिकना नहीं चाहिए, फिर चाहे वह संवैधानिकपीठ संसद को ही यह सिफारिश क्यों न करे कि उसे महिला के साथ पति द्वारा जबरिया सेक्स के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
अमरीका में शेयर मार्केट से जुड़े हुए कम्प्यूटर एल्गोरिदम बनाने वाले एक विशेषज्ञ ने अभी एक किताब लिखी है कि किस तरह वक्त बचाया जा सकता है। इस लेखक, निक सॉनेनबर्ग कई जगह भाषण देते हैं, और दुनिया के कामयाब कामगारों को उनके रोज के काम में वक्त बचाने की तरकीबें बताते हैं। दरअसल शेयर मार्केट का कारोबार ऐसा होता है कि किसी कंपनी के शेयरों में पूंजीनिवेश करते हुए अगर एक सेकेंड की भी देरी होती है, तो उसमें भाव ऊपर-नीचे हो सकता है, और नफा नुकसान में बदल सकता है। एक-एक पल की कीमत वहां समझ आती है। और ऐसे एक-एक पल न सिर्फ फैसले लेते वक्त महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि जिंदगी में हर जगह महत्वपूर्ण रहते हैं, हर दिन, और हर वक्त। लोग रोज के कामकाज में अगर कुछ वक्त बचा सकते हैं, तो उस वक्त का एक उत्पादक उपयोग हो सकता है। यह वक्त बचाना रोज के ऐसे छोटे-छोटे कामों में हो सकता है कि वहां पर वक्त की बर्बादी का किसी को ध्यान भी नहीं रहता।
कामयाब लोगों में से कुछ लोग जो कि अपनी कल्पनाशीलता की वजह से आगे बढ़ते हैं, उनकी बात छोड़ दें, तो बाकी अधिकतर लोग वक्त को लेकर किफायत बरतने वाले भी रहते हैं। दिन में घंटे तो चौबीस ही रहते हैं, सोने के वक्त में तो कटौती हो नहीं सकती है, लेकिन काम और निजी जिंदगी की बाकी चीजों में रात-दिन का दोतिहाई वक्त गुजरता है, और इन्हीं 16 घंटों में खासी किफायत और खासी बचत की जा सकती है। हर किसी की जिंदगी में तरीके और कामकाज बहुत अलग-अलग रहते हैं, इसलिए कोई एक फॉर्मूला हर किसी पर फिट नहीं बैठ सकता, लेकिन यह चौकन्नापन हर किसी के काम आ सकता है कि एक-एक सेकेंड की बचत के कौन-कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाएं। रोज कपड़ों को किस तरह रखा जाए, लैपटॉप बैग, और कपड़ों की जेब में कौन सा सामान कहां रखा जाए, ताकि ढूंढने में कुछ पल भी खराब न हो, किस तरह कागजों के गट्ठे को व्यवस्थित करके रखा जाए, ताकि अलग-अलग कागज तुरंत हाथ आ जाएं, चाबियां कैसे जगह पर रखें ताकि ढूंढने में समय बर्बाद न हो, बाजार से लाने वाले सामान किस तरह सामानों की लिस्ट किस तरह बनाई जाए ताकि दुबारा चक्कर न लगे, और कम से कम समय में खरीददारी पूरी हो जाए, ऐसी हजार किस्म की बातें हो सकती हैं जिनमें से कुछ दर्जन बातें तो हर किसी के काम आ सकती है। लोगों को रोज दवाईयां लेनी रहती हैं, और उन्हें एक साथ इस तरह व्यवस्थित नहीं रखा जाता कि वक्त बर्बाद किए बिना उन्हें निकाला जा सके। ऐसा ही रसोई के कामकाज में होता है, ऑफिस के कामकाज में होता है, और रोजाना आवाजाही के रास्तों को तय करने में भी होता है कि किस वक्त कौन सी सडक़ खाली रहती है। कुछ लोग ऑनलाईन कुछ कामों को घर पर करने के बजाय ऑफिस में आकर करें, तो हो सकता है कि घर से जल्दी निकलने पर सडक़ खाली मिले, और ऑफिस में आकर उसी काम को करते हुए सफर का वक्त बच जाए। आमतौर पर लोग अपने खुद के वक्त को इतना कीमती नहीं मानते कि वे अलग-अलग वक्त पर सडक़ों पर ट्रैफिक के दबाव को ध्यान में रखकर काम को पहले या बाद में कर लें, लेकिन जिंदगी में कामयाब होना है तो वक्त की जरा-जरा सी बर्बादी को रोकना जरूरी है। आज का वक्त कई तरह के डिजिटल उपकरणों का है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, और दूसरी चीजों को चार्ज करने की जगह और वक्त से भी कई बार समय बचता है, और कभी-कभी तो किसी नाजुक मौके पर इनमें चार्जिंग न रहने से काम ही ठप्प हो जाता है। इसलिए वक्त और मेहनत, इन दोनों की किफायत का मिजाज ही बनाना पड़ता है। जो लोग चौकन्ने रहेंगे, वे लोग हर मामले में चौकन्ने रहेंगे, और जो लोग लापरवाह रहेंगे, वो हर काम में वक्त बर्बाद करते रहेंगे।
जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, या कि किसी मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो वक्त और अधिक मायने रखता है, और उन्हें अपने नोट्स, अपनी किताबें, इंटरनेट पर सर्च की गई जानकारी को अलग-अलग फाईल और फोल्डर बनाकर रखना आना चाहिए। जिन लोगों को बार-बार सफर पर जाना पड़ता है, और कई तरह के सामान रखने पड़ते हैं, वे अगर कोई छोटा सा सामान भूल जाएं, तो हो सकता है कि दूसरे शहर में रात-बिरात दवा की एक टेबलेट ढूंढते हुए पांच रूपए की दवा पर पांच सौ रूपए की टैक्सी का खर्च भी जुड़ जाए। हर किसी की जिंदगी में ऐसी अलग-अलग बातें रहती हैं, जिन पर ध्यान देने से, और अपने वक्त की कीमत समझने से लोग खुद भी सुधार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा न हो पाए, तो उसके लिए हर शहर में कुछ जानकार लोग ऐसी क्लास भी ले सकते हैं, कि हर दिन कुछ वक्त कैसे बचाया जाए, और उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। कहने-सुनने में यह बात कुछ हल्की और कम महत्वपूर्ण लग सकती है, लेकिन जब हम बचाए गए ऐसे पलों को पूरी जिंदगी के हर दिन के साथ जोडक़र देखेंगे, तो समझ पड़ेगा कि हम कितनी बड़ी बचत या कितनी बड़ी बर्बादी की बात कर रहे हैं। जो लोग किसी किताब को पढ़ते हुए बीच में छोडऩे पर बुकमार्कर नहीं लगाते हैं, वे दुबारा शुरू करने पर दो-चार पन्ने दुबारा पढऩे बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बुकमार्कर पर ऊपर-नीचे होने वाला तीर का ऐसा निशान भी बनाकर रखते हैं कि किसी लाईन पर ले जाकर उसे रख दिया जाता है कि किताब बंद करते समय उसे कहां तक पढ़ा गया था।
यह चौकन्नापन एकाएक नहीं आ सकता, और जिंदगी के किसी एक दायरे में अलग से नहीं आ सकता, इसके लिए लोगों को अपना स्वभाव ही सावधानी का ढालना पड़ता है, और लगातार ध्यान भी रखना पड़ता है कि कहां लापरवाही से समय बर्बाद हो रहा है। अगर किसी शहर में टाईम मैनेजमेंट सिखाने वाले कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं, तो वे बहुत से लोगों को यह अहसास करा सकते हैं कि वे हर दिन किन कामों में कितना वक्त बचा सकते हैं। लेकिन यह किफायत उन्हीं लोगों के काम की है जो कि अपने बचे हुए वक्त को किसी तरह इस्तेमाल करते हैं। जो लोग रोजाना टीवी या मोबाइल फोन की स्क्रीन पर घंटों तक रील्स देख सकते हैं, वे वक्त बचाकर भी क्या कर लेंगे, बिना काम की कुछ और रील्स देख लेंगे।
फिलहाल यह याद रखने की जरूरत है कि गया हुआ वक्त कभी लौटता नहीं, इसलिए आए हुए वक्त का अच्छे से अच्छा, और अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
आज रोज के मुद्दों से हटकर एक काल्पनिक मुद्दे पर लिखने की जरूरत लग रही है। दुनिया के अलग-अलग देशों में जिस रफ्तार से मौसम की मार अधिक कड़ी होती जा रही है, और बार-बार बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह तो समझ आ रहा है कि यह सिलसिला बेकाबू है, और इसके पहले कि लोग समझ पाएं कोई देश-प्रदेश या तो डूब जाएंगे, या सूखे के शिकार होकर खाली हो जाएंगे। दुनिया के देशों को हांकने वाले लोगों को अब तक जलवायु परिवर्तन के खतरों का अंदाज नहीं हो रहा है, क्योंकि ताकतवर देश अपनी अधिक खपत के चलते इसके लिए अधिक जिम्मेदार हैं, और इसकी मार जिन गरीब देशों पर अधिक पड़ रही है वे कुछ करने की हालत में नहीं हैं।
ऐसे में हम दो चीजों को मिलाकर देखना चाहते हैं। पहला तो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जो कि लगातार जंगली हिरण की तरह छलांगें लगाकर आगे बढ़ रहा है, और उसकी क्षमता और संभावना आज भी कहां तक पहुंच गई है, यह किसी के सामने साफ नहीं है। दूसरी तरफ दुनिया में वैचारिक रूप से इंसाफ के हिमायती लोग हैं, जिनमें से कई लोग तरह-तरह के हथियारबंद आंदोलनों को छेड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसाफ उसी रास्ते लाया जा सकता है। इसके साथ-साथ अब कम्प्यूर हैकिंग और साइबर हमलों के इस युग में हथियारबंद होना भी जरूरी नहीं रह गया, क्योंकि महज कम्प्यूटरों का इस्तेमाल करके हथियारों के मुकाबले हजारों गुना अधिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिसमें लहू भी नहीं बहता। ऐसे ही अगर दुनिया के कुछ वैचारिक रूप से आतंकी लोग यह तय कर लें कि जिन देशों, तबकों, या लोगों की वजह से दुनिया खत्म हो रही है, और वे ऐसे लोगों को हटा देना चाहें, तो क्या यह मुश्किल होगा? हम किसी को हिंसा सुझा नहीं रहे हैं, लेकिन धरती की बर्बादी से फिक्रमंद कुछ लोगों को बिना हिंसा के अगर इसे रोकना सूझेगा, तो वे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से क्या-क्या कर सकते हैं यह जरूर सोचना चाहिए।
हमारे जैसी बहुत मामूली जानकारी, और जरा सी समझ रखने वाले लोग भी यह समझ सकते हैं कि धरती की तमाम बर्बादी हाल के कुछ सौ बरसों के भीतर की है, और आबादी के एक छोटे हिस्से की खपत और कारोबारी चाह के चलते धरती खत्म हो रही है। इंसानों के रहने के तौर-तरीकों, और उनकी हसरतों के कारण धरती के साधन अंधाधुंध रफ्तार से खत्म हो रहे हैं, और सबसे संपन्न तबका इसके लिए सबसे अधिक जवाबदेह है। ऐसे में धरती को बचाने का बीड़ा उठाने वाले कुछ लोगों को लग सकता है कि धरती पर सबसे अधिक खपत वाले लोगों को कैसे रोका जाए? संपन्न और विकसित देशों में टिड्डों की तरह फुदकने वाले छोटे-छोटे निजी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों की शिनाख्त एआई के लिए पल भर का काम है, और इन सबके संचार उपकरण कहीं न कहीं कम्प्यूटरों से जुड़े हुए हैं, अगर कोई पर्यावरण-आतंकी ठान लें, तो वे इन सबको तरह-तरह से खराब या खत्म करने का काम कर सकते हैं। हम जुर्म के तरीके बताना नहीं चाहते, लेकिन जुर्म के खतरों की तरफ से आगाह जरूर कर रहे हैं।
इसी तरह दुनिया में बिजली की सबसे अधिक निजी खपत करने वाले ग्राहकों की जानकारी बिजली कंपनियों के कम्प्यूटरों से पल भर में निकाल ली जाएगी, उनके पते मिल जाएंगे, और अगर एक साथ ऐसे करोड़ों ग्राहकों की बिजली सप्लाई में खलबली मचा दी जाएगी, तो बिजलीघर ठप्प पड़ जाएंगे। इंसाफ के लिए साइबर-आतंक पर अगर लोग उतारू हो जाएंगे, तो वे सबसे संपन्न तबके के लोगों की शिनाख्त के हजारों मौजूद तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, बैंकों के सबसे बड़े ग्राहकों को देख लेंगे, शेयर मार्केट और कारोबार के सबसे बड़े खिलाडिय़ों को देखे लेंगे, और दुनिया में सबसे महंगी कारों के ग्राहक, सबसे बड़े मकानों के मालिक पहचान लेंगे, और इन सबकी जिंदगी के किसी भी पहलू से जुड़े हुए कम्प्यूटरों पर हमले करके इनका जीना हराम कर देंगे, ताकि धरती के सामानों और साधनों की इनकी खपत ठप्प पड़े। पता लगेगा कि न इनके बैंक खाते काम कर रहे हैं, न इनके अस्पताल रिकॉर्ड मिल रहे हैं, और न ही इनके फोन या ईमेल काम कर रहे हैं। आज के मामूली साइबर मुजरिमों से परे, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की अकल्पनीय ताकत से लैस नए किस्म के समर्पित ईको-आतंकी अगर जुट जाएंगे, तो वे धरती पर अधिक खपत और फिजूलखर्ची की तमाम चीजों को ठप्प कर सकते हैं। सबसे ऑलीशान होटल और रिसॉर्ट ठप्प कर सकते हैं, फैशन के कारोबार तबाह कर सकते हैं जो कि फिजूल की खपत खड़ी करते हैं।
जिन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लैस साइबर-मुजरिमों की ताकत का अंदाज नहीं है, वे यह समझ लें कि इंटरनेट से किसी भी तरह जुड़ी उनकी गाडिय़ां किसी भी दिन ठप्प हो जाएंगी, मैकेनिक को बुलाने मोबाइल काम नहीं करेंगे, ईमेल बंद हो जाएंगे, एटीएम कार्ड काम नहीं करेंगे, बैंकों के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रह जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल बेकाबू हो जाएंगे, पेट्रोलियम कंपनियों से पंपों तक ईंधन नहीं आ पाएगा, बिजली और गैस सप्लाई ठप्प हो जाएगी, पानी का इंतजाम ठप्प हो जाएगा, ट्रेन और प्लेन के रिजर्वेशन खत्म हो जाएंगे, इतना सब कुछ एक साथ हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? हॉलीवुड की कई फिल्मों में पिछले बीस-पच्चीस बरस में इस किस्म की तबाही दिखाई गई है, और आज के लोग तो अगर उनका फोन और ईमेल ठप्प हो जाए, तो भी दिन भर का काम चलाने लायक नहीं रह जाएंगे।
इंसान जिस रफ्तार से पर्यावरण, दूसरे प्राणियों, जैव विविधता, प्रकृति, और धरती को खत्म करने में लगे हुए हैं, ऐसे में सचमुच ही कुछ ऐसे आतंकी खड़े हो सकते हैं जो घड़ी को सौ-दो सौ बरस पहले ले जाकर वहां छोडऩा चाहें। ऐसे फिक्रमंद-आतंकी बिजली, दूसरे तरह के प्रदूषण, और खपत, इसको एकमुश्त नीचे लाकर जलवायु परिवर्तन को बहुत अधिक धीमा कर सकते हैं, और किसी अपराध कथा लेखक के लिए यह एक दिलचस्प विषय हो सकता है कि धरती को बचाने के लिए बर्बाद करते लोगों को कैसे तबाह किया जाए। इसमें हमको जरा भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि कुछ किस्म की राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले लोग भी यह मान सकते हैं कि धरती को और पर्यावरण को बचाने के लिए, दुनिया की अधिकतर गरीब आबादी को बचाने के लिए, धरती की बर्बादी के जिम्मेदार सबसे संपन्न तबकों को कैसे रोक दिया जाए। आज भी कुछ साइबर-घुसपैठिए दुनिया भर के कम्प्यूटरों में घुसपैठ करके तरह-तरह से वसूली करते ही हैं, अगर कोई ऐसा समूह तैयार हो जाए जिसकी दिलचस्पी वसूली में न होकर संपन्न जिंदगी को रोक देने में हो, तो उसके लिए कोई बहुत अधिक औजारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। धरती के लोगों को एक तरफ तो अपनी खपत के बारे में सोचना चाहिए कि उससे जलवायु परिवर्तन किस तरह हो रहा है, दूसरी तरफ सरकारों को भी यह देखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के साथ मिलकर जलवायु-आतंकवादी, या पर्यावरण-आतंकवादी किस तरह बिना खून बहाए कुछ तबकों या देशों की जिंदगी पर ब्रेक लगा सकते हैं। यह उम्मीद तो हमें है नहीं कि अपनी जीवनशैली से धरती को बर्बाद करने वाले लोग हमारी इस चेतावनी से संभलेंगे, और किफायत बरतेंगे, लेकिन सरकारों में कुछ जिम्मेदार लोग हो सकते हैं जो कि ऐसे हमलों की कल्पना करके उससे बचने के कोई तरीके हों, तो उनके बारे में सोचें। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
अमरीका के इतिहास में ऐसा कम ही होता है कि किसी विश्वविद्यालय में पुलिस घुसे। न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में फिलीस्तीन के समर्थन में कई दिनों से छात्रों के प्रदर्शन चल रहे हैं जो कि अब बढ़ते-बढ़ते दो दर्जन अमरीकी विश्वविद्यालयों सहित पश्चिम के कोई आधा दर्जन देशों में फैल चुके हैं। और ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन की अर्जी पर पुलिस यूनिवर्सिटी में घुसी, और छात्रों को गिरफ्तार किया। ये छात्र अपने आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण और छात्रों तक सीमित रख रहे हैं, और एक छात्र नेता ने इजराइल के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी की थी, तो उसे आंदोलन से तुरंत ही अलग कर दिया गया। गैरछात्रों के भी इस आंदोलन में आने पर रोक लगाई गई है, और जगह-जगह चल रहे ये आंदोलन विश्वविद्यालय के इजराइल से जुड़े किसी भी अनुदान, रिसर्च ग्रांट, शैक्षणिक संबंध खत्म करने की बात कह रहे हैं। अमरीकी विश्वविद्यालयों का इजराइल के साथ गहरा रिश्ता है, और गाजा पर इजराइल की बमबारी को देखते हुए अमरीकी नौजवानों का एक मुखर तबका झंडे उठाए खड़ा है कि ऐसे हमलावर देश से उनके विश्वविद्यालय का कोई भी संबंध नहीं रहना चाहिए। यह आंदोलन कोलंबिया विश्वविद्यालय से शुरू होकर बहुत सी दूसरी जगहों पर फैला है, और अब यह ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्रिटेन जैसे दूसरे पश्चिमी देशों तक पहुंच गया है। अमरीका में ही अब तक हजार से अधिक छात्र गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और ये छात्र अमरीकी विश्वविद्यालयों के ऐसे किसी भी कंपनी से लेन-देन और रिश्ते खत्म करने की मांग कर रहे हैं जो कि गाजा पर हो रहे हमलों से किसी भी तरह की कमाई कर रही हैं। इसमें अमरीकी कंपनियां भी हैं। यह बात याद रखने की है कि फिलीस्तीन के गाजा पर चल रहे इजराइली हमलों से अब तक 34 हजार से अधिक फिलीस्तीनी मारे गए हैं।
अमरीका में छात्र आंदोलनों की यह ताजा लहर, ताजा हवा का एक झोंका है। यह नौजवान पीढ़ी में अपने देश से परे के मुद्दों से भी जुडऩे, और उनके प्रति जागरूक रहने का एक बड़ा सुबूत है। फिलीस्तीनी अपनी ही जमीन पर शरणार्थी की तरह बेघर जी रहे लोग हैं, जिनसे अमरीकी विश्वविद्यालयों या छात्रों का कोई भला नहीं हो सकता। उनका भला तो अतिसंपन्न इजराइली सरकार, वहां की कंपनियां, और वहां से जुड़े हुए कारोबारियों से हो सकता है क्योंकि अमरीकी विश्वविद्यालय निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर हजारों किस्म के शोध करते हैं, ग्रांट पाते हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय छात्र-छात्राओं के समूह अगर फिलीस्तीन के साथ खड़े हैं, और विश्वविद्यालय के इजराइल से किसी भी तरह के संबंध तोडऩे पर अड़े हैं, तो यह अपने हितों के खिलाफ जाकर एक सार्वजनिक हित की बात करने की मिसाल है, और इसके लिए अमरीकी छात्र आंदोलन की तारीफ की जानी चाहिए। जो नौजवान पीढ़ी अपने देश में वोट डालने के लायक हो जाती है, उस पीढ़ी को अपने देश-प्रदेश से लेकर दुनिया के बाकी हिस्सों के मुद्दों पर सोचना-विचारना भी चाहिए, और जिस देश की युवा पीढ़ी ऐसी नहीं रहती, और मुर्दा सरीखी रहती है, जैसी कि आज हिन्दुस्तान में है।
हिन्दुस्तान का एक हिस्सा मणिपुर देश के इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन सैकड़ों लाशें गिर जाने पर भी बाकी हिन्दुस्तान के लोगों के माथों पर शिकन नहीं आई, और वे मणिपुर को हिन्दुस्तान के बजाय पड़ोसी म्यांमार का हिस्सा अधिक मानते रहे। ऐसी मुर्दा हिन्दुस्तानी नौजवान पीढ़ी को अमरीका का आज का छात्र आंदोलन दिखाना चाहिए कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में हो रही बेइंसाफी पर नौजवान पीढ़ी का क्या रूख रहना चाहिए। यह एक अलग बात है कि अमरीका के छात्र आंदोलन हो सकता है कि नवंबर में वहां होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव पर कोई निर्णायक असर न डाल सकें, लेकिन अगर चुनाव में मुकाबला बहुत कड़ा रहेगा, तो टक्कर की ऐसी नौबत में छात्रों का रूख तय कर सकता है कि फिलीस्तीन के मुद्दे पर अमरीका के किस राष्ट्रपति को चुनना बेहतर होगा। हम अमरीकी चुनाव को लेकर कोई भविष्यवाणी करने की हालत में नहीं हैं, लेकिन वहां ऐसा माना जाता है कि डोनल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के गोरे वोटरों के बीच फिलीस्तीन को लेकर हमदर्दी नहीं रहती है, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी में ऐसे हमदर्द अधिक हैं। ऐसे में इन छात्र आंदोलनों का नुकसान किसे झेलना पड़ेगा यह बता पाना अभी आसान नहीं है, लेकिन अमरीका का इतिहास बताता है कि वियतनाम पर अमरीका के हमले के खिलाफ भी वहां के छात्र उठ खड़े हुए थे। और यह कैसा गजब का संयोग है कि 2 मई 1964 को इसी न्यूयॉर्क के इसी कोलंबिया विश्वविद्यालय में चार सौ छात्रों ने वियतनाम पर अमरीकी हमले के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, और न्यूयॉर्क शहर में जुलूस निकाला था। इसके बाद अमरीकी सरकार के खिलाफ यह आंदोलन जगह-जगह कई विश्वविद्यालयों में फैला था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ भी अमरीकी विश्वविद्यालयों ने आंदोलन किया था, और ऐसी कंपनियों से विश्वविद्यालय के रिश्ते तोडऩे की मांग की थी जो रंगभेदी दक्षिण अफ्रीकी सरकार के साथ कारोबार करती हैं। खुद अमरीका के भीतर रंगभेद के खिलाफ अमरीकी छात्रों के सभी नस्लों के नौजवान आंदोलन करते रहे हैं।
हिन्दुस्तान में छात्र आंदोलन या नौजवान आंदोलन मुर्दा पड़े हुए हैं। यह नौबत इस देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। लोग 18 बरस की उम्र से वोट डालने का हक पा लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने देश-प्रदेश के असल जलते-सुलगते मुद्दों की जानकारी पाने की भी फुर्सत नहीं है। उन्हें काम धेले का नहीं है, और जागरूकता पाने के लिए वक्त घड़ी का नहीं है। आज लोकतंत्र के बहुत से पहलुओं को देखकर अगर कलेजा ठंडा करने की जरूरत लगती है, तो हिन्दुस्तान के बाहर देखना पड़ता है। हिन्दुस्तान के नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा आज धर्म के चक्कर में इस हद तक डूब गया है कि उसे धर्म ही सबसे बड़ा कर्म लगने लगा है। यह धर्म हिन्दुस्तानी जनचेतना पर अफीम की तरह असर कर रहा है, और लोगों की लोकतंत्र के प्रति जागरूकता को संवेदनाशून्य बना चुका है। इस देश की नौजवान पीढ़ी को आज इस वक्त अमरीकी विश्वविद्यालयों में चल रहे छात्र आंदोलन को देखना चाहिए, और फिर यह सोचना चाहिए कि क्या हिन्दुस्तान में छात्र फिलीस्तीन के लिए न सही, अपने खुद के लिए आवाज उठाने का हौसला रखते हैं? (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
पहले गुजरात के सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार पार्टी को दगा देकर बैठ गया, और फिर मध्यप्रदेश के इंदौर में तो भाजपा के वहां के सबसे बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने खुद गाड़ी में ले जाकर कांग्रेस उम्मीदवार का नाम वापिस करवा दिया। इसके बाद इन दो सीटों पर तो कोई चुनाव बचा ही नहीं। इनके अलावा मध्यप्रदेश की खजुराहो सीट पर इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का पर्चा खारिज हो गया था क्योंकि उस पर दस्तखत नहीं था। उसे भी सोचा-समझा काम माना जा रहा है। अभी हो सकता है कि देश में कुछ और जगहों पर भी ऐसा हो जाए। लोकतंत्र में कानून के तहत जिस तरह की साजिशों की गुंजाइश रहती है, यह उनमें से कुछ नमूने हैं। न तो ऐसा पहली बार हो रहा है, और न ही भाजपा पहली पार्टी है जो कि ऐसा करवा रही है। लेकिन हैरान यह बात करती है कि जो पार्टी चार सौ से अधिक सीटों का दावा कर रही है, उसे ऐसा करवाने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या भाजपा का आत्मविश्वास (या अतिआत्मविश्वास?) कुछ कमजोर पड़ रहा है कि वह मोदी सरकार और अपनी राज्य सरकारों की सफलता के दावे छोडक़र मंगलसूत्र को मुद्दा बना रही है?
लेकिन इससे परे यह भी याद रखने की जरूरत है कि जब जिस पार्टी की हवा चलती है, वह इसी तरह के काम करने में लग जाती है। छत्तीसगढ़ में 2000 में मध्यप्रदेश से अलग होकर पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी, तो एक गैरविधायक अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने। उनके पास कांग्रेस विधायकों का पर्याप्त बहुमत था, लेकिन उन्होंने विधानसभा में आने के लिए एक भाजपा विधायक से इस्तीफा दिलवाकर वहां से उपचुनाव लड़ा जो कि भाजपा का राजनीतिक मखौल उड़ाने जैसा काम था। इसके बाद उन्होंने भाजपा के दर्जन भर विधायक खरीदे, क्योंकि विधानसभा के भीतर तो कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत था, लेकिन कांग्रेस विधायक दल के भीतर बहुत कम लोग जोगी के नामलेवा थे। इसलिए भाजपा से इतने विधायकों को तोडक़र जोगी ने कांग्रेस विधायक दल में अपनी निष्ठावान सदस्य बढ़ाए थे, और अपनी ताकत का अनुपात बेहतर किया था। इसके तुरंत बाद 2003 का चुनाव हुआ, तो कांग्रेस की बुरी शिकस्त हुई, जोगी सरकार को जनता ने खारिज किया, लेकिन जोगी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने बस्तर के उस वक्त के भाजपा सांसद बलीराम कश्यप के साथ मिलकर भाजपा से परे एक सरकार बनाने की कोशिश की, इसके लिए नगद रकम भी खर्च की गई, और कांग्रेस विधायक दल की तरफ से जोगी ने राज्यपाल के नाम एक समर्थन पत्र भी दिया जिसमें सोनिया गांधी की सहमति-अनुमति होने का झूठा दावा किया गया था। वह पूरा मामला भांडाफोड़ होने से वह छत्तीसगढ़ की इतिहास का सबसे बड़ा, और देश के इतिहास का एक सबसे बड़ा विधायक खरीद-बिक्री कांड हुआ था।
लोगों को याद होगा इसके बाद प्रदेश में तीन बार राज करने वाली भाजपा की रमन सिंह सरकार के चलते हुए बस्तर के अंतागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को बेचते हुए अजीत जोगी और उनका बेटा अमित जोगी टेलीफोन रिकॉर्डिंग में पकड़ाए, और खरीदते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह, और उनका दामाद कॉल रिकॉर्डिंग में फंसे। जोगी प्रदेश कांग्रेस में कोई और नेता बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, उन्होंने अपने प्रभाव वाले उम्मीदवार को सत्तारूढ़ भाजपा के हाथ बेच दिया था, और इस खरीद-बिक्री की टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स बताती थी कि अजीत जोगी ने उस वक्त के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को नीचा दिखाने के लिए क्या-क्या नहीं किया था। इस अंतागढ़ टेपकांड के सारे सुबूत सामने आने के बाद अमित जोगी को पार्टी से निलंबित किया गया था, और इसके साथ ही जोगी का कांग्रेस से नाता भी खत्म हुआ था। आज जिस तरह गुजरात के सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार ने आखिरी पल में जाकर अपना नामांकन वापिस लिया है, और उसके साथ-साथ सत्तारूढ़ भाजपा की तमाम मशीनरी ने सूरत के बाकी सारे उम्मीदवारों को शाम-दाम-दंड-भेद से बिठा दिया था, और भाजपा उम्मीदवार की देश में सबसे पहली जीत घोषित हो पाई, ठीक वैसा ही काम छत्तीसगढ़ की अंतागढ़ सीट पर भी किया गया था। अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा प्रत्याशी को छोडक़र बाकी हर उम्मीदवार को बिठा दिया गया था, और सिर्फ एक उम्मीदवार सत्ता की पकड़ में नहीं आया था, इसलिए चुनाव की नौबत आई थी, वरना सूरत की तरह वहां भी बिना चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया गया होता।
देश में वामपंथी दलों को छोडक़र अधिकतर पार्टियां ऐसी रही हैं जिन्हें किसी भी तरह की खरीद-बिक्री से परहेज नहीं रहा। नेता निजी स्तर पर बिकते हैं, और पार्टियां संगठन के स्तर पर खरीददारी करती हैं, भारतीय संसदीय व्यवस्था दुनिया की एक सबसे अश्लील और बेशर्म मंडी बनी हुई है। दिक्कत यह है कि चुनाव कानूनों के तहत इनमें से कोई भी बात जुर्म नहीं है, और लोग अपनी काया या आत्मा जो भी बेचें, उसमें कुछ गैरकानूनी नहीं रहता। इतना जरूर है कि इस देश में देह बेचने वाली महिलाओं को तो जेल भेजने का पूरा इंतजाम है, लेकिन आत्मा बेचने वाले उम्मीदवारों, निर्वाचित नेताओं, और बाकी राजनेताओं के सम्मान के लिए मालाएं हैं, कानून की अदालत में रियायत है, जांच एजेंसियों से छूट है। अभी इंदौर में जिस कांग्रेस उम्मीदवार ने आखिरी पल में अपना नाम वापिस लिया और भाजपा में शामिल हुआ, उसके बारे में बताया जा रहा है कि राज्य पुलिस ने उसके खिलाफ कोई पुराना मामला ढूंढकर उसमें कोई नई गंभीर दफा जोड़ी थी, और रातों-रात कांग्रेस से गद्दारी करने के पीछे शायद वह भी एक वजह थी।
आज देश भर में मोदी सरकार की जांच एजेंसियों के घेर में आए हुए लोगों के भाजपा में जाने के बहुत से मामले गिनाए जाते हैं। लेकिन यह याद रखने की जरूरत है कि इमरजेंसी के वक्त जगजीवन राम को कांग्रेस छोडक़र विपक्ष में जाने से रोकने के लिए किस तरह की कोशिशें की गई थीं, और फिर मानो उन्हें सजा देने के लिए उनके बेटे सुरेश राम की 21 बरस की छात्रा-मित्र के साथ नग्न तस्वीरों से मेनका गांधी की पत्रिका, सूर्या, का पूरा एक अंक ही भर दिया गया था। इस पूरे स्कैंडल से जगजीवन राम के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की हसरतें धरी रह गई थीं। इसलिए किसी को पार्टी छोडऩे से रोकने के लिए, या पार्टी छोडऩे की सजा देने के लिए तरह-तरह के अनैतिक कामों का इस देश में लंबा इतिहास रहा है। आज भाजपा लोगों को घेरकर जांच और मुकदमे की नोंक पर अपनी पार्टी में ला रही है, लेकिन यह नया सिलसिला नहीं है, इन दिनों बहुत अधिक बढ़ा हुआ जरूर है। ऐसा लगता है कि न तो भारत का चुनाव कानून, और न ही किसी दूसरे तरह के कानून ऐसी साजिशों को रोक पा रहे हैं, हमारा यह मानना है कि दलबदल करने वाले लोगों के खिलाफ कानून कड़ा करने की जरूरत है। लोग अगर थोक में भी दलबदल करें, तो भी इसे नए दल के रूप में मान्यता देने के बजाय सभी का बचा हुआ कार्यकाल खत्म करने के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या वह प्रावधान अधिक न्यायसंगत होगा? इसके अलावा नई पार्टी में किसी के जाने पर कुछ बरस तक उसके चुनाव लडऩे पर रोक रहनी चाहिए, ऐसा इसलिए भी होना चाहिए कि रातों-रात इम्पोर्ट करके अगली सुबह उम्मीदवार बनाने की बेइंसाफी खत्म हो सके। आज भाजपा ने दूसरी पार्टियों से इतने अधिक लोगों को लाकर उम्मीदवार बनाया है कि एक मजाक चल रहा है कि जो लोग बचपन से शाखा जाते थे, और जनसंघ के वक्त से पार्टी में लगातार बने हुए हैं, उन्हें भाजपा टिकटों में आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मजाक से परे हकीकत यह है कि अपनी पार्टी को धोखा देकर दूसरी पार्टी से चुनाव लडऩे के सिलसिले को कुछ खत्म किया जाना चाहिए, इसे कैसे किया जा सकता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए।
हिन्दुस्तान-पाकिस्तान सरहद के दोनों ओर गिने-चुने ताकतवर लोगों की सरकारी और फौजी नफरत या रणनीति के बीच पाकिस्तान की 19 बरस की आयशा के सीने में हिन्दुस्तानी दिल धडक़ता है। उसके दिल के ट्रांसप्लांट के बिना उसका अधिक वक्त जिंदा रहना मुमकिन नहीं था, और हिन्दुस्तान के चेन्नई के अस्पताल और डॉक्टरों ने यह ट्रांसप्लांट किया, और इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान में रकम भी इकट्ठा नहीं हो पाई थी, हिन्दुस्तानी डॉक्टरों और अस्पताल में एक ट्रस्ट की मदद से आयशा को नई जिंदगी देने की यह पहल और कोशिश की है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्यम ट्रस्ट अब तक 175 हार्ट ट्रांसप्लांट में मदद कर चुका है, और दूसरे बहुत से इलाज और ऑपरेशन में भी।
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सरहदी तनातनी चल रही है, उसके पहले तक लोगों की सीधी आवाजाही थी, ट्रेन और बस से लोग आते-जाते थे, और अनगिनत पाकिस्तानियों को हिन्दुस्तान की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से नई जिंदगी मिलती थी। जब तक सरकारों के बीच तनातनी नहीं हुई, तब तक हिन्दुस्तान में जनता को यह कभी नहीं लगा कि पाकिस्तानियों को हिन्दुस्तान में इलाज क्यों मिले। लेकिन जब सरकारों, फौजों, और राजनीतिक दलों को खाई खोदना सुहाने लगा, तो फिर जनता के बीच भी नफरत के फतवे तैरने लगे। इलाज की बात तो अलग रही, जो रोजाना के हर किस्म के कारोबार की बात थी, और दोनों देशों के बीच आपसी मुनाफे का जो हाल था, उसे भी राजधानियों में बैठे लोगों की राजनीति और रणनीति ने खराब कर दिया। दोनों मुल्कों के बीच करोड़ों लोगों की सरहद पार रिश्तेदारी है, उनका भी आना-जाना बंद सरीखा हो गया। अब किसी और मुल्क से होते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच आवाजाही हो पाती है, और वह भी बड़ी सिमट गई है। दोनों देश सरहद पर फौजी खर्च बर्बाद किए जा रहे हैं, बर्फ लदी सरहद पर हर बरस जाने कितने ही जवान शहीद या कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन राजधानियों को रिश्ते सुधारना नहीं सुहा रहा है। तनाव को इस दर्जे पर ले जाया गया है कि फिल्म और टीवी के कारोबार में भी सरहद पार के लोगों का आकर काम करना रोक दिया गया है, और जो जनता दोनों तरफ के फिल्म, संगीत को पसंद करती है, उसे भी मन मारकर चुप रहना पड़ता है।
लोगों को याद होगा कि जब सुषमा स्वराज हिन्दुस्तान में विदेश मंत्री थीं, तब पाकिस्तान में भारत की एक गीता नाम की लडक़ी जाने किस तरह वहां गुम हो गई थी, और वहां के एक बहुत बड़े समाजसेवक, अब्दुल सत्तार ईधी परिवार की देखरेख में थी, और वहां पर वह हिन्दू धर्म का पालन भी करती थी, और उस परिवार ने उसे बेटी की तरह अपनाया हुआ था। सरहद के दोनों तरफ इंसानियत की खूबी कही जाने वाली ऐसी बहुत सी कहानियां बिखरी हुई हैं, और इनसे दोनों तरफ इंसानों का एक-दूसरे पर भरोसा बना हुआ है। दिक्कत सिर्फ राजधानियों में बसे हुए नेताओं और फौजी अफसरों को है जिनको अपने घरेलू दिक्कतों से उबरने के लिए भी सरहद पर तनातनी और पड़ोसी से रिश्ते बिगाडऩे में सहूलियत लगती है। नतीजा यह है कि दोनों देशों के गरीबों की रोटी के हक बेचकर फौजों पर खर्च किया जा रहा है, और हवा में दुश्मन पेश करके अपने-अपने लोगों को हवा में लाठी चलाने की खुशी मुहैया कराई जा रही है।
हम फिर आयशा की बात पर लौटें, तो इन दोनों मुल्कों की हकीकत यही है। किस तरफ के डॉक्टर, किस तरफ के मरीज, किस तरफ किसी मरीज से मिला हुआ दिल, किस तरफ जमा की गई रकम, इनमें से कुछ भी आड़े नहीं आता, और भले लोग बिना किसी भेदभाव के, किसी धर्म या मजहब का ख्याल किए बिना एक-दूसरे के काम आते हैं। हम यहां पर इस बात और बहस में भी जाना नहीं चाहते कि कौन किसके अधिक काम आते हैं, और कौन किसके कम। लेकिन सच तो यह है कि एक फिल्म, बजरंगी भाईजान, की कहानी की तरह दोनों तरफ के लोग एक-दूसरे की मदद करने को अपनी जान देने पर भी उतारू रहते हैं, और असल जिंदगी की ढेरों कहानियां इस फिल्म की तरह हैं। सरहद के दोनों तरफ और दोनों धर्मों के लोगों में से गिनती में ऐसे लोग कम ही हैं जो कि नफरत के फतवों पर जिंदा रहते हैं, ऐसे लोग खबरों में सुर्खियां अधिक पाते हैं, और नफरती टीवी चैनल इन्हीं की हेट-स्पीच पर सवार होकर गलाकाट मुकाबला करते हैं, लेकिन इससे दोनों मुल्कों के कारोबार की बचत नहीं हो पा रही, और गरीबों की बड़ी रकम तनातनी में बर्बाद भी हो रही है। आज जब दुनिया के कुछ देशों के बीच की सरहद मिटाकर उन्हें एक किया जा रहा है, उस वक्त हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच की दीवार ऊंची की जा रही है। इस नौबत को अगर समझदारी से खत्म किया जाए, तो शायद दोनों तरफ हर गरीब बच्चे को रोजाना एक गिलास दूध मिल पाएगा।
तमिलनाडु के जिस ट्रस्ट, जिस अस्पताल, और जिन डॉक्टरों ने यह ऑपरेशन किया है, और जिस मरीज से यह दिल मिला होगा, इन सबका योगदान दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने में बहुत बड़ा है। ये लोग न तो सरहद पर हैं, न मुल्कों की राजधानियों में हैं, लेकिन इनकी रहमदिली और दरियादिली से एक नौजवान लडक़ी को नई जिंदगी मिली है, और दोनों तरफ के अमन-पसंद लोगों को अपनी बात आगे बढ़ाने की एक वजह भी मिली है। हम इस एक हार्ट ट्रांसप्लांट को महज एक जिंदगी देने वाला नहीं मानते, हम इसे सरहद के आरपार सद्भावना बढ़ाने का एक मौका भी मानते हैं, और जिन लोगों का इंसानियत के बेहतर पहलुओं पर भरोसा हो, उन्हें ऐसे मामले बढ़ाते भी रहना चाहिए। जिस तरह फिल्म बजरंगी भाईजान देखने वालों को यह समझ पड़ता है कि सीमा के कंटीले तार दोस्ती और मोहब्बत को नहीं रोक पाते हैं, भला काम करने की नीयत को नहीं रोक पाते हैं, ठीक वैसी ही भावना और मदद अभी के इस ट्रांसप्लांट में सामने आई है। हमारी दोनों ही मुल्कों से यह गुजारिश है कि फौजी तनातनी से परे आम जनता की आवाजाही, कारोबार, खेल, फिल्म, टीवी, और साहित्य सरीखे मामलों को सरकारी दखल से अलग रखें, और इंसानों के बीच बेहतर आपसी रिश्ते एक दिन सरकारों को भी साथ बैठकर सुलह करने को मजबूर कर सकते हैं। यह एक अलग बात है कि कोई सुलह न होना इन सरकारों को अधिक सुहा रहा होगा, लेकिन हम इसी बात पर आज की चर्चा खत्म करना चाहेंगे कि चेन्नई के अस्पताल में हिन्दुस्तानी दिल पाने वाली पाकिस्तानी युवती इन दोनों मुल्कों के बीच एक किस्म का पुल बनी है, और इस पर चलकर बेहतर रिश्तों की आवाजाही होनी चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
उत्तरप्रदेश के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में फार्मेसी के चार छात्रों ने इम्तिहान की उत्तर पुस्तिका में बस जय श्रीराम लिख दिया था, और उन्हें 56 फीसदी अंक देकर पास किया गया। जब सूचना के अधिकार के तहत किसी और ने ये उत्तरपुस्तिकाएं मांगीं, तो इसका भांडाफोड़ हुआ। इसके बाद विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी बनाई, और इन उत्तर पुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन करवाया, तो उन्हें शून्य नंबर मिले। विश्वविद्यालय की जांच में दो शिक्षकों को इस काम के लिए दोषी ठहराया है। एक पूर्व छात्र ने आरटीआई से कॉपियां निकलवाईं, और राजभवन शिकायत की तब जाकर पिछली दिसंबर में जांच का आदेश हुआ था। इस मामले में रिश्वत भी एक वजह हो सकती है, लेकिन जिस तरह से धर्म के नाम का इस्तेमाल किया गया है, उससे तो पक्के धर्मालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टेबाजी ऐप के नाम से किसी की धार्मिक भावना को आज तक ठेस नहीं पहुंची है, उसी तरह जय श्रीराम लिखकर फेल को पास करवाने के कारोबार से भी भक्तों पर असर पड़ा नहीं दिखता है।
हिन्दुस्तान में ऐसा लगता है कि धार्मिक भावनाएं अब सहूलियत का सामान हो गई हैं, जब किसी से हिसाब चुकता करना हो तब इन भावनाओं को भडक़ाया जाता है, पुलिस या अदालत तक रिपोर्ट लिखाई जाती है, गले काटने के फतवे दिए जाते हैं, और बाकी वक्त लोगों का भक्तिभाव अन्ना हजारे के अंदाज में सोए रहता है। जिस तरह महाराष्ट्र के तथाकथित खादीधारी-गांधीवादी अन्ना हजारे कुछ चुनिंदा और नापसंद नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ छांट-छांटकर आंदोलन करते हैं, और बाकी भ्रष्ट लोगों के हाथ मजबूत करते हैं, आज हिन्दुस्तान में धार्मिक भावनाओं का हाल कुछ वैसा ही हो गया है। देश की तीन चौथाई से अधिक आबादी मांसाहारी है, लेकिन कौन कब मांस खाए, और कब न खाए, यह एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, तेजस्वी यादव के मछली खाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से चुनावी सभा में इस पर हमला किया। दूसरी तरफ गोवा और केरल से लेकर उत्तर-पूर्व तक के भाजपा नेता गोमांस की खुली वकालत करते हैं, लेकिन उनसे देश के हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होने दी जातीं, ऐसे राज्यों में वोटरों को साधने के लिए गोमांस की गारंटी दी जाती है, और देश में बाकी जगह सरकारें तय करती हैं कि कब किसे क्या खाना चाहिए।
हिन्दुस्तान में जिंदगी के असल मुद्दों को हाशिए पर धकेल दिया गया है, और पन्नों के बीच में इतनी गैरजरूरी बातें लिख दी गई हैं कि असल मुद्दों के लिए कुछ शब्दों की जगह भी न बचें। और हैरानी यह है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सतही और गैरजरूरी मुद्दों में इस कदर मगन हो गया है कि उसे अपनी खुद की असली दिक्कतों से लेना-देना नहीं रह गया है। पौराणिक कहानियों में जिस तरह से त्यागियों को बताया जाता है, हिन्दुस्तान में आज वोटरों का एक बड़ा हिस्सा वैसा ही त्यागी हो गया है, और वह शेर पालने का खर्च उठाने के लिए पांच सौ लीटर भी पेट्रोल-डीजल लेने की अपनी हिम्मत बताता है। असल जिंदगी में शेर पाने से क्या हासिल होगा इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। लोगों की आर्थिक स्थिति अपने बच्चों के दूध के लिए गाय-बकरी पालने की भी नहीं है, लेकिन उनका उन्माद उन्हें शेर पालने का हौसला देता है। यह एक अभूतपूर्व और असाधारण दर्जे की समझ है, जिसकी पूरी दुनिया में शायद ही कोई मिसाल मिले। अपनी राजनीतिक पसंद के लिए लोग अगर हर तकलीफ को अनदेखा करने के लिए, हर तकलीफ को उठाने के लिए तैयार हैं, तो फिर लोकतंत्र के लिए तकलीफ के अलावा इसमें और क्या है? और जब वोटर-आबादी का एक तिहाई हिस्सा ऐसा समर्पित हो जाए, तो इस समर्पण से चुनावी मुकाबला भला क्या हो सकता है?
लोगों के मन में राजनीतिक प्रतिबद्धता रहे यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह प्रतिबद्धता उनसे सही और गलत में फर्क करने की ताकत अगर छीन ले, तो यह प्रतिबद्धता आत्मघाती होती है। भारतीय लोकतंत्र आज ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। आज तकनीकी रूप से चुनाव कराना कामयाब होने को लोकतंत्र मान लिया गया है, और थोक में दल-बदल को संवैधानिक। इन दोनों मकसदों को पाने के लिए कितना जायज, और कितना नाजायज किया जा रहा है, यह बात अगर लोगों के लिए मायने नहीं रखती है, तो फिर ऐसा चुनाव लोकतंत्र के लिए भला क्या मायने रख सकता है? यह नौबत भयानक है। हिन्दुस्तान सहित बहुत से देश ऐसे रहे हैं जहां पर कुछ बड़े नेताओं का व्यक्तिवाद बड़ा लोकप्रिय रहा है। उन्हें तर्कों से परे समर्थन मिलते रहा है, लेकिन जब इसके साथ-साथ धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता का एक घोल बन जाता है, तो फिर उसके नशे का न तो कोई जवाब हो सकता, न ही कोई तोड़ हो सकता। भारत आज ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। इसके साथ-साथ जब न सिर्फ चुनावी राजनीति, बल्कि तमाम पांच बरसों की राजनीति, और जनधारणा प्रबंधन जैसे काम एक बहुत ही अनोखे पेशेवर अंदाज में किए जाने लगे हैं, तो हिन्दुस्तान के अधिकतर राजनीतिक दलों को इस बदले हुए माहौल में टिके रहने की तरकीब समझ नहीं आ रही है। और लोकतंत्र को कानून के दायरे में कई किस्म की राजनीतिक और चुनावी तरकीबों की इजाजत देता है, और देश में आज वही हो रहा है।
यह बात शुरू हुई थी फार्मेसी के इम्तिहान में विज्ञान की बातें लिखने के बजाय जय श्रीराम लिखकर आने वालों को पास करने से। जब खालिस विज्ञान की जगह खालिस धर्म ले ले, तो आज के वक्त को कुछ हजार साल पहले चले जाना चाहिए, और इन बरसों के विज्ञान को अछूत मानकर उसकी सहूलियतों से परहेज करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा के एक विधायक रिकेश सेन ने एक हिन्दू धार्मिक कार्यक्रम में कल भाषण देते हुए कहा कि देश के अंदर धर्म परिवर्तन कराने की कोई कोशिश करे तो उसकी गर्दन काटकर रख देना। एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट देश में नफरती-जहरीली बातों पर रोक लगा रहा है, कड़ाई बरत रहा है, तब गला या सिर काट देने की बातें पचाने की ताकत इस देश का चुनाव आयोग ही रखता है। और चुनाव आयोग की असाधारण पाचन क्षमता की डॉक्टरी जांच सुप्रीम कोर्ट को भी करवाना चाहिए क्योंकि आयोग की यह पाचन शक्ति लोकतंत्र को ही पचाकर खत्म कर रही है, और चुनाव को उसने महज एक मशीनी काम बनाकर रख दिया है। आज यहां पर हमने कुछ कतरा-कतरा बातों को जोडऩे की कोशिश की है, इसे पढऩे वाले लोग भी इससे जुड़ी हुई कुछ और बातों को जोडक़र देख सकते हैं।
अभी यह मामला अदालत में है, और न इस पर कोई फैसला हुआ है, और न ही वॉट्सऐप चलाने वाली कंपनी मेटा ने इसे हिन्दुस्तान में बंद किया है, लेकिन भारत सरकार के सूचना तकनीक कानून के मुताबिक अगर इस मैसेंजर सर्विस को सरकार के मांगे संदेश की जानकारी देनी होगी, तो उसके बजाय मेटा इस सर्विस को बंद कर देने के लिए तैयार है। कल इस कंपनी ने साफ-साफ कहा है कि वॉट्सऐप-संदेशों की गोपनीयता भंग करने के बजाय वह हिन्दुस्तान से इस सर्विस को हटा ही लेगी। वैसे तो यह शुरूआती टकराव सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, लेकिन फिर भी सरकार के कानून और कंपनी के तेवरों में यह एक सवाल खड़ा तो कर ही दिया है कि लोकतंत्र में निजता का कितना महत्व होना चाहिए, और सरकार जिसे कानून के खिलाफ माने, उसे उजागर करने की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए। भारत में टेक्नॉलॉजी तो मोटेतौर पर दुनिया के किसी भी सबसे विकसित देश जितनी है, लेकिन निजता के अधिकारों का महत्व यहां पर विकसित लोकतंत्रों के आसपास भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि बिना लोकतंत्र के टेक्नॉलॉजी कितनी खतरनाक हो सकती है, जनता के हक के लिए भी, और सरकार की जिम्मेदारी के लिए भी, यह समझने की जरूरत है।
आज भारत में देश की सरकार, और प्रदेशों की सरकारों से लोगों के मन में इतनी दहशत है कि वे लोगों के कॉल डिटेल्स और संदेशों में ताक-झांक करती हैं। जब इजराइल का बना हुआ, फौजी लाइसेंस पर मिलने वाला, पेगासस नाम का घुसपैठिया सॉफ्टवेयर भारत में इस्तेमाल करने की बात आई, तो केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया, और यह कहा कि वह यह भी टिप्पणी नहीं करेगी कि उसने यह सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एक तकनीकी विशेषज्ञ कमेटी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, और यह मुद्दा वक्त की मौत खत्म हो गया कि क्या देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं, और प्रमुख पत्रकारों के मोबाइल फोन पर केन्द्र सरकार की एजेंसियों ने पेगासस से घुसपैठ की थी, या नहीं। लेकिन लोगों के मन में इस बात को लेकर न सिर्फ सरकारी एजेंसियों पर शक है, बल्कि लोग जिनसे फोन पर बात करते हैं उन पर भी शक रहता है कि वे लोग बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं, या वॉट्सऐप जैसे मैसेंजरों की वीडियो कॉल को भी किसी दूसरे फोन को सामने रखकर उस पर तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं? दरअसल वक्त ऐसा ही आ गया है कि न सिर्फ सरकार चलाने के लिए, बल्कि राजनीति चलाने के लिए भी, और कारोबारी मुकाबलों के लिए भी लोग प्रतिद्वंद्वियों की जासूसी करते हैं, और ऐसे वक्त में लोगों को यह मानकर चलना गलत नहीं है कि वे अगर जरा भी महत्वपूर्ण हैं, तो निशाने पर हैं।
फिर सरकारी अफसर, खासकर खुफिया एजेंसियों के लोग, आने वाली हर सरकार के राजनेताओं को ऐसी कई तरकीबें बताते हैं कि कानूनी-गैरकानूनी तरीकों से कैसे मुकाबले में आगे रहा जा सकता है, और दूसरे लोगों को पीछे छोड़ा जा सकता है। ऐसे आसान औजारों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की सहूलियत हर ताकतवर के मन में लालच पैदा कर देती है, और फिर यह इंसानी मिजाज तो रहता ही है कि दूसरों की बंद जिंदगी में कैसे ताक-झांक की जाए। लोग तुरंत ही कानूनी और गैरकानूनी जासूसी के नफे देखने लगते हैं, और हिन्दुस्तान में शायद ही किसी को यह याद रहता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमरीका के राष्ट्रपति रहे रिचर्ड निक्सन को किस तरह विपक्ष की जासूसी करने के आरोप में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जिस किसी नेता को दूसरों की जासूसी करवाने में मजा आता हो, उन्हें यह देखना चाहिए कि अमरीकी राष्ट्रपति का इस हरकत के बाद क्या हाल हुआ था, और महाभियोग से बचने के लिए इस्तीफा देने वाले निक्सन पहले राष्ट्रपति हुए थे जिन पर विपक्षियों की जासूसी की तोहमत पूरी तरह साबित भी हुई थी।
भारत में आज सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली सिरे से सिरे तक सुरक्षित मैसेंजर सर्विस वॉट्सऐप सबसे अधिक लोकप्रिय है, और छोटे-छोटे कारीगर, और कामगार भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और निजी संदेशों से परे कारोबारी संदेशों को देखें तो भी हिन्दुस्तान में हर दिन दसियों करोड़ ऐसे संदेश आते-ृजाते हैं जिन पर इस देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा टिका हुआ है। हम केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी और फिक्र की बात नहीं करते, वह तो प्राथमिकता रहनी ही चाहिए, लेकिन उससे संबंधित संदेशों का महत्व इस मैसेंजर सर्विस से देश की अर्थव्यवस्था के साथ तौलकर भी देखना चाहिए कि अगर यह सेवा खत्म हो गई, तो कोई दूसरी सेवा क्या इस जरूरत को पूरा कर सकेगी? क्या भारत सरकार खुद ऐसी कोई मैसेंजर सर्विस शुरू कर सकेगी जिस पर लोगों को भरोसा भी होगा। आज तो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया से लेकर ईमेल, और मैसेंजर सर्विसों तक हर चीज निजी हाथों में हैं क्योंकि सरकारी औजारों पर किसी को गोपनीयता का भरोसा नहीं हो सकता। आज से करीब 25 बरस पहले बनी एक अमरीकी फिल्म, एनेमी ऑफ द स्टेट, लोगों को जरूर देखनी चाहिए कि निगरानी रखने की टेक्नॉलॉजी और सरकारी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल से कोई लोकतांत्रिक सरकार भी अपने विरोधियों को किस तरह खत्म कर सकती है। यह फिल्म 25 बरस पहले की अमरीकी सरकार की ताकत का एक नजारा पेश करती है, और तब से अब तक तो टेक्नॉलॉजी ने कई पीढिय़ां तय कर ली हैं, अब निगरानी और नुकसान की सरकारी ताकत कई गुना बढ़ गई है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत के लिए भी आज दुनिया की किसी सरकार के हाथ में नागरिकों की हर गोपनीयता देने का मतलब लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म कर देना होगा। जहां तक जनता की निजता की बात है, कोई सरकारों पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता, यह बात हमने हिन्दुस्तान और इसके प्रदेशों में लंबे समय से देखी हुई है, और जब निगरानी और जांच एजेंसियां सत्तारूढ़ नेताओं के साथ मिलकर मुजरिम गिरोह की तरह काम करने लगती है, तो जनता की निजता की चौकीदारी का, और उसमें ताक-झांक का हक इन लोगों को नहीं दिया जा सकता। आज हिन्दुस्तान में लोगों की निजी जिंदगी से लेकर हजार किस्म के काम-धंधों के बारे में सोचना चाहिए कि वॉट्सऐप जैसी मैसेंजर सर्विसों के बिना इस देश के लोगों का काम कैसे चलेगा? और यह बात तो जाहिर है ही कि जब लोगों की निजी जिंदगी में ताक-झांक के लिए कोई कंपनी सरकार को दरवाजे में एक सुराग बनाकर देगी, तो सरकार उस छेद को अपना सिर भीतर डालने जितना तो बना ही लेगी। अच्छा है कि यह मामला अदालत में पहुंचा हुआ है, और इस पर सरकारी रूख से परे कानूनी नजरिया भी सामने आ जाएगा।
छत्तीसगढ़ के जिन निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों का बिना भुगतान इलाज होता है, और जिसका भुगतान बाद में सरकार करती है, उनका काम ठप्प हो गया है। अस्पतालों का कहना है कि राज्य में आयुष्मान योजना का भुगतान ही हजार करोड़ से अधिक बकाया हो गया है, और ऐसे में उनके लिए यह मुमकिन नहीं है कि इस योजना के तहत इलाज और ऑपरेशन करें, और अस्पताल भी चलाएं। इस योजना में 40 फीसदी योगदान राज्य सरकार का रहता है, और 60 फीसदी रकम केन्द्र सरकार से आती है। छत्तीसगढ़ में पिछली भूपेश सरकार के समय से सैकड़ों करोड़ का यह बकाया चले आ रहा था, जो अब बढ़ते-बढ़ते शायद 13 सौ करोड़ तक पहुंच गया है। यह हालत भी तब है जब 6 महीने के फासले में दो-दो चुनाव हो रहे हैं, और 6 महीने बाद पंचायत-म्युनिसिपल चुनाव भी हैं, और वैसे में अगर गरीब जनता का इलाज बंद हो रहा है, तो उसके चुनावी-राजनीतिक नतीजे तो होंगे ही। पिछले विधानसभा चुनाव के समय केन्द्र सरकार से ग्रामीण रोजगार की योजना मनरेगा के भी 6-7 सौ करोड़ रूपए आने बाकी थे, और मजदूरी का भुगतान कई महीनों से नहीं हुआ था। एक और विभाग की बात करें तो जिन निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार योजना के तहत गरीब बच्चों का दाखिला होता है, वहां पर सरकार से उनकी फीस न पहुंचने की वजह से उन स्कूलों को भी परेशानी हो रही है। कुल मिलाकर कोई भी सरकार हो, उसकी जनकल्याण की योजनाओं का हाल इसलिए बदहाल है कि चुनावी नजरिए से इनकी घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन राज्य के बजट में इनका ठीक से इंतजाम नहीं रहता, और साथ-साथ बजट में दिखाई गई कमाई कभी पूरी नहीं आती। इन सबसे परे केन्द्र और राज्य सरकारों पर कोरोना-लॉकडाउन के दौर में जो भारी-भरकम बोझ पड़ा, उसमें भी हर राज्य कर्ज में दब गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई।
अभी चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुजुर्गों के इलाज की एक नई योजना भी घोषित की है, और चुनाव प्रचार के रूप में उसके फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। अब आज अगर पुरानी योजनाओं का यह हाल है कि न तो पिछली कांग्रेस सरकार, और न ही वर्तमान भाजपा सरकार सरकार की मौजूदा योजनाओं के तहत इलाज का खर्च उठा पा रही हैं, निजी अस्पताल अपने बिल लिए हुए बंद होने की कगार पर हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह की नई योजना की घोषणा के पहले यह तौलना जरूरी है कि इनका भुगतान कहां से होगा। चुनावी घोषणाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है कि जनता को मुफ्त में देने के वायदों की सीमा कैसे तय की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके उनकी राय पूछी भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर एक बार सरकार बना लेने के लिए राजनीतिक दल कोई भी वायदा करने के लिए तैयार हैं, और फिर चाहे उसे पूरा न कर सकें। छत्तीसगढ़ में यह बहुत भयानक नौबत है कि निजी अस्पताल सरकार की योजनाओं के तहत इलाज करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उधारी की उनकी क्षमता खत्म हो चुकी है।
चुनाव जीतने के गलाकाट मुकाबले से परे यह समझने की जरूरत है कि राज्यों को अंधाधुंध कर्ज लेकर रेवड़ी बांटने के अंदाज में सहूलियतें नहीं बांटनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार ने अपनी राजनीतिक घोषणा के तहत हर आय वर्ग के लोगों का मुफ्त सरकारी इलाज करवाने का वायदा किया था, और उसे लागू भी कर दिया था। नतीजा यह था कि महंगी कारों में अस्पताल पहुंचने वाले लोग भी मुफ्त में इलाज पा रहे थेे, और सरकार वादाखिलाफी की तोहमतों से बचने के लिए गरीब-अमीर सभी को मुफ्त इलाज दे रही थी, निजी अस्पतालों में भी। इस सिलसिले ने न सिर्फ सरकार के इस विभाग की कमर तोड़ दी, बल्कि राज्य का पूरा विकास भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। जनकल्याण की कोई भी योजना जरूरतमंद तबके के लिए ही होनी चाहिए। बहुत बड़े संपन्न किसानों की कर्जमाफी से लेकर, पैसेवालों के मुफ्त इलाज तक, राजनीतिक दल लापरवाही से कही हुई अपनी बातों पर अड़े रहने के लिए जनता के बजट का कितना भी हिस्सा खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। बिजली की रियायत देने के लिए गरीब-अमीर हर किसी को एक सीमा तक छूट देना भी इसी किस्म का बेदिमागी का फैसला है, क्योंकि जिनके घर एसी चलते हैं, हजारों रूपए का बिल आता है, उन्हें दो सौ यूनिट की छूट क्यों देनी चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के दौरान ही यह बात साफ होनी चाहिए कि राजनीतिक दल जब कभी ऐसी कोई घोषणा करें, तो उसके साथ यह शर्त जुड़ी रहे कि लाभ पाने वाले लोगों के बारे में नियम और शर्त भी घोषित की जाए, और अनुमानित खर्च भी बताया जाए। इसके बिना किसी तरह के जनकल्याण की कोई योजना, या कोई रेवड़ीनुमा योजना घोषित नहीं होनी चाहिए। इसे राजनीतिक दलों की मान्यता के चुनाव आयोग के नियमों से भी जोड़ा जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट जैसा कि कुछ दूसरे मामलों में करता है, संसद को भी सुझा सकता है कि वह इस बारे में कोई व्यापक कानून बनाए। आज देश के कई प्रदेशों की हालत मुफ्त की योजनाओं की वजह से खराब है। पंजाब मुफ्त की बिजली देकर दीवालिया होने की कगार पर है, गुजरात और हरियाणा में आयुष्मान योजना बंद ही कर दी है, बंगाल की हालत सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने की नहीं है। यह सिलसिला चुनावी जीतने के लिए किए जाने वाले वायदों की वजह से इस नौबत तक पहुंचा है। यह बंद होना चाहिए। देश में वित्तीय अनुशासन बने रहने के लिए यह भी होना चाहिए कि जनता के समझ आने वाली जुबान में केन्द्र और राज्य हर सरकार को अपनी योजनाओं की लागत समझाना चाहिए, और राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र की लागत साथ लिखनी चाहिए। आज कहने के लिए हर गरीब को अनाज, मकान, बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त इलाज, मुफ्त पढ़ाई जैसी हजार बातें कही जाती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मनरेगा के मजदूरों को भी महीनों तक मजदूरी नहीं मिलती। देश में यह राजनीतिक पाखंड खत्म होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की सुनवाई के दौरान ही ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि राजनीतिक दल, और केन्द्र या राज्य सरकारें जनता के सामने पारदर्शी हिसाब रखने को मजबूर हों। फिलहाल देश के राज्यों को इस बात से जूझना है कि जो इलाज जनता को चाहिए, उसका भुगतान कैसे होगा, और अभी इस चुनाव में जिन और लोगों को मुफ्त इलाज से जोडऩे की घोषणा हुई है, उनका खर्च कहां से आएगा?
राजस्थान के पिछले कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक सबसे भरोसेमंद ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने लोकसभा चुनाव मतदान के बीच गहलोत पर उनके कार्यकाल के दौरान गंभीर गलत काम करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह तक कहा है कि गहलोत ने पार्टी के भीतर अपने प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट के फोन टेप कराए थे। उन्होंने यह भी कहा कि किस तरह से मुख्यमंत्री सचिवालय, और पुलिस-प्रमुख जैसे लोग फोन टैप करने में शामिल थे। लोकेश शर्मा ने यह भी कहा कि पेपर लीक कराने के मामले में भी गहलोत सरकार शामिल थी। यह तो राजस्थान का ताजा मामला हुआ, छत्तीसगढ़ में कल तक कांग्रेस पार्टी में रहे एक मंझले नेता ने आज पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रूपए रिश्वत लेकर उन्हें टैक्समाफी देने का आरोप लगाया है। इसी तरह दूसरे प्रदेशों में भी देखें तो जहां-जहां कोई सत्तारूढ़ पार्टी जब गर्दिश में पड़ती है, तो उसमें सत्ता के कई भरोसेमंद लोग तरह-तरह के भांडाफोड़ करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बैनर्जी की तृणमूल कांग्रेस छोडक़र निकलने वाले बहुत से नेताओं ने भाजपा में जाने के बाद सरकार के भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ किया है।
अब सवाल यह उठता है कि सत्ता जब कोई भी गलत काम बिना कई लोगों के शामिल हुए नहीं कर सकती है, तो फिर वह, या उसके बड़े लोग किस तरह के हौसले के साथ अंधाधुंध, उगाही करने लगते हैं, जुर्म के दर्जे की साजिशें करने लगते हैं, और खतरा भी उठाते हैं? छत्तीसगढ़ के पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मायने में अब तक खुशकिस्मत बने हुए हैं कि उनके चारों तरफ के लोग ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं, उनकी सरकार हांकने वाले अविश्वसनीय ताकतवर अफसर आज जेल में हैं, लेकिन किसी ने भूपेश बघेल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, कम से कम अब तक तो ऐसा सामने नहीं आया है। अब सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री के दाएं हाथ से लेकर बाएं हाथ तक, उनके कानों से लेकर उनकी आंखों तक, तमाम लोग जब जेल में पहुंचे हुए हैं, या अदालत के कटघरे में हैं, तो नौबत इतनी खराब होने क्यों दी गई थी? देश के दूसरे प्रदेशों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आज भी कुछ जाहिर और कुछ रहस्यमय वजहों से एक बनी हुई है, लेकिन राजस्थान के पिछले सीएम गहलोत के ओएसडी सरीखे एक-दो लोग भी अगर इस प्रदेश में निकल आएंगे, तो क्या होगा? लेकिन सत्ता से मिलने वाली बददिमागी बड़ी भयानक होती है। एक किसी शायर ने लिखा था- तुमसे पहले ओ जो इक शख्स यहां तख्त-नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीं था।
न सिर्फ सरकारी भ्रष्टाचार के मामले में बल्कि सरकारी बददिमागी और राजनीतिक रंजिशों के मामले में भी लोगों को अक्ल नहीं आती है कि किसी दिन उनकी सत्ता नहीं भी रहने वाली है। ऐसा इमरजेंसी के दौरान भी हुआ था जब इंदिरा और उनके तानाशाह बेटे ने यह मान लिया था कि आपातकाल की ताकत जिंदगी भर रहने वाली है। जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के पिछले पांच बरस देखे हैं, उन्हें भी सत्ता के कुछ ऐसे ही यकीं देखने मिले थे। और आज देश के कई नेताओं के बयान सुनें तो भी यही लगता है कि उन्हें कभी सत्ता खत्म होने की कोई आशंका है ही नहीं। जबकि दुनिया में बहुत बड़े-बड़े राजा-महाराजा आए-गए हो गए हैं, जिनके आज कोई नामलेवा भी नहीं बचे हैं। कुछ इसी अंदाज में लोग भ्रष्टाचार में भी लगे रहते हैं। कई पार्टियां तो ऐसी रहती हैं कि सत्ता में आते ही पिछली सरकार के भ्रष्ट तंत्र का इस्तेमाल तुरंत शुरू कर देती हैं, और वहां से आगे फिर अपनी कल्पनाशीलता दिखाती हैं, नए-नए रास्ते और निकालती हैं। सरकार बनती नहीं हैं कि उसके भ्रष्ट होने की पुख्ता कहानियां हवा में तैरने लगती हैं। उन लोगों को देखकर लगता है कि या तो ये तमाम बदनामी के साथ सारे राजनीतिक पूंजीनिवेश का मुनाफा पांच बरस में निकाल लेना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए जाहिर है कि उन्हें आसपास के बहुत से लोगों को राजदार बनाना पड़ता है, और ऐसे ही राजदार आगे जाकर किसी दूसरी पार्टी में दाखिल होकर, या अदालत में वायदा माफ गवाह बनकर जुर्मों का जिक्र करने लगते हैं, सुबूत देने लगते हैं। हमको इसमें नुकसान का कुछ नहीं दिखता। जो नेता और अफसर जुर्म करते हैं उनके खिलाफ बेवफाई करने वालों को हम गद्दार कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि उससे देश का और कानून का तो भला ही हो रहा है। और किसी एक व्यक्ति के जुर्म के साथ वफादार रहने के बजाय देश के कानून के साथ वफादारी बेहतर है। ऐसा जितना अधिक से अधिक हो, जनता के हित में उतना ही अच्छा है। और जब सौ-पचास लोग अपने पुराने साथियों के भांडाफोड़ की वजह से जेल जाएंगे, तभी लोगों का हौसला गिरोहबंदी करके जुर्म करने पर से कम होगा। इंसानी रिश्तों में नेक काम के लिए अगर वफादारी निभती है, तो वह काम की है, जब नेता, पार्टियां, और सरकारें संगठित मुजरिम गिरोहों की तरह काम करने लगते हैं, तब तो उनके बीच के बेवफा लोग ही लोकतंत्र के प्रति वफादार कहे जा सकते हैं। इसलिए हम ऐसी किसी निजी वफादारी की कमी गहलोत के ओएसडी के भांडाफोड़ में नहीं देखते। चारों तरफ इसी तरह का भांडाफोड़ होते रहना चाहिए, और उसी से सत्ता के जुर्म घट सकते हैं।
यूपीए के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह की न कही हुई बातों को लेकर भी जिस तरह आज चुनावी बयानबाजी में उन पर तोहमतें लगाई जा रही हैं, उनको देखना भी भयानक है। किसी की बातों को तोडऩा-मरोडऩा तक तो ठीक है, लेकिन किसी की बातों के गोले का चूरा बनाकर, उसे मिट्टी की तरह सानकर उससे क्यूब की तरह चौकोन ढांचा बना देना तो कुछ ज्यादती ही है। गनीमत यह है कि मनमोहन सिंह की कही बातें वीडियो पर दर्ज हैं, ये एक अलग बात है कि आज के चुनावी माहौल के बिना भी जिन लोगों को झूठ फैलाना है, उन्हें कोई वीडियो सूबूत रोक नहीं पाता। मनमोहन सिंह ने देश के साधनों पर दलित, आदिवासियों, पिछड़े लोगों, और मुस्लिमों के पहले हक होने की जो बात कही थी, उसमें से पहले के तीनों तबकों को हटाकर सिर्फ मुस्लिम का नाम लेकर यह दहशत पैदा करना कि कांग्रेस आएगी तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर उसे घुसपैठियों में बांट देगी, बयानबाजी के अब तक के स्तर को भी एकदम से पीछे छोडऩे वाली बात रही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अभी हाल ही में तो देश की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने के लिए मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहे थे, लेकिन फिर वे पहले दौर के मतदान के बाद एकदम से जाने क्यों हिंदू-मुस्लिम, और घुसपैठिया-आबादी पर उतर आए हैं।
खैर, इस हड़बड़ी की जो भी वजह हो हम उसे चुनावी रूझान से जोडक़र देखना नहीं चाहते, लेकिन कल से कांग्रेस के एक दूसरे नेता के एक बयान को लेकर भाजपा के नेता टूट पड़े हैं। विदेश में बसे इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने अभी अमरीका के उत्तराधिकार टैक्स की तारीफ की है, और कहा है कि यह एक दिलचस्प कानून है जिसमें किसी दौलतमंद के मरने पर उसके बच्चों को सिर्फ 45 फीसदी संपत्ति मिलती है, और 55 फीसदी संपत्ति सरकार ले लेती है। उन्होंने कहा कि यह बड़ा दिलचस्प कानून है कि आप जीते-जी संपत्ति जुटाओं लेकिन जब आप जा रहे हैं तो संपत्ति का एक हिस्सा जनता के लिए छोडऩा होगा, पूरी संपत्ति नहीं, आधा हिस्सा। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा नहीं है, किसी अरबपति के जाने पर सब कुछ उसके बच्चों को ही मिलता है, देश या समाज को कुछ नहीं मिलता। सैम पित्रोदा की बात पर हमने अमरीका के इस कानून को पढ़ा तो यह वहां के कुछ राज्यों में ही लागू दिख रहा है, और मृतक के जीवनसाथी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, करीबी रिश्तेदारों को बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। यह टैक्स अधिक पैसेवालों पर ही लागू है।
अमरीका के इस उत्तराधिकार कानून पर अधिक चर्चा आज का मकसद नहीं है, लेकिन चूंकि सैम पित्रोदा इस बात पर भाजपा ने कांग्रेस की जमकर निंदा की है, और खुद कांग्रेस ने इसे सैम की निजी राय बताया है, और कहा है कि वे स्वतंत्र विचारक भी हैं, और हर बार वे कांग्रेस का रूख नहीं बोलते हैं। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने कहा है कि उनके बयान को बिना किसी संदर्भ के भारत के बारे में यह कहकर पेश करना कि कांग्रेस की सरकार बनने पर लोगों की आधी संपत्ति चली जाएगी, एक बहुत ही झूठा चुनाव प्रचार है। खुद सैम पित्रोदा ने भाजपा के खड़े किए हुए विवाद पर कहा कि उन्होंने निजी तौर पर अमरीका के उत्तराधिकारी टैक्स के बारे में जो कहा उसे तोड़-मरोडक़र गोदी मीडिया इस तरह पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बात तो किसी ने नहीं कही है कि भारत में लोगों की 55 फीसदी संपत्ति छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि क्या बातचीत में अमरीका की मिसाल देना गलत है?
इस विवाद को हम यही पर छोड़ते हैं, और इसके साथ-साथ अमरीका के इस टैक्स के बारे में बात करते हैं क्या सचमुच ही यह टैक्स बहुत खराब है? आज भी भारत में मां-बाप की छोड़ी हुई जमीन को बेचने पर लोगों को एक कैपिटेशन टैक्स देना पड़ता है जो कि उस जमीन की खरीदी कीमत, और उसके बाद कीमत में बढ़ोतरी का हिसाब लगाकर बिक्री के वक्त होने वाले मुनाफे पर लगने वाला टैक्स है। इसी तरह अगर भरत में संपन्नता के एक स्तर के ऊपर अगर उत्तराधिकार टैक्स किसी शक्ल में लगता भी है, तो उसमें क्या बुराई है? देश के आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि सबसे अमीर लोग और अधिक अमीर होते चल रहे हैं, और गरीबों की हालत और अधिक खराब होते चल रही है। यह फासला बढ़ते जा रहा है। ऐसे में अगर एक सीमा से अधिक अमीर लोगों के गुजरने पर इस देश में उनकी की गई कमाई पर अगर उत्तराधिकार टैक्स लगता है, तो उसका इस्तेमाल देश के उस ढांचे पर किया जा सकता है जिस ढांचे की वजह से देश में उद्योग-कारोबार चल रहे हैं, और कमा रहे हैं। हमारा ख्याल है कि किसी की संपत्ति छीने बिना संपन्नता के एक दर्जे के ऊपर अगर ऐसा टैक्स लगाकर देश को मजबूत किया जा सकता है, तो उस पर बात तो होनी चाहिए। यह वह देश है जहां पर 25 करोड़ लोगों को बिना भुगतान के अनाज मिलने पर ही वे भुखमरी से बचते हैं। ऐसे में देश के सबसे संपन्न दो-चार फीसदी लोगों की संपत्ति को अगली पीढ़ी तक जाते हुए कुछ कम कर दिया जाए, तो उससे क्या अमीरों का हौसला एकदम ही पस्त हो जाएगा? इस बात को सैम पित्रोदा के नाम से जोडक़र न देखें, इसे डोनल्ड ट्रम्प के नाम से जोडक़र देख लें, जो कि अभी पिछली बार तक अमरीका के राष्ट्रपति थे, अभी फिर राष्ट्रपति बनने की दौड़ में हैं, और नरेन्द्र मोदी के दोस्त भी हैं।
छत्तीसगढ़ के धमतरी में कल एक शादी समारोह में म्यूजिक डीजे पर नाचने के दौरान झगड़ा हुआ, और दो नौजवानों की चाकू के वार से मौत हो गई, और एक गंभीर जख्मी है। डीजे के शोरगुल को लेकर और उसके साथ जुड़ी हुई बाकी तमाम किस्म की अराजकता पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पिछले एक-दो बरस से बड़े कड़े तेवर दिखा रहा है, और राज्य के मुख्य सचिव से एक से अधिक बार इस पर निजी हलफनामा ले चुका है कि लोगों का जीना हराम करने वाला यह शोरगुल कैसे थमेगा? अदालत ने कई किस्म की सख्ती दिखाई है और यह भी कहा है कि इस राज्य के अफसर संगीत के नाम पर इस शोरगुल को रोकना भी नहीं चाहते। अदालत का सरकारी अफसरों के साथ संघर्ष देखें, तो लगता है कि अदालत का कोई बस चल नहीं रहा है, जिस तरह घर में किसी बुजुर्ग की कही हुई बात को बाकी लोग अनसुना करते हों, उसी तरह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बोले चले जा रहा है, और अफसरों पर उसका धेले का असर नहीं हो रहा है। शादियों के इस मौसम में पूरे प्रदेश में जगह-जगह न सिर्फ लाउडस्पीकरों को लेकर हाईकोर्ट के हुक्म पैरोंतले रौंदे जा रहे हैं, बल्कि शहर की जिंदगी भी ट्रैफिक जाम में बर्बाद की जा रही है, और शायद ही किसी जगह पुलिस और प्रशासन ने शादी के नाम पर ऐसी अराजकता रोकने की कोशिश भी की हो।
अब सवाल यह उठता है कि अगर बुनियादी कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस और प्रशासन के पीछे हाईकोर्ट के जज लाठी लेकर लगे रहें, तो यह अधिक बड़ा अपमान किसका माना जाए? जजों का, या कि अफसरों का? क्या आईएएस-आईपीएस जैसी बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय सेवाओं से आने वाले अफसरों को इतने में तसल्ली हो जाती है कि वे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और हाईकोर्ट जजों के बंगलों को लाउडस्पीकरों की पहुंच से परे रख लेते हैं, अपने घरों में चैन से सो जाते हैं, और बाकी पूरे प्रदेश को अराजक गुंडों के रहमोकरम पर छोड़ देते हैं? हमने इसी प्रदेश में, राज्य बनने के दशकों पहले यह देखा हुआ है कि एक डिप्टी कलेक्टर, और एक डीएसपी रैंक के अफसर पूरे शहर के अवैध कब्जे हटवा देते थे, ट्रैफिक सुधार देते थे, डिप्टी कलेक्टर म्युनिसिपल कमिश्नर अवैध कब्जे तोड़वा देता था। आज छोटी-छोटी कुर्सियों पर आईएएस-आईपीएस बैठे हुए हैं, एक-एक जिले के पांच जिले बन गए हैं, और जहां दो बड़े अफसर रहते थे, वहां अब दर्जन भर से अधिक अफसर अखिल भारतीय सेवाओं के हैं, लेकिन उनका असर खत्म हो गया है। या तो राजनीति इतनी हावी हो गई है कि उसने अफसरों के हाथ बांध दिए हैं, या फिर अफसर ही अपनी महत्व मानी जाने वाली कुर्सियों पर खुद को महफूज बनाकर चलते हैं, और किसी को भी नाराज करना नहीं चाहते। नतीजा यह है कि जनता पीढ़ी-दर-पीढ़ी अराजक होते चल रही है, और उसके मन में नियम-कानून के लिए परले दर्जे की हिकारत मजबूत पैर जमाते जा रही है। अफसरों के दर्जन भर बार चेतावनी जारी करने के बाद भी सडक़ किनारे धंधा करने वाले छोटे-छोटे लाउडस्पीकरों वाले लोग भी जब उनकी बात नहीं सुनते, हाईकोर्ट की चेतावनियों की परवाह नहीं करते, तो यह जाहिर है कि जनता के मन में नियम-कानून का सम्मान पूरी तरह खत्म हो गया है।
यह नौबत देश में ऐसे नियम-कानून होने के मुकाबले अधिक खतरनाक है। अगर नियम-कानून ही न रहे, तो कम से कम जनता उनको तोडऩे की कुसूरवार नहीं रहती है, लेकिन जब छोटी-छोटी बातों को लेकर बड़े-बड़े नियम अदालती फैसलों से लागू होते हैं, और कानून देश को एक अधिक सभ्य जगह बनाने की कोशिश करता है, उस वक्त भी अगर बड़े-बड़े अफसर अपनी छोटी-छोटी रह गई रियासतों में कड़े रूख वाले अदालती फैसलों को भी लागू नहीं करवा पाते, तो यह कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो जाने का एक बड़ा सुबूत है। जब जनता कुछ नियम तोडऩे के लिए आजाद रहती है, तो फिर वह चाकू-छुरी लेकर चलने, गाडिय़ों के साइलेंसर फाडक़र चलने को भी अपना हक मान लेती है, और छत्तीसगढ़ के जनजीवन में यह नौबत सिर चढक़र बोल रही है। नमूने के लिए हर जिले की पुलिस ऐसे कुछ लोगों को पकड़ लेती है, लेकिन हकीकत यह है कि उसका अनुपात असल बदअमनी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। और दिक्कत यह है कि कानून मानने वाले, शरीफ लोग अधिक तकलीफ पाते हैं क्योंकि उनके मन में यह रंज भी रहता है कि वे हर कानून का पालन करते हैं, लेकिन कानून तोडऩे वालों से तकलीफ झेलते हैं, और सरकार उनकी मदद के लिए मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वह तो हाईकोर्ट के सख्त फैसलों को लागू करने के लिए भी मौजूद नहीं है।
हम अगर फिर से तरह-तरह के लाउडस्पीकरों के हल्ले की बात पर लौटें, तो शादियों के इस मौसम में चारों तरफ लोगों ने मनमानी की है, और कई किलोमीटर तक जाने वाले शोरगुल को भी पुलिस-प्रशासन ने नहीं रोका है। अब तो दूर-दूर तक तरह-तरह की रौशनी फेंकने वाले लैम्प बाजारों में खुले बिक रहे हैं, और न इनके इस्तेमाल पर कोई रोक लगाई जा रही, न ही इनकी बिक्री पर। बहुत जाहिर तौर पर ऐसी लाईटें एक गंभीर प्रदूषण पैदा करती हैं, और ट्रैफिक के लिए खतरा खड़ा करती हैं, लेकिन जब तक ये सत्ता पर काबिज कुछ बड़े लोगों के लिए परेशानी का सबब नहीं बनेंगी, तब तक इनको रोकने की जहमत कोई नहीं उठाएंगे। आज तो हालत यह है कि बाजारों में दुकानदार इतने किस्म के लैम्प बाहर लगाकर रखते हैं कि वे चौराहों की ट्रैफिक लाईट का धोखा भी देते हैं, फिर भी इनको रोकने की कोई कोशिश नहीं होती है।
ये तमाम बातें नियमों को इस तरह तोडऩा नहीं है कि कहीं कोई एक ट्रक प्रतिबंधित समय में कहीं घुस गई हो। यह तो नियम-कानून तोडऩे का पूरा का पूरा हाईवे चल रहा है, और कोई रोकथाम नहीं है। अब तो हाईकोर्ट पर भी दया आती है कि उसे कितनी बार कितने लोग जाकर बताएं कि उसकी अवमानना हो रही है। अदालत भी शायद यह समझ चुकी है कि उसके बस में बस अपनी अवमानना कराना ही रह गया है, और वह दूसरे लोगों का आ-आकर यह याद दिलाना नहीं चाहती है। वैसे भी हम अखबार का जिम्मा सार्वजनिक मुद्दों पर खुलकर लिखने जितना मानते हैं, और किसी जर्नलिस्ट के एक्टिविस्ट की तरह अदालत जाने के खिलाफ हैं, इसलिए हम खुद होकर तो अदालत के सामने इस बात को नहीं रखते, लेकिन जिन लोगों ने इन मुद्दों पर जनहित याचिकाएं लगाई थीं, उन्हें जरूर लाउडस्पीकरों और उससे जुड़ी कल की हत्याओं के बारे में अदालत को बताना चाहिए, और यह भी बताना चाहिए कि हाईकोर्ट के जांच कमिश्नर नियुक्त हुए बिना प्रदेश में जनता को जहन्नुम की जिंदगी से कोई नहीं बचा सकते। छोटे-छोटे बच्चों, बीमार लोगों, बूढ़ों, दूसरे प्राणियों, और रात-दिन की शिफ्ट में काम करते हुए आराम की जरूरत वालों की जिंदगी नर्क बनी हुई है, और कानून तोडऩे वालों के लिए यह प्रदेश स्वर्ग बना हुआ है। हाईकोर्ट जजों के रिहायशी इलाके, और अदालत का इलाका लाउडस्पीकरों से मुक्त रखा गया होगा, लेकिन अदालत को प्रदेश भर से इसकी रिपोर्ट जरूर बुलवाना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
छत्तीसगढ़ पुलिस का एक नया कारनामा हाईकोर्ट की मेहरबानी से उजागर हुआ है। अपने पड़ोसी द्वारा सडक़ पर अपना अहाता बनाने की शिकायत करने के लिए एक रिटायर्ड शिक्षिका और उनकी इंजीनियर बेटी पुलिस थाने पहुंचे थे, पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया, शाम को अदालत में पेश किया, और कानूनी मदद नहीं लेने दी, और बॉंड भरकर जमानत पर रिहा होने का मौका भी नहीं दिया। पुलिस ने इस रिटायर्ड शिक्षिका को थाने में थप्पड़ भी मारे। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने इसे स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना है, और इन्हें तीन लाख रूपए मुआवजा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। जमानत पर रिहाई के पहले मां-बेटी तीस घंटे जेल में रखे गए थे, और उसका यह मुआवजा अब सरकार की जेब से जाने वाला है। यह तो शहर का मामला है, और शिकायकर्ता हाईकोर्ट तक जाने की ताकत रखते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के गांव-देहात और जंगलों में बसे हुए लोग इतने कमजोर रहते हैं कि उनके लिए थाने तक जाना भी मुश्किल रहता है, और अगर किसी कानूनी मदद से वे अदालत तक पहुंच भी पाते हैं, तो कई बार तो उनके मामले खारिज ही हो जाते हैं। हम हाईकोर्ट का यह ताजा फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं कि इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस को कुछ सबक मिलने के आसार बन सकते हैं। हमारा यह भी ख्याल है कि जो पुलिसवाले इस मामले में जिम्मेदार पाए जाते हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए, और पुलिस को यह अक्ल भी मिलनी चाहिए कि शिकायतकर्ता महिलाओं की ऐसी गिरफ्तारी जैसी अराजकता इस प्रदेश में अभी नहीं है। अभी ऐसी कोई इमरजेंसी लगी हुई नहीं है कि पुलिस इतनी मनमानी कर सके, और न ही ये शिकायतकर्ता मां-बेटी पेशेवर मुजरिम हैं जिन्हें कि जेल भेजने की नीयत से इस तरह का इंतजाम किया गया। एक अवैध कब्जा और अवैध निर्माण करने वाले की हिमायती बनकर अगर पुलिस ने शिकायतकर्ता को चुप करवाने की सुपारी उठाई थी, तो इसकी सजा भी उन सबको मिलनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार थे। हम हाईकोर्ट के इस कड़े फैसले को किसी संदेह के लायक नहीं मान रहे हैं, और यह फैसला न सिर्फ पुलिस बल्कि दूसरे सरकारी विभागों के लिए भी एक मिसाल बननी चाहिए। हमें सरकारी नियमों की बारीकियां नहीं मालूम हैं लेकिन अगर इन पुलिसवालों की बददिमागी से सरकार को जुर्माना देना है, तो उसकी वसूली भी इन लोगों से होनी चाहिए।
आज हिन्दुस्तान के बहुत से राज्यों में गलत काम करने वालों का ही राज चलता है। जैसा कि इस मामले में हुआ है, अवैध कब्जा और अवैध निर्माण करने वाले को पुलिस से इस दर्जे की गैरकानूनी मदद भी मिली है। अवैध कामों में ही कमाई मोटी रहती है, और ऐसे माफिया का भागीदार बनने के लिए पुलिस और दूसरे सरकारी विभाग सभी उतावले बने रहते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही एक सबसे महंगी रिहायशी कॉलोनी ऐसी है जिसके मालिक ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोटवार की जमीन अपने घेरे में लेकर कॉलोनी का नक्शा भी पास करा लिया है, और शहर की सबसे महंगे प्लाट भी वहां बेच दिए हैं। जिस-जिस विभाग में इसकी शिकायत हुई, वहां के अफसरों ने भी इस कॉलोनी में जमीनें ले ली, मंत्रियों और नेताओं ने पहले से बहती गंगा में हाथ धो लिए थे। नतीजा यह है कि हर तरह के अवैध काम करने के बाद भी, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ऐसी कॉलोनी पनप रही है, और उपकृत आला अफसरों की मेहरबानी से वह अपनी दूसरी कॉलोनियों में भी तरह-तरह के अवैध काम कर रही है। यह किसी एक कारोबारी का हाल नहीं है, और न ही किसी एक कारोबार का, जिनका सरकारी नियमों से कोई भी वास्ता पड़ता है, उन सबके कामों के अवैध दर्जे का यही हाल है। इसलिए ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ जब कोई शिकायत आती है, तो शिकायतकर्ता को निपटाने के लिए इनकी कॉलोनियों के प्लाट और मकान मालिक बने नेता और अफसर टूट पड़ते हैं। सरकार और कारोबार का यह माफियाई-रिश्ता इतना मजबूत है कि फेविकोल को इसी को अपने इश्तहार में इस्तेमाल करना चाहिए।
फिर पुलिस की बात पर लौटें, तो पुलिस की कोई भी कार्रवाई यह तौल लेने के साथ शुरू होती है कि जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उससे कमाई की कोई उम्मीद है, या नहीं, उसकी कोई राजनीतिक पहुंच है या नहीं, और अगर राजनीति पहुंच है तो वह सत्तारूढ़ पार्टी में है, या विपक्ष में। जिस तरह हंसों के बारे में कहा जाता है कि वे मोती चुन लेते हैं, उसी तरह हिन्दुस्तानी पुलिस बिना राजनीतिक खतरे वाले मामलों को चुन लेती है, और फिर जिससे कमाई नहीं होने वाली है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है। जिस जांच एजेंसी को बिना पूर्वाग्रह के सच को परखना चाहिए, उसके काम की शुरूआत ही फायदे के एक फैसले पर पहुंच जाने से होती है, और फिर उस फैसले के मुताबिक सुबूत जुटाने का सिलसिला चलता है। यह बात बस्तर जैसे इलाके में, नक्सल प्रभावित जंगल और गांव में आदिवासियों के खिलाफ अक्सर ही इस्तेमाल होती है, और उनके तो मामले भी हाईकोर्ट में जाकर दर्जनों के हिसाब से थोक में खारिज हो जाते हैं। वह एक अलग और लंबा सिलसिला है, इसलिए उसकी चर्चा यहां मुमकिन नहीं है। लेकिन बिलासपुर में एक मां-बेटी को जिस तरह उनकी शिकायत शांत करवाने के लिए, और एक अवैध कब्जा-निर्माण करने वाले का साथ देने के लिए पुलिस ने जिस तरह मां-बेटी को जेल भेजा, वह शहरी छत्तीसगढ़ के लिए भी थोड़ी सी अटपटी बात है, और प्रदेश की भाजपा सरकार के राजनीतिक, और दूसरे संगठनों के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी सरकार की पुलिस अगर इस तरह मुजरिम-दर्जे का काम कर रही है, तो उसे सुधारा जाना चाहिए। ऐसा न होने पर पुलिस सत्ता को कितने गहरे गड्ढे में गिरा सकती है, यह राज्य में पिछले पांच बरस में अच्छी तरह साबित हो चुका है। प्रदेश की भाजपा सरकार को ऐसे अफसरों से सावधान रहना चाहिए जो कि सत्तारूढ़ नेताओं को तुरंत तो खुश करके रखें, लेकिन पांचवें बरस तक इतने गहरे गड्ढे में डाल दें कि संघ के तमाम लोग मिलकर भी भाजपा को नुकसान से न निकाल सकें। हम इस चर्चा को किसी के राजनीतिक नफे-नुकसान के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बेकसूर जनता के लोकतांत्रिक हक के लिए यह बात कर रहे हैं, लेकिन इस मिसाल को देना जरूरी इसलिए है कि सत्तारूढ़ नेता इस एक खतरे को कुछ जल्दी समझ पाते हैं।
ब्रिटेन की खबर है कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दूसरे देशों से आकर ब्रिटेन में काम या कारोबार करने वाले लोगों को उनके अपने देश की कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 15 साल से घटाकर 4 साल कर दिया है। उल्लेखनीय है कि ऋषि सुनक की भारतवंशी पत्नी की भारत से होने वाली कमाई पर ब्रिटेन में टैक्स न देने को लेकर पिछले बरस यह परिवार बड़े अप्रिय विवादों में घिरा था, और उसके तुरंत बाद टैक्स कानूनों को चुनौती दिए बिना अक्षता मूर्ति ने नियमों से अधिक टैक्स देने की घोषणा की थी। वे भारत में अपने पिता, नारायण मूर्ति से मिली जायदाद, और अपने खुद के काम की कमाई पर ब्रिटेन में बहुत कम टैक्स दे रही थीं, या टैक्स नहीं दे रही थीं। अब तक वहां के कानून में ऐसा ही प्रावधान था, लेकिन अब इस नए कानून के आने से ब्रिटिश पीएम परिवार पर लगी यह तोहमत भी हट सकेगी। वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहले वित्तमंत्री थे, और वित्तमंत्री रहते हुए उनकी पत्नी टैक्स छूट का जिस तरह फायदा उठा रही थी, उसे ब्रिटिश खजाने के साथ नाइंसाफी बताया गया था। उस शर्मिंदगी से उबरने के लिए ऐसा लगता है कि ऋषि सुनक ने इस नए कानून को बनाने में अधिक दिलचस्पी ली है। अभी तक भारत से जाकर ब्रिटेन में काम या कारोबार करने वाले लोगों को वहां अपनी भारतीय आय पर 15 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ता था, और सिर्फ ब्रिटिश कमाई पर टैक्स लगता था। एक खबर बताती है कि पिछले पांच बरस में 83 हजार से अधिक भारतीयों ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी, यह एक ऐसी योजना के तहत हुआ था जिसमें अतिसंपन्न लोगों को ब्रिटेन में मोटे पूंजीनिवेश के एवज में तुरंत ही वहां नागरिकता मिल जाती थी। अब इन नए टैक्स नियमों की वजह से ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तानियों में ‘अंग्रेज’ बनने का आकर्षण कुछ कम होगा।
ऋषि सुनक की इस पहल को इस संदर्भ में भी देखना चाहिए कि भारत से किसी तरह का रिश्ता रखने वाले दूसरे देशों के बड़े कारोबारियों या सत्तारूढ़ नेताओं को लेकर भारत में जो एक बावलापन अक्सर ही सतह पर दिखता है, वह किसी काम का नहीं रहता, उसकी कोई जमीन नहीं रहती। भारतीय मूल की मां वाली अमरीकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को लेकर भारत में यह सनसनी फैली थी कि मानो अब अमरीकी रूख भारत के लिए बदल जाएगा। सच तो यह है कि दुनिया के किसी भी देश से दूसरे देश में पहुंचने वाले लोग जहां रहते हैं, काम करते हैं, राजनीति में आकर सत्ता तक पहुंचते हैं, वे उसी देश के होकर रह जाते हैं। सोनिया गांधी इटली से भारत आकर यहां राजनीति की ऊंचाईयों पर पहुंचीं, लेकिन क्या यूपीए सरकार के दस बरसों में वे इटली के साथ किसी तरह की रियायत कर पाईं? ऐसी ही नौबत कमला हैरिस या ऋषि सुनक की रहती है, या कनाडा में मंत्री बनने वाले बहुत से भारतवंशियों की भी रहती है। उनकी जड़ें, उनके डीएनए जरूर भारत से जुड़े रहते हैं, लेकिन वे अपने वर्तमान देश के ही रहते हैं, वहीं के लिए वफादार रहते हैं। सच तो यह है कि जब अपने जन्म या पुरखों के देश के साथ किसी रियायत का मौका आता है तो ऐसे नेता इसलिए हिचक जाते हैं कि उनके जरा भी नर्म बर्ताव उन पर यह तोहमत लगवा सकता है कि वे अपने पुरखों की जमीन के प्रति पूर्वाग्रह दिखा रहे हैं। इसलिए ईमानदार दिखने के लिए उन्हें कड़ाई कुछ अधिक बरतनी पड़ती है, जैसी कि आज ऋषि सुनक के फैसले से दिखाई पड़ रही है।
आज के वक्त जब दुनिया भर के लोग दूसरे देशों में जाकर वहां बहुत कुछ हासिल करते हैं, उस वक्त उनकी कामयाबी के बाद यह सोच लेना कि उनकी पहली वफादारी अपने जन्म के देश से होगी, बहुत बड़ी खुशफहमी है, और बेईमानी की उम्मीद है। हर किसी को अपने मौजूदा काम, मौजूदा देश, और मौजूदा विचारधारा के प्रति वफादार रहना चाहिए। अपने डीएनए से वफादारी किसी वैज्ञानिक शोध के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं हो सकती। आज अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हर किसी को अपने वर्तमान के साथ ईमानदार रहना चाहिए, और तमाम लोग ऐसे रहते भी हैं, तभी वे कामयाब हो पाते हैं। हिन्दुस्तान के लोगों की एक दिक्कत यह भी है कि वे दुनिया भर में बसे हुए भारतवंशियों की कामयाबी को भारत की कामयाबी मान बैठते हैं। ये सारे लोग जो भारत से जाकर अपनी पीढ़ी में या अगली पीढ़ी में कामयाब हुए हैं, वे उन देशों के माहौल की वजह से, और अपनी मेहनत की वजह से कामयाब हुए हैं। हिन्दुस्तान में अगर सफलता की इतनी ही संभावनाएं रहतीं, तो सुंदर पिचई अमरीका जाकर गूगल के मुखिया बनने के बजाय भारत में किसी कंपनी के मुखिया बने होते, या उन्होंने यहां वैसी कोई कंपनी खड़ी कर दी होती। लेकिन चुनावी बॉंड का यह ताजा मामला बताता है कि भारत में कंपनियों को किस तरह के माहौल में काम करना पड़ता है, और उनके आगे बढऩे की संभावनाएं किस तरह कदम-कदम पर घटती जाती हैं। भारत को तो दूसरे देशों में सफल भारतवंशियों को देखकर यह आत्ममंथन करना चाहिए कि उसकी अपनी जमीन पर कारोबार या राजनीति में इतनी खरपतवार क्यों है कि यहां प्रतिभा की फसल ठीक से फल-फूल नहीं पाती। अमरीका या ब्रिटेन जैसे देश में कारोबारी अपनी राजनीतिक विचारधारा को लेकर भी खुलकर सक्रिय रहते हैं, और उन्हें उसका कोई नुकसान भी शायद नहीं उठाना पड़ता। भारत को हर दिन कुछ घंटे आईने के सामने बैठकर यह देखना चाहिए कि इतनी प्रतिभाशाली लोग देश के बाहर जाकर ही प्रतिभा को इस तरह साबित क्यों कर पाते हैं? साथ-साथ दूसरे देशों में भारतवंशियों की कामयाबी का जश्न हिन्दुस्तान की कामयाबी की तरह मनाना बंद भी करना चाहिए, ऐसे झूठे गौरव, और ऐसी असली खुशी के बीच कोई तालमेल नहीं रहता।
अमरीका के एक प्रमुख विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक ताजा रिसर्च बताती है कि किस तरह किसी की तारीफ करने पर उन पर एक सकारात्मक असर पड़ता है, और ऐसा ही असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो दूसरों की अच्छे कामों की तारीफ करते हैं। इस विश्वविद्यालय ने मनोविज्ञान विभाग की एक रिसर्च से पता लगता है कि तारीफ दोनों तरफ के लोगों का भला करती है। यह शोध करने वाली एक प्रोफेसर का कहना है कि तारीफ लोगों का दिन बना देती है, और करने वाले को कोई लागत भी नहीं आती है। कुछ दूसरे विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं का भी कुछ ऐसा ही सोचना है जिन्होंने तारीफ के मनोविज्ञान पर गंभीर काम किया है। उनका कहना है कि जिनके काम को दूसरे लोग भी अच्छा समझते हैं, उन्हें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। इससे लोगों के मन की यह जिज्ञासा भी शांत होती है जिससे कि वे यह जानना चाहते हैं कि और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हिन्दी जुबान में एक बात कई बार कही जाती है- सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग?
यह सचमुच ही लोगों के लिए परेशानी का एक सबब होता है कि उनके किसी काम या उनकी किसी बात पर लोग क्या कहेंगे? जब लोग किसी बात की तारीफ करते हैं, तो यह एक कामयाबी रहती है, और बेहतर करने की प्रेरणा भी इससे मिलती है। घर पर अगर खाना बनाने के लिए तनख्वाह पर किसी को रखा गया है, तो उनकी तारीफ करना जरूरी नहीं रहता, लेकिन कभी उनके पकाए और खिलाए हुए की तारीफ करके देखें तो समझ आएगा कि अगली बार वे ऐसी तारीफ पाने के लिए और क्या-क्या मेहनत करेंगे। यह भी जरूरी नहीं रहता कि लोग दूर के लोगों की, और महज औपचारिकता के लिए तारीफ करें। हम पहले भी कई बार इस बात को लिख चुके हैं कि लोगों को किसी भी व्यक्ति से उनकी दिन की पहली बातचीत नकारात्मक नहीं करना चाहिए। किसी बात के लिए आलोचना भी करनी हो, तो भी पहले तारीफ के लायक कोई बात ढूंढकर चाहे मामूली ही क्यों नहीं, तारीफ करनी चाहिए, और फिर बाद में आलोचना के लायक बात छेडऩी चाहिए। अगर पहले तारीफ की बात कर ली जाए, तो लोग आलोचना को भी बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर पाते हैं।
तारीफ कितनी मायने रखती है, यह उन लोगों से बेहतर कोई नहीं जानते जिनकी जिंदगी में कोई अक्सर ही तारीफ करने वाले थे, और किसी वजह से अब नहीं रह गए। उनकी जिंदगी एकाएक वीरान हो जाती है, और जिंदगी से तारीफ एकाएक गायब हो जाने से, उनके काम पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। इसलिए समझदारी इसमें है कि जिन लोगों के मन में आपके काम के लिए, आपके लिए सचमुच ही तारीफ है, उन लोगों की कद्र की जाए, उन्हें पास रखा जाए, उनके पास रहा जाए। ऐसा भी नहीं कि इस बात को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक या शोधकर्ता ही लगेंगे। आम लोग भी मामूली समझबूझ से इस बात को समझ सकते हैं कि इर्द-गिर्द के लोगों के अच्छे कामकाज के लिए उनकी तारीफ करके किस तरह उनसे बेहतर काम करवाया जा सकता है। दरअसल अधिकतर काम ऐसा रहता है जिसमें आम प्रदर्शन और खास प्रदर्शन दोनों ही एक ही किस्म के लोगों से हासिल किया जा सकता है। अगर एक ही व्यक्ति बेदिली से, अनमने ढंग से कोई काम करे, तो वह बहुत आम दर्जे का हो जाता है, और अगर उसी काम को करते हुए उसके दिमाग में यह रहे कि इसकी वजह से उसे तारीफ भी मिल सकती है, तो उसकी जरा सी अतिरिक्त दिलचस्पी उस आम काम को खास काम में तब्दील भी कर सकती है। जब आप आसपास के किसी के बेहतर काम की तारीफ करते हैं, तो भविष्य में भी उनसे वैसे ही बेहतर प्रदर्शन की एक किस्म से गारंटी भी कर लेते हैं।
हमने पहले भी अलग-अलग कई जगहों पर इस बात को लिखा है कि लोगों को ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए जिनके दिल-दिमाग में दूसरों के लिए सिर्फ नापसंदगी और आलोचना भरी हुई है, जिन्हें आसपास कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हर कोई बुरे लगते हैं। ऐसे लोगों के इर्द-गिर्द बने रहने से आपको भी पूरी दुनिया बुरी लगने लगती है, और किसी के अच्छे काम भी कभी तारीफ के लायक नहीं लगते हैं। जिंदगी और दुनिया तो वही रहते हैं, सिर्फ आप अपने रूख और नजरिए की वजह से इर्द-गिर्द की हकीकत की इतनी बुरी तस्वीर मन में बना लेते हैं कि पूरे वक्त आपका का बर्ताव एक निंदक का होकर रह जाता है। कबीर ने भी जब यह कहा था कि निंदक नियरे राखिए, तो यह उन लोगों के लिए कहा था जो अपने आसपास आलोचकों को बर्दाश्त करते हैं, और वे लोग अपनी गलतियां तुरंत जान जाते हैं। लेकिन कबीर ने यह बात निंदकों के भले के लिए नहीं कही थी जिन्हें पूरे वक्त किसी न किसी की निंदा सूझती है। कई लोगों का तो हाल यह रहता है कि जब तक दूसरों की निंदा न कर लें, तब तक खाना हजम नहीं होता, यह लगते रहता है कि आज का दिन बेकार गुजर रहा है कि काम की कोई बात ही नहीं हो पाई।
कुल मिलाकर बात यह है कि जिंदगी में अगर जायज जरूरत रहने पर लोगों की आलोचना करनी है, तो वह एक सकारात्मक सुझाव की तरह अधिक रहनी चाहिए, न कि निंदा और भर्त्सना की तरह। और आसपास जाने-पहचाने, या अनजाने, जैसे भी लोग हों, उनकी कोई बात अगर अच्छी लगे, उनका कोई काम अच्छा लगे, तो उनकी तारीफ का कोई मौका नहीं छोडऩा चाहिए। हमने आज की इस चर्चा की शुरूआत तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध के नतीजे से की है कि किस तरह तारीफ उसके दोनों सिरे के लोगों का भला करती है, लेकिन आगे के निष्कर्ष हमारे खुद के हैं कि लोगों को कम से कम कुछ ऐसे लोग इर्द-गिर्द जरूर रखना चाहिए जिनके मन में उनके लिए, उनके काम के लिए तारीफ है, क्योंकि ऐसे लोग जिंदगी से एकदम से चले जाने पर जिंदगी से एक प्रेरणा ही चली जाती है, और फिर उसकी जगह वैसी कोई दूसरी सकारात्मक चीज नहीं आ पाती है। ऐसे लोगों से बचकर रहें जिनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ढूंढ-ढूंढकर लोगों की आलोचना करने में गुजर जाता है, तमाम वक्त ऐसी नकारात्मक बातों को सुनने के बाद आपकी अपनी जिंदगी से भी उत्साह जाने लगता है।