संपादकीय
4 जून की सुबह से ही देश में शुरू हुई उथल-पुथल दो दिन के भीतर ही काफी हद तक थम चुकी है, और अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनने, और मोदी के प्रधानमंत्री बनने में कोई शक बाकी नहीं है। एक दिन की अटकलबाजी बड़ी तेजी से बारिश की बूंदों से बैठ गई बूंद की तरह थम चुकी है, और नीतीश कुमार और चन्द्राबाबू नायडू को लेकर शुरू हुई अटकलें एक दिन के भीतर ही शांत हो चुकी हैं। जहां तक भाजपा और एनडीए के सदमे से उबरने का सवाल है, तो आंकड़ों की हकीकत देखकर वे भी उबर रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो नरेन्द्र मोदी ही बनेंगे, और कहने के लिए यह तो है ही कि भाजपा की अपनी सीटें बाकी तमाम विपक्ष की मिली हुई सीटों से भी अधिक हैं। निराशा के बीच भी नरेन्द्र मोदी ने भाजपा कार्यालय से अपने भाषण में तीसरी बार सत्ता में लौटने की ऐतिहासिक कामयाबी को गिनाया, और ओडिशा राज्य को विधानसभा, और लोकसभा दोनों में जीत लेने का शुक्रिया अदा करने के अंदाज में उन्होंने जय-जगन्नाथ से बात शुरू की, ओडिशा की चर्चा की, और भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद की चर्चा की। इस मौके पर राम मंदिर की चर्चा अब प्रासंगिक नहीं रह गई थी क्योंकि रामलला अपनी अयोध्या में ही भाजपा को नहीं जिता पाए, और अयोध्या वाले उत्तरप्रदेश में भाजपा का बड़ा नुकसान देखने मिला है, जबकि राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा से पूरे देश में बड़े फायदे की उम्मीद की जा रही थी। पांच बरस के भीतर बीजेपी की लोकसभा सीटें 303 से गिरकर 240 पर आ गई हैं, और उत्तर भारत के चार राज्यों, यूपी, राजस्थान, बिहार, और हरियाणा में उसकी पिछले चुनाव की सीटें आधी रह गई हैं। ऐसे में जब ओडिशा ने भाजपा को इस बार 21 में से 20 लोकसभा सीटें दी हैं, और राज्य में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को हटाकर भाजपा को आधे से अधिक विधानसभा सीटें दी हैं, और भाजपा की सरकार बनाई हैं, तो मोदी का भगवान जगन्नाथ का आभार मानना स्वाभाविक ही था।
अब इन आंकड़ों से परे की बात देखें, तो मोदी के पिछले दो कार्यकाल से उनका यह कार्यकाल अलग रहने वाला है। दरअसल उनका यह कार्यकाल उनके सारे सत्ताकाल से अलग रहने वाला है। गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने राज्य सरकार के साथ-साथ भाजपा और संघ परिवार के संगठनों पर एकतरफा राज किया था। वहां जो कुछ थे, वे ही थे। इसके साथ ही जब वे पहली बार दिल्ली पहुंचे, तब अपनी एनडीए सरकार के दोनों कार्यकाल में जो कुछ थे, वे ही थे। वे मंत्रिमंडल में पहुंचकर अपने उन राष्ट्रव्यापी और ऐतिहासिक फैसलों की घोषणा करते थे जो कि मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के पहले लागू होने वाले थे। वे एक राजा के अंदाज में अपने दरबार को अपने फैसले बताते थे, लेकिन लोगों का यह अंदाज है कि अब इस कार्यकाल में नौबत बदली रहेगी। तेलुगु देशम और जेडीयू जैसी पार्टियां मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के एवज में आन्ध्र और बिहार के लिए विशेष दर्जा भी मांग सकती हैं, लोकसभा अध्यक्ष और ऐसे दूसरे कई पद मांग सकती हैं, और मंत्रालयों के बंटवारे में भी वे अपनी कई शर्तें रख सकती हैं। इसके साथ ही एक बात यह भी है कि मोदी को पहली बार गठबंधन-धर्म का सम्मान करने की नौबत आ सकती है, या आ चुकी है। इसके तहत हो सकता है कि वे मुस्लिमों के प्रति पिछले कुछ महीनों के अपने ताजा रूख को उसी आक्रामकता के साथ जारी न रख सकें क्योंकि सहयोगी दलों में कई ऐसे हैं जिन्हें मुस्लिमों से इस दर्जे का परहेज नहीं है। गंभीर समाचार माध्यमों की यह व्याख्या है कि मोदी अपनी सरकार के अकेले निर्णायक की तरह जिस अंदाज में काम करने के आदी हैं, उनके लिए यह बड़ा अटपटा होगा कि उन्हें औरों की बात भी सुननी होगी। यह नौबत उनके लिए अटपटी हो सकती है, लेकिन हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के लिए यह बहुत बड़ा समझौता होगा, ऐसा मानना भी ठीक नहीं होगा।
एनडीए गठबंधन के भीतर भाजपा का दबदबा कुछ कमजोर होना तय है, लेकिन भाजपा के भीतर मोदी और शाह का दबदबा कम होगा, ऐसा कोई आसार अभी दिखता नहीं है। ऐसा इसलिए भी है कि एनडीए के दूसरे ताकतवर सहयोगी दल अपने हक के लिए चाहे जितने अड़ें, भाजपा के भीतर के मामलों से उनका कुछ लेना-देना नहीं रहेगा, और भाजपा के भीतर मोदी और शाह की लीडरशिप को फिलहाल तो कोई चुनौती नहीं दिख रही है। इस मतगणना के पहले ही जिस तरह भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में बहुत ही असाधारण अंदाज में यह कहा था कि भाजपा अब बहुत ताकतवर पार्टी हो गई है, और उसे अब आरएसएस की उस तरह की जरूरत नहीं रह गई है। नड्डा ने मतगणना के दस दिन पहले के इंटरव्यू में कहा था कि भाजपा उस वक्त से बहुत आगे बढ़ गई है, और सक्षम हो गई है, और अपने को चलाकर अपना काम करने में अब उसे आरएसएस की जरूरत नहीं रह गई। उनसे पूछा गया था कि अटल बिहारी बाजपेयी के पीएम रहने के वक्त से अब तक भाजपा में आरएसएस की मौजूदी में क्या फर्क पड़ा है, तो उनका कहना था-शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आपको चलाती है।
चुनाव के बीच में तो भाजपाध्यक्ष के इस इंटरव्यू पर आरएसएस की कोई प्रतिक्रिया देखने में नहीं आई थी, लेकिन आज बदले हुए हालात में जब भाजपा अपने आपमें 2019 जितनी ताकतवर नहीं रह गई है, तो यह देखना है कि अब उसे संघ की जरूरत एक बार फिर लग रही है या नहीं। और यह भी ऐसे समय जब मोदी सरकार के भीतर अपने पिछले पीएम-सीएम के तमाम कार्यकाल जितनी आजादी और जितने अधिकार वाले शायद नहीं रह जाएंगे। यह वक्त हो सकता है कि मोदी को गठबंधन-धर्म निभाना भी सिखा सके, और हो सकता है कि यह संघ की जरूरत से उबर चुके भाजपाध्यक्ष नड्डा के लिए भी आत्ममंथन का हो।
सहयोगी दलों पर निर्भरता बहुत नुकसानदेह नहीं रहती है। हमारा देखा हुआ है कि यूपीए-1 सरकार वामपंथी दलों के बाहरी समर्थन से चल रही थी, और गठबंधन के साथियों के दबाव के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार में भ्रष्टाचार उतना नहीं हो पाया था जितना कि बाद में वामपंथियों की जरूरत खत्म हो जाने के बाद हुआ था। हो सकता है कि सहयोगी दलों पर आश्रित रहते हुए मोदी सरकार का एजेंडा देश में अधिक लोकतांत्रिक रहे, और यह सरकार पिछले दो कार्यकाल के मुकाबले बेहतर भी साबित हो। सहयोग का मोहताज होना कई बार अपने आपको सुधारने का मौका भी देता है। इसलिए हम इसे अगले पांच बरस में विपक्ष की बारी आ जाने जैसा नहीं मानते। हो सकता है कि इस बार के झटके से उबरते हुए मोदी और उनके सहयोगी इतने संभल जाएं कि अगले चुनाव में इससे बड़ा झटका न खाएं। खैर, एनडीए, या इंडिया-गठबंधन, इनमें से किसका भला-बुरा होता है, इससे अधिक फिक्र हमें देश के भले-बुरे की है। अब जब एनडीए पांच बरस के लिए जनता द्वारा चुन ली गई है, तो इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उसके बड़े भागीदारों पर भी मोदी से कम नहीं है। देखना है कि कौन अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी कितनी निभाते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
हिन्दुस्तान के आम चुनाव दुनिया के सबसे ही अनोखे होते हैं। शायद ही कोई ऐसा देश होता हो जिसमें इतनी क्षेत्रीय पार्टियां हों, कई राष्ट्रीय पार्टियां हों, कुछ क्षेत्रीय गठबंधन हों, कुछ राष्ट्रीय गठबंधन हों, और कई गठबंधन हर पांच बरस में कुछ-कुछ बदल भी जाते हों। वैसे भी यह देश अपने आपमें योरप की तरह का है जिसके अलग-अलग देश मिलकर कुछ खास एजेंडा के लिए यूरोपीय समुदाय जैसा एक संगठन बनाते हैं, और इन देशों में यूरोपीय संसद के सांसद चुनने के लिए अलग से चुनाव भी होते हैं। लेकिन ऐसे एक संगठन की तरह होने के साथ-साथ भारत तो एक देश है जहां पर एक राष्ट्रीय सरकार है, और ढाई दर्जन प्रादेशिक सरकारें हैं। दर्जन भर से अधिक भाषाएं हैं, और सैकड़ों बोलियां हैं। आधा दर्जन से अधिक धर्म हैं, और सैकड़ों जातियां हैं। दर्जनों राजनीतिक दल देश में मान्यता प्राप्त हैं, और कुछ दल एक से अधिक प्रदेशों में भी जाकर चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी ने दो प्रदेशों में सरकार बनाने में कामयाबी पाई है। वामपंथी दल पश्चिम बंगाल के अलावा केरल और त्रिपुरा में भी राज करते रहे।
भारत के इन ताजा चुनावी नतीजों को देखें तो यह देश हैरान करता है। धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की तमाम कोशिशों को नकारते हुए वोटरों ने जिस तरह चुनाव को एक धार्मिक जनमत संग्रह में बदलने से इंकार कर दिया, वह देखने लायक है। राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र जैसे विषयों के शोधकर्ताओं के लिए भारतीय राजनीति और चुनाव से अधिक दिलचस्प तो पूरी दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। राजनीतिक बेईमानी की जितनी विविधताएं भारत में देखने मिलती हैं, वे दुनिया के कुछ देशों में इक्का-दुक्का मामलों में यहां से अधिक हो सकती हैं, लेकिन ऐसी विविधताओं वाली नहीं हो सकतीं। फिर हर मौसम में जिस तरह कुछ पेड़ों के फूलों और पत्तों के रंग बदल जाते हैं, कोई फल से लद जाते हैं, उसी तरह हिन्दुस्तान की राजनीति में पार्टियों और गठबंधनों के ईमान बदल जाते हैं, उनके एजेंडा बदल जाते हैं। कहां तो कोई पार्टी कुनबापरस्ती के खिलाफ आसमान सिर पर उठाकर रखती है, और फिर परले दर्जे की कुनबापरस्त पार्टियों, और बलात्कारी कुनबों में से किसी को गोद में बिठाती हैं, तो किसी को सिर पर चढ़ाती हैं। नीति और सिद्धांत की बेईमानी की हिन्दुस्तान से बड़ी विविधता शायद किसी देश में न होती हो।
और फिर हिन्दुस्तान एक ऐसा देश भी है जो चुनाव आयोग की वोट डालने की मशीनों के ठीक काम कर लेने को लोकतंत्र की कामयाबी भी मान लेता है। हर पांच बरस में चुनावों की निरंतरता ही हिन्दुस्तानी आबादी के लिए लोकतंत्र है। हजारों बरसों में दुनिया की सभ्यता ने विकसित होते-होते हाल के कुछ सौ बरसों में लोकतंत्र के जिन बुुनियादी तत्वों को समझा था, और जिन पर चलना शुरू किया था, उन्हें पूरी तरह कुचलकर, चूर-चूर करके भी हिन्दुस्तानी यह मानते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र को एक ढांचे की तरह मान लिया गया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, और ऊंचाई सबसे अधिक होने से ही वह सबसे बड़ा लोकतंत्र हो गया हो। चाहे वह अभिव्यक्ति और आजादी के अलग-अलग बहुत से पैमानों पर जमीन पर औंधेमुंह गिरा हुआ देश ही क्यों न बन चुका हो, उसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, और इस पर गर्व किया जाता है। सच तो यह है कि हिन्दुस्तान लगातार चुनावों में भी जितने किस्म की बेईमान, अनैतिक, अलोकतांत्रिक, और भ्रष्ट बातों का इस्तेमाल करके सरकार चुनता है, उन्हें देखें तो यह लगेगा कि यह चुनना भी कुछ चुनना है? यह लोकतंत्र भी कोई लोकतंत्र है?
यह भी समझने की जरूरत है कि जनमत, जनादेश, समाज या नागरिकों को सामूहिक जनचेतना जैसे भारी-भरकम शब्दों का इस्तेमाल भारत के लोकतंत्र के गौरवगान के लिए अक्सर ही होता है, और उनकी हकीकत क्या है? जिस देश में किसी बलात्कारी के बेटे को उम्मीदवार बनाने की अकेली योग्यता यह हो कि वह दबंग बलात्कारी, या दंगाई अपने दम-खम से अपनी अगली पीढ़ी की राजनीतिक स्थापना कर सकता है, तो वहां पर ऐसे लोगों की जीत हो जाने को किस तरह की सामूहिक जनचेतना कहा जाएगा? जिस तरह देश के तमाम छोटे-बड़े गठबंधन वक्त-जरूरत कुनबापरस्ती को कोसते रहें, और अपनी जरूरत पर खालिस कुनबापरस्त पार्टियों को सिर पर बिठाते रहें, तो उसे क्या कहा जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राहुल गांधी को शहजादा कहते-कहते, कुनबापरस्ती और परिवारवाद को कोसते-कोसते अपना गला सुखा बैठते थे, लेकिन जमाने तक उनके एनडीए को खालिस कुनबापरस्त शिवसेना, और अकाली दल, तेलुगु देशम, और नेशनल कांफ्रेंस जैसी सभी पार्टियां सुहाती रहीं। अगर कांग्रेस भी एनडीए में शामिल हो जाती, तो उसे भी कुनबापरस्ती की तोहमत से छुटकारा मिल जाता। राजनीति शास्त्र के किसी शोधकर्ता के लिए भारतीय राजनीति में कुनबापरस्ती अपने आपमें कई पीएचडी का मुद्दा हो सकता है, और यह भारतीय लोकतंत्र का एक बड़ा छोटा सा तत्व रह गया है। इस देश की विविधता यह देखकर भी हैरान करती है कि किस तरह धर्म और जाति के आधार पर, किस तरह भडक़ाई गई सांप्रदायिकता के आधार पर, और किस तरह चुनाव और बाकी राजनीति में सफेद झूठ के इस्तेमाल से चुनाव जीते जाते हैं। इन्हें देखें तो लगता है कि जिस देश का चुनाव आयोग इनमें से किसी पर लगाम नहीं लगा सकता, वह अपने आपकी तारीफ किसी मशीन बेचने वाले की मशीन की गारंटी की तारीफ में पढ़े जाने वाले कसीदों की तरह करता है। हिन्दुस्तान एक अजीब देश इस मायने में भी है कि यहां लोगों को मतदाताओं की संख्या का आकार गौरव का सामान लगता है।
जिस तरह हिन्दुस्तान के चुनाव भ्रष्टाचार पर टिके रहते हैं, कई पार्टियां करोड़ों रूपए लेकर टिकट देती हैं, इसके बाद टिकट पाने वाले उम्मीदवार चुनावी खर्च की सीमा से सैकड़ों गुना ज्यादा भी खर्च करके किसी फंदे में नहीं फंसते, और संसद या विधानसभाओं में पहुंच जाते हैं, ताकत रहने पर मंत्री भी बन जाते हैं, यह सब दिल दहलाने वाला नजारा है। लेकिन इन सबको भी लोकतंत्र की तथाकथित कामयाबी और निरंतरता के नाम पर अनदेखा कर दिया जाता है। भारतीय लोकतंत्र अब न गरीबों का हिमायती रह गया है, न ही धर्म और जाति के आधार पर जो तबके गरीब हैं, उनका हिमायती। यह लोकतंत्र कानून बनाने से लेकर कानून लागू करने तक, और उस कानून के आधार पर फैसला देने तक, किसी भी तरह के काम में दौलतमंदों के पास गिरवी रखे गए सामान की तरह हो गया है। पिछले कुछ दशकों में किस तरह हिन्दुस्तानी लोकतंत्र धीरे-धीरे सबसे अधिक पैसेवालों का जरखरीद सामान हो गया है, किस तरह अरब-खरबपतियों की पसंद उम्मीदवारी तय करने से लेकर चुनाव जितवाने तक, और फिर मंत्री बनवाने तक काम आने लगी हैं, यह देखना भी भयानक है। और हिन्दुस्तानी लोग धीरे-धीरे होने वाले इस पतन को देखने के इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें अब यह बड़ा स्वाभाविक लगने लगा है। लेकिन देश के बाहर से अगर शोधकर्ता यहां आएंगे, तो उन्हें भारतीय लोकतंत्र में अंतर्निहित विसंगतियां और विरोधाभास सतह पर तैरते हुए दिखेंगे, जिन्हें देखने के हम आदी हो चुके हैं, और हमें इनका अहसास होना बंद हो चुका है।
हम किसी एक पार्टी या गठबंधन, एक प्रदेश या एक चुनाव को लेकर ये तमाम बातें नहीं लिख रहे हैं। हमारा यह साफ मानना है कि भारतीय लोकतंत्र में तमाम किस्म के भ्रष्ट तत्व धीरे-धीरे करके जिस तरह और जिस हद तक नवसामान्य मान लिया गया है, वह लोकतंत्र के पतन का एक बड़ा लक्षण है। एक निहायत ही भ्रष्ट, नाजायज, और अनैतिक चुनाव को अगर कामयाब लोकतंत्र मानकर उसे दुनिया में सबसे अधिक गर्व के लायक मान लिया गया है, तो इसकी बुनियादी खामियों पर कभी शर्मिंदगी और सुधार की तो गुंजाइश ही नहीं रहेगी। खैर, दुनिया में लोगों को वैसी ही सरकार मिलती है, जैसी सरकार के वे हकदार रहते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
-सुनील कुमार
हिन्दुस्तानी आम चुनाव के नतीजे उन लोगों को तो चौंकाने वाले हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया, और एक्जिट पोल का मजा लेते बैठे थे। इन सबके मुताबिक देश में एक मोदी लहर चल रही थी, जिसमें इंडिया नाम का गठबंधन बह जाने वाला था। लेकिन अभी जब नतीजे आ रहे हैं, तो दोपहर 4 बजे के रूझान के आंकड़ों को लेकर हम यह टिप्पणी लिख रहे हैं। सभी 543 सीटों पर वोटों की गिनती चल रही है, और चार सौ पार के एक मुश्किल नारे के साथ देश के इतिहास का सबसे आक्रामक चुनाव अभियान चलाने वाले, एनडीए के चेहरे नरेन्द्र मोदी को दावे और एक्जिट पोल की उम्मीद के मुताबिक कामयाबी मिलते नहीं दिख रही है। इस पल के आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले भी काफी कम सीटें मिल रही हैं। एनडीए को 295 सीटें मिल रही हैं, जिनमें से भाजपा की सीटें 239 हैं। लोगों को याद होगा कि पिछले आम चुनाव में भाजपा की अपनी कमल छाप सीटें 303 थीं, और इस बार वह 63 सीटें खोते दिख रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास पिछले लोकसभा चुनाव में 52 सीटें थीं, जो कि अब 100 होते दिख रही हैं, यानी कांग्रेस को 48 सीटों का इजाफा हुआ है। इंडिया-गठबंधन पिछले चुनाव में इस शक्ल में नहीं था, और इस बार उसमें दूसरी पार्टियां जुड़ी हैं, और इस गठबंधन को 230 सीटें मिलने का आसार दिख रहा है। ये चुनावी नतीजे बहुत अधिक फेरबदल वाले नहीं दिख रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अपने दावों, उम्मीदों, और मीडिया-समर्थन के मुताबिक अधिक होता न देखकर भाजपा में एक निराशा होगी, लेकिन देश की अगली सरकार तो किसी कीर्तिमान से नहीं बनती है, गिनती से बनती है, और गिनती तो यही है कि एनडीए की अगुवाई कर रही भाजपा अपना अगला प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। यह रिकॉर्ड भी कोई कम नहीं है, और जीतकर लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले मोदी शायद नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे। भाजपा को अपना ही नारा खासे वक्त तक चुभते रह सकता है, अबकी बार चार सौ पार अब जमीन पर तीन सौ तक भी पहुंचते नहीं दिख रहा है। इससे अधिक तो भाजपा की अपनी कमल छाप सीटें पिछली बार थीं।
यह आम चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक था। एक तरफ तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक, तृणमूल से लेकर दक्षिण की पार्टियों तक, उधर कश्मीर में फारूख से लेकर बिहार में लालू तक, अनगिनत मोदी विरोधी नेता और पार्टी लगातार केन्द्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर बने हुए थे। हो सकता है कि इनमें से बहुत से भ्रष्टाचार में शामिल रहे हों, लेकिन इनके मुकाबले देश में एक ऐसी तस्वीर बन रही थी कि भाजपा, और एनडीए के तमाम लोग दूध के धुले हुए हैं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई अच्छी बात है, लेकिन जब 95 फीसदी मामले सिर्फ विपक्ष के लोगों पर हों, तो जनता को भी यह बात कहीं न कहीं दिख रही होगी, और चुभ रही होगी। यही वजह है कि एनडीए गठबंधन ने तो कुल 63 सीटें खोई हैं, लेकिन उसके भीतर भाजपा ने 66 सीटें खोई हैं। अब जब चुनावी नतीजे सामने हैं, तो भाजपा के एजेंडे को भी देखना होगा जिसने इस चुनाव को मुंह से कहे बिना देश में एक धार्मिक जनमत संग्रह में तब्दील कर दिया था। उसके तमाम नारे, मनमोहन सिंह की न कही हुई बात का हिन्दू-मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल, मुसलमानों को कहीं घुसपैठिया कहना, कहीं ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को शामिल करने का विरोध करना, तो कहीं मंगलसूत्र छीन लिए जाने का डर दिखाना, ऐसी इतनी बातें चुनाव प्रचार में खुद प्रधानमंत्री के भाषणों में कही गईं, कि पार्टी के बाकी नेताओं के भाषणों और बयानों में उसी की गूंज चलती रही। और तो और भाजपा ने एक बहुत बड़ा बेबुनियाद, और भडक़ाऊ नारा अपने सर्वोच्च स्तर से चलाया था कि अगर इंडिया-गठबंधन की सरकार बनी तो राम मंदिर पर बाबरी ताला डल जाएगा। यह सुनते हुए भी चुनाव आयोग उसी तरह सोते रहा, जिस तरह अपने पोते के सैकड़ों बलात्कार की शिकायतें सुनते हुए एचडी देवेगौड़ा सो रहे थे, या अपने को पसंद सरकार के भ्रष्टाचार अनदेखे करते हुए अन्ना हजारे सोते हैं। केन्द्र सरकार के एक विभाग की तरह काम करने की तोहमत झेल रहे चुनाव आयोग को भी भाजपा को धर्म के आधार पर बयानबाजी न करने को कहना पड़ा। हालांकि आयोग अपने बाकी फैसलों, और बाकी कार्रवाई से मजाक का सामान बनते रहा, और सोशल मीडिया पर उसके बारे में यह लिखा जाता रहा कि आयोग भाजपा सरकार में शामिल नहीं होगा, वह बाहर से समर्थन जारी रखेगा। भाजपा का नारा तो आज मतगणना के बाद हारा है, चुनाव आयोग अपनी साख बहुत पहले से हार चुका है, और इससे कम विश्वसनीयता वाले लोग इसके पहले कभी चुनाव आयोग पर नहीं बैठे थे। फिर भी जो भी हो, एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार एक स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता पर आ गया है, और गठबंधन को अपने नुकसान पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि कौन सी ऐसी वजहें थीं कि वह चार सौ सीटों के अपने नारे, और पिछली लोकसभा में अपनी 353 सीटों के आंकड़ों से इतना पीछे रह जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र में आत्मविश्लेषण न करने, अपने तौर-तरीकों को न सुधारने, किसी की आलोचना बर्दाश्त न करने का पूरा कानूनी हक हर किसी को रहता है। लेकिन ऐसे हक का ऐसा इस्तेमाल लोगों को और गहरे गड्ढे में डालता है। भाजपा के सामने अभी लंबा राजनीतिक जीवन है, और उसे पिछले पांच बरस के अपने तौर-तरीकों के बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए कि देश की बहुसंख्यक हिन्दू आबादी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिमों के खिलाफ इस हद तक हमलावर अभियान भी उसे ईडी-आईटी-सीबीआई से जख्मी पार्टियों पर फतह क्यों नहीं दिला पाया? क्या देश की जनता का राजनीतिक और धार्मिक बर्दाश्त उतना अधिक नहीं है जितना कि भाजपा उम्मीद कर रही थी? यह मौका जेल और कटघरों में खड़े इंडिया-गठबंधन के नेताओं के लिए भी चाहे कानूनी राहत का न हो, राजनीतिक राहत का तो है ही कि जनता ने इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई को पसंद नहीं किया, और एनडीए-गठबंधन के भीतर भाजपा की शिकस्त गठबंधन की कुल शिकस्त से अधिक बड़ी हुई। अभी आज यहां पर हम अलग-अलग क्षेत्रीय पार्टियों, और राज्यों के नतीजों का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, और महज राष्ट्रीय स्तर पर सामने आई एक बड़ी तस्वीर पर छोटी सी टिप्पणी कर रहे हैं।
अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां पर यह अखबार बसा हुआ है, तो यहां की 11 में से 10 सीटों पर भाजपा को जीत मिलते दिख रही है, और यह जीत पिछले लोकसभा चुनाव से एक सीट अधिक ही है। इसलिए यह राज्य की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के लिए एक राहत की बात भी होगी कि उन्होंने भाजपा की सीटों में कुछ इजाफा ही किया है। छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट से ज्योत्सना महंत मौजूदा कांग्रेस सांसद हैं, और वे ही कोरबा सीट से भाजपा की दिग्गज नेत्री सरोज पांडेय को हराते हुए दिख रही हैं, वे छत्तीसगढ़ से अकेली कांग्रेस सांसद रहेंगी, अगर आगे की मतगणना में यही रूख कायम रहता है। उनके पति डॉ.चरणदास महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और प्रदेश कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता भी हैं, और अपनी सज्जनता के लिए जाने जाते हैं। पति-पत्नी की यह मिलीजुली जीत दोनों के राजनीतिक कद और उनकी ताकत में इजाफा करेगी। खासकर उस हालत में जब पांच बरस प्रदेश के अभूतपूर्व ताकत वाले मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल चुनाव हारते दिख रहे हैं, और कांग्रेस के कई बड़े-बड़े नेता छत्तीसगढ़ में चुनाव हार रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नतीजों का विश्लेषण भी हम अलग से करेंगे, आज मतगणना के आंकड़ों के बीच यह टिप्पणी टीवी स्क्रीन पर बदलते हुए नंबरों का एक विश्लेषण है। बाकी बातें आने वाले दिनों में। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी सामने हैं जिनके मुताबिक ओडिशा में पिछले 24 बरस से मुख्यमंत्री चले आ रहे नवीन पटनायक की सरकार को बेदखल करके भाजपा वहां राज्य सरकार बनाने के करीब है। दूसरी तरफ आन्ध्र में एनडीए के साथ की घोषणा कर चुके चन्द्राबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी भारी लीड के साथ सरकार बना रही है, और नायडू ने अभी खुलकर घोषणा की है कि वे एनडीए के साथ रहेंगे।
चलते-चलते बस एक बात और, एक्जिट पोल से देश के मनोरंजन की एक शाम अच्छी गुजरी थी, और जैसी शिकस्त एनडीए की हुई है, उससे बुरी शिकस्त एक्जिट पोल की हुई है।
एक फिलीस्तीनी आतंकी या फौजी संगठन हमास के हमले के बाद इजराइल ने पिछले कुछ महीनों में फिलीस्तीन के गाजा शहर पर हर किस्म के हमले करके अब तक 35 हजार से अधिक लोगों को मार डाला है, और जख्मियों की कोई गिनती नहीं है। लोगों के खाने-पीने का सामान नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मदद गाजा में पहुंचने नहीं दी जा रही, और अमरीका जैसे बेईमान देश एक तरफ मदद भेजने का नाटक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इजराइल को बम दिए जा रहे हैं ताकि वह और अधिक फिलीस्तीनी मार सके। दुनिया का सबसे ताकतवर मवाली देश अमरीका अब लगातार यह नाटक कर रहा है कि वह युद्धविराम की कोशिश कर रहा है, और उसने इजराइल को कुछ किस्म के हथियारों की सप्लाई स्थगित की हुई है। ऐसा लगता है कि एक गिरोहबंदी के तहत अमरीका और इजराइल दुनिया के दिखावे के लिए एक नूराकुश्ती लड़ रहे हैं, और इतिहास में अमरीका फिलीस्तीनियों के जनसंहार से अपनी असहमति दर्ज करा रहा है, लेकिन नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के पहले अमरीकी सरकार अमन के लिए काम करते दिखना चाहती है। ऐसा पाखंड दुनिया के कई मोर्चों पर भरा हुआ है, और इसे देखने-समझने की जरूरत है, और यह देखने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों के परंपरागत तौर-तरीकों से परे हटकर देखने की ताकत भी चाहिए।
आज खुद इजराइल की सरकार के भीतर इस बात को लेकर बड़ी असहमति है कि गाजा पर किया गया यह हमला खत्म कैसे होगा? हिन्दुस्तान में एक कहानी कही जाती है कि किस तरह अभिमन्यु ने मां के पेट में रहते हुए चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था, लेकिन उसने चक्रव्यूह में से निकलना नहीं सीखा था, और असल जंग में वह उसी में फंसकर मारा गया था। अमरीका करीब 20 बरस तक वियतनाम पर हमला करके एक जंग चलाते रहा, और फिर इस बेनतीजा जंग को छोडक़र उसे निकलना पड़ा। इस जंग के दौरान करीब 9 बरसों में अमरीका ने वियतनाम पर करीब 26 करोड़ क्लस्टर बम दागे थे। हम इस जंग की पूरी कहानी पर यहां जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अमरीकियों ने वियतनामियों की एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया था। अमरीकी सैनिकों ने वियतनामी युवतियों से जितने बच्चे पैदा किए थे, वे अमरीका के सामने एक नई चुनौती पेश करते हुए खड़े थे। दूसरी तरफ अमरीका ने एक वक्त इराक पर हमला किया, बरसों तक वहां के शासन को अपने कब्जे में रखा, और वहां से बेनतीजा निकलना पड़ा। फिर अफगानिस्तान की बारी थी, वहां हमला करके अमरीका ने पूरा शासन अपने कब्जे में रखा, 20 बरस इस देश को हांकने के बाद अमरीका किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा, और अफगानिस्तान को एक बार उन्हीं खूंखार तालिबानों के हवाले करके निकला, जिनसे अफगानिस्तान को आजाद कराने का दावा करते हुए वह वहां घुसा था।
किसी देश की मौजूदा सरकार को हटाने के लिए उस पर हमला करना, सरकार को बेदखल करना तो कम मुश्किल काम रहता है। अधिक मुश्किल रहता है उस सरकार की जगह नई सरकार कायम करना। और सरकार को बेदखल करने की नीयत न भी हो, तो भी किसी देश में वहां की सरकार और जनता के कंधे पर बंदूक रखकर अपने दूसरे फौजी इरादों को पूरा करना यूक्रेन में देखने मिल रहा है, जहां रूसी हमले का सामना करने के लिए अमरीका और योरप के देश यूक्रेन की फौजी हथियारों से मदद कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के हाथ उन्होंने पीछे बांध रखे हैं। अभी तक अमरीका और नाटो के बाकी देश जो हथियार यूक्रेन को दे रहे थे, उनके साथ यह शर्त लगा रखी थी कि उनका इस्तेमाल रूस के भीतरी ठिकानों पर वार करने के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए रखा गया था कि रूस इससे भडक़कर कोई परमाणु युद्ध न छेड़ दे। लेकिन यूक्रेन को गले-गले तक इस जंग में धंसा देने के बाद नाटो देश यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह मदद कब तक जारी रखी जाएगी, कब तक रूस को खोखला करने की नीयत पूरी हो सकेगी, और रूसी हमलों के बाद यूक्रेन नाम के बचे हुए खंडहर को किस दाम पर खड़ा किया जा सकेगा। वियतनाम से लेकर इराक, अफगानिस्तान, यूक्रेन, और अब गाजा तक की फौजी कार्रवाईयां उस चक्रव्यूह की तरह हैं जिनमें घुसना तो अभिमन्यु को आता था, लेकिन जिससे निकलना नहीं आता था। यूक्रेन अमरीका और योरप के गले की हड्डी बन गया है, ठीक इसी तरह आज फिलीस्तीन का गाजा इजराइल और अमरीका सहित इस गिरोह के बाकी देशों के सामने आज की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है कि यह दुनिया फिलीस्तीन का क्या करने जा रही है? इस नौबत का इजराइल के पास भी कोई समाधान नहीं है, और इजराइल आज एक ऐसा देश हो गया है जहां प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के मुकदमे तैयार खड़े हैं, और जिसने देश के सबसे कट्टरपंथी दलों की मदद लेकर इजराइल के इतिहास की सबसे संकीर्णतावादी सरकार बनाई है। और आज जब फिलीस्तीन के साथ इजराइल के किसी किस्म के युद्धविराम की बात हो रही है, तो ये कट्टरपंथी पार्टियां इजराइली प्रधानमंत्री की सरकार गिरा देने की धमकियां दे रही हैं। आज इजराइल के सामने यह लाख रूपए का सवाल खड़ा हुआ है कि वह फिलीस्तीन का क्या करेगा? जिसकी जमीन पर अवैध कब्जा करके इजराइलियों ने अपना देश बसा लिया है, और फिलीस्तीनियों को उनकी ही जमीन पर शरणार्थी और फौजी बंधक बनाकर रखा है, क्या उस पूरी आबादी के खत्म हो जाने तक फौजी हमले जारी रखने की इजाजत दुनिया उसे देगी, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक इजराइल का अधिक बड़ा बहिष्कार दुनिया में होने लगेगा? इजराइल के पास फिलीस्तीन पर किए जा रहे जुल्म को खत्म करने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि बीते बरसों में लाखों फिलीस्तीनियों को मार डालने के बाद बचे हुए लाखों फिलीस्तीनियों के जख्म और उनकी नफरत से इजराइल कैसे महफूज रह सकेगा?
दुनिया में जब कभी बड़े फौजी फैसले लिए जाते हैं, तो उनमें अक्सर ही नागरिक-समझ की कमी रहती है। फौजी फैसले यह नहीं बताते कि जब मोर्चे से फौज हट जाएगी, तो रोजाना का काम कैसे चलेगा? जिस फिलीस्तीन को दुनिया का सबसे बड़ा मलबा बना दिया गया है, जहां दुनिया के इतिहास के सबसे अधिक संख्या के आम नागरिकों को इतने कम वक्त में, संयुक्त राष्ट्र की रोक-टोक के बावजूद मारा गया है, उस फिलीस्तीन पर जंग रोककर इजराइल कैसे अपने आपको बचा सकेगा, यह बहुत बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा है। दूसरी तरफ दो बरस से लगातार यूक्रेन की फौजी और दीगर किस्म की मदद करते हुए अमरीका और योरप थके हुए हैं, लेकिन रूस को खोखला करने की अपनी नीयत के चलते वे यूक्रेनी फौजियों और जनता की कुर्बानी दिए जा रहे हैं। अब यह बेनतीजा दिखती जंग यूक्रेन पर किस-किस तरह से भारी पड़ेगी, पड़ रही है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जंग को इतने ऊपर तक ले जाने के बाद अब उसे खत्म करके एक देश को फिर से कैसे बसाया जाए, यह इलाज किसी के पास नहीं है।
दिक्कत यह है कि ऐसी नौबतों से जूझने के लिए, ऐसी बर्बादी को रोकने के लिए जिस संयुक्त राष्ट्र संघ का असर हो सकता था, उसे दुनिया की महाशक्तियों की वीटो-ताकत ने बेअसर कर रखा है। वरना यह आज के वक्त की एक बड़ी जरूरत की संस्था थी, जिसकी हेठी अमरीका ने इराक और अफगानिस्तान पर हमले वक्त भी की, और फिलीस्तीन के खिलाफ तो अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र को कुछ समझा ही नहीं। आज की यह नौबत दुनिया के सीखने की है कि जंग छेडऩा आसान होता है, उसे खून-खराबा खत्म होने के बाद अमन में तब्दील करना नामुमकिन सरीखा होता है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने दो दिन रायपुर के आईआईएम में देश के दूसरे आईआईएम से भी आए हुए विशेषज्ञों के व्याख्यान सुने, और शासन चलाने के बेहतर तरीकों पर उनसे जानकारी हासिल की। सोच थोड़ी नई है क्योंकि प्रदेश चलाने वाले लोग किसी की क्लास में जाकर बैठें, ऐसा कभी नहीं होता है, आमतौर पर निर्वाचित नेताओं को सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान मान लिया जाता है। जिस तरह किसी हीरे को और शुद्ध करना मुमकिन नहीं रहता, उसी तरह सत्तारूढ़ पार्टी के निर्वाचित, मनोनीत, या संगठन पर काबिज नेता अपने को समझते हैं। इसलिए अगर छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने यह तय किया कि उसे शासन-प्रशासन के जानकार और विशेषज्ञ लोगों से कुछ सीखना है, तो यह एक अनोखी पहल है जिससे दूसरे देश-प्रदेश भी सीख सकते हैं। इस पर छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली थी जिसका कहना था कि भाजपा ने प्रदेश में 15 बरस राज किया है, और अगर आज के भाजपा मंत्रियों को कुछ सीखना था, तो अपने ही भूतपूर्व मंत्रियों से सीखना चाहिए था। यह सलाह किसी विरोधी या दुश्मन को तो दी गई हो सकती है, यह सही नहीं हो सकती। 15 बरस बाद जिस सरकार ने सत्ता इस बुरी तरह गंवाई थी, उससे सीखने की बात कोई दुश्मन ही कर सकते हैं। सच तो यह है कि जिंदगी के बहुत से दायरों में बाहर के लोग ही गलतियां बताने, सुधार सुझाने, और नई बातें सिखाने के लायक हो सकते हैं। इसीलिए बाहरी व्यक्तियों, या आऊटसाइडर्स का एक अलग महत्व होता है क्योंकि उनके स्वार्थ ऐसे भीतरी लोगों से जुड़े हुए नहीं होते हैं जिन्हें सिखाने की जिम्मेदारी मिली है। अब वैसे तो किसी भी राज्य में प्रशासन के मुखिया, मुख्य सचिव मंत्रियों को सिखाने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन वे इसी व्यवस्था का हिस्सा रहते हैं, और इन्हीं निर्वाचित मंत्री-मुख्यमंत्री के मातहत काम करते हैं, इसलिए बाहरी विशेषज्ञों और जानकारों से शासन-प्रशासन की कुछ बातों को सीखना काम का हो सकता है।
दूसरी तरफ किसी भी देश-प्रदेश में कई ऐसे दूसरे तबके रहते हैं जिनसे चाहे सीखने जैसे शब्दों में न कहें, लेकिन जिनसे समझना काम का हो सकता है। किसी भी प्रदेश में गंभीर अखबारनवीस, जनसंगठनों के लोग, जिंदगी के अलग-अलग दायरों के विशेषज्ञ और जानकार ऐसे हो सकते हैं जिनसे बात करके सरकार कुछ सीख सके। यह तो ठीक है कि चुनाव और मतगणना के बीच यह तकरीबन खाली वक्त छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने आईआईएम के विशेषज्ञ प्राध्यापकों को सुनने में लगाया, और अगर हम दुनिया में भारत की विशेषज्ञता का सम्मान देखते हैं, उसकी कामयाबी देखते हैं, तो उनमें आईआईएम और आईआईटी दो सबसे प्रमुख संस्थान हैं। इसलिए चाहे यह शोहरत पाने की एक कसरत हो, है तो सही दिशा में। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ और चीजों पर भी सरकार को मेहनत करनी चाहिए, अगर उसकी नजर में विशेषज्ञ का सचमुच ही सम्मान है।
हम बहुत से विभागों के कामकाज, और म्युनिसिपल जैसी स्थानीय संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों को देखते हैं, तो बहुत तकनीकी मामलों में भी किसी तकनीकी विशेषज्ञ से कोई राय नहीं ली जाती, और निर्वाचित नेता या गिने-चुने प्रशासनिक अफसर तकनीकी फैसले लेते भी रहते हैं। अक्सर यह लगता है कि शिक्षाशास्त्री, इंजीनियर, डॉक्टर या दूसरे विषय विशेषज्ञों की कोई जरूरत नहीं है, और राज्य में हर किस्म के फैसले सत्तारूढ़ निर्वाचित नेता, या उनके चुने गए अफसर ले सकते हैं। इसी का नतीजा रहता है कि कोई सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी महीनों तक अपनी पसंद से ऐसी योजनाएं बनाते रहते हैं जो उन्हें वोटों के लिए जरूरी लगती हैं, और जो अगली सरकार को भी पसंद आएं, ऐसी कोई गारंटी नहीं रहती। विशेषज्ञों के सम्मान की सोच बहुत अच्छी है, जो सचमुच ही बड़े नेता से महान नेता बनना चाहते हैं, उन्हें किसी भी तरह के नीतिगत फैसले लेने के पहले, जनकल्याण के कार्यक्रम बनाने के पहले जानकार-विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए, अपनी सोच के विरोधियों से भी विचार-विमर्श करना चाहिए, और उसके बाद सत्ता अपने फैसले लेने को आजाद तो रहती है।
दरअसल सत्ता लोगों में यह अहंकार भर देती है कि उन्हें कुछ भी सीखने-समझने की जरूरत नहीं है, और वे 24 कैरेट सोने की तरह खरे हैं। यही खुशफहमी उन्हें बड़े नेता से महान नेता बनने नहीं देती। समझदार वे लोग रहते हैं जो कि दूसरों के तजुर्बों से लगातार सीखते चलते हैं, अपनी सोच को लागू करने की ताकत जब हो, तब दूसरों की राय सुनकर एक बेहतर नीति या योजना बनाने की समझदारी निर्वाचित नेताओं में रहनी चाहिए। बहुत आसपास के दूसरे नेता या अफसर तो आमतौर पर ठकुरसुहाती में लग जाते हैं, और अपने नेता के पांव भी जमीन पर नहीं पडऩे देते। हमने किसी दूसरे संदर्भ में पहले यह बात लिखी थी कि जो लोग बिना बात पांव पकड़ते रहते हैं, वे लोग कोई गलती या गलत काम दिखने पर भी हाथ पकडक़र रोक नहीं सकते। इसलिए बाहरी लोगों से सीखना तो महत्वपूर्ण है ही, जिंदगी में रोज के कामकाज में भी जानकार लोगों, विरोधियों, आलोचकों, और विशेषज्ञों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। निर्वाचित और सत्तारूढ़ होने के बाद किसी भी नेता की कोशिश महान काम करके महान नेता बनने की रहनी चाहिए। लेकिन लोग सत्ता से चिपके रहने, अधिक से अधिक कमा लेने को ही सब कुछ समझ लेते हैं। जो लोग इससे उबर पाते हैं, वही लोग सचमुच के नेता बनते हैं।
इस देश के एक सबसे महान दार्शनिक कबीर ने यह लिखा था, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय। बड़े-बड़े काबिल और कामयाब नेताओं को हमने ऐसे ही बर्बाद होते देखा है क्योंकि उन्होंने अपने आसपास चापलूसों की फौज इकट्ठा कर रखी थी। और हामी भरने वाले दरबारियों के बीच किसी का कद नहीं बढ़ सकता। राज्य शासन से बाहर के विशेषज्ञों से कुछ सीखने की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार की यह पहल अच्छी है, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सरकार में सत्तारूढ़ नेता और अफसर अलग-अलग विषयों और क्षेत्रों के जानकार लोगों के तजुर्बे का फायदा रोजाना के कामकाज में भी लेंगे। पांच बरस के कार्यकाल में कुछ दिनों की यह पहल तो अच्छी है, लेकिन इसका नियमित रूप से इस्तेमाल भी होना चाहिए। मंत्रालय से लेकर म्युनिसिपलों तक जब जानकार विशेषज्ञों का सम्मान होगा, तो ही सत्तारूढ़ नेता भी असल कामयाबी पा सकेंगे। सत्ता पर काबिज बने रहना ही जो लोग कामयाबी मान लेते हैं, वे वहीं थमकर रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। देखना यह भी रहता है कि सत्तारूढ़ नेताओं के राजनीतिक और प्रशासनिक सहयोगी उन्हें अपनी कैद से कितना बाहर निकलने देते हैं। हमने कई सरकारों में सत्तारूढ़ नेताओं को अपने ही दायरे के कैदी बनते देखा है, और उसका क्या चुनावी नतीजा रहा है, यह भी लोगों को अच्छी तरह याद होगा। फिलहाल प्रदेश के दूसरे स्थानीय निर्वाचित नेताओं के लिए भी ऐसे सत्र आयोजित किए जाने चाहिए जिनसे वे नगरीय विकास, स्थानीय शासन, पंचायती राज, और ग्रामीण विकास के अलग-अलग पहलुओं को बेहतर सीख-समझ सकें। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
भारत के आम चुनाव के आज के आखिरी मतदान में लोकसभा की दस फीसदी से अधिक सीटों पर वोट डल रहे हैं। सात राज्यों, और एक केन्द्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर इस वक्त वोट डल रहे हैं, और देश एक अभूतपूर्व गर्मी का सामना कर रहा है। कल एक दिन में लू से देश भर में करीब तीन सौ लोगों के मरने की खबर है, और बहुत से ऐसे लोग गुजरे होंगे जिनकी मौत इस वजह से दर्ज नहीं हो पाई होगी। पिछले ढाई महीने से चले आ रहा यह आम चुनाव जब एक राज्य बिहार में एक दिन में 15 चुनाव कर्मियों की लू से मौत दर्ज करता है, तो जाहिर है कि वोटरों में से भी बहुत से लोग निकलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यह सही वक्त है कि पांच बरस बाद के अगले आम चुनाव, या उसके बीच किसी बरस में मई-जून में अगर किसी राज्य के चुनाव होने हैं, तो उनकी तारीखों के बारे में अभी से तय कर लिया जाना चाहिए। और आम जनता के लिए चुनाव महज एक-दो घंटे मतदान केन्द्र आना-जाना हो सकता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी चुनाव इंतजाम में कई-कई दिन ट्रेनिंग पाते हैं, मतदान और मतगणना की तैयारी करते हैं, और सुरक्षा कर्मचारी तो इस गर्मी में सैकड़ों या हजारों किलोमीटर तक का सफर करके खतरनाक जगहों पर पहुंचते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब मई-जून के ये महीने भयानक गर्मी के रहते हैं, और हर बरस गर्मी बढ़ते चलती है, तो संसद या विधानसभाएं अपने कार्यकाल और अगले चुनाव को लेकर समय रहते कोई फैसला क्यों नहीं लेती हैं? क्या सांसद और विधायक अब एयरकंडीशंड कारों से बाहर निकलना जरूरी नहीं समझते? अगर आमतौर पर ऐसा होता भी है, तो भी इस बार का पूरा चुनाव अभियान तो गर्मी में ही गुजरा है, और पिछले कई हफ्तों में लगातार ऐसी भयानक गर्मी रही है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी दर-दर भटकने का अपना काम ठीक से नहीं कर पाए होंगे।
भारत में वैसे तो देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम हमेशा ही बहुत अलग-अलग रहता है, अब जैसे आज जब एक दिन में लू से तीन सौ लोग मरे हैं तो उसी दिन मणिपुर में भयानक बाढ़ आई हुई है, और असम में भी। असम में बाढ़ से आधा दर्जन लोगों के मरने की खबर है, और मणिपुर, मेघालय में भी भूस्खलन और सडक़-पुल डूब जाने या बह जाने की खबरें हैं। लाखों लोग बहुत प्रभावित हुए हैं, और उन्हें राहत शिविरों में रखा गया है। यह देश इतना विशाल है कि एक तरफ बाढ़ है, और दूसरी तरफ सूखे की वजह से बेंगलुरू जैसे शहर को खाली करवाने की सरकारी कोशिश चल रही है। लेकिन इस बीच भी पहाड़ों पर सर्दी खत्म हो जाने के बाद, और गर्मियां शुरू होने के पहले पूरे देश का मौसम कुछ ऐसा रहता है कि उस वक्त के चुनाव सबके लिए सहूलियत के हो सकते हैं, और उन चुनावों में जनता की भागीदारी भी अधिक हो सकती है। अप्रैल-मई-जून के बजाय अगर ये चुनाव फरवरी-मार्च-अप्रैल में हुए रहते, तो तमाम लोगों को बड़ी सहूलियत रहती। इस लोकसभा का कार्यकाल दो महीने कम करके आसानी से हर पांच बरस के चुनावी महीनों को बदला जा सकता था, अब भी बदला जाना चाहिए।
पता नहीं सुप्रीम कोर्ट इतनी मौतों को देखते हुए भी इस मामले में कोई दखल देने के लिए तैयार होगा या नहीं, न भी हो, वहां पर अगर किसी जनहित याचिका के तहत इस मुद्दे पर बहस ही हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सरकार और संसद के सोच-विचार के लायक कहकर छोड़ दे, तो भी इस पर बहस आगे बढ़ सकती है। देश में चुनाव तैयारी में ही सरकारी और राजनीतिक करोड़ों लोगों को हफ्तों तक काम करना पड़ता है, और उन पर यह जुल्म बंद होना चाहिए। फिर जिस अंदाज में मौतें हो रही हैं उनको देखते हुए किसी तरह की सरकारी या राजनीतिक जिद भी जायज नहीं है कि संसद के 60 महीने के कार्यकाल में से दो महीने कम नहीं किए जा सकते। इस मामले पर फैसला विधानसभाओं को जोडक़र लेना चाहिए क्योंकि इस चुनाव में ही कुछ विधानसभाओं का चुनाव हो ही रहा है। और बीच के बरसों में भी इन महीनों में कुछ और विधानसभाओं के या स्थानीय संस्थाओं के चुनाव होते हों, उन पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि चुनाव तो पांच बरस में एक बार ही आते हैं, और उन्हें हर बार झुलसाती हुई गर्मी में क्यों रखा जाए? आज तो हालत यह है कि देश के अलग-अलग प्रदेशों में सरकारें लोगों से यह अपील कर रही हैं कि वे दोपहर 12 से 4 के बीच बहुत जरूरी न हों, तो घरों से न निकलें। अब ऐसे में लोगों से चुनाव प्रचार करने, और वोट डालने निकलने की उम्मीद करना तो बहुत ही नाजायज होगा।
दुनिया में मौसम की मार बढ़ती चल रही है, हर बरस गर्मी बढ़ती चली जा रही है। आज ही खबरों में यह है कि नागपुर में कल तापमान 56 डिग्री था। आज तो 45 डिग्री पर भी लोग गिरकर मर रहे हैं, 56 डिग्री गर्मी कैसी रही होगी? आज ही की एक दूसरी खबर बताती है कि ईरान में कल 66 डिग्री सेल्सियस तापमान था। एक मेडिकल जानकारी वाला लेख बतलाता है कि 45 डिग्री के ऊपर इंसानों के दिमाग पर किस तरह का असर पडऩे लगता है। दिल्ली में कल 52.9 डिग्री तापमान था, और जो योरप आमतौर पर ठंडा माना जाता है, उसके भी अलग-अलग शहरों में बीते कुछ बरसों से लगातार बड़ी गर्मी दर्ज की जा रही है। मौसम के जानकार लोगों का कहना है कि यह गर्मी तो हर बरस बढ़ती ही चलेगी। सरकार को न सिर्फ चुनावों के लिए अलग महीने तय करने चाहिए, बल्कि सडक़ और भवन निर्माण जैसे बहुत से कामों के लिए यह तय कर लेना चाहिए कि उन्हें गर्मियों के पहले या उसके बाद किस तरह से करवाया जा सकेगा। फिलहाल आज मतदान निपट जाए, 4 तारीख को मतगणना निपट जाए, और अगली सरकार के सामने मई-जून के किसी भी राज्य के चुनावों के साथ-साथ संसद के अगले चुनावों का कैलेंडर बदलने का मुद्दा लाना चाहिए। कायदे से तो हमारे बजाय सांसदों और विधायकों को ही यह बात उठानी चाहिए थी, लेकिन उन पर शायद गर्मी की सीधी मार अब नहीं पड़ती है, इसलिए जनता के बीच से कुछ लोगों को संसद और विधानसभा के लिए, और जरूरत पड़े तो अदालत तक जाकर भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए। चुनाव प्रचार, इंतजाम, और हिफाजत, इन तीनों कामों में लगे हुए करोड़ों लोगों में से दो-चार फीसदी लोगों को भी एयरकंडीशनर नसीब नहीं होते हैं, इसलिए कानून बनाकर ही मौतों का यह खतरा घटाया जा सकता है।
अमरीका की जनता ने अभी कुछ घंटे पहले एक इतिहास रचा है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने जनता के बीच से चुने गए एक दर्जन ज्यूरी सदस्यों ने पिछले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप पर एक लंबी सुनवाई के बाद यह माना है कि उन पर लगे सभी 34 आरोप सही हैं। यह मामला एडल्ट फिल्मों की एक अभिनेत्री के साथ ट्रंप के एक पुराने सेक्सकांड का है जिसमें कुछ भी जुर्म नहीं था। नई-नई मुलाकात में ट्रंप ने इस अभिनेत्री, स्टॉर्मी डेनियल्स से 2006 में सेक्स किया था, और बाद में जब 2016 में वे जब राष्ट्रपति चुनाव लडऩे लगे, तो उन्होंने अपने वकील के मार्फत इस अभिनेत्री की चुप्पी खरीदी, और इसके लिए अपनी कंपनी की तरफ से कानूनी फीस के नाम पर इस वकील को एक लाख तीस हजार डॉलर दिए थे जो कि वकील ने इस अभिनेत्री को दिए। लेकिन बाद में जब यह मामला सुर्खियों में आ ही गया, और ट्रंप की तरफ से इस अभिनेत्री के खिलाफ उनके आम अंदाज में अपमानजनक बातें कही गईं, तो इस अभिनेत्री ने खुलकर सेक्स और चुप्पी के भुगतान का यह मामला उजागर किया। बाद में न्यूयॉर्क के सरकारी वकील ने ट्रंप के खिलाफ यह मुकदमा शुरू किया कि यह चुप्पी खरीदना चुनावी खर्च का हिस्सा था जिसे चुनावी खर्च में नहीं दिखाया गया, और मतदाताओं को अंधेरे में रखा गया। इस विवाद से जुड़ा हुआ एक पहलू यह भी था कि ट्रंप ने अपने इस चुनावी खर्च को अपनी कंपनी का कानूनी खर्च दिखाया, जो कि एक अलग बेईमानी थी। ऐसे बहुत से पहलू इस मुकदमे के 34 मुद्दे थे, और जनता के बीच से चुने गए ज्यूरी सदस्यों ने एकमत से इन सभी मुद्दों पर ट्रंप को गुनहगार माना है, और अब इस पर सजा का ऐलान अलग से होगा। जिस जनता ने 2016 में ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया था, उसी जनता के बीच से चुने गए ज्यूरी सदस्यों ने आज उन्हें गुनहगार ठहराया है। अमरीका की तरह एक वक्त हिन्दुस्तान में भी कुछ जगहों पर अदालतों में जनता के चुनिंदा प्रतिनिधि ज्यूरी बनकर बैठते थे, और वे ही गुनहगारी तय करते थे। अमरीका में अब भी यह व्यवस्था जारी है, और इस तरह जिस अमरीकी जनता ने एक वक्त ट्रंप को चुना था, उसी ने अब ट्रंप को खारिज कर दिया है। हालांकि इसके बाद भी चुनाव में ट्रंप का हार जाना तय नहीं दिख रहा है।
अमरीका बड़ा अजीब देश है, राष्ट्रपति चुनाव में दसियों लाख या करोड़ों डॉलर का खर्च होता है। हिन्दुस्तान में कई सीटों पर चुनाव आयोग की निर्धारित सीमा से सौ गुना खर्च होता है, लेकिन हिन्दुस्तान में हर खर्च कालेधन से हो जाता है, उसके लिए किसी बैंक खाते से भुगतान की जरूरत नहीं रहती। अब अगर ट्रंप हिन्दुस्तान में रहते, तो इतनी रकम एक छोटे से बंडल में बांधकर स्टॉर्मी डेनियल्स को दे दी जाती, और उसका कोई सुबूत भी नहीं रहता। लेकिन अमरीका में कालाधन उस तरह आम इस्तेमाल में नहीं रहता, और लोगों को चुनावी चंदे और खर्च के हिसाब में अधिक पारदर्शी रहना पड़ता है। अब इस मामले में सजा पाने के साथ ही ट्रंप अमरीका के पहले ऐसे भूतपूर्व राष्ट्रपति बन जाएंगे जिन पर आपराधिक मुकदमा चला, और जिन्हें सजा हुई। वे नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपनी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से एक बार फिर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस अदालती सजा से उन्हें जेल जाना पड़े, या न जाना पड़े, मतदाताओं के बीच उनकी कुछ तो फजीहत होगी ही। खुद रिपब्लिकन पार्टी के बहुत से नेता ही ट्रंप की उम्मीदवारी के खिलाफ हैं, क्योंकि अभी अधिक गंभीर कुछ दूसरे आपराधिक मामले बचे ही हुए हैं, जिनमें ट्रंप को बड़ी कैद हो सकती है। जब वे 2020 का चुनाव हारे थे, तो उनके समर्थकों ने अमरीकी संसद पर बड़ा हिंसक हमला किया था, और बहुत से संसद सदस्यों की जिंदगी मुश्किल से बची थी। उस वक्त ट्रंप ने अपने हमलावर सदस्यों को रोका नहीं था, बल्कि उन्हें उकसाया था। उनके उस वक्त के कमरे में मौजूद कुछ सहयोगियों ने अमरीकी संसद की सुनवाई में यह बयान भी दिया है कि उन्होंने ट्रंप को समर्थकों को शांत करने कहा था, लेकिन ट्रंप ने उनकी बात नहीं सुनी।
अमरीका भी बड़ा अजीब देश है जिस रिपब्लिकन पार्टी में बहुत से दूसरे अच्छे उम्मीदवार मौजूद हैं, वहां यह पार्टी दूसरी बार ट्रंप जैसे घटिया इंसान को उम्मीदवार बना रही है। किसी नेता की जीत की संभावनाओं से वे न तो महान हो जाते, और न ही भले। और यह बात ट्रंप पर पूरी तरह खरी उतरती है कि कामयाबी के अलावा उसकी और कोई खूबी नहीं है, और पिछले चुनाव के पहले तो उसने खुलेआम महिलाओं को दबोच लेने को लेकर इतनी घटिया बातें कही थीं कि उन्हें हिन्दी के पाठक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ट्रंप का पूरा का पूरा राष्ट्रपति-कार्यकाल घटिया हरकतों से भरा रहा, लेकिन पार्टी को चार बरस के फासले से अब होने जा रहे अगले चुनाव में भी ट्रंप से परे कोई नहीं सूझा। डोनल्ड ट्रंप की पूरी जिंदगी कानून से लुकाछिपी में ही गुजरी है। एक बड़े खरबपति कारोबारी होने के नाते वे उस धंधे के उसूलों के मुताबिक तमाम तिकड़म करके टैक्स चोरी करते रहे, और उन पर उसके मुकदमे भी चल रहे हैं। उन पर एक दूसरा मुकदमा यह चल रहा है कि पिछले राष्ट्रपति चुनाव में जब उनकी हार घोषित हो चुकी थी, तब उन्होंने एक राज्य के अपनी पार्टी के गवर्नर पर बहुत दबाव डाला था कि वह गिनती में गड़बड़ी करके ट्रंप को जीता हुआ घोषित कर दे। उस गवर्नर ने ऐसा करने से मना कर दिया था।
अब कुछ लोग रिपब्लिकन पार्टी को यह समझा रहे हैं कि वे ट्रंप की जगह किसी और को उम्मीदवार बनाएं क्योंकि ट्रंप को कई मामलों में कैद हो जाने का खतरा है, और वैसे में क्या जेल में रहते हुए ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकेंगे, इस पर लोगों को बड़ा शक है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अपनी पार्टी के भीतर भी ट्रंप प्रतिबद्ध वोटरों का समर्थन खोएंगे क्योंकि ऐसी शर्मिंदगी अब तक किसी भी नेता ने किसी भी पार्टी के लिए खड़ी नहीं की थी। लोगों का यह भी मानना है कि जो वोटर किसी पार्टी के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं, वे भी ट्रंप के खिलाफ रहेंगे, और असल चुनावी फैसला यही बीच के वोटर करते हैं। लेकिन ट्रंप दुनिया के सामने एक बेमिसाल नेता हैं जो कि इतने किस्म के कानूनी मामलों में फंसे होने पर भी अगला राष्ट्रपति बनने के लिए जान देने पर उतारू हैं। ट्रंप को किसी बात से शर्मिंदगी नहीं होती है, और यह अपने किस्म का अकेला मुजरिम नेता है, जिसके नए-नए मामले सामने आते भी रहते हैं। अमरीका में यह भी माना जा रहा है कि ट्रंप समर्पित समर्थकों में इस अदालती फैसले से कोई फर्क नहीं पडऩे वाला है, और वे लोग ट्रंप के भक्त किस्म के लोग हैं, जो कि हर कीमत पर उसे चाहते हैं।
ट्रंप को इस मामले में 11 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी, और उसके बाद उनके सामने बड़ी अदालत तक जाकर इस फैसले के खिलाफ अपील करने की गुंजाइश भी रहेगी। ऐसा लगता है कि यह मामला नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तक किसी अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच सकेगा, और ट्रंप के दीवाने भक्तों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका नेता कितना भ्रष्ट, या कितना दुष्ट है। इस बरस दुनिया के 60 देशों में चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में हर देश की मिसाल दूसरे देश में चर्चा तो बनती ही है। देखना है कि यह बरस पूरा होने तक दुनिया अधिक कट्टर और दकियानूसी बनती है, या उदारता की कोई जगह निकलती है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
हिन्दुस्तान में हर दिन हजारों लोगों को क्रिप्टोकरेंसी, गोल्ड मार्केट, और शेयर बाजार में पूंजीनिवेश का झांसा देकर हजारों करोड़ की ठगी की जा रही है। और यह सिर्फ इसी देश का मामला नहीं है, आज ही यह खबर आई है कि नाइजीरिया के मुजरिमों का एक गिरोह पूरी दुनिया में कम उम्र बच्चों और किशोरों को इंटरनेट पर किसी तरह से फांस लेता है, और उसके बाद उनकी नंगी तस्वीरें या वीडियो जुटाकर उनको ब्लैकमेल करना शुरू करता है। ऐसे कई बच्चे खुदकुशी भी कर लेते हैं। हालत यह हो गई है कि अपनी नग्न तस्वीरें भेजने से लेकर किसी के कहे हुए अपना बैंक खाता किसी के हवाले कर देने, किसी भी संदिग्ध और रहस्यमय कारोबार में पूरा पैसा डाल देने जैसे काम खासे पढ़े-लिखे और अपने को होशियार समझने वाले लोग भी बिजली की रफ्तार से करते हैं। अभी-अभी छत्तीसगढ़ में भिलाई की एक मेडिकल प्रोफेसर क्रिप्टोकरेंसी झांसे में आ गई, और 58 लाख रूपए ठगों के अलग-अलग खातों में डाल दिए गए। दूसरी तरफ वहीं पर बीएसपी के एक दूसरे रिटायर्ड अफसर ने महीने भर में ऐसे ही ठगों को सवा करोड़ से अधिक दे दिए। अब पुलिस मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन ऐसे मामलों में टेलीफोन नंबर बंद मिलने लगते हैं, और बैंक खातों से पैसा कई दूसरे खातों से होते हुए गायब हो चुका रहता है। वॉट्सऐप पर इस अखबार के संपादक सहित दूसरे लोगों को हर दिन किसी न किसी ऐसे पूंजीनिवेश समूह में जोड़ दिया जाता है, जिसमें ठगों का जत्था कीर्तन करने के अंदाज में भारी मुनाफा गिनाते रहता है, और नए लोगों को झांसा देते रहता है।
हिन्दुस्तान में जिस रफ्तार से डिजिटलीकरण हुआ है, उस रफ्तार से डिजिटल-जागरूकता नहीं बढ़ी है। लोगों के बैंक खाते, और भुगतान के दूसरे तरीके तो उनके मोबाइल फोन पर आ गए हैं, और कुछ नंबर दबाते ही वे रकम ट्रांसफर कर सकते हैं, या किसी तरह का ओटीपी उनके खाते में आने पर लोग पूरा अकाऊंट ही खाली कर देते हैं। इससे परे सैकड़ों लोन ऐप ऐसे हैं जो कि लोगों को टेलीफोन पर ही कर्ज मंजूर कर देते हैं, और उनके मोबाइल फोन ऐप डाउनलोड करते ही फोन के तमाम फोटो-वीडियो, और फोनबुक पर साइबर-साहूकारों का कब्जा हो जाता है। इसके बाद वे कर्ज उगाही के लिए अंधाधुंध अंदाज में ब्लैकमेल करते हैं, धमकाते हैं, फोन पर से हासिल कर लिए गए फोटो-वीडियो फोनबुक के हर किसी को भेज देने की धमकी देते हैं, और नमूने के बतौर कुछ लोगों को भेजकर दबाव भी बनाते हैं। भारत सरकार लगातार ऐसे कई मोबाइल ऐप बंद करती है, और फिर यही कारोबारी कुछ दूसरे नामों से फिर नया ऐप लांच करते हैं, और जालसाजी जारी रखते हैं।
अभी दुनिया में तकरीबन तमाम मोबाइल ऐप सिर्फ गूगल और एप्पल के मोबाइल सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध रहते हैं, और यूरोपियन यूनियन सहित कई जगहों पर इन दो लोगों के एकाधिकार के खिलाफ कार्रवाई की बात चल रही है। लेकिन इन दोनों कंपनियों का तर्क यही है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर आने वाले हर मोबाइल ऐप की इतनी गहरी छानबीन करते हैं कि उनसे धोखाधड़ी का खतरा कम रहता है। खासकर एप्पल ने अभी हाल ही में यह दावा किया है कि उसके प्लेटफॉर्म की सुरक्षा तकनीक की वजह से जालसाज लोग वहां जगह नहीं पा सकते, और एप्पल के फोन इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत अधिक सुरक्षित रहते हैं। अब एक दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि एक तरफ तो बड़ी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर मोबाइल ऐप को जगह देने के पहले उसकी जांच करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किए गए मोबाइल ऐप के मार्फत हर तरह की धोखाधड़ी चल रही है। वॉट्सऐप पर जो पहली नजर में धोखाधड़ी के ग्रुप बनाए जाते हैं, उनकी शिनाख्त करना इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए कि इस लोकप्रिय मैसेंजर सर्विस की मालिक मेटा नाम की कंपनी उसकी शिनाख्त न कर सके। लेकिन न सिर्फ वॉट्सऐप पर, जिस पर कि संदेशों के गोपनीय रखने का दावा किया जाता है, बल्कि फेसबुक जैसे खुले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर दिन लाखों ऐसे इश्तहार आते हैं जो जाहिर तौर पर धोखाधड़ी के हैं। इनके खिलाफ वहीं पर यह टिप्पणी की जाए कि ये फ्रॉड हैं, धोखाधड़ी हैं, तो भी फेसबुक उनको परखता नहीं है। दूसरी तरफ फेसबुक पर ऐसे इश्तहार हर दिन आते रहते हैं जिनमें कई किस्म के कपड़े और दूसरे सामान बहुत असंभव किस्म के सस्ते दाम पर दिखाए जाते हैं, और उनका एडवांस पेमेंट कर देने के बाद न सामान आता, न कोई जवाब आता। हमारा ख्याल है कि धोखेबाजी के ऐसे इश्तहार दिखाने पर फेसबुक के खिलाफ जुर्म दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि मामूली समझ रखने वाले लोगों को भी पहली नजर में यह दिख जाता है कि कौन-कौन से इश्तहार धोखा देने वाले हैं, तो वह फेसबुक के बड़े माहिर कम्प्यूटरों को कैसे समझ नहीं आएगा।
कुल मिलाकर कम्प्यूटर, इंटरनेट, और मोबाइल फोन की दुनिया लोगों को बहुत बड़े खतरे में भी डाल रही है। लोग सोशल मीडिया पर बालिग किस्म के मामलों में भी हॅंस रहे हैं, और ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं, लोन देने वाले लोग इस कदर ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आत्महत्याएं हो रही हैं। अब नाइजीरिया के लोगों का गिरोह पश्चिमी दुनिया में इस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं कि बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। जो रिटायर्ड लोग अपनी पूरी जिंदगी की बचत किसी पूंजीनिवेश के झांसे में डुबा दे रहे हैं, तो वे भी जीते जी मरने की हालत में पहुंच गए हैं। अलग-अलग देशों की सरकारों को अपने स्तर पर, और सामूहिक रूप से भी साइबर-जुर्म रोकने के लिए अधिक कोशिश करनी होगी, क्योंकि मुजरिम पकडऩे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल हो, या न हो, जुर्म करने के लिए तो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल बढ़-चढक़र शुरू हो गया है, और मुजरिम अपने शिकार छांटने के लिए खासकर एआई-औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत जैसे देश में डिजिटल तकनीक को जिंदगी के बहुत से दायरों में सरकार ने अनिवार्य सरीखा कर दिया है। लोगों की जानकारी सरकार के ही कई-कई विभागों और योजनाओं के कम्प्यूटरों पर चढ़ती है। इनमें से कौन सी जानकारी सरकार बाजार को इस्तेमाल के लिए दे रही है, और कौन सी जानकारी बाजार चुरा रहा है, यह जानना कुछ मुश्किल है, लेकिन अभी दुनिया भर में चल रहे अध्ययन बताते हैं कि साइबर-ठगी, जालसाजी के शिकार होने वाले बच्चों की उम्र अब घटती चल रही है। और बच्चे कम उम्र में ही ठगी के शिकार भी हो रहे हैं, और यौन शोषण जैसे गंभीर जुर्म भी उनके खिलाफ हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया भर की सरकारें मिलकर भी मुजरिमों से बहुत पीछे चल रही हैं, और यह सिलसिला बदलने की जरूरत है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
मोबाइल फोन के कैमरों की मेहरबानी से सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्ते मरने और मारने तक पहुंच रहे हैं। कल एक महिला ने फांसी लगा ली क्योंकि उसकी नाबालिग बेटी का एक नग्न वीडियो एक नाबालिग लडक़े ने बना लिया था, और उसे चारों तरफ फैला दिया था। अपनी 13 बरस की बेटी का ऐसा वीडियो फैलने से तकलीफ पाती हुई मां ने खुदकुशी कर ली। कल की ही बिल्कुल आसपास की खबरें यह हैं कि एक नौजवान ने अपनी नाबालिग प्रेमिका को मिलने बुलाया था, और वहां पर उसकी सहमति से या उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथियों ने उस नाबालिग लडक़ी से बलात्कार किया। ऐसे 6 लोगों ने उससे बलात्कार करके वीडियो बनाया, बलात्कारियों में तीन नाबालिग भी हैं, और सभी पकड़े जा चुके हैं। पड़ोस के एक दूसरे शहर की खबर है कि एक ज्योतिषी मुकुंज त्रिपाठी ने पड़ोस की प्रेमिका के पति से छुटकारा पाने के लिए उसे मारा, लाश को पॉलीथीन की परतों में लपेटा, और अपने मकान की रसोई में पांच फीट गड्ढा खोदकर दफन कर दिया, अब पांच महीने बाद जाकर इस मामले का भांडाफोड़ हुआ है। इस प्रेमसंबंध की जानकारी पति को लग गई थी, और वह मिलने से मना करता था। चारों तरफ नाबालिगों के प्रेमसंबंध, देहसंबंध, शादीशुदा लोगों के तरह-तरह के जायज और नाजायज संबंध इतने खून-खराबे तक पहुंच रहे हैं कि हैरानी यह होती है कि अगर किसी के मन में सचमुच ही प्रेम है, तो क्या वे इतनी रफ्तार से ब्लैकमेलर और हत्यारे, या बलात्कारी हो सकते हैं?
दरअसल समाज इन मामलों से पूरी तरह बेफिक्र है। लोग इसे पुलिस और अदालत का मामला मानकर अनदेखा कर देते हैं, कि बाकी लोगों को भला इससे क्या लेना-देना? लेकिन जब समाज में ऐसी घटनाएं बढ़ती चलती हैं, तो यह भी समझने की जरूरत रहती है कि बलात्कार, कत्ल, और खुदकुशी से नीचे भी कई ऐसे किस्म की हिंसा रहती है जो कि पुलिस रिकॉर्ड और खबरों में नहीं आ पातीं। जिन परिवारों में जायज और नाजायज संबंधों को लेकर तनाव चलते रहता है, वहां पर बच्चों पर इसका कैसा असर पड़ता है, जिन लोगों को इसकी जानकारी रहती है, उन पर कैसा असर पड़ता है? ये मामले पुलिस का सामान बनने के पहले ही समाजशास्त्रीय अध्ययन का मुद्दा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और आज मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की मेहरबानी से किशोर-किशोरियां भी तरह-तरह के रिश्तों में उलझ रहे हैं, और तात्कालिक भरोसे के चलते कई तरह के फोटो-वीडियो में शामिल हो जाते हैं, जो कि बाद में ब्लैकमेलिंग या बदला लेने के लिए फैला दिए जाते हैं, और बहुत सी जिंदगियां खत्म करते हैं।
हर दिन इस छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ में दर्जन भर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें किसी नाबालिग को शादी का झांसा देकर उससे बलात्कार का जुर्म दर्ज हुआ है, या गिरफ्तारी हुई है। अब नाबालिग लड़कियों को शादी की उम्मीद में किसी से देहसंबंध बनाने की ऐसी कितनी जरूरत होनी चाहिए? शादी की ऐसी हड़बड़ी भी क्यों होनी चाहिए? बहुत से मामलों में ऐसा भी लगता है कि नाबालिग लडक़ी अपनी मर्जी से ऐसे संबंध बनाती है, लेकिन कानूनी रूप से उसकी सहमति की कोई कीमत नहीं रहती है, और बाद में शादी न होते दिखने पर बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई जाती है। सवाल यह भी उठता है कि एक नाबालिग लडक़ी की शादी हो कैसे सकती थी? लडक़े-लड़कियों को उनके बदन, सेक्स, वीडियो के खतरे, और शादी की उम्मीद के बहुत ही कमजोर होने की हकीकत का पता क्यों नहीं होता? सच तो यह है कि हिन्दुस्तान में मां-बाप, स्कूल-कॉलेज, या समाज लडक़े-लड़कियों के प्रेम और देहसंबंध की उम्र आ जाने के बाद भी उनसे जिंदगी की हकीकत की कोई चर्चा करना नहीं चाहते। नतीजा यह होता है कि वे सेक्स से होने वाली बीमारियों के खतरों से भी नावाकिफ रहते हैं, गर्भ का खतरा भी समझ नहीं पड़ता है, और अपने सेक्स-वीडियो बनवाते हुए उन्हें प्रेमी से अंतरंगता के अलावा कुछ नहीं दिखता है। नतीजा यह होता है कि अपनी कोई भी उम्मीद पूरी न होने पर शादी का वायदा करके बलात्कार करने की रिपोर्ट लिखा दी जाती है, जिसके तहत सामाजिक दबाव बनाना, या सजा दिलवाना कुछ आसान रहता है।
हिन्दुस्तान में शादीशुदा लोगों के विवाहेत्तर संबंधों को कई बार हिंसा तक पहुंचते देखा जाता है। शादी को एक किस्म से पूरी जिंदगी का रिश्ता मान लिया जाता है, और तलाक को एक सामाजिक धब्बा। नतीजा यह होता है कि लोग अनचाहे या नापसंद हो चुके रिश्तों को ढोते हैं, और अपने तन-मन की तसल्ली के लिए कहीं और रिश्ता बना लेते हैं। इसके मुकाबले उन देशों में हिंसा कम होती है जहां पर लोग आसानी से बिना शादी साथ रहते हैं, बिना शादी बच्चे पैदा कर लेते हैं, शादी के बाद तलाक भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहता है, और तलाकशुदा लोग दूसरी शादियां आसानी से कर लेते हैं। हिन्दुस्तान में इनमें से किसी भी चीज के लिए सामाजिक बर्दाश्त नहीं है, और लोग ऐसे घोषित विकल्पों के बजाय अघोषित नाजायज विकल्प ढूंढते रहते हैं, जिसकी वजह से हिंसा कुछ अधिक होती है।
यह सिलसिला खत्म करने के लिए किशोरावस्था से पहले ही लडक़े-लड़कियों को प्रेम और देहसंबंधों के बारे में बतलाना होगा। कैसे रिश्ते कैसी जटिलता लेकर आते हैं, यह चर्चा भी करनी होगी। उन्हें दिमागी रूप से तैयार करना होगा कि वे किस सीमा से अधिक भरोसा किसी पर न करें। इसी तरह शादीशुदा जोड़ों के बीच अगर भरोसा खत्म हो चुका है, और बाहर रिश्ते बनाए जा रहे हैं, तो इसे या तो बर्दाश्त करना आना चाहिए, या फिर ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना। किसी भी तरह का खून-खराबा रिश्तों को खत्म नहीं करता है, वह आजादी खत्म करता है जो कि जेल में रहते हुए नसीब नहीं रहती है। दुनिया में कोई भी रिश्ते इंसान की सामाजिक आजादी खत्म करके जेल जाने लायक नहीं होते हैं। जब किसी को मारकर जेल जाना जरूरी लगे, तो ऐसे इंसान से मौजूदा रिश्तों को मारकर खुली दुनिया में ही आजादी पा लेनी चाहिए, और अपनी-अपनी मर्जी के रास्तों पर निकल पडऩा चाहिए। लगता है कि हिन्दुस्तानी समाज के अधिकतर हिस्से में किशोरावस्था से लेकर शादीशुदा लोगों तक में समझदारी की बहुत कमी है, और हिंसा की बड़ी अधिकता है, चाहे अपने बारे में, चाहे दूसरों के बारे में। और इसके साथ-साथ एक बात और, यहां के लोग सबसे अधिक भरोसे के रिश्तों में सबसे अधिक दगाबाज भी हैं, यही वजह है कि धोखा देने के साथ-साथ बदला लेने के लिए अच्छे दिनों के वीडियो इस तरह फैलाते हैं कि लोगों को शर्मिंदगी में जान दे देनी पड़े। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
तेलंगाना में पिछली बीआरएस सरकार के दौरान जो लोग मुख्यमंत्री के.चन्द्रशेखर राव के विरोधी या आलोचक लगते थे उसकी भारी खुफिया जासूसी करवाई जाती थी। और यह काम किसी निजी एजेंसी से करवाने के बजाय राज्य सरकार की खुफिया पुलिस ने ही किया था। अभी तेलंगाना के एक भूतपूर्व पुलिस अफसर ने पिछली सरकार के दौरान काम करते हुए की गई इस तरह की जासूसी की बहुत सी जानकारी जांच करने वालों को बताई है। यह जांच तेलंगाना में नई कांग्रेस सरकार आने के बाद शुरू हुई है क्योंकि पिछली सरकार के बारे में यह माना जा रहा था कि वह विरोधियों और विपक्षियों की जासूसी करवाती थी। पिछले साल भाजपा के एक नेता ने भी यह बयान दिया था, और अब कांग्रेस सरकार इसकी व्यापक जांच करवा रही है।
तेलंगाना के लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री केसीआर, और उनके मंत्री बेटे के.टी.रामाराव ने अपनी सत्ता के चलते हुए नेताओं, अफसरों के साथ-साथ उद्योगपतियों और फिल्मी सितारों तक के फोन टैप करवाए थे, या उनकी तरह-तरह से निगरानी करवाई थी। इन तमाम चीजों का राज्य की आंतरिक सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं था, और राजनीतिक हिसाब-किताब चुकता करने के साथ-साथ लोगों के कारोबारी राज जानकर उनसे वसूली और उगाही करने के लिए भी ऐसा किया गया था। यह भी चर्चा थी कि केसीआर ने जिन फिल्मी सितारों के फोन टैप करवाए थे, उनमें से कुछ के निजी जिंदगी के राज इस तत्कालीन मंत्री के हाथ लगे थे, और वहां से एक के जीवनसाथी तक यह बात पहुंची, और एक अभिनेत्री का तलाक भी इसी वजह से होने की चर्चा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बांदी संजय कुमार ने कल यह मांग की है कि केसीआर और उनके बेटे को फोन टैपिंग में गिरफ्तार किया जाए, और उनकी विधानसभा की सदस्यता को खत्म किया जाए। उन्होंने साथ-साथ यह भी मांग की कि राज्य की कांग्रेस सरकार इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को दे दे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसमें पर्याप्त तेजी नहीं दिखा रही है, जबकि गिरफ्तार किए गए एक भूतपूर्व पुलिस डीसीपी ने पर्याप्त सुबूतों वाली गवाही दी है।
ऐसी शिकायत अलग-अलग कई राज्य सरकारों के कार्यकाल में उठती रही है। छत्तीसगढ़ में जोगी को तो कुल तीन साल का कार्यकाल मिला था, और उस वक्त राज्य में खुफिया विभाग का ढांचा भी बहुत अच्छी तरह नहीं बन पाया था। लेकिन रमन सिंह के समय से ऐसी चर्चाएं रहती थीं कि अवैध रूप से खरीदी गई करोड़ों की एक मोबाइल फोन टैपिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें विरोधियों या विपक्षियों पर निगरानी रखी जाती है। यह बात कभी साबित नहीं हो पाई, लेकिन सत्ता के करीबी कुछ लोग ऐसी फोन टैपिंग से मिली जानकारी की ताकत का प्रदर्शन करते रहते थे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की पिछली सरकार के समय तो हालत यह थी कि सत्ता में जो लोग जरा भी मायने रखते थे वे सिर्फ आईफोन के फेसटाईम पर बात करते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि देश की खुफिया एजेंसियां भी उसमें घुसपैठ नहीं कर पाती हैं। जो लोग सैकड़ों-हजारों करोड़ रूपए के जुर्म में शामिल रहते थे, वे खुद, और अपने आसपास के लोगों के भी आईफोन हर महीने-दो महीने में बदलवाते चलते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत अर्जी के खिलाफ तर्क देते हुए ईडी ने बताया था कि शराब घोटाले के सुबूतों को छुपाने के लिए, नष्ट करने के लिए केजरीवाल और सत्ता के शराब से जुड़े 36 लोगों ने करीब 170 मोबाइल फोन नष्ट किए थे। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश सरकार के किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सिर्फ आईफोन पर ही बात हो पाती थी। राज्य के सत्तारूढ़ लोगों को केन्द्र की एजेंसियों से हैकिंग का खतरा रहता था, और राज्य के विपक्षी लोगों को भूपेश सरकार द्वारा फोन टैपिंग का डर रहता था। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान में केन्द्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर फोन टैप करने के जो अधिकार मिले हैं, उनका बड़ा बेजा इस्तेमाल होता है, और लोगों की निजता और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता खत्म होती है।
ऐसे में कोई हैरानी नहीं है कि भारत के लोगों को यह आशंका है कि केन्द्र की मोदी सरकार ने इजराइल के सबसे बदनाम, फौजी दर्जे के घुसपैठिया सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल अपने विपक्षी नेताओं, और चुनिंदा पत्रकारों पर कर रही है। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद जब एक अदालत ने एक कमेटी बनाई, और उसे जांच की, तो उसे जिन 29 लोगों ने अपने मोबाइल फोन जांच के लिए दिए थे, उनमें से किसी पर भी पेगासस स्पाईवेयर नहीं मिला था, लेकिन उनमें से पांच पर कुछ और संदिग्ध घुसपैठ मिली थी। आज देश भर में अपने आपको जो भी महत्वपूर्ण समझते हैं, वे लोग मोबाइल फोन के सिमकार्ड पर कोई संवेदनशील बात करना नहीं चाहते। वे अलग-अलग किस्म के इंटरनेट-आधारित फोनकॉल, और मैसेंजर एप्लीकेशनों का इस्तेमाल करते हैं, और मानकर चलते हैं कि सरकार उन पर आसानी से निगरानी नहीं रख पाएगी। लेकिन किसी गाड़ी की आवाजाही को ट्रैक करने के छोटे से, सिक्के सरीखे, उपकरण इतने आम हैं कि किसी के भी बैग में, कार या दूसरे सामान में उसे आसानी से सरकाया जा सकता है, और फिर अपने मोबाइल फोन के रास्ते उस पर निगरानी रखी जा सकती है। इसके अलावा किसी के घर, दफ्तर, या किसी और जगह पर खुफिया कैमरे या माइक्रोफोन बड़ी आसानी से लगाए जा सकते हैं, और लोगों की निजता अब तकरीबन खत्म सरीखी है। लोग किसी से मिलने के लिए जा सकते हैं, और वहां से निकलने के पहले उनकी टेबिल के नीचे माइक्रोफोन चिपकाकर निकल सकते हैं, जिसे कुछ दूसरी से मोबाइल फोन से सुना जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है।
सत्ता जब किसी की निगरानी पर उतारू हो जाती है, तो फिर उस देश के जज भी महफूज नहीं रह जाते। बहुत से देशों में यह माना जाता है कि सरकारें अपनी पसंद के फैसले पाने के लिए जजों पर निगरानी रखती हैं, और उनकी कमजोर नब्ज हाथ में आते ही उनसे मर्जी का काम करवाने लगती हैं। भारत के एक प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के बागी तेवरों वाले विधायकों पर नजर रखने के लिए उन्हें महंगे मोबाइल फोन का तोहफा दिया गया, और उसमें डाले गए स्पाईवेयर से उसकी बातचीत और उसके संदेश पहले से तय की गई किसी जगह पर पहुंचते रहे। चर्चा यह भी रहती है कि हिन्दुस्तान की कुछेक सरकारें जो खुद कई किस्म की हैकिंग नहीं कर पाती हैं, वे भी दुनिया के दूसरे बदनाम देशों के हैकरों को भाड़े पर लेकर उनसे अपने विरोधियों और आलोचकों की हैकिंग करवाती हैं, जो कि सरकार के काम तो आ जाती है, लेकिन उसकी तोहमत सरकार पर नहीं आती है।
आज जैसे-जैसे लोगों का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, और इंटरनेट या सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी बढ़ रही है, वैसे-वैसे वे नाजुक होते जा रहे हैं। डिजिटल उपकरण और इंटरनेट, ये दोनों मिलकर किसी का कुछ भी निजी नहीं रहने दे रहे हैं। ऐसे में भारत में सरकारों की निगरानी रखने की ताकत पर दुबारा गौर करने की जरूरत है। यह कानून बहुत पहले बना था, उस वक्त तारों से जुड़ा हुआ टेलीफोन ही रहता था। अब दुनिया बहुत बदल गई है, और अब लोग न चाहते हुए भी उपकरणों से घिरे रहते हैं। ऐसे में भारत में निगरानी रखने के कानून और उसके अमल को पारदर्शी बनाने की जरूरत है, ताकि विपक्ष, विरोधियों, और आलोचकों का शिकार करने के लिए इस कानून की बंदूक का इस्तेमाल न हो। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
पुणे में एक अरबपति बिल्डर के नाबालिग बेटे ने नशे में धुत्त, करोड़ों की कार को देर रात अंधाधुंध रफ्तार से चलाते हुए दो लोगों को मौके पर ही मार डाला था, उसे बचाने के लिए पूरी दुनिया जुट गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने किसी बड़े अफसर को इसकी खबर नहीं की। मौके पर भीड़ ने इस रईसजादे को पकड़ लिया था इसलिए उसे थाने तो ले जाना पड़ा लेकिन वहां उसकी पसंद का पीजा बुलाकर उसकी खातिरदारी की गई, दूसरी तरफ दूसरे प्रदेशों के जो दो लोग मारे गए थे उनकी तरफ से मौके के जो गवाह थाने पहुंचे थे, उनके साथ पुलिस ने बदसलूकी की थी। फिर जब किशोर न्यायालय में इस रईसजादे को पेश किया गया तो पल भर में जज ने जमानत दे दी, और सजा दी निबंध लिखने की। इसके अलावा इस लडक़े के नशे में होने की जांच के लिए पुणे के जिस मशहूर सरकारी अस्पताल में इसे ले जाया गया वहां इसके खून की जांच होनी थी, और उसमें यह नशे में नहीं पाया गया। अब पुलिस ने इस अस्पताल के फोरेंसिक विभाग के एचओडी सहित दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है कि उन्होंने इस लडक़े को बचाने के लिए इसके खून का नमूना कचरे में फेंक दिया, और किसी दूसरे मरीज के खून को इस लडक़े के नाम से लगा दिया। पुलिस का यह बदला यह रूख इस बात के बाद में हुआ है कि इस एक्सीडेंट को लेकर देश भर में भारी हंगामा चल रहा है, और पुलिस कार्रवाई पर जमकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह इस बात के बाद भी हुआ है कि किशोर न्यायालय के जज की दी गई जमानत अगले दिन खारिज करके इस लडक़े को सुधारगृह भेजा गया है। फिर मानो यह सब काफी न हो, यह खबर फैलाई गई कि कार की मोटरसाइकिल सवारों को मारी गई टक्कर के वक्त कार ड्राइवर चला रहा था, और यह नाबालिग लडक़ा साथ बैठा हुआ था। बाद में इस ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि किस तरह इस अरबपति परिवार में लडक़े का दादा ड्राइवर पर दबाव बना रहा था कि वह ऐसा झूठा बयान दे। नाबालिग बेटे को कार देने, दारू पीने के लिए क्रेडिट कार्ड देने, और बिना नंबर प्लेट की कार रखने पर इस लडक़े का बिल्डर-बाप भी गिरफ्तार हो चुका है। और अब ड्राइवर का अपहरण करके कैद करने, और उसे धमकाने और सुबूत नष्ट करने के आरोप में दादा भी गिरफ्तार हो गया है। यह तो मामला इतनी खबरों में आ गया है कि पुलिस को उन शराबखानों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी जब्त करनी पड़ी जिनमें यह नाबालिग रईसजादा अपने दोस्तों के साथ शराब पीते घूमते दिख रहा है।
इस पूरे सिलसिले को देखें तो साफ दिखता है कि एक पैसे वाले मुजरिम को बचाने के लिए हिन्दुस्तानी लोकतंत्र पूरे का पूरा टूट पड़ता है। अभी तो पर्दे के पीछे की कोशिशें सामने नहीं आई हैं, और हम तो सिर्फ जो कार्रवाई हो चुकी है उसके आधार पर यह फेहरिस्त सामने रख रहे हैं। अब देखा जाए तो पुलिस से लेकर अस्पताल के डॉक्टरों तक, और किशोर न्यायालय के जज तक जो रूख सामने आया है, उसमें मारे गए बेकसूर लोगों को कोई इंसाफ मिलने की गुंजाइश कहां दिखती है? यह तो मामला आगे चलेगा तो पता लगेगा कि जिन लोगों ने मौके पर इस लडक़े को गाड़ी चलाते पकड़ा था, उनमें से कुछ लोगों के बयान बदल जाएंगे, या फिर वे गायब भी हो जाएंगे, या कर दिए जाएंगे। हिन्दुस्तानी लोकतंत्र इस बुरी तरह भ्रष्ट है कि इस पर मुजरिमों को बच जाने का पूरा भरोसा हो सकता है, बेकसूरों के बचने की या इंसाफ पाने की गुंजाइश बड़ी कम रहती है। अभी तो सडक़ों पर इन मौतों को चार दिन ही गुजरे हैं, और इतने में ही इतने किस्म की साजिशें सामने आ गई हैं। अब जब आगे यह घटना खबरों से परे हो जाएगी, तब पता लगेगा कि एक-एक सुबूत को कैसे खरीदा जाएगा, डॉक्टर से पुलिस और अदालत तक की कार्रवाई में कौन-कौन से गड्ढे खड़े किए जाएंगे ताकि यह अरबपति मुजरिम निकल सके। और अभी तो एक-एक पेशी के दसियों लाख रूपए लेने वाले महंगे वकीलों का काम तो शुरू ही नहीं हुआ है, उनमें से तो इतने काबिल निकल सकते हैं कि वे अदालत में साबित कर दें कि महंगी कार को नुकसान पहुंचाने के एवज में, और इस नाबालिग लडक़े को बदनाम करने के जुर्म में दो मरने वाले लोगों के पंचतत्व को कैद सुनानी चाहिए। पता लगेगा कि महंगे वकील की मांग पर इन दोनों की अस्थियां विसर्जित करने के बजाय उन्हें दो घड़ों में उम्रकैद सुना दी जाएगी। शुरू से ही मुजरिम को बचाने की जो कोशिशें चालू हुई हैं, वे आगे चलकर उसे सजा से बचाने में कामयाब भी हो सकती हैं। इस मामले का आखिरी फैसला होने तक यह समझ पड़ेगा कि इसके रास्ते में कितने ईमानदार और कितने बेईमान लोग आए थे। देश में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को भी ऐसे मामले पढ़ाने चाहिए, और आईपीएस के लिए चुने गए लोगों को भी। और खोजी पत्रकारिता में अगर अब भी कुछ लोग दिलचस्पी रखते हैं जिनके अखबार या टीवी चैनल को ऐसे बिल्डरों के इश्तहारों की परवाह न हो, तो वे भी ऐसे मामलों से ये सीख सकते हैं कि रईसजादों की रिपोर्टिंग करने में कहां-कहां पर साजिश परखने का काम करना चाहिए।
ऐसा लगता है कि किसी मामले का एकदम से खबरों में आ जाना ही उस मामले में कुछ हद तक इंसाफ की गुंजाइश पैदा करता है। जहां कहीं भी अखबारनवीसी थोड़ी सी बाकी हो, वहां पर इसे जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खबरों ने ही इस मामले को पटरी से उतारने की अनगिनत साजिशों को अब तक नाकामयाब किया है। इस मामले से परे भी जहां-जहां बड़े लोग शामिल होते हैं, मोटी रकम का खेल रहता है, वहां पर मुजरिमों को बेगुनाह साबित करने के लिए कई बार तो किसी बेकसूर को भी फंसा दिया जाता है, ताकि लोगों का ध्यान पैसे वाले असल मुजरिमों की तरफ से हट जाए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
अमरीका के कैलीफोर्निया में एक आदमी के गायब होने पर पुलिस ने उसके बेटे को पकड़ा, और उसे अपने पिता की हत्या की बात कबूल करने के लिए मजबूर किया। उससे लगातार 17 घंटे तक पूछताछ की गई थी जो तभी बंद हुई जब उसने बाप को मारना मान लिया। उसके बाद पता लगा कि बाप मरा ही नहीं था, वह अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाकर रह रहा था, और पुलिस ने केस हल करने के नाम पर इस आदमी को पकडक़र मुजरिम साबित कर दिया था। अब कैलीफोर्निया की अदालत ने पुलिस पर 8 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है कि उसने मानसिक प्रताडऩा से इस नौजवान से यह बयान हासिल कर लिया था, और इसके लिए पुलिस ने कई किस्म की प्रताडऩा-तकनीकें इस्तेमाल की थीं जिनमें उसके चहेते कुत्ते को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी शामिल थी। अदालत में बेगुनाही साबित होने के बाद पुलिस ने उससे नगद हर्जाना देने का समझौता किया, और अमरीकी कानून के मुताबिक इस पर अदालती मुहर लगी।
हिन्दुस्तान में इस तरह के मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है, और बहुत गरीब, और बहुत बेसहारा लोग झूठे मामलों में फंसा दिए जाते हैं, लेकिन बरसों तक चले मुकदमे के बाद जब वे छूटते हैं, तो भी उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिल पाता है जबकि उनकी खासी जिंदगी का नुकसान हो चुका रहता है। भारत में भी ऐसे मामलों में मुआवजे का प्रावधान करना चाहिए क्योंकि गरीबों की जिंदगी का खोया हुआ हिस्सा उनके परिवार को तोड़ देने वाला भी रहता है, और बहुत से परिवार ऐसे रहते हैं जो फर्जी मामलों में फंसाए गए उनके किसी सदस्य की कमाई पर ही जिंदा रहते हैं। भारत में पुलिस की गलती या गलत काम से अगर ऐसा होगा, तो उसके लिए मुआवजा कहां से आएगा, यह एक सवाल उठ खड़ा हो सकता है, लेकिन यह सरकार के सोचने की बात है कि वह अदालती दावों के निपटारे के लिए अपनी एजेंसियों को कोई बीमा मुहैया कराए, या किसी और तरीके से ऐसे मुआवजे का इंतजाम करे, लेकिन ऐसे प्रावधान के बिना सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा। दिक्कत यह है कि भारत में न्याय प्रक्रिया का बहुत सा हिस्सा इस कदर भ्रष्ट है कि जिन मामलों में बीमा कंपनियों को कोई निपटारा करना पड़ता है, उनमें भी अधिक बड़ा दावा न देना पड़े, इसके लिए कंपनियां कई तरह से रिश्वत भी देने लगती हैं। लेकिन एक विचार की तरह भारत के तमाम तबकों के सामने इस पर बात होनी चाहिए कि झूठी मुकदमेबाजी के शिकार गरीबों को कैसे इंसाफ और मुआवजा दिलाया जा सकता है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय की सरकार सडक़ों पर खुले घूमते गाय, सांड, और बछड़े-बछिया के लिए गौवंश अभ्यारण्य बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से इसकी घोषणा हुई है, और कहा गया है कि इससे सडक़ों पर भूखे-प्यासे भटकते, और घूरों पर कचरा या प्लास्टिक खाते गौवंशी मवेशियों की हालत सुधर सकेगी। सरकार अगर तय कर लेगी, तो वह अपनी गाय-समर्थक राजनीतिक नीति के मुताबिक भी इस काम को अच्छे से कर सकती है। और यह काम आज की एक बहुत बड़ी जरूरत भी है। आज देश भर में बहुत से, या अधिकतर प्रदेशों में गौवंश को मारने पर कानूनी रोक लगी हुई है। भाजपा और उसके समर्थक हिन्दूवादी संगठनों के बीच गाय को बूचडख़ाने जाने से रोकना इतना बड़ा मुद्दा है कि इस चक्कर में देश भर में जगह-जगह पर बेकसूर मवेशी-व्यापारी भी मारे गए हैं कि वे गायों को बूचडख़ाने ले जा रहे हैं। बहुत से प्रदेशों ने मवेशियों को लाने ले जाने के खिलाफ कड़े कानून बना लिए हैं, और इन्हें लागू करने के नाम पर सडक़ों पर अराजकता और गुंडागर्दी करने वाले संगठन भी सत्ता की मेहरबानी से लैस रहते हैं। देश भर से कई इतनी हिंसक घटनाएं सामने आई हैं कि उनसे हिन्दुस्तान की एक बड़ी खराब तस्वीर दुनिया भर में बनी है। दूसरी तरफ गाय से जुड़ी हुई कोई भी बात देश के अधिकतर हिस्से में आनन-फानन हिन्दू-मुस्लिम तनाव का सामान भी बन जाती है, इसलिए गायों को संभालकर रखना अपने प्रदेश की शांति को संभालकर रखने सरीखा है।
जब से देश भर में गायों और गौवंश के बाकी जानवरों को काटने पर कानूनी और गैरकानूनी दोनों किस्म की रोक बढ़ी है, तब से ये जानवर तरह-तरह की सामाजिक और आर्थिक समस्या भी बनते जा रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और अधिकतर खेत बिना किसी बाढ़ के होते हैं, और ऐसे में अगर गांव-शहर में ये जानवर बढ़ते ही चले जाएंगे, तो कहीं न कहीं, कुछ न कुछ तो खाएंगे। नतीजा यह हो रहा है कि उत्तर भारत के बहुत से प्रदेशों में खेतों को चर जाने वाले जानवर एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान खड़ा कर रहे हैं, और इनकी वजह से बहुत किस्म के लड़ाई-झगड़े भी बढ़ते चल रहे हैं। उत्तरप्रदेश ऐसी घटनाओं को लगातार दर्ज कर रहा है। महाराष्ट्र की खबरें हैं कि वहां पर किसान पुराने बैलों को बेचकर उस दाम से एक नया बैल ले लेता था, लेकिन अब यह जुर्म हो चुका है, इसलिए बूढ़े बैल किसान पर बोझ बने बैठे हैं, और किसान न तो उन्हें भूखे मरने दे पा रहा है, न ही उसके पास उन्हें खिलाने को कुछ है। नतीजा यह हो रहा है कि परंपरागत कृषि अर्थव्यवस्था में बूढ़े जानवरों से मुक्ति पा लेने का जो तरीका था, वह नए जानवर पाने में भी काम आता था, लेकिन अब वह सब एक जुर्म में गिनाने लगा है, इसलिए किसान पर दिक्कत और खतरा दोनों बढ़ गए हैं।
छत्तीसगढ़ में ऐसे अनगिनत मामले हुए हैं जब तेज रफ्तार हाईवे पर, या शहरों के भीतर भी सडक़ों पर जानवर रहते हैं, और बारिश में या रात-बिरात वे दिखते नहीं हैं, और उनसे टकराकर बहुत से इंसानों की भी मौत होती है। प्रदेश की पिछली भूपेश बघेल सरकार ने गांवों में गौठान खोलकर इन जानवरों को दिन भर वहां रखने की योजना बनाई थी, लेकिन उसका गांवों पर चाहे जो भी असर हुआ हो, उसका शहरों तक विस्तार नहीं हुआ था, और शहर ऐसे नामालिक जानवरों से बहुत बुरी तरह परेशान हैं। इसलिए अगर सडक़ों और शहरों से इन जानवरों को स्थाई रूप से हटाकर किसी छायादार, पानी वाले इलाके में इनके लिए कोई डेरा बनाया जा सके, तो उससे ही सरकार की गौरक्षा की नीयत पूरी हो पाएगी, और इन जानवरों के साथ-साथ इंसानों को भी राहत मिलेगी। आज जानवरों की वजह से ट्रैफिक में जितनी बाधा आती है, उससे भी कुल मिलाकर तो रफ्तार घटती है, प्रदूषण बढ़ता है, और लोगों का वक्त भी जाया होता है, हादसों में बहुत सी जिंदगियां भी जाती हैं। इसलिए यह फैसला जानवर और इंसान, सडक़ का ट्रैफिक, और शहरों में सुरक्षित जिंदगी सबके हित का है। लेकिन जैसा कि किसी भी सरकारी योजना में होता है, योजना की कामयाबी उसके अमल में होती है। देखते हैं इस पर अमल में कितनी कामयाबी मिलती है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
इन दिनों नाबालिगों के बीच दूसरों के साथ हिंसा, और आत्मघाती हिंसा, इन दोनों ही मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। जुर्म करने के मामले में बहुत से नाबालिग बच्चे या किशोर बड़ी रफ्तार से आगे बढ़े हैं, और भारतीय समाज है कि इस रूख को अनदेखा कर रहा है। अब कल की ही घटना है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक गांव में रहने वाले 11 बरस के बच्चे ने नाना-नानी के घर से 21 सौ रूपए निकाल लिए थे, इस पर उसे डांटा गया, और उसने गांव की ही स्कूल में जाकर फांसी लगा ली। ऐसा कई मामलों में हुआ है, कहीं भाई-बहन का मोबाइल फोन को लेकर झगड़ा हुआ, और किसी एक ने फांसी लगा ली, या दूसरे का कत्ल कर दिया। कुछ ऐसे मामले पिछले महीनों में सामने आए हैं जिसमें घर के भीतर ही बच्चों ने कोई पोर्न फिल्म देखकर परिवार की ही लडक़ी से बलात्कार किया। पसंद का मोबाइल फोन न मिलने पर खुदकुशी करने वाले कुछ बच्चे भी दर्ज हुए हैं। अब इन मामलों में, परिवार, समाज, और सरकार क्या कर सकते हैं? या तो आज की तरह इसे अनदेखा कर सकते हैं, और इसे पुलिस, अदालत, जेल, या सुधारगृह का मामला मानकर भूल सकते हैं, या फिर आगे ऐसी वारदातों में कमी आए, उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं।
दुनिया में वही देश सभ्य और विकसित माने जा सकते हैं जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। और जब बच्चे आत्मघाती हो रहे हैं, तो यह जाहिर है कि उनके भीतर तनाव, निराशा, कुंठा का स्तर बहुत बढ़ गया है। छोटे-छोटे बच्चे अगर अपनी किसी गलती, या गलत काम पर जरा सी डांट भी सुनने को तैयार नहीं हैं, तो यह उनके भीतर सहनशीलता की कमी है। हो सकता है कि परिवार के बुजुर्ग लोगों का बोलने का लहजा किसी मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के पैमानों पर ठीक न बैठे, लेकिन सदियों से भारतीय समाज जिस तरह की व्यवस्था पर चलते आ रहा है, उसमें अभी एक-दो दशक पहले तक बच्चों के तनाव का यह हाल नहीं था। अब तो एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब हत्या या आत्महत्या की खबरों में नाबालिगों का जिक्र न हो। और इस ताजा मामले में तो तीसरी कक्षा के बच्चे ने घर की ही डांट से खुदकुशी कर ली, तो फिर परिवार क्या बच्चों के पैसे चुराने पर भी उन्हें नहीं डांटेंगे? पिछली कई घटनाओं में बच्चों ने इम्तिहान के बीच भी मोबाइल पर खेल खेलने से रोकने पर खुदकुशी करना तय कर लिया, अब भला कौन से ऐसे मां-बाप होंगे जो कि इम्तिहान के दौरान भी बच्चों को पढऩे के लिए न बोलें?
हम पहले भी इस तरह की आत्मघाती, या दूसरों के खिलाफ नाबालिग हिंसा के मामलों में, या परिवार के भीतर-भीतर दूसरे लोगों के भी एक-दूसरे को मार डालने के मामलों में यह कहते आए हैं कि भारत में अधिक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की जरूरत है। यहां पर दरअसल धार्मिक आस्था, और अंधविश्वास की वजह से मनोविज्ञान को कोई महत्व दिया नहीं जाता। लोग ताबीज को अधिक असरदार मानते हैं, झाड़-फूंक के वीडियो दिखते हैं, और कई किस्म के बाबा देश के अलग-अलग इलाकों में मनोरोगियों के साथ तरह-तरह की नाटकीय हरकतें करते हुए उन पर से भूत-प्रेत हटाने का पाखंड करते दिखते हैं। जब देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ताबीज और झाड़-फूंक से या किसी बाबा के हाथों पिटकर ठीक होने को तैयार बैठा है, तो सरकार को भी मनोचिकित्सकों और परामर्शदाताओं की जरूरत नहीं लगती है। आज देश के शहरी इलाकों में जहां पर ये विशेषज्ञ मौजूद भी हैं, वहां भी लोग धड़ल्ले से पाखंडियों के पास जाते हैं, और अंधविश्वास से आस्था-चिकित्सा पाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के ऐसे देशों के लिए आस्था-चिकित्सा को मान्यता दी है जहां पर डॉक्टरी सहूलियत हासिल नहीं है, लेकिन अपने आपको विकसित देश करार देने वाला हिन्दुस्तान भी आज 21वीं सदी में जादू-टोने और तांत्रिकों के सहारे मनोरोगियों का इलाज करते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं करता है।
हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम बहुत बार यह लिख चुके हैं कि देश में मनोवैज्ञानिक पढ़ाई के माध्यम से परामर्शदाता तैयार करने का काम करना चाहिए, और इसके लिए विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर कोर्स चलाने चाहिए, और जिस तरह स्कूली शिक्षकों के लिए बीएड जैसे कोर्स अनिवार्य किए गए हैं, उसी तरह उनके लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श का कोर्स भी जरूरी करना चाहिए, और धीरे-धीरे सरकार हर स्कूल में ऐसे कम से कम एक-दो शिक्षक नियुक्त कर सकती है जिससे हिंसा के स्तर से नीचे की परेशानी वाले बच्चों को भी मदद मिल सके। जिन बच्चों का बचपन मानसिक जख्मों से गुजरा रहता है, वे बड़े होने पर भी मानसिक समस्याओं के शिकार रहते हैं। इसलिए अगर उन्हें बचपन में ही परेशानियों से मुक्ति मिल सके, तो उनका बचपन भी अधिक स्वस्थ रहेगा, और बड़े होने पर भी वे बेहतर दिल-दिमाग वाले होंगे। लेकिन पता नहीं क्यों सरकारों को मनोवैज्ञानिक परामर्श का महत्व नहीं आता, और न ही उसकी जरूरत लगती है। परामर्श की पढ़ाई को एक अतिरिक्त योग्यता मानकर ऐसे शिक्षकों को कोई अतिरिक्त भत्ता भी दिया जा सकता है, और स्कूली बच्चों के साथ-साथ उनके मां-बाप की उलझनें भी सुलझाई जा सकती हैं, क्योंकि परिवारों के तनाव सुलझे बिना बच्चों को पूरी तरह तनावमुक्त नहीं किया जा सकता।
अभी तो समाज के अधिकतर बच्चों को हासिल सरकारी स्कूलों में बुनियादी पढ़ाई का भी हाल बहुत खराब है, खेलकूद की गुंजाइश नहीं सरीखी है, ऐसे में परामर्श की सुविधा की हमारी सलाह हो सकता है कि हकीकत से वाकिफ लोगों को एक बकवास लगे। लेकिन हमारा मानना है कि मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं को अलग से नियुक्त न भी करके अगर शिक्षकों में से ही लोगों को एक या दो साल के कोर्स करवाए जाएं, तो भी बिना किसी लंबे-चौड़े खर्च के बच्चों की मदद हो सकती है, और आम हिन्दुस्तानियों के लिए स्कूलों में ऐसी मदद मिलना ही उनकी जरूरत पूरी कर सकता है। जिस रफ्तार से बच्चों में जुर्म बढ़ रहे हैं, हिंसा और सेक्स में बढ़ोत्तरी हो रही है, उन सबको एक-एक घटना मानकर उस पर पुलिस कार्रवाई से बीमार समाज का कोई भी इलाज नहीं हो रहा, इसे एक बड़ी समस्या मानने के बाद ही उसके समाधान का सफर शुरू हो सकेगा।
पश्चिम के तीन देशों ने अभी फिलीस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। इजराइल फिलीस्तीन पर जैसे भयानक हमले कर रहा है, और अब तक शायद उसने 35 हजार लोगों को मार डाला है, और दसियों लाख लोगों को भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिया है, उसके खिलाफ दुनिया में जगह-जगह पर जनमत उठ खड़ा हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा है, और उसने फिलीस्तीनियों को इस तरह से मार डालने को एक नस्ल का जनसंहार करार दिया है। इस तर्क के आधार पर इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए वारंट की मांग भी की है। अभी यह मामला साफ नहीं है कि इस अदालत का आदेश इजराइल पर किस तरह से लागू होगा, लेकिन इस बीच स्पेन, आयरलैंड, और नॉर्वे, योरप के इन तीन देशों ने फिलीस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है जो कि मोटेतौर पर एक प्रतीकात्मक कार्रवाई है। और जैसी कि उम्मीद की जा सकती थी, इजराइल ने इन तीनों देशों को कहा है कि उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उसने इन देशों से अपनी राजदूत भी बुला लिए हैं। इजराइल का तर्क है कि फिलीस्तीन पर काबिज आतंकी संगठन हमास ने जिस तरह इजराइल पर हमला किया था, बेकसूर नागरिकों को मारा, और महिलाओं सहित सैकड़ों नागरिकों का अपहरण किया, उसे देखते हुए फिलीस्तीन को मान्यता देने का मतलब आतंक का हौसला बुलंद करना है। जो भी हो, एक-एक करके दुनिया के बहुत से देश अमरीकी दादागिरी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और फिलीस्तीन का साथ दे रहे हैं, इजराइल के खिलाफ अलग-अलग मंचों पर आवाज उठा रहे हैं। खबर बताती है कि कोलंबिया ने फिलीस्तीन में दूतावास खोलने का ऐलान किया है, और कई देश फिलीस्तीनियों की मानवीय मदद रोकने के लिए इजराइल के खिलाफ कई तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सबसे बेईमान देश अमरीका साबित हो रहा है जो इजराइल को बीच-बीच में जुबानी नसीहत देता है, और फिर उसे हथियारों की खेप और भेज देता है ताकि वह बेकसूर फिलीस्तीनियों को थोक में मार सके।
दुनिया की व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की जैसी भूमिका रखी गई थी, वह फिलीस्तीनियों पर जुर्म के मामले में पूरी तरह से बेअसर और बोगस साबित हुई है क्योंकि अवैध कब्जा करने वाला हमलावर और हत्यारा देश इजराइल जब कभी संयुक्त राष्ट्र में परेशानी में पडऩे वाला रहता है, अमरीका उसे बचाने के लिए वीटो नाम के विशेषाधिकार का इस्तेमाल करता है। अमरीकी शह पर ही इजराइल लगातार फिलीस्तीनी जमीन पर काबिज होते चल रहा है, और इस बार उसने हमास के आतंकी हमले का जवाब देते हुए फिलीस्तीन के गाजा शहर को दुनिया का सबसे बड़ा मलबे का ढेर बना दिया है, और फिलीस्तीनियों को बेघर, फिलीस्तीन को दुनिया का एक सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना दिया है। हिटलर ने अपने वक्त जर्मनी में यहूदियों के साथ जो कुछ किया था, ठीक वही इजराइल फिलीस्तीनियों के साथ कर रहा है। जो नस्लवादी जनसंहार हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ किया था, वही का वही इजराइल ने गाजा में कर दिखाया है, और अब वहां की बाकी जगह पर कैसे इजराइलियों को बसाया जा सकता है, कैसे फिलीस्तीनियों को उनके देश से बेदखल किया जा सकता है, यह गुंडागर्दी चल रही है। इसमें अमरीका एक तरफ फिलीस्तीनियों के लिए राहत की शक्ल में खाना भेजने का नाटक कर रहा है, और फिलीस्तीनियों पर बरसाने के लिए इजराइल को बमों का जखीरा भी भेज रहा है। अमरीका के इस पाखंड के खिलाफ खुद अमरीकी विश्वविद्यालयों में छात्रों का एक बड़ा आंदोलन चला है, और ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर में होने वाले अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में फिलीस्तीन का मुद्दा नौजवान वोटरों को प्रभावित कर सकता है।
जब दुनिया में बड़ी-बड़ी ताकतें इस हद तक खेमेबाजी में रहती हैं, तब छोटे-छोटे देश अपनी मिसाल पेश करके एक नैतिक दबाव तो खड़ा करते ही हैं। जिस योरप में अमरीकी पिट्ठू ब्रिटेन इजराइल को बचाने अपनी फौज भेजता है, उसी योरप में तीन देशों ने ब्रिटेन को आईना दिखाया है। यह एक ऐतिहासिक मौका है, और ऐसे वक्त दुनिया के किन देशों ने किसका साथ दिया, किसने आंखें फेर लीं, और किसने जनसंहार में मदद की, इन सबका नाम इतिहास में अच्छी तरह दर्ज होगा। हिटलर का इतिहास दर्ज होना अब तक खत्म नहीं हुआ है, जबकि उसके जनसंहार की पौन सदी हो चुकी है। आज भी जगह-जगह हिटलरी नस्लवादी सामूहिक हत्याओं के गवाह या उनसे बच निकले लोग कहीं-कहीं सामने आते हैं, और मरने के पहले उनके बयानों की शक्ल में हिटलर का इतिहास दर्ज होते चलता है। दुनिया इस बात की भी गवाह है कि हिटलर का अपना देश जर्मनी उसके खून-खराबे को लेकर इस किस्म की ऐतिहासिक शर्मिंदगी से डूबे रहता है कि वहां आज हिटलर का नाम एक कलंक है, और लोग अपने कुत्तों का नाम भी हिटलर नहीं रखते। इजराइल ने अपने इतिहास की आज तक की सबसे कट्टर सरकार देखी है, और वह सरकार भ्रष्टाचार के मामले भुगत रहे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अगुवाई में सबसे अधिक नस्लवादी जनसंहार कर रही है। फिलीस्तीनियों की नस्ल को ही खत्म कर देना आज के इजराइल का मकसद है, वह हिटलर के ही अंदाज में एक नस्ल को खत्म कर रहा है, लेकिन उससे आगे बढक़र वह एक देश को भी खत्म कर रहा है, और उस पर पूरी तरह कब्जा करके अपने नागरिकों को वहां बसा रहा है। आज दुनिया में बहुत से प्रगतिशील और उदारवादी यहूदी-इजराइली ऐसे हैं जो कि नेतन्याहू-सरकार के फैसलों के खिलाफ खड़े हैं, और अमरीका में जगह-जगह होने वाले प्रदर्शनों में वे इजराइल के खिलाफ और फिलीस्तीन के साथ खड़े रहते हैं।
किसी देश का अपने आपमें महान लोकतंत्र बनना उसकी अपनी आर्थिक और फौजी ताकत पर निर्भर नहीं करता। उस देश में भीतर और बाकी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए, इंसाफ के लिए उस देश का क्या रूख है, इसी से उस देश की साख बनती है, और उसके मुखिया की इज्जत। आज दुनिया के जो देश फिलीस्तीन को एक मुस्लिम देश मानकर इस बात पर खुश हो रहे हैं कि मुस्लिम मारे जा रहे हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि दुनिया के एक हिस्से में इतिहास की सबसे बड़ी बेइंसाफी चलती रहे, तो दुनिया के बाकी हिस्सों में भी अमन-चैन कायम नहीं रह सकता। आज दुनिया के बड़े देश अपनी सरहदों से परे भी धरती के अलग-अलग हिस्सों में अपने फौजी ताकत के अड्डे बनाने में लगे रहते हैं, और आज तो आर्थिक साम्राज्य भी एक किस्म की फौजी ताकत ही है। ऐसे में इजराइली हत्यारी-सरकार का साथ देने के लिए चुप रहने वाले देशों का भी नाम दर्ज हो रहा है।
छत्तीसगढ़ में नई भाजपा सरकार ने नक्सल मोर्चे पर जो पहल की है, वह देखने लायक है। उपमुख्यमंत्री और प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा पहली बार विधायक और मंत्री बने हैं, और उन्होंने अपने शुरूआती इंटरव्यू से ही नक्सलियों से शांतिवार्ता का इरादा जाहिर किया था। बाद में वे लगातार कुछ और मौकों पर भी इस बात को दुहराते रहे, और यह भी कहते रहे कि नक्सली अगर वीडियो कॉल पर भी बात करना चाहते हैं, तो वे इसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन इसके साथ-साथ बस्तर के नक्सल मोर्चे पर लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी जारी है, और इस सरकार ने पिछले कुछ महीनों में ही सौ से अधिक नक्सली मारने में कामयाबी पाई है। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि इतनी मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों को बहुत कम नुकसान पहुंचा है। यह बात जरूर है कि एक मुठभेड़ ऐसी हुई है जिसमें चार बेकसूर ग्रामीणों को मुठभेड़ के बीच गोलियां लगी और वे मारे गए, लेकिन पुलिस उन्हें नक्सली बता रही है। नक्सली अपने लोगों के मारे जाने पर खुलकर इस बात को मंजूर करते आए हैं कि मारे गए लोग उनके थे, लेकिन अभी 30 अप्रैल को हुई मुठभेड़ में मारे गए लोगों में चार को नक्सलियों ने अपना न होना बताया है, और अनगिनत मीडिया कैमरों के सामने इन चारों के परिवार ने भी यही बात कही है। अगर राज्य सरकार सचमुच ही नक्सल मोर्चे को शांत करना चाहती है, तो मुठभेड़ में नक्सलियों को खत्म करने के साथ-साथ उसे बेकसूर ग्रामीणों की मौत पर सच को मंजूर भी करना होगा, और इनके परिवारों को मुआवजा भी देना होगा। आज किसी बेकसूर आदिवासी को नक्सली करार दे देने से सरकार उनके परिवार को कोई भी मुआवजा देने से बच जाती है। ऐसी नौबत में लोगों का भरोसा सरकार पर नहीं रहेगा, और नक्सलियों से बातचीत में भी ऐसी मौतें एक रोड़ा रहेंगी।
आज इस मुद्दे पर लिखने की जरूरत इसलिए लग रही है कि गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि राज्य में नक्सल-पुनर्वास नीति फिर से बनाई जा रही है, और इसके लिए राज्य सरकार ने इंटरनेट पर तमाम लोगों से राय मांगी है कि पुनर्वास कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नक्सली भी अपने सुझाव दे सकते हैं कि वे किन शर्तों पर आत्मसमर्पण करके लोकतंत्र की मूलधारा में आना चाहेंगे। इसके कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि नक्सली प्रदेश के जिस शहर में पुनर्वास चाहेंगे, उन्हें वहां मकान दिया जाएगा। यह बात देश में पहली बार ही हो रही है कि नक्सलियों से भी यह पूछा जा रहा है कि वे किस तरह का पुनर्वास चाहते हैं। नए गृहमंत्री का यह रूख पिछली कई सरकारों के रूख से बिल्कुल ही अलग है। राज्य ने अब तक चार मुख्यमंत्री देखे हैं, और किसी भी सरकार का रूख नक्सल पुनर्वास को लेकर, शांतिवार्ता को लेकर इतना सकारात्मक नहीं रहा है। अब यह एक अलग बात है कि यह सरकार अपनी इन घोषणाओं को लेकर सचमुच ही इतनी ईमानदार है, या इसके पीछे कोई राजनीति भी है। चूंकि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री लगातार एक सरीखी बात कर रहे हैं, और नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों की अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कामयाबी के बाद भी शांतिवार्ता की बात पर कायम हैं, इसलिए हम पहली नजर में इसे सरकार का ईमानदार रूख ही मान रहे हैं।
अब सवाल यह उठता है कि सरकार और नक्सलियों के बीच बातचीत की जमीन तैयार करने के लिए इन दोनों पक्षों से परे के लोग क्या कर सकते हैं? बस्तर का पिछले 25 बरस का इतिहास बताता है कि जब-जब वहां कोई अपहरण हुआ, या नक्सलियों और सरकार के बीच किसी भी तरह की अघोषित बातचीत की नौबत आई, ऐसे तमाम मौकों पर बस्तर में काम कर रहे पत्रकारों ने बड़ा योगदान दिया है। जब राज्य के एक आईएएस अफसर और नक्सल प्रभावित जिले सुकमा के कलेक्टर का अपहरण हुआ था, तब भी बातचीत का सिलसिला शुरू करवाने में और कलेक्टर की रिहाई में स्थानीय पत्रकार सक्रिय थे। राज्य में उस वक्त भाजपा की सरकार थी, और नक्सलियों और राज्य शासन दोनों की आम सहमति से कुछ अफसरों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक कमेटी बनी थी जिसकी कई बैठकें हुई थीं, और बहुत से बेकसूर आदिवासियों को छुड़वाने, उनके मुकदमे खत्म करवाने की शर्त पर इस आईएएस की रिहाई हुई थी। उस कमेटी का इस्तेमाल इस रिहाई के साथ ही खत्म कर दिया गया था, जबकि बातचीत जिस हद तक पहुंच गई थी, उसे नक्सल आंदोलन खत्म करने के लिए शांतिवार्ता में तब्दील किया जा सकता था। पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और उनके अफसरों ने, केन्द्र की मनमोहन सिंह सरकार ने, किसी ने भी उस बातचीत को शांतिवार्ता तक ले जाने की जहमत नहीं उठाई, वरना आज जिस तरह विष्णु देव साय की सरकार, और इसके गृहमंत्री विजय शर्मा लगातार शांतिवार्ता और नक्सल-पुनर्वास की बात जिस तरह से कर रहे हैं, वैसी बात अगर उस समय हुई होती तो हो सकता है कि उसके बाद से अब तक की हजारों नक्सलियों, सुरक्षा कर्मचारियों, और ग्रामीणों की मौत टल सकती थी।
खैर, जब जागे, तभी सबेरा। राज्य सरकार को इसी सक्रियता और गंभीरता से नक्सलियों से बातचीत की पहल जारी रखना चाहिए। हमारा मानना है कि दोनों ही पक्षों को बातचीत के लिए किसी तरह की शर्त नहीं रखना चाहिए, वरना पहले कभी-कभी इस बुनियादी बात पर ही शांतिवार्ता की चर्चा खत्म हो गई कि पहले बस्तर से सुरक्षा बलों को हटाया जाए, या पहले नक्सली अपने हथियार डालें। अब यह जाहिर है कि ये दोनों ही पक्ष अपना-अपना एजेंडा लेकर काम कर रहे हैं, और यह सिलसिला जारी रह सकता है, लेकिन साथ-साथ बातचीत की पहल भी शुरू हो सकती है। इसके लिए ऐसी नामुमकिन या नामंजूर बातों को नहीं उठाना चाहिए जिससे कि बात न हो सके। गृहमंत्री विजय शर्मा का यह मानना ठीक है कि सिर्फ मुठभेड़ से नक्सल समस्या हल नहीं हो सकती, और वे बड़े मौलिक तरीकों से इसे सुलझाने में लगे हैं, जो कि अपने किस्म की पहली ऐसी कोशिश है। आज जिन लोगों की इन दोनों तबकों से किसी तरह की बात होती है, उन्हें भी अपने रिश्तों और असर का इस्तेमाल बातचीत शुरू करवाने में करना चाहिए। इसमें कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, या पत्रकार हो सकते हैं। यही असली लोकतंत्र है जिसमें सरकार बंदूकों की अपनी तमाम ताकत, और अपने अधिकारों के बावजूद किसी हथियारबंद आंदोलन को खत्म करवाने के लिए बातचीत का सिलसिला भी शुरू करना चाहती है। आज नक्सलियों को भी चाहिए कि अपनी लोकतांत्रिक मांगों को लेकर वे सरकार के साथ बैठें, और हिंसा का रास्ता छोडऩे के लिए बातचीत शुरू करें। आज यह बात अच्छी तरह स्थापित और साबित हो चुकी है कि भारत की केन्द्र और राज्य की सरकारों की मिलीजुली ताकत के सामने किसी हथियारबंद आंदोलन के कामयाब होने की कोई संभावना नहीं है। इस हकीकत को समझते हुए नक्सलियों को आदिवासियों के हित में तमाम किस्म की लोकतांत्रिक मांगें सामने रखना चाहिए, और उन्हें लोकतंत्र की मूलधारा में जिस हद तक भी राजनीतिक भूमिका मंजूर हो, उसे करना चाहिए। हथियारबंद आंदोलनों का अब भारत जैसे देश के भीतर कोई भविष्य नहीं है। यह मौका देश की तमाम लोकतांत्रिक ताकतों की मध्यस्थता का भी है कि वे छत्तीसगढ़ सरकार और नक्सलियों के बीच बातचीत के लिए जमीन तैयार करें। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
‘छत्तीसगढ़’ अखबार के यूट्यूब चैनल ‘इंडिया-आजकल’ पर कल छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों के संचालक-एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मिलने वाले दाखिले के खिलाफ सामाजिक तनाव का जो जिक्र किया, वह स्तब्ध करने वाला था। अगर जिला अदालत के एक जज को यह मंजूर नहीं कि निजी स्कूल में उसके बच्चे के साथ उनकी काम वाली की बच्ची को भी दाखिला मिले, तो यह समाज में भेदभाव की एक गहरी और चौड़ी खाई बताता है। आमतौर पर लोग अपने मन की भेदभाव की भावनाओं को अपने तक सीमित रख लेते हैं, लेकिन जब लोग दूसरों के सामने खुलकर कहीं आरक्षण के खिलाफ, तो कहीं सरकारी योजनाओं में महिलाओं को मिलने वाली हिफाजत के खिलाफ बोलते हैं, तो लगता है कि 21वीं सदी में भी उनके भीतर पत्थरयुग की वह सोच जारी है जिसे लोकतंत्र छू भी नहीं गया था, क्योंकि लोकतंत्र उस वक्त आया ही नहीं था। इसी बातचीत में यह भी पता लगा कि छत्तीसगढ़ के कुछ नामी-गिरामी स्कूल फर्जी तरीके से अल्पसंख्यक स्कूल बन गए हैं ताकि उन्हें गरीब बच्चों को रियायती सरकारी फीस पर दाखिला न देना पड़े, और बिना नाम बताए उन्होंने एक ऐसी बड़ी स्कूल का जिक्र किया है जहां सरकारी योजना के तहत आरटीई में दाखिला पाने वाले गरीब बच्चों को अलग क्लास में बिठाकर अलग टीचर से पढ़वाया जाता है, और उनका यूनीफॉर्म भी अलग रखा जाता है। पैसेवालों के स्कूलों में इस तरह का भेदभाव बहुत हैरान तो नहीं करता, लेकिन कानून के खिलाफ जाकर वे ऐसा भेदभाव करेंगे, यह बात हैरान जरूर करती है। राजीव गुप्ता की कही ये बातें भी भयानक थी कि प्रदेश के कुछ सौ स्कूलों में से सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जो कोचिंग सेंटरों की मदद करने के लिए छात्र-छात्राओं का झूठा दाखिला दिखाते हैं, और उन्हें फर्जी हाजिरी देकर इम्तिहान में बैठने का रास्ता जुटा देते हैं। एक तरफ तो निजी स्कूलों में इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, और सरकार में बैठे लोगों को इन पर कार्रवाई शायद इसलिए नहीं सुहाती है कि सत्तारूढ़ लोगों के बच्चे महंगी कोचिंग पाने के लायक रहते हैं, पाते हैं, और इसलिए उनके मां-बाप के हित में यह नहीं रहता कि कोचिंग की व्यवस्था खत्म हो, और कोचिंगवंचित गरीब बच्चे भी सत्ता के संपन्न बच्चों की बराबरी से मुकाबले में आ जाए।

क्लिक करें और यह भी देखें : जज को अपनी घरेलू कामगार की बच्ची के साथ बेटा पढ़ाना मंजूर नहीं!
हिन्दुस्तान में महंगे कोचिंग सेंटरों का हाल यह है कि वे अपने खुद के डमी स्कूल चलाते हैं ताकि छात्र-छात्राओं को फर्जी हाजिरी दे सकें, और पूरे वक्त उन्हें कोचिंग सेंटरों में बिठा सकें। ऐसे ही दो डमी स्कूलों की मान्यता अभी छत्तीसगढ़ में सीबीएसई ने खत्म की है। इन पर निजी स्कूल संचालकों के एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता से कुछ सीधी बातें। लेकिन इसके अलावा शिक्षा के अधिकार का प्रदेश में क्या हाल है, यह जानना भी सनसनीखेज था, राजीव ने एक महंगे स्कूल और एक जज के बारे में जो बताया, वह चौंकाने वाला है! ‘छत्तीसगढ़’ अखबार के संपादक सुनील कुमार की राजीव गुप्ता से बातचीत।
आज ही छत्तीसगढ़ के अलग-अलग अखबारों में राज्य के स्कूलों का भयानक दर्जे का संगठित भ्रष्टाचार छपा है। एक प्रमुख अखबार ‘ दैनिक भास्कर’ की रिपोर्ट है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में डेढ़ लाख डुप्लीकेट छात्रों का दाखिला दिखाया गया है, जिससे सरकार को हर बरस 730 करोड़ का चूना लगाया जा रहा है। अभी एक सरकारी वेबसाईट पर डेटा अपडेट होने पर यह फर्जीवाड़ा पकड़ाया है। इसके पीछे वजहें चाहे जो हों, लेकिन सरकारी विभागों में कहीं फर्जी राशन कार्ड रहते हैं, कहीं स्कूली बच्चों की गिनती ज्यादा बताकर यूनीफॉर्म, मिड-डे-मिल, साइकिल, और बाकी सहूलियतों का पैसा खा-पी लिया जाता है। प्रदेश के एक दूसरे प्रमुख अखबार ‘नवभारत’ में भी एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि निजी स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिला पाने वाले गरीब बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ भी देते हैं, लेकिन स्कूल उनके न आने की जानकारी सरकार को नहीं देते, और उसकी फीस लेते रहते हैं। ये तमाम बातें निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों, इन दोनों में बड़े पैमाने पर चल रहे भ्रष्टाचार को बताती हैं।
इनके अलावा छत्तीसगढ़ की स्कूल शिक्षा में सरकारी स्कूलों का हाल बहुत खराब बताया जाता है, और वहां गरीब बच्चे दोपहर के भोजन के अलावा कम दिलचस्पी लेते हैं, और शिक्षकों को भी इससे सहूलियत रहती है कि बच्चे न आने या चले जाने के चक्कर में रहें, बहुत से जगहों पर शिक्षक नशे में स्कूल पहुंचते हैं, कुछ जगहों पर स्कूल में बैठकर नशा करते हैं, और छात्राओं से छेड़छाड़ के बहुत से मामले प्रदेश भर में जगह-जगह सामने आए हैं जिनमें कहीं हेडमास्टर, कहीं शिक्षक, कहीं हॉस्टल प्रभारी गिरफ्तार भी हुए हैं। यह बात राज्य बनने के समय से लगातार सामने आ रही है कि किस तरह स्कूलों की फर्नीचर खरीदी में 35 फीसदी से अधिक कमीशन का संगठित भ्रष्टाचार चलता है, और इससे कुछ ज्यादा ही कमीशन किताब खरीदी में लिया जाता है। जब भविष्य की बुनियाद को ही भ्रष्टाचार से जर्जर किया जा रहा है, तो अगली पीढ़ी किस तरह की तैयार होगी यह बात साफ है।
लोगों को याद होगा कि एक वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने यह फैसला दिया था कि तमाम नेता और बड़े अफसर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं ताकि स्कूलों की हालत सुधर सके। यह बात आई-गई हो गई, एक विचार के रूप में यह बात ठीक थी, लेकिन कानूनी रूप से यह फैसला कमजोर था क्योंकि किसी समाजवादी व्यवस्था में ही ऐसा करना मुमकिन था, न कि भारत जैसे पूंजीवादी-लोकतंत्र में। इसलिए हाईकोर्ट जज की इस जायज सोच पर भी कोई अमल नहीं हो पाया। लेकिन देश को अपनी शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था के बारे में यह सोचना चाहिए कि निजी और सरकारी स्कूलों के बीच एक लंबे फासले की वजह से इनके बच्चों के बीच आगे चलकर कोई बराबरी नहीं रह जाती। देश में वैसे भी एक दूसरी बहस चल रही है कि पढ़ाई को कुचल डालने वाली कोचिंग इंडस्ट्री के आतंक को कैसे घटाया जाए। यह इतना कमाई का कारोबार है कि इसने स्कूल शिक्षा के नाम पर परले दर्जे की बेईमानी कायम कर रखी है, और बड़े दाखिला इम्तिहानों की तैयारी करने वाले बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से एक किस्म से बरी कर दिया गया है। स्कूल की जिंदगी सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं रहती है, जैसी कि कोचिंग सेंटरों की रहती है। स्कूल की जिंदगी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, उनकी सामाजिक समझ विकसित करने के लिए, उनमें टीम भावना लाने के लिए ही रहती है। देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था ने इन सबको पूरी तरह से खत्म कर दिया है, और पढ़ाई के नाम पर कोचिंग को ही जरूरी साबित कर दिया है, जिसका खर्च देश का सबसे ऊपर का एक फीसदी तबका ही उठा पाता है। जब स्कूल शिक्षा से लेकर कोचिंग तक देश में गैरबराबरी इतना राज कर रही है, तो फिर गरीब बच्चों के लिए गुंजाइश ही कहां रह जाती है। और अब यह सिलसिला वापिस लौटते दिख भी नहीं रहा है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अभी कुछ ही दिन पहले केडिया के शराबखाने से काम करके लौटते कामगारों से भरी हुई एक बस रास्ते में मुरम खदान के गड्ढे में गिर गई थी, और उसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसके पहले इसी बरस इस प्रदेश में कहीं 5 तो कहीं 8 लोगों की सडक़-मौत होते ही रही है। लेकिन कल का कवर्धा का हादसा सबसे ही बुरा रहा जिसमें तेन्दूपत्ता तोडक़र लौट रहे बैगा आदिवासी मजदूरों को ढोकर ला रही गाड़ी खाई में गिर गई, और 19 लोग मारे गए। इनमें से 18 महिलाएं और नाबालिग लड़कियां हैं, और एक पुरूष है। ऐसा बताया जा रहा है कि छोटे आकार की एक मालवाहक गाड़ी 35-36 लोगों को ढोकर ला रही थी, और पहाड़ी ढलान पर ड्राइवर ब्रेक फेल हो जाने की बात कहते हुए कूद गया, और कुछ और लोग भी कूदकर जान बचाने में कामयाब रहे। लेकिन गाड़ी के साथ खाई में गिरे लोगों की बड़ी तकलीफदेह मौत हुई। इस बड़े पैमाने पर जब कोई हादसा होता है, तो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री इन सभी की तरफ से शोक और श्रद्धांजलि संदेश जारी होते हैं, और राज्य सरकार की तरफ से मदद की घोषणा भी होती है। ये दोनों बातें भी कल हो गई हैं, और कई घायल अस्पताल में हैं जिनसे जाकर नेताओं के मिलने का सिलसिला चल रहा है।
ऐसी हर बड़ी सडक़ दुर्घटना के बाद हम अपने थके-हारे मन से इस जगह पर लिखते हैं, और सत्ता के नाराज होने का खतरा उठाते हुए भी उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। कल पहले की तरह सरकार ने अपनी जिम्मेदारी शोक, श्रद्धांजलि, और मदद से पूरी कर ली है। लेकिन क्या इन तीनों चीजों से अगली एक भी सडक़-मौत थमने वाली है? क्या सरकार की जिम्मेदारी महज शोक, श्रद्धांजलि, और राहत जैसे किसी त्रिकोण से पूरी हो जाती है? क्या सडक़ों सहित पूरे प्रदेश में राज करने वाली सरकार कुछ घंटों के भीतर पूरी जिम्मेदारी से हाथ धोकर उन हाथों से बाकी काम करने में लग सकती है? कहने के लिए तो जिस संरक्षित बैगा आदिवासी समुदाय के जो लोग मारे गए हैं, उन्हें विशेष दर्जा प्राप्त कहा जाता है, और इनमें से कुछ जातियां तो राष्ट्रपति की गोद ली हुई बताई जाती हैं। लेकिन इस जाति की डेढ़ दर्जन महिला मजदूरों की इस मौत पर राष्ट्रपति की श्रद्धांजलि से अधिक कोई ड्यूटी बनती है? क्या राष्ट्रपति देश में अलग-अलग जगहों पर अपने बेकसूर दत्तक पुत्र-पुत्रियों की बेवक्त की मौतों पर कुछ और भी जानकारी हासिल करना चाहेंगी जिससे कि इन जातियों के लोगों, और देश के बाकी नागरिकों की थोक-मौतों का सिलसिला कुछ धीमा हो सके? और यही बात प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है कि क्या उनकी श्रद्धांजलि से देश की यह हकीकत बदल जा रही है कि गरीब और मजदूर इस देश में भेड़-बकरियों, गाय-भैंसों, और बोरियों की तरह लादकर ले जाए जाते हैं?
हिन्दुस्तान की दिक्कत यह हो गई है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी सरकार की जिम्मेदारी बस शोक, श्रद्धांजलि, और मदद पर खत्म हो जा रही है। यह बात किसी पेड़ के पत्तों पर दवा छिडक़ने जैसी है जिसकी कि जड़ों में ही कोई बीमारी लगी हुई है। हिन्दुस्तान में ऐसे सडक़ हादसों के पीछे एक बुनियादी खामी चली आ रही है जिससे जूझे बिना अगली कोई मौत थमने वाली नहीं है। आज इस देश में गांव-गांव तक गरीब और मजदूर मालवाहक गाडिय़ों पर सफर करते हैं, और इतने सारे खड़े हुए हिलते-डुलते लोगों की वजह से गाड़ी का संतुलन भी बिगड़ता है, और गाडिय़ां अमूमन बदहाल तो रहती ही हैं। नतीजा यही होता है कि जिस तरह किसी दूसरे मालवाहक के पलटने पर बक्से या बोरियां बिखर जाते हैं, उसी तरह कल आदिवासी मजदूरों के बदन बिखर गए, और जिंदगियां खत्म हो गईं। जब तक मालवाहक गाडिय़ों पर थोक में गरीबों का ढोना बंद नहीं होगा, ऐसी मौतें कैसे बंद हो सकती हैं? कहने के लिए यह बहाना बड़ा लोकप्रिय है कि जंगल और गांव में मुसाफिर गाडिय़ां मिलेंगी कहां से? लेकिन जब वहां मालवाहक गाडिय़ां मिल सकती हैं, तो अगर नियमों को सख्ती से लागू कराया गया रहता तो अब तक मुसाफिर गाडिय़ां भी चलन में आ चुकी रहतीं। मालवाहक गाडिय़ां भी तो किसी वक्त चलन में आईं, और उसके बाद बैलगाडिय़ां घटीं। लेकिन जब तक भ्रष्ट सरकारी अमला इंसानी जिंदगियों के लिए संवेदनाशून्य बने रहेगा, जब तक इस अमले को भेड़-बकरियों और इंसानों में कोई फर्क नहीं लगेगा, तब तक गरीबों की मौतें होती रहेंगीं। कल होना तो यह चाहिए था कि शोक, श्रद्धांजलि, और मदद-राहत से परे भी राज्य सरकार यह घोषणा करती कि वह हर सडक़ हादसे का अध्ययन करके उस तजुर्बे का इस्तेमाल करके आगे ऐसी मौतों को घटाने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार ने अपनी रस्म राहत पर खत्म कर दी। सरकारी खजाने से राहत दे देना आसान है, पूरे प्रदेश में सडक़ों और गाडिय़ों की बदअमनी-अराजकता को सुधार पाना बड़ा मुश्किल है, और आज तो सरकारों का जो हाल दिखता है, उसमें वह नामुमकिन सरीखा है।
अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से छत्तीसगढ़ का ट्रांसपोर्ट विभाग राजनीतिक उगाही और इंतजामों का अड्डा बना हुआ है। यह हाल देश के अधिक दूसरे शहरों का भी है, और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी बहुत बार सार्वजनिक मंचों से देश में आरटीओ के भ्रष्टाचार की बात कह चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री ही ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री हैं, और कल बिना अपनी गलती के जो 19 मेहनतकश मजदूर बेवक्त मारे गए हैं, वे भी तमाम आदिवासी हैं। इस हादसे के बाद सरकार की तरफ से जो हुआ है उससे बहुत अधिक होने की जरूरत है, और सरकार को राज्य की सडक़ों पर रोजाना होने वाली अनगिनत मौतों को टालने के लिए गैरसरकारी अध्ययन करवाना चाहिए। सरकार का अपना पूरा ढांचा इस बुरी तरह भ्रष्ट और बेअसर हो चुका है कि वह राजधानी रायपुर में भी म्युनिसिपल की बड़ी-बड़ी फौलादी मशीनों में कचरा और मलबा उठाने वाले फौलादी हिस्से पर मजदूर महिलाओं को ढोकर आते-जाते देखते रहता है। किसी चौराहे पर पुलिस को यह नहीं सूझता कि जेसीबी नाम से पहचानी जाने वाली ऐसी मशीनों पर मजदूरों को सामने बिठाकर दौड़ती फौलादी गाडिय़ों को रोके जिसमें कि किसी भी टक्कर में सबसे पहले इन महिलाओं के पैर कटेंगे।
दरअसल सरकार और समाज का सारा इंतजाम तथाकथित वीआईपी तबके की सहूलियतों तक सीमित हो गया है। सरकारी गाडिय़ों के काफिले बिना जरूरत भी दौड़ते रहते हैं, और जिन इंसानों की सेवा करने के नाम पर संविधान की शपथ लेकर ये नेता सत्ता पर आते हैं, वे इंसान पलटी हुई गाडिय़ों से जानवरों की तरह कुचलकर मरते रहते हैं। इस मामले में किसी जनहित याचिका को लेकर हाईकोर्ट तक दौड़ लगाने का भी कोई फायदा हमें नहीं दिखता क्योंकि बड़े जज सरकार के छोटे-छोटे अमले को उनका रोज का काम तो सिखाने आ नहीं सकते। प्रदेश की जनता भी अजीब किस्म की मुर्दा है कि डेढ़ दर्जन से अधिक इन आदिवासी लाशों के अंतिम संस्कार के पहले ही सरकार ने हाथ धो लिए हैं, और जनता इन करकमलों से आज कहीं उद्घाटन करवानेे में भी लग गई होगी। जो समाज अपने सबसे भयानक हादसों से भी कोई सबक नहीं लेता है, वह अगले हादसे की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ते रहता है। कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर ऐसा कोई और हादसा होगा, और उस वक्त हम इस संपादकीय में से कुछ शब्द फेरबदल करके फिर इसे पूरे का पूरा छापने के लायक रहेंगे। जो देश-प्रदेश अपने इंसानों को बोरियों और मलबे की तरह मालवाहक पर नियमित रूप से, और लगातार ढोता है, उसे अपने को सभ्य कहलाने का कोई हक नहीं है।
दुनिया में मोबाइल फोन के मामले में सबसे महंगी कंपनी, एप्पल ने अभी यह दावा किया है कि उसके एप्लीकेशन स्टोर पर जो धोखेबाज लोग अपने एप्लीकेशन डालने की कोशिश करते हैं, उनमें से 17 लाख एप्लीकेशन उसने रोक दिए, और इसकी वजह से एप्पल उपभोक्ता ठगी का शिकार होने से बच गए, और करीब 7 बिलियन अमरीकी डॉलर, यानी करीब 584 अरब रूपए डूबने से बचे। किसी कारोबारी कंपनी के दावों पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम एप्पल की सामने रखी गई जानकारी बता रहे हैं कि कंपनी का कहना है कि उसने चोरी गए एक करोड़ चालीस लाख क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए, और 33 लाख ऐसे अकाऊंट को रोक दिया जो कि इन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। एप्पल का दावा है कि 2023 में उसने चोरी गए 35 लाख क्रेडिट कार्ड से खरीददारी रोकी, और उसके सुरक्षा पैमाने बहुत ऊंचे रहने से उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों का बड़ा नुकसान बचता है।
हम किसी एक कंपनी के ऐसे दावे पर गए बिना हिन्दुस्तान जैसे देश में देख रहे हैं जहां पर कि पिछले कुछ बरसों में मोदी सरकार ने डिजिटल लेन-देन को खूब आगे बढ़ाया है, और छोटे-छोटे कामों के लिए भी लोग मोबाइल फोन से भुगतान करने लगे हैं, और हम किसी का मखौल उड़ाने के लिए यह बात नहीं कह रहे, लेकिन कहीं-कहीं से ऐसी तस्वीरें भी आती हैं कि कुछ भिखारी भी अपने पास क्यूआर कोड लेकर बैठते हैं, ताकि लोग उन्हें डिजिटल भुगतान कर सकें। कई मंदिरों में भी शायद ऐसा ही इंतजाम किया गया है। ऐसे डिजिटल भुगतान में तो धोखाधड़ी और जालसाजी सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन मोबाइल फोन पर तरह-तरह के एप्लीकेशन, और बैंकों के कामकाज, आधार कार्ड से लेकर कुरियर कंपनी के भेजे जाने वाले ओटीपी तक, इतने तरह के डिजिटल काम लोगों के सामने आते हैं कि वे कभी नासमझी में, कभी हड़बड़ी में, तो कभी धोखा खाकर टेलीफोन पर ओटीपी मांगने वालों को फोन देखकर बता देते हैं, और मिनटों में उनके बैंक खाते खाली हो जाते हैं। यह सिलसिला भयानक इसलिए है कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग इतने चौकन्ने और जानकार नहीं रहते कि वे हर ओटीपी की गंभीरता को समझ सकें। लेकिन जिनको हम बहुत जानकार मानते हैं ऐसे सरकारी अफसर, बैंक कर्मचारी भी इन दिनों वॉट्सऐप पर धड़ल्ले से चलने वाले धोखेबाज गोल्ड-इन्वेस्टमेंट ग्रुप से लेकर फेसबुक पर धोखेबाजों के इश्तहार तक कई चीजों के शिकार हो रहे हैं। इन दो के अलावा तरह-तरह के एप्लीकेशन कर्ज देने के नाम पर लोगों को फंसाते हैं, उनके मोबाइल फोन पर कब्जा कर लेते हैं, और फिर उनकी राज की बातें निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, खुदकुशी तक के लिए मजबूर करते हैं। भारत सरकार ने ऐसे कई चीनी लोन एप्लीकेशन ब्लॉक भी किए हैं, लेकिन सरकार जितने एप्लीकेशन ब्लॉक करती है, उससे अधिक गूगल प्ले स्टोर जैसी जगहों पर फिर आ जाते हैं, और लोगों को बहुत आसान कर्ज का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं।
हम दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनियों की बात करें, तो एप्पल का आईफोन कोई भी नया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आसानी से डाऊनलोड भी नहीं करने देता, वह कई तरह की इजाजत मांगता है, कई तरह के पासवर्ड मांगता है, सावधान करता है, तब कहीं जाकर उस पर कोई एप्लीकेशन डाऊनलोड किया जा सकता है। नतीजा यह होता है कि धोखेबाज एप्लीकेशन डाऊनलोड करने के पहले लोगों को कुछ मिनट का वक्त लगाना पड़ता है, और इतनी देर में हो सकता है कि उन्हें सावधानी सूझ जाए। दूसरी तरफ एप्पल जैसी ही बड़ी कंपनी मेटा अपने फेसबुक और वॉट्सऐप पर ऐसी-ऐसी धोखेबाजी को बढ़ावा देती है जिन्हें देखकर बच्चे भी समझ जाएं कि यह जालसाजी है। फेसबुक पर तो अलग-अलग अखबारों के नाम से हिन्दुस्तान के कुछ सबसे बड़े कारोबारियों के फर्जी और गढ़े हुए इंटरव्यू दिखाकर, लोगों को क्रिप्टोकरेंसी और दूसरे पूंजीनिवेश की तरफ खींचा जाता है, और हमने खुद ने ऐसी जालसाजी पर बार-बार लिखा है कि यह फ्रॉड है, लेकिन फेसबुक इस धोखाधड़ी को स्पॉंसर्ड पोस्ट दिखाते हुए बनाए रखता है। मतलब यह कि इसके लिए वह भुगतान ले रहा है। हमारा ख्याल है कि हिन्दुस्तान के आईटी कानून के मुताबिक इसे लेकर फेसबुक और वॉट्सऐप को कटघरे में लाया जा सकता है कि वे जानते-समझते यह धोखाधड़ी जारी रख रहे हैं।
हिन्दुस्तान में हर दिन दसियों हजार लोग साइबर-फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, और इतनी तो शिकायतें पुलिस के पास पहुंचती हैं, असलियत में तो इससे कई गुना ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपने ठग लिए जाने का अहसास भी नहीं हुआ होगा, और वे पुलिस तक पहुंचे भी नहीं होंगे। आज भारत सरकार अपनी सारी तकनीकी क्षमता, और एकाधिकार के साथ भी अगर बहुत संगठित साइबर जालसाजी पर रोक नहीं लगा पा रही है, अगर वह महादेव ऐप जैसी सट्टेबाजी पर रोक नहीं लगा पा रही है, अगर वह फेसबुक और वॉट्सऐप को संगठित अपराध पर कार्रवाई न करने के लिए कटघरे में नहीं ला पा रही है, तो यह सरकार की लापरवाही के अलावा कुछ नहीं है। अमरीका और यूरोपीय समुदाय तो मेटा जैसी कंपनी को बच्चों पर बुरे असर की जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी संसदीय जांच भी कर रहे हैं, और मेटा पर बड़े लंबे-चौड़े जुर्माने की तैयारी भी चल रही है।
एप्पल का दावा अगर सही है, तो भारत सरकार को यह भी देखना चाहिए कि ऐसे कौन-कौन से धोखेबाज और जालसाज एप्लीकेशन हैं जो गूगल प्ले स्टोर जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, और हर दिन लोगों को लूट रहे हैं। सरकार को जालसाज और धोखेबाज कंपनियों, उनके कर्मचारियों के नंबर, इंटरनेट कनेक्शन, बैंक खाते, आधार कार्ड या पैनकार्ड जैसी शिनाख्त, इन सब पर बहुत रफ्तार से रोक लगानी चाहिए ताकि उनसे चलने वाले दूसरे जालसाज एप्लीकेशन भी पकड़ में आ सकें। आज जितनी सरकारी कार्रवाई सुनाई पड़ती है, और जितनी जालसाजी सामने आती है, उन दोनों को देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार जालसाजों के सौ-पचास मील पीछे चल रही है। साइबर-क्राईम की दुनिया में पुलिस की लाठी वाली रफ्तार से काम नहीं चलेगा, पुलिस को मुजरिमों की रफ्तार और उनके तौर-तरीके समझकर उनके आगे-आगे भी चलना पड़ेगा, तभी आम जनता लुटने से बच पाएगी। भारत सरकार चाहे तो एप्पल जैसी कंपनी से यह समझ सकती है कि वह किन एप्लीकेशनों को किस आधार पर रोकती है, और उनमें से जो भारत में कानूनसम्मत लगें, उन्हें यहां पर एंड्रॉयड फोन के लिए भी रोका जा सकता है जिससे कि जालसाजी कम होगी। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
इन दिनों दुतरफा प्रेमसंबंधों, या इकतरफा आकर्षण, शादीशुदा जिंदगी के भीतर, या विवाहेत्तर संबंधों को लेकर इतने किस्म के कत्ल हो रहे हैं कि अखबार निचोड़ें तो उसमें से खून टपकने लगे। खबरें डराती हैं कि इस कदर बढ़ा हुआ व्यक्तिगत और सामाजिक तनाव कहां जाकर खत्म होगा। यह तो हुई हिंसा की बात, लेकिन हिंसा से परे भी इतने किस्म के जुर्म रोज दर्ज हो रहे हैं कि पुलिस जाने कैसे इन तमाम मामलों को अदालत में फैसले तक पहुंचा सकेगी। हर दिन आसपास से ही कई ऐसी गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि नाबालिग को शादी का धोखा देकर उससे बलात्कार किया, और ऐसा करने वाला बालिग गिरफ्तार हुआ। इन मामलों से परे बहुत से और किस्मों के सेक्स-जुर्म सामने आ रहे हैं जो कि अलग-अलग किस्म की कहानियां बताते हैं।
अब जो बात समझ नहीं पड़ती है, वह यह कि नाबालिग लड़कियों को ऐसे देहसंबंध में पडऩे की क्या हड़बड़ी है जिसमें उनसे शादी का कोई वायदा किया गया है? यह बात भी लडक़ी के बयान में ही सामने आती है, और हम किसी एक मामले में कोई शक किए बिना यह सोचते हैं कि क्या ये तमाम शिकायतें सही रहती हैं, या संबंध आपसी रजामंदी से बनते हैं, और चूंकि नाबालिग की सहमति का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए बालिग नौजवान तुरंत गिरफ्तार भी हो जाते हैं। नाबालिग लड़कियों से देहसंबंध बनाने वाले बालिग नौजवानों से हमारी कोई हमदर्दी नहीं है, इसलिए उनके जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों से लड़कियों का भी जो नुकसान होता है उसे तो उन्हीं को झेलना पड़ता है। वैसे प्रसंग से हटकर एक बात हम यहां कहें जो कि हम बार-बार लिखते हैं, तो बलात्कारी की संपत्ति का एक हिस्सा बलात्कार की शिकार लडक़ी या महिला को मिलना चाहिए, ऐसा अगर होने लगे तो बलात्कारी कुछ हद तक तो हिचकना शुरू हो जाएंगे कि जेल से छूटने के बाद भी परिवार की धिक्कार और अधिक जारी रहेगी, क्योंकि बाकी परिवार संपत्ति का एक हिस्सा खो बैठेगा।
कल छत्तीसगढ़ में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के एक गांव में एक नौजवान ने एकतरफा प्रेम में एक शादीशुदा, एक बच्चे की मां, और गर्भवती युवती को मार डाला क्योंकि वह एक वक्त उससे प्रेम करता था, शादी करना चाहता था, और लडक़ी के परिवार ने उसकी शादी कहीं और कर दी थी। तब से जब लडक़ी मायके आती थी, वह उसे परेशान करता था, और ऐसे ही एक हमले में उसे कैद भी हो चुकी थी। अब वह कैद से छूटकर आया था, और युवती अपने तीन बरस के बेटे सहित मां के घर आई हुई थी। इस हत्यारे ने इस परिवार में जाकर युवती के साथ-साथ उसके मां-बाप, बहन, बेटे को मार डाला, और इस खूनी मंजर के बीच खुदकुशी भी कर ली। एकतरफा प्रेम में ऐसा भयानक खूनखराबा हमें हाल-फिलहाल में याद नहीं पड़ रहा है, और एक साथ पांच कत्ल और एक खुदकुशी की खबर से सबका दिल भी दहल गया है। छठवां कत्ल अजन्मे बच्चे का हुआ है। एकतरफा कहे जा रहे इस प्रेम की हिंसा देखते हुए अब यह सोचने की जरूरत पड़ रही है कि समाज में प्रेम, देह, और शादी की ऐसी कितनी कमी हो गई है कि उसके लिए इस तरह की, इतनी बड़ी हिंसा की नौबत आ रही है?
इसे सिर्फ एक सिरफिरे आशिक का काम मानकर पुलिस के अंदाज में मामले को बंद कर देना ठीक इसलिए नहीं होगा कि इससे समाज की व्यापक बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। हिन्दुस्तानी समाज में प्रेम की जगह और संभावना जिस हद तक घटती चल रही है, उससे भी ऐसी हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। लोगों को किसी एक से प्रेम होता है तो उसे ही वे जिंदगी का अंत मान लेते हैं, और दोनों तरफ के परिवार सहमत न हो तो ऐसे प्रेमीजोड़े आए दिन अपनी जिंदगी का अंत करते रहते हैं। यह पूरा सिलसिला समाज के इस प्रतिरोध से भी बढ़ रहा है जो कि दूसरे धर्म, दूसरी जाति, दूसरी आर्थिक संपन्नता में अपने परिवार का रिश्ता नहीं होने देना चाहते। नौजवान दिल हैं कि तन और मन की उनकी जरूरतें, परिवार की रोक-टोक से परे खड़ी होती हैं, और बढ़ती हैं। भारत का आम समाज जब तक प्रेम का दुश्मन बने रहेगा, तब तक आत्मघाती या जानलेवा हिंसा बनी रहेगी।
आपसी रिश्तों में हिंसा के एक दूसरे किस्म के मामले कुछ अलग तरीके से चौंका रहे हैं। इन दिनों लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहां पर किसी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर या भाड़े के हत्यारे जुटाकर अपने पति का कत्ल करवा दिया। अभी तक इसका उल्टा तो होते आया था कि पति कत्ल करवाते थे, और पत्नियों की जान जाती थी। हाल के बरसों में ये दूसरी किस्म की खबरें भी लगातार बढ़ रही हैं, और कुछ मामलों में तो बिना किसी प्रेमी के भी अपने शराबी या बदचलन पति से थकी हुई महिला खुद भी उसका कत्ल कर दे रही है, या भाड़े के हत्यारे जुटा रही है। हम इसे हाल के बरसों में भारतीय महिला का एक अलग किस्म का सशक्तिकरण भी देख रहे हैं जिनमें वह अपने पर होते जुल्म को और अधिक बर्दाश्त करने से मना कर दे रही है, और प्रतिरोध, प्रतिकार, या प्रतिहिंसा पर उतर आ रही है। अगर भारतीय महिलाओं में अपने अधिकारों के लिए इस किस्म की हिंसक जागरूकता आती है, तो इससे परिवारों के भीतर हिंसा की घटनाओं में एकदम से इजाफा होगा क्योंकि अभी तक तो महिलाएं हिंसा झेलते ही आई हैं।
हमारा ख्याल है कि समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने वाले लोगों को ऐसी पारिवारिक और निजी हिंसा की वजहों पर शोध करना चाहिए। यह सामाजिक अध्ययन इसलिए भी जरूरी है कि परिवारों और समाज के भीतर की हिंसा को बढऩे से रोकने के कुछ तरीके सोचे जा सकें, और परामर्शदाताओं को भी ऐसी शोध से मदद मिल सके। फिलहाल चारों तरफ फैल रही अभूतपूर्व और असाधारण दिख रही हिंसा से बचने के तरीके सोचने चाहिए, और आसपास के लोगों में अगर हिंसक भावना दिखे तो उन्हें समझाने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत बड़ी हिंसक भावना बिना किसी लक्षण के अचानक खड़ी नहीं हो जाती, इसलिए करीबी लोगों को ऐसी नौबत का अंदाज पहले से लग सकता है, और वे चाहें तो विचलित व्यक्ति को समझा-बुझाकर, और बाकी परिवार के साथ परामर्श करके हिंसा के खतरे को घटा सकते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
भारत के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाले इम्तिहान, नीट, के पर्चे लीक करके उसे आधा-पौन करोड़ तक में एक-एक छात्र को बेचने, और उसके आधार पर तैयारी करवाकर इम्तिहान दिलवाने का भांडा फोड़ हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में अदालत ने इम्तिहान पर रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन केन्द्र सरकार को नोटिस जरूर जारी किया है जो कि नीट इम्तिहान आयोजित करती है। इस जनहित याचिका में अदालत से कहा गया है कि इसका एक पर्चा लीक हुआ है, और उसके आधार पर अगर इम्तिहान होता है तो उससे दाखिला प्रभावित होगा, और प्रतिभाशाली छात्रों का हक मारा जाएगा। याचिका में कहा गया है कि मोटी रकम देकर ऐसे पर्चे खरीदने वाले लोगों से बाकी छात्रों का समानता और बराबरी के अवसरों का बुनियादी हक मारा जा रहा है, और कुछ संपन्न छात्रों को इससे नाजायज फायदा मिल रहा है। खबरें बताती हैं कि गुजरात और बिहार में संगठित शिक्षा-माफिया इस पर्चा-लीक के पीछे है, और बहुत से ऐसे बयान मिल गए हैं जिन्होंने बताया कि उनके मां-बाप ने लीक हो चुके पर्चे का इंतजाम किया था, और उन्हें रात भर इन्हीं सवालों की तैयारी करवाई गई, और अगले दिन यही पर्चा आया भी।
अब देश भर में कुछ अलग-अलग मेडिकल-दाखिला इम्तिहान होते थे जिनको सबको खत्म करके राष्ट्रीय स्तर पर नीट लेना शुरू किया गया, और उस वक्त भी दक्षिण भारत के तमिलनाडु जैसे राज्य नीट का जमकर विरोध कर रहे थे। जबकि आम धारणा यह है कि दक्षिण में पढ़ाई का स्तर बेहतर है, और राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी दाखिला इम्तिहान में दक्षिण भारत के राज्य, और महाराष्ट्र जैसे बेहतर पढ़ाई वाले राज्य के छात्र-छात्राओं का दबदबा रहेगा। लेकिन अब अगर गुजरात और बिहार के करोड़पति मां-बाप पर्चे खरीदकर अपने बच्चों के पास होने की गारंटी करवा ले रहे हैं, तो इससे पूरे देश में ही प्रतिभाशाली बच्चों की संभावनाएं खत्म होती हैं। यह सिलसिला कई तरह से खतरनाक है, एक तो इससे देश की सरकार और लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा खत्म होता है, और फिर गरीब बच्चों के मन में यह निराशा स्थाई रूप से बैठ जाएगी कि वे कुछ भी कर लें, दाखिला तो करोड़पतियों के पर्चे-खरीदे बच्चों का ही होगा। गरीब बच्चों के मनोबल टूटने का एक लंबा नुकसान होगा जिससे उबरना भी मुश्किल होगा। और फिर ऐसे बच्चे आगे चलकर सरकार, कानून, और लोकतंत्र के लिए मन में हिकारत पाल लेंगे, और देश के लिए यह भारी पड़ेगा।
सिर्फ यही दाखिला इम्तिहान नहीं, अलग-अलग राज्यों में, और केन्द्र सरकार की नौकरियों के लिए जितने तरह की चयन-परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी जहां-जहां बेईमानी होती है, राजनीतिक या आर्थिक आधार पर लोगों को चुना जाता है, उससे भी गरीब और मेहनती बच्चों में डिप्रेशन भर जाता है। उनकी पढ़ाई-लिखाई में दिलचस्पी भी घट जाती है कि आगे जाकर स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई से तो नौकरी भी नहीं मिल पाएगी, और नौकरी तो खरीदनी ही पड़ेगी। जब देश की नौजवान पीढ़ी और उससे भी कम उम्र के बच्चों में यह धारणा घर कर जाएगी तो लोगों के मन में पढ़ाई का महत्व खत्म हो जाएगा। यह कुछ उसी किस्म का होगा जिस तरह कि जब सरकारें बहुत भ्रष्ट हो जाती हैं, तो लोगों की टैक्स देने में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। लोगों को लगता है कि हम ईमानदारी से टैक्स दें, और उस पैसे को खर्च करते हुए सत्ता पर बैठे नेता और अफसर बेईमानी करते रहें, तो फिर ऐसा टैक्स दिया ही क्यों जाए? आज वैसे भी हिन्दुस्तान में स्कूलों की पढ़ाई एक नकली पुतले की तरह बन गई है, और पैसे वाले मां-बाप अपने बच्चों के लिए किसी महंगे कोचिंग सेंटर में दाखिला जुटाते हैं, और वह कोचिंग सेंटर बच्चों को स्कूल के बोझ से बचाने के लिए अपनी किसी डमी स्कूल में उनका दाखिला दिखा देते हैं, और बिना क्लास में गए उन्हें हाजिरी मिलती रहती है। दशकों से यही सिलसिला चले आ रहा है, और अब जाकर किसी एक स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ऐसे स्कूलों की मान्यता खत्म की है जो छात्र-छात्राओं को दिखावे का एडमिशन दिखाती हैं।
भारत की शिक्षा व्यवस्था वैसे भी गरीब और अमीर के बीच, सरकारी और निजी के बीच, हिन्दी और अंग्रेजी के बीच, तरह-तरह के विरोधाभासों से भरी हुई है, और ये विसंगतियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। जिस तरह से निजी महंगी स्कूलों के बाद अब निजी महंगे विश्वविद्यालय हावी हो गए हैं, उनसे भी यह समझ पड़ता है कि आगे की ऊंची पढ़ाई में दाखिले के लिए पैसों का बोलबाला काम आता है क्योंकि महंगी कोचिंग पाने वाले बच्चों की संभावना मुकाबले में बढ़ जाती है। अब इससे भी सौ कदम आगे जाकर अगर खरीदे गए पर्चों से तैयारी करके कुछ अतिसंपन्न बच्चे दाखिला पा जाएंगे, तो इससे नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की दाखिला-परीक्षा शुरू करना ही नाजायज होगा। जिन दो राज्यों गुजरात और बिहार में साजिश करके नीट का पर्चा लीक किया गया है, दोनों ही जगहों पर भाजपा-एनडीए की सरकारें हैं, और केन्द्र सरकार को इस भयानक जुर्म को अपनी राज्यों की सत्ता के साथ जोडक़र भी देखना चाहिए। कहने के लिए जिस इम्तिहान का इंतजाम बड़ा सख्त है उसके पर्चे जुटाने और बेचने में अगर गुजरात और बिहार इस तरह उजागर हुए हैं, तो यह बात वहां की राज्य सरकार के भी फिक्र करने की है जिसकी कि इज्जत इससे खराब हो रही है।
हमारा ऐसा ख्याल है कि दाखिला-इम्तिहानों से लेकर नौकरियों तक अगर कोई संगठित जुर्म हो रहा है, तो उसके लिए अधिक सजा का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी एक-एक परीक्षा को प्रभावित करने का काम लाखों बच्चों की जिंदगियां प्रभावित करता है, और फिर कॉलेजों में दाखिले से लेकर सरकारी नौकरियों तक में अगर कम प्रतिभाशाली बच्चे चुन लिए जाते हैं, तो आगे की पढ़ाई और नौकरी दोनों की क्वालिटी खराब होना तय है। केन्द्र सरकार को अपने इस इम्तिहान की साख बचाने के लिए भी इस बार की पूरी साजिश का भांडाफोड़ करना चाहिए, और आगे ऐसा न हो उसके लिए बेहतर इंतजाम करना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाम पर लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच सुप्रीम कोर्ट से एक असाधारण जमानत पाकर चुनाव प्रचार तक बाहर तो आ गए, लेकिन उनकी बोलती बंद है। इसके पहले कि वे चुनाव प्रचार के लिए निकल पाते, उनकी एक सबसे पुरानी सहयोगी और पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर उन्हीं के घर के ड्राईंग रूम में उन्हीं के निजी सहायक ने हमला किया, और स्वाति को पीटा। स्वाति की रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस ने उनका मेडिकल करवाया है, और अब केजरीवाल के इस बहुत पुराने निजी सहायक विभव कुमार की तलाश जारी है। इस हमले को चार दिन हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद-प्रवक्ता संजय सिंह ने मीडिया के सामने मंजूर किया है कि अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास पर उनसे मिलने पहुंचीं स्वाति से ड्राईंग रूम में केजरीवाल के निजी सहायक ने बहुत बुरा सुलूक किया है जो शर्मनाक है, और मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई करेंगे। बात-बात में सार्वजनिक आरोप उछालने वाले और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाने वाले अरविंद केजरीवाल अपने खुद के घर में एक महिला सांसद की पिटाई पर चार दिन में मुंह भी नहीं खोल पा रहे हैं, और यह हमलावर उनका निजी सहायक उसके बाद भी लखनऊ एयरपोर्ट पर देखा गया है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि इस निजी सहायक ने उन्हें चेहरे पर थप्पड़ें मारीं, गंदी गालियां दीं, और कहा कि वह उन्हें तबाह कर देगा। उन्होंने पुलिस को यह भी कहा है कि उनकी छाती पर और उनके बदन के निचले हिस्से में भी विभव कुमार ने वार किए। स्वाति के फोन से सीएम हाऊस के भीतर से ही दिल्ली पुलिस को फोन करके बताया गया था कि सीएम की पीए ने उन पर हमला किया है।
नीति और सिद्धांत की बात करने वाला कोई नेता न भी हो, दिल्ली का सीएम या अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक न भी हो, कोई आम इंसान भी अपने घर पहुंची महिला को अपने पीए से पिटवाने की हिंसानियत नहीं दिखा सकते। अब यह केजरीवाल परिवार के भीतर की बात है कि स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया है, या राजनीति में अभी सक्रिय हुईं उनकी पत्नी ने। दिल्ली की अफवाहें यह भी कहती हैं कि सुनीता केजरीवाल स्वाति मालीवाल को नापसंद करती हैं, और वे भी इस हमले के पीछे हो सकती हैं। जो भी हो, अगर सीएम की बीवी उनके सरकारी निवास पर एक महिला राज्यसभा सदस्य पर हमला करवा रही है, तो यह भी केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती थी कि वे अपने पीए और पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते। अब हो सकता है कि केजरीवाल को यह मलाल हो रहा हो कि वे सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आए ही क्यों कि उनके सार्वजनिक जीवन का यह सबसे बड़ा बवाल खड़ा हो गया जो कि उन्हें सिर्फ धिक्कार का हकदार बनाता है। गिने-चुने दिनों के चुनाव प्रचार के लिए इतनी लड़ाई के बाद मिली जमानत मानो नाली में बह जा रही है, और केजरीवाल किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ उनकी प्रेस कांफ्रेंस में उनसे सिर्फ स्वाति मालीवाल पर सवाल किए गए, उनके होंठ सिले रहे, और उनकी तरफ से संजय सिंह मणिपुर से लेकर कर्नाटक के रेवन्ना सेक्सकांड तक को गिनाते रहे, सिवाय स्वाति मालीवाल मामले पर जवाब देने के।
बाजार में दो तरह की चर्चाएं हैं, एक तो यह कि अपने को जमानत दिलवाने वाले, और ईडी के खिलाफ बाकी मामले लडऩे वाले दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने के लिए केजरीवाल की तरफ से स्वाति मालीवाल पर दबाव डाला जा रहा था कि वे इसी बरस राज्यसभा में पाई अपनी सीट खाली कर दें। दूसरी अप्रिय निजी जीवन की चर्चा का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं कि केजरीवाल के जेल रहने पर उनकी पत्नी ने किस तरह राजनीतिक मामलों में अगुवाई शुरू की थी, और सोनिया गांधी के साथ मंच पर दिखी थीं। यह पूरा सिलसिला किसी डबरे के पानी में कीचड़ घुल जाने से गंदला हो गया लगता है। जिस केजरीवाल ने नैतिकता की दुहाई देते हुए अन्ना हजारे नाम के खादी की खाल ओढ़े एक पाखंडी के साथ मिलकर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार हराने का काम किया था, वही केजरीवाल अब ईमानदारी और नैतिकता के हर पैमाने पर खोटा साबित हो रहा है। सिर्फ दिल्ली और पंजाब की चुनावी कामयाबी सब कुछ नहीं होती। देश की कुछ और पार्टियां भी सारी नैतिकता और ईमानदारी, सारा लोकतंत्र छोडक़र चुनावी कामयाबी पा रही हैं, ऐसे में केजरीवाल और उनकी पार्टी का औरों से कोई फर्क नहीं रह गया है। अपनी पार्टी और अपने घर के इस भयानक विस्फोटक, अभूतपूर्व और शर्मनाक जुर्म के बारे में वो मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उन्हें लोकतंत्र के नाम पर जमानत देने वाले सुप्रीम कोर्ट जजों को भी शायद निजी हैसियत में यह मलाल हो रहा होगा कि उन्होंने भला यह किस आदमी के लिए इतने बड़े लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार लेकर जमानत दे दी।
इस पूरे मामले से केजरीवाल एक बहुत ही घटिया नेता और इंसान की तरह सामने आए हैं, इसके साथ-साथ यह बात भी भयानक है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से राजनीतिक दल में बदला यह एनजीओ भी डेढ़ दशक के भीतर ही एक कुनबापरस्त और तानाशाह पार्टी में बदल गया है। आज इस मौके पर यह भी याद पड़ता है कि किस तरह प्रशांत भूषण, योगेन्द्र यादव, आशुतोष जैसे कितने ही लोग केजरीवाल को छोडक़र चले गए, और आम आदमी पार्टी से बाहर हो गए। इतन कम दौर में इतने उत्थान और ऐसे पतन वाले केजरीवाल शायद अकेले ही नेता होंगे। बड़ी बात यह नहीं है कि केजरीवाल के बंगले पर उनकी राज्यसभा सदस्य पर उनके पीए ने शारीरिक हमला किया, बड़ी बात यह है कि इस पर चार दिन बाद भी मुख्यमंत्री को कुछ करना जरूरी नहीं लगा है। यह तो मुख्यमंत्री के रूप में संविधान की ली गई शपथ के भी खिलाफ है। यहां पर यह चर्चा करना भी जरूरी है कि यह मामला सिर्फ राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच का नहीं है, जो कि बड़े उत्साह से ओवरटाईम कर रहा है, बल्कि यह राज्यसभा के सभापति की दखल का मामला भी है क्योंकि स्वाति मालीवाल राज्यसभा सदस्य हैं।
हम शराब घोटाले में केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी पर साढ़े तीन सौ करोड़ रिश्वत के आरोपों को भी राजनीतिक या सरकारी मानकर अदालती फैसले तक उसे सीमित महत्व का मान सकते थे, लेकिन एक महिला के साथ केजरीवाल परिवार द्वारा करवाई गई ऐसी भयानक हिंसा को शराब घोटाले के मुकाबले अधिक अनैतिक काम मान रहे हैं जिसका कोई बचाव नहीं हो सकता। इस घटना के बाद केजरीवाल की चुप्पी जितनी लंबी खिंचती चली जाएगी, उनकी नाक उतनी ही कटती चली जाएगी। यह मामला देश की हर पार्टी के लिए एक मिसाल रहेगा, और सबके लिए यह सबक भी रहेगा कि एक महिला राज्यसभा सदस्य को इस तरह पिटवाकर कोई बच नहीं सकते। अब दिल्ली सीएम के बंगले में लगे हुए सारे कैमरे जो कि लगाए तो उनकी हिफाजत के लिए गए थे, अब वे काम आएंगे उनके खिलाफ सुबूत जुटाने में। हमें उम्मीद है कि केजरीवाल के काबिल वकील अभिषेक मनु सिंघवी उन्हें यह सलाह देंगे कि सीएम हाऊस के कैमरों की रिकॉर्डिंग को मिटाना एक जुर्म के सुबूत नष्ट करने का एक और जुर्म होगा।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ वहां राजभवन की एक अस्थाई महिला कर्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था जिसकी जांच बंगाल की पुलिस कर रही है, और उसने राजभवन कर्मचारियों से पूछताछ की इजाजत के अलावा राजभवन का सीसीटीवी फुटेज मांगा है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक राज्यपाल के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती, इसलिए वे अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन राज्यपाल सी.वी.आनंद बोस ने इस महिला की शिकायत पर पुलिस जांच के बाद करीब सौ चुनिंदा पत्रकारों को राजभवन में इकट्ठा करके शिकायत में बताए गए घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज में से चुनिंदा हिस्सा उनके सामने अपने को बेकसूर साबित करने की कोशिश में रखा। खबरें बताती हैं कि इस फुटेज में शिकायतकर्ता महिला को भी दिखाया गया, जिससे उसकी निजता भंग हुई। यौन शोषण की शिकायत पर किसी भी महिला की पहचान, उसका नाम, कुछ भी उजागर करने पर कानूनी रोक है, और राज्यपाल ने ठीक यही किया। राज्य का संवैधानिक प्रमुख अगर ऐसी हरकत करता है, और उसे संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, तो फिर ऐसी सुरक्षा के बारे में एक बार और सोचना चाहिए। लोगों को याद होगा कि आन्ध्रप्रदेश के राजभवन में कुछ दशक पहले उस वक्त राज्यपाल रहे नारायण दत्त तिवारी के भी कुछ वीडियो सामने आए थे जिनमें वे राजभवन के किसी कर्मचारी के साथ तो नहीं थे, लेकिन वहां के अतिथिगृह में आकर ठहरी एक महिला के साथ थे। ऐसे वीडियो के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। देश में अलग-अलग कई राजभवनों में राज्यपाल जितने छिछोरे किस्म के मामलों में उलझे हुए दिखते हैं, उनसे लगता है कि उन्हें मिली हुई ऐसी संवैधानिक सुरक्षा खत्म करनी चाहिए। वैसे भी किसी भी ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को सिर्फ उसकी जिम्मेदारी के कामकाज से जुड़ी हुई कोई सुरक्षा देना शायद जायज होता हो, लेकिन निजी चाल-चलन, निजी भ्रष्टाचार, यौन शोषण जैसे मामलों में किसी को संवैधानिक हिफाजत देना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। अब राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ मानो यह शिकायत काफी नहीं थी कि एक ओबीसी नृत्यांगना ने बंगाल राज्यपाल के खिलाफ बंगाल पुलिस को एक शिकायत की थी जिसकी जांच अब पुलिस ने पूरी की है, और राज्य शासन को रिपोर्ट दे दी है। इस नृत्यांगना ने दिल्ली के एक होटल में ठहरने के दौरान उनसे मिलने के लिए दिल्ली का बंग भवन छोडक़र बिना सुरक्षा अकेले पहुंचे हुए राज्यपाल का जिक्र किया था, और शिकायत की थी कि उन्होंने होटल में उसका यौन उत्पीडऩ किया था। बंगाल पुलिस के मुताबिक बंग भवन में राज्यपाल के ठहरने, निकलने, और होटल में आने, वहां से जाने का सीसीटीवी फुटेज देख लिया गया है, और पहली नजर में इस महिला की शिकायत पुलिस ने सही पाई है।
अब भारत में किसी भी व्यक्ति को ऐसी संवैधानिक सुरक्षा मिलना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है जो कि उसके काम से जुड़ी हुई नहीं है। यही शिकायत अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी या आम नागरिक के खिलाफ होती, तो उन्हें तो कोई हिफाजत नहीं मिल सकती थी। ऐसे में आम और खास के बीच यौन शोषण जैसे आरोप, या मध्यप्रदेश में एक वक्त राज्यपाल रहते हुए रामनरेश यादव के व्यापमं घोटाले में शामिल होने के आरोप सामने आए थे, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद पुलिस कोई कार्रवाई पाती, उसके पहले ही वे गुजर गए, और कई किस्म की कानूनी परेशानियों से बच भी गए। अब ऐसे मामलों में किसी को कानूनी कार्रवाई से हिफाजत देना पूरी तरह अलोकतांत्रिक और नाजायज है। 2015 में जब यह मामला सामने आया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई थी जिसमें एमपी के गवर्नर को हटाने की मांग की गई थी, और उस वक्त अदालत ने केन्द्र सरकार से इस पर जवाब भी मांगा था। उस वक्त की खबर बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने रामनरेश यादव को भी नोटिस जारी किया था जो कि अपने किस्म का एक असाधारण मामला था।
लोकतंत्र में जनता के ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोगों को इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी शर्मिंदगी और कानूनी कार्रवाई झेलने के बजाय, ऐसे आरोप लगने पर वे कम से कम राजभवन की हिफाजत को छोडक़र घर तो चले जाएं। लेकिन ऐसे लोग इस दहशत में रहते होंगे कि राजभवन छोड़ते ही उन पर कार्रवाई हो सकती है, और इसीलिए वे कुर्सी से अधिक से अधिक वक्त तक चिपके रहना चाहते होंगे। और रिटायर होने के पहले ही गुजर जाने वाले राज्यपाल की तरह बाकी लोग भी उम्मीद करते होंगे कि हो सकता है कि रिटायरमेंट आने के पहले मौत ही आ जाए, तो किसी कार्रवाई का कोई टंटा ही नहीं रहेगा। और इस देश में तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने एक बेमिसाल मिसाल छोड़ी है कि बंगले के दफ्तर में मातहत कर्मचारी के यौन शोषण का आरोप लगने पर वे खुद ही इसकी सुनवाई के लिए बनी बेंच के मुखिया बनकर बैठ गए थे। इससे अधिक शर्मनाक कोई मिसाल देश के इतिहास में आज तक नहीं हुई है, और हमने यह बेंच बनने के दिन से ही इसे शर्मनाक करार देना शुरू किया था, यह एक अलग बात है कि साल-दो साल बाद जब रंजन गोगोई की किताब प्रकाशित हुई थी तो उन्होंने इस बेंच में खुद के बैठने को गलत फैसला माना था, तब तक हम दर्जन भर बार से अधिक अपने संपादकीय और कॉलम में इसे धिक्कार चुके थे।
हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के हर राज्यपाल के साथ वहां चलने वाले स्थाई टकराव को अनदेखा करना नहीं चाहते। लेकिन अगर एक के बाद एक महिलाएं राज्यपाल पर यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, तो हम इनके पीछे कोई राजनीति मानने से इंकार करते हैं, और उन महिलाओं का जांच और कार्रवाई का हक राजनीति से ऊपर मानते हैं। ऐसे में देश के संविधान में यह फेरबदल करना चाहिए कि निजी आचरण, भ्रष्टाचार, यौन शोषण जैसी शिकायतों पर किसी राज्यपाल, राष्ट्रपति, या जज, देश में किसी को भी कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। लोकतंत्र जरा भी सभ्य होता तो बंगाल सरीखे राज्यपाल इस्तीफा देते, और फिर चाहे अपनी मोटी पेंशन से थाईलैंड आते-जाते रहते। लेकिन कुकर्मों को संवैधानिक हिफाजत देना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है, और हमारा ख्याल है कि एक व्यापक मुद्दा बनाकर अगर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई जाएगी, तो उसकी सुनवाई की संभावना बनती है। देश में किसी वकील को, या जागरूक नागरिक को यह पहल करनी चाहिए। और क्या होगा, अधिक से अधिक सुप्रीम कोर्ट पिटीशन को खारिज करके लाख-पचास हजार रूपए जुर्माना लगा देगा, उसके लिए भी जनता के बीच से क्राउड फंडिंग से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
आज से करीब 11 बरस पहले केदारनाथ में विनाशकारी बाढ़ आई थी जिसमें पहाडिय़ों के कई हिस्से धसक गए थे, चट्टानें दूर-दूर तक बह गई थीं, बड़ा भूस्खलन हुआ था, और हजारों लोग मारे गए थे। कुदरत की वह मार जून के महीने में हुई थी जिसकी बरसी को आज ठीक एक महीना बाकी है। ऐसे में आज उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा को देखें, तो ऐसा लगता है कि सरकारों और लोगों ने कोई सबक नहीं लिया है। चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन किए जाते हैं। आज सुबह तक की खबर बताती है कि सैकड़ों बरस से चली आ रही इस यात्रा में इतने अधिक लोग पहुंच चुके हैं कि 45 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, और लोग 25-25 घंटे बाद आगे बढ़ पा रहे हैं। यह भी खबर है कि दर्जनभर लोग दर्शन के इंतजार में सडक़ पर लगे जाम में ही गुजर चुके हैं। इस पहाड़ी रास्ते की जैसी तस्वीर पिछले दो-चार दिनों से दिख रही है, और वीडियो तैर रहे हैं वे भयानक हैं, और एक खतरनाक नौबत दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वहां रिकॉर्ड संख्या में लोग पहुंचे हैं, और पहाड़ की सडक़ क्षमता भी जवाब दे चुकी है। नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा ने इस बार इतने श्रद्धालुओं को खींचा है कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि जहां ऐसा भयानक ट्रैफिक जाम है, जहां दसियों हजार दर्शनार्थी फंसे हुए हैं, वहां पर अगर किसी भी तरह की विपदा आती है, तो क्या होगा? क्या किसी भी तरह का इंतजाम इससे निपट सकेगा? जहां दसियों हजार गाडिय़ां एक-दूसरे से सटी खड़ी हैं, वहां पर अगर एक दुर्घटना हुई, तो क्या होगा?
दुनिया भर के तीर्थों का कुछ ऐसा ही हाल रहता है क्योंकि वहां की धार्मिक मान्यताएं त्यौहारों और महूरतों से जुड़ी रहती हैं, और समय-समय पर सीमित जगह पर पहुंचने वाले अपार श्रद्धालु कई तरह के हादसों के शिकार होते हैं। अभी 2015 में ही सऊदी अरब के मक्का में हज करने गए हुए तीर्थयात्रियों के बीच भगदड़ हुई, और उसमें कुचलकर दो हजार से अधिक लोग मारे गए थे। हज यात्रा सऊदी अरब की बड़ी सख्त सरकार के फौलादी नियंत्रण में होती है जिसके लिए दुनिया के अलग-अलग देशों से आने वाले लोगों का सालाना कोटा तय किया जाता है ताकि भीड़ अधिक न बढ़े। इसके बावजूद वहां भगदड़ में बड़ी संख्या में मौतों का लंबा इतिहास है। 1990 में करीब 15 सौ लोग मारे गए थे, 2006 में साढ़े 3 सौ, और 2015 में 22 सौ से अधिक। वहां पर अग्नि दुर्घटनाओं में भी 1975 में 2 सौ लोग, 1997 में साढ़े 3 सौ लोग मारे गए।
भारत के केदारनाथ में 2013 में आई बाढ़ में 6 हजार लोगों के मरने की खबर है, और बहुत से ऐसे लोग गायब हैं जिनके घर-बार के लोग भी नहीं हैं जो उनके गायब होने की रिपोर्ट कर सकें। अब सवाल यह उठता है कि इस ताजा-ताजा हादसे के बाद आज 11 बरस में ही अगर उसके सारे बुरे तजुर्बे को भुला दिया गया है, और इतना बड़ा खतरा खड़ा किया गया है, तो इसके लिए उत्तराखंड की राज्य सरकार के अलावा किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? जैसा कि किसी भी पहाड़ी राज्य में होता है, वहां दाखिले की तमाम सडक़ें सरकार के अच्छे काबू में रहती हैं, और सरकार की मर्जी के बिना, उसकी इजाजत के बिना कोई गाड़ी आगे तो बढ़ नहीं सकती। अब यह बात हमारी सबसे बुरी कल्पना से भी परे है कि ऐसे नाजुक पहाड़ी इलाके में, प्राकृतिक विपदा के खतरों को अनदेखा करते हुए 45 किलोमीटर लंबा जाम लगने दिया गया है। आज की यह नौबत सबसे पहले तो यह सुझाती है कि तीर्थयात्रा के इस रास्ते पर दाखिले को पूरी तरह रोक दिया जाए, और जब तक पहाड़ पर चढ़ी हुई गाडिय़ां लौटकर न आ जाएं, जब तक आवाजाही की सौ फीसदी सुरक्षित योजना न बना ली जाए, तब तक सब कुछ रोक दिया जाए, सिर्फ लोगों को दर्शन के बाद, या कि जैसा हजारों लोग कर रहे हैं, दर्शन के बिना भी वापिस आने दिया जाए। ऐसे दर्शन भी भला किस काम के जिनमें बदइंतजामी के चलते सडक़ों पर लोग मर जाएं, और 24-24 घंटे गाडिय़ां हिल न सकें, लोगों को खाना-पानी न मिल सके। आज 21वीं सदी में कम्प्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, उपग्रह से बने नक्शे और पिछले बरसों के आंकड़े लेकर बैठे अफसर अगर ऐसी स्थिति का अंदाज नहीं लगा सके, और उन्होंने यह भयानक बड़ा खतरा खड़ा कर दिया, तो यह नौबत टलते ही कुछ बड़े अफसरों को हटाना भी चाहिए।
भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट सरकारों के नियमित कामकाज में दखल देने से बचते हैं। लेकिन यह नौबत तो दसियों हजार जिंदगियों पर एक खतरे की तरह है, और किसी अदालत को खुद होकर नाजुक पहाड़ पर गाडिय़ों के ऐसे जनसैलाब को रोकना चाहिए, जिसमें किसी हादसे या मुसीबत की नौबत आने पर फौज भी कुछ नहीं कर सकेगी। धर्म ही नहीं, किसी भी तरह के आयोजन में ऐसी खतरनाक गिनती वाली भीड़ सरकारी जुर्म से कम नहीं है। आज धरती पर जगह-जगह मौसम की बुरी मार और बहुत अधिक बुरी होती जा रही है, और वह बार-बार पड़ रही है। नवंबर तक चलने वाली इस चारधाम यात्रा में अगर ऐसी भीड़ पर कोई बादल फटा, 11 बरस पहले जैसी कोई बाढ़ आई, तो क्या होगा? उसके लिए कुदरत, ईश्वर, सरकार, या श्रद्धालुओं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? कोई राज्य अपने किसी इलाके में एक वक्त में कितनी गाडिय़ों को इजाजत दे, यह तो बड़ी आसानी से काबू करने लायक बात है। प्रदेश में आने वाली सडक़ें किसी गांव के मेले की तरह चारों तरफ से खुली तो नहीं रहती हैं कि आज उत्तराखंड का प्रशासन कह रहा है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में आ गए। अभी गनीमत यही माननी चाहिए कि इनमें से किसी गाड़ी में आग नहीं लगी, कोई भगदड़ नहीं हुई, लोगों में झगड़ा नहीं हुआ, और अब तक सब कुछ चैन से चल रहा है। लेकिन यह सरकारी इंतजाम की वजह से चल रहा है कहना गलत होगा, यह सरकारी बदइंतजामी के बावजूद अनायास ठीक चल रहा है, यह कहना बेहतर होगा।
उत्तराखंड के पहाड़ों को लेकर बार-बार यह बात होती है कि यहां न तो पनबिजलीघर बनाना सही है, न किसी तरह के बांध बनाना, और न ही सुरंगें, पुल, और इतनी सडक़ें बनाना ठीक है। विशेषज्ञ और जानकार लगातार आगाह करते हैं कि पहाड़ इतने ढांचे, और इतने पर्यटकों का बोझ ढोने लायक नहीं हैं। लेकिन इंसान हैं कि इन पहाड़ों में चारों तरफ से छेद किए जा रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, फौलादी ढांचों के बोझ से पहाड़ों की कमर तोड़ रहे हैं, और मलबे की गाद से नदियों को पाट रहे हैं जिनसे उनमें बाढ़ आ रही है। पहाड़ी राज्य अपनी सैलानी-अर्थव्यवस्था की जरूरत को गिनाते हुए पहाड़ों का किसी मैदानी इलाकों की तरह दोहन करने में लगे हुए हैं। यह सिलसिला लंबे समय तक नहीं चलेगा। कुदरत की मार दुनिया में जगह-जगह ऐसी जगहों पर हो रही है जिन्हें बड़ा महफूज माना जाता था। और यह केदारनाथ तो अभी-अभी लाशों के ढेर का गवाह बना हुआ है। हमारा ख्याल है कि चाहे यह राज्य सरकार के स्तर के फैसले हों, जिनमें केन्द्र की भी कोई मामूली इजाजतें लगती हों, लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ताकि उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए गैरकारोबारी विशेषज्ञों की एक कमेटी बनवाई जा सके जो कि पहाड़ की सीमाओं को तय कर सके कि वहां कितने और लोग झेले जा सकते हैं। इसके बिना किसी वक्त और बड़ा हादसा होगा, पिछली बार तो 6 हजार लोग मारे गए थे, आज की तरह अगर वहां पर 25-50 हजार लोगों की मौजूदगी में कोई हादसा होगा तो उसकी जिम्मेदारी राज्य और केन्द्र सरकार पर होगी, और शायद सुप्रीम कोर्ट पर भी।
छत्तीसगढ़ में सरकार ने शराब दुकानों के साथ ग्राहकों के पीने के लिए अहाते खोलना तय किया है, और उसकी नीलामी से बहुत बड़ी रकम सरकार को मिल गई है। मध्यप्रदेश के वक्त से शराब का कारोबार जरूरत से अधिक नियमों से बांधा हुआ है, और ये नियम गलत काम को रोकने के लिए नहीं रहते, किसी धंधे को बंद करवाने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं, और इन्हीं के दम पर शराब-कारोबार के हर पहलू से मनमानी उगाही होती है। शराब कारखानों से शुरू होकर, शराबखानों और दुकानों तक, ट्रांसपोर्ट और गोदाम तक, हर जगह इतने गैरजरूरी और बारीक नियम लाद दिए गए हैं कि एक मामूली सा अफसर भी नाराज होकर धंधे को बंद करवा सकता है, धंधा बंद तो होता नहीं, उससे हफ्ता तय हो जाता है। ऐसे में मध्यप्रदेश की तज पर छत्तीसगढ़ शराब-कारोबार को अतिनियंत्रित करता है, और इसी अनुपात में सरकारी भ्रष्टाचार भी बढ़ता है।
अब जाकर व्यवस्थित रूप से शराब दुकानों के पास अहाते खोले जा रहे हैं जहां बैठकर लोग शराब पी सकेंगे, और इसे चलाने वाले कारोबारी वहां खाने-पीने का सामान बेच सकेंगे, गिलास वगैरह बेचेंगे, और मिलने वाली खाली बोतलों से भी कुछ कमाई करेंगे। लेकिन कुछ कारोबारियों की छोटी या बड़ी कमाई से परे यह एक बड़ी जरूरत इसलिए है कि जो गरीब या मध्यमवर्गीय लोग शराब खरीदते हैं, उनके घर तो इतने बड़े रहते नहीं कि वे वहां बैठकर पी सकें, फिर लोग अपने परिवार के सामने बैठकर पीना चाहते भी नहीं हैं। ऐसे में आज हर दुकान के इलाके में हजारों लोग किसी न किसी सार्वजनिक जगह पर बैठकर शराब पीते हैं, और पुलिस कार्रवाई की लिस्ट देखें तो उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई से भरा रहता है। जो लोग पुलिस का कामकाज जानते हैं वे इस बात को समझ सकते हैं कि जितने लोग पकड़ाते हैं उससे दर्जनों या सैकड़ों गुना अधिक लोग ले-देकर छूट जाते होंगे। हमारा खुद का देखा हुआ है कि हर तालाब और मैदान के आसपास, हर बगीचे के भीतर-बाहर, किसी सडक़ के सुनसान हिस्से में, या किसी भी चारदीवारी के पीछे बैठकर लोग शराब पीते हैं, और किसी शहर की पुलिस के बस का यह नहीं होता कि वह इतने शराबियों को पकड़ सके। एक शराबी को पकडऩे का मतलब उसकी मेडिकल जांच से लेकर कागजी कार्रवाई तक कई घंटे का सिलसिला रहता है, और अगर पुलिस यही करती रहे, तो और कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए एक सामाजिक जरूरत की तरह लोगों को शराब पीने की एक जगह मुहैया कराना जरूरी है, और छत्तीसगढ़ में सरकार ने यह ठीक काम किया है। शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन यह एक किस्म की अनिवार्य बुराई है, जब तक इस नशे का कोई बेहतर और अधिक सुरक्षित विकल्प अमल में नहीं लाया जा सकता, इस पर रोक लगाने का कोई अच्छा जरिया नहीं दिखता है। गुजरात और बिहार का तजुर्बा यह है कि शराब की तस्करी में वहां का सरकारी अमला पूरे का पूरा भ्रष्ट हो गया है, और शराब वहां धड़ल्ले से खुलेआम मिलती है। इसलिए जब तक लोगों के बीच यह अनिवार्य बुराई कानूनी दर्जा प्राप्त है, तब तक इसे गैरजरूरी नियमों से लादकर और अधिक भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। अहाते खुलने से सार्वजनिक जगहों पर गैरशराबियों को कुछ राहत मिल सकेगी, और सरकार को भारी-भरकम टैक्स देकर दारू खरीदने वालों को चैन से बैठकर पीना नसीब हो सकेगा।
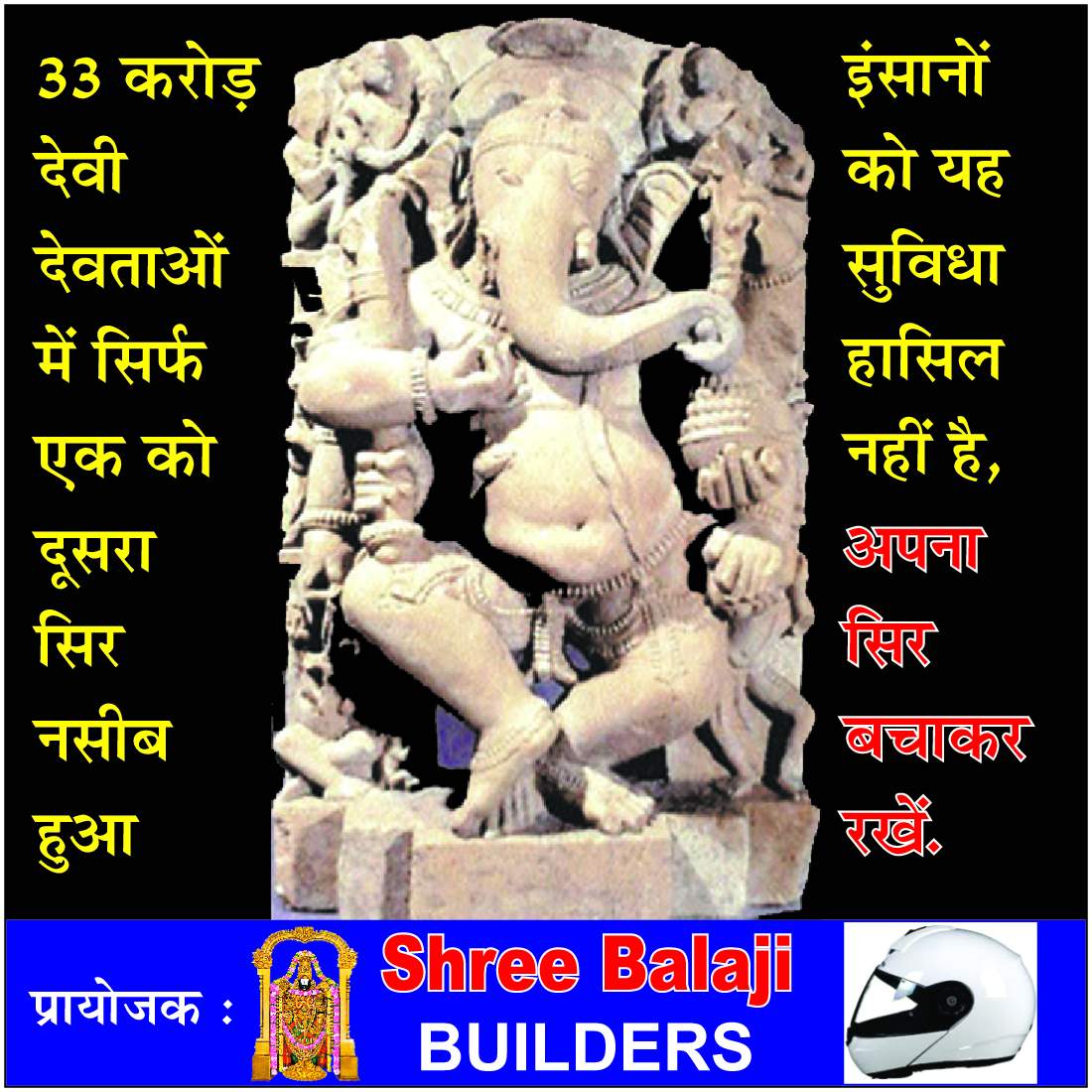










.jpg)



















