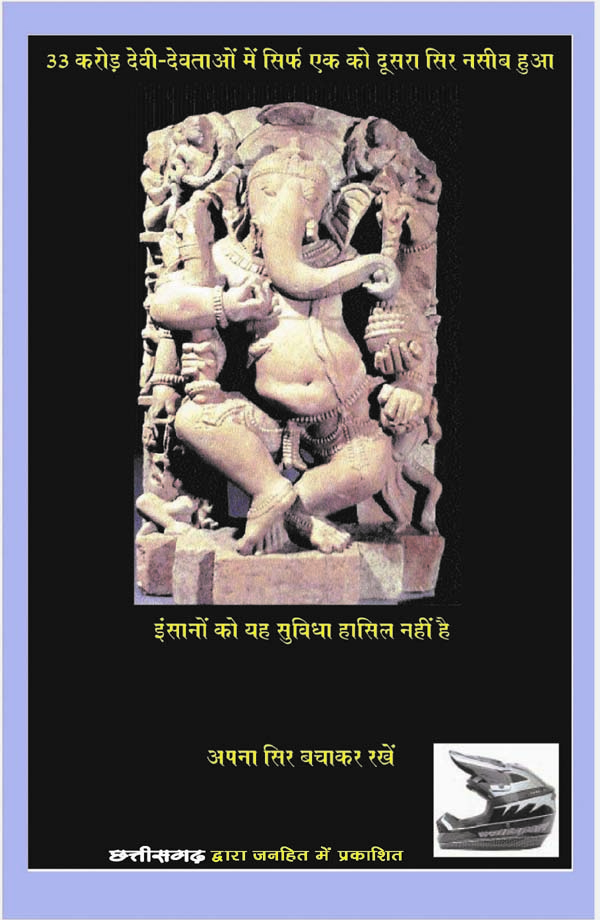संपादकीय

हिन्दुस्तान में कभी देश की सरकार तो कभी किसी प्रदेश की सरकार को लेकर राजनीतिक स्थिरता पर बातचीत होती है। पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान की सबसे लंबी वाममोर्चा सरकार तीन दशक से अधिक तक लगातार चली थी। अभी हाल तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की डॉ. रमन सिंह सरकार पन्द्रह बरस चली थी, और कुछ दूसरे राज्यों में किसी एक पार्टी या एक मुख्यमंत्री की सरकार इससे भी अधिक समय तक चली हैं। सरकार की लंबाई एक बात होती है, और सरकार का संसदीय बाहुबल एक दूसरी बात होती है। इस देश में कुछ पार्टियों का संसदीय बाहुबल देश या प्रदेश की सरकारों को चलाने के लिए जरूरत से खासा अधिक था, और वैसे में संसदीय कामकाज पर इस अतिरिक्त बाहुबल का कैसा असर पड़ता है, यह सोचने की बात है।
जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की सहानुभूति लहर के चलते उन्हें कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा संसदीय बाहुबल मिला था। वह सरकार विशुद्ध कांग्रेस की सरकार थी, किसी साथी दल की कोई जरूरत नहीं थी, और उसी का नतीजा था कि शाहबानो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए राजीव सरकार ने एक संविधान संशोधन किया था जो कि मुस्लिम कट्टरपंथी मर्दों को तो खुश करने वाला था, लेकिन जिसने मुस्लिम महिला के हक पर लात मारी थी। उस वक्त तो फिर भी संसद में इस मुद्दे पर खासी बहस हो गई थी, और अलग-अलग पार्टियों और विचारधाराओं को बोलने का मौका मिला था। लेकिन अभी की मोदी सरकार में जब तीन कृषि कानून बनाए गए, तो उन पर कोई सार्थक चर्चा नहीं होने दी गई, और एनडीए सरकार के भीतर भी भाजपा ने महज अपने ही बाहुबल से इन विधेयकों को कानून बनवा दिया, और इस मुद्दे पर गठबंधन छोडऩे वाले अपने एक सबसे पुराने साथी, अकाली दल के अलग होने से भी भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि गठबंधन सरकार के भीतर भी भाजपा अकेली ही सरकार बनाने की गिनती रखती थी।
समय-समय पर देश की संसद ने, और कभी-कभी राज्यों की विधानसभाओं ने भी ऐसे मौके दर्ज किए हैं जब व्यापक जनहित और महत्व वाले विधेयकों को बिना जरूरी चर्चा के बाहुबल के ध्वनिमत से पारित करा दिया गया। लोकतंत्र में संसद को बनाया इसलिए गया है कि वहां पर सरकार से सवाल पूछे जा सकें, देश-प्रदेश के हालात पर जानकारी मांगी जा सके, सरकार को जहां अपने बजट को सामने रखकर लोगों को सरकारी खर्च की योजना बताई जा सके, और कमाई के तरीके गिनाए जा सकें। इसके अलावा जब कभी कोई नए विधेयक आते हैं, संविधान संशोधन की जरूरत रहती है, तो अलग-अलग प्रदेशों, अलग-अलग पृष्ठभूमि, अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा से आए हुए सांसदों की बात को सुना और समझा जा सके, तब उसके बाद कोई नया कानून बनाया जाए, या पुराने को बदला जाए। देश भर से आए हुए सैकड़ों सांसदों की राय सुनना संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियाद है, और इस बुनियाद के बिना जब कोई इमारत खड़ी की जाती है, तो एक आंदोलन की आंधी से वह उसी तरह गिर सकती है जिस तरह कृषि कानून औंधे मुंह गिरे।
संसदीय बाहुबल की अधिकता का एक बड़ा खतरा यह रहता है कि सत्तारूढ़ पार्टी किसी संसदीय फैसले के लिए किसी भी असहमति को सुनने को मजबूर नहीं रहती, उसे किसी को सहमत कराने की जरूरत नहीं रहती, और वह संसद के भीतर ठीक उसी तरह कोई कानून बना या बिगाड़ सकती है जिस तरह वह अपनी पार्टी की बैठक के भीतर कोई मनमाना फैसला ले सकती है। यह सिलसिला बहुत तानाशाह और खतरनाक तो है ही, इससे संसदीय व्यवस्था का एक सीधा-सीधा नुकसान भी होता है। जिन लोगों ने राजनीति और सामाजिक जीवन में दशकों गुजार दिए हैं, ऐसे लोगों से संसद भरी रहती है। ये लोग हर दिन सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, और अलग-अलग मुद्दों पर जनता की राय से वाकिफ रहते हैं। वैसे तो भारत के मौजूदा संसदीय कानून के मुताबिक सभी सांसद या विधायक अपनी पार्टी के फैसलों से बंधे रहते हैं, और उन्हें किसी भी मुद्दे पर अपनी पार्टी के हुक्म के मुताबिक ही वोट डालना होता है, वरना उनकी सदस्यता खतरे में रहती है। लेकिन ऐसी सीमाओं के भीतर भी सांसदों की निजी सोच, उनके निजी तजुर्बे बहस में सामने आते हैं, और एक-एक सांसद बीस-तीस लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके मार्फत उनके इलाकों के लोगों की सोच संसद के रिकॉर्ड में आने की एक संभावना तो रहती ही है।
सदन में पार्टी व्हिप से बंधे सांसदों का एक नुकसान देश के संसदीय लोकतंत्र को यह होता है कि वे पार्टी की घोषित सोच से परे शायद ही कुछ बोल पाते हैं। ऐसे में देश की जनता के बीच से चुनाव की अग्निपरीक्षा से होते हुए जो सांसद संसद में पहुंचते हैं, वे अपनी मौलिक बातें वहां बहुत कम कर पाते हैं। उन्हें पार्टी की तरफ से पहले से बता दिया जाता है कि किस मुद्दे पर क्या कहना है। इस तरह देश के सबसे चुनिंदा दिल-दिमागों का मौलिक योगदान संसद और लोकतंत्र को बहुत कम मिल पाता है। पार्टी अनुशासन के नाम पर भारतीय संसदीय व्यवस्था में सांसदों को इस तरह बांध दिया जाता है कि लोकतंत्र में विचारों की जो विविधता होनी चाहिए, वह महज पार्टियों की विविधता तक सीमित रह जाती है। एक तो निजी सोच का खुलकर सामने आना बहुत कम रह गया है, और फिर पार्टियों के बीच किसी मुद्दे पर बहस भी गैरजरूरी मान ली गई है क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी बिना बहस भी किसी विधेयक को पास कराने का बाहुबल रखती है।
भारत के ताजा इतिहास के जानकार लोगों को यह सोचना चाहिए कि क्या अपने भीतर जरूरत से अधिक कड़े अनुशासन वाली पार्टी संसदीय विचार-विमर्श में कम योगदान देने वाली पार्टी भी हो जाती है? दूसरी बात यह कि क्या किसी पार्टी या गठबंधन की जरूरत से अधिक मजबूती पूरी संसद में ही किसी विचार-विमर्श को हाशिए पर धकेल देती है? और चूंकि हिन्दुस्तान ऐसे एक से अधिक दौर देख चुका है जहां सांसदों या पार्टियों की बातों को अनसुना करना किसी दिक्कत की बात नहीं रह गई है, इसलिए ऐसे तरीकों के बारे में सोचना चाहिए कि सांसदों की निजी सोच को देश की बहस की मेज पर किस तरह लाया जा सकता है? पार्टियां इस बात को शायद ही पसंद करें, क्योंकि वे सदन के भीतर अपने सदस्यों को निर्वाचित जनप्रतिनिधि की तरह देखना नहीं चाहतीं, बल्कि पार्टी के एक अनुशासित सिपाही की तरह देखना चाहती हैं। इस तरह जनता के प्रति सांसद की जवाबदेही खत्म हो जाती है, और वह पार्टी के प्रति सौ फीसदी अनुशासन की नौबत बन जाती है। ऐसे में क्या संसद के बाहर एक समानांतर बहस के बारे में सोचा जा सकता है? या फिर पार्टियों का अनुशासन ऐसी भी किसी बात को होने नहीं देगा? लोकतंत्र के भीतर हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर सोच की विविधता वाली बहस का जो महत्व होना चाहिए, वह किसी गठबंधन की सरकार में विपक्ष के वोटों की जरूरत के बीच तो कायम रह सकता है, लेकिन अंधाधुंध गैरजरूरी बाहुबल रहने पर उसकी संभावना शून्य हो जाती है। भारतीय लोकतंत्र इसका क्या रास्ता निकाल सकता है?
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)